वीरेंद्र जैन के उपन्यासों में पारिस्थितिकी चिंतन
- 1 February, 2015
शेयर करे close
शेयर करे close
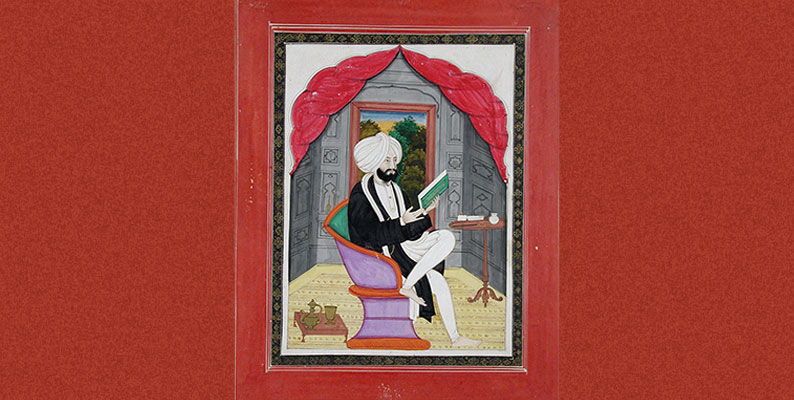
शेयर करे close
- 1 February, 2015
वीरेंद्र जैन के उपन्यासों में पारिस्थितिकी चिंतन
माधव गाड्गिल कमिटी रपट को केंद्र हरित टैब्यूनल ने नकार दिया। कुछ महीनों तक माधव गाड्गिल कमिटी रपट और कस्तूरी रंगन कमिटी रपट का बोलबाला था। पारिस्थितिकी से संबंधित अब तक आये रपटों में ये दो ही सबसे चर्चित एवं विवादास्पद हैं। जहाँ गाड्गिल कमिटी रपट अपनी सरलता, गहनता और प्रासंगिकता के कारण अब तक भारत में आये पारिस्थितिकी रपटों में सबसे महत्त्वपूर्ण है, वहाँ कस्तूरी रंगन कमिटी रपट थोड़ा गौण है। गाँधी जी की विकास नीति–ग्रामस्वराज का आधुनिक रूप गाड्गिल कमिटी रपट में हम देख सकते हैं। लेकिन यहाँ चर्चा का विषय यह है कि ये रपटें किस प्रकार राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक विवादों के कारण बन गए, कुछ लोगों ने क्यों इसके खिलाफ आवाज उठाई; राजनीतिक एवं धर्मिक लोग क्यों इन रपटों से डरते हैं? इन विवादों के संदर्भ में वीरेंद्र जैन के ‘डूब’ और ‘पार’ उपन्यास और उनके द्वारा हमारे सामने रखने वाले विकास की राजनीति पर एक बहस अनुचित नहीं होगा। विकास की अवांछित नीति ने भारत के पर्यावरण को बरबाद कर डाला। अनियंत्रित प्राकृतिक शोषण किस प्रकार मानव और प्रकृति के लिए घातक है इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है उत्तराखंड की बाढ़। इस संदर्भ में इन उपन्यासों के माध्यम से स्वातंत्र्योत्तर भारत के ऐतिहासिक, समाजशास्त्रीय, सांस्कृतिक, राजनीतिक और अर्थशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में विकास नीतियों को देखना अनिवार्य बन जाता है। वीरेंद्र जैन के ‘डूब’ और ‘पार’ उपन्यास, औद्योगिकरण की वजह से समाज और संस्कृति में हुए परिवर्तन और उससे उभरी समस्याओं को पेश करते हैं।
आज के संदर्भ में विकास का मतलब एक देश की स्वतःअर्जित करने वाली आर्थिक स्थिति में है। स्वातंत्र्योत्तर भारत के विकास का इतिहास पंचवर्षीय योजनाओं से ही शुरू होता है। भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है खेती। इसलिए देश की विकास नीति खेती को लक्ष्य बनाकर तैयार की गयी, जिसका परिणाम थी हरित क्रांति। अनुबंध रूप से अनेक बाँधों और नहरों का निर्माण होने लगा। अधिक से अधिक इलाकों में खेती, उच्चतम ऊर्जा उत्पादन आदि को लक्ष्य बनाकर बड़े-बड़े बाँधों का निर्माण होने लगा। भारत के भाखड़ा नांगल, हीराकुंड, सरदार सरोवर, टिहरी आदि इसके उदाहरण हैं।
1950 के आसपास से ही विश्व की बड़ी-बड़ी आर्थिक शक्तियाँ विकास पद्धतियों के प्रचार की कोशिश में लगी रहीं। एशिया, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका आदि भूखंडों के कोलनीकृत प्रदेशों और भारत को भी उन्होंने अपना लक्ष्य बनाया। इससे मिलने वाली धनराशि को लक्ष्य बनाकर बड़े-बड़े बाँधों का निर्माण करने लगे। स्वातंत्र्योत्तर भारत के शासकों ने भी सिंचाई के एक अच्छे उपाय के रूप में बाँध निर्माण को मान लिया। ‘डूब’ और ‘पार’ नेहरू की विकास नीति का खुलासा है। नेहरू के लिए बाँध ‘आधुनिक भारत का मंदिर’ है। बेतवा नदी के बहाव को रोककर राजघाट बाँध का निर्माण किया जाता है। मगर इससे लड़ाई और उसके जैसे अनेक गाँवों के डूब जाने की संभावना थी। वर्षों पुरानी संस्कृति भी इसके साथ डूब जाएगी। ये उपन्यास मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश की सीमाओं से बहती बेतवा नदी की, उसमें बनने वाले राजघाट बाँध की और वहाँ की जनता की त्रासदी की कहानी है। सिंचाई, ऊर्जा उत्पादन और बाढ़ पर नियंत्रण आदि के लिए बाँधों का निर्माण किया जाता है। ये उपन्यास इस परंपरागत ज्ञान को तोड़कर बाँध निर्माण की पारिस्थितिकी पर बल देते हुए एक प्रतिरोधी मानसिकता पाठकों के सामने रख देते हैं।
हर एक विकास योजना अपने साथ अनेक समस्याओं को समाज के सामने खड़ी करती है। स्थानीय लोगों का विस्थापन इसकी मुख्य समस्या है। विकास योजनाओं की बात उठाते समय सबसे पहले उभरनेवाला सवाल पुनर्वास का है। इसमें कोई संदेह नहीं कि बाँध जैसी विशालकाय निर्मिति का प्रभाव भी बड़ा ही होगा। बाँध निर्माण अधिकतर पहाड़ी या वन प्रदेशों में होने के कारण उसका प्रभाव सीधे आदिवासियों और पहाड़ी लोगों पर पड़ता है। यह एक अहम मुद्दा है, क्योंकि आदिवासियों की जिंदगी वनों और नदियों से जुड़ी हुई है। इसलिए उस क्षेत्र में होने वाली हर एक निर्मिति का दुष्परिणाम सबसे पहले उन्हीं को भुगतना पड़ता है। वन, पहाड़ और नदी से अलग होने से उनकी स्वाभाविक जिंदगी बरबाद हो जाती है। भारतीय संदर्भ में विस्थापितों को दिये जाने वाले मुआवजे कभी भी उनकी आजीविका की पैतृक संपत्ति के विकल्प नहीं होते हैं। इसलिए पुनर्वास की योजनाओं के बारे में सोचते समय इस बात पर ध्यान रखना आवश्यक है कि उन्हें, पहले के समान अपनी संस्कृति के साथ जीना है। ‘पार’ की दुनिया कहती है कि ‘तब हम कंद-मूल, फल-फूल, जड़ी-बूटी, जलावन-छाजन कहाँ से पाएँगे? हमरी तो डाग ही आसरा है।’ यह सवाल वास्तव में उनके अस्तित्व का है।
लड़ैई और जीरोन अनेक प्रकार के अभावों से भरे भारतीय गाँव हैं। इसलिए एक दिन राजघाट बाँध की परियोजना का ऐलान हुआ तो उन इलाकों के लोगों में रोजगार की एक नयी आशा स्वाभाविक है। पर असल में लड़ैई गाँव को क्या मिला? रोजगार तो दूर की बात है, वहाँ के लोगों को अपनी जमीन से ही हाथ धोना पड़ा। केवल बाहर के लोगों को ही नौकरी दी गयी थी। दु:ख की बात यह है कि लड़ैई के ही नहीं बल्कि आसपास के गाँव वालों को भी नौकरी नहीं मिली। ‘डूब’ उपन्यास में इसका उल्लेख मिलता है ‘क्योंकि काम तेजी से करना है। यहाँ के स्थानीय आदमी मन लगाकर पूरे समय काम नहीं करेंगे। क्योंकि वे अपने तीज-त्योहार मनाना नहीं छोड़ेंगे काम के खातिर। घर परिवार के शादी ब्याह में शामिल होना भी न त्यागेंगे। कोई बीमार दुखी हुआ तो उसकी तीमारदारी में जुटना भी नहीं छोड़ेंगे। सरकार बाबू से कि ठेकेदार के मुँह से कोई ऊँच-नीच बात निकल गई तो उनसे झगड़ने से बाज भी न आयेंगे।’ यह औद्योगिकरण के साथ उभरी समस्या थी। यहाँ सरकार और ठेकेदारों को काम करने वाली मशीनें ही चाहिए मनुष्य के रूप में। उन्हें सामाजिक मनुष्य की जरूरत नहीं है। यहाँ मनुष्य और उसके स्वातंत्र्य का कोई स्थान नहीं है। मात्र लाभ ही है इन विकास योजनाओं के पीछे का यथार्थ।
‘पार’ में उपन्यासकार ने इस साजिश को व्यक्त किया है। बाहर से आये लोगों का शोषण आसानी से किया जाता है। उन लोगों के लिए एक अलग बस्ती बनाई जाती है। बाहर से आये हुए लोगों के पास हर चीज की कमी होती है। उन लोगों को हर काम, नये सिरे से ही शुरू करना होता है। इन लोगों को लक्ष्य करके ठेकेदार और साहूकार लोग आसपास ही बसते हैं। स्थानीय लोग हैं तो आसानी से इकट्ठे हो जाते हैं। अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाते हैं। ‘पार’ के अरविंद, राम दुलारे से कहते हैं कि ‘बसे-बसाए गाँव में श्रमिक संगठित होते हैं। उनका मनचाहा उपयोग या शोषण संभव नहीं होता। इसीलिए ऐसे श्रमिकों को काम पर नहीं रखते ठेकेदार। इसीलिए बाहर से मजदूर लाते हैं। यह केवल यहीं की नहीं, हिंदुस्तान भर में यही चलन है।’ आजकल की बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ इन श्रमिक संगठनों से डरती हैं। वास्तव में श्रमिक संगठन उनकी आर्थिक शोषण नीति के खिलाफ है।
बाँध निर्माण के पीछे की पुरानी मान्यता बदल गयी है। आज उसके पीछे केवल आर्थिक लाभ मात्र है। बाँध निर्माण आज एक बड़ा व्यवसाय है। विश्व बैंक की सहायता से चलने वाला यह व्यवसाय भारत जैसे देशों को अपने एक सुरक्षित स्थान के रूप में मानता है। इस प्रकार राष्ट्र की संपत्ति बहुराष्ट्रीय कंपनियों की तिजोरियों में जाती है। भारत की राजनीति इसको सुस्थिर विकास की संज्ञा देती है। ‘डूब’ के मास्साव कहते हैं–‘कि अपने देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू देश को एक नयी शक्ल-सूरत देना चाहते हैं। हमारी पार्टी चाहती है कि पूरे देश में नये-नये उद्योग-धंधे लगे। नयी किस्म की तालीम दी जाए। अच्छे से अच्छे अस्पताल होंगे। अच्छे से अच्छे रहन-सहन हो सकता है। अच्छी आमदनी हो…इसलिए देश में भाखड़ा नांगल जैसे बड़े बाँध बनाने की योजना बनी, जिससे बिजली बन सके, कारखाना चल सके, शहर रोशन हो सके, तभी से मेरे मन में यह इच्छा पल रही है कि आपलोग के विकास के लिए भी ऐसी ही योजना मंजूर कारवाई जाए।’ ‘पार’ के घेरे साव बताता है कि ‘नदी को बाँधने के दिन तक तो जरूर एक न एक आपद विपद आती रहेगी, लेकिन नदी के बाँधते ही आफतों से अपना कंटक कट जाएगा। फिर तो खुशहाली आएगी। खेतों को भरपूर पानी मिलेगा, हर जिस्म को लत्त मिलेगा, बच्चों को शिक्षा ज्ञान, जवानों को रोजगार, बूढ़ों को उपकार। घर-घर में बिजली होगी।…उस बिजली से मशीनें चलती हैं। कारखानें चलते हैं। उनमें कपड़े बनते हैं। खिलौने बनते हैं। चीलगाड़ी बनती हैं। पंखा बनते हैं।’ इन दोनों उपन्यासों के माध्यम से यह सच्चाई हमारे सामने आती है कि विकास नीति एवं उसके लिए नारा लगानेवाले राजनीतिक लोगों की भाषा एक समान है। मतलब हर एक विकास नीति का लक्ष्य भी एक ही है ‘आर्थिक।’ यह समझकर ‘पार’ के अरविंद पांडे राम दुलारे को खत लिखते हैं कि ‘नेहरू के सपनों के भारत, इंदिरा के सपनों के भारत के बाद अपने गाँव को राजीव के सपनों का भारत न बनने देना चाहते हो तो तुम गाँव लौट आओ राम दुलारे।’ यह आह्वान वास्तव में पूरे देश के नवजवानों के लिए है।
इन धोखों के खिलाफ आवाज उठाना ‘देशद्रोह’ है। जनता के जीने के अधिकार के लिए करने वाली लड़ाई को सरकार के खिलाफ की लड़ाई के रूप में मानते हैं। ‘पार’ के राम दुलारे विरोध के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि उनको मालूम है कि उनको लड़ना है एक देश के प्रजातंत्रीय सरकार के खिलाफ, कानून व्यवस्था के खिलाफ; इस तरह विकास योजनाओं के खिलाफ आवाज उठाएँगे तो देशद्रोह घोषित किया जाएगा। बाँध से जो क्षति हो सकती थी, वह तो हो चुकी है। कभी-कभी हम भविष्य में घटनेवाली वारदात को जानकर भी कुछ नहीं कर पाते। शायद इसलिए नर्मदा बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ता चितपुकर यह सोच रखते हैं कि कुछ कर नहीं सके तो भी कम से कम नुकसान को कम करने के लिए कुछ कर ही सकते हैं।
विकास की योजनाओं के कारण विस्थापित होने वाले लोगों की मानसिकता दयनीय है। अपने ही देश में शरणर्थी बनना कितना भयानक है। सरकार की ओर से मिलने वाले मुआवजे से वे दो बैल भी नहीं खरीद सकते। ‘डूब’ के मातो की घोषणा इस सत्य का खुलासा है कि ‘क्षत्रीय से वैश्य हो गये सरकार’ अपनी सरकार के प्रति गहरा विश्वास, आत्मीयता, रखनेवाले 105 वर्षीय प्रज्ञा संपन्न किसान मातो अंततः इस सत्य को पहचानते हैं कि ‘लाबरी है जा सरकार, महा लाबरी। महा झूठी, सरासर झूठी।’ जनता को उचित मुआवजा भी नहीं मिलता है। सरकार का कहना है ‘बसने के लिए दो हजार रुपये हमसे लो जहाँ मिले वहाँ बसो। हमारे पास जगह नहीं है तुम्हें बसाने की। हाँ! चाहे तो दो हजार के बदले ललित पुरा में रेलवे पटरी के इस तरह बीस गज जमीन हम दे सकते हैं।’ मुआवजे की दर पाँचवें-छठे दशक में तय की गयी। पर दिया गया है आठवें-नवें दशक में। इस बीच जमीनों का दाम कई बार बढ़ गया है। योजनाओं के ऐलान होते ही उसके आसपास के सुरक्षित इलाकों में भूमि का दाम बढ़ जाता है। यहाँ के विस्थापितों को बसाने के लिए कहाँ से जमीन मिलेगी।
बाँधों से बनी बिजली और पानी से आम लोगों को कोई फायदा नहीं मिलता, बल्कि बड़े-बड़े खेत, बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ, बड़े-बड़े शहर एवं मॉलों को ही मिलता है। विकास के नाम पर हो रही इन योजनाओं का बुरा प्रभाव हमेशा आम जनता पर पड़ता है। ‘सरकार को बेतवा में मिलट्री कैंप कायम करता हुआ कि सागर की मिलट्री कैंप को विस्तार देता हुआ कि राजघाट बाँध, जामिनी घट बाँध, कि माता टीला बाँध, कि सड़के चौड़ी करती हुई, रेल पटरी बिछाती हुई…इन सबके लिए जमीन की दरकार। जमीन लेनी हुई किसानों से, गाँव वालों से।’ ये सब आधुनिक समय की उपनिवेशीय नीतियाँ हैं।
भारतीय समाज की एक विशेषता है–संरक्षण और शोषण। सामंती व्यवस्था उन्हें संरक्षण की आशा देते हुए शोषण करती हैं। यहाँ औपनिवेशिक शक्तियाँ नया रूप धारण करके विकासशील, अविकसित देशों को अपनी आर्थिक गुलाम बनाती हैं। वे विकास कार्य कर्मों के रूप में आते हैं। वीरेंद्र जैन के उपन्यास विकास के विरोधी नहीं है। लेकिन मुट्ठी भर लोगों की सुविधा नीति का विरोध करते हैं। यह वास्तव में औपनिवेशिक शक्तियों का नया रूप है।
इसके साथ विकसित होता एक व्यवसाय है बाँधों का निर्माण। बिजली के उत्पादन से बढ़कर विश्व बैंक की सहायता से बननेवाले इन बाँधों का निर्माण बहुराष्ट्रीय कंपनियों एवं राजनीतियों का षड्यंत्र है। भारत के सीमेंट के उत्पादन के 21 से अधिक प्रतिशत बाँधों के निर्माण क्षेत्र से ही उपयोग किया जाता है। इस्पात एवं तार के उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बाँधों के क्षेत्रों में ही उपयोग करते हैं। बाँध निर्माण के हजारों वर्षों का इतिहास है। हर एक देश में बाँधों के निर्माण को वहाँ के शासक अपनी प्रौढ़ता को दिखाने के माध्यम के रूप में उपयोग करते हैं। बाँध का निर्माण एक नदी के स्वाभाविक बहाव को रोकता ही नहीं बल्कि एक नदी को पूर्णतः बिगाड़नेवाली निर्मिति ही है। यह दूसरी तरफ से पूरी परिस्थिति को और उसके संतुलन को भी तहस-नहस करता है। नदी का वास्तविक चरित्र उसका बहाव है। उसे रोकने से उसकी रासायनिक घटना, नैतिक गुण सब नष्ट हो जाते हैं। नदी में जीने वाले जीव जंतुओं की जिंदगी भी बरबाद हो जाती है। उसके तटों में रहनेवाले लोगों की जिंदगी को, उसकी खेती को नष्ट करते हैं। अनेक लोग का जन्म स्थान नष्ट होता है। अपने ही देश में शरणार्थी बनना पड़ता है। चीन के त्री गोर्ज, ब्राजील के बिलबिला, वियटनां के टाबू, भारत के सरदार सरोवर आदि इसके लिए उदाहरण हैं। देखने की बात यह है कि विश्व में निर्मित बाँधों में कुल 6000 क्यूबिक किलो लीटर जल को इकट्ठा करके रखा हुआ है। मतलब विश्व की सभी नदियों में बहने वाले पानी के तीन गुना अधिक है।
उपन्यासों से मिले आँकड़ों के अनुसार दोनों राज्यों के 224 किलोमीटर इलाका बाँध प्रभावित इलाका है। यह बाँध पूरे होने तक हमारी वन संपदाओं, वनस्पतियों और वन्य प्राणियों की जो हानि हो चुकी उसकी पूर्ति कब, किससे हो सकेगी? प्राकृतिक वनों की संरचना एक जटिल प्रक्रिया है। हजारों वर्ष का विकास उन्हें वनस्पति-विविधता देता है। कृत्रिम रूप से रोपित वनों में वह बात आ ही नहीं सकती। राम दुलारे का यह चिंतन वास्तव में सारी विकास नीतियों पर प्रश्नचिह्न डालनेवाला है।
एक विशालकाय बाँध अनेक हेक्टर वनों को अपने साथ डुबाते हैं। बदले में किये जाने वाले वनीकरण प्राकृतिक वनों का स्थान नहीं ग्रहण करते। बड़े-बड़े बाँध नदियों की परिस्थितियों को नष्ट करते हैं। नदी के नीचे क्षेत्र के लोगों की खेती, मछुवारों की आजीविका पर बुरी तरह से प्रभाव डालता है। वर्षाकालीन नुकसान से प्रकृति को बचाने का उपचार कार्यक्रम के रूप में बाँध माने जाते हैं। लेकिन यहाँ उपचार कार्यक्रम से बढ़कर नदी एवं उसके आसपास की परिस्थिति का रोगीकरण ही वास्तव में होता है। नदी में बहने वाला जल उसके तटों के भूगर्भजल के आँकड़ों को बढ़ाता है। उसके अलावा वर्षा काल में पहाड़ों से अनेक प्रकार की धातुओं और रेत को उसके तटों में ले जाती है। इससे नदी तटों की मिट्टी खाद पदार्थ संपन्न बन जाती है।
विश्व में होने वाले बदलाव से हम मुँह नहीं मोड़ सकते हैं। पुरानी बैलगाड़ी के चलते रहने पर ही हमारी संस्कृति कायम रहेगी है, वैसी धारणा नहीं बल्कि विकास योजनाएँ वहाँ के भौगोलिक एवं प्रांतीय विशेषताओं के आधार पर होनी चाहिए। किसी भी विकास योजना के बारे में तथाकथित स्थानीय इलाके के स्थानीय लोगों को जानने तथा उसका प्रभाव किस प्रकार उन पर पड़ने की संभावना है आदि जानने का हक उन्हें है। इससे संबंधित सारी जानकारियों को प्राप्त कराना एक प्रजातंत्रीय देश के लिए अनिवार्य है। निर्णय लेने का अधिकार जनता को देना चाहिए। वास्तव में इसको ही सुस्थिर विकास कहते हैं। गाड्गिल कमिटी रपट भी इस अधिकार की विकेंद्रीकृत रीति को ही बल देता है। वह एक समाज की सांस्कृतिक एवं राजनीतिक विकास भी है। ‘पार’ के मुखिया दुनिया से कहते हैं कि ‘देखो दुनिया, जमाना बदल रहा है। हमारा मन चाहता है कि हम बदले जमाने के संग-संग। पर सब कायदे एक साथ तोड़े नहीं जा सकते, छोड़े नहीं जा सकते। हमें बदलना तो होगा। लाजिमी बदलना होगा। मजबूरन बदलना होगा। पर सब कुछ एक साथ बदलने से कुछ न बचेगा। नया कुछ गढ़ा नहीं जा पाएगा, पुराना हाथ से छूट जाएगा। कुछ हाथ न लगेगा।’ मुखिया की यही सोच एक पहचान है। हर एक विकास योजना को लागू करते समय इस सत्य को साथ लेना चाहिए। उसे वहाँ के स्थानीय लोगों को सहायक सिद्ध होना है। भारत जैसे देशों में विकास योजनाओं का परिणाम विस्थापितों का अनाथत्व है। जीवन की आशाओं से वह बाहर फेंके जाते हैं। स्थानीय प्रशासन एवं स्थानीय लोगों के संयोग एवं प्रदेश के संरक्षण एवं पुनःनिर्माण भी एक साथ होना चाहिए।
‘किसी एक जाति, किसी एक हुनर के लोगों से नहीं बनता गाँव। ऐसे लोगों के जमावड़े से कारखाना तो बन सकता है, कमाई भी होती है वहाँ, उत्पादन भी, बस्ती भी बस जाती होगी। वहाँ, लेकिन एक पेशे के लोगों से गाँव नहीं बनता कभी।’ 105 वर्षीय माते का यह कथन परिस्थिति के साथ मानव की आत्मीयता के भाव को व्यक्त करता है। इससे यह भी व्यक्त होता है कि मनुष्य प्रकृति का अभिन्न अंग है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि मनुष्य इस धरती का एकमात्र अधिकारी है। इस कथन से यह शंका भी उत्पन्न होता है कि अगर जमीन हमारी नहीं है तो हम कैसे उसकी बिक्री कर सकते हैं। यह एक आत्म पहचान है। इसको पारिस्थितिक आत्मीयता भी कह सकते हैं। वास्तव में ये उपन्यास इस पहचान की आवश्यकता को व्यक्त करते हैं। पूरे विश्व को कायम रखने के लिए यही एकमात्र उपाय है।
जल का प्रबंध और उपयोग के लिए भारत में सबसे पुरानी और प्रकृति के अनुरूप पद्धतियाँ थीं। पानी की आवश्यकता के अनुसार छोटे तालाबों के जरिये खेतों में पानी नहरों से ले जाया जाता है। यहाँ छोटे-छोटे ऊर्जा उत्पादन केंद्रों की स्थापना करने से स्थानीय लोगों के उपयोग के लिए ऊर्जा मिलती है और प्रकृति के लिए नुकसान भी नहीं होता। यह हमारी प्रकृति के लिए बहुत ही अनिवार्य है। आज भारत की नदियाँ और उसकी पोषक नदियाँ कांक्रीट के दीवारों के बीच समेटी गयी हैं। ध्यान देने की बात यह है कि बाँधों में 90 प्रतिशत जैव वैविध्य से भरे क्षेत्रों में है। बिजली के उत्पादन के नाम पर अनेक हेक्टर वनों को कटा दिया है। वन, प्रदेशों के वातावरण को बनाये रखते हैं। बारिश के समय मिट्टी पानी के साथ मिलकर नीचे की ओर तेजी से बहता है। बिजली को ले जाने के लिए टवर लैन को विस्तार करने के लिए और अवर को स्थापित करने के लिए वनों और पहाड़ों को काटना पड़ता है। लेकिन देखने की बात यह है कि भारत में 600 मीलियन लोग बिजली के बिना जी रहे हैं।
उपन्यास में चित्रित डूब वास्तव में औद्योगिक विकास से उत्पन्न डूब है। वह हमेशा गाँवों को तहस-नहस करता है, क्योंकि हर एक विकास के पीछे का लक्ष्य शहरीकरण को बढ़ावा देना है। शहर के जीवन को और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए वे गाँव के लोगों को डूबने देते हैं। इसके परिणामस्वरूप गाँव के लोगों को मजदूर बनकर शहर जाना पड़ता है। गाँव के किसानों को शहर में गुलाम-सी जिंदगी जीना पड़ता है। यह हर एक विकास नीति की अंतिम दशा है। वह चाहते नहीं तो भी विवश है। भारत गाँव खेती पर ही निर्भर है। वहाँ नदी, तालाब, नाल सब आपस में संबंध रखकर आगे बढ़ते हैं। लेकिन बाँध के आने पर वहाँ का सरस, तालाब, नाली सब नष्ट हो जाते हैं। गाँव की आपसी मेल-जोल ही नष्ट हो जाती है। ‘डूब’ और ‘पार’ उपन्यास समकालीन कांक्रीट सागर में डूब जाने के लिए विवश जनता के यथार्थ का अनावरण करते हुए उसके पार के सपने को दिखा देने वाले हैं।
‘जहाँ जल हो, छाँह हो, उजियारा हो, जमीन हो, वहाँ जीवन तो कब का दस्तक दे चुका होगा।’
Image: A Sikh Sardar reading from a book, seated in front of a window
Image Source: Wikimedia Commons
Image in Public Domain