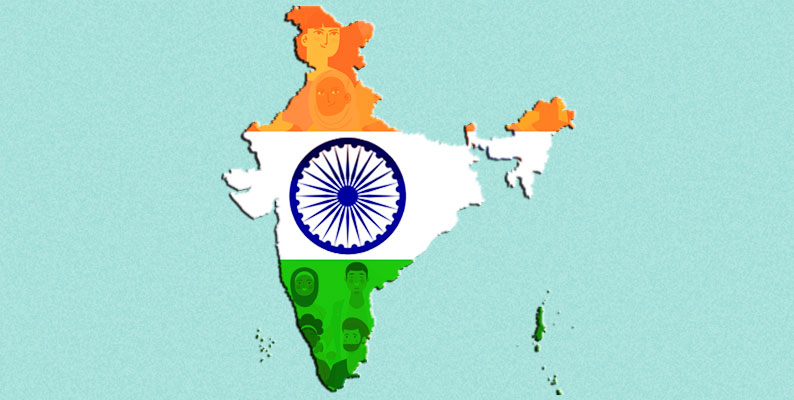संस्कृत-साहित्य में एकांकी
- 1 July, 1953
शेयर करे close
शेयर करे close

शेयर करे close
- 1 July, 1953
संस्कृत-साहित्य में एकांकी
आधुनिक साहित्य के कतिपय विकसित अंग–स्थापत्य और प्रवृत्तियों की दृष्टि से–पश्चिम की आभा से ही आभासित हैं। उनमें ‘वेदमूलकता’ का संधान आग्रहमात्र होगा। उदाहरण के लिए, आधुनिक उपन्यास कादंबरी की औरस संतान नहीं हैं; आधुनिक छोटी कहानियाँ पंचतंत्र, भोजप्रबंध आदि की परंपरा की नहीं हैं और आधुनिक एकांकी भी भास से प्रभावित नहीं हैं।
इतने पर भी, भारतीय नाट्य-साहित्य एकांकी की कल्पना से सर्वथा वंचित था, यह स्थापना पश्चिम के प्रति अंध पक्षपात-प्रदर्शन करने के अतिरिक्त कुछ नहीं। यह और बात है कि ‘एकांकी’ नाम ‘one-act play’ के अनुकरण पर प्रचलित है–इसका प्राच्य नामों से विशेष संबंध नहीं है ! अथवा, मूल रूप में ये सारी वस्तुएँ भारतीय परंपरा में विद्यमान रही हैं; किंतु आधुनिक साहित्य ने उनसे प्रभाव ग्रहण नहीं किया, वह सीधे पश्चिम से प्रणोदित होता रहा है।
अवश्य मैं मुंशी के ‘भगवान परशुराम’, ‘भगवान कौटिल्य’, किंवा निराला की ‘प्रभावती’ में बाणभट्ट की-सी महान प्रतिभा के दर्शन करता हूँ, और उदयशंकर भट्ट, रामकुमार वर्मा आदि के एकांकियों में प्राच्य संस्कृति की शृंखला को नई छवि-छटा से विच्छुरित भी पाता हूँ; किंतु यह सब पूर्व के प्रति पूर्वग्रह के परिणामस्वरूप कदापि नहीं। तब कह सकता हूँ कि रूपक के प्रधान दस भेदों में जो एक ‘अंक’ नामक भेद है और जो एक ही अंक का होता भी है; किंतु जिसकी प्रकृति करुण रस प्रधान होती है, संपूर्ण सादृश्य की उपेक्षाकर, हम चाहें तो, एकांकी के मूल शास्त्रीय रूप में उसे याद कर सकते हैं।
‘संस्कृत साहित्य में एकांकी’ पर विचार-विमर्श करने के पहले यह लक्ष्य करना अत्यंत आवश्यक है कि हमारे यहाँ साहित्य के प्रत्येक अंग-उपांग का वर्गीकरण पश्चिमी वर्गीकरण से बिलकुल ही पृथक् प्रकार का है । सुस्पष्ट शब्दों में, यहाँ कलामात्र की आत्मा के रूप में ‘रस’ को स्वीकृत कर लिया गया है। अत: हमारी विभाजन-प्रणाली रस को केंद्रित कर, उसी के आस्वाद की प्रक्रिया पर निर्भर है।
रसास्वाद ही यहाँ साहित्य या कला का चरम अभिप्राय समझा जाता रहा है। मुद्राराक्षस जैसे राजनैतिक नाटक में भी हम इतिहास, राजनीति आदि बौद्धिक तत्वों को रसोन्मुख पाते हैं। रस-सृष्टि के इसी आग्रह के कारण हम चाणक्य और चंद्रगुप्त जैसे महान व्यक्तियों के उच्च चरित्र-चित्रण के बावजूद नाटक का नाम ‘मुद्राराक्षस’ देखते हैं। अस्तु, प्रस्तुत ‘एकांकी’ के स्वरूप-निरूपण तथा वर्गीकरण के मूल में भी यही ‘रस’ है।
आचार्य धनंजय ने अपने ‘दशरूपक’ में रूपक के प्रधान दस भेद बतलाए हैं–
नाटकं सप्रकरणं भाण: प्रहसनं डिम:
व्यायोगसमवकारौ वीथ्यकङहामृगा इति ।
अर्थात–नाटक, प्रकरण, भाण, प्रहसन, डिम, व्यायोग, समवकार, वीथो, अंक और ईहामृग–ये दस रूपक कहे जाते हैं। इन दसों में पाँच एकांकी हैं–भाण, प्रहसन, व्यायोग, वीथी और अंक। भाण में किसी कल्पित धूर्त नायक का चरित्र चित्रित होता है। इसमें शृंगार अथवा वीर-रस की प्रधानता होती है। संस्कृत-साहित्य में ‘भाण’ प्रचुर परिमाण में उपलब्ध होते हैं, जैसे–वसंततिलक, पद्मताडितक आदि। इनके अतिरिक्त वत्सराज का ‘कर्पूर चरित्र’, वामनभट्ट बाण का ‘शृंगार-भूषण’ भी उल्लेख्य भाण-ग्रंथ हैं।
प्रहसन में कोई कवि-कल्पित धृष्ट नायक होता है और वह भरसक तपस्वी, संन्यासी अथवा ब्राह्मण ही रहता है। भाण में भी और प्राय: प्रहसन में भी ‘मॉनोलॉग’ (monologue) की भाँति नाना अवस्थाओं के भीतर से एक चरित्र का चित्रण मुख्य होने के कारण स्वगत-भाषण अथवा ‘आकाशभाषित’ के सहारे उक्ति-प्रत्युक्तियों के लिए पर्याप्त अवकाश रहता है। मत्तविलास, लटकमेलक तथा वत्सराज-कृत ‘हास्य-चूड़ामणि’ संस्कृत के प्रतिनिधि प्रहसन हैं।
व्यायोग तीसरा प्रकार है एकांकी का। इसकी कथावस्तु कल्पित न होकर इतिहास-पुराण से गुंफित होती है। इसके नायक की प्रकृति में भी विविधता पाई जाती है। वह देवता हो सकता है; राजर्षि हो सकता है; धीरोद्धत भी हो सकता है। इसमें हास्य-रस की प्रधानता हो सकती है, शृंगार-रस की और शांत-रस की भी। इस प्रकार वस्तु-विस्तार के साथ-साथ रस-विस्तार के लिए भी यहाँ काफी गुंजाइश रहती है।
ईस्वी सन् 1909-10 में स्वर्गीय महामहोपाध्याय टी. गणपति शास्त्री ने दक्षिण-ट्रैवनकोर में महाकवि भास के जिन 13 नाटकों का पता लगाया था, केवल उनमें भी पाँच एकांकी हैं और संयोगवश वे सब-के-सब ‘व्यायोग’ हैं। क्रमश: उनके नाम हैं–मध्यमव्यायोग, दूतवाक्य, दूतघटोत्कच, कर्णभार और ऊरुभंग। इनके अतिरिक्त विश्वनाथ कृत ‘सौगंधिकाहरण’, प्रह्लादन देव-कृत ‘पार्थ पराक्रम’, कांचनाचार्य-कृत ‘धनंजय-विजय’, रामचंद्र रचित ‘निर्भय-भीम’, वत्सराज-रचित ‘किरातार्जुनीय’ और धर्मपंडित-निर्मित ‘नरकासुर-विजय’ संस्कृत के प्रतिनिधि ‘व्यायोग’ हैं।
‘वीथी’-नामक प्रकार में भी एक ही अंक होता है और एक ही कवि-कल्पित नायक भी, जो उत्तम, मध्यम या अधम–कैसा भी हो सकता है । वह ‘आकाश-भाषित’ द्वारा ही अपनी उक्ति प्रत्युक्तियों से, विशेषकर शृंगार और सामान्य रूप में दूसरे-दूसरे रसों को भी अभिव्यक्त करता है। स्थापत्य की दृष्टि से इसके एक ही अंक में पूरे नाटक की-सी कसावट होती है; क्योंति इसमें ‘मुख’ और ‘निर्वहण’ संधियों तथा बीज, विंदु, पताका आदि ‘अर्थ-प्रकृतियों’ का सम्यक् निर्वाह अपेक्षित होता है। ‘साहित्यदर्पण’ में इसके और तेरह अंगों का उल्लेख किया गया है, जिनके संबंध में विश्वनाथ की टिप्पणी दर्शनीय है–
‘एतानि च अंगानि नाटकादिषु संभवन्त्यपि वीथ्यामवश्यं विधेयानि । वीथीव नानारसानां चात्र मालारूपतया स्थितत्वाद् वीथीयम् ।’ वह कहते हैं कि यों तो इन अंगों का प्रयोग नाटकों में हुआ ही करता है; किंतु ‘वीथी’ में तो ये सर्वथा अत्याज्य हैं; यहाँ इनका निश्चित निर्वाह होना ही चाहिए, जैसा कि ‘मालविका’ नामक वीथी में हुआ है।
और रूपक के ‘अंक’ नामक प्रमुख भेद के विषय में यह चर्चा की जा चुकी है कि वह करुण रस प्रधान होता है; उसके पात्र–नायक भी प्राकृत जन ही होते हैं; उसमें स्त्रियों के विलाप-कलाप के साथ-साथ गेय पदों की भी खपत हो सकती है। इसकी कथा-वस्तु प्रख्यात भी होती है और कवि कल्पित भी। एक अंक के तंग दायरे में वस्तु तथा विधान के इस लचीलेपन को पचा लेना इसकी विशेषता है।
आधुनिक युग को, कर्म संकुल घोषित करते हुए आलोचकों के एक वर्ग ने छोटी कहानी को उपन्यास का समयोपयोगी संक्षिप्त रूप सिद्ध करने की चेष्टा की थी। वह एकांकी को भी बड़े नाटक का लघु रूप ही समझता था। अवश्य अब ये साहित्य के स्वतंत्र अस्तित्व घोषित तथा प्रमाणित हो चुके हैं। किंतु संस्कृत-साहित्य के समुद्र का अवगाहन करने पर पूर्वोक्त एकांकियों पर कर्म-संकुलतावाला तर्क तो किसी भी प्रकार नहीं लागू होता। कारण, जहाँ संस्कृत के श्रव्य काव्यों का आरंभ वेद, वाल्मीकि और व्यास से हुआ, वहाँ भरत मुनि के अनुसार दृश्य काव्य का उद्गम ‘अमृत मंथन’ नामक ‘समवकार’ तथा ‘त्रिपुरदाह’ नामक डिम है और ये दोनों-के-दोनों एकांकी रूपकों से कुछ ही बड़े आकार-प्रकारवाले होते हैं। समवकार में अधिक-से-अधिक तीन और ‘डिम’ में चार अंक होते हैं–जबकि शताब्दियों बाद संस्कृत में दस-दस अंकों तक के महानाटक लिखे गए हैं। इतना ही नहीं, जिस भास को स्वयं कालिदास ने न केवल पूर्ववर्ती माना है, अपितु अपनी नाट्यकला की चटकीली चाँदनी से सहृदयों के हृदय को उजागर करने वाला भी प्रमाणित कर दिया है–‘मालविकाग्निमित्र’ की प्रस्तावना में इस आशंकापूर्ण उक्ति से कि–‘प्रथितयशसां भासंसौविदल्लकविपुलादीनां प्रबंधानतिक्रम्य वर्तमानकवे: कालिदास क्रियायां कथं परिषतो बहुमान:?’ उसने भी नाट्यकला के उस प्रारंभिक युग में पाँच-पाँच ‘एकांकी’ लिखे थे, क्या यही एकांकी की स्वतंत्र और महत्त्वपूर्ण सत्ता पर पर्याप्त प्रकाश नहीं डालता ? यह नहीं उद्घोषित करता कि एकांकी बड़े नाटक का संक्षिप्त रूप नहीं है, प्रत्युत् उसका कौशल, निर्वाह की दृष्टि से, नाटक से भी कठिन है और उसका क्रमिक विकास भी अपने ही ढंग से होता रहा है।
इस अवसर पर पाश्चात्य एकांकियों के संबंध में कुछ ऐसी ही कही हुई ‘जौन हैंपडेन’ (John Hampden) की दो पंक्तियों का स्मरण हो आता है–It is not that the one-act play is a new thing. The anonymous authors of the mystry plays and of ‘Everyman’, ‘The Interlude of Youth’ and ‘The world and the child’, demonstrated long ago the heights which it can reach. इसी प्रकार उसके संकलित Lady Gregory से Nora Ratcliff तक के इस युग के बीसों एकांकियों में परिस्थितियों और मन:स्थितियों के बीच हम जैसी अन्विति पाते हैं, भास से कंचनाचार्प्य तक के एकांकियों में वैधानिकता और रसात्मकता की वैसी ही अनुस्यूति प्रौढ़ि और विदग्धंता का भी अनुभव करते हैं, जो 15 सौ वर्षों से सहृदयों के हृदयों को जीतती चली आ रही है। दूसरे शब्दों में, उन एकांकियों ने युगोचित उपयोगिता खोकर टिकाऊ आनंद को वरण कर लिया है।
यहाँ आनंद के जिस स्थिति विशेष से मेरा तात्पर्य है, उसका स्पष्टीकरण आवश्यक है। मध्ययुग के कवियों ने सौंदर्य का ढक्कन उठाकर जिस सत्य का साक्षात्कार कराया है, उसे जीवन की मूल प्रेरणा भी कहा जा सकता है। वह जीवन के प्रति आस्थावान् थे, अत: उसकी सौंदर्य चेतना ‘नीर-भरी बदरी’ नहीं है; वह शुद्ध आनंद के चक्कर में रहस्यमयी भी नहीं हो गई है। अत: मम्मट ने काव्य का प्रयोजन बतलाते हुए जिस ‘सक्ष्य: परनिवृत्ति’ अथवा ‘कांता-सम्मित उपदेश’ का उल्लेख किया है, अधिक-से-अधिक वे वहीं तक पहुँचना चाहते थे। उनका दृष्टिकोण आदर्शोन्मुख यथार्थ या यथार्थोन्मुख आदर्शवादी रहा है। वे हास्य और व्यंग्य की सृष्टि जीवन की जटिलताओं के समाधान के रूप में कम और विनोद तथा उपदेश के लिए अधिक कर सके हैं। उनका यह जीवन-दर्शन कालिदास में अतिशय उदात्त रूप में अभिव्यक्त हुआ है और वत्सराज, कांचनाचार्य ऐसों में साधारण अथवा निम्न स्तर पर उतर कर।
अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण को प्रकट करूँ, तो कहूँगा, पूर्वोक्त कोई भी एक एकांकी (चाहे वह भास का हो या वत्सराज का) मुझे उस स्थिति तक नहीं प्रभावित कर पाता, जिस तक ‘नॉरमैन किनेल’ का विस्टर ह्यूगो के ‘ले मिरेले’ या ‘ला मिजरेब्ल’ के प्रारंभिक कथांश पर आधारित ‘Bishop’s Candlesticks’–नामक एकांकी कर सका है। भारतीय कला जिस सात्विक आनंद का आग्रह करती है, उसकी सजल अनुभूति यहाँ होती है।
जो हो, ऊपर जिन पाँच प्रकार के एकांकियों की विस्तारपूर्वक चर्चा की गई है, वे दस मुख्य रूपकों में से हैं। किंतु इन दस रूपकों के अतिरिक्त अट्ठारह उपरूपक भी हैं–नाटिका, त्रोटक, गोष्ठी, सट्टक, नाट्य रासक, प्रस्थान, उल्लाप्य, काव्य, प्रेंखण, रासक, संलापक, श्रीगदित, शिल्पक, विलासिका, दुर्मल्लिका, प्रकरणी, हल्लीश और भाणिका। और, सौभाग्यवश इन अट्ठारहों में दस एकांकी हैं–गोष्ठी, नाट्यरासक, उल्लाप्य, काव्य, प्रेंखण, रासक, श्रीगदित, विलासिका, हल्लीश और भाणिका।
विश्वनाथ के अनुसार गोष्ठी में प्रहसन शृंगारयुक्त एक अंक होता है, आठ-दस प्राकृत पुरुष-पात्र और पाँच-छ: स्त्री-पात्र होते हैं, जैसे, रैवतमदविका नामक गोष्ठी।
‘नाट्यरासक’ आधुनिक संगीतरूपक जैसा होता है। इसका अंक ताल और लय से बंधा हुआ रहता है। शृंगारपूर्ण हास्य की इसमें प्रधानता होती है। इसका नायक उदात्त और नायिका वासकसज्जा होती है, जैसे–‘नर्मवती’ अथवा ‘विलासवती’।
‘उल्लाप्य’ का नायक दिव्य उदात्त होता है। उसका कथानक देवोचित चरित्र से युक्त रहता है। शृंगार, हास्य तथा करुण-रसों का प्राधान्य रहता है, जैसे–पार्थ-पाथेय या देवीमहादेव।
‘काव्य’ में हास्य-रस की प्रमुखता रहती है। और तो और, इसमें स्त्री ही नायक का कार्य करती है, जैसे–यादवोदय।
‘प्रेंखण’ में नीच नायक होता है। उसके कथनोपकथन में औद्धत्य तथा रोषपूर्ण भाषण की प्रचुरता होती है, जैसे–बालिवध।
‘रासक’ में प्रख्यात नायिका और मूर्ख नायक होते हैं। उसमें भाँति-भाँति की भाषाओं का प्रयोग होता है, जैसे–मेनकाहित।
‘श्रीगदित’ में नायक प्रख्यात तथा उदात्त होता है और तदनुरूप नायिका भी सुप्रसिद्ध हुआ करती है। इसकी कथावस्तु भी विख्यात ही रहती है, जैसे–क्रीड़ारसातल।
‘विलासिका’ शृंगारवहुला होती है। उसमें लास्य के दस अंकों का निर्वाह किया जाता है अर्थात् इसे आधुनिक शब्दों में नृत्यरूपक भी कहा जा सकता है। इसका नायक हीन प्रकृति का होता है। कुछेक आचार्यों का मत है कि इसमें नायिका नहीं होती अत: इसका उचित नाम ‘विलासिका’ नहीं ‘विनायिका’ होना चाहिए।
‘हल्लीश’ का अंकव्यापी वातावरण लय-तालमय होता है। यह भी मुख्यत: संगीत रूपक है, जैसे–केलिरैवतक।
और, ‘भणिका’ की नायिका उदात्त तथा नायक हीन प्रकृति का होता है, जैसे–‘कामदत्ता’।
इस प्रकार पाँच रूपक और दस उपरूपक एकांकी होते हैं और ये पंद्रहों प्रकार नवल आविष्कार नहीं, प्रत्युत् पंद्रह सौ वर्षों की परंपरा रखते हैं। यह उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट हो जाता है।
इन प्राचीन संस्कृत एकांकियों के साथ आधुनिक एकांकियों का तुलनात्मक अध्ययन अत्यंत रोचक होगा, इसमें संदेह नहीं; किंतु यहाँ उसके लिए अवकाश कहाँ?
एकांकी में नाटक के संपूर्ण लक्षण को आत्मसात् करने की क्लिष्ट कल्पना कभी नहीं हुई। एकांकी के व्यक्तित्व का उभार उसकी अपनी ही सीमाओं के भीतर होता है। वह जीवन की एक विशेष स्थिति या परिस्थिति की झाँकी लेता है, जीवन की संपूर्णता को आँकने की चेष्टा नहीं करता। इसीलिए एकांकी का मुख्य लक्ष्य एक विशिष्ट स्थिति या परिस्थिति में ही जीवन को प्रस्तुत करना होता है। अवश्य इस लक्ष्य को विश्वजनीन या विराट् रूप देने की सुविधा भी रहती है। वस्तुत: एकांकी की कला के सफल निर्वाह के लिए उपर्युक्त लक्ष्य की सीधी, सादी और सुगठित अभिव्यक्ति अनिवार्य है। इसमें रूढ़ नाटकीय जटिलताओं के लिए स्थान नहीं है।
Original Image: A woman holding a Veena Mughal India 18 century
Image Source: Wikimedia Commons
Image in Public Domain
This is a Modified version of the Original Artwork