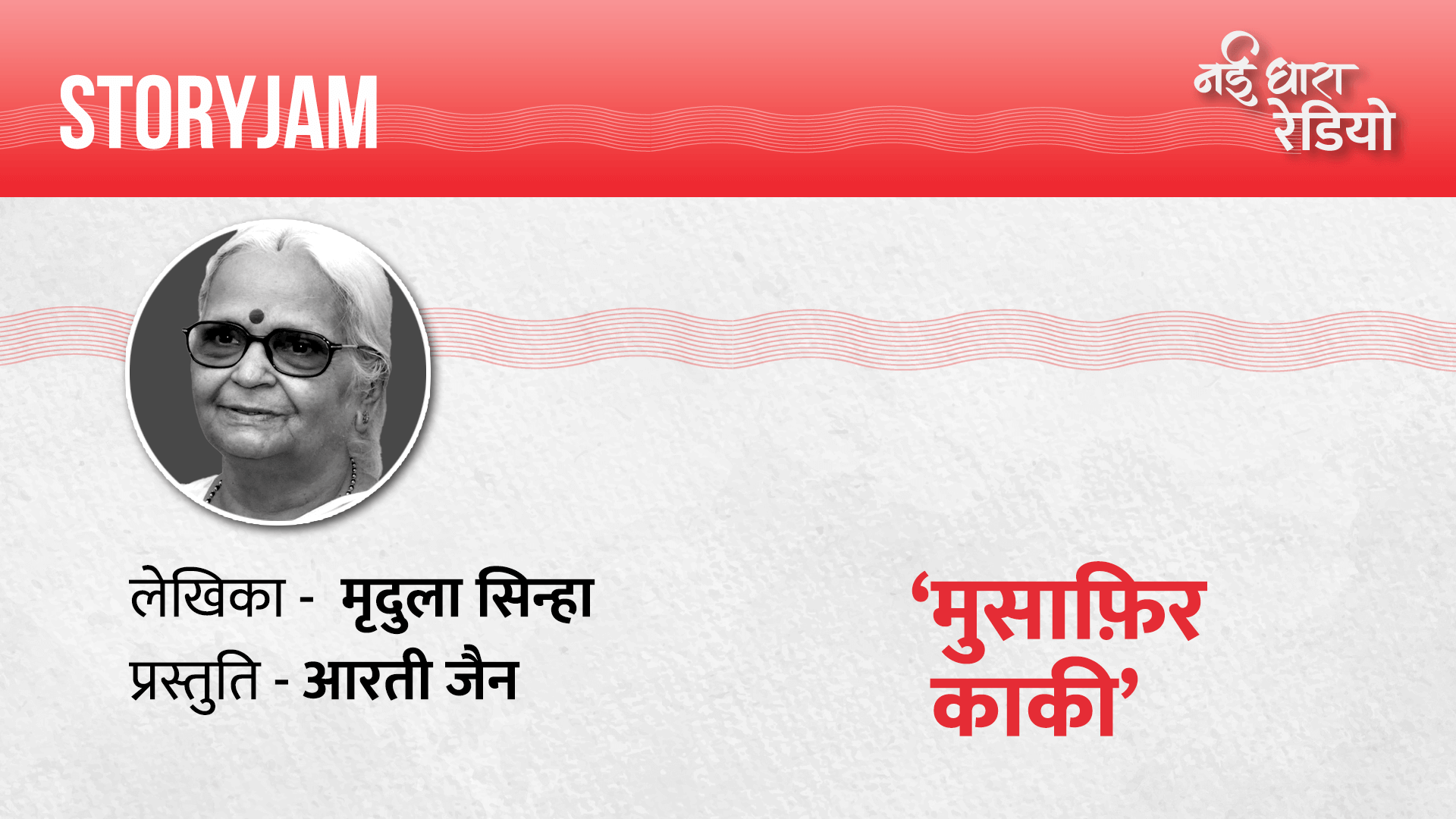मुसाफिर काकी
- 1 October, 2016
शेयर करे close
शेयर करे close

शेयर करे close
- 1 October, 2016
मुसाफिर काकी
दादी की वह कोई पहली यात्रा नहीं थी। वह तो पर्व-त्योहार पर गंगा-स्नान से लेकर मेला-ठेला घूमने-घुमाने में दक्ष हो गई थीं। अयोध्या, मथुरा, काशी, जनकपुर धाम के साथ चारों धामों की यात्रा समाप्त कर गंगासागर भी हो आई थीं। और इन तीर्थस्थलों की यात्रा कर-करके वे ऐसी यात्रा-नायिका बन गई थीं कि गाँव की महिलाओं का झुंड लेकर बिना किसी पुरुष की सहायता के निकल पड़ती थीं। कभी-कभी तो बिल्कुल अकेली। जिन अधवयसा अथवा नवोढ़ा को अपने घरवालों से तीर्थ जाने की अनुमति नहीं मिलती हो, वह अपना अंतिम अस्त्र अपनाती थीं–‘मैं अकेले थोड़े जा रही हूँ, मुसाफिर काकी के साथ जा रही हूँ।’
फिर तो उनका यह अस्त्र अचूक बैठता था। जब मुसाफिर काकी संग-साथ हों तो अपने घरवालों से क्या पूछना। राघव काका की अम्माँ गाँव भर की काकी थीं। किसी की घूमनी काकी, किसी की दुःखहरनी काकी; किसी की मोहिनी काकी तो किसी की मुसाफिर काकी। मुसाफिर काकी भी प्रसिद्ध हो गईं। शायद तीन सौ पैंसठ दिनों का एक-चौथाई भाग वह गाँव से बाहर ही रहतीं। एक यात्रा से लौटकर आतीं तो गाँव भर में उनका यात्रा-वृत्तांत यात्रारत रहता, उनकी अगली यात्रा की तैयारी शुरू हो जाती। तैयारी भी कोई ऐसी-वैसी नहीं, हर यात्रा के दौरान उन्हें एक नया कड़वा मधु अनुभव होता। अनुभवों के अनुकूल यात्रा सतर्कता बरतने में कोई कोताही नहीं होने देतीं। मर्दानी कमीजनुमा ब्लाउज की जेब से जेबकतरे ने एक बार पैसा क्या निकाल लिया, उन्होंने कमीज की डिजाइन ही बदल दी। रुपये रखने की जेब अंदर बन गई। बिल्कुल छाती के बीचोंबीच। एक बार ट्रेन से उतरते वक्त उनकी चोटी फँस गई, फिर क्या था–दूसरी यात्रा पर जाने से पूर्व बाल ही कट गए। यात्रा में थैला का मुँह खुला था, कुछ सामान गिर गए; फिर तो जो थैले उनके साथ जाएँ, सबके मुँह सिले हुए। उनकी सहयात्री महिला-पुरुष को उनकी आज्ञा के अनुसार ही साज-सामान लेकर चलना पड़ता था, वरना नंबर ही कट जाए।
किसी महिला ने यात्रा के दौरान उनके साथ कदम नहीं मिलाया, गंगा में डूब नहीं लगाई या अधिक डूब लगा ली या उनकी आज्ञा के बगैर किसी दूसरे मुसाफिर से बात कर ली, उसका नंबर फिर कभी न आया। किसी का नंबर आने के कई कारण होते थे। गाँव में कोई महिला बहुत दिनों से मैके नहीं गई तो मुसाफिर काकी का मन पिघल जाता। कहतीं–‘बेचारी चार वर्ष से अपने आँगन में कैद है। उसको इस बार गंगा नहला लाऊँगी।’ किसी को बहू ने तंग किया हो, मुसाफिर काकी कहतीं–‘चल-चल। इस बार तुम्हें गंगासागर ले चलती हूँ। फिर इसको पता चलेगा, सास के बिना कैसे गृह-कारज चलता है।’
गाँव की मुसाफिर काकी यानी मेरी दादी जब कभी तीरथ-धाम से लौटकर आतीं, घर भर के सदस्यों के लिए छोटी-मोटी चीजों से उनका एक थैला भरा होता। हम सब घेरकर बैठ जाते। माँ-चाची उनके लिए गरम पानी करतीं, उनके पैर-हाथ धोतीं, नहलातीं, खाना खिलातीं। कई दिनों तक गाँव भर की औरतों से उनकी खाट घिरी रहती। सब बारी-बारी से उनका शरीर दबातीं। तेल लगातीं और आशीर्वाद पातीं। सुहागन को सिंदूर लगाकर मिसरी की गोली देतीं। विधवाओं के लिए तुलसी की माला तो कोई भगवान् की छोटी पीतल-काँसे की मूर्ति। उपहार से भी अधिक लोगों की रुचि उनके यात्रा-वृत्तांत में होती।
एक बार तिरुपति जाते हुए उन्हें रास्ते में कई मुसाफिर मिल गए थे। उनकी भाषा काकी के पल्ले नहीं पड़ी। काकी सुनातीं–‘अब क्या बताऊँ! दो छोंड़ा सीट पर जमकर बैठ गया। घिसके ही नहीं। हम नीचे बैठे हुए। हमने खूब गाली दी। गाली सुनकर भी ‘ही-ही-ही’ करता रहा। एकदम थुथुर। तब हम सोचे कि ई प्यार से ही मानेगा। हम बोले, ऐ बबुआ, हम तोहर आजी हुई। हमरा आसपास हमार संगी-साथी हँसे लागल-ई कि बुझी आजी-उजी। दोसरा देस के हैं। अब का करें। परदेस में तो हित-मुहब्बत से चले के परेला। उ त आजी सुनते पिघल गया। बोला, ‘आजी’ और उठकर खड़ा हो गया। इशारे से अपनी जगह दे दिया। फिर तो रास्ते भर हमार खूब सेवा किया। पूछने पर बताया कि अंधरा परदेश का मुसाफिर था।’
यह वृत्तांत सुनकर मेरे पिता जी हँसते-हँसते लोट-पोट हो गए। लोगों के पूछने पर बोले, ‘वे लड़के आंध्र प्रदेश के रहे होंगे। अब देखो ईआ को। उसे अंधरा परदेश कह रही है। और दादी को आजी कहना तो सार्वदेशिक शब्द है ही।’ काकी भी हँस पड़ी–‘अरे वही अंधरा परदेश। अब हम का करें। कभी करकट परदेश, कभी मदरसा, कभी कानपुर, नागपुर सब देश के लोग मिलते रहते हैं।’
काकी के लिए देश, परदेश और गाँव का भेद मिट चुका था। उनके लिए कानपुर, नागपुर, जयपुर, जालंधर सब परदेश थे। पर सब जगह के लोग एक। काकी कहतीं–‘अलग-अलग बोली है तो का, सबसे हम ईशारा से बात कर लेली। हमार बोली सब समझेला।’ काकी तीर्थाटन करते-करते समाजसेवी भी हो गई थीं। गाँव की कई लड़कियों की शादी वे तीर्थस्थान पर ही तय कर आतीं। गाँव आकर उसके घरवालों को बतातीं। गाँव वालों की क्या हिम्मत, जो मुसाफिर काकी की बात काट दें।
प्रवचन सुन-सुनकर सुजान हो गई थीं। इसलिए क्या मर्द, क्या औरत, सबको रामायण-भागवत-सुखसागर का प्रसंग सुनाती रहतीं। किसी तीर्थस्थान पर किसी अच्छे साधु-महात्मा से भेंट हो गई, उसे न्योत लाती थीं–‘आप हमारे गाँव में चलिए। ई सब कथा गाँव में सुनाओगे तो झगड़ा-झंझट कम हो जाएगा। सब घर स्वरग बन जाएगा।’ फिर तो गाँव वालों की मदद से साधु के प्रवचन का आयोजन होता। काकी मगन हो जातीं–‘ई हमार गाँव आज अयोध्या, मथुरा, काशी हो गईल।’ गाँव लौटकर भी उनकी दिनचर्या साधु-संतों से धर्मस्थलों पर सुने नियमों के अनुकूल होती। उनके कारण वह अकेला गाँव था, जहाँ छुआछूत नहीं थी। कोई दबंग सास भी अपनी बहू को यातनाएँ नहीं देती। किसी पुरुष का अपनी पत्नी पर उठा हाथ थरथरा जाता काकी के भय से। पर उन्हें साधु-असाधु की खूब पहचान थी। गेरुआ वस्त्र में कोई ढोंगी उनसे टकरा जाए, फिर तो उसकी खैर नहीं। एक ऐसे ही असाधु के गेरुआ वस्त्र उतरवाकर उसे सादी धोती पहनवा दी थी–‘निरलज्ज कहीं का! काम-धाम नहीं करेगा। भीख माँगेगा। ले यह कुदाल। मेरा खेत कोड़, फिर भरपेट खाना खिलाऊँगी।’ फिर तो चार दिनों तक उससे खेत कोड़वाती और भोजन करवाती रहीं।
ऐसे मौके पर गाँव के पुरुष भी उनका साथ देते। वे उनको कहतीं, ‘अरे बचवा! तू लोग मेरा नाम मुसाफिर काकी रख दिया। मुसाफिर तो सब हैं। ई भवसागर में सब मुसाफिर ही तो हैं। देह त्यागने का समय आया तो समझो यात्रा खत्म। इसलिए कहती हूँ कि नेम-धरम से रहो। जहाँ से आए हो, वहीं जाना है।’
क्या बूढ़ा क्या जवान, क्या स्त्री क्या पुरुष, सब उनकी बात ध्यान से सुनते। कोई कहता–‘अरे…रे, यही सब बात तो बड़े महात्मा जी बोले थे। यही हमारी काकी बोली हैं।’ दूसरा कहता–‘तो हमारी काकी मुसाफिर काकी कौन महात्मा से कम हैं। देश-परदेश घूम-घूमकर महात्मा हो गई।’ हर यात्रा के उपरांत गाँववालों के लिए एक नया संदेश लेकर आतीं। इडली चखकर और अपनी दाल-भरी पूड़ी, चूड़ा चखाकर आतीं। कभी सरसों का साग और मक्का की रोटी के पंजाबी संस्करण का प्रचार अपने गाँव में करतीं तो कभी दालबाटी-चूरमा का मिलान अपनी लिट्टी से करती आतीं। इडली और डोसा के उनके लिए कोई नयापन नहीं था। उनके गाँव का वगेया और चावल की रोटी ही तो थी।
काकी गंगासागर गई थीं। लौटने पर लोगों ने आँखों में आँसू भरकर उनके तोता की मृत्यु की खबर सुनाई। उन्हें अनुमान था कि अपने प्रिय तोता के लिए काकी रोएँगी, चिल्लाएँगी। काकी बोलीं, ‘इतने ही दिन का साथ था उसका और मेरा। गंगासागर में एक साधु मिले। कह रहे थे–इस भवसागर में सब संबंध वैसे ही तो हैं, जैसे नदी के जल में बहती हुई लकड़ियों का टुकड़ा मिल जाए, फिर धार के मोड़ के साथ बिछड़ जाए।’ लोग हतप्रभ होकर काकी के यात्रा अनुभव से झड़ते मोतियों को चुनते रहते। काकी एक अक्षर भी नहीं जानती थीं। पर धर्मस्थलों पर बँटे पर्चा-पत्रों को बड़े जतन से सहेजकर ले आतीं। गाँव के पढ़े-लिखे युवकों से पढ़वाकर सुनतीं और सुनातीं।
हरिद्वार में महाकुंभ लग रहा था। काकी की यात्रा की तैयारी शुरू। मैंने भी जिद ठान ली–‘मैं भी जाऊँगी।’ काकी ने इनकार कर दिया–‘नहीं-नहीं, तुमको लेकर नहीं जाऊँगी।’ मैंने शिकायत की–‘क्यों, गाँव भर की औरतों को लेकर जाती हो। मुझे क्यों नहीं?’ बोलीं, ‘बेटी! तुम्हारी उमर छोटी है। जमाना खराब हो गया। अब मैं तुम्हें सँभालूँगी कि अपने को। मैं भी तो बूढ़ी हो गई। न जाने कब कहाँ मेरी यात्रा खत्म हो जाए।’ मैंने जिद ठान ली। मेरी जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा। हरिद्वार जाने से पूर्व वे गाँव भर में घूमती रहीं। एक भी घर नहीं छोड़ा। लोगों को आश्चर्य भी हुआ। गाँव भर के लोग उन्हें विदा देने आए। मुसाफिर काकी के साथ स्त्री-पुरुषों की बड़ी जमात थी। कम उम्र की अकेली मैं। दादी ने गाड़ी में चढ़ने से पूर्व अपनी कमर में साड़ी का एक छोर कसकर बाँधा। दूसरा छोर मेरी कमर में बाँधने लगीं। मेरे एतराज करने पर कहने लगीं–‘चुपचाप जैसा कहती हूँ वैसा ही कर।’ पूरी यात्रा में उनसे बँधी रही। हरिद्वार पहुँचकर देखा तो टेंट-ही-टेंट। एक इंच जगह खाली नहीं। काकी के संगी-साथी बेचैन हो गए–‘हमारा टेंट कहाँ लगेगा? पड़ाव कहाँ डालेंगे?’ काकी ने सब इंतजाम कर दिया। शृंगेरी मठ के साधुओं ने बड़ी जगह ले रखी थी। उसमें से एक ने काकी को पहचान लिया–‘आओ माता जी, यहीं रहो। बहुत दिन बाद मिलीं।’
‘हम अकेले नहीं हैं।’
‘तो क्या हुआ, आ जाओ। सब आ जाओ।’ फिर तो जम गई काकी की मंडली। सुबह-सुबह काकी गंगास्नान के लिए निकलतीं। मेरी कमर अपनी कमर से बाँधना नहीं भूलतीं। भजन गाती हुई। टोली का आकार बढ़ता जाता। काकी ऊँचे स्वर में गातीं–‘राम हे लक्ष्मण, बन के अहेरिया रे, सीता सुंदर डुमरी के हो फूलवा।’ पीछे से सब लोग दुहराते चलते। काकी का एक और गीत सबको मनभावन लगता–
‘अपना किशोरी ले के टहल बजबई,
हम मिथिला में रहबई। मिथिला में हई चारो धाम हे
मिथिला में रहबई।’
काकी के अंधरा परदेश के या करकट परदेश के साथी हों, सब समझते थे उनके गीत के भाव को। डूब जाते थे। दिन में शंकराचार्य का प्रवचन होता और रात्रि को काकी भाव-मग्न होकर गुनगुनाने लगतीं तो उसके सामने लोग माइक रख देते। फिर तो भीड़ जम जाती। वेद मंत्रों के मैथिली पद्य अनुवाद। सरस लगता लोगों को। एक दिन तो स्वयं शंकराचार्य झूम उठे। उनकी आँखों से अश्रुधार बह चली। सीता चरित का मैथिली में गायन कर रही थीं काकी। काकी गीतकार भी थीं। समयानुकूल गीतों की रचना कर लेती थीं। अपने करुण स्वर में जब समदावन (बेटी विदाई के समय गाया जानेवाला गीत) गातीं, स्वयं रोती और सबको रुलातीं–‘बाट रे बटोहिया कि तू हू मोर भैया, हमरो संदेश लेले जा। अम्मा से कहिह पत्थर होई बैठि हे हमहु बैठव हिया हार।’ विदा ली हुई बेटी का माँ के नाम संदेश। सब रो पड़ते। काकी दिनभर घूमतीं और सबको घुमाती रहतीं। साधु-संतों का प्रवचन सुनतीं। बीच में अपने लोगों से बिछुड़ी एक बुढ़िया मिल गई, कोई खोया हुआ बच्चा मिल जाए, ले आतीं अपने पास। दूसरे दिन उसके लोगों को ढूँढ़, उनके हवाले कर ही निश्चिंत होतीं।
दूसरे दिन मुख्य स्नान था। नागा साधुओं, शंकराचार्यों का स्नान होनेवाला था। काकी रातभर गाती रहीं–भोर होने पर चल पड़ी गंगास्नान के लिए। भजन में गंगा मैया का वर्णन करती हुई। दस-बीस से बढ़कर सौ-सैकड़ा, फिर हजारों की संख्या में लोग साथ चलने लगे। फँस गई हमारी टोली। भीड़ आगे खिसकने का नाम न ले। दादी जोर से राम का नाम भजने लगीं। पता नहीं उन्हें क्या सूझी, उस जमी भीड़ में बड़ी मुश्किल से अपना हाथ अपनी कमर तक ला पाईं। कमर पर बँधी साड़ी का छोर खोल दिया। उनकी बाईं ओर पुलिसवालों का एक मंच बना रखा था। मुझे धक्का देकर कहा, ‘चढ़ जा तू इस पर।’
‘नहीं दादी मैं…मैं तुम्हारे साथ रहूँगी।’ मेरी रुआँसी आवाज। वह चिल्लाई ‘चढ़ जा ऊपर। मैं कहती हूँ जा।’ एक पुलिसवाले को डाँटकर बोलीं, ‘खींच इसे ऊपर। मेरी पोती है। सँभालकर रखना। अभी आकर ले जाऊँगी।’ पुलिसवाले ने मुझे खींच लिया। भीड़ का एक हुजूम पीछे से आया। काकी को बहा ले गया। उनके साथ और भी लोग। देखते-देखते आदमी आदमी के सिर पर तैरने लगे। मैं ऊपर से देख रही थी। चिल्लाई–‘दादी अ अ दादी अ अ!’ मेरी गलाफाड़ आवाज उन तक नहीं पहुँच पाई। और जब मुझे उन तक पहुँचाया गया, उनकी आवाज समाप्त हो गई थी।
मैं दादी का शरीर पकड़ पुकारती रही। एक साधु ने मुझे उठाया–‘बेटी! तुम्हारी दादी अब तुम्हारी पुकार नहीं सुनेगी। स्वर्ग सिधार गईं। अब तुम्हें ही इनका संस्कार करना होगा।’ मैं कुछ नहीं समझी। हमारे साथ आए गाँव के एक बुजुर्ग ने कहा, ‘ऐसा कैसे होगा? यह तो लड़की है।’ साधु मुस्कुरा पड़े–‘क्या फर्क है लड़की लड़का में? यह तो तुम्हारी मुसाफिर काकी थी, क्या नारी नहीं थी? तुम सबको सँभालती थी। है ऐसा कोई मर्द तुम्हारे गाँव में!’
मानो काकी आदेश दे रही हों–‘ये सच्चा साधु है। इसकी बात मान लें।’ गाँववालों ने साधु की बात मानकर मेरे हाथ से ही दादी को मुखाग्नि दिलवाई। साधु-महात्मा, अंधरा परदेश, करकट परदेश-देश के कोने-कोने से आए लोग काकी की अंतिम यात्रा में शरीक हुए। एक गंगा की तरह चलायमान मुसाफिर की यात्रा गंगा किनारे समाप्त हुई।
Image :Old Woman with Distaff
Image Source : WikiArt
Artist : Bartolome Esteban Murillo
Image in Public Domain
Note : This is a Modified version of the Original Arwork