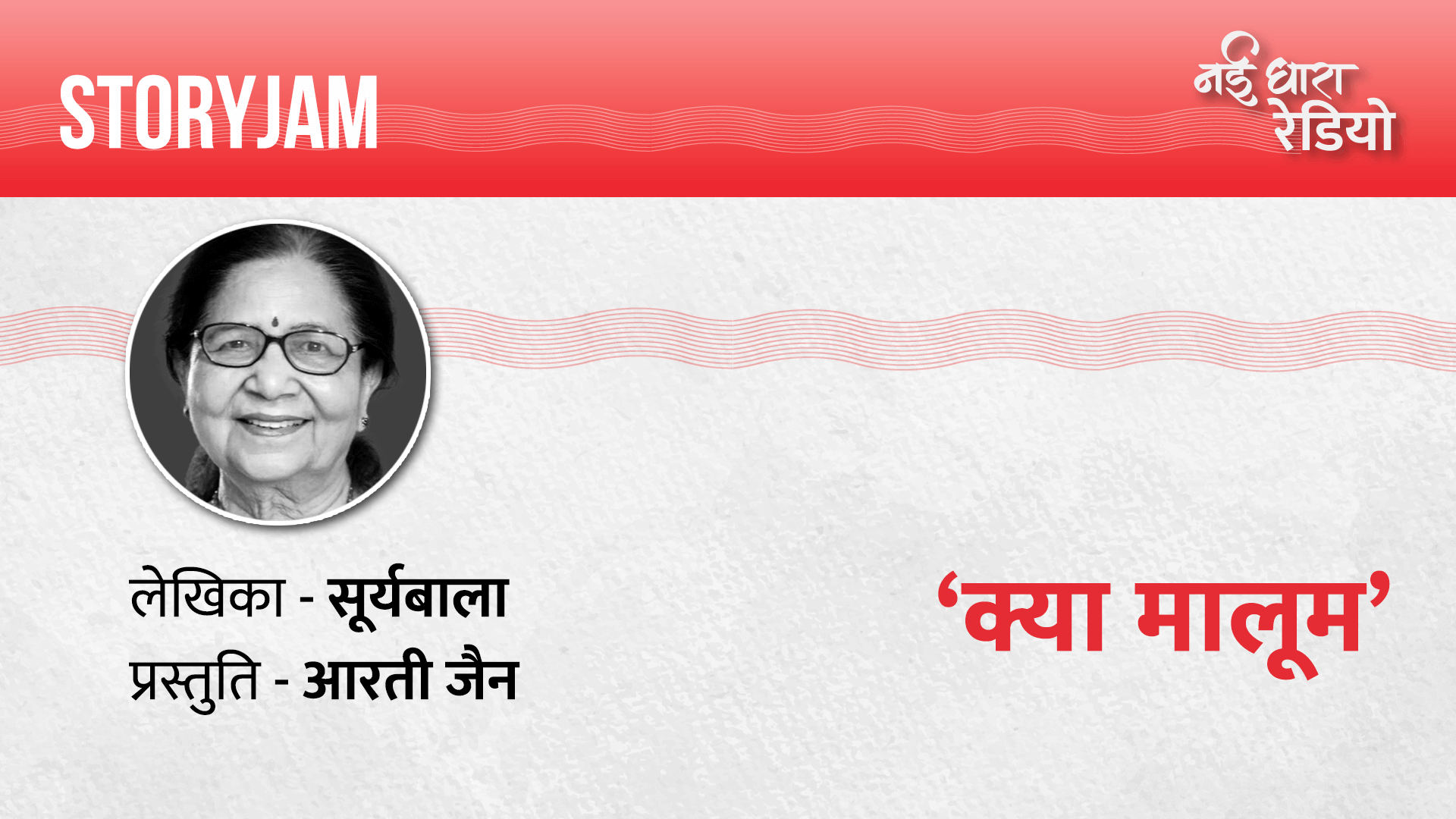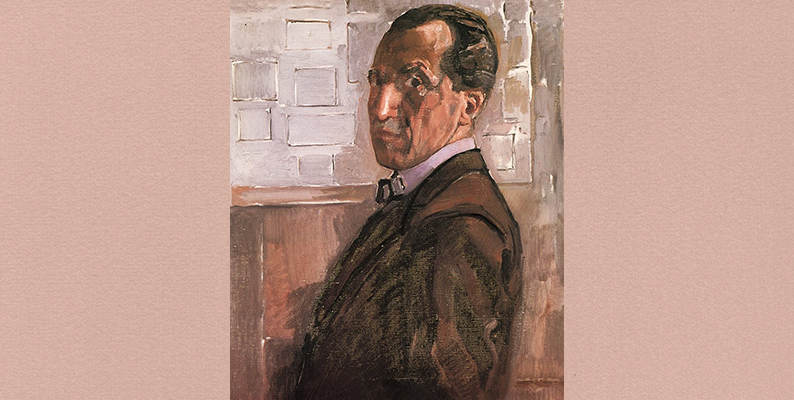स्वप्न, द्वंद्व और उपलब्धियों के बीच स्त्री लेखन की चुनौतियाँ
शेयर करे close
शेयर करे close

शेयर करे close
- 1 June, 2022
स्वप्न, द्वंद्व और उपलब्धियों के बीच स्त्री लेखन की चुनौतियाँ
व्याख्यान
मैं स्त्री-लेखन को पिछली सदी की एक महत्त्वपूर्ण घटना एक उपलब्धि मानती हूँ…जब, सदियों से शिलावत अपने अंदर की अहिल्या को स्त्री ने स्वयं अपनी कमल का स्पर्श देकर जगाया होगा। यों बहुत आकस्मिक भी नहीं कह सकते इसे क्योंकि इसके पहले भी युग, समय के अंतरालों को भेद कर जब-तब गार्गी, सावित्री, अपाला, नटी विनोदिनी, हंसा वाडेकर और रूकैया सखावत हुसैन ने भी स्त्री जीवन की घुटन भरी गुफाओं के बाहर खुली हवा में साँस लेने के रास्ते तलाशने के प्रयास किए थे…किंतु तब उनका वह प्रयास दुःस्साहस का पर्याय मानकर विस्मृत तिरस्कृत कर दिया गया था। अस्तु…
लेकिन पिछली सदी में क्रमशः अस्तित्व में आई स्त्री-लेखन की प्रवाहमान धारा में स्त्री स्वयं अपने अनुभव, अनुभूतियों का प्रामाणिक बयान दर्ज करने के लिए उद्यत थी। अब तक पुरुष (लेखकों) की दृष्टि से देखी और उकेरी जाती स्त्री अब स्वयं, ‘कर्म’ से कर्ता हो रही थी। कथा-लेखन के इस स्वतःस्फूर्त अभियान में स्त्री के वे सारे स्वप्न निहित थे जो उसने अब तक अपने अवचेतन में देखे होंगे और रूढ़ियों की जकड़नों के बीच से मुक्ति की आकांक्षाओं ने साँकले खोलने का उद्यम ठाना होगा। सत्यतः तो युगों से अशिक्षा, अज्ञान और अंधविश्वासों के अँधेरों में घुटती स्त्री को उजाले में लाने का पूरा श्रेय उन महान समाजसेवियों, साहित्यकारों और स्वाधीनता संग्राम से जुड़े देश भक्तों की सदय दृष्टि और जुझारू प्रयत्नों को जाता है, जिन्होंने स्त्री के रास्ते रोशन करने के लिए समाज की घोर प्रतिगामी शक्तियों के विरोध झेले थे। स्त्री-शिक्षा, समाज सुधार और अंध विश्वास के निषेध में उठी उनकी बुलंद आवाजों और अथक प्रयासों ने स्त्री को ऊर्जा और आत्मविश्वास से संतृप्त किया था। इसी का प्रतिफल था कि मुक्तिगामी और विकासोन्मुख ‘समाज की स्त्री’ के साथ साथ, ‘साहित्य की स्त्री’ भी अपनी पगडंडी तलाश रही थी। तभी तो घुटन के बीच जीती स्त्री के मन-जीवन की विडंबना के दस्तावेजी और मार्मिक आख्यान उन दिनों महादेवी की ‘शृंखला की कड़ियाँ’ जैसी कृतियों तथा सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताओं तथा कहानियों में दर्ज होते जा रहे थे।
इन सारे नेपथ्य और भारतीय समाज में आ रहे बदलावों के बीच से हिंदी साहित्य के आकाश में स्त्री-लेखन का एक नया सौर मंडल क्रमशः रोशन होता चला गया था जिसकी प्रस्तावना कृष्णा सोबती, उषा प्रियंवदा और मन्नू भंडारी जैसी लेखिकाओं ने लिखी थी। यहाँ जितने स्वप्न और आकांक्षाएँ थीं उतना ही विस्तृत अंतर्द्वंद्वों का संसार भी था। अब स्त्री के सामने घर के बाहर का खुला संसार, खुली हवाएँ थीं, नई संभावनाओं वाला बदलता समाज था तो उन रास्तों में आई नई द्विधाएँ भी थीं। शिक्षित होती कामकाजी स्त्री के सामने आर्थिक आत्मनिर्भरता का सम्मोहक स्वप्न था तो घर-बाहर की दुहरी जिम्मेदारियों की विडंबना भी। एक तरफ पंख पसारते प्रेम की अनुभूतियाँ थीं, तो दूसरी तरफ अपवाद स्वरूप ही आईं, ‘मित्रो मरजानी’ के रूप में स्त्री की यौनिक इच्छाओं का खुला विस्फोटक स्वीकार भी था। कुल मिलाकर इन तीनों लेखिकाओं के लेखन में स्वातंत्र्योत्तर भारतीय समाज की स्त्री के बाहर और अंदर की सारी उमंग, ऊर्जा, द्वंद्व और टकराहटों का एक भरापूरा संसार उपस्थित था।
बावजूद इसके ‘महिला-लेखन’ शब्द, यह नामकरण, अस्तित्व में तब आया जब सातवें-आठवें दशक में देखते-देखते चार-छह वर्षों के अंतराल पर दर्जन से ऊपर युवा लेखिकाएँ, कथा-लेखन के सदर दरवाजे से अपनी शिनाख्त करवा चुकी थीं, तथा शेष भी करवाती जा रही थीं। धर्मयुग, सारिका, साप्ताहिक हिंदुस्तान, कल्पना, कहानी, ज्ञानोदय, कादम्बिनी सभी प्रमुख पत्रिकाओं में ‘महिला कथा लेखन’ अंकों तथा विशेषांकों की बाढ़ सी आ गई थी। ऊर्जा और उत्साह से भरपूर स्त्री-कथाकारों की यह वेगवती धारा, सारे कथा-आंदोलनों और विचारधारात्मक आग्रहों से अलिप्त अपने अंदर-बाहर का मार्मिक और सीधा सच्चा आख्यान प्रस्तुत कर रही थी। नई कहानी ‘अकहानी’ और तमाम सारी फतवे बाजियों से ऊबा, त्रस्त हिंदी का एक विशाल पाठक वर्ग सोत्साह इस लेखन से जुड़ रहा था, उन्हें सराह रहा था। अपने संपादकों, प्रकाशकों और पाठकों से मिली प्रेरणा, प्रोत्साहन के बल पर दत्तचित्त एक जुनून की तरह कथा लेखन में जुटी इन कलमों ने अपनी तीनों वरिष्ठ लेखिकाओं द्वारा डाली सुदृढ़ नींव पर ‘महिला-लेखन’ की भीत्ति उठायी थीं, मेहराबें काढ़ी थीं, रोशनदान और झरोखे खोले थे। उनके पृथक संस्कारों, संवेदना, अनुभव और शिल्प से सँवारा, एक आंदोलन नहीं बल्कि, एक अभियान की तरह कथालेखन का यह कारवाँ चल पड़ा था।… आज तक चल रहा है।… लेकिन अस्तित्व में आने से लेकर अपने लेखन की प्रतिष्ठापना तक की यह यात्रा आसान नहीं थी महिला लेखन के लिए बल्कि एक तरह की ‘ऑब्सटेक्ल रेस’ थी। लेखिकाओं के जीवट और जिजीविषा का प्रामाणिक दस्तावेज थी उनकी रचनाधर्मिता। जीवन में भी और लेखन में भी दुहरे अस्तित्व संघर्ष की चुनौतियों के बीच लिख रही थीं ये लेखिकाएँ।
लोकप्रियता मिलते जाने के साथ ही महिला लेखन पर स्वभावतः आरोप लगने भी प्रारंभ हो गए थे। लोकप्रियता वैसे भी हिंदी में किसी रचनाकार को एक विडंबना की तरह ही मिलती है। अतः लोकप्रिय मानकर स्त्री के लिखे को कहीं उपेक्षित किया गया तो कहीं सीमित, दृष्टि और घरबारी अनुभवों का आख्यान माना गया। संपन्न घर की, सुशिक्षित महिलाओं का शगल और ‘टाइम-पास’ तक मान लिए गए इस लेखन से आलोचक, समीक्षक और मठाधीशी दृष्टियाँ यथा संभव कतराकर निकलने का रास्ता तलाशती रहती थीं। उन दशकों में महिला-लेखन शब्द से स्वयं लेखिकाओं द्वारा ही आपत्तियाँ उठाने का एक प्रमुख कारण यह भी था कि इस नामकरण से ‘दोयम दर्जे’ के लेखन के ध्वन्यार्थ निकलते थे, जो सच नहीं थे। सच तो यह है कि उत्कृष्ट, सामान्य और अति सामान्य लेखन हर युग, समय में होते ही रहते हैं।
महत्त्वपूर्ण यह भी कि विवादों और स्पष्टीकरणों में न उलझते हुए इन सारे आरोपों-प्रत्यारोपों का प्रत्युत्तर स्त्री रचनात्मकता की उत्तरोत्तर उत्कृष्टतर और वैविध्यपूर्ण होती जा रही कृतियों और रचनाओं ने दिया। क्रमशः गतिशील अंतिम दशक तक आते-आते स्त्री-कथाकारों की ‘वापसी’, ‘यही सच है’, ‘लपटें’, ‘प्रेत’, ‘बाऊजी और बंदर’, ‘सुनंदा छोकरी की डायरी’, ‘हरी बिंदी’, ‘सुलेमान’, ‘पानी की दीवार’, ‘दूबधान’, ‘तीसरी हथेली’ की कहानियों से लेकर औपन्यासिक कृतियों तक, कथ्य एवं शिल्प के स्तर पर वैविध्य, गहराई, विचार और संवेदना के नए कीर्तिमान गढ़े। स्त्री-मन के अदृश्य प्रकोष्ठों से लेकर सांस्कृतिक अवमूल्यन तक से उपजे मोहभंगों को समेटने वाली ये कृतियाँ, हिंदी की महती उपलब्धि प्रमाणित हुई। अगले, पिछले दशकों को मिलाकर तब तक ‘आपका बंटी’, ‘महाभोज’, ‘पचपच खंभे…’, ‘रुकोगी नहीं राधिका’, ‘आदमीनामा’ से लेकर ‘अनित्य’, ‘कठगुलाब’, ‘आँवाँ’, ‘गिलिगडु, ‘इदन्नमम’, ‘बेघर’, ‘सुक्खम्-दुख्खम’, ‘यामिनी कथा’, ‘मेरे संधिपत्र’, ‘पाषण युग’, ‘कथा सतीसर’, ‘ऐलान गली जिंदा है’, ‘तत्सम’, ‘जिंदा मुहावरे’, ‘शाल्मली’, ‘सिरजनहार’, ‘भामती’, ‘पंचवटी’, ‘पीली आँधी’, ‘पटरंग पुरपुराण’ जैसी कृतियाँ पर्याप्त चर्चित हो चुकी थीं।
उल्लेखनीय यह भी कि लगभग सारी प्रमुख लेखिकाओं के कथ्य और शिल्प में विस्मयकारी अंतर था। राजी सेठ से लेकर, ममता कालिया, चित्रा मुद्गल, उषा किरण खान, मैत्रेयी पुष्पा, मृदुला गर्ग, सुधा अरोड़ा, चंद्रकांता और इन पंक्तियों की लेखिका तक किसी की भी कुछेक पंक्तियाँ पढ़ने के साथ ही बेहद सहजता से पहचानी जा सकती हैं कि यह किस लेखिका की रचना है। कहीं संवेदना की अतल गहराई है, कहीं वैचारिक स्तर पर गहन विश्लेषण, कहीं मोहभंग की दो टूक सच्चाइयाँ, तो कहीं अवसाद की घनीभूत छाया।… इतना ही क्यों, कहीं खनकदार चुटकियों में समेटी जाती स्त्री जीवन की विडंबना, कहीं विचार और संवेदना की थिराती सतहें और कहीं स्त्री-स्वातंत्र्य की दो टूक ऐलानियाँ जंग भी। कहीं ग्राम्यांचल से गाँव-जवार तक धूल झाड़कर खड़ी चैतन्य होती स्त्री है तो कहीं इतिहास के तथ्यों के बीच से उकेरे जाते उसके जीवन के मार्मिक सच।
संभवतः उन्हीं दशकों में खुली अर्थव्यवस्था और वैश्विक सौंदर्य प्रतिस्पर्द्धाओं वाले समाज के समानांतर, साहित्य में भी बाजारवादी शक्तियाँ अपनी पैठ बना रही थीं। आठवें-नौवें दशक से ही कथा लेखन की पुरुषवर्चस्वी ताकतों ने बड़ी गुरूगंभीर, अतिबौद्धिक और अत्याधुनिक मुद्रा में स्त्री रचनाधर्मिता को ‘लेखकीय प्रतिबद्धता’, ‘पारदर्शिता’ और ‘अनुभूति’ की प्रामाणिकता वाले नये शब्दकोश को नये सिरे से परिचित कराना प्रारंभ किया। समाज की स्त्री और कथालेखन में प्रवृत्त स्त्री अर्थात लेखिकाओं का सच्चा हितैषी और संरक्षक होने का दावा करने वाली इन शक्तियों ने बड़े सम्मोहक अंदाज में ‘स्त्री-विमर्श’ का नारा बुलंद करते हुए ‘दृढ़ और निर्भीक’ जैसे शब्दों की आड़ में ‘दुःसाहसी’ और ‘बोल्ड’ लेखन की ओर प्रेरित, प्रोत्साहित किया तथा स्त्री मात्र की मुक्ति को क्रमशः देहमुक्ति से जोड़ते हुए यौनिक स्वच्छंदतावाद की ओर उकसाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी।
अपनी ही कुछ पुरानी पंक्तियाँ कोट करूँ तो ‘बोल्ड और दुस्साहसिक लेखन के लिए रातों-रात चर्चा और सुर्खियों की ऐसी रेड-कारपेट बिछा दी जाती है कि नए ही नहीं पुरानों के भी भटक जाने की पूरी गुंजाइश बनी रहती हैं।’ कुल मिलाकर स्त्री-लेखन को बरगलाने वाली साजिशें पूरी जमात पर अमादा थीं।
बेशक अधिकांश वरिष्ठ और परिपक्व कलमें, इस प्रवृत्ति बनाम साजिश की भर्त्सना और विरोध करते हुए अपने रचनात्मक विवेक पर टिकी रहीं…लेकिन ‘लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई’ वाली पंक्तियाँ चरितार्थ होनी ही थीं। ‘ब्रेनवाश’ इतना असरदार था कि साहित्य का बाजार उन दशकों की कई आत्मकथाओं सहित, विमर्शी और फार्मूलाबद्ध लेखन से पटता चला गया। गनीमत यही थी कि खोटे सिक्के, खरे सिक्कों को बाजार के बाहर नहीं कर पाए। फलत:, एक साथ, लेखिकाओं की तीन पीढ़ियों से छन कर आते उत्कृष्ट, उत्तरदायी और वैविध्य स्त्री-लेखन की यात्रा सतत् गतिमान है।
रचनाधर्मिता की यह युवा पौध आत्मविश्वस्त होने के साथ-साथ आसन्न खतरों से खबरदार भी है। लेखन की बढ़ी हुई चुनौतियों से वे अवगत नहीं, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता लेकिन विचलन की संभावनाओं से इनकार भी नहीं किया जा सकता जिसके मूल में वे ही अति बौद्धिक (तथाकथित) फतवेबाजियाँ हैं जो स्त्री-लेखन के बाजार को क्रमशः एक बड़े शॉपिंग मॉल में बदल देना चाहती हैं…जबकि सभ्यता के और-और दुर्दांत होते जा रहे इस समय में, स्त्री-लेखन को मनुष्य के मूलभूत जीवन-मूल्यों को पुनः प्रतिष्ठित करने की पहल करनी है। छितरते, विछिन्न होते मानवीय संबंधों को विनष्ट होने से बचाना है; क्योंकि हवाओं के रूख का कोई ठिकाना नहीं। वह कभी भी यह ट्रेंड बरपाते हुए निकल जाता है कि भाषा से लेकर शिल्प कौशल तक में कुछ अश्लील होता ही नहीं, हो सकता ही नहीं…अश्लील तो दृष्टा की दृष्टि होती है। प्रलोभन की यह हरी झंडी अनजाने, अनायास, ऐसे लेखन की प्रेरणा बनती है जिसकी गलियों से सिर नीचा करके चलने के सिवा और कोई उपाय नजर नहीं आता। मैं गलत हो सकती हूँ, और अपनी बात मनवाने के लिए जरा भी जोर न देते हुए हमेशा से अपनी यह बात दुहराती आई हूँ कि कालजयी लेखन कभी भी ‘बोल्ड’ और ‘दुस्साहसी’ शब्दों का मुहताज नहीं हुआ करता। दुर्भाग्यपूर्ण सिर्फ यह है कि ‘अश्लील’ को न प्रमाणित किया जा सकता है, न परिभाषित, सिर्फ महसूस किया जा सकता है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन प्रतिगामी ताकतों के सामने रचनाकार का विवेक ही उसे सँभाल सकता है। वरना ‘निःशुल्क प्रवेश’ की तख्ती वाला यह रास्ता सीधे यौनिक स्वच्छंदतावाद और पोर्न चित्रणों के ऊपर बड़ी अजीजी से ‘प्रतिबद्ध’ और ‘प्रामाणिक लेखन’ का टैग लगा पीठ थपथपा देता है।
मैं पुनः गलत हो सकती हूँ पर मेरा यह भी मानना है कि ‘विषय’ अथवा ‘कथ्य’ कोई भी अश्लील नहीं हुआ करता, ‘शृंगार’ से सेक्स तक…अश्लील उन्हें अभिव्यक्त करने का तरीका हुआ करता है। और ‘सब कुछ’ का स्थूल, विस्तृत बयान, मेरी दृष्टि में, कहीं-न-कहीं रचनाकार की अक्षमता का प्रतीक होता है। प्रायः अन्य देशी-विदेशी भाषाओं, विशेषकर अँग्रेजी का उदाहरण देकर समझा दिया जाने वाला यह तर्क भी मेरी अल्पबुद्धि से ऊपर है कि यदि अन्य भाषाओं में खुलेपन का यह ट्रेंड चल रहा है तो हिंदी में क्यों नहीं चल सकता। यहाँ फिर मेरा मानना है कि बहुत से ऐसे टर्म्स मुहावरे हैं जो इंगलिश के सभ्य समाज और साहित्य में धड़ल्ले से उपयोग किए जाते हैं, लेकिन भारतीय सभ्य समाज में नहीं…फिर साहित्य में उसे लाने का हठ क्यों? हर भाषा की प्रकृति दूसरी से भिन्न होती है। वर्जित शब्दों के उपयोग की रीति और शर्तें भी भिन्न…ऐसे में लेखक के रचनात्मक विवेक पर इस तरह के दबाव डालने की कोशिश क्या ज्यादती नहीं?
स्त्री-रचनाशीलता के लिए आज पहली चुनौती यही है कि वह ‘विमर्शी जिन्न’ के ‘आफ्टर-इफेक्ट’, हैंगोवर से बची रहे। इस तरह के फार्मूलों और दबावों ने स्त्री-लेखन की संभावनाओं को सीमित किया है और उसकी गहराई तथा विस्तार को बाधित। इन दबावों का ही परिणाम था कि एक समय में ‘चैतन्य’, ‘समर्थ स्त्री’ का वह नया नकोर मॉडल बेहद लोकप्रिय होता चला गया, जिसमें कहानी या उपन्यास की स्त्री को तो ‘आक्रामक’, ‘मुखर’ और ‘विद्रोही’ होना ही है अन्यथा वह चेतना संपन्न और समर्थ स्त्री कैसी? यथास्थिति से विद्रोह और बगावत ही स्त्री का सर्वोपरि गुण माना जाने लगा। ‘परिपक्वता’ शब्द ‘रूढ़ और दकियानुसी’ का जुड़वा हो बैठा। निश्चित रूप से जहाँ कुछ कहानियाँ, औपन्यासिक कृतियाँ तदरूप कथा वस्तु और घटनाक्रम की वजह से ऐसे स्त्री चरित्रों के साथ प्राय: न्याय संगत सिद्ध हुए वहीं भिन्न कथा वस्तु और अतिसंवेदनशील स्थितियों में भी विचार और विवेक से पहले, विद्रोह और विरोध का पल्ला थामकर अपनी जीत का ऐलान करने वाली समर्थ और आक्रमक स्त्री चरित्रों की बाढ़ सी आ गई। यह समझने में भी वक्त लगना ही था कि प्रायः कागज पर लड़ी जाने वाली लड़ाइयाँ और विद्रोह जीवन में यथा रूप नहीं उतारे जा सकते।
कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना कि जब तक रची जाती कहानियाँ, कृतियों पर विमर्श हो रहे हों, तब तक ठीक लेकिन जब विमर्शों को ही ध्यान में रखकर कहानियाँ लिखी जाने लगे तो साहित्य की विश्वसनीयता खंडित हो, संदेह के घेरे में आ जाती हैं।
अतः नयी स्त्री-रचनाशीलता के लिए यह समझना भी आवश्यक है कि उसके लिए ‘स्त्री-मानस’ की बहुत सारी गहराइयाँ थहाना अभी शेष है। हमें इन अदेखे प्रकोष्ठों की शोध करनी होगी। अब तक के अपने बनाए, इस्तेमाल में आ चुके साँचों को स्वयं तोड़ना होगा। अपने लिखे के प्रतिपक्ष को भी प्राथमिकता देनी होगी।…
स्त्री जितना दिखती है, सिर्फ उतनी भर नहीं होती…मनसा, वाचा, कर्मणा, अपनी सारी क्रिया-प्रतिक्रियाओं के बावजूद हर स्त्री दूसरी से अलग भिन्न होती है। उसकी समस्या और उद्विग्नताओं को स्त्री मात्र की समस्या या स्थिति मानकर एक सी पर्ची नहीं काटी जा सकती, न एक से निदान ही सुझाए जा सकते हैं। साहित्य और समाज में भी चल रहे सारे कागजी नारों, सिद्धांतवादी और विमर्शों से अलग नई कलमों को वह स्त्री उकेरनी होगी जो अपने ऊपर हुए सारे नये-पुराने प्रयोगों के बीचों-बीच विमूढ़ सी खड़ी है…चौराहे पर लगी अतिबौद्धिक तख्तियाँ ‘शर्तिया इलाज’ के तौर पर व्यक्ति सत्ता को पोसने वाले अति आधुनिक और उत्तर आधुनिक टॉनिक प्रेस्क्राइब कर रही होगीं, लेकिन स्त्री को सोचना होगा कि पुराना सब कुछ त्याज्य नहीं होता और न नया सब कुछ ग्राह्य। स्त्री के अंदर अपने जीवन को बरत पाने का वह विवेक हो कि कहाँ पूर्वाग्रह मुक्त होकर परंपरा से जुड़ना है और कहाँ खुले दिल-दिमाग से आधुनिकता को अपनाना है। स्त्री को बेशक अपनी व्यक्ति सत्ता और ‘स्पेस’ के दावों के साथ खड़े रहना है, लेकिन उसकी सीमाएँ भी समझनी हैं तथा स्व-अस्तित्व के साथ सह-अस्तित्व के सामंजस्य और समरसता की शर्तों और महत्त्व को भी स्वीकारती हों। वह गलत का विरोध करने के लिए सदैव प्रस्तुत हो, और हर अन्याय शोषण के खिलाफ विद्रोह की समझ और सामर्थ्य भी रखती हो, लेकिन विरोध और विद्रोह तब और कैसे किया जाए इसकी तरकीब और युक्ति भी जानती हों।
जीवन की जटिलताओं के बीच कभी-कभी तो स्थितियाँ ऐसी भी आती हैं जब गलत और अन्याय करने वाले को इसका अहसास तक नहीं होता। ऐसी भूलें, मानसिक तथा भावनात्मक हिंसा, जाने कितनी शक्लों में आती हैं और प्रायः शारीरिक हिंसा से ज्यादा मर्मातंक सिद्ध होती हैं। इन सारी स्थितियों से निपटने के लिए जो रास्ते तलाशे गए, जो निदान बताए गए, वहाँ पहुँचकर भी स्त्री ने महसूस किया कि उसकी तलाश पूरी नहीं हुई, प्रयोग सही साबित नहीं हुए…तो!… हथियार डालने तो नहीं हैं, लेकिन बदलने की बात तो सोची ही जा सकती है। हताशा, अनास्था अथवा आक्रामकता, विखंडन और बिखराव भी, अंततः स्त्री को छूछा ही छोड़ने वाले हैं। तो कुछ प्रयोग जीवन और संबंधों को जोड़ने की दिशा में भी क्यों न करके देख लिए जाएँ। आखिर जीवन एक प्रयोगशाला ही तो है, विशेषकर स्त्री का जिसमें उम्र भर उसके प्रयोगों का सिलसिला चलता ही रहता है।
ऐसा मैं इसलिए भी कह रही हूँ, क्योंकि आज की नई पीढ़ी प्रायः ‘विचार’ और ‘धैर्य’ को सिरे से नकारने सी लगी है। उसके लिए त्वरित निर्णय और ‘उसका ही’ निर्णय, सर्वोपरि होता है…भले ही इसकी परिणति उसे टूटकर किरचों में बिखरा ही क्यों न दे…तब भी अपने ‘इगो’ को स्वाभिमान समझने की गलती वह बार-बार दुहराती रहती है। समाजशास्त्र और मनोविज्ञान में घुसपैठ सिर्फ इसलिए करनी पड़ी क्योंकि स्त्री-लेखन की जिम्मेदारियाँ आज बहुत बढ़ गई विशेषकर मेरी नज़र में। इसलिए भी क्योंकि मैं स्त्री को बहुत ऊँचा करके आँकती हूँ, और उससे बहुत सारी अपेक्षाएँ लगा बैठती हूँ। ये अपेक्षाएँ भी स्त्री के साथ-साथ विश्व समाज से जुड़ी होती हैं। सैकड़ों बार की दुहारायी अपनी बात आज फिर दुहराऊँगी कि इस समय को, इस अंधेमोड़ तक लाने के लिए बेशक स्त्री जरा भी जिम्मेदार नहीं है, लेकिन अपने चारों तरफ की दुनिया से लेकर इस विश्व को वापस सुंदर और बेहतर बनाने का कौशल सिर्फ स्त्री के पास है। बशर्ते वह अपनी सही सामर्थ्य और चेतना का अहसास और इस्तेमाल करना जानती हो।…
स्त्री-लेखन को अपने अनुभव, अनुभूतियों और स्मृतिकोषों के बीच से ‘वह स्त्री’ उकेरनी है जिसे अपने ‘स्त्री’ होने पर गर्व हो, जो अपनी प्रकृतिप्रदत्त, बुद्धिमत्ता चातुर्य और प्रबंधन-क्षमता से समृद्ध स्त्रीत्व को लेकर आत्मविश्वस्त हो। जो मोहबंधों, रिश्तों को हमारे जीवन का अपरिहार्य पाथेय मानती हो और सारी टूटन, बिखराव और विशृंखलताओं के ऊपर सेतुबंध के लिए सत्त तत्पर हों।
ये सब कहने का मेरा आशय सिर्फ इतना है कि पिछले बीस वर्षों में मैंने विश्व के सर्वाधिक विकसित और समृद्ध देशों के समाज, परिवार, रिश्तों और स्त्री को बहुत निकट से देखा है। दो वर्षों पूर्व आए मेरे उपन्यास, ‘कौन देस को वासी : वेणु की डायरी’ का तो केंद्र-कथ्य ही यही है कि अति आधुनिकता के सारे प्रयोग जो वहाँ पिटकर असफल सिद्ध हो चुके हैं उसकी परिणतियाँ देखने के बाद भी हम चेतते क्यों नहीं? सुबह का भूला शाम को घर वापसी के बारे में क्यों न सोचे। उन अतिआधुनिक समाजों की हताशा, अनास्था और संबंधों के बीच पनपे भयानक अविश्वास हमें सहमाते हैं। उनके बीच टूटती स्त्री तथा माता-पिता के अलगावों के फलस्वरूप टूटन, अकेलेपन और विक्षिप्तता के शिकार बच्चे, हमारी चिंताओं के मूल में होने चाहिए। अतः हम वहाँ के वर्तमान को अपने समाज का वर्तमान होने से बचाएँ। स्थिति की भयावहता समझते हुए भी विश्वसमाज के अन्यान्य क्षेत्र जुटमिल कर वह सब नहीं कर पा रहे…तो कम-से-कम साहित्य ही वह पहल करें…कथा-साहित्य और स्त्री-कथा लेखन…मैंने इधर युवा और नई लेखिकाओं को काफी पढ़ा है। उनकी गहरी संवेदना, ज्ञान और अनुभव, शिल्प को महसूसा है, रचनात्मक पूँजी का कारून का खजाना उनके पास है। सिर्फ किस दिशा में उनका इस्तेमाल करना है, इसका एक संकेत भर करना मैंने अपना धर्म समझा–अस्तु!
अंत में, मुझे यह समय, यह अवसर देने के लिए आप सब का, समूचे ‘नई धारा’ संस्थान तथा उनके सहयोगियों का हृदय से धन्यवाद।… छोटे मुँह कोई बड़ी बात निकल गई हो तो उसके लिए बार-बार क्षमा भी…वस्तुतः जो कुछ कहा, वह मेरी दुःखती रग, दुःखता मन था जो बार-बार मेरी रचनाओं में भी छन कर, उतर कर आता ही रहता है।
(‘नई धारा’ द्वारा 1 दिसंबर, 2021 को पटना के उदय राज जन्मशती महोत्सव में दिया गया 16वाँ उदय राज सिंह स्मारक व्याख्यान।)
Image : Portrait of a Young Woman
Image Source : WikiArt
Artist : Mary Cassatt
Image in Public Domain