बेघर होने की त्रासदी : ‘डार से बिछुड़ी’
- 1 April, 2015
शेयर करे close
शेयर करे close
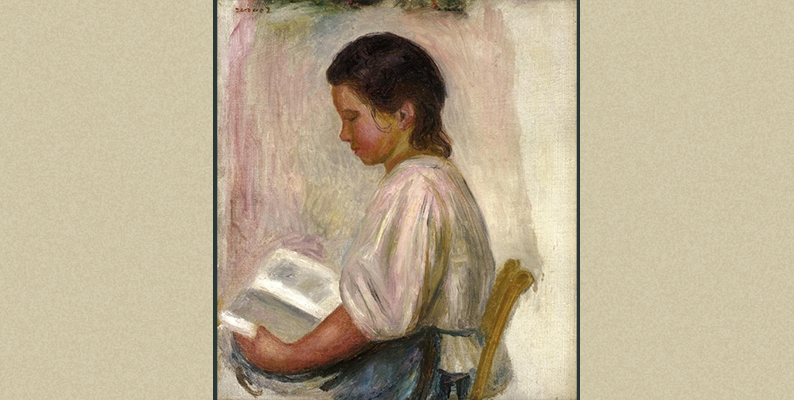
शेयर करे close
- 1 April, 2015
बेघर होने की त्रासदी : ‘डार से बिछुड़ी’
कृष्णा सोबती के कथा-साहित्य की यात्रा शुरू होती है–‘डार से बिछुड़ी’ से। यह उपन्यास सन् 1958 में ही प्रकाशित हो चुका था। प्रथम रचना के प्रकाशन के साथ ही कृष्णा सोबती के हिस्से ख्याति आ लगी थी, क्योंकि प्रकाशन के साथ ही ‘डार से बिछुड़ी’ ने अपने नए तरो ताजापन से हिंदी पाठकों को चौंका दिया था। परंपरागत शैली से हटकर कथ्य की अलग बुनावट ने पाठक वर्ग पर अपना प्रभाव डाला। इसलिए ‘डार से बिछुड़ी’ के प्रकाशन के साथ ही उनकी रचनाओं पर नजर रखी जाने लगी। बहुत कम ऐसे लेखक होते हैं, जिनकी पहली रचना के साथ ख्याति उनके खाते में दर्ज हो जाती है। कथाकार कृष्णा सोबती ऐसे ही लेखकों में शुमार हैं, जिनकी गिनी-चुनी रचनाओं ने ही उन्हें प्रशंसाएँ और प्रसिद्धियाँ दिलाईं और उनकी रचनाएँ लीक से हटकर मानी जाने लगीं। गौरतलब है कि ‘सिक्का बदल गया’ कहानी के आने के बाद ही कृष्णा सोबती कथा लेखिका के रूप में चर्चित हो चुकी थी।
‘डार से बिछुड़ी’ कहानी ‘निकष’ पत्रिका में विशेष कृति के रूप में सबसे पहले प्रकाशित हुई थी, जिसके संपादक धर्मवीर भारती थे। संपादक महोदय ने शब्दों के साथ छेड़छाड़ किये बगैर इसे ज्यों-का-त्यों छापा था। ‘शब्दों के आलोक’ अपनी पुस्तक में कृष्णा सोबती लिखती हैं, ‘निकष में अपनी लंबी कहानी ‘डार से बिछुड़ी’ के संपादक के रूप में भारती मेरे उस रचनात्मक समय के लिए महत्त्वपूर्ण थे, ‘डार से बिछुड़ी’ को विशेष कृति के रूप में प्रकाशित करना मुझे अपनी पंक्तियों के प्रति एक सादा, सच्चा आत्मविश्वास मिलना था। ‘डार से बिछुड़ी’ उपन्यास में सुदूर उत्तर-पश्चिम के सीमा-प्रांत की अपरिचित लेकिन अति परिचित लगनेवाली जिंदगी को गूँथा गया है। कृष्णा सोबती विभाजनकालीन दौर की जीवंत साक्षी रही हैं। उस दौर को करीब से देखा, समझा और महसूस किया था। इससे पहले की बहुत-सी घटनाएँ उन्होंने देख, सुन रखी थीं, जिसमें से एक सिक्ख और फिरंगियों के युद्ध की घटना थी, ‘सिक्ख और फिरंगी युद्ध की जाने कितनी कहानियाँ हमने सुन रखी थी।’ गुजरात के चिल्लियाँ वाले मैदान में सिक्ख और फिरंगियों के बीच जो घमासान युद्ध हुआ था, जिसमें फिरंगियों की पूरी तरह से विजय हुई थी, उसी ऐतिहासिक वृत्तांत को कथा की पृष्ठभूमि में गूँथा गया है।
उपन्यास की नायिका पाशो खत्री परिवार की बेटी है। इसकी नायिका पाशो अपनी नानी-मामी के साथ रहती है। खत्रियों के परिवार की पाशो जब बड़ी हुई तो खोजो के घर पटरानी बन बैठने वाली माँ की लांछना सर पर थी। इसलिए पाशो को लेकर नानी, मामा और मामियों की अतिरिक्त सजगता और सावधानियाँ थीं। उसे न तो माँ का प्यार मिला, न उनके संरक्षण में पली-बढ़ी, न शिक्षा थी, न विद्या, न पिता की छाँह, न कोई सहेली संगी। माता-पिता के स्नेह से वंचित नानी, मामा-मामियों के लाड़-प्यार के बीच पली-बढ़ी। जैसे-जैसे वह बड़ी हुई उस पर पहरा उतना ही सख्त हुआ। उसके आने-जाने का हिसाब रखा जाता, तनिक-सी देर हुई नहीं कि माहौल में घबराहट आ घुलती, डाँट-फटकार, गाली-गलौज, कुटना-पीटना तो रोज का काम था। उसके साज-धाज, पहनाव-ओढ़ाव पर सबकी कड़वी निगाहें जमीं रहतीं। गले तक दुपट्टे को देख निगाहें गढ़ जाती–पीढ़ी ले बर्तन-भांडे में लगती तो मामियों की आवाज गूँजती। ‘नखरे तो देखो लाडो के पीढ़ी ले भांडे मलने बैठी है! अरी बुरों की, पीढ़ी पर बैठती है, भले घर की बहू-बेटियाँ…!’ वह घरवालों के लिए कुलबोरनी, नासहोनी, अभागिनी बन गयी थी क्योंकि खत्रियों की बेटी और पाशो की विधवा माँ अपने परिवार की मान-मर्यादा को मिट्टी के झोंक-शेखों के घर की पटरानी बन बैठी तो उस माँ की जाया घरवालों को कैसे सुहाती। रोक-टोक, ताने-उल्हाने रोज-रोज घुट्टी की तरह जबरर्दस्ती इसलिए डाले जाते ताकि पाशो भी अपनी माँ की राह न चल निकले। नानी उसे कहती है, ‘इस मुँह उसका नाम न लूँ बिटिया। उसी की करनी तुझे भरनी थी। तेरे दोनों मामू उसे कितना मानते थे, यह लोक-जहान जानता है, पर वह नासहोनी तो घर-भर का मुँह काला कर गयी।’ माँ के कारण ही मामा-मामियों के परिवार में उसे काफी तकलीफ दिया जाता था। नानी-मामियाँ उसे शक की दृष्टि से देखते थे, उसे करमजली कहकर पुकराते। उसके रहन-सहन पर नजर रखी जाती थी।
नन्ही-सी पाशो को चारों ओर से फटकार ही फटकार मिलता रहता। परिवार में उसकी स्थिति नौकरानी और बेजुबान गाय से अधिक नहीं थी। हर समय पहरेदारी के बीच उसे रहना पड़ता, उसके पहनाव-ओढ़ाव पर सबकी आँखें लगी रहती हैं–‘आग लगे तेरी जवानी को! रांबयां, खेल इसका फुनगियोंवाला परांदा…’ उसका एकमात्र यही दोष था कि उसकी माँ इस छोटी-सी बच्ची को छोड़कर शेख जाति के एक सज्जन के साथ भाग गयी थी। माँ के इस कुकर्म से समूचे क्षत्रिय कुल पर जो कलंक लगा, उसी का फल पाशो को भी भोगना पड़ा। रोज-रोज के उलाहने और फब्तियों से पाशो का जी छल्ली होता रहा। एक दिन पड़ोस का एक लड़का करीमू के हाथ में पाशो की चमकी का रुमाल देखकर बड़े मामू ने लड़की की खूब पिटाई की और उसे मौहरा (जहर) देने की साजिशें होने लगी। पाशो को इसकी भनक लग चुकी थी और वह रातोंरात कोठों के रास्ते शेख जी के घर जा पहुँची। मामू के झगड़े के डर से शेख ने उसे अपनी उम्र के दोस्त दीवान जी के घर भेज दिया और वहाँ दीवान जी के घर में उसका खूब स्वागत होता और वह दीवान जी के घर दीवान जी बनकर रहने लगी। लेकिन दीवान जी की मौत के बाद स्थिति एक वस्तु से अधिक कुछ न थी। दीवान जी के बाद बरकते (दूर का रिश्तेदार में भाई) के लिए वह मनोरंजन के सिवा कुछ न थी। बरकते की माँ कहती है–‘पली-पलाई है री मालन बेटे को खुश करना सीख।’
भारतीय समाज व्यवस्था में विधवा स्त्री की स्थिति एक वस्तु से अधिक कुछ नहीं रही। उसका जीवन अभिशप्त बन रहता है। पाशो के विधवा होने पर उसके जीवन की त्रासदी की शुरुआत होती है। दीवान जी के जाने के बाद दीवान जी के छोटे भाई ने उसे अपनी संपत्ति समझ अपने लिए रख लिया। ‘तेरा तो नाम-चाम सब मेरा है री पगली! और हाथ बढ़ा मेरा पल्ला खींच लिया, तो भी न काँपी, न चिल्लाई। ऐसे पड़ी रही कि पानी की मार से गली-गलाई काठ होऊँ।’
‘पड़ी रही…पड़ी रही…पड़ी रही…। उठी नहीं?’
विधवा स्त्री की दुर्दशा और बेवशी को पाशो के माध्यम से कृष्णा सोबती ने स्पष्ट किया है। आज भी पितृ सामाजिक व्यवस्था में विधवा स्त्री सुरक्षित नहीं है। बरकत जैसे बहुतों के लिए वह वस्तु से अधिक कुछ नहीं है। लेकिन इतने से ही पाशो के जीवन का अभिशाप कहाँ खत्म होने वाला था। बरकत दीवान अपने ऋण को चुकाने के लिए उसे एक बूढ़े के हाथ बेंच देता है। डोली वालों की हाँक पर घर के धनी बाहर निकल आये, रुक्का पढ़ थलथली आजाज में बोले–‘अच्छा-अच्छा सो भला…! शुकर है बरकत दीवान ने मेरा ऋण तो चुकाया!’
फिर पाशो के घूँघट पर आँखें गड़ा कहा–‘भागभरी, यह घर-बाहर सँभाल और द्रोपदी बनकर सेवा कर मेरी और मेरे बेटों की। द्रोपदी, खैर मना इस अच्छे घर पहुँच गयी, नहीं तो बरकत कसाई एक बार नहीं, सौ बार तुम्हें बेच खाता।’ बूढ़े पर पाशो की विनती का कोई असर नहीं होता, ‘भागभरी, गहरी बात कहता हूँ। सीधी राह चलेगी। भला! तीन-तीन पहरू हैं घर में, भूलकर भी ड्योढ़ी से बाहर पाँव न रखना! समझ रख बीवी, बरकते को घड़ा भर मोहरे दी है, तू अब इस घर की दात्त!’ पाशो इसे अपनी नियति मान लाला के घर को सँभालने में लग जाती है। महाभारत में द्रौपदी को एक ‘वस्तु’ मानकर ही दाँव पर लगा दिया गया था और चौपड़ में पांडव बाजी हार जाते हैं, द्रौपदी अपमानित होती है, पूरी स्त्री जाति अपमानित होती है। आज भी वह मानसिकता नहीं बदली है। ‘द्रौपदी’ का अर्थ ही आज क्रय-विक्रय के रूप में लगाया जाता है। चूँकि लाला ने पाशो को एक घड़े मोहरे के बदले खरीदा और बरकते ने उसे ‘वस्तु’ समझकर अपना ऋण चुकाने का बेहतर माध्यम समझा। इसलिए वह भी द्रौपदी बन गयी और इसलिए लाल उसे ‘द्रौपदी’ कहता है। लाल के बेटे भी उसे अपनी सुविधानुसार इस्तेमाल करते हैं। लाल का छोटा बेटा कहता है, ‘मँझले की नवेली, मेरे संग एक बार लश्कर तो चलो, इस कटोरी आँखों पर बड़े-बड़े सरदारों की नजर न ठहर जाए तो कहना।’
पाशो अपने एक गलत निर्णय के कारण एक के बाद एक भंवर में फँसती जाती है। यह रचना आज से साठ वर्ष पहले लिखी गयी, लेकिन तब से लेकर आज तक स्त्री का मूल्य पुरुष समाज के लिए एक वस्तु से अधिक कुछ नहीं है। वह आज न तो घर में सुरक्षित है न घर के बाहर। दीवान जी की मृत्यु के बाद पाशो के लिए उसका अपना घर ही उसके लिए असुरक्षित होता जाता। मनुसंहिता के अनुसार स्त्री परिवार के बीच सुरक्षित रह सकती है। कुँवारेपन में पिता और भाई के संरक्षण में, विवाहोपरांत पति के घर में। लेकिन जब परिवार ही उसके लिए असुरक्षा का घेरा बन जाए, तब स्त्री के लिए दूसरा उपाय क्या है! घर से बेघर हुए पाशो भी हवा में टूटे पत्ते की तरह दर-दर भटकती है और पुरुष के हाथों इस्तेमाल होती रहने के बाद अंत में परिवार की डार से आ मिलती है। ‘डार’ से ‘बिछुड़ी’ पाशो के लिए उसका हर ठौर-ठिकाना त्रासद ही बना रहा।
‘डार से बिछुड़ी’ की नायिका पाशो पुरुष समाज के लिए एक व्यक्ति न होकर सामान की तरह बन जाती है। वह मानो मनुष्य नहीं, एक गठरी है, जिसे कोई भी उठाकर चलते बनता है। उसके साथ गुलामों जैसा बर्ताव किया जाता है, उसे ‘द्रौपदी’ बनाकर घर-भर की सेवा का दायित्व सौंप दिया जाता है। जिस मौत के डर से वह घर से बाहर निकली, उसे न जाने कितनी मौतें मरनी पड़ी। पाशो के रूप में असहाय स्त्री का चित्रण है जो परिस्थितियों के समक्ष एक बेजुबान गाय की तरह पड़ी रही। यहाँ तक कि उसका अपना घर ही उसके लिए असुरक्षा का डेरा बन पड़ा। लेकिन पाशो के अंदर की औरत समय और परिस्थितियों के कारण विद्रोह नहीं कर पाती। ऐसे में एक प्रश्न हमारे सामने कृष्णा सोबती जाने-अनजाने ही छोड़ जाती हैं कि आखिर स्त्री सुरक्षित कहाँ है? आज यह प्रश्न मीडिया और स्त्री बहस संबंधी मुद्दों में बार-बार उठाया जा रहा है लेकिन आज भी उस ठाँव! जिस तरह पतझड़ में टूटे पत्तों का कोई ठौर नहीं होता, कोई भविष्य नहीं होता, वैसे ही पतझड़ में ‘डार’ से विलग हुई पाशो का भी कोई और ठौर नहीं रहा, कोई भविष्य नहीं रहा, वह भी परिस्थिति के हाथों बहती चली गयी… बहती चली गयी।
अनुभव से मथकर निकले नानी के इन बोलो ने उस पर कोई असर न छोड़ा था कि ‘संभलकर री, एक बार थिरका पाँव जिंदगानी धूल में मिला देगा’ और अंत तक बहते-भटकते परिस्थितियों के हाथ की कठपुतली बनी पाशो समझ ही गयी, ‘सच ही सब धूल हुआ–इस अभागी की लाज, शरम, इज्जत, आबरू।’
जीवन की ठोकरों और भटकनों ने उसे खुद अपनी स्थिति का एहसास करा दिया था। वह स्वयं अपनी इस स्थिति का विश्लेषण करती है–‘आँगन के बीचोंबीच छोटे कुएँ की चरखड़ी पर लज लटकती थी। गागर उठा नीचे बहा दी तो जान पड़ा, मैं भी चरखड़ी पर चढ़ी लज हूँ। कभी इस गागर, कभी उस गागर।’ और सचमुच ही पाशो तूफान दरिया में भटकते तिनके सी कभी यहाँ, तो कभी वहाँ, आज दीवान जी के घर तो कल मझले के लेकिन अगर गहरायी से सोचा जाए, तो उसकी जिंदगी में थिरकने जैसा था ही क्या अपनी माँ कहलानेवाली ‘छवि’ को एक बार देख लेना चाहती थी और उसकी यह इच्छा स्वाभाविक ही थी, ‘चाहती, किसी दिन चुपके से खोजों ही हवेली जाऊँ और किसी झरोखे से अपनी माँ कहलाने वाली की एक झलक तो पाऊँ।’ परिस्थिति की भयावहता ने उसे भीतु बना दिया था। पाशो का अपना कोई वजूद नहीं रहा। वह मानो ‘गुदड़ी’ हो जिसका हर किसी ने अपनी सुविधा से इस्तेमाल किया। कभी बरकते ने अपनी सुविधा हेतु खींच लिया फिर अपनी सुविधा से बेंच दिया। कभी लाला ने अपनी सुविधा से गृहस्थी सँभालने के लिए खरीद लिया, कभी मझला अपनी गृहस्थी बसाने के ख्याल से उठा ले गया, वह मानो व्यक्ति नहीं चीज है, पशु है जिसे जिसका मन हो सो उठाकर ले जाए, वहाँ उसका घर सँभाले, बिस्तर गर्म करे और वंश चलाने के लिए संतान दे। वह भले ही अपनी जमीन से विलग हुई थी लेकिन उसकी आत्मा तो वहीं से बंधी टिकी रही–नानी, मामू-मामियों के बीच, माँ, शेख जी और लाली (उसका बेटा) कभी अपनी जमीन से उखड़ी ही नहीं, वह तो वहीं रही–सिर्फ उसकी आत्मा वहाँ से छुटकर भटकने-मँडराने लगी, जैसे जड़ से उखड़ते ही अशरीरी हो गयी।
परिस्थिति के हाथ की कठपुतली बनी पाशो अपनी स्थिति से लड़ने या उबरने की कोशिश भी छोड़ चुकी थी। एक बार अपनी जड़ से उखड़ी पाशो ने समझ लिया था कि विरोध का मतलब मौत है, इसलिए भटकती जिंदगी ने उसे परिस्थितियों का दास बनना सीखा दिया था, जो सामने मिला उसे ही अपनी किस्मत माना, तूफान ने जिधर फेंका, उसे ही अपना आश्रय समझा, जहाँ गयी वहीं की हो रही–
‘नवेली, तुम्हें अपने संग ले जाऊँगा। तुम मेरे पास रहोगी…’
डरकर सिर हिलाया–
‘यह न कहो–यह न कहो
इस अभागी को अब इस घर से न निकालो।’
एक बार ‘आसन्न मौत’ की भयावहता से डर कर भागी पाशो न जाने कितनी बार और कितनी मौतें मरी। बाद में स्थिति से लड़ना भी छोड़ दिया। पूरी तरह से खुद को परिस्थिति के हवाले कर दिया। अतीत को अपनी छाती से चिपकाये वह वहीं की दुआ सलामती करती है। संवेदनशील सहृदयी पाशो सबके दु:ख को अपना दु:ख मानती है और प्रार्थना करती है, ‘मैं तो पराये घर हूँ, पर इस घर के कर्ता-धर्ता की यह दशा! हे! हे जानी जान, ऐसे हाल-हीले किसी के न हो! कोई पड़ा-पड़ा अकेले मरने की बाट जोहे…’ वह अपने क्रय-विक्रय के अपमान को भूलकर बीमार लाले की सेवा में कोई कसर न उठा रखी। सेवा-सत्कार पाकर सिर हिला-हिला लाल-बोला, ‘दीवानों की, मैं जी भर तृप्त हुआ। रब्ब तुम्हें बहुत-बहुत सुख-चैन दे।’
कृष्णा सोबती ने अपनी इस रचनात्मक कृति में जिस चाव से ‘पाशो’ जैसे चरित्र की रचना की है, वह समाज से अलग नहीं बल्कि इसी समाज के चेहरे से हमें रू-ब-रू कराया है। बहुत से पाठकों और आलोचकों ने पाशो को एक दुर्बल विवश चरित्र माना है, अगर परिवेश और परिस्थितियों के बीच रखकर उसका आंकलन करें तो ‘पाशो’ की जो छवि उभरती है वह उसके परिवेश और परिस्थितियों के कारण है। कुएँ से निकल दलदल में धँसने से तो अच्छा है कुएँ का अँधेरा। चारों ओर युद्ध का माहौल, दूसरे स्थान तक पहुँचने का कोई सुरक्षित साधन नहीं। ‘मौत’ को गले लगाना तो जीवन से भागना है और पाशो भागती नहीं बल्कि विषय परिस्थितियों के बीच जूझते हुए भी एक उम्मीद की आस जलाये रखती है–
‘दिवानों के घर कब जाना हुआ था बाबा? वहाँ की कोई खोज-खबर?’
‘इस बार उधर का पैंडा नहीं मारा बेटी!
‘कोट की ओर कब जाना होगा?’
अपनी ओढ़नी का छोर पकड़कर बाबा की ओर बढ़ा दिया। शेख के यहाँ मेरी माँ को सौंप देना बाबा।’
कृष्णा सोबती ने पाशो की रचना के जरिये स्त्री जीवन के समक्ष जीवन से मौजूद खतरों और उसकी विडंबनाओं को रेखांकित किया है। स्त्री-जीवन की विडंबना है उसका ‘स्त्री’ होना, तिस पे भी उसका असहाय और निर्बल होना।
‘डार से बिछुड़ी’ का प्रकाशन समय 1958 है। यानी आज से छह दशक पहले भी स्त्री की स्थिति जहाँ थी, आज भी वहीं हैं, समय बदला जरूर है पर स्त्री के लिए समाज और परिवार पहले से ज्यादा असुरक्षित और भयावह ही हुआ है। आज भी ऐसा परिवेश नहीं बन पाया है, जहाँ वह अपने को सुरक्षित महसूस कर सकें। इस तथ्य को कृष्णा सोबती ने आज से छह दशक पूर्व ही रेखांकित कर दिया था।
‘पाशो’ के लिए मामा-मामी का घर ही असुरक्षित हो जाता है। जहाँ वह निखालिस वस्तु रह जाती है। स्त्री की अपनी इच्छा, अभिलाषा कुछ नहीं। स्त्री के लिए घर की, बाहर की दुनिया तब तक सुरक्षित न रहेगी जब तक बरकत करीम, मझले और छोटे की मानसिकता में स्त्री महज चीज के रूप में रहेगी। पाशो की जिंदगी में तूफान का मूल कारण फत्तेह अली का बेटा करीमू ही था, जिसके हाथ में पाशो की चमकी का रूमाल देखा गया और उसी के कारण पाशो को ठिकाने लगाने की साजिशें होती हैं और उसी वजह से पाशो को घर से बेघर हो दर-दर भटकना पड़ा। बदलती स्थिति को अपना भाग्य मान पाशो भी उसी स्थिति में रहने को बाध्य हुई क्योंकि कुएँ से निकलती तो खाई में गिरती। इसलिए जहाँ जाती है, वहीं की होकर रह जाती है। ऐसी समाज व्यवस्था में जहाँ स्त्री, स्त्री न होकर कोई सामान हो, मनुष्य न होकर पशु हो, चीज हो, जिसे जिसका मन हो उठाकर ले जाए, अपनी सुविधानुसार उसकी खरीद-बिक्री करें, उसे मात्र कोख समझे–वह स्त्री के अनुकूल नहीं। यदि समाज ही ऐसा है, जिसमें स्त्री मनुष्य न होकर पशुवत जीवन जीने के लिए विवश है, तब समाज के सभी सदस्यों की नैतिक जिम्मेदारी हो जाती है कि वे ऐसा समाज बनाये, जिसमें सभी मनुष्य की तरह सम्मानपूर्वक जी सकें। यही जनतांत्रिक संदेश कृष्णा सोबती अपनी प्रायः रचनाओं के जरिये रखती हैं।
Image : Young Girl Reading
mage Source : WikiArt
Artist : Pierre Auguste Renoir
Image in Public Domain