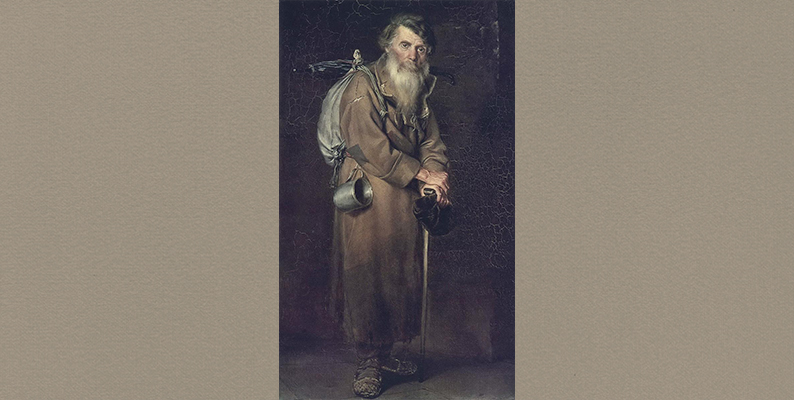रमणिका गुप्ता से अंतरंग बातचीत
- 1 June, 2016
शेयर करे close
शेयर करे close

शेयर करे close
- 1 June, 2016
रमणिका गुप्ता से अंतरंग बातचीत
संघर्ष-कोख से उपजी एक साहित्यकार
अवचेतन मन के गुह्य संसार में, परिस्थितिजन्य अनेक सवाल अपना समाधान खोजने, उत्तर की प्रत्याशा में सतत् संग्रहित होते रहते हैं और अनुकूल अवसर आते ही प्रश्नानुसार जिज्ञासाओं के समाधान होते जाते हैं। बीज प्रकृति में नियमतः यही होता है। विगत कई दशकों से मैं एक ऐसी महिला शख्सियत को निकट से देखना, समझना और जानना चाहता था, जिन्हें लेकर मुझमें अनेक सवाल गहराते रहे थे, और उन सारी जिज्ञासों के उत्तर मुझे गत साल प्राप्त हुए, जब मैं अपनी काव्य पुस्तक ‘संवेदनाओं के क्रांति बीज’ के प्रकाशन के क्रम में उनके निवास पर उनसे मिला और फिर उनसे लगातार चार दिनों की बातचीत ने मेरी उन सारी बातों का समाधान कर दिया, जो मैंने उन्हें पढ़कर कई बीते दशकों में जाना था।
यह विरल महिला है रमणिका गुप्ता, जो अपनी बुद्धि, तर्क और विवेक के वैचारिक संकल्प की दृढ़ता में, विरोध और विद्रोह के हवनकुंड की लपटों से पैदा हो शोषित, पीड़ित, वंचित और प्रताड़ित मानवता के हित, उनके जीवन के हर मोर्चे पर, मौत से जूझती हुई झंडाबरदार बनी रही हैं। पाखंड, अंधविश्वास, धर्मांधता और कुरीतियों के खिलाफ लड़ती हुई ये आदमी के आड़े आने वाले विश्वासों, आस्थाओं और धर्मों यहाँ तक कि ईश्वर के खिलाफ भी नारेबाजी में अग्रणी रही हैं। इस शख्सियत ने राजनीति और राजनेताओं के दोगलेपन और उनकी काली पलटनों की करतूतों को निकट से देखा व भोगा है; कोयला खदानों के मजदूरों के लिए किए गए अपने संघर्ष काल में यूनियन नेता के रूप में इन्होंने सामंतों, जमींदारों, राजनेताओं, गुंडों और कोल माफियाओं से लोहा लेते हुए ये अनेक बार मौत के आगोश से बाहर निकली हैं, पर कभी समझौता नहीं किया। इन्होंने अपनी महत्वाकांक्षा के सामरिक जीवन में आकश में उड़ने को अपने डैनों को सदा खुला रखा है। यह वह नारी मन है, जिसने एक ओर जहाँ प्रेम की पराकाष्ठा को जीया है, वहीं दूसरी ओर विच्छेद और विछोह को गीता की स्थितप्रज्ञता के रूप में जीया है तथा उपनिषद् की चरैवेति-चरैवेति इनके जीवन का मूलमंत्र रहा है। और फिर शब्दों को हथियार बनाती हुई, दर्रों के अंत:पर्तों को खोलती, अपनी संवेदना की दुनिया के साथ साहित्य में समर्पित होकर अपनी ख्यात पत्रिका ‘युद्धरत आम आदमी’ के विगत चार दशकों से अनवरत प्रकाशन और पुस्तकों की सर्जना कर एक कीर्तिमान स्थापित किया है। ये दलित और आदिवासी साहित्य की दुनिया के सशक्त हस्ताक्षर हैं। इन्होंने अन्या के रूप में पीड़ित नारियों, दलितों एवं आदिवासियों को अपने साहित्य में समेटे, साहित्य में जो शोधकार्य किया है, वह एक ऐतिहासिक दस्तावेज है।
रमणिका जी का लेखन, इनका निकट से देखा और खुद का भोगा गया यथार्थ है, यह मात्र कल्पना रचित बैठकखाने का साहित्य नहीं; यहाँ ये एक एक्टिविस्ट सर्जक के रूप में अन्य साहित्यकारों से अलग हैं। इनका साहित्य इनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा में सृजित नहीं, बल्कि आदमी की पीड़ा का समाधान खोजती उसके कारकों के खिलाफ युद्ध की घोषणा है। इनके लेखन और जीवन में कहीं कोई विसंगतियाँ नहीं हैं। ये जीवन की ईमानदार भावनाओं के शब्द-संसार में जीती रही हैं। ये अपने पारदर्शितापूर्ण जीवन की अनोखी कहानी हैं, जहाँ कोई दुराव-छिपाव नहीं। इनका साहित्य नारी के स्वतंत्र वजूद और अस्मिता के मर्यादित जीवन के लिए मनुवादी अवधारणाओं के तहत नारी मन को, यौन कुंठाओं से ग्रसित हीन भावनाओं से जर्जर होने नहीं देना चाहता। मुझे जब ऐसी ही इन्कलाबी बहुआयामी व्यक्तित्व के नारी मन को खँगालने का सुखद अवसर मिला, तो उनकी सुनी और पढ़ी बातें एक साथ साक्षात् खड़ी मिलीं।
उनसे पहली मुलाकात में ही मुझे लगा कि मैं एक सच्चे साहित्यकार से मिल रहा हूँ, जिनका भीतर और बाहर एक समान है। उनके संवेदनात्मक पक्षों ने मुझे अभिभूत कर दिया। सहयोग की जितनी बातें मैंने सोची थी, ये उससे कई कदम आगे थीं। किताबों से घिरे अपने बेड के समीप इन्होंने बड़ी आत्मीयता से बैठने को कहा। दिन के 10 बजे मैं इनसे मिला था और ये उनींदी दिख रही थीं–बोली मैं रात के 3 बजे तक आपकी काव्य-पुस्तक ‘संवेदनाओं के क्रांति बीज’ की पांडुलिपि पढ़ती रही थी, उसे समाप्त कर ही सोई। पांडुलिपि जब मैंने पलट कर देखा तो उसमें जगह-जगह अधोरेखांकन और टिप्पणियाँ थीं; पचासी पार की उम्र में भी इनकी इस कार्य क्षमता ने मुझे विस्मित किया।
लगातार चार दिनों तक उनसे मिलने का क्रम जारी रहा, साहित्य और उनसे जुड़े जीवन के विभिन्न पहलुओं की चर्चाएँ होती रहीं; उनके संघर्षरत जीवन की परतें एक-एक कर खुलती रहीं। इनका सब कुछ उनके दुस्साहसपूर्ण जीवन जीने का एक अप्रतिम आख्यान है। इनका सब कुछ एक जिद के तहत, जो ढाल लिया, सो ढाल लिया है। मूल्यों के लिए जान की बाजी लगा देना इनकी दिनचर्या है।
अपनी मुलाकात के अंतिम दिन, भागलपुर लौटने से पूर्व, मैंने कहा दीदी जी, बहुत सारे सवाल मुझमें गहरा रहे हैं, क्या उन सवालों के साथ आपसे गुजरूँ? बात छूटते ही, इन्होंने झट से कहा–मैं तो बैठी ही हूँ, पूछिये, यों तो मुझे एक आयोजन में जाना है, पर जवाब देकर ही जाऊँगी। इनकी बेहिचक साफ सुथरी बातें और गहराई से शब्द पाते पारदर्शी उत्तर की ईमानदार शृंखला पर उनके उभरे व्यक्तित्व ने जहाँ मुझे स्तब्ध कर दिया, वहीं इनकी स्वतंत्र तार्किक चिंतन की निर्भीक बातों ने मुझे जीवन के कुछ नव्य आयामों के बीच सोचने को मजबूर किया। प्रश्नों के स्पष्ट उत्तरों के साथ इन्होंने बीच-बीच में अपने बीते जीवन के कई अंत:पर्तों को उधेड़ कर उस पर बेबाक टिप्पणी की। इनके विचारों और अवधारणाओं में कहीं कोई आवरण न था और न आसमान छू लेने की कोशिश में इन्होंने जमीन छोड़ी थी।
मैं जानता था कि इनके जीवन का जो आखिरी पड़ाव है, वह इनका साहित्य है, जहाँ ये शब्दों को हथियार बना मूल्यों की लड़ाई के महाभारत में हैं–जहाँ कविताएँ विशेष रूप से क्रांति का हरावल दस्ता बन, जन मानस को आंदोलित व ऊर्जस्वित कर उसे एक सही दिशा देती हुई समय के साथ उसकी चुनौतियों का सामना करती जीती है। इसलिए मैं इनसे इनकी कविताओं में इनकी मनोस्थिति जानना चाहा कि–क्या आज की कविताएँ जिनके लिए लिखी जा रही हैं, उन तक पहुँचती हैं? क्या कवियों को बिना एक्टिविस्ट हुए, आज की कविताएँ, जो जनपक्षीय हैं अपने लक्ष्य को बेध पाएँगी? मैं यह भी जानना चाहूँगा कि क्या साहित्य आपको विरासत में मिला है?
कुछ क्षण बड़ी गंभीर मुद्रा में अपने बीते दिनों में समाती हुई इन्होंने अपनी बातें सहज होकर रखीं–‘मेरे पिता जी प्यारेलाल वेद भी कविता किया करते थे। मेरी भाभी नृत्यांगना थी, वे स्वयं रवींद्र संगीत पर भाव नृत्य करती थी। मैंने भी नृत्य का प्रशिक्षण लिया था और नाचती भी थी। कविता लिखना मैंने 14 वर्ष की उम्र से ही शुरू किया था। मेरी पहली कविता 1945 में जन्म व मृत्यु पर थी। ‘मृत्यु’ शीर्षक कविता मैंने अपनी दादी के निधन पर अपनी संवेदनात्मक स्थिति पर लिखी थी। इसके बाद मैंने प्रेम और प्राकृतिक सौंदर्य पर कविताएँ लिखी। मैंने प्रेम भी किया और प्रेम विवाह भी, वह भी अंतर्जातीय, परिवार के काफी विरोध के बावजूद। मैंने अपने भावनात्मक और संवेदनात्मक जीवन में तथाकथित पारंपरिक मूल्यों को आड़े आने नहीं दिया। जब चीन और पाकिस्तान का आक्रमण देश पर हुआ था, तो मैं काफी सक्रिय भूमिका में थी। साहित्यिक, सामाजिक, प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पर पूरे बिहार में मेरी चर्चा थी। मैं घूम-घूमकर क्रांति गीत गाती थी। सिविल डिफेंस का प्रशिक्षण ली थी, राइफल चलाना सीखी थी और मैं जीप वाली दीदी कहलाने लगी थी। अपने सैनिक भाइयों के लिए चंदा इकट्ठा करती थी। उस समय मेरी निम्न कविता बड़ी ख्यात थी–‘रंग बिरंगी तोड़ चूड़ियाँ, हाथों में तलवार गहूँगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी।’ यों कहिए कि मैं उन दिनों एक्टिविस्ट साहित्यकार के रूप में थी और लगता था कि कविताएँ अपने उद्देश्य की पूर्ति में हैं। धनबाद से मैंने देशप्रेम की कविता की शुरुआत की थी।
बाद के दिनों में मुझे कोयला खदान के अंचलों में, धनबाद, झरिया, बोकारो और हजारीबाग में खान मजदूरों, कामगारों और महिला आदिवासियों की दुर्दशा, शोषण और उत्पीड़न ने बहुत संवेदित किया और तब से मैं उनके लिए संघर्ष में जुट गई और यहाँ से फिर मेरी इन्कलाबी कविता का दौर चला। मंचों पर, मजदूरों की बस्तियों में, उनके लिए छेड़े अभियान की कविताएँ होने लगी। संघर्ष काल के भोगे जीवन पीड़ाओं के बीच कविताएँ अपने विकास की ऊँचाई पाने लगी, यह सत्य भी उद्घाटित हुआ कि संघर्ष काल में सृजित कविताएँ उत्कृष्ट कविताएँ होती हैं। खदान अंचलों में उन दिनों मेरी कविताओं की धूम थी। मैं उन दिनों दबे-कुचले आदिवासियों की झोपड़ियों में रहती थी। उन्हीं का जीवन जीती थी और उनकी पीड़ाओं के साथ उनके लिए क्रांति गीत का सृजन करती थी। जमीन और जंगल से उनके विस्थापन के खिलाफ, हजारों हजार की संख्या में कई बार जेल की यात्रा की थी और अपनी कविताओं से उन्हें ऊर्जस्वित और प्रोत्साहित करती थी। साहित्य के क्षेत्रों में आज जो दलित लेखक हैं, वे सामाजिक न्याय, अधिकार और सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। वे प्रायः एक्टिविस्ट की भूमिका में हैं। परिस्थितियाँ आज यह हैं कि सुविधाभोगी मध्यवर्ग सारी सामाजिक क्रांतियों के आड़े आ रहा है। उनमें आम हितचिंतन की बातें नहीं रही हैं। वे दिन ब दिन घोर व्यक्तिवादी हो रहे हैं। आज की बाजारवादी संस्कृति में मध्यवर्ग अपने लिए सारी सुविधाएँ समेट लेने की होड़ में गरीबों से नफरत करते हैं और अमीरों से प्रेम, जबकि वे खुद गरीब हैं। ये अमीरों और गरीबों के बीच बफर स्टेट बने हुए हैं। यों कटु सत्य यह है कि मध्य वर्ग पूँजीवादियों का ऐलसिसियन डॉग बनकर यदा-कदा भूँकता रहता है पर किसी को काट पाने की क्षमता नहीं रखता। साहित्य तो मूल्यों के हित में समय की चुनौतियों का सामना करता है। साहित्यकारों को तो खुद से निकल कर आम आदमी की परिस्थितियों के बीच जीना है। यह साहित्य और जीवन दोनों को विस्तार देता है। मैं अपने जीवन के चालीस साल इसी रूप में गुजारी हूँ। साहित्य की आज की स्थिति यह है कि यह आम आदमी से दूर चली जा रही है। इसके कारणों की तलाश होनी चाहिए। खासकर कवियों को आज अपनी कविताओं के साथ एक्टिविस्ट होना होगा। जिनके लिए कविताएँ लिखी जा रही हैं, उन तक कविताएँ पहुँचनी चाहिए, ताकि वे समझें कि कविताओं में उनका ही दर्द और फिर उसका निदान भी है। –लेखक मनुष्यता के खिलाफ जो हो रहा है, उससे मुठभेड़ करता है। जो लोग खतरे के डर से सकारात्मक बदलाव की भूमिका में नहीं पलते, वे लेखक नहीं हो सकते। आज कविता शहरी जीवन के बैठकखाने की उपज हो रही है, जहाँ दर्द है, पीड़ा है, उत्पीड़न और शोषण है, जहाँ कराह और भूख है, वहाँ कविताएँ नहीं हो रहीं। शहर के सुविधाभोगी साहित्यकार सोचते हैं कि वे एक्टिविस्ट होकर न लिख पाएँगे। उन्हें साहित्यकार की ख्याति चाहिए, समाज और व्यक्ति के लिए साहित्य उनका उद्देश्य नहीं। साहित्य आज निहित महत्वाकांक्षा की चीज हो गई है।’
फिर मैंने इन्हें साहित्य से अलग करते हुए पूछा–दीदी जी, आपने अपने जीवन के वसंत काल बीहड़ों और जंगलों में संघर्ष करती, पुरुष साथियों के साथ गुजारी हैं, फिर राजनीति में प्रवेश के बाद बिहार विधानसभा और परिषद् की सदस्या के रूप में राजनेताओं के साथ गुजारी है, पुनः कच्छ की लंबी यात्रा भी अपने पड़ावों के बीच, आपने अपने पुरुष साथियों के साथ की है। ऐसी बातें हवा में है कि राजनीति से जुड़ी महिला की अस्मिता के साथ कुछ अच्छा नहीं गुजरता, कुछ स्पष्ट करना चाहेंगी? इन प्रश्नों के आलोक में, राजनीति और यौन संबंधों की उनकी बेबाक और बेपर्द कथन ने मुझे बगलें झाँकने को मजबूर कर दिया। ऐसी निर्भीक और स्पष्टवादी महिला से मेरा पहला संवाद था। अपनी अनुभूतियों और भोगे गए यथार्थ के चोट खाते मन की गहराई से उन्होंने कहा–‘राजनीति में महिला को पुरुष नेता का सहारा लेना पड़ता है, बिना पुरुष देह की लतिका बने वह फुनगी तक नहीं पहुँच पाती है। राजनेताओं की द्विअर्थी बातों के बीच उन्हें थेथर बनकर जीना होता है और अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के डगर पर चलती हुई वह, कालक्रम में वहाँ यौन संबंधों के अपराधबोध से मुक्त हो जाती है। मुझे भी अपनी खास रणनीति के तहत कुछ परिस्थितिजन्य समझौते करने पड़े थे, पर यह मैंने अपने को बेवश और असमर्थ मानते हुए नहीं किया था। मैं फ्राइड की मनोवैज्ञानिक अवधारणाओं से सहमत हूँ। इसलिए मैं यौन संबंधों में कोई कुंठा नहीं पालती और यौन इच्छाओं को कमजोरी से नहीं जोड़ती। मैं इसे एक प्राकृतिक जरूरत के तौर पर स्वीकार करती हूँ।
मैं अपनी राजनीति के शुरुआती दौर में काँग्रेस में थी। फिर काँग्रेस छोड़कर संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी में शामिल हो गई थी। प्रारंभ में काँग्रेस के प्रति जो मेरी सोच थी, वह बिहार आकर खत्म हो गई थी। काँग्रेसियों की यहाँ यह स्थिति थी कि वे स्त्री कार्यकर्ता को अपना कलेवा मानते थे। भूख लगने पर वे स्त्रियों को अपना स्वार्जित जन्मसिद्ध अधिकार मानते थे। लेकिन मैं कभी भी उनकी मान्यता के साथ न थी। किसी का सहारा ले मैं फुनगी तक न पहुँचना चाहती थी। इसलिए काँग्रेस के बहुत सारे नेतागण मुझसे चिढ़ते थे और नाराज रहते थे। मैंने कभी उनकी परवाह न की थी और कभी-कभी थप्पड़ भी जड़ने पड़े थे। इन परिस्थितियों के बीच मैंने काँग्रेस से त्यागपत्र दे दिया और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी में आ गई। इस पार्टी में औरतों के प्रति सोच कुछ अलग थी। अपनी औरतों को छोड़कर दूसरों की औरतों को स्वतंत्र देखने में वे काफी उदार थे। लेकिन समानवादियों में सेक्स के प्रति दूसरों से भिन्न कुछ अवधारणाएँ थीं, खासकर युवा वर्ग में। वे मुक्त यौन संबंधों के समर्थक तो थे, पर जबरन संबंधों के नहीं। इसके राजनेताओं में ऐसे संबंधों को लेकर आापसी ईर्ष्या भी पनपती रहती थी। 1967 में पाकिस्तान को कच्छ के कुछ गाँव देने के भारत सरकार के निर्णय के खिलाफ संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी और जनसंघ आंदोलनरत थे। इसी आंदोलन के क्रम में सोशलिस्ट साथियों पार्टी के कार्यकर्ता कच्छ की यात्रा पर थे। मैं भी अपने ग्यारह साथियों के साथ उस यात्रा में थी। मेरे साथ एक दलित महिला भी थी। यात्रा के क्रम में एक ट्रक चालक द्वारा अभद्र व्यवहार किए जाने पर वह महिला भयभीत हो गई थी और बीच में ही यात्रा छोड़कर वह वापस चली जाना चाहती थी। मैंने उस महिला को समझाया था कि हम देश के खास मिशन पर हैं, कठिनाइयाँ आएँगी पर मिशन सर्वोपरि है। द्वितीय विश्वयुद्ध में रूस पर जब हिटलर ने हमला किया था और नाजी सेना अंदर तक प्रवेश कर चुकी थी, तो जवान रूसी लड़कियाँ अपनी आबरू की चिंता न कर, दुश्मनों की गुप्त सूचनाएँ अपने देशवासियों को लाकर देने के लिए रात-रातभर जर्मन अफसरों के कैंपों में गुजारती थी। दलित महिला ने अपने लौटने का निर्णय रद्द कर दिया और कच्छ में गिरफ्तारी दी।’
फिर मैं रमणिका जी के राजनीतिक जीवन से हटकर साहित्य में प्रवेश करते हुए, उनसे पूछा–‘आप राजनीति छोड़कर पूर्णकालिक साहित्य साधना में जुट गईं, इसके पीछे मैं आपका तर्क जानना चाहूँगा।’
‘मेरा मुकाम है पीड़ित मानवता के दर्दों के खिलाफ अनवरत संघर्ष, और वह मैं साहित्य के माध्यम से ही कर पाऊँगी और कर रही हूँ; जहाँ-जहाँ उनकी कराह और आह है, वहाँ मैं खड़ी रहती हूँ, हाशिये की जमातों के प्रति दृष्टिकोणात्मक बदलाव लाने, उन्हें हीन भावना से मुक्त कराने उन्हें आत्मविश्वास और आत्म सम्मान के साथ उनमें लड़ने का मन देकर उनमें लीडरशिप विकसित करने में, मैं समर्पित हूँ।
इसके बाद फिर काव्य मंच और दलित साहित्य की बातें आईं तो इन्होंने टिप्पणी की–‘आज काव्य मंच दिशाहीन हो अपने उत्तरदायित्वबोध से अलग है। यह समय की चुनौतियों को अनदेखा करता हास्य-व्यंग्य के भोड़े प्रदर्शन और दैहिक सौंदर्य जनित प्रकृत भावनाओं को उजागर करने में है। यह एक गैर जिम्मेदाराना हरकत में मनोरंजन की वस्तु बन गया है।’ –दलित साहित्य की बात आने पर इन्होंने कहा–‘समय की पुकार के साथ दलित साहित्य आज दलितों, शोषितों, वंचितों के लिए संघर्षरत है। यह उसके सामाजिक न्याय, उसकी पहचान और उसके आत्मसम्मान के लिए लड़ रहा है। वास्तविकता यह है कि समाज में बदलाव लाकर उसे लोकतांत्रिक बनाने का काम किसी राजनेता या सरकार से संभव नहीं, इसके लिए जिस सामाजिक क्रांति की आवश्यकता है, वह संस्कार, संवेदना और मनोभावना साहित्य ही पैदा कर सकता है। आज देश को एक राजनेता नहीं समाज सुधारक चाहिए, जहाँ साहित्य की जबर्दस्त भूमिका है। साहित्य समाज बदलने का एक कारगर हथियार बन सकता है।
फिर इन बातों से अलग हो मैं इनके बचपन में लौट आया और इनसे प्रश्न किया–‘सुना है, आप बचपन से ही क्रांतिधर्मी और विद्रोही स्वभाव की थीं, जो बातें आपकी तर्क बुद्धि में न समाती थी, आप उसके खिलाफ तत्काल खड़ी हो जाती थीं। मुस्कुराते हुए इन्होंने कहा–‘यदि मैं जिद्दी न होती और अपने हकों पर नहीं अड़ती तो आज मैं कहीं गृहिणी बनी 8-10 बच्चों की माँ बनी रोटियाँ पका रही होती। समाज में बदलाव लाने के लिए जरूरत होती है जिद की और अपना घर छोड़ने की हिम्मत की। मैं तो बचपन से ही गलत परंपराओं, रूढ़ियों, पाखंडों, कुरीतियों और अंधविश्वासों के खिलाफ रही हूँ। यहाँ तक कि धर्म और ईश्वर के खिलाफ भी मैं आवाज उठाती रही हूँ। मैं ‘धर्म और ईश्वर’ की नहीं, आदमी की बातें करना पसंद करती हूँ। मुझे रूढ़ियाँ तोड़ने में बड़ा मजा आता था। अधिक मजा तो तब आता था, जब लोग इस पर तिलमिलाते थे। मुझे अपने परिवार में विद्रोही और जिद्दी का दर्जा मिला था, क्योंकि पर्दा प्रथा का विरोध कर बिना सिर ढके बाहर आया जाया करती थी। जब भी परिवार के साथ बाहर जाना होता, माँ कहती–तुम हमलोग से पीछे अलग होकर चलो। मुझे हमेशा सामाजिक क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाने की धुन रहती थी, कभी भी छाया बनकर जीना मैंने पसंद नहीं किया।’
इन बातों के बीच समय लंबा खींचा गया और उन्हें पूर्व निर्धारित किसी कार्यक्रम में जाना था। मैं उनके चेहरे से इन बातों को ताड़ रहा था। अतः क्षमा माँगते हुए, उनसे विदा हो बाहर निकल गया।
Image : A Lady Reading
mage Source : WikiArt
Artist : Gwen-John
Image in Public Domain