माधवदेव और भक्ति आंदोलन
- 1 April, 2025
शेयर करे close
शेयर करे close
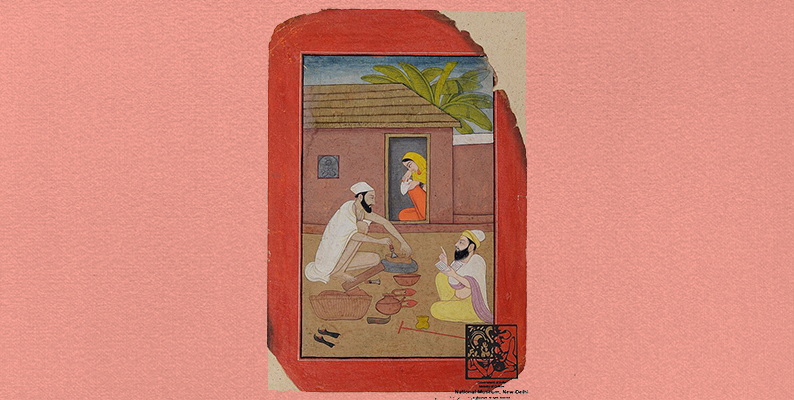
शेयर करे close
- 1 April, 2025
माधवदेव और भक्ति आंदोलन
सोलहवीं सदी के भारतीय साहित्य में हमें आध्यात्मिक चेतना का सन्निवेश दिखाई पड़ता है। यह साहित्य मूलतः भारत की प्राचीन भाषाओं अर्थात संस्कृत-प्राकृत के आधार लिखा गया है। इस क्रम में आधुनिक भारतीय भाषाएँ अपनी परंपरा से जुड़ती हैं। संस्कृत को छोड़कर इन आधुनिक भाषाओं में रचना करना सचमुच एक क्रांतिकारी कार्य था। लेकिन यह उस युग की आवश्यकता भी थी, क्योंकि आम जन संस्कृत नहीं जानते थे और उन्हें संस्कृत रचनाओं का भावार्थ बताना पड़ता था।
सोलहवीं सदी में हम आधुनिक भारतीय भाषाओं में अत्यंत प्रतिभाशाली कवियों की उपस्थिति पाते हैं। कवि होने के साथ ये भक्त हैं, संत हैं, महात्मा हैं, संगीत कला में निष्णात हैं और वे अपने समय को आत्यंतिक रूप से प्रभावित करने वाले हैं। ऐसे भक्त कवियों ने दूर-दूर तक यात्राएँ कीं और व्यापक जन-संपर्क विकसित किया। इस सदी की रचनाओं में भक्ति-काव्य की प्रधानता है, जिसने समूचे देश में एक सांस्कृतिक चेतना का प्रसार किया। महत्त्वपूर्ण बात यह है कि इस चेतना का प्रसार संस्कृत भाषा के माध्यम से न होकर भारतीय भाषाओं के माध्यम से होता है। भक्ति की इस चेतना का प्रादुर्भाव दक्षिण से सातवीं सदी में होता है और सोलहवीं सदी में यह ब्रजभाषा में अपने सर्वोच्च शिखर पर पहुँचती है। उस सयम की प्रतिनिधि काव्यभाषा ब्रज भाषा थी और एक तरफ़ तो इससे गुजराती, पंजाबी, मराठी आदि भाषाएँ जुड़ रही थीं तो दूसरी तरफ़ बांग्ला, असमिया और ओड़िया भाषाएँ।
भक्ति आंदोलन मध्य युग का एक ऐसा जीवंत आंदोलन था, जिसने समूचे भारत को प्रभावित किया। यहाँ की सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक गतिविधियों पर इस आंदोलन का गहरा प्रभाव पड़ा। डॉ. रामविलास शर्मा ने लिखा है ‘कैसा महान युग था वह। दक्षिण में पुरंदरदास, उत्तर में सूरदास, पश्चिम में नरसी मेहता और पूर्व में शंकरदेव। ये लोग ख़ूब यात्राएँ करते थे। पुरंदरदास ने तीन बार उत्तर भारत की यात्रा की। शंकरदेव बारह वर्ष तक भारत के विभिन्न प्रदेशों में घूमते रहे। इस तरह उन्होंने अपने प्रदेश की जातीय संस्कृति के साथ पूरे देश की राष्ट्रीय संस्कृति को अपने अनुभव से समृद्ध किया’ (भारतीय साहित्य का भविष्य)।
शंकरदेव तथा राघवदेव सोलहवीं सदी में असम के दो ऐसे अनुपम व्यक्तित्व हैं जिनके कारण असम में सांस्कृतिक पुनरुत्थान संभव हो सका। आठवीं से चौदहवीं सदी तक असम में तंत्र-मंत्र का व्यापक प्रभाव रहा। सिद्धों एवं नागपंथियों के कारण वहाँ का लोक जीवन तंत्र-मंत्र से गहरे प्रभावित रहा, यहाँ तक कि कुछ मंदिरों में नर बलि तक दी जाती थी। धर्म के नाम पर समाज में अंधविश्वास एवं व्यभिचार का बोलबाला था। इससे लोगों की आस्था धर्म से उठने लगी थी। इन्हीं परिस्थितियों में शंकरदेव का आविर्भाव हुआ। उन्होंने शाक्त संप्रदाय में चली आ रही बलि पूजा और तांत्रिकों तथा कर्मकांडी ब्राह्मणों का विरोध किया। उन्होंने बहुदेव पूजा और तंत्र-मंत्र का खंडन करते हुए ‘एक शरण नाम धर्म को प्रचारित किया। इसमें भक्ति-भावना के साथ सामाजिक और मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठापना की गई। माधवदेव को शंकरदेव ने आध्यात्मिक और धार्मिक गुरु होने के नाते वैष्णव सूत्रों और आदेशों की दीक्षा दी। अपनी अंतिम यात्रा के प्रस्थान से पूर्व उन्होंने माधवदेव को असम के वैष्णव समुदाय के नेतृत्व के लिए अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। माधवदेव को असमिया भाषा का सूरदास कहा जाता है। सूरदास की ही तरह ये श्रीकृष्ण लीला के एकनिष्ठ गायक एवं भक्त थे।
माधवदेव का जन्म असम के लखीमपुर ज़िले की लेटेकुपुखुरी गाँव में सन् 1489 ई. में हुआ। उनके पिता का नाम गोविंद गिरि और माँ का नाम मनोरमा देवी था। माधवदेव का आरंभिक जीवन बहुत ही ग़रीबी में कष्टपूर्वक व्यतीत हुआ। आजीविका की तलाश में परिवार को जगह-जगह भटकना पड़ा। बाद में बान्दुका नामक स्थान पर राजेन्द्र अध्यापक की पाठशाला में भर्ती होकर उन्होंने भागवत पुराण, न्याय, तर्कशास्त्र, संस्कृत काव्य, व्याकरण का अध्ययन किया। पिता की मृत्यु हो जाने पर परिवार का बोझ उन पर आ पड़ा, तथा जीवन-यापन के लिए उन्हें व्यवसाय भी करना पड़ा। इस बीच वे विभिन्न स्थानों का परिभ्रमण भी करते रहे।
माधवदेव की आस्था शाक्त परंपरा में थी, जिसमें देवी के समक्ष बलि तक दी जाती थी। उनके बहनोई गयापाणी परम वैष्णव थे। उन्होंने ही यह कहते हुए माधवदेव को शंकरदेव से मिलवाया कि उनके धर्म संबंधी तर्कों का उचित उत्तर वही दे सकते हैं, जिन्होंने असम में नवीन वैष्णव आस्था का प्रचार किया है। माधवदेव के साथ शास्त्रार्थ करते हुए शंकरदेव ने निवृत्ति मार्ग को श्रेष्ठ सिद्ध किया और अद्वैत ब्रह्म विष्णु के अवतार श्रीकृष्ण की महत्ता स्थापित की।
माधवदेव ने शंकरदेव द्वारा प्रवर्तित नव वैष्णव पंथ का प्राणपण से प्रचार-प्रसार किया। 1568 में अपने गुरु के स्वर्गवास के बाद उनके उत्तराधिकारी के रूप में पंथ की सांगठनिक व्यवस्था न केवल सुदृढ़ की बल्कि उसे एक व्यावहारिक रूप भी दिया। पंथ के विभिन्न कार्यों–धर्म प्रवर्तन, प्रवचन, सामूहिक प्रार्थना सेवा, नाट्य प्रस्तुति आदि के लिए अपने बारह शिष्यों का चयन कर प्रदेश के विभिन्न भागों में भेजा। उन्होंने वैष्णव मठों की तरह ही प्रतिष्ठानों, सत्रों को स्थापित किया और समाज के सभी वर्गों में किसी तरह का विभेद किए बग़ैर पंथ की शिक्षाओं एवं आदर्शों का प्रचार किया। उनमें अद्भुत संगठन क्षमता थी, साथ ही साहित्य रचना में निष्णात एवं संगीत में प्रवीण थे। अपने इन्हीं गुणों के कारण वे इस नव प्रवर्तित पंथ को स्थायित्व देने और उसे लोकप्रिय बनाने में सफल रहे। अपने निर्देशन में उन्होंने बरपेटा में एक नए सत्र का निर्माण कराया। प्रार्थना भवन के चारों तरफ़ ‘गृहस्थ एवं ब्रह्मचारी उपासकों’ के लिए अलग-अलग कुटीर बनवाए तथा झील पर उनके लिए अलग-अलग घाटों का भी निर्माण कराया। सत्र के व्यवस्थित संचालन के लिए एक उपभोक्ता भंडार की शुरुआत की गई और सत्र के विभिन्न कार्यों के लिए कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की गई।
माधवदेव ने सत्र में एक नई परंपरा का शुभारंभ किया। वह था किसी देव प्रतिमा के स्थान पर शंकरदेव या उनकी अपनी किसी महत्त्वपूर्ण भक्ति-रचना की पूजा। इसे ‘गुरु आसन की पूजा’ कहा जाता था। इसके लिए शंकरदेव द्वारा असमिया में रूपांतरित ‘भागवत पुराण’ अथवा माधवदेव कृत ‘नामघोष’ या ‘भक्ति रत्नावली’ को मान्यता दी गई थी। इस प्रकार आराध्य देव की प्रतिमा या चित्र की जगह पवित्र ग्रंथों की पूजा को चलन में लाने का श्रेय माधवदेव को जाता है। धार्मिक ग्रंथों की पूजा अथवा उनके प्रति श्रद्धा भाव जताना जैन, सिख और दादू पंथ में भी है। लेकिन सिखों के ग्रंथ-साहिब की तरह आसन पर रखी पोथी की औपचारिक पूजा नहीं की जाती बल्कि उसमें पवित्र ग्रंथ के प्रति श्रद्धा का भाव अंतर्निहित रहता है।
मध्यकालीन संतों और पंथ प्रवर्तकों में अधिकांश संगीतकार, कवि और सर्जक थे। कबीर, मीराबाई, तुकाराम, नामदेव आदि ने अपने मधुर गीतों से आमजन को अनुप्राणित किया था। माधवदेव भी अपने गुरु की तरह विख्यात संगीतज्ञ थे। उन्होंने एक सौ इक्यानवे भक्ति गीतों की रचना की थी जिनमें से डेढ़ सौ के लगभग आज भी वैष्णव मंडलियों में प्रचलित हैं और इनका गायन होता है। ये विभिन्न शास्त्रीय रागों में निबद्ध हैं और इन्हें बड़गीत के नाम से जाना जाता है।
माधवदेव की रंगमंच और नाटक में गहरी रुचि थी। उनके द्वारा रचित छह नाटकों का उल्लेख मिलता है। लेकिन उनके नाटकों की संख्या को लेकर विवाद है। परंपरा में यह माना जाता है कि उन्होंने अपने दो नाटकों–‘गोवर्धन यात्रा’ और ‘राम यात्रा’ की प्रस्तुतियों का स्वयं निर्देशन किया था जो अब अप्राप्य हैं। कुछ विद्वान उनके इन विलुप्त नाटकों को छोड़कर उनके नाटकों की संख्या नौ और कुछ बारह तक मानते हैं। सत्येन्द्र नाथ शर्मा का मानना है कि ‘शंकरदेव की नाट्य परंपरा को माधव ने इस समर्थ रूप में आगे बढ़ाया कि वह आज भी जीवंत बनी हुई है। एक कलाकार के रूप में माधवदेव ने असम के साहित्य पर अपने सृजन एवं सामर्थ्य का अमिट एवं चिर प्रकाशमान प्रभाव छोड़ा है। उनकी साहित्यिक कृतियों को 1. काव्य, 2. भक्ति संकलन तथा अनुवाद, 3. नाटक तथा 4. उपासना-गीत की चार श्रेणियों में बाँटा जा सकता है। ‘आदिकांड’ (रामायण) तथा ‘राजस्य काव्य’ पहली श्रेणी में आते हैं, जबकि ‘भक्ति-रत्नावली’, ‘नाम मल्लिका’, ‘नामघोष’ तथा ‘जन्म-रहस्य’ को दूसरी श्रेणी में रखा जा सकता है।’
‘आदिकांड’ रामायण के आदिकांड का असमिया अनुवाद है, जबकि ‘भक्ति रत्नावली’ विष्णु संन्यासी की कृति का असमिया अनुवाद।
माधवदेव रचित गीतों को तीन वर्गों में विभाजित किया गया है : 1. विनय और 2. प्रार्थनापरक गीत और 3. कृष्ण लीला विषयक गीत। विनय और प्रार्थनापरक गीतों में माधवदेव का दैन्य भाव परिलक्षित होता है। इन गीतों में ‘हीन’, ‘परम मुरूख’, ‘दास’, ‘दीनमति’, ‘अधम’, ‘शठ’, ‘पामर’, ‘मंदमति’, ‘जड़’, आदि शब्द बार-बार आए हैं जो उनके दास्य भाव की भक्ति को प्रकट करते हैं। उन्होंने अपना सर्वस्व श्रीकृष्ण के भरोसे छोड़ रखा है और प्रभु चरणों में उनकी अटूट आस्था है। दूसरी तरह के गीतों में श्रीकृष्ण के रूप-सौंदर्य का वर्णन है। उनके दर्शन मात्र से मन आह्लादित हो जाता है। तीसरे प्रकार के गीतों में श्रीकृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। कृष्ण के बालरूप के चित्रण में वे सूरदास के समतुल्य हैं और उन्हीं की तरह वात्सल्य रस का कोना-कोना झाँक आए हैं। माधवदेव के काव्य की विशेषता बताते हुए डॉ. कृष्ण नारायण मागध लिखते हैं : ‘गीतिकाव्य का संपूर्ण माधुर्य माधवदेव के गीतों में प्राप्त है। दैन्य और आत्मनिवेदन के गीत जहाँ हृदय को बेधते हैं, वहीं कृष्ण की बाल लीला से संबंधित पद्य नवीन रूप में उल्लसित भी करते हैं। कृष्ण की चतुराई, ढिठाई, बतकरई, बहानेबाज़ी, छेड़छाड़, ज़िद, होड़ा होड़ी आदि ऐसी अनेक मनोहारी चेष्टाएँ हैं, जिनके निरूपण और अंकन में माधवदेव का कवि कर्म और कौशल अष्टछाप शिरोमणि सूरदास से भी टक्कर लेता प्रतीत होता है।’
माधवदेव द्वारा बड़गीतों एवं नाटकों में प्रयुक्त भाषा की अपनी विशिष्टता है। असमिया से भिन्न इस भाषा को ब्रजबुलि या ब्रजावली कहा गया। इसके नाम से भान होता है कि शायद यह ब्रज प्रदेश में बोली जानेवाली ब्रजभाषा है, लेकिन ऐसा नहीं है। बापचंद महंत ने इसीलिए इसे ‘ब्रजबुलि’ न कहकर ब्रजावली कहा है। ब्रजबुलि का साहित्य पंद्रहवीं और सोलहवीं सदी में बंगाल में पल्लवित एवं पुष्पित हुआ। डॉ. सुकुमार सेन ब्रजबुलि की उत्पत्ति ब्रजावली बोली से मानते हैं। उनका कहना है कि माधवदेव ने सोलहवीं सदी के मध्य भाग में वैष्णव पदावली की भाषा के लिए ‘ब्रजावली’ का प्रयोग किया। इसमें ब्रजभाषा के शब्दों का भी समावेश है। इसका कारण यह माना गया कि गौड़ीय वैष्णवों की एक शाखा बंगाल से जाकर ब्रज प्रदेश में निवास करने लगी थी। इस संबंध के कारण ब्रज के शब्द ब्रजबुलि में आ गए।
विद्वानों का एक वर्ग यह भी मानता है कि ब्रजबुलि की उत्पत्ति अवहट्ट से हुई और इस पर मैथिली आदि स्थानीय भाषाओं का प्रभाव पड़ा। वैष्णव पदावली का प्रमुख वर्ण्य विषय राधा-कृष्ण लीला है जो संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश से होते हुए लोक साहित्य में आई। डॉ. कणिका तोमर मैथिली के उमापति ओझा और विद्यापति को ब्रजबुलि का जनक मानती हैं। उनका कहना है कि पूर्वी अवहट्ट के बीज को मैथिली के वारि सिंचन द्वारा पनपाया गया और यही कारण है कि मैथिली के साथ ब्रजबुलि का घनिष्ठ संबंध है।
असम में ब्रजबुलि के विकास का एक प्रमुख कारण था महाकवि शंकरदेव का मैथिली भाषियों से सीधा संबंध। अपनी तीर्थ यात्रा के क्रम में उन्होंने पाया कि वैष्णव धर्म के प्रसार में ब्रजबुलि तथा मैथिली की बड़ी भूमिका है, अतः असम में वैष्णव धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने और उनके अनुयायियों ने इनका आश्रय लिया और प्रचुर मात्रा में ब्रजबुलि साहित्य की रचना की। यहाँ पर ये गीत विद्यापति के अनुकरण में लिखे गए। असम में बड़गीत और नाटकों द्वारा ब्रजबुलि साहित्य का विकास और प्रसार हुआ। इन्हें रचने वालों में शंकरदेव और माधवदेव अग्रणी हैं।
माधवदेव धर्माचार्य हैं, धर्मोपदेशक हैं, समाज सुधारक हैं, नाटककार, कवि और संगीतज्ञ हैं। असमिया साहित्य में अपने गीतों और लघु नाटकों के लिए वे चिरंजीवी बने रहेंगे। माधवदेव का तत्वज्ञान और उनकी भक्ति का मूल स्वर मानवतावादी है। माधुर्य, रस, छंद, अलंकार आदि की कसौटी पर उनकी रचनाएँ कालजयी ठहरती हैं।
माधवदेव सोलहवीं सदी में असमिया के प्रमुख रचनाकारों में से एक हैं। सोलहवीं सदी के भारतीय साहित्य पर दृष्टि डालें तो पाएँगे कि मुख्य रूप से वह भक्तिकाव्य है। इसके कारण समूचे देश में एक सांस्कृतिक चेतना का प्रसार हुआ। दक्षिण से प्रादुर्भूत यह चेतना वृंदावन में आकर नवीकृत हुई। सातवीं सदी में दक्षिण से प्रारंभ हुई भक्ति की यह यात्रा सोलहवीं सदी में वृंदावन आकर नया रूप ग्रहण करती है। ध्यान देने की बात यह है कि यह चेतना संस्कृत भाषा के माध्यम से नहीं, बल्कि भारतीय भाषाओं के माध्यम से आती है।
भक्ति काव्य के प्रमुख आधार ग्रंथ संस्कृत के थे। ये वेदांत और उसकी विभिन्न शाखाओं से संबंधित ग्रंथ थे। शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य जैसे आचार्यों की विचारधारा से भक्ति काव्य प्रभावित रहा। ग्रंथों में भगवद् गीता, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, भागवत पुराण आदि का प्रभाव था। वाल्मीकि रामायण और महाभारत भी भक्तिकाव्य के प्रेरणा-स्रोत रहे। भिन्न-भिन्न भाषाओं में लिखे जाने के बावजूद उनका मूल स्वर एक है, जिससे आम जन ने जीवनी-शक्ति ग्रहण की है।
चैतन्य महाप्रभु (सन् 1486-1534 ई.) ने भक्ति-भाव को अपने जीवन का अंग बनाया। उनके परम आराध्य श्रीकृष्ण थे। उनकी भक्ति भावना को देखकर लोग उन्हें श्रीकृष्ण ही मानते थे। उन्होंने वृंदावनधाम की यात्रा की और वहाँ जाकर ब्रज की धूल को माथे से लगाकर भावलीन हो गए। उन्होंने ओड़िशा, बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश की यात्राएँ की और जनजीवन में भक्ति भाव को प्रचारित-प्रसारित किया।
गुरु नानक (1469-1539 ई.) का समय पंद्रहवीं सदी का उत्तरार्ध और सोलहवीं सदी का पूर्वार्द्ध है। उन्होंने आध्यात्मिक जीवन को सर्वोपरि माना और जनता की भाषा में अपने को अभिव्यक्त किया। उनकी मूलवाणी पंजाबी में है, लेकिन उसमें अनेक भाषाएँ सम्मिलित हैं। उन्होंने अनेक धर्माचार्यों, फ़क़ीरों से धर्म-समागम कर एक समन्वयकारी मानव-पथ प्रशस्त किया। ‘गुरु ग्रंथ साहिब’ गुरु वाणी अनेक राग-रागिनियों पर आधारित है। वे सिख पंथ के आधार स्तंभ थे। उन्होंने अपने समकालीन अन्य संतों की तरह सामाजिक कुरीतियों, पाखंड तथा धर्म के नाम पर होनेवाले अनाचार का विरोध किया और लोगों को अध्यात्म की दिशा में प्रेरित किया।
अगर हम व्यापक रूप से विचार करें तो पाएँगे कि भक्ति काव्य के साथ संगीत का घनिष्ठ संबंध रहा है। मुख्य रूप से यह गीति काव्य है और गेय है। अधिकांश संत संगीत से परिचित हैं ओर उनकी रचनाएँ राग-रागनियों में निबद्ध हैं। संतों ने काव्य रचना तो की ही है, उसे गाया भी है। पूरे भारतवर्ष में ऐसे संत हुए हैं। सूरदास अपने पदों का गायन करते थे। ऐसे ही मीरा भी अपने पदों को गाती थीं। तुलसी और भक्त कवियों की रचनाएँ भी गेय हैं। दक्षिण में कनकदास और पुरंदरदास भी गायक थे। वस्तुतः भक्ति काव्य गाते हुए पढ़ा जाता है। कीर्तन, भजन, नामस्मरण की परंपरा अद्यावाही प्रवरमान है।
हिंदी में भक्तिकाल के चार महाकवि माने जाते हैं–कबीर, मलिक मुहम्मद जायसी, तुलसीदास और सूरदास। ये हिंदी के क्लासिकल कवि माने जाते हैं और हिंदी के कवि होने पर भी इनकी भाषाएँ अलग-अलग हैं। कबीर के काव्य में खड़ी बोली के रूप मिलते हैं। वे एक ऐसे एकेश्वरवाद की स्थापना करते हैं जिसमें ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण है लेकिन धार्मिक अनुष्ठानों को नकारा गया है। वे अवतारवाद की आलोचना करते हैं और मनुष्य की स्वतंत्रता के पक्षधर हैं। कबीर महान संत और समाज सुधारक के साथ अनुपम कवि भी हैं। डॉ. मैनेजर पांडेय का मानना है : ‘कबीर की भक्ति भावना, नैतिक चेतना और सामाजिक विवेक में बौद्धों, सिद्धों, नाथों, सूफ़ियों की विचारधाराएँ आकर मिलती हैं तो उससे निर्गुण और सगुण भक्ति की अनेक धाराएँ निकलती भी हैं। कबीर को सूफ़ी कवि जायसी आदर के साथ याद करते हैं और रविदास, दादू, धन्ना आदि उनका महत्त्व स्वीकार करते हैं। मीराबाई की भक्तिभावना और कविता पर कबीर का गहरा प्रभाव है।’
भक्त कवियों में जैसी व्यापक लोक स्वीकृति तुलसीदास को मिली, वैसी अन्य किसी को भी नहीं। उनका ‘रामचरितमानस’ भारतीय संस्कृति और वाड्मय का मेरूदंड है। यह भारतीय जनमानस में इस तरह परिव्याप्त है कि लोग उनकी चौपाइयों को रोज़मर्रा के जीवन में कहावतों की तरह प्रयुक्त करते हैं। उनकी अन्य कृतियाँ भी अपने आप में विशिष्ट हैं। उन्हें सोलहवीं सदी का हिंदी का प्रतिनिधि कवि माना जाता है।
सूरदास ब्रजभाषा के प्रमुख भक्त कवि हैं और उन्होंने पहले से चली आ रही ब्रज भाषा को अधिक व्यंजनापूर्ण बनाया और उसे परिष्कृत किया। उन्होंने काव्य भाषा की जो परंपरा निर्मित की वह लगभग चार सौ वर्षों तक प्रवाहमान रही। उनका प्रामणिक ग्रंथ ‘सूरसागर’ है। प्रेम और भक्ति उनकी कविता के केंद्रीय तत्व हैं। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने उनकी कविता की प्रशंसा करते हुए लिखा कि ‘वात्सल्य और शृंगार के क्षेत्र में तो इस महाकवि ने औरों के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं।’
उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का एक सुदीर्घ इतिहास है। इसमें मीरा, रैदास, मलूकदास, रज्जन और सुंदरदास आदि सगुण-निर्गुण शाखा के संत शामिल हैं। इनमें से अनेक संतों के नाम से उनके पंथ बने, जो अब भी अपनी विशिष्ट पद्धति से चल रहे हैं। यह कहा जा सकता है कि भक्ति आंदोलन ने पूरे भारतवर्ष को आंदोलित किया और उसकी रसधारा ने जन-समाज को निमज्जित किया।