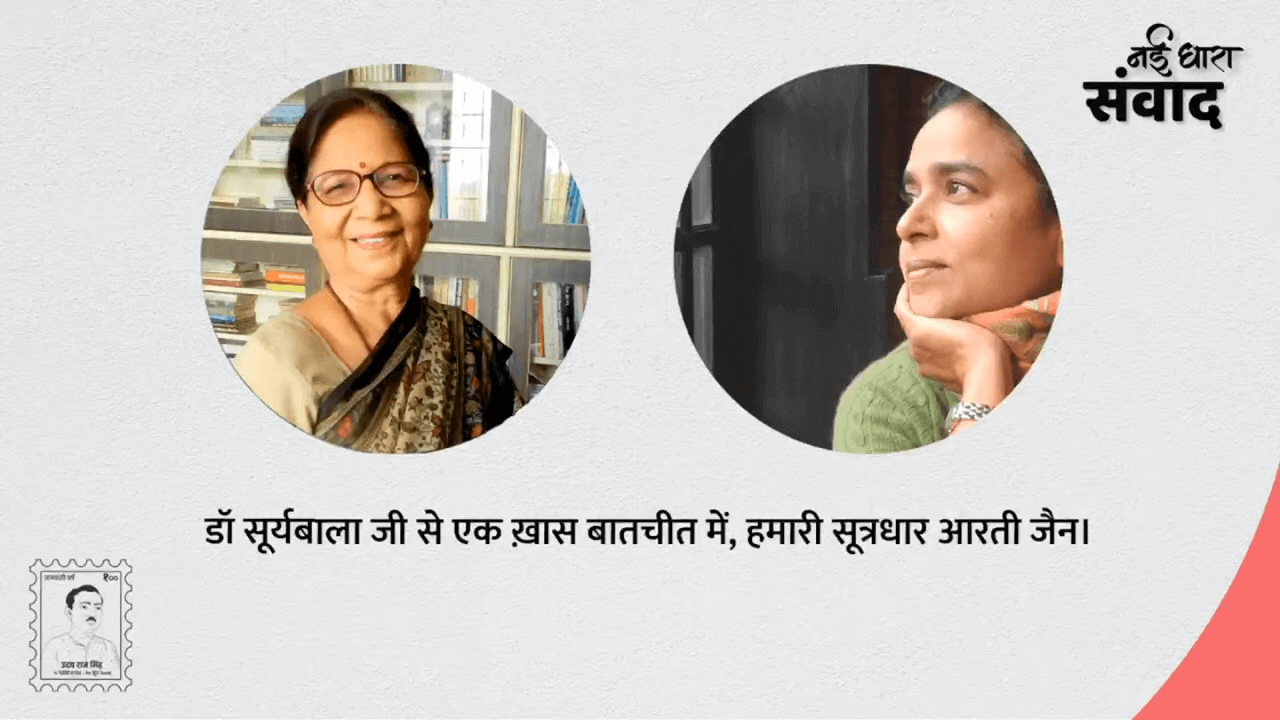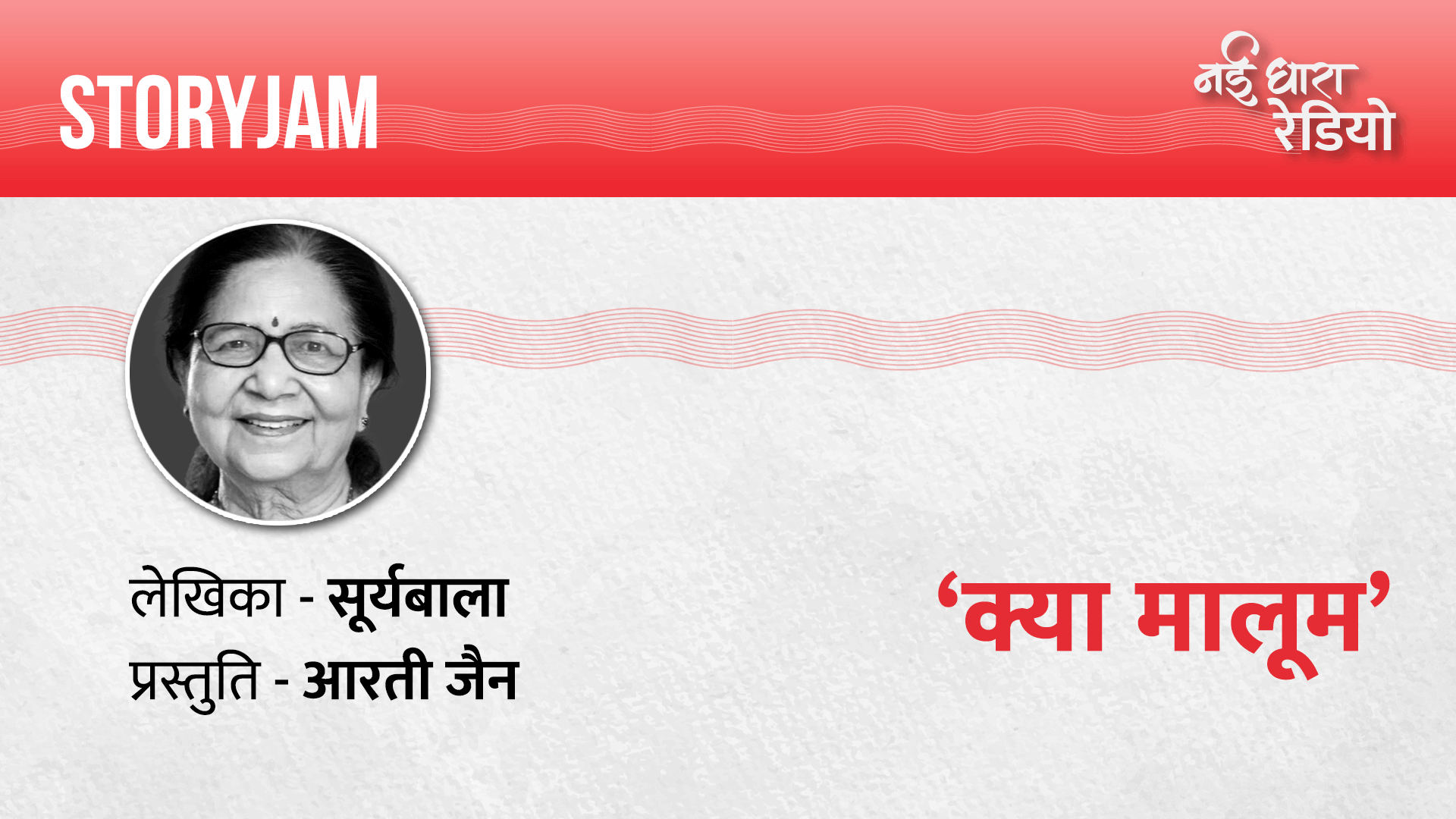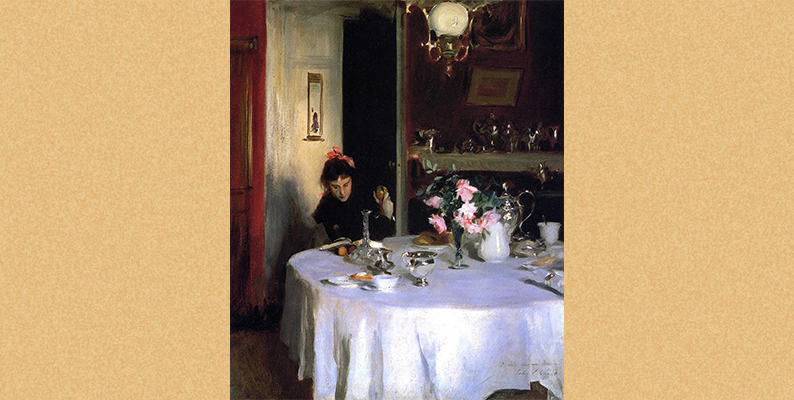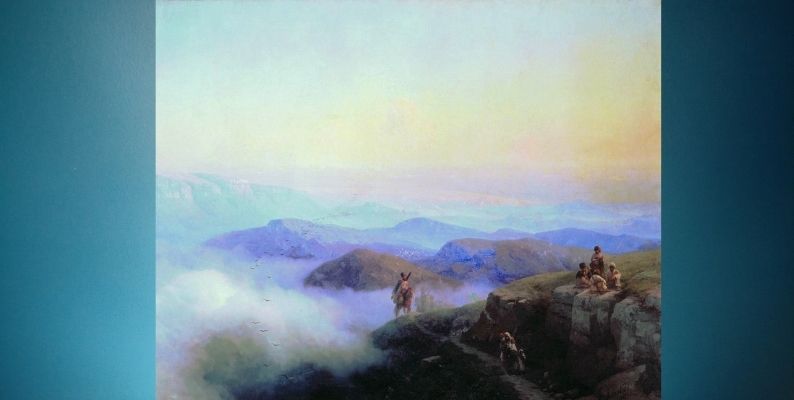यादों में पिता
शेयर करे close
शेयर करे close
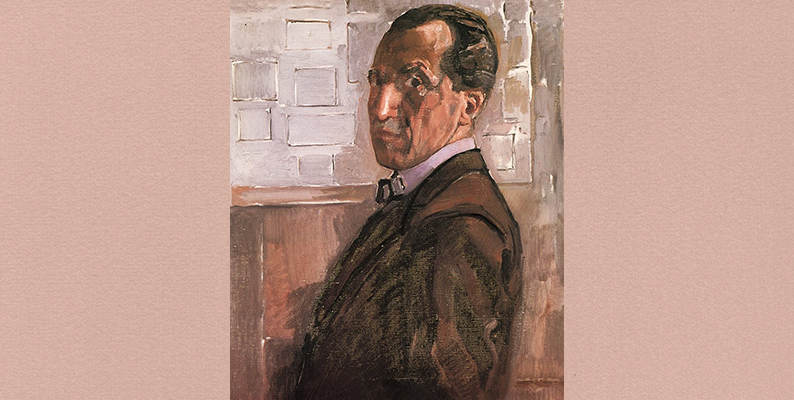
शेयर करे close
- 1 April, 2021
यादों में पिता
‘डिप साब’ बोले तो वही, जिला-विद्यालय-निरीक्षक अँग्रेज़ी के ज़माने वाले डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ़ स्कूल्स…एक मध्यम वर्ग का सरकारी मुलाज़िम ही…लेकिन रुतबा और शौक़, रजवाड़ों को मात करने वाला। शायद यह शहर के ही उच्च वर्गीय तरक़्क़ी पसंद रईसज़ादों की सोहबत और दोस्ती का असर रहा हो…जैसे राय साहब टोडरमल के छोटे भाई बीरबल…जिनकी हवेलीनुमा कोठियों के आयोजनों और शुभकार्यों में नामी-गिरामी गायिकाएँ, नर्तकियाँ बक़ायदे पर्देदारी में शिरकत करने के लिए ससम्मान बुलाई जाती थीं। (बाद की एकाध राय साहब की संरक्षिता की वंशजाओं में सुप्रसिद्ध ठुमरी गायिका सिद्धेश्वरी देवी, अलखनंदा जैसी उस ज़माने की प्रख्यात कत्थक नर्तकियों का शुमार था।)
बहरहाल, ‘डिप साब’ ने उन रजवाड़ों से सिर्फ़ सुरुचि और कलात्मकता का ही सलीक़ा सीखा था। बाक़ी की अच्छा खाने, अच्छा ही पहनने, अच्छे गीत-संगीत, (हारमोनियम बाँसुरी) सुरुचिपूर्ण साज-सज्जा और सलीक़े की शौक़ीनी उनके अपने स्वभाव की देन थी। ज़िंदादिल और वाक्पटु इतने कि तिहाई सदी पहले के उनके कई मौलिक जुमले आज तक कुटुंब के परिहासी मुहावरे बने हुए हैं। जैसे किसी अतिअशिष्ट, उजड्ड की बात चलने पर–कौन? फ़लाना? उसे तो पूँछ लगा दो तो पेड़ पर चढ़ जाए…यानी? …कि थोड़ी सी कसर है बाक़ी…सुनने वाला ठठा कर हँसता…
परिहासी कटाक्ष की ऐसी-ऐसी बानगी, उनकी विदग्धता की प्रतीक तो होती ही, उनकी हद की अनुशासन प्रियता और नो-नॉनसेंस की तरफ़ भी बक़ायदे इशारा कर देती। बारीकी से ही पर प्रतिरोधी पर ताने तिश्नों के वाक् प्रहारों से भी चूकते नहीं थे…लेकिन उतनी ही शाइस्तगी से सामने वाले का वार भी हँसते-हँसते झेल ले जाने की कूबत रखते थे। (बशर्ते वह सही हो…) अपनी चूकों पर खुलकर क्षमा माँगना भी उन्हें आता था, चाहे प्रतिवादी उनसे बारह वर्ष छोटी उनकी पत्नी और बड़ी, छोटी बेटियाँ ही क्यों न हों।
आज आधी सदी बाद भी, जहाँ एक तरफ़, गुस्से से गरजते-तरजते, पिता की हुँकार मेरे कानों को सहमाती है तो दूसरी तरफ़ सिर्फ़ घंटे-दो-घंटे बाद ही पछतावे से विगलित माँ से माफ़ी माँगते पिता का आर्द्र स्वर भी। लेकिन उसे छोटी उम्र में मुझे यह सब बेहद नागवार गुज़रता था…उनका गरजना तरजना ही नहीं, माफ़ी माँगना भी…मुझे गुस्सैल पिता ही नहीं, माफ़ी माँगने वाले पिता से भी अरुचि और चिढ़ हो जाती थी। लेकिन आज समझ पाई हूँ कि बड़ी-से-बड़ी ग़लती पर किया जाने वाला पश्चाताप ही तो आदमी को मनुष्य बनाता है। फिर पिता, अपने मिज़ाज की ‘नो-नॉनसेंस’ वाली आदत से भी तो लाचार थे।
ये फ़लानी कान पकड़कर खड़ी क्यों हैं भाई?….
उस ज़माने में हम छुटकनियाँ बहनों के आचरण और व्यवहार की पहरेदारी इतनी सतर्कता से की जाती कि कभी भी अपनी किसी अशिष्टता या बेजा हरकत पर (ग़लतियों की गंभीरता के हिसाब से) हममें से कोई भी घर के किसी कोने में कान पकड़ कर खड़ी नज़र आ सकती थी। सज़ा थोड़ी ज़्यादा लंबी होने पर मेरे लिए ही बनी एक छोटी कुर्सी पर मुझे कान पकड़ कर बिठा दिया जाता। यह सज़ा, दीवाल की तरफ़ मुँह कर खड़े होने की मिलती तो फिर भी ग़नीमत होती लेकिन यदि इसकी उल्टी होती, अर्थात सारे आते-जाते लोगों के सामने (होंठों में मुस्कुराते नौकरों-चाकरों तक) हम कान पकड़ कर खड़े या कुर्सी पर बैठे होते तो उस शर्मिंदगी की कल्पना किसी के लिए मुश्किल होगी। कभी-कभी तो कोई मेहमान या दूध, भाजी वाला पूछ भी बैठता–‘ये फ़लानी’ यहाँ कान पकड़ कर खड़ी क्यों है भाई–तब हम पर घड़ों पानी पड़ जाता। लेकिन यह भी याद है कि कुछ देर बीतते-न-बीतते, पिता से गुफ़्तगू करती माँ की आवाज़ आती–‘सुन रहे हैं आप!…’ कहिये तो इन्हें अब माफ़ी दे दी जाए।… इन्होंने ग़लती मान ली है। कह रही हैं कि आगे से कभी फ्रॉक पर स्याही, या नाक में उँगली, या मुँह से ‘हट्ट’ या ‘केदार’ को ‘केदरवा’ नहीं बुलाएँगी।…
तो चलो, भई सज़ा माफ़। ग्लानि और शर्मिंदगी से छुटकारा, बहुत बड़ी राहत होती हमारे लिए। ‘रिहाई’ की घोषणा के साथ ही हम सचमुच दिल से अपने थानेदार पिता के शुक्र-गुज़ार महसूस करते…और दुबारा वैसी ग़लती न करने की क़सम के साथ ख़ुश-ख़ुश भाग निकलते…वह तो बड़ी होने के बाद पता चला कि ‘माफ़ीनामे’ वाली माँ की पेशकश भी, पिता के इशारों पर ही चलाई गई होती। तो वह बचपन बहुत अबोध, भोला और अनुशसित था। बड़ों के आदेश, निर्देश या सलाहों पर उखड़ कर बग़ावत पर नहीं उतरा करता था, और न अपने आपको ‘बड़ों’ से भी ज़्यादा बड़ा और समझदार प्रमाणित करने की ज़िद पर अड़ा होता था। उल्टे उनका किंचित संकोच और लिहाज़, अक्सर ग़लत उठते क़दमों को रोक भी दिया करता था। (अब तो, ‘सॉरी’, बच्चे नहीं, ‘बड़े’ ही ‘सॉरी’ बोलते देखे जाते हैं।)
उस अँधेरी शाम की ख़ौफ़ज़दा याद–बावजूद इस सबके पिता के प्रति विद्रोह या बग़ावत वाली बात मन में कभी नहीं आई…
सिवा उस एक अँधेरी शाम के…
जब सूरज डूबते ‘किदवई’ चाचा अपनी गाड़ी में आए और घर के बाहर खेलती हम तीनों बहनों से ‘डिप साब’ के बारे में पूछने लगे…हमारे कहने पर कि बाबू जी तो दौरे पर गए हैं चाचा जी…
उन्होंने झटपट निर्णय लिया–‘अच्छा-अच्छा…तो आओ तुम तीनों को नुक्कड़ तक की सैर करा लाता हूँ…आ जाओ अंदर…
मैं तो ख़ैर कुल चार की थी लेकिन आठ और दस की बड़ी बहनें भी जब तक कुछ कह पातीं, उनके ड्राइवर ने दरवाज़ा खोल कर हमें अंदर बिठा दिया था। इधर ‘चाचा जी’ का लिहाज़, उधर माँ को न बता पाने का डर। इन सबसे अनजान, किदवई चाचा अपने बेफ़िक्र अंदाज़ में हमें शहर की सड़कों पर घुमाते और बताते जा रहे थे। बीच-बीच में पिछली सीट पर बैठी हम बहनों को नींबू, संतरे की खट्टी-मीठी गोलियाँ भी थमाते जा रहे थे।
भय, अदब और शिष्टाचार की मारी दोनों बड़ी बहनें, बीच-बीच में सहमे शब्दों में, ‘चाचा जी! देर हो रही है…जैसे वाक्य दुहराती जा रही थीं लेकिन किदवई चाचा सगर्व हमें आश्वस्त कर रहे थे–अरे तो कौन तुमलोग अकेली हो बच्चियों, मैं हूँ न!… कह देना, किदवई चाचा के साथ गए थे…
अंततः हम लौटे। सड़क पर पूरा अँधेरा घिर आया था–घर से थोड़ी दूर पर ही रामधारी लालटेन लिए आता दिखाई दिया…(प्रतापगढ़ में तब बिजली नहीं थी…) और कार रोक कर पूछने पर बोला…
‘बहिनी-लोगों को देखने निकले हैं… ‘साहेब’ दौरे से आ गए…’
ओह! हमारे प्राण सूख गए।
पत्तों से काँपते, डर से अधमरे, हम तीनों कार से उतरे।
हमारे अंदर लहर मारती दहशत बेकार नहीं थी। अहाता पार करते-करते पिता की तेज़ गरज सुनाई पड़ने लगी। जैसे पूरे घर में तूफ़ान बरपा हो। माँ से लेकर नौकर, महाराज सब पर गाज गिरी हो। (बहुत बाद में माँ ने हमें बताया था कि स्वाधीनता प्राप्ति के बाद के उन दिनों में हिंदू-मुस्लिम दंगों के भड़कने की गुंजाइश बराबर बनी रहती थी।)
थर-थर काँपती हम तीनों बहनों को हमारे इक्के वाले सईस की किनारे वाली कोठरी से अंदर ले जाया गया। वहीं से माँ की आवाज़ सुनाई दे रही थी हमें–‘कहा न, तीनों बहुत रो रही हैं। कह रही हैं, अब कभी ऐसी ग़लती नहीं होंगी। गुस्सा थूकिये, बच्चियाँ रो रही हैं आपकी…’ उस समय अपनी दोनों रोती बहनों पर मुझे बेतरह तरस आ रहा था। रो मैं भी रही थी लेकिन ज़ाहिर था कि मुख्य अपराधी बड़ी, ‘समझदार’ बहनें ही मानी जा रही थीं।
उस दिन का अपने अंदर उबलता गुस्सा मुझे अभी तक याद है, ज़्यादा अपनी बहनों की बेबसी और लाचारी पर कि उन्हें सफ़ाई देने का मौक़ा क्यों नहीं दिया जा रहा? आपलोगों ने ही तो सिखाई है हमें, बड़ों से मुँह न लगने और जवाब न देने जैसी बातें। किदवई साहब हमें ज़बरदस्ती ले गए और नुक्कड़ तक के बदले टाउनहॉल तक घुमा लाए तो हमारी ग़लती?… हम क्या कार से कूद पड़ते? हमें तो तमाम सारी नसीहतें दी जाती हैं लेकिन इस तरह बेकसूर बच्चियों पर घर के मालिक का गरजना, तरजना और सहमी हुई माँ से लेकर सारे घर पर कहर बरपा देना पिता टाइप बड़ों को शोभा देता है क्या?
गुस्सा माँ के घिघियाने पर भी आ रहा था। समूचा माहौल बेलज़्ज़त और शर्मनाक महसूस हुआ था। साढ़े तीन-चार वर्ष की बच्ची को उससे कहीं ज़्यादा समझ होती है, जितनी बड़े समझते हैं। (फिर से अपनी ‘माय नेम इश ताता’… कहानी याद आ रही है। कहानी में ‘ताता’ की लगभग यही उम्र है।)
ऐसे किसी प्रसंग पर, और प्रसंग तो घटते ही रहते थे, पिता का गुस्सा और हद से गुज़रती अनुशासन-प्रियता मुझे बेहद नागवार गुज़रती, बल्कि अत्याचार लगती। कभी घर के सबसे छोटे बच्चे की देख-रेख के लिए रखे छोटे मुंडु को बीड़ी पीते देख कर, कभी बच्चे को गोद में लिए किसी और लड़के के साथ धागे में कंकड़ बाँध ‘लंगर’ लड़ाते देख कर, तो कभी पानी से भरे ग्लास में उँगली डाल कर लाते देखकर या फिर भूल से उसके मुँह से निकली कोई सड़क छाप गाली सुन कर…कब कौन सा नौकर, किस ग़लती के लिए कितनी निर्दयता से पीटा जाएगा, कोई ठिकाना नहीं था।
नौकर तो नौकर, तय किए से ज़्यादा पैसे माँगे या उदंडता से बोला तो रिक्शे वाला तुरंत पिट गया और बात का जवाब दिया तो चपरासी की छुट्टी…और तो और, स्कूल में उनकी लाड़ली बच्ची को, घंटी बजने के बाद भी, कक्षा में न जाकर बाहर खंभे से खेलती देखकर, अध्यापिका ने हल्की सी ठुनकी दे दी तो अध्यापिका सस्पेंड।…
विरासत में मिली ऐसी उदंड क्रूरताओं की जाने कितनी मिसालें हमारी पीढ़ी की स्मृतियों में दीवालों पर टँगी चीते, भालू की खालों सी दर्ज हैं।
ये बड़े लोग गुस्सा आने पर नौकरों को इस तरह पीटते कि नौकर कम हाँफता, वे ज़्यादा। लेकिन दुनिया का सबसे ममतालु पिता भी था वह–
तो क्या इतना क्रूर था मेरा पिता भी!… लेकिन तब वह अपनी पत्नी, बच्चियों पर ही नहीं, बरामदे में टँगे पिंजरों में चहकती बज्जी और ललमुनियों तक पर इतनी ममता कैसे उड़ेलता था?
यह पिता हर हफ़्ते पिंजरों के ऊपर पानी की धार डालकर, पंखों से पानी छिटकती ललमुनियों को प्यार से निहारता, उनकी कटोरियाँ साफ़ कर दाना चुग्गा डालता, टिहकारते मिठ्ठू को सहलाता देख जा सकता था!
इतना ही क्यों आँगन के हौज़ की नारंगी, चित्तीदार, सुनहरी मछलियों को बग़ल में रखी पानी भरी बाल्टी में डाल कर, गोल पत्थर की पूरी हौज़ी खुरच-खुरच कर साफ़ किया जाता। नया, साफ़ पानी डलवा कर मछलियाँ वापस हौज़ में छोड़ी जातीं। फिर बीचों-बीच का चुनार मिट्टी का ‘मरमेडों’ जैसी आकृति वाला फ़व्वारा चालू किया जाता।
फ़व्वारे से बरसती धारों में भींगने के लिए हमें लालायित देखकर यही पिता, मुस्कुराकर अनुमति भी दे देता।
स्वयं तौलिया बाँधे, रामधारी के साथ पीली, हरी पत्तियों वाले क्रोटन से लेकर पाम क्रोटन गुड़हल तक की गुड़ाई निराई करता। बैठक में सजे, बड़े-बड़े पीतल के स्टैंड वाले गमलों को पॉलिश से चमकाने के निर्देश दिए जाते। अलमारियों में फ़िट आइने पोछे जाते। राजा रवि वर्मा के ‘गंगावतरण’ और हंस से संदेश भेजती ज़री बार्डर की गुलाबी साड़ी वाली दमयंती के चित्रों के फ़्रेम पुछवाए जाते। दरी, कालीने झड़वाई जातीं। माँ इन सबसे पूरी तरह असंपृक्त, आराम से दूसरे कामों में लगी होतीं। यह उनका डिपार्टमेंट नहीं था।
हम बेटियों में किसी को तेज़ बुख़ार होता, यह पिता रात-रातभर आइस-कैंप और ‘माथे पर यूडी क्लोन की ठंडी पट्टी, रखे सिरहाने बैठा रहता। दसियों बार थर्मामीटर से बुख़ार नापता। सन्नाटी रातों में गली से किसी अर्थी के गुज़रने की आवाज़ आते ही वह अग़ल-बग़ल चारपाइयों पर सोई अपनी बच्चियों को थपथपाना नहीं भूलता–‘मैं यही हूँ बेटे, डरने की कोई बात नहीं।’
‘जी-बाबूजी…’ हम सहमी आवाज़ में कहते।
बसंत पंचमी की आधी रात जब इस पिता की अर्थी उठी थी तो सबसे पहले यही याद आया था।…
Image name:Self Portrait
Image Source: WikiArt
Artist: Piet Mondrian
This image is in public domain