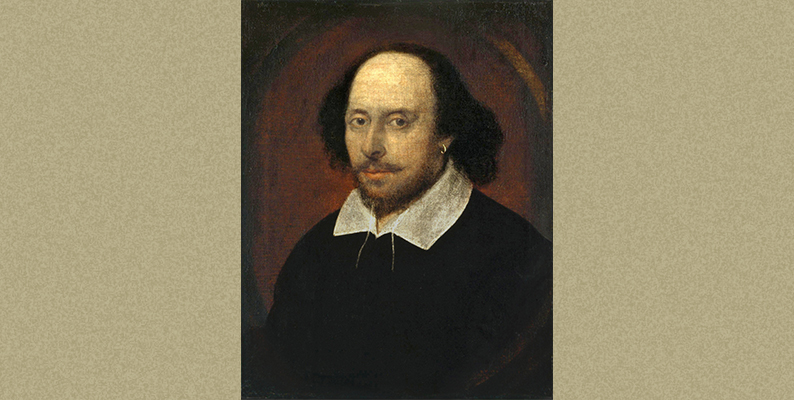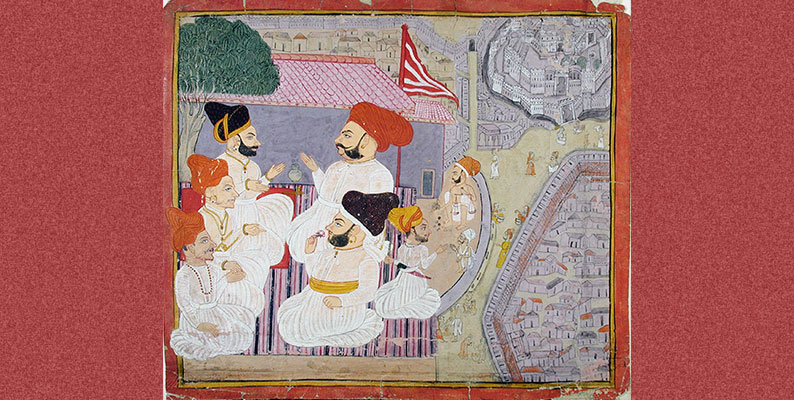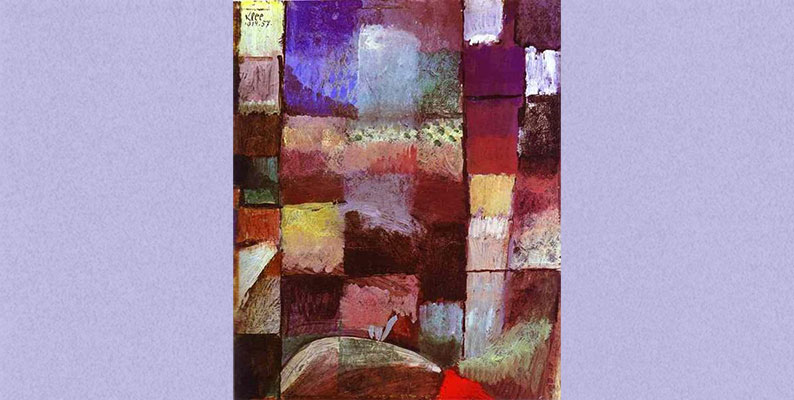हमें यह कहना है!
- 1 August, 1951
शेयर करे close
शेयर करे close

शेयर करे close
- 1 August, 1951
हमें यह कहना है!
श्रावण के साथ दो पावन स्मृतियाँ बँधी हैं–एक तुलसीदास की, दूसरी प्रेमचंद की। दोनों की कलात्मक तुलना की बात नहीं; किंतु दोनों एक बात में बहुत मिलते हैं–जन-जीवन के साथ अपनी कला का निकटतम संपर्क स्थापित करने में। खास कर भाषा के क्षेत्र में। दोनों ने अपनी रचनाओं में जनता की भाषा का विपुल प्रयोग किया। तुलसीदास जी के पहले जन-भाषा का प्रयोग कबीर ने किया था और प्रेमचंद जी के पहले देवकीनंदन खत्री ने। कबीर की साखियाँ अनपढ़ जनता की जबान पर जो पाँच सौ साल पहले चढ़ीं, वे आज तक वहाँ अपना स्थान अक्षुण्ण रखती हैं। देवकीनंदन खत्री की सरल भाषा ने प्रारंभिक दिनों में बहुत लोगों को हिंदी पढ़ने की ओर प्रवृत्त किया। जब गाँधी जी की नजरों में खत्री जी की भाषा आई, तो उसे ही राष्ट्रभाषा के उपयुक्त उन्होंने करार दिया था। किंतु भाषा जब कला का माध्यम बनती है–उच्चकोटि की कला का–तब उसे अपने धरातल को ऊँचा करना ही पड़ता है। कबीर संत थे, खत्री जी तिलस्मी उपन्यासकार। उनका माध्यम सरलतम भाषा भी बन सकती थी। किंतु तुलसी और प्रेमचंद कलाकार थे–उच्चकोटि के कलाकार। अत:, उनकी भाषा ऊँचे स्तर तक गई, किंतु अन्य कलाकारों की तरह उन्होंने अपनी भाषा को मिट्टी के संपर्क से दूर नहीं होने दिया। उनकी भाषा का मूल आधार जन-भाषा ही रही। इसका सुफल भी हमलोगों की आँखों के सामने है। प्राचीन कवियों में जिस प्रकार तुलसीदास जी की सर्वश्रेष्ठता दिन-दिन विकसित होती जा रही है; उसी प्रकार आधुनिक काल के कलाकारों में प्रेमचंद की गरिमा गहरी से गहरी प्रतिष्ठित होती जा रही है। एक उदाहरण लीजिए। हिंदी-संसार अन्य कवियों और लेखकों की जयंतियाँ भी मनाता है; किंतु जिस उत्साह और धूमधाम से इन दोनों की जयंतियाँ मनाई जाती हैं, क्या अन्य अवसरों पर हम वैसा जोश या लगन देख पाते हैं?
जब-जब हम महापुरुषों की जयंतियाँ मनाते हैं, तो उनके कर्तृत्वों का मूल्यांकन करते हैं। यह स्वाभाविक भी है। किंतु यह मूल्यांकन कभी-कभी बहुत अखरता है, जब हम देखते हैं, मौलिकता के फेर में पड़कर उनके व्यक्तित्वों या उनके कर्तृत्वों की कचूमर तक निकालने लगते हैं। ऐसा करने से आलोचक या वक्ता की ओर लोग तुरंत आकृष्ट तो होते हैं, किंतु, लंबी दौर में यह प्रवृत्ति घातक ही सिद्ध होती है। मूल्यांकन हम करें, किंतु, तुलसीदास के आदर्शों के अनुसार संत-हंस गुन गहँहि पय, परिहरि बारि-बिकार। विकारों के पानी को तो हम छोड़ दें, गुण के दूध को ही हम हंस की तरह ग्रहण करें। खास कर ऐसे अवसरों के मूल्यांकनों का लक्ष्य होना चाहिए आलोच्य कलाकारों द्वारा प्रदर्शित नए पथ की ओर अँगुलि-निर्देश! इन्ही दो महान कलाकारों को लीजिए। आज हमारे लिए इनका महत्त्व पहले से बहुत अधिक है। खास कर भाषा के क्षेत्र में यदि हमने इनका अनुसरण छोड़ दिया, जैसी प्रवृत्ति आज दिखाई पड़ती है, तो फिर हिंदी के लिए तो बुरे दिन आने वाले ही हैं। हिंदी पर दो ओर से हमला है। एक तरफ वे लोग हैं, जो उसे जन-जीवन से बिल्कुल पृथक कर एक आकाशी भाषा बनाने पर तुले हैं! संस्कृत को लोग ‘देववाणी’ कहते हैं; सुनते हैं, भारत सरकार रेडियो का हिंदीकरण आकाशवाणी के रूप में कर रही है। किंतु ऐसे लोगों को याद रखना चाहिए कि जिस प्रकार देववाणी बन कर संस्कृत हवा में ही रह गई या पुरानी पोथियों में ही; उसी प्रकार आकाशवाणी बनकर हिंदी भी उसी भाग्य को या दुर्भाग्य को प्राप्त करके ही रहेगी! किंतु ,दूसरी ओर ऐसे भी लोग हैं, जो हिंदी को खामखा चों-चों का मुरब्बा बनाने पर तुले हैं। वे समझते हैं, हिंदी में जितनी ही अधिक विदेशी भाषा ठूसेंगे, वह उतनी ही समृद्ध और शक्तिशाली बनेगी। वे भूल जाते हैं कि शरीर जितना पचा सके, उतना ही भोजन उसके लिए उपादेय होता है–अधिक पुष्टिकर या अधिक मात्रा का भोजन भी हानि ही करता है–विजातीय पदार्थों के ग्रहण की तो बात ही अलग। इस दृष्टि से देखिए, तो तुलसीदास और प्रेमचंद ने हमारे लिए बड़ा ही सुंदर मध्यम मार्ग प्रदर्शित किया है।
साहित्यिक संस्थाओं का संगठन और संचालन किस प्रकार हो, यह प्रश्न आज हिंदी-संसार के सामने पूरी विभीषिका के साथ उपस्थित है। हिंदी-संसार की दो सर्वमान्य संस्थाएँ रही हैं–काशी नागरी प्रचारिणी सभा और हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग। प्रारंभ में ये दोनों संस्थाएँ स्थानीय रहीं जैसा कि इनके नामों से ही प्रगट है। किंतु धीरे-धीरे इनका क्षेत्र हिंदी-संसार भर में फैल गया। खास कर सम्मेलन ने तो विस्तार की दृष्टि से बड़ी उन्नति की। किंतु आज ये दोनों की दोनों संस्थाएँ दलबंदियों के चलते परेशान हो रही हैं। जिन लोगों ने अपने खून और पसीने से काशी नागरी प्रचारिणी सभा को सींचा, उनमें से जो बचे-खुचे लोग रह गए हैं, उनसे पूछिए, तो पता चले किस प्रकार उन्हें खदेड़-खदेड़ कर उस संस्था से अलग किया गया है। सम्मेलन से टंडन जी का पद-त्याग उसके अध:पतन के शीर्षबिंदु की ओर इशारा करता है। क्या हिंदी की ऐसी दो प्रतिष्ठित और सर्वमान्य संस्थाओं की वर्तमान स्थिति हमें यह सोचने को लाचार नहीं करती कि इन संस्थाओं के नींव में ही कोई ऐसी त्रुटि थी, जो अब सारी इमारत को ही खतरे में डालने जा रही है। जब ये संस्थाएँ कायम की गईं, हिंदी अपनी प्रारंभिक अवस्था में थी। उसके विकास और अभ्युदय में, प्रचार और प्रसार में इन संस्थाओं ने बहुत काम किया। उस समय इन संस्थाओं का रूप ऐसा रखा गया कि अधिक से अधिक लोग इनमें सम्मिलित हों, अधिक से अधिक लोगों की सहायता और सहयोग प्राप्त हो। इसलिए स्वभावत: ही इनका रूप भी बहुत कुछ जनतंत्रात्मक रखा गया। उनके इस रूप के कारण नए लोग उनमें आते रहे, इस तरह इन संस्थाओं को नए-नए लोगों की योग्यता और अनुभव से लाभ पहुँचता रहा। किंतु, अब देखा यह जा रहा है कि यह जनतंत्रात्मक रूप दलबंदी का कारण बन रहा है! राजनीति में दलबंदी विकास की ओर ले जाता है। किंतु साहित्य में तो वह विष का ही बीज बोता है, इसे अनुभव ने सिद्ध कर दिया है।
अत: क्या यह सोचने की बात नहीं हो गई है कि हम अपनी साहित्यिक संस्थाओं को कोई नया रूप दें? परिस्थिति में जो एक महान् अंतर आ गया है, उसका भी इसी ओर इशारा है! वह अंतर यह है कि अब राष्ट्रभाषा हो जाने के बाद हिंदी के प्रचार का बहुत बड़ा भार सरकार पर आ गया है और अब इसे उसी के द्वारा हमें कराना भी चाहिए। सरकारी शक्ति और साधनों से यह काम बहुत ही सुगमता और शीघ्रता से किया भी जा सकता है। ऐसी हालत में हमारी साहित्यिक संस्थाओं का प्रमुख कार्य प्राचीन साहित्य का संचयन और नवीन साहित्य का निर्माण या उसका दिशा-निर्देश ही हो सकता है। यह काम वे ही कर सकते हैं जो साहित्यकार हैं। अत: अब हमारी साहित्यिक संस्थाओं का पुनर्संगठन परिषद्–एकेडमी–के रूप में ही करना समयोचित होगा। सुनते हैं, टंडनजी कुछ इसी दिशा में सोच रहे हैं और पटना में नियोजित सम्मेलन की नियमावली समिति के अधिकांश सदस्यों का भी यही अभिमत है। सम्मेलन के स्वरूप में परिवर्तन होते ही उसकी संबद्ध संस्थाओं पर स्वभावत: इसका प्रभाव पड़ेगा। यही नहीं अन्य संस्थाओं को भी पुनर्संगठन की ओर ध्यान देना होगा। यदि नियमावली समिति ने इतना भी कर लिया, तो पटना का विशेष अधिवेशन सम्मेलन के इतिहास में एक नई दिशा के प्रदर्शन का प्रतीक बन जाएगा, इसमें संदेह नहीं।