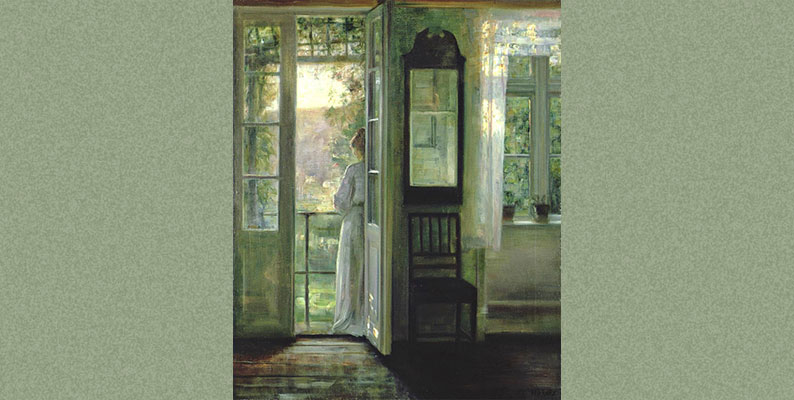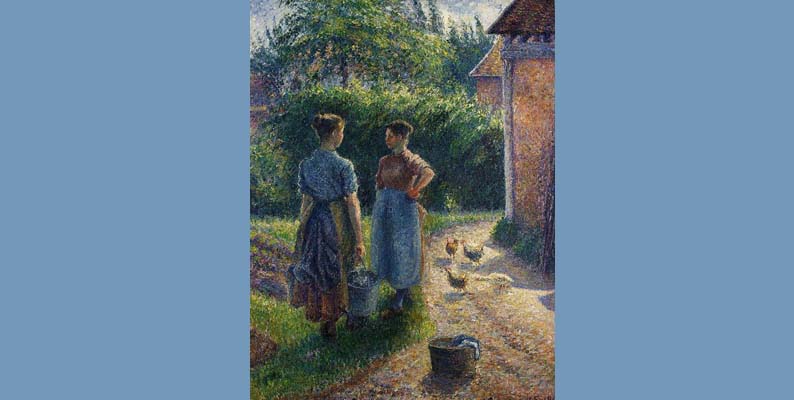अम्बेदकर और दलित हिंदी कविता
- 10 April, 2025
शेयर करे close
शेयर करे close

शेयर करे close
- 10 April, 2025
अम्बेदकर और दलित हिंदी कविता
‘स्वातंत्र्योत्तर हिंदी कविता और नए रचनात्मक सरोकार’ पर विचार करती हूँ तो सबसे पहले यह सवाल खड़ा होता है कि स्वातांत्र्योत्तर हिंदी कविता के नए रचनात्मक सरोकार क्या रहे हैं? आज देश को आजाद हुए कई दशक बीत गए हैं। आजादी की इस लंबी यात्रा में हिंदी कविता ने क्या नई रचनात्मकता पैदा की है? उसके सामाजिक सरोकार क्या रहे हैं? क्योंकि साहित्य समाज का प्रतिबिंब हुआ करता है। कविता साहित्य की एक ईकाई की तरह ही है। हिंदी कविता में क्या बदलाव आए हैं? उसकी क्या जिम्मेदारियाँ रही हैं? उसकी आजादी के बाद के क्या जुड़ाव रहे हैं? इस तरह के बहुत से प्रश्न हैं जो हिंदी कविता के साथ जुड़े हुए हैं। हम इन्हीं प्रश्नों पर यहाँ चर्चा करेंगे।
हम सब यह जानते हैं कि आजादी के बाद इस लंबे अंतराल में समाज का वातावरण बदला है। राजनैतिक बदलाव भी समय-समय पर होते रहे हैं। साहित्य समाज का दर्पण होता है। समाज में जो परिवर्तन होते रहे हैं, वे हमें कविता में भी देखने को मिलते रहे। जिन दिनों देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, उस समय के कवि सीधे-सीधे राष्ट्र के सरोकारों वाली कविताएँ लिख रहे थे। उसमें चाहे मैथलीशरण गुप्त हों, माखनलाल चतुर्वेदी हों या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान हों या कथा साहित्य में प्रेमचंद हों या फिर प्रेमचंदकालीन स्वामी अछूतानंद कवि व पत्रकार और सामाजिक आंदोलनकर्मी हों। इनकी कविताएँ व साहित्य हमें यह बताता है कि साहित्यकार समय सापेक्ष हुआ करता है।
यहाँ हम स्वातंत्र्योत्तर हिंदी कविता में आए नए रचनात्मक सरोकारों पर बात कर रहे हैं। मैंने अपने शोध का विषय रखा है ‘स्वातंत्र्योत्तर हिंदी कविता में नए रचनात्मक सरोकार और हिंदी दलित कविता’, जिस पर विचार करती हूँ तो आजादी के बाद हिंदी दलित कविता में निरंतर नए-नए सरोकार जुड़ते रहे हैं। उनकी विचारधारा साफ तौर पर महात्मा ज्योतिबा फुले, कबीर, रैदास, स्वामी अछूतानंद और डॉ. भीमराव अम्बेडकर के लोकतांत्रिक विचारों से जुड़ती है। उनके सामाजिक आंदोलनों की चेतना हिंदी दलित कविता में स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। इसमें स्त्रियाँ आज के बीसवीं सदी के अंतिम दशक में आकर ही जुड़ पाती हैं। इसका आशय यह नहीं कि स्त्रियाँ इस योग्य ही नहीं थीं। सीधा और बड़ा कारण है कि वे शिक्षा में नहीं थीं। कुछ दलित पुरुष जो थोड़े बहुत शिक्षित हो गए वे ही साहित्य से जुड़ पाए। उन्होंने ही कविताएँ लिखीं। प्रथम दौर में उनकी कविताओं में उनकी सामाजिक, आर्थिक स्थितियाँ ही चित्रित हुई हैं। समयांतराल में उनके कविता के प्रति सरोकार बदलते रहे हैं। हिंदी के सुविख्यात दलित कवि ओमप्रकाश वाल्मीकि अपने पहले कविता संग्रह ‘सदियों के संताप’ जो 1989 में प्रकाशित हुआ था, इस संग्रह के शीर्षक से ही बहुत कुछ स्पष्ट हो जाता है। सदियों का संताप यानी हजारों सालों के दु:ख की अभिव्यक्ति।
उस समय तक दलितों में उपजातियों का द्वंद्व नहीं था। दलित शब्द अपने आप में बहुत बृहद है। सामाजिक व्यवस्था में जिन जातियों को अछूत बनाया गया वे सब इस परिधि में समाहित थीं। उस समय के साहित्यकार ओमप्रकाश वाल्मीकि तक अपने प्रारंभिक दौर में राजनैतिक सरोकारों से मुक्त थे। इसलिए ‘दलित’ शब्द भी एक टूल बन गया था। यह व्यापक अर्थों में प्रयुक्त हो रहा था। दलित साहित्य पर शोध कार्य करने में इन पंक्तियों की लेखिका ने जब जेएनयू से दलित साहित्य पर पहला शोध किया था, तब उपजातियों की चेतना के साहित्यकारों को छाँट कर काम नहीं किया था। आज भी सभी अछूत जातियों के साहित्यकारों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थितियाँ एक सी हैं। उनकी मुक्ति के रास्ते भी एक से ही हैं। सुविख्यात कवि ओमप्रकाश वाल्मीकि जी की कविताओं से कुछ उदाहरण यहाँ प्रस्तुत हैं। ‘मानचित्र’ शीर्षक कविता की कुछ पंक्तियाँ देखें–
‘मेरे जिस्म के मानचित्र पर उभर रहे हैं–बनकर फफोले
कहीं बेलछी
तो कहीं शेरपुर
कहीं पारस बिगहा
तो कहीं नारायणपुर
इन फफोलों को सहलाने के लिए
मेरे हाथ मेरे पास नहीं हैं
वे तो बहुत पहले
मेरे बाप-दादों ने
रख दिए थे गिरवी
किसी सेठ-साहूकार की तिजोरी में
दो मुट्ठी चावल के बदले।’
यहाँ स्पष्ट देखा जा सकता है कि कवि ओमप्रकाश वाल्मीकि सामाजिक सरोकारों से गहरे जुड़े हुए हैं। वाल्मीकि जी की प्रारंभिक कविता डॉ. अम्बेदकर की उस चेतना से जुड़ती है जब वे कहते थे कि ‘गुलाम को गुलामी का अहसास करा दो। वह अपनी मुक्ति की लड़ाई खुद लड़ लेगा।’ वाल्मीकि जी की कविताएँ दलित खासकर वाल्मीकि समाज में हो रहे जातीय भेदभाव और आर्थिक एवं शैक्षिक पिछड़ेपन का अक्स दिखाती है, जो चेतना का कार्य किसी हथियार की तरह ही होता है। इनकी उक्त कविता से एक ऐसा बिंब उभरता है जिसमें समाज में किसी भी तरह से बराबरी नहीं है, सामाजिक रूप से न आर्थिक रूप से। एक मुट्ठी चावल के लिए बाप-दादा कर्जे में डूबे हैं, जिसका दंड बेटा और पोता झेलने को अभिशप्त है। बेलछी, शेरपुर, पारस बिगहा और नारायणपुर सिर्फ जगहों के नाम भर नहीं हैं। ये ऐसे गाँव हैं जहाँ सभी अछूत जातियों की तबाही के पर्याय बन गए हैं। इसी तरह वाल्मीकि जी की ‘ठाकुर का कुआँ’ कविता प्रेमचंद की कहानी ‘ठाकुर का कुआँ’ से आगे की विस्तृत कथा कविता में कह देती है। नमूने के लिए कविता की कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत हैं–
‘चूल्हा मिट्टी का
मिट्टी तालाब की
तालाब ठाकुर का
भूख रोटी की
रोटी बाजरे की
खेत ठाकुर का
बैल ठाकुर का
हल ठाकुर का
हल की मूठ पर हथेली अपनी
फसल ठाकुर की
कुआँ ठाकुर का
पानी ठाकुर का
खेत-खलिहान ठाकुर के
गली-मुहल्ले ठाकुर के
फिर अपना क्या?
गाँव?
शहर?
देश?’
यह कविता अछूत जातियों के लिए पूरे भारत के गाँव का मानचित्र उभार कर रख देती है। यह किसी एक जाति की स्थितियाँ नहीं हैं। समूचे अछूत जातियों का हाल यही है। अपवाद को छोड़ कर। कवि ने ‘ठाकुर’ शब्द का प्रतीकात्मक अर्थ लिया है। वह किसी एक जाति तक सीमित नहीं है। वह शोषक व्यवस्था का प्रतीकात्मक अर्थ बन कर उभरा है, जिसमें अछूत जातियों के लिए गाँव, शहर और देश में कहीं भी कुछ भी नहीं है। इस कविता के माध्यम से कवि सामाजिक सरोकारों से गहरे से जुड़ा है। यह समस्या किसी एक व्यक्ति या किसी जाति विशेष की नहीं है। यह हमारे राष्ट्र के नागरिकों की स्थितियों को दिखाती है। साथ ही यह कविता बहुत कुछ बदलाव की बात भी कहती है। वाल्मीकि जी की यह कविता संग्रह 1989 में छपी अवश्य है, मगर देश के हालात अभी भी जस के तस बने हुए हैं। यदि कहें, और भी बिगड़े हैं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। ओमप्रकाश वाल्मीकि की कविताओं के शीर्षक बोलते हैं। उनके अगले कविता संग्रह का भी शीर्षक है ‘बस्स बहुत हो चुका’ यानी दलित जातियों का उत्पीड़न और उनकी स्थितियाँ बदलते समय में बदल नहीं रही हैं। इसीलिए वे उसे रोकने की बात इस संग्रह में मानो कह रहे हों। बस्स, बहुत हो चुका। इसमें उनका आक्रोश भी दिखाई देता है और उत्पीड़न रोकने की चेतना भी। तभी तो वे इस संग्रह में ‘वे नहीं जानते’ कविता में लिखते हैं–
‘गली-मुहल्लों की गंदगी ढोते-ढोते
भूल जाती है माँ
पीछे छोड़ आई दो मासूम आँखों को
जो टकटकी लगाए
देख रही हैं राह
उसके लौट आने की।’
ये कविताएँ बताती हैं कि समय बदल रहा है, पर दलितों का जीवन नहीं बदला। आजाद भारत में दलित आजाद क्यों नहीं है? ओमप्रकाश वाल्मीकि की कविताएँ लगातार ये सवाल उठा रही हैं। यही उनके सामाजिक सरोकार थे।
स्वातंत्र्योत्तर भारत में ओमप्रकाश वाल्मीकि के अलावा अन्य दलित कवियों के क्या रचनात्मक सरोकार हैं? मैंने शोध की दृष्टि से उनकी भी पड़ताल की है। नमूने के लिए मैं यहाँ कुछ अन्य कवियों की कविताओं का उदाहरण प्रस्तुत करूँगी। सर्वप्रथम डॉ. धर्मवीर की ‘भारत का मोहन चमार’ शीर्षक कविता की पंक्तियाँ देखें–
‘वह भारत का मोहन चमार है
बत्तीसी बाहर को और आँखें भीतर को
सिर सिद्ध किया हुआ शमशान
पूरा शरीर नर-कंकाल
चलता-फिरता अस्थियों का अजायबघर
छुआ-छूत का विज्ञापन
बेलता-चलता, निर्धनता का प्रचार।’
यहाँ डॉ. धर्मवीर के कवि की रचनात्मकता के सरोकार स्वतंत्रता के बाद भारत में चमार जाति के लोगों की स्थिति का एक नमूना पेश करना है कि आजाद भारत में चमार किन हालातों में जीने को विवश है। उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से काव्य सौंदर्य को भी बनाए रखा इस कविता में और सहजता भी नहीं छोड़ी है। हम यहाँ कह सकते हैं कि कविता के क्षेत्र में विषय और रचनात्मकता दोनों ही दृष्टियों से नयापन है, जो आलोचकों, समीक्षकों और पाठकों को सोचने को और नए तरह से विमर्श करने के लिए मानस तैयार कर देते हैं। दलित साहित्य में हर कवि एक तरह से नहीं सोच रहा है और न लिख रहा है। उसकी सोच और प्रस्तुति में भी अंतर देखने को मिलता रहा है। जहाँ उपर्युक्त कविताओं में दलितों की सामाजिक और आर्थिक स्थितियों का चित्रण हुआ है तो श्यौराज सिंह बेचैन के सरोकार इससे आगे भी जाते हैं। वे दलितों की सामाजिक और आर्थिक स्थितियों के साथ-साथ उनकी शैक्षिक स्थितियों और मनःस्थितियों को भी कविता में पिरोते रहे हैं। उनकी कविता की कुछ बानगी देखें–
‘सुन बहिना!
मेरे जियरबा की बात
उदासी मेरे मन बसी…
मैं न पढ़ी, न
मेरे बालका
शोषण करे हैं
मेरे मालिका
मोइ न मिल्यौ री
स्वराज।’
एक अन्य कविता में स्त्री की व्यथा इस प्रकार चित्रित हुई है। उसकी कुछ पंक्तियाँ यहाँ प्रस्तुत हैं–
‘किसी आँख में लहू है
किसी आँख में पानी है
औरत की गुलामी भी
एक लंबी कहानी है।’
कवि श्यौराज सिंह बेचैन की ये दोनों कविताएँ 1987 में ‘नई फसल’ उनके कविता संग्रह में प्रकाशित हुई थीं। इधर इसे पुनः ‘नई फसल और कुछ अन्य कविताएँ’ शीर्षक से प्रकाशित किया है। इस बीच समयातंराल लंबा है मगर कविता की विषय-वस्तु ऐसी जान पड़ती है कि यह आज के परिवेश में लिखी गई कविताएँ हैं। गाँव में शिक्षा का स्तर और गिरा है। आर्थिक शोषण का स्तर भी बढ़ा है। गाँव में रहने वाली शोषित, वंचित, उपेक्षित और पिछड़े समाज की स्त्रियों को न शिक्षा मिल पा रही है और न उनकी आर्थिक और सामाजिक गुलामी कम हुई है। वह आजाद गुलाम है। स्त्री के बारे में यह अभिव्यक्ति तो एक पुरुष कवि की थी। स्वयं स्त्री क्या सोचती है। मेरे मन में हमेशा यह जानने की जिज्ञासा रहती है कि क्या दलित स्त्री की अभिव्यक्ति पुरुष की अभिव्यक्ति से अलग है? या उसी जैसी ही है? दरअसल दलित स्त्री की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थितियाँ पुरुष से अलग है ही नहीं। उसका जीवन उससे भी बदतर है। सुशीला टाकभौरे जानी-पहचानी कवयित्री रही हैं। उनकी कविता की कुछ पंक्तियाँ नमूने के लिए यहाँ प्रस्तुत हैं। वे ‘स्त्री’ शीर्षक कविता में लिखती हैं–
‘एक स्त्री
अब भी कोई कोशिश करती है
लिखने की, बोलने की, समझने की,
सदा भयभीत सी रहती है
मानो
पहरेदारी करता हुआ
कोई
सिर पर सवार हो,
पहरेदार,
जैसे एक मजदूर औरत के लिए
ठेकेदार
या खरीदी संपत्ति के लिए
चौकीदार।’
यहाँ कवयित्री के सरोकार बदल गए हैं पुरुष की कविता की अपेक्षा। एक स्त्री क्यों भयभीत सी रहती है कुछ पढ़ते-लिखते या कुछ और काम करते हुए? कौन उसकी पहरेदारी कर रहा है? यहाँ ज़ाहिर है शिक्षित स्त्री का भय उभर कर आया है जो वह अपने को मजदूरिन जैसी स्थिति में स्वयं को देखती है। एक शिक्षित और अशिक्षित स्त्री की कमोवेश स्थितियाँ इस कविता से एक सी दिखाई दे रही हैं। आखिर क्यों? एक सवाल बना हुआ है। आज के समय में स्त्रियाँ स्वयं साहित्य रच रही हैं। उनसे स्त्री-विमर्श की चेतना भी समाज में स्त्रियों के प्रति दोहरे बर्ताव का वातावरण कम नहीं कर पा रही है। यह सोच सिर्फ स्त्रियाँ या दलित स्त्रियाँ ही नहीं सोच रही हैं। यह आज का जागरूक दलित कवि भी ऐसी ही सोच रखता है। हिंदी के सुविख्यात बुंदेली दलित कवि कालीचरण स्नेही ने तो ‘स्त्री विमर्श’ नाम से अनेक साखियाँ लिखी हैं जिनमें इतिहास से लेकर आज तक स्त्री की दशा और उनके प्रति समाज के नजरिये को बहुत ही खूबसूरती के साथ रखा है। उनमें से कुछ साखियाँ यहाँ मैं उद्धृत कर रही हूँ–
‘नहीं उजागर कर सकी, कोई लेखनी साँच
‘भँवरी’ के मन की व्यथा, कौन सकेगा बाँच
औरत को इस देश में, हरदम रखा गुलाम
चाल-चलन के नाम पर, किया खूब बदनाम
लगा रखे हर ओर से, औरत पर प्रतिबंध
विचरण करता मर्द नित, दुनिया में स्वच्छंद
घर-बाहर हर मोड़ पर, होती रोज़ जलीज
औरत जूती पैर की, ऐसी देत दलील।’
आज गैरदलित स्त्रियों को सम्मान, पद, प्रतिष्ठा और उनका प्रतिनिधित्व दलित स्त्रियों की अपेक्षा अधिक प्राप्त हो गया है। अभी भी दलित स्त्री अपने अस्तित्व और अस्मिता के लिए जूझ रही है। घर और बाहर दोनों जगह उसे लड़ना पड़ रहा है। कई जगह तो उसके अस्तित्व को उभरने ही नहीं दिया जा रहा है। तब अस्मिता की बात पीछे रह जाती है। दलित स्त्री को समाज में सम्मान नहीं है। वह अभी भी पूरे समाज की पैरों की जूती बनी हुई है। उस पर कदम-कदम पर प्रतिबंध लगा हुआ। आखिर क्यों? जबकि पुरुष पूरी दुनिया में कहीं भी विचरण करे। यह कौन लोग हैं जो औरत को वस्तु मानते हैं। उसे अपने अधीन रखना चाहते हैं। उसके व्यक्तित्व को कुचलने का प्रयत्न लगातार करते रहते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि यही स्थितियाँ स्त्री महसूसती है और यही दलित कवि। इस दृष्टि से दलित कवि स्त्रियों के प्रति अधिक संवेदनशील दिखाई दे रहा है। यही उसके आज के समय में नए रचनात्मक सरोकर बन कर उभर रहे हैं, जो किसी भी समाज और देश की प्रगति के लिए आवश्यक होते हैं। मलखान सिंह का नाम प्रखर कवि के रूप में उभरा था। कुछ कविताएँ उन्होंने बहुत ही प्रखरता के साथ लिखी थीं। कवि के सरोकार इस समाज की स्त्रियों से इस प्रकार जुड़ते हैं–
‘मेरी माँ मैला कमाती थी
बाप बेगार करता था
और मैं मेहनताने में मिली जूठन को
इकट्ठा कर खाता था
आज बदलाव इतना आया है कि
जोरू मैला कमाने गई है
बेटा स्कूल गया है और
मैं कविता लिख रहा हूँ।’
यहाँ कवि मलखान सिंह की उक्त कविता में कई ऐसे प्रश्न खड़े होते हैं जिन पर एकमत नहीं हुआ जा सकता। यह कविता एक तो वाल्मीकि समाज के स्त्री-पुरुष के परस्पर दिनचर्या को दर्शाती है, जहाँ स्त्री कमेरी है और पुरुष निकम्मा है। वह कमाती है पुरुष घर बैठा रहता है और कविता लिखता रहता है। यह बात वाल्मीकि समाज पर भले लागू हो जाए समस्त दलित समाज का सच नहीं हो सकती। दूसरी बात यह है कि जूठन लेने और खाने का काम वाल्मीकि जाति के लोग करते हैं, बाकी समाज में जूठन लेने और खाने का काम नहीं किया जाता। भले ही कितने ही अभाव में रहें। खुद्दारी उनकी पहचान रही है। सच्चाई तो यह है कि वे ही दलित कवि कविताएँ लिख पाते हैं जो कहीं-न-कहीं काम करते हैं। घर बैठकर मनोरजंन के लिए दलित कवि ने कभी कविताएँ नहीं लिखीं, पर कवि मलखानसिंह का अनुभव सब दलित कवियों का नहीं हो सकता। उनके कवित्व के कुछ सरोकार अलग हैं।
समग्रत: कहा जा सकता है कि स्वातंत्र्योत्तर हिंदी दलित कविता के सरोकार विविध रूपों में उभर कर आए हैं, जिसमें सामाजिक विसंगतियों का एक विस्तृत वितान फैला हुआ है तो आर्थिक विषमता को भी दलित कवि नजरअंदाज नहीं करते हैं, क्योंकि उनका आर्थिक आधार का रास्ता समाज के रास्ते से होकर ही गुजरता है। कुछ कवियों ने अपनी कविताओं में शिक्षा को गंभीरता से उठाया अवश्य है। वे जानते हैं कि डॉ. भीमराव अम्बेदकर ने पहला नारा ही शिक्षित बनाने का दिया था। संगठित होने और संघर्ष होने की बात वह बाद में करते हैं। डॉ. अम्बेदकर ने ही अँग्रेजी शिक्षा को, अँग्रेजी भाषा को शेरनी की दूध कहा था। उनका कहना था जिसने जितना ज्यादा अँग्रेजी रूपी भाषा का दूध पिया, वह उतना ही अँग्रेजों के खिलाफ दहाड़ा था। यह बात आज भी उतनी ही प्रासंगिक बनी हुई है जितनी डॉ. अम्बेदकर के समय में थी। स्वातंत्रयोत्तर हिंदी दलित कविता डॉ. अम्बेदकर के विचारों के साथ ही आ रही है। डॉ. अम्बेदकर को छोड़कर कविता ही नहीं दलित साहित्य की कोई भी विधा आगे नहीं बढ़ सकती। हाँ, उसके सामने समय सापेक्ष अनेक चुनौतियाँ हर रोज़ पैदा हो रही हैं। दलित कवियों को उनका सामना करना ही पड़ेगा। कविताओं के विषय उसे बदलने पड़ेंगे। तभी उसकी कविता राजनीति के लिए मशाल का काम कर पाएगी।