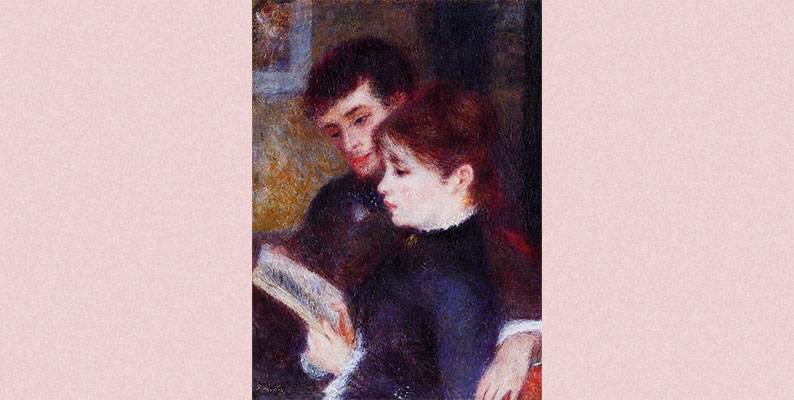‘आलोचना’ के संबंध में
- 1 June, 1953
शेयर करे close
शेयर करे close

शेयर करे close
- 1 June, 1953
‘आलोचना’ के संबंध में
प्रिय बंधु,
सुना है कि राजकमल प्रकाशन, दिल्ली की ओर से समाचार-पत्रों में घोषणा की गई है कि आगे से ‘आलोचना’ (त्रैमासिक) का संपादन, मेरे स्थान पर, चार लेखकों का एक संपादकमंडल प्रयाग से किया करेगा। अनेक साहित्यिक बंधुओं ने यह भी सूचना दी है कि इस जोड़-तोड़ में सफल होने और हिंदी आलोचकों तथा साहित्यकारों का सहयोग पूर्ववत् पाते जाने के लिए राजकमल वाले बनारस और इलाहाबाद में मुझे हर तरह से बदनाम करते फिरे हैं, कि इस प्रसंग में सारी गलती मेरी ही है। यह सब सुनकर मुझे क्षोभ हुआ है, क्योंकि मुझे सहसा इस बात पर विश्वास नहीं होता कि कोई भी व्यक्ति स्वार्थवश इतनी अकृतज्ञता और असत्य का व्यवहार कर सकता है। राजकमल वालों के एकतरफा, निरंकुश और स्वार्थी व्यवहार के बावजूद मैं अबतक मौन रहा हूँ। आशा थी कि संभवत: उनका मानवीय विवेक स्वयं उन्हें धिक्कारेगा और उन्हें अपनी कृतघ्नता पर खेद होगा। लेकिन जिसके आगे वाणिज्य और मुनाफा ही सब कुछ है, दुर्भाग्य से उसके लिए मानवीय और नैतिक मूल्यों का कोई अर्थ नहीं होता। मैं अब भी अपने मौन से उनके दुर्व्यवहार की उपेक्षा कर जाता, लेकिन उन्होंने मनगढ़ंत और झूठी बातों का प्रचार करके मेरी साहित्यिक प्रतिष्ठा को क्षति पहुँचाने की ही चेष्टा नहीं की है बल्कि हिंदी-साहित्यिकों की पाँत में फूट डालने का भी प्रयत्न किया है। और ऐसा लगता है कि कुछ साहित्यिक बंधु पूरी स्थिति न जानने के कारण उनके भुलावे में आ गए हैं। इसलिए हिंदी लेखकों और पाठकों के समझ सही तथ्यों को खोलकर रखने के लिए विवश हूँ। यह ब्यौरा रोचक नहीं है, किंतु फिर भी प्रकाशकों की हीन मनोवृत्ति पर प्रकाश डालता है और हमें इस कटु सत्य से पुन: अवगत कराता है कि हिंदी साहित्य की निस्वार्थ सेवा तक के मार्ग में उनकी वाणिज्य-वृत्ति बाधक बन जाती है।
लगभग दो वर्ष पूर्व (मई 1951) जब मैं चार वर्ष के काश्मीर-प्रवास के बाद लौटा तो मन में यह साध लेकर कि तत्काल जिन संकीर्ण मतवादों के कारण भिन्न-भिन्न साहित्यिक विचारधाराओं और प्रवृत्तियों के लेखकों में फूट पड़ी हुई है और जिससे साहित्य की प्रगति अवरुद्ध है, उसे पाटने के लिए अपने समस्त साहित्यिक उद्योगों को लगा दूँगा। आते ही मैंने राजकमल वालों से, जो मेरी पुस्तक ‘काश्मीर : देश व संस्कृति’ के प्रकाशक भी थे, एक ऐसी पत्रिका निकालने के संबंध में बातचीत की जिसमें मुनाफा कमाना उद्देश्य न हो, बल्कि साहित्य सेवा ही जिसका मुख्य लक्ष्य हो। सोचने-समझने के उपरांत वे ‘आलोचना’ प्रकाशित करने के लिए इस शर्त पर राजी हुए कि मैं एक वर्ष तक उनसे संपादन का कुछ न लूँ। उसके बाद वे उचित आनरेरियम का प्रबंध करेंगे। तबतक वे केवल मेरे दफ्तर आने-जाने में जो खर्च पड़ेगा उसके लिए ‘आलोचना’ की बिक्री में से सवा 6 प्रतिशत देंगे जो आठ महीने बाद 56 रुपए बना, यानी 7 रुपया मासिक। इस पर कदाचित् उन्हें स्वयं ही संकोच लगा, क्योंकि मुझे गाज़ियाबाद से महीने में आठ-दस बार आना होता था, और उन्होंने अपनी ओर से, मुझसे बिना पूछे ही आगे से प्रतिशत का हिसाब हटाकर 150 रुपये प्रति अंक, या 50 रुपया मासिक आने-जाने के व्यय के लिए कर दिया। लिखा-पढ़ी प्रारंभ से ही कोई नहीं हुई थी। उस समय भी उनके मन में कोई छल-छंद था, यह तो नहीं जानता, क्योंकि बातचीत से एक स्थाई समझौते के रूप में यही तय हुआ था कि इस साहित्यिक-अनुष्ठान में हम दोनों सहयोग करेंगे, वे प्रकाशन का भार उठाएँगे, और मैं संपादन का–लेखकों की पारिश्रमिक देना भी प्रकाशन के अंतर्गत रखा गया था। संपादकीय नीति पर उनका कोई पूर्वग्रह नहीं चलेगा, और न प्रकाशन और बिक्री की व्यवस्था पर मेरा, क्योंकि दोनों में से किसी ने किसी को नियुक्त नहीं किया था। एक वर्ष बाद जो आनरेरियम दोनों के सम्मिलित परामर्श से तय होगा, वह वेतन नहीं समझा जाएगा, केवल पत्र-पुष्प के रूप में होगा और तब प्रकाशन के खर्च में जोड़ा जाएगा। मेरे सामने एक साहित्यिक दायित्व की पूर्ति का प्रश्न था, इसलिए मैंने विश्वास किया। मैंने ‘आलोचना’ की भावी-रूपरेखा और चार अंकों की योजना बनाई, और मैंने जून 1951 में अपने खर्च पर उत्तर प्रदेश के मुख्य साहित्यिक केंद्रों का दौरा किया और साहित्यिकों का सहयोग जुटाया। लौटकर एक अपील प्रकाशित की, जिसके साथ राजकमल वालों की व्यवस्थापकीय विज्ञप्ति भी थी। फिर ‘आलोचना’ निकली। जैसी निकली वह सर्वविदित है। हिंदी के अग्रणी आलोचकों और विचारकों ने इस ऐतिहासिक निर्माण-कार्य के लिए मुझे सराहा और अपना पूरा सहयोग दिया, जिसके लिए मैं उनका चिर कृतज्ञ हूँ। इस प्रकार लेखकों के बीच की खाई पाटती, साहित्य में वैज्ञानिक और निष्पक्ष समीक्षा की परंपरा बनाती, लेखकों-पाठकों के सम्मुख महत्त्वपूर्ण साहित्यिक प्रश्न उठाती और साहित्य के स्तर को ऊँचा करने की प्रेरणा देती हुई ‘आलोचना’ प्रगति कर चली। किंतु इस शुभ कार्य की पूर्ति के लिए मुझे स्वयं कितनी दारुण कठिनाइयाँ झेलनी पड़ीं, अपने परिवार के दायित्वों को निभाने के लिए कितना अतिरिक्त परिश्रम करना पड़ा और फिर भी कितना कर्ज़ बढ़ गया, यह इस प्रसंग का व्यक्तिगत पहलू है, इसलिए इसका उल्लेख व्यर्थ है।
चार अंक निकल जाने के पश्चात् मैंने राजकमल वालों को उनके प्रारंभिक वायदे का स्मरण दिलाया। उन्होंने टाला। फिर मैंने ‘इतिहास-अंक’ और ‘इतिहास-परिशिष्टांक’ भी निकाल दिए, किंतु उनकी ओर से आनरेरियम की चर्चा न हुई। तब लगभग 21 महीने गुज़र जाने पर मैंने पुन: उन्हें स्मरण दिलाया। एक लंबी बहस चल पड़ी। मैंने कहा कि ‘वेतन’ का तो प्रश्न ही नहीं है, पर इतनी प्रतिष्ठित पत्रिका का आनरेरियम भी 200 रुपये प्रतिमास से क्या कम होना चाहिए। उन्होंने कहा कि साहित्य-सेवा का उद्देश्य मेरे सामने हो, उनके लिए नहीं है। उनका तो वाणिज्य है। घाटा पूरा करना और लाभ उठाना है, इसलिए वे 100 रु. प्रति मास या 300 रुपया प्रति अंक से अधिक न दे सकेंगे। फिर मैंने ही मध्यमार्ग सुझाया, और वे 150 रुपया पर राजी हो गए। किंतु दूसरे दिन ही मुझे उनका पत्र मिला कि यह आनरेरियम सातवें अंक से होगा। मैंने लिख भेजा कि यह अनुचित होगा, एक वर्ष तक की बात थी, इसलिए उचित यही होगा कि पाँचवें अंक से, अर्थात् ‘आलोचना’ के दूसरे वर्ष से यह व्यवस्था चले। उत्तर में एक गुस्से से भरा पत्र मिला, जिसमें आनरेरियम संबंधी फैसले को रद्द करने और बोर्ड के डायरेक्टरों के फैसले का इंतज़ार करने की सूचना दी गई, और साथ ही एक प्रच्छन्न संकेत भी कि वे मुझसे संबंध-विच्छेद कर सकते हैं। पत्र पढ़कर पीड़ा हुई। फिर भी समझौते का मार्ग निकालने के लिए मैंने उनसे कहा कि केवल दो अंकों की बात है, फिर मध्य का मार्ग ग्रहण कीजिए और पाँचवें से न सही, छठे अंक से ही यह समझौता लागू कीजिए। वे राजी लगे, लेकिन कुछ दिनों बाद उनका पत्र मिला जिसमें उन्हें आनरेरियम की जगह पहली बार ‘वेतन’ शब्द का प्रयोग किया। मेरे ऊपर दोष मढ़ा कि ‘आलोचना’ की आर्थिक स्थिति को जानते हुए भी मैं अपना ‘वेतन’ बढ़वाने के लिए इतना जोर दे रहा हूँ। इसलिए वे एक वर्ष के लिए 7 वें अंक से 450 रुपया प्रति अंक स्वीकार तो कर रहे हैं, यद्यपि उसे उचित नहीं समझते। साथ ही उन्होंने शर्त यह रखी कि प्रत्येक अंक की पूरी सामग्री प्रकाशन की तारीख से एक माह पूर्व उनको देनी होगी और ‘आलोचना’ संबंधी पीर-बबर्ची-भिश्तीख़र सबका काम उठाने का दायित्व भी लेना होगा। यह पत्र पढ़कर मुझे राजकमल वालों की अकृतज्ञता पर ग्लानि और क्षोभ हुआ। किंतु फिर भी जैनेंद्र जी का आग्रह मानकर मैंने उन्हें लिख भेजा कि चूँकि हम दोनों ने अपने सम्मिलित प्रयत्न, सहयोग और त्याग से इस पत्रिका को बनाया-चलाया है, इसलिए उनकी आर्थिक कठिनाइयों को ध्यान में रखकर मैं सातवें अंक से ही यह आनरेरियम स्वीकार कर लूँगा। रही और काम-धाम संबंधी शर्तों की बात, सो उनके बारे में हम दोनों का पूर्ण सहयोग जरूरी है ताकि पत्रिका समय पर निकलती रहे। मैंने समझा विवाद समाप्त हुआ, लेकिन इसके उत्तर में उनका एक लंबा पत्र मिला। उन्हें ‘पारस्परिक सहयोग’ शब्द पर घोर आपत्ति हुई। लिखा कि ऐसा कोई सहयोग हमारे बीच नहीं रहा, मैंने संपादन किया तो उन्होंने आवश्यकता से अधिक वेतन दिया। यह भी लिखा कि वे 150 रुपया मासिक वेतन के लिए अस्थाई रूप से ही राजी हुए हैं। यदि इस वर्ष भी घाटा रहा तो अगले वर्ष काट कर 100 रुपया मासिक ही कर दिया जाएगा। साथ में एक अल्टीमेटम भी था कि यदि 24 घंटे के अंदर उनकी सब शर्तों का मैं ज्यों का त्यों न मान लूँगा, तो वे ‘आलोचना’ का दूसरा प्रबंध करने को स्वतंत्र होंगे। मेरे स्वाभिमान ने इस पत्र का उत्तर देना स्वीकार न किया। तीसरे दिन उनका अंतिम पत्र मिला कि उन्हें दु:ख है कि हमारा संबंध इतने खेदपूर्ण ढंग से टूट गया। इसलिए संबंध मैंने नहीं तोड़ा, उन्होंने ही टूट जाने की सूचना दी। इसके बाद से उन्होंने कभी मिलने की भी सौजन्यता नहीं दिखाई। इतना ही नहीं, श्री नामवर सिंह, गोपालकृष्ण कौल आदि लेखकों के प्रति भी, जिन्होंने केवल मेरे कारण एक पाई लिए बिना ही सहकारी संपादक के रूप में निरंतर सहयोग दिया, उन्होंने कभी कृतज्ञता प्रदर्शित नहीं की।
इन तथ्यों के आधार पर, मुझे विश्वास है, हिंदी के साहित्यकार और पाठक सत्यासत्य का निर्णय कर सकेंगे। केवल मुझे ही नहीं बल्कि दिल्ली के अन्य साहित्यकारों को भी, जो इन घटनाओं से परिचित हैं, ऐसा लगा है कि राजकमल वालों ने जानबूझ कर ऐसी स्थिति पैदा करनी चाही है जिससे ‘आलोचना’ से मेरा संबंध टूट जाए। इतना तो स्वयं उनके बताने से मुझे मालूम होता रहा है कि कतिपय देशी-विदेशी क्षेत्रों में, जहाँ से राजकमल वाले अतिरिक्त लाभ उठाते आए हैं, मेरे और मेरी नीति के बारे में घोर आपत्ति रही है। जो भी हो, इतना तो निश्चित है कि हिंदी के साहित्यकारों को ‘आलोचना’ के द्वारा संहत करने का मैंने जो उद्योग किया है, राजकमल वाले स्वार्थवश उस पर पानी फेरने के लिए तुले हुए हैं। आभार स्वीकार करना तो दूर, उन्होंने अपने प्रचार में कुछ ऐसे हथकंडों का भी प्रयोग किया है जो अशोभन है। अपने साहित्यिक कार्य के लिए मैंने कभी पुरस्कार या सम्मान की आकांक्षा नहीं की। ये वस्तुएँ इस समाज में दुर्लभ हैं। निर्माण कोई करता है, लाभ दूसरा उठाता है। पूँजी की जहाँ सत्ता है वहाँ यही तर्क चलता है। लेकिन हिंदी के लेखक और पाठक भी इस अवसरवादी तर्क से ही चालित होंगे, ऐसा अविश्वास मुझ में नहीं है। ‘आलोचना’ द्वारा जिस कार्य का भार मैंने अपने कंधों पर हिंदी लेखकों के सहयोग से उठाया था, ‘आलोचना’ के बिना भी मैं उसे पूर्ववत् जारी रखूँगा। ‘आलोचना’ तो एक उपलक्ष्य मात्र थी। मैं ‘अखिल भारतीय आलोचना परिषद्’ के निर्माण की बात गत वर्ष से सोचता आया हूँ। यदि उसका निर्माण हो सका तो संभव है कि हिंदी के साहित्यकार दो-एक ऐसी पत्रिकाओं में अपने सहयोग को संगठित कर सकेंगे जो सर्वथा लेखकों की अपनी हो, जिनपर प्रकाशकों के स्वार्थ की कहीं कोई छाया न हो।
[श्री शिवदान सिंह जी के इस पत्र पर हम अपनी राय संपादकीय में दे रहे हैं ।]
Image: The Artists Father Reading his Newspaper
Image Source: WikiArt
Artist: Paul Cezanne
Image in Public Domain