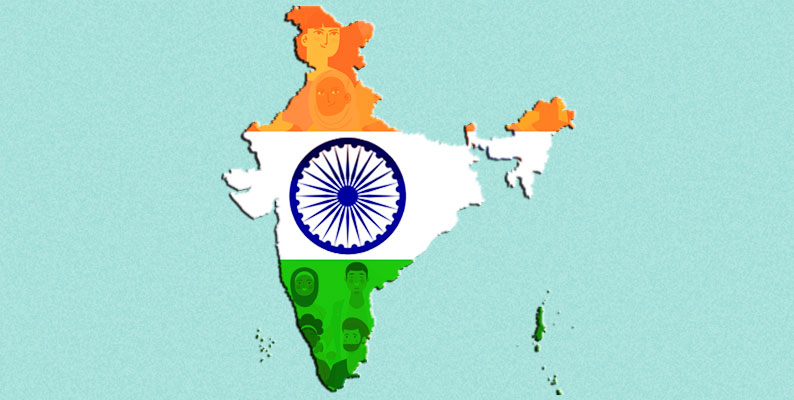मंगलवाद
- 1 April, 1951
शेयर करे close
शेयर करे close

शेयर करे close
- 1 April, 1951
मंगलवाद
आचार्य जानकीवल्लभ जी सुललित गीतों के गायक और मर्मस्पर्शी कविताओं के कवि ही नहीं; एक उच्चकोटि के चिंतक और समीक्षक भी हैं। इनके चिंतन और समीक्षा में, इनके व्यक्तित्व की तरह, एक अद्भुत मौलिकता और रंजकता है। ‘मंगलवाद’ में सिर्फ पांडित्य नहीं है, उन दो गुणों का संतुलित समावेश भी है!
वाणी का व्यापार वक्तव्य विषय के लिए प्रवर्तित करने के पूर्व पुस्तक-प्रणेता ‘मंगल’ (की कामना) करते हैं। मंगल शब्द कल्याण अथवा शुभ का पर्यायवाची है[i]। मेदिनी के अनुसार इस शब्द का तीनों लिंगों में प्रयोग होता है। इसके स्त्रीलिंग रूप–मंगला के दो अर्थ होते हैं–उजली दूब और देवी पार्वती। पुलिंग रूप (मंगल:) का अर्थ ग्रह-विशेष है। और, नपुंसक रूप (मंगलम्) का प्रयोग तीन अर्थों में होता है–(1) कल्याण (2) सर्वार्थ और (3) रक्षण। कहने का तात्पर्य कि मंगल शब्द कल्याण का पर्यायवाची है।
इसके अतिरिक्त मंगल का प्रयोग मंगलमय, मंगलकारी आदि अनेक अर्थों में भी, लक्षणा एवं व्यंजना द्वारा, व्याकरणानुमोदित रूपों में, प्रचलित है। कालिदास ने लिखा है–
‘राम इत्यभिरामेण वपुषा तस्य नोदित:
नामधेयं गुरुश्चक्रे जगत्प्रथम-मंगलम्।’
निश्चय ही यहाँ ‘मंगल’ का अर्थ (अर्थांतर से असंकमित) केवल मंगल नहीं है। किंतु ‘मंगलायतनं हरि:’ के समान ‘मंगल-भवन अमंगल-हारी’ या ‘मुद-मंगल-दाता’ आदि का भी प्रचलन[ii] है ही। सुस्पष्ट शब्दों में, यह शब्द विशेषण और विशेष्य–दोनों रूपों में प्रयुक्त होता है।
‘मंगल’ शब्द गत्यर्थक ‘मगि’ धातु से उदित् होने के कारण नुम् कर देने और ‘मंगरेलच’ (उ. 748) सूत्र के अनुसार ‘अलच्’ प्रत्यय करने पर सिद्ध होता है। ‘मंग्यते अनेनेति मंगलम्’–यही इसकी व्युत्पत्ति होगी।
पतंजलि ने अपने ‘महा-भाष्य’ में पाणिनि के प्रथम सूत्र–‘वृद्धिरादैच्’ पर भाष्य लिखते हुए बताया है–
“मांगलिक आचार्यो महत: शास्त्रौघस्य
मंगलार्थे वृद्धिशब्दमादित: प्रयुंक्ते”
और, कालिदास ने भी लिखा है–
“पुरोपकण्ठोपवनाश्रयाणां
कलापिनामुद्धतनृत्यहेतौ
प्रध्मातशंखे परितो दिगंता–
स्तूर्यस्वने मूर्च्छति मंगलार्थ।”
यहाँ पतंजलि के ‘मंगलार्थे’ और कालिदास के ‘मंगलार्थे’ में मंगल शब्द विशेष्य-वाचक है। जब कि ‘जगत्प्रथम-मंगलम्’ या ‘तथापि स्मतृणां वरद परमं मंगलमसि’ आदि में वह सुस्पष्ट ही विशेषण-वाचक है।
तो ‘मगि’ धातु को गत्यर्थक मानें अथवा ‘सर्पणार्थक’ (मगि सर्पणे),–जब भी ‘सर्पण’ (सरकना; साँप की-सी चाल चलना) गति-विशेष ही है; किंतु यहाँ लक्ष्य करने की बातें दो हैं–
(1) गति के तीन अर्थ होते हैं–(क) गमन (ख) मोक्ष और (प्राप्ति) और (ग) पूर्वोक्त विग्रह–मंग्यते अनेन इति मंगलम् के अनुसार गत्यर्थक ‘मगि’ धातु का अर्थ प्राप्ति (लब्धि) समझना होगा। मंग्यते=प्राप्यते (इष्टम्) अनेन इति मंगलम्, अर्थात् जिससे इष्ट वस्तु की प्राप्ति हो उसे मंगल कहते हैं। इसके साथ ही, यह भी स्मरण रखना होगा कि इसी विग्रह या व्युत्पत्ति के समान एक और भी विग्रह या व्युत्पति है जिसमें इसके (प्राप्ति अर्थ के) ठीक विपरीत अर्थवाली धातु का प्रयोग होता है परंतु दोनों का फलितार्थ प्राय: समान ही रहता है। सर्पणार्थक मगि धातु से ‘मंगल’ की वह दूसरी व्युत्पत्ति या विग्रह है–
(2) मंगति=अपसरति (सर्पति) दुरदृष्टम्=अनिष्टम् अनेन इति मंगलम्। अर्थात् जिससे अनिष्ट दूर हो जाए उसे ‘मंगल’ कहते हैं।
कहना अनावश्यक है कि पहली क्रिया (धातु) का भाव विध्यात्मक (Positive) और दूसरी का निषेधात्मक (Negative) है–एक से (इष्ट की) प्राप्ति होती है और दूसरी से (अनिष्ट का) नाश होता है। और दोनों को मिला देने से न केवल मंगल की परिभाषा ही बन जाती है, प्रत्युत मंगल के दो प्रत्यक्ष प्रयोजनों का भी पता लग जाता है। इस प्रकार केवल भाषा-शास्त्र की सहायता से भी मंगल की परिभाषा गढ़ी जा सकती है और उसके दो प्रकट प्रयोजनों को पकड़ा जा सकता है–
परिभाषा
अनिष्ट को अपसारित कर इष्ट को प्राप्त करना ही मंगल है।
प्रयोजन
मंगल के दो प्रयोजन हैं–(1) इष्ट की प्राप्ति और (2) अनिष्ट का नाश।
इसीलिए मंगल का एक अर्थ ही अभीष्ट अर्थ की सिद्धि माना गया है–‘अभिप्रेतसिद्धिर्मंगलम्।’ अवश्य इस लक्षण में एक शंका की गुंजाइश भी रह गई है। क्योंकि यदि किसी व्यक्ति के मन में खोट हो और वह किसी ऐसे इष्ट की खोज में हो जो वेद-विरुद्ध अथवा लोकनिंदित समझा जाता हो, तो उसकी प्राप्ति को भी, इस लक्षण के अनुसार, मंगल माना जाएगा। परंतु उसे तो कोई भी मंगल मानने से रहा। इसलिए अभिप्रेत के साथ एक विशेषण जोर दिया जाना चाहिए और वह विशेषण होगा–‘अगर्हित’, अर्थात्, अगर्हित (अनिंदित; लोकवेद-विहित) अभिप्रेत अर्थ की सिद्धि को मंगल कहते हैं।
जिसके करते समय ही मन आह्लादित होता और प्रिय वस्तु की प्राप्ति भी संभावित रहती है, उसे ही मंगल कहते हैं। अवश्य इस मानसिक आह्लाद के पीछे भी कोई घृणित कीटाणु न छिपा रहना चाहिए।
किसी ने कितना ठीक लिखा है:–
‘प्रशस्तचरणं नित्यमप्रशस्तविवर्जनम् एतच्च मंगलं प्रोक्तमृषिभिर्मंत्रदर्शिभि:।’
अर्थात्, मंत्रद्रष्टा ऋषियों के अनुसार अप्रशस्त का परित्याग और प्रशस्त का आचरण ही मंगल है।
वैशेषिक दर्शन के उपस्कारक महामहोपाध्याय शंकर मिश्र ने बताया है कि मंगल एक कर्म है जिसका फल विघ्नों का ध्वंस और ग्रंथ की समाप्ति है। उसका स्वरूप भी अपने इष्ट देवता का नमस्कार आदि है।[iii]
एक ने कहा है कि विष्णु परम पवित्र मंगल हैं।[iv] और यह तो सभी जानते हैं कि विष्णु शब्द का अर्थ व्यापक या सर्वव्यापी (ब्रह्म) है। विष्णु पुराण का वचन है–
‘अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभ संततिम्
स्मृतिमात्रेण यत् पुंसां ब्रह्म तन्मंगलं विदु:।’
कि वस्तुत: वह ब्रह्म ही मंगल है जो स्मरण मात्र से अशुभों का निराकरण और शुभ की परंपरा का विस्तार करता है। अस्तु,
मंगल-कारक (गोरोचन आदि) को भी मंगल कहा जाता है। ऐसा अर्थ लक्षणा द्वारा ही प्राप्त होता है। संक्षेप में यही समझना चाहिए कि मंगल शब्द यथावसर, वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक तीनों हो सकता है। ‘मंगलकारक’ से मेरा अभिप्राय मंगल प्रयोजक से है।
मंगलकारकों की एक छोटी-मोटी तालिका भी मिल जाती है। ब्रह्म-विद्, गौ, अग्नि, सुवर्ण-घृत, सूर्य, जल और राजा–इन आठों को ‘मंगल-द्रव्य’ माना गया है। इसी प्रकार दूब, दही, घी, भरा घड़ा, बछड़े को दूध पिलाती हुई गाय, सोना, गोबर-मिट्टी का बना हुआ स्वस्तिक, अक्षत, धान का लावा, शहद आदि को भी मंगल प्रयोजक कहा गया है।
ये इतने नाम मंगल-द्रव्यों की इयत्ता के सूचक नहीं हैं। ऐसे ही और-और भी हो सकते हैं; होते हैं! भारवि और माघ ने अपने अपने काव्य-ग्रंथ ‘किरातार्जुनीय’ तथा ‘शिशुपालवध’ में नमस्कार या आशीर्वाद के रूप में पृथक् मंगल नहीं किया है। यहाँ तक कि जगण से आरंभ होने वाले छंद से ही दोनों ने अपने-अपने ग्रंथ का उद्घाटन किया है और छंद:शास्त्र के अनुसार जगण का फल भय अथवा रोग कहा गया है, अत: उसका प्रथम प्रयोग निंद्य माना गया है।
अवश्य पूर्वोक्त महाकवियों का यह साहस नहीं है और न कोई क्रांतिकारिणी चेष्टा ही है। प्रत्युत मल्लिनाथ की दरसाई हुई युक्ति के अनुसार यह छंद के आदि अक्षर ‘श्री’ के प्रयोग का माहात्म्य है जिससे वर्ण या गण-दोष का सकंट भी कट गया है और प्रकारांतर से मंगल भी हो गया है। श्री शब्द अपनी संपूर्ण सुंदरता के साथ देवता-वाचक भी है। फलत: देवता का स्मरण मंगल-प्रयोजक हो जाता है।[v] इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि देवता-देवियों के नामों को भी मंगल-‘द्रव्यों’ की सूची में रखा जाना चाहिए–गणेश जी तो मंगल मूर्ति कहे ही जाते हैं–‘मोदकप्रिय मुद-मंगल-दाता’ महाभाष्यकार पतंजलि का उद्धरण ऊपर दिया जा चुका है। उसमें उन्होंने ‘वृद्धि’ शब्द का प्रयोग मांगलिक माना है। ऐसे ही ‘ओंकार’ और ‘अथ’ शब्द के लिए कहा गया है कि ये दोनों अनादि काल में ब्रह्मा का कंठ भेदकर आप-ही-आप निकल पड़े थे, अत: मांगलिक हैं।[vi] वेद का आदि (मांगलिक) अक्षर ‘ॐ’ है जिसका अर्थ ब्रह्म समझा जाता है। और जैमिन के मीमांसासूत्रों अथवा व्यास के ब्रह्मसूत्रों का आरंभ ‘अथातो धर्मजिज्ञासा’ या ‘अथातो ब्रह्मजिज्ञासा’ से हुआ है जिनके आदि में ‘अथ’ का मांगलिक प्रयोग किया गया है।
शांकर-भाष्य के स्वाध्यायियों से यह अविदित न होगा कि वहाँ ‘अथ’ का अर्थ मंगलपरक शंकराचार्य ने नहीं माना है और न उसका ‘अधिकार’ अर्थ ही उन्हें अभिमत है। किंतु फिर भी उन्होंने अपने पक्ष के हेतु का निदर्शन करते हुए एक बड़ी ही अच्छी बात लिख दी है कि दूसरे अर्थ में प्रयुक्त ‘अथ’ शब्द के श्रवण से मंगल होता है[vii]–स्वयं मंगल के ही अर्थ में उसका प्रयोग करने से नहीं। ऐसा ही ओंकार के लिए भी समझना चाहिए, क्योंकि उसके उच्चारण-जन्य नाद में ही मांगलिकता रहती है, वह शब्द तो अपने तईं ब्रह्म का पर्यायवाची है।
यहाँ एक रहस्य का उद्घाटन होता है जो मुझे अत्यंत स्वाभाविक एवं मनोवैज्ञानिक प्रतीत होता है। वह यह कि शकुन का विचार करने वाले भी यात्रा पर जल से भरा घड़ा देखने का यह तात्पर्य नहीं स्वीकार करते कि अपने किसी व्यक्ति को उसी विशिष्ट निमित्त से जल भरने के लिए कुछ क्षण पहले भेज दिया जाना चाहिए। वस्तुत: यात्रा के लिए चल पड़ने पर यदि आकस्मिक रूप से भरा घड़ा दिख जाए, तभी उसे मंगल का सूचक समझना चाहिए।[viii] उसी प्रकार अपने प्रासंगिक अर्थ के लिए ओंकार या अथ का प्रयोग होने पर, उसके नाद मात्र के किसी प्रकार कर्ण-कुहर में प्रवेश करने से ही अनायास मंगल हो जाता है।
पाणिनि के ‘भूवादयो धातव:’ सूत्र पर भाष्य लिखते हुए पतंजलि ने वकार का प्रयोग भी मंगलार्थक माना है। यह अवश्य है कि वकार मंगल का जनक नहीं, सूचक है।
अब अप्रासंगिकता के भय से विस्तार में न जाकर उपसंहार किया जा रहा है। सर्वप्रथम सिंहावलोकन करते हुए मंगल शब्द के व्युत्पत्ति लभ्य अर्थों के लिए इतना और जोड़ देना आवश्यक है कि पूर्वोक्त दोनों व्युत्पत्तियाँ अपने आप में पूर्ण हैं अत: उन्हें परस्पर की अपेक्षा नहीं। अर्थात् इष्ट की प्राप्ति के साधक और इष्ट के पथ के विघ्नों के बाधक–दोनों की पृथक-पृथक मान्यता हो सकती है।
अब यह देखना चाहिए कि ऊपर के विवेचन से ‘मंगल’ के लिए क्या निष्कर्ष निकलता है! मेरे विचार से दो बातें सामने आती हैं–
(1) मंगल धर्म है, और
(2) मंगल कर्म है।
मैं इस दूसरे के ही पक्ष में हूँ। सुस्पष्ट शब्दों में, मैं मंगल को आचरण मानता हूँ। मंगलाचरण शब्द बहुत-प्रचलित है ही। निश्चय ही परंपरा से प्रचलित इस शब्द की व्युत्पति ‘मंगल के आचरण’ को लक्ष्य कर हो सकती है; किंतु तब ‘मंगल’ धर्म-परक रहेगा। और जो मैं कहना चाह रहा हूँ, उसमें मंगल से अभिन्न आचरण है, (मंगलाभिन्नम् आचरणम्; मंगलम् एव आचरणम्) ऐसी उसकी व्युत्पत्ति समझनी चाहिए। मेरे ऐसा समझने, मानने या कहने के कारण हैं। अब उन्हीं पर विचार किया जा रहा है।
मंगलाचरण और उसके प्रयोजन
आचरण का अर्थ आचार या व्यवहार है। ग्रंथ के आदि, मध्य एवम् अंत में मंगल आचरण करना चाहिए यह शिष्टाचार है।[ix] यों तो शिष्टाचार का सामान्य अर्थ सदाचार ही होता है; किंतु ‘शिष्ट’ से कुछ विशिष्ट अभिप्राय भी समझा जाता है। श्रद्धा-भक्ति समेत वेद से अनुमत कम करने वाले को शिष्ट कहते हैं। महाभारत में लिखा है[x] कि ऐसे मननशील व्यक्ति को शिष्ट कहते हैं जिसके हाथ-पाँव न हों, दृष्टि स्थिर एवं शांत हो। जिसके अंग-प्रत्यंग में गंभीर शांति विराज रही हो और वाणी में संयम तथा मर्यादा हो।
[xi]महाभाष्य में तो और भी स्पष्ट रूप में लिखा हुआ है कि इसी आर्यावर्त्त के निवासी जो निर्लोभ, जितेंद्रिय, किसी न किसी विद्या के पारंगत, ब्रह्म-विद (ब्राह्मण)[xii] हैं उन्हें ही शिष्ट समझना चाहिए।
और ऐसे ही शिष्टों का आचार किसी ग्रंथ के आदि, मध्य और अंत में मंगल के पक्ष में है। श्रुति का भी आदेश है कि प्रारंभ किए हुए की समाप्ति की कामना रखनेवाले को मंगल आचरण करना चाहिए।[xiii] मंगल अभिमत का हेतु है, इस अंश में शिष्ट मात्र एकमत हैं और इसके प्रमाण में श्रुति ही सर्वोपरि मानी जाती है।
पतंजलि ने पाणिनि के ‘वृद्धिरादैच’ तथा ‘भूवादयो धातव:’ सूत्रों पर भाष्य करते हुए क्रमश: लिखा है–
(1) मंगलादीनि हि शास्त्राणि प्रथन्ते, वीरपुरुषाणि भवन्ति, आयुष्मत्पुरुषाणि चाध्येतारश्च वृद्धियुक्ता यथा स्युरिति।[xiv]
(2) मंगलादीनि मंगलमध्यानि मंगलांतानि हि शास्त्राणि प्रथन्ते वीरपुरुषाणि च भवंत्यायुष्मत्पुरुषाणि चाध्येतारश्च मंगलयुक्ता यथा स्युरिति।[xv]
तात्पर्य यह कि–
“जिस शास्त्र के आदि में मंगल होता है वह फैलता है, ख्याति प्राप्त करता है। उसके पढ़ने-पढ़ाने वाले वीर तथा दीर्घायु होते हैं। उनकी वृद्धि होती है; अभ्युदय होता है।
“जिस शास्त्र के आदि, मध्य एवं अंत में मंगल रहता है उसका प्रसार होता है, वह प्रौढ़ि तथा दीर्घायु प्रदान करने वाला होता है और उसके अध्येता मंगल से युक्त होते हैं।”
कहना अनावश्यक है कि मंगलवादियों के द्वारा पतंजलि के ये वाक्य कितने अभिनंदित हुए हैं।
इसी प्रकार ‘सांख्यदर्शन’ का एक सूत्र मंगलाचरण पर प्रकाश डालता है–
“मंगलाचरण शिष्टाचारात् फलदर्शनात् श्रुतितश्चेति।” –सां. द. 5।1
इसमें तीन हेतुओं का उल्लेख कर मंगलाचरण को समर्थित किया गया है; उसकी आवश्यकता प्रमाणित की गई है। वे हेतु हैं–
(1) शिष्टाचार
(2) फल दर्शन और
(3) श्रुति।
शिष्टाचार की रक्षा के लिए मंगलाचरण होना चाहिए। अभिमत कर्म की निर्विघ्न परिसमाप्ति रूप फल मंगलाचरण से देखने में आता है, अत: उसकी अनिवार्यता प्रतीत होती है। और फिर श्रुति का समर्थन तो उसे प्राप्त है ही।
फलत: मंगलाचरण होना चाहिए और हो सके तो आदि, मध्य और अंत–तीनों स्थानों में उसका प्रयोग चलने देना चाहिए। ‘सिद्धांतकौमुदी’ में भट्टोजि दीक्षित ने ऐसा ही किया है। इसका फल भी उन्हें हाथों-हाथ मिला है। आज दिन ‘सिद्धांतकौमुदी’ के बिना संस्कृत-विद्या में प्रवेश पाना ही असंभव हो गया है। किसी लेखक को इससे अधिक सिद्धि और किसी ग्रंथ को इससे अधिक प्रसिद्धि क्या प्राप्त हो सकती है?
‘पाणिनि’ ने ‘अष्टाध्यायी’ के आदि में और ‘शाकटायन’ ने ‘उणादि’ सूत्रों के अंत में मंगलाचरण किया है–क्रमश: ‘वृद्धिरादैच्’ और ‘मंगेरलच्’ लिखकर। कवि-कुल-गुरु कालिदास ने अपने तीनों नाटकों और अंतिम महाकाव्य (जो रामायण, महाभारत के बाद संस्कृत का श्रेष्ठतम काव्य ग्रंथ है)–रघुवंश के आदि में भी शिव-संबंधी मंगलाचरण किया है और मेघदूत में महाकाल के प्रसंग में मध्य मंगल किया है, कुमारसंभव तो शिव-पार्वतीमय है ही। पुन: प्रत्येक नाटक के अंत में भरतवाक्य के रूप में मंगलाचरण हो गया है, मध्यमंगलों की भी कमी नहीं रही है।
यह सब देखने से इतनी-सी बात तो स्पष्ट हो ही जाती है कि मंगलाचरण आस्तिकता का सूचक है। प्रत्येक कर्म के आरंभ में किसी न किसी रूप में ईश्वर-स्मरण ही इसका उद्देश्य है। यह इस देश की प्रकृति के सर्वथा अनुकूल है भी। किंतु जब से तर्कों के रूप में बुद्धि-वैभव हुआ है, ईश्वर का अस्तित्व भी अनुमान का विषय होने के कारण वाद-विवाद का अखाड़ा बन बैठा है। तब से मंगलाचरण भी श्रद्धा की अभिव्यक्ति मात्र न रह कर, अपनी उपयोगिता की सिद्धि के लिए तर्कों का सहारा पाने लगा है। न्याय-दर्शन, वैशेषिक दर्शन आदि में इसकी चर्चा है। मैं यहाँ संक्षेप में उसका आभास मात्र देना चाहता हूँ। विषय की स्पष्टता के लिए प्रश्नोत्तर की शैली अपनाई जा रही है।
प्रश्न–मंगलाचरण निष्प्रयोजन या निष्फल है क्योंकि वह न विघ्न-ध्वंस का और न ग्रंथ की समाप्ति का ही कारण बन पाता है। इसका कारण यह है कि ग्रंथों की रचना तो नास्तिक लोग भी करते हैं; किंतु उन्हें मंगलाचरण की आवश्यकता नहीं होती और इससे उनकी कुछ क्षति भी नहीं दिखलाई देती।
उत्तर–मंगलाचरण निष्प्रयोजन या निष्फल नहीं हो सकता क्योंकि यदि वह प्रशस्त शिष्टाचार मात्र भी हो तो उसकी सफलता बनी रहती है। क्योंकि शिष्टाचार का पालन भी प्रत्येक शिष्ट व्यक्ति का कर्तव्य होता है, फलत: उसे एकांत निष्फल तो नहीं ही कहा जा सकता। अब रही बात शिष्टाचार के पालन रूप फल से अधिक लब्धि की। सो उसके लिए ग्रंथ-समाप्ति रूप फल को लेना चाहिए, क्योंकि यह फल प्रत्यक्ष देखा जा सकता है, इसके लिए किसी प्रकार की कल्पना न करनी होगी। और उचित भी यही है, क्योंकि दृष्टफल को छोड़ कर अदृष्टफल की कल्पना कोई क्यों करने बैठे।
हाँ, जहाँ (नास्तिकों के ग्रंथों में) मंगल न देखने को मिले वहाँ अलबत्ता कल्पना कर लेनी चाहिए कि जन्मांतर (पूर्वजन्म) के मंगल ने ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति में सहायता पहुँचाई है। इसी प्रकार जहाँ (कादंबरी, रसगंगाधर आदि ग्रंथों में) मंगलाचरण रहने पर भी ग्रंथ-समाप्ति नहीं देखी जाती, वहाँ समझना चाहिए कि विघ्न मंगल की अपेक्षा अधिक बलवान् था, अथवा विघ्नों की प्रचुरता थी जिसके अनुपात में मंगल न्यून पड़ता था। प्रचुर मंगल ही बलवत्तर विघ्नों के निराकरण का कारण हो सकता है।
विघ्न-ध्वंस समाप्ति रूप कार्य को उत्पन्न करने में मंगल का द्वार है। अर्थात् विघ्नों के ध्वंस द्वारा मंगल समाप्ति रूप कार्य का कारण सिद्ध होता है! यह मत प्राचीनों का है।
और नवीनों का कहना है कि मंगल का फल विघ्न-ध्वंस ही हो सकता है, ग्रंथ की समाप्ति तो लेखक की प्रतिभा आदि कारण-कलाप से संबंध रखती है। ‘आदि’ में विघ्न-ध्वंस को भी रखा जा सकता है।
प्रश्न–यदि ऐसा हो तब तो उस व्यक्ति द्वारा किया हुआ मंगल व्यर्थ हो जाएगा, जिसके कभी विघ्न हुआ ही न हो, क्योंकि ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जिसे जीवन के किसी भी मोड़ पर विघ्न से भेंट न हुई हो, और वैसा व्यक्ति अपनी कृति में मंगलाचरण भी कर सकता है।
उत्तर–मंगलाचरण कभी व्यर्थ नहीं हो सकता। क्योंकि यह कोई आवश्यक नहीं कि यदि पहले कभी विघ्न न हुआ हो तो वह आगे भी कभी न हो। ऐसी स्थिति में, विघ्न की आशंका तक को मिटा देने के लिए यदि मंगल किया जाए तो उसकी व्यर्थता की कल्पना ही व्यर्थ कही जाएगी। शिष्टाचार भी इसी पक्ष में है। कोई किसी शर्त के साथ तो शिष्टाचार का पालन कर चुका।
दूसरी बात यह है कि यदि किसी भी स्थिति में मंगल को निष्फल मान लें, तब तो पूर्वोक्त श्रुति ही अप्रामाणिक हो जाएगी। और श्रुति की अप्रमाणिकता असंभव है। इसलिए वहाँ उसके अभिप्राय को थोड़ी और गहराई से समझना होगा। ‘पापी को प्रायश्चित करना चाहिए’ इस वेद-वाक्य के अनुसार निष्पाप व्यक्ति को तो प्रायश्चित्त कदापि न करना चाहिए; किंतु यदि कोई निष्पाप व्यक्ति किसी प्रकार के पाप के भ्रम से प्रायश्चित कर डालता है तो जैसे इसी कारण से पूर्वोक्त वेद-वाक्य अप्रमाणित नहीं हो जाता वैसे ही विघ्न-विषयक श्रुति भी विघ्न की विद्यमानता में ही व्यवहृत होगी। अर्थात् विघ्न के रहने पर ही उसके ध्वंस के लिए प्रवृत्त कराएगी। फलत: वह निष्फल नहीं हो सकती और न शंका मात्र के निवारण के लिए भी किया गया मंगल ही निष्फल सिद्ध हो सकेगा।
इस प्रकार मंगलाचरण के तीन प्रयोजनों (शिष्टाचार की रक्षा, विघ्न-विघात एवं प्रारिप्सित की परिसमाप्ति) की संक्षिप्त आलोचना की जा चुकी, अब चौथे–अंतिम पर भी, थोड़े से शब्दों में, विचार किया जा रहा है। किंतु इस प्रयोजन की अवतारणा के पूर्व उसकी आवश्यकता समझ लेनी होगी। ऐसा कहा जा सकता है कि श्लोक-बद्ध (या वाक्य बद्ध, बाह्य) मंगलाचरण की कोई आवश्यकता नहीं है–मन से या मन में भी मंगल कर लिया जा सकता है, ईश्वर-स्मरण तो विशेष कर मानसिक कार्य है ही। और, ऐसा करने पर न शिष्टाचार का विरोध होता है, न विघ्न-विघात की कमी रहती है। फिर, मुँह खोल कर श्लोक आदि के द्वारा वाचिक मंगल का आचरण अनावश्यक-सा प्रतीत होता है। इसी के समाधान के लिए चतुर्थ (या तृतीय ही, यदि विघ्न-विघात और प्रारिप्सित-परिसमाप्ति को पृथक-पृथक न स्वीकार करें।) प्रयोजन का उल्लेख किया जाता है। वह प्रयोजन है–शिष्य-शिक्षा। अर्थात् सीखने वालों को यह सीख देने के लिए कि ग्रंथ के आदि, मध्य, या अवसान में मंगल किया जाना चाहिए। क्योंकि मानसिक रूप में मंगल कार्य संपन्न कर लेने पर इसकी गुंजाइश नहीं रह सकती। प्रत्येक पाठक पर यह रहस्य नहीं प्रकट हो सकता। और तब मंगल का उद्देश्य भी नहीं पूरा होता।
एक अस्तव्यस्तता और आ जाएगी! वह इस प्रकार कि तब इस विषय का निर्णय करना कठिन हो जाएगा कि कौन-सा ग्रंथ आस्तिक का बनाया हुआ है और कौन-सा नास्तिक का; किसमें मानसिक मंगल किया गया है और किसमें नहीं। अत: वाचिक मंगल करना अनिवार्य है।
इसके अतिरिक्त, नास्तिक लोग किसी भी रूप में मंगल नहीं करते, यह भी दावे के साथ कह सकना कठिन है। क्योंकि इतने अधिक रूपों में ‘अपरोक्ष सत्ता’ की अनुभूति संभव है कि उन सब को सहसा अस्वीकृत कर देना असंभव-सा प्रतीत होता है। एक श्लोक है–
“यं शैवा: समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदांतिनो
बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटव: कर्त्तेति नैयायिका:
अर्हन् इत्यज जैनशासनरता: कर्मेति मीमांसका:
सोऽयं वो विदधातु वाच्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरि:।”
और ये सभी तत्त्व श्रुतियों से अनुमोदित भी हैं–
‘शिव’ (1) ‘महारुद्रादभूप्रकृतिरत: सूत्रं ततोऽहमिति ततो विश्वन्।’ –शैव
‘ब्रह्म’ (2) ‘एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन।’ –वेदांती
‘बुद्ध’ (3) ‘प्राण्यालम्भ नं संसृति नन्दयेति माम्।’ –बौद्ध
‘कर्ता’ (4) ‘सनातना: पशव: प्रविशन्ति प्रमेयानुभूतै: कर्तैव तत:।’ –नैयायिक
‘अर्हन्’ (5) ‘स्वभाव एवेश्वरो नान्योऽस्ति कदाऽप्यस्यानीदृशत्वापत्ते:।’ –जैन
‘कर्म’ (6) ‘कर्मणा जायते नश्यति भयाभयसुखानि।’ –मीमांसक
इत्यादि।
बहुत्व के भीतर से इसी एकत्व का साक्षात्कार करनेवाले ऋषि ने, इसीलिए, कहा–‘एकं सद् विप्रा बहुधा वदंति।’ मैं तो अपने देश की अंत:प्रकृति और प्रवृत्तियों का सूक्ष्म निरीक्षण करने पर यही मानने को तैयार नहीं हूँ कि यहाँ वस्तुत: कोई नास्तिक हो सकता है। जहाँ की सांस्कृतिक उदारता इस सीमा पर पहुँच चुकी हो कि ‘यद् यत् कर्म करोमि तत्त-दखिलं शम्भो तवाराधनम्’–वहाँ नास्तिकता के लिए कहीं बिंदु मात्र अंतराल भी शेष रह गया है?
फिर भी उदयनाचार्य का कहना है कि नास्तिकों के ग्रंथों की निर्विघ्न समाप्ति देखकर उनके पूर्व जन्म में किए हुए मंगलाचरण की कल्पना करनी चाहिए। अन्यान्य आचार्य इससे भिन्न प्रकार की कल्पना करते हैं। उनका मत है कि नास्तिक भी कायिक, मानसिक अथवा ग्रंथ से बाहर वाचिक भी मंगलाचरण कर सकता है। ऐसी स्थिति में पूर्व जन्म तक की दौड़ क्यों कर लगाई जाए? उदयनाचार्य की ही[xvi] एक पंक्ति को पकड़ कर मैं तो ऐसी अटकल लगाता हूँ कि खंडन-मंडन करने के बहाने से ही सही, अनवरत ईश्वर-संबंधी चिंतन करते रहने वाला नास्तिक भी, किसी न किसी रूप में, ईश्वर-स्मरण रूप मंगलाचरण करता ही है। शरद् बाबू ने भी अपने एक उपन्यास में किसी नास्तिक के लिए दार्शनिक उदारता दरसाते हुए लिखा है कि वह वस्तुत: नास्तिक नहीं, ‘नास्ति’-रूप में विद्यमान ईश्वर का उपासक है। महाकवि श्रीहर्ष ने अपने महाकाव्य (नैषधीय चरित) में नल से प्रार्थना करवाई है कि
“नो ददासि यदि तत्वधियं में
यच्छ मोहमपि तं रघुवीर
येन रावणचमूर्युधि मूढ़ा
त्वन्मयं जगदपश्यदशेषम्।” 21।7
हे राम, यदि तुम मुझे तात्विक ज्ञानदान के योग्य नहीं समझते तो कम से कम वैसा प्रगाढ़ अज्ञान भी तो दे दो कि जिससे लड़ाई के मैदान में बावली हुई रावण की सेना सब कहीं तुम्हीं तुम को देखती थी।
अज्ञान पथ का यह वह क्षितिज है, दूसरी ओर से आकर ज्ञान का पथ भी जिससे आ मिलता है और फिर क्षितिज की उदारता उन दोनों को अपनी लचीली बाँहों से बाँध लेती है।
मंगल के प्रकार
मंगल भावात्मक रूप में तो अखंड ही हो सकता है; किंतु व्यावहारिक रूप में उसके प्रयोग-भेद होते हैं जिस कारण उसे कम से कम तीन प्रकारों में निर्दिष्ट किया गया है। वे तीन प्रकार हैं:–
(1) नमस्कारात्मक
(2) आशीर्वादात्मक और
(3) वस्तुनिर्देशात्मक।
इस वर्गीकरण को मान्यता देने के लिए यह वाक्य प्राय: उद्धृत होता है:–
‘आशीर्नमस्क्रिया वस्तुनिर्देशो वा ऽपि तन्मुखम्।’
मंगल के ये प्रकार अपने नाम से ही अपनी परिभाषा गढ़ते दीख पड़ते हैं। ईश्वर-स्मरण का वह प्रकार जिसमें ग्रंथकार नमस्कार द्वारा प्रतिबंधक विघ्नों का नाश करने की प्रार्थना करता है कि जिस विघ्न-ध्वंस के परिणाम-स्वरूप ग्रंथ की निर्विघ्न परिसमाप्ति होती है, नमस्कारात्मक मंगल कहलाता है। यहाँ यह स्मरण रखना होगा कि नमस्कार का यह प्रकार सर्वत्र अभिधा द्वारा नहीं स्फुट होता, प्रत्युत महाकवियों ने तो विशेष कर व्यंजना द्वारा ही इसे अधिक अभिव्यक्त किया है, जो (अभिव्यक्ति) और अधिक चमत्कारकारी होने के कारण प्रारंभ में ही कवि की उच्चतम कोटि की प्रतिभा का आभास दे देती है। काव्यप्रकाश का मंगलाचरण इसी दूसरी शैली का है। रामचरित मानस में पहली (अभिधा) शैली का है–
“वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छंदसामपि
मंगलानांच कर्त्तारौ वंदे वाणी-विनायकौ।।”
‘सूर-सागर’ का मंगलाचरण है:–
“चरन-कमल बंदौ हरि-राइ
जाकी कृपा पंगु गिरी लंघै अंधे कौं सब कछु दरसाइ।
बहिरौ सुनै, गूँग पुनि बोलै, रंक चलै सिर छत्र धराइ।
सूरदास स्वामी करुनामय, बार-बार बंदौ तिहि पाइ।”
यही सब नमस्कारात्मक मंगल के निदर्शन हैं।
आशीर्वादात्मक मंगल पाठकों, दर्शकों या श्रोताओं के विघ्नध्वंस के लिए प्रयुक्त होता है, जैसे नमस्कारात्मक में ग्रंथकार अपने विघ्नों का ध्वंस करने के लिए मंगल करता है। क्योंकि नवीनों ने विघ्नध्वंस का ही साक्षात् कारण मंगल को माना है और समाप्ति का परंपरया, अर्थात् विघ्नध्वंस द्वारा। जो भी हो, मैं इस भेद के भीतर से एकता का संकेत कर चुका हूँ। ग्रंथकार अपने लिए ईश्वर-स्मरण करे या पाठकों के लिए, उद्देश्य-अंश में कुछ नहीं बनता-बिगड़ता है। बस ‘एक तत्व की ही प्रधानता’ वाली बात ठहरी। मंगल का यह प्रकार नाटकों में प्राय: देखने में आता है।
वस्तु-निर्देशात्मक मंगल की कल्पना बड़ी अनोखी है। यह बहुत कुछ गौतम बुद्ध को वेद-निंदक या नास्तिक कह लेने के बाद, उन्हें विष्णु का अवतार मान लेने-जैसे समन्वयवाद की चेष्टा है। इसकी कल्पना में बड़ी दूर-दर्शिता है। वाचिक मंगलाचरण करने न करने मात्र के अंतर से आस्तिकता-नास्तिकता की खुदी खाई इससे पट गई है।
संदर्भ में जिस विषय का उपपादन करना हो, आरंभ से ही, बिना किसी भूमिका के, उसका प्रतिपादन करने लग जाना वस्तुनिर्देशात्मक मंगल आचरण है। वृहत्त्रयी कहे जाने वाले संस्कृत के तीनों महाकाव्यों (किरातार्जुनीयम्, शिशुपालवधम् और नैषधीयचरितम्) में यही (वस्तु-निर्देशात्मक) मंगल है। ‘प्रियप्रवास’ तथा ‘कामायनी’ में भी ऐसा ही है। यही मंगलवाद का संक्षिप्त परिचय है। विस्तार के लिए ‘तत्व-चिंतामणि’ आदि ग्रंथ देखने चाहिए।
संदर्भ
[i] श्व:श्रेयसं, शिवं, भद्रं, कल्याणं, मंगलं, शुभम्। अ. को. 1।25
[ii] यहाँ प्रचलन कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि ये प्रयोग व्याकरण-विरुद्ध है अथवा देशज है और व्याकरण ने इनकी अनुवर्त्तिता मात्र की है।
[iii] मंगलंच विध्नध्वंसद्वारक समाप्तिफलकं कर्म। तच्च देवता नमस्कारादिरूपमेव।
[iv] पवित्रं मंगलम् परम्।
[v] ‘देवतावाचका: शब्दा ये च भद्रादि वाचका:
ते सर्वे नैव निंद्या: स्युर्लिपितो गणतोऽपि वा।’
[vi] ओंकारश्चाथ शब्दश्च द्वावेतौ ब्रह्मण: पुरा
कण्ठं भित्त्वा विनिर्य्यातौ तेन मांगलिकावुभौ।
[vii] अर्थांतरप्रयुक्त एव हि अथ शब्द: श्रुत्या मंगलप्रयोजनो भवति। –शा. भा. 1।
[viii] अपूर्व एव हि लाभो दध्यादेर्लोके मंगलं सूचयति।
[ix] ग्रंथादौ, ग्रंथमध्ये, ग्रंथांते च मंगलमाचरणीयमिति शिष्टाचार:
[x] न पाणिपादचपलो न नेत्रचपलो मुनि: न च वागंगचपल इति शिष्टस्य लक्षणम्।
[xi] एतस्मिन्नार्यावर्ते निवासे ये ब्राह्मणा: कुंभीधान्या अलोलुपा अगृह्यमाणकारणा: किंचिदंतरेण कस्याश्चिद् विद्याया: पारंगता: तत्र भवन्त: शिष्टा:।’
–‘पृषोदरादीनि यथोपदिष्टम्’ (6।3।109) सूत्र पर भाष्य।
[xii] मनु ने भी–“एतद्देशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मन:
स्वं-स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानव:।” लिखा है।
[xiii] समाप्तिकामो मंगलमाचरेत्।
[xiv] ‘वृद्धिरादैच्’ के वृद्धि शब्द को ध्यान में रख कर इसके आरंभ में यह भी लिखा हुआ है–
“मांगलिक: आचार्यो महत: शास्त्रौघस्य मंगलार्थे वृद्धिशब्दमादित: प्रयुंक्ते।”
[xv] यहाँ वकार के आगम को ध्यान में रख कर आरंभ में लिखा हुआ है–
“मांगलिक आचार्यो महत: शास्त्रौघस्य मंगलार्थे वकारमागमं प्रयुंक्ते।”
[xvi] “इत्येवं श्रुति नीति-सम्प्लव-जलैर्भूयोभिराक्षालिते
येषां नास्पदमादधासि हृदये ते शैलसाराशया:
किंतु प्रस्तुतविप्रतीपविधयोऽप्युच्चैर्भव चिच्न्तका:
काले कारुणिक, त्वयैव कृपया ते भावनीया नरा:” –न्यायकुसुमांजलि
Image Courtesy: LOKATMA Folk Art Boutique
©Lokatma