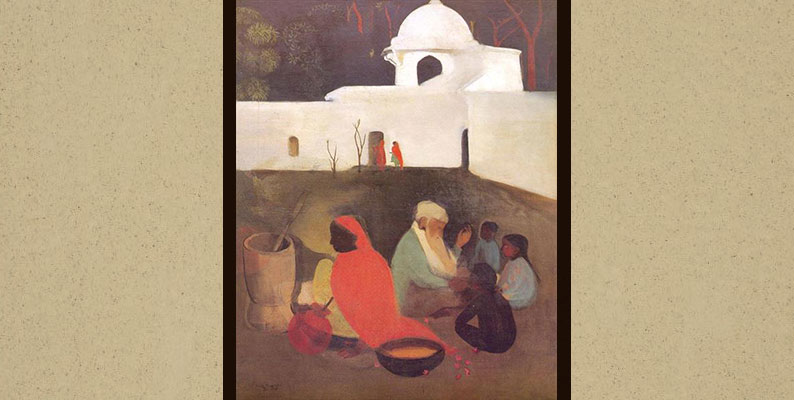आलोचना के नाम पर
- 1 April, 1950
शेयर करे close
शेयर करे close

शेयर करे close
- 1 April, 1950
आलोचना के नाम पर
वर्तमान हिंदी आलोचना को कई वादों में विभक्त किया जा सकता है–रसवाद, प्रगतिवाद, यौनवाद, प्रशंसावाद, काव्यवाद, उद्धरणवाद और अंतत: आतंकवाद। इन वादों की एकांगिता से हिंदी-साहित्य की किस प्रकार अपार क्षति हो रही है इसे सुधी लेखक की लेखनी से ही देखिए–
कहना कठिन है की वर्तमान हिंदी-साहित्य का सतत प्रसार और चतुर्दिक प्रगति आश्चर्य का विषय अधिक है या हर्ष का अथवा खेद का! कविता की बहुलता देखकर संदेह होने लगता है कि कविता लिखने वालों की संख्या अधिक है या पढ़ने वालों की। सड़कों पर संभाल कर, देखभाल कर न चलिए, तो हर दस कदम पर किसी कहानीकार से टकरा जाने की संभावना है। और आलोचना? राम कहिए। आलोचना ही तो एक ऐसी चीज है जिसे बिना किसी तूल-तवील के, बिना किसी साधन के, बिना किसी बुद्धि-वैभव के सभी करने की योग्यता रखते हैं। बात यह है कि हिंदी का ककहरा ख़त्म करते-करते प्रत्येक व्यक्ति कोई न कोई डगर पकड़ लेता है! इतनी सस्ती साहित्यिकता और संभव भी कहाँ है? आवाज सुरीली हुई, तो एक सुंदर-सा उपनाम रख लिया, दो-चार कवि-सम्मेलनों में गाना गाया और महाकवि बन बैठे। ‘रसीली कहानियाँ’, ‘मनोहर कहानियाँ’ जैसी ‘उच्चकोटि’ की पत्रिकाओं के रहते किसी की भी कहानीकार बनने की साध अपूर्ण नहीं रह सकती। और यदि इन दोनों में से कोई मार्ग अपनाना संभव नहीं हुआ, तो फिर आलोचक की गद्दी से कौन उतार सकता है?
इस निबंध में हिंदी साहित्य के किसी दूसरे अंग की चर्चा न कर, केवल उसके आलोचना- साहित्य के संबंध में ही मैं दो शब्द कहना चाहता हूँ; हिंदी में आलोचना के नाम पर जो बहुत कुछ लिखा जा रहा है उसकी एक संक्षिप्त पर विशद रूप रेखा प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जिससे, मेरा विश्वास है कि आपका पर्याप्त मनोरंजन होगा।
सबसे पहले रसवाद। यह सिद्धांत इतना प्राचीन और दृढ़ है कि इसके संबंध में अधिक कहने की आवश्यकता नहीं। संस्कृत की परंपरा से अनुस्यूत रहने के कारण उसकी रसवादी आलोचना से हिंदी का प्रभावित होना सर्वथा न्याय एवं स्वाभाविक है। पर आश्चर्य तो तब होता है जब आज के आलोचक-प्रवर रस का नाम सुनते ही नाक-भौं सिकोड़ लेते हैं, आउट-ऑफ-डेट, औब्सोलीट, रूढ़िवादी आदि फतवे दे बैठते हैं। एक ओर तो यह होता है और दूसरी ओर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना प्रणाली की प्रशंसा करते समय यह भुला दिया जाता है कि वह आउट-ऑफ-डेट रसवादी आलोचना ही थोड़ा पाश्चात्य रंग-ढंग अपनाकर क्रांतिकारी आलोचना के रूप में प्रकट हुई है, कि उस आलोचना की आत्मा और शरीर तो रस की ही है, केवल साजसज्जा अभिनव है; बोतल नई भले ही हो, शराब पुरानी ही है। हिंदी के अधिकांश आलोचकों में सुनी-सुनाई बातों को बिना विचारे दुहराने की जैसी प्रवृत्ति है, वैसी अपनी बुद्धि से कुछ काम लेने की नहीं। जहाँ पश्चिम की चीजें आँख बंद कर ग्रहण कर ली जाती हैं। वहाँ अपने प्राचीन साहित्य पर भी यदि थोड़ा दृष्टिपात करने का श्रम किया जाता, तो बहुत अच्छा होता।
तो मैं यहाँ रसवादी आलोचना के गुण-दोषों का विवेचन नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि चाहे जिस चीज का भी प्रयोग हो, शुद्ध होना चाहिए। आलोचना के प्रसंग में कई आलोचक रस का भी नाम लेना आवश्यक समझते हैं, लेकिन उसके संबंध में जब कुछ कहने लगते हैं, तो ऐसी असंगत भ्रांत एवं हास्यास्पद बातें कह जाते हैं कि देखने पर आश्चर्य होता है। रस तो खैर बहुत उलझा हुआ और गहन विषय ही है, उसका एक अंग जो अलंकार है तथा जो अपेक्षाकृत कहीं सुगम है, उसमें भी ऐसी भूलें की जाती हैं कि जिन्हें देखकर एकबार बिना वाहवाही दिए मन नहीं मानता। यदि रस-संबंधी असंगतियों की थोड़ी भी व्यापक चर्चा की जाए तो इस निबंध का कलेवर बेमानी हो जाएगा, अत: वैसा संभव नहीं है। अलंकार जैसी सुगम वस्तु से संबंध रखने वाली एक दो महान भ्रांतियों का निर्देश कर अपने कथन का समर्थन कर लेना चाहता हूँ।
ये उद्धरण उस व्यक्ति की आलोचना से हैं जो आज के ‘सबसे’ बड़े आलोचक हैं–चूँकि उन्होंने जितने कम समय में और जितनी आलोचना की पुस्तकें लिखी हैं कि उनका वह कार्य संसार का आठवां आश्चर्य होने का दावा भी कर सकता है। उनकी पुस्तकों की पहुँच सबों तक है अत: उनके द्वारा की गई भ्रांतियाँ भी अधिक से अधिक लोगों को भ्रम में डालने की शक्ति रखती है। मेरा तात्पर्य श्री रामरतन भटनागर से है जिनकी उपाधि का प्रत्येक अक्षर सार्थक है। यदि सभी भूलों का उल्लेख किया जाए तो एक पोथा तैयार हो जाए; यह तो पोथी भी नहीं, महज एक निबंध है। पर एक दो नमूने भी कुछ कम मजेदार नहीं हैं।
आपके शब्दों में राधा का ‘अनुपम बाग’ के रूप में यह साँग-रूपक देखिए–
‘अद्भुत एक अनूपम बाग।
जुगल कमल पर गजवर क्रीड़त
तापर सिंह करत अनुराग
हरि पर सरवर, सर पर गिरिवर,
गिरि पर फूले कंज पराग।
रुचित कपोत बसे ता ऊपर,
ता ऊपर अमृत फल लाग
फल पर पुहुप, पुहुप पर पल्लव,
तापर सुक पिक मृगमद काग।
खंजन धनुष चंद्रमा ऊपर,
ता ऊपर इक मनिधर नाग।’
पता नहीं, अलंकार का यह शुद्ध निर्देश देख कर दिवंगत आलंकारिकों की आत्मा क्या सोचती होगी? अथवा स्वयं सूरदासजी गोलोक से अपने इस आलोचक के हाथों अपनी कविता की ऐसी सुंदर समीक्षा देखकर क्या विचारते होंगे? भूल भी होती तो किसी ऐसे स्थल पर, जहाँ भूल का होना क्षम्य समझा जाता। यहाँ तो कहना होगा कि दिन के प्रखर प्रकाश में सूर्य छिप गया है। मैंने भी अलंकार का थोड़ा-बहुत अध्ययन किया है, किंतु कहीं भी सांग-रूपक का यह रूप देखने को नहीं मिला। अलंकार की परिभाषा के अनुसार आँख बंद कर एक बच्चा भी इस पद में अतिशयोक्ति अलंकार की ही स्थिति बताएगा। शायद भटनागर जी की दृष्टि में सांग-रूपक और रूपकातिशयोक्ति में कोई अंतर नहीं है! दोनों जगह रूपक शब्द जो आ गया है।
फिर एक जगह आप कहते हैं–“सूर में स्मृति मूलक अलंकारों का प्रयोग विरोध-मूलक अलंकारों से अधिक मिलता है। इनमे संदेह और स्मरण प्रधान हैं।” संदेह और स्मरण को स्मृति-मूलक अलंकार कहना तो मौलिक अवश्य है, पर आलंकारिकों ने इनके मूल में स्मृति की नहीं, सादृश्य की ही स्थिति मानी है। यदि इस कथन का विश्लेषण किया जाए तो उसका रूप होगा स्मृति-मूलक संदेह और स्मृति-मूलक स्मरण। स्मृति-मूलक स्मरण का क्या अर्थ होता है, यह कम से कम मेरी समझ में नहीं आता। हाँ, सादृश्यमूलक स्मरण मैं समझ सकता हूँ। फिर संदेह स्मृति से होता है, यह भी एक अबूझ पहेली है। सादृश्य के कारण संदेह होते देखा-सुना अवश्य गया है। अग्निपुराण के भगवान् व्यास से लेकर आज तक के किसी भी अलंकारिक को स्मृति के आधार पर अलंकारों का वर्गीकरण करते हुए मैंने नहीं देखा है। पर मौलिक व्यक्ति की शायद यही विशेषता है जो काम किसी ने नहीं किया हो उसे वह कर दिखावे!
‘रूपकातिशयोक्ति में किसी वस्तु के रूप के संबंध में अतिशयोक्ति की जाती है।’ इस कथन के बाद भटनागर जी की मौलिकता का लोहा अवश्य मान गया, शास्त्रीयता का भले ही न मानूँ। यदि भटनागरजी सभी अलंकारों की ऐसी ही परिभाषाएँ लिख मारें तो निश्चय जानिये की कोई भी व्यक्ति इन परिभाषाओं की सहायता से अलंकार-ग्रंथों को त्रिकाल में भी नहीं समझ सकता।
वैसे ही–
‘मुरली तऊ गोपालहिं भावति।
सुन री सखी जदपि नंद-नंदन
नाना भाँति नचावति।’
इस अंश में न मालूम किस अलंकार-ग्रंथ के आधार पर आपने विभावना अलंकार मान लिया है? विरोधाभास का भी आभास देते तो बहुत बुरा नहीं था। उड़े भी तो ऐसा कि विभावना पर जा गिरे!
पूरे दो पृष्ठों में सरसरी नजर से देखने पर केवल चार भूलें हैं। अधिक गिनाना संभव नहीं क्योंकि “बाढ़ै कथा पार नहि लहउँ।” तभी तो साल में दस कवियों की खासी अच्छी, मोटी-तगड़ी आलोचना आसानी से लिखी जा सकती है। सोच-विचार कर शुद्ध लिखने के चक्कर में पड़ा रहने वाला बेचारा तो एक भी कवि की आलोचना नहीं लिख पाएगा। इस तरह की भ्रामक और ऊलजलूल बातों के लिखने से क्या लाभ! इस छोटे-से निबंध में रसवाद के और अंगों की भूलों या और आलोचकों के संबंध में कुछ कहना सर्वथा असंभव ही है। मैंने पहले ही निवेदन किया कि उसके लिए पोथा लिखना आवश्यक होगा। जिन्होंने रसवाद के भीतर बिना पैठे, ऊपर से छू-छाकर ही आलोचना के लिए लेखनी उठा ली है वे तो ऐसी कमाल की बातें कहते हैं कि कुछ मत पूछिए।
आलोचना की दूसरी प्रचलित प्रणाली वह है जिसे प्रगतिवादी या मार्क्सवादी कहते हैं। इस श्रेणी की आलोचना में साहित्य की अच्छाई-बुराई की परख केवल हँसिए-हथौड़े के मानदंड से की जाती है। कोई कितना भी बड़ा कलाकार क्यों न हो, यदि वह किसान-मजदूरों के आंदोलन की, या कम से कम उनकी समस्याओं की चर्चा नहीं करता, तो वह कौड़ी का तीन है और उसकी रचना प्रतिक्रियावादी होने के नाते रद्दी की टोकरी ही में स्थान पाने की अधिकारिणी है। इन आलोचकों की कृपा से प्रगतिवादी परंपरा की प्राचीनता कबीर तक प्रमाणित हो चुकी है। विश्वास न हो तो ‘हंस’ का प्रगति-अंक उठाकर रामविलास शर्मा द्वारा संग्रहीत ‘हिंदी कविता की प्रगतिशील परंपरा’ देख लीजिए। तुलसीदास के विशाल साहित्य में इन लोगों को काम के केवल दो कवित्त मिले हैं; शेष सब निरर्थक, सब वाहियात। रामचरितमानस या विनयपत्रिका सामंतवादी या बुजुआ साहित्य है, क्योंकि उसमें मजदूर-आंदोलन की प्रतिध्वनि नहीं है। तुलसी की वह अमर प्रगतिशील पंक्तियाँ हैं :–
‘खेती न किसान को,
भिखारी को न भीख, बाल,
बनिक को बनिज,
न चाकर को चाकरी।
जीविका-विहीन लोग
सीधमान सोच बस,
कहैं एक एकन सों
कहाँ जाइ का करी।’
यदि गोस्वामी जी की सारी रचनाएँ नष्ट भी हो जाएँ तो केवल ये दो-चार पंक्तियाँ उनकी महत्ता अक्षुण्ण रखने के लिए पर्याप्त हैं! कबीर ने भी कविता कहने लायक केवल 12 पंक्तियाँ लिखीं जो उस प्रगतिशील परंपरा में उद्धृत हैं। बाकी की कोई गणना नहीं, कोई कीमत नहीं? पहली बार संपादित होने वाले इस प्रगति-अंक में प्रगतिशील परंपरा कबीर तक पहुँची है, दूसरी बार कालिदास तक पहुँचेगी और तीसरी बार में वाल्मीकि तक। और फिर तो सारा भारतीय वाड्मय प्रगतिशील! यह है चिंतन की मौलिकता, विचार की स्वतंत्रता! यदि रामविलास जी ने थोड़ा श्रम किया होता तो जायसी, सूर, मीरा आदि से भी प्रगतिशील कविता की एक-दो पंक्तियाँ न सही, एक दो शब्द भी अवश्य ही मिल जाते और इस तरह प्रगतिशील परंपरा कुछ और अधिक दृढ़ हो जाती! ये बेचारे प्रगतिशीलों की पंक्ति में बैठने के सौभाग्य से जो वंचित रह गये वह उनके महान दुर्भाग्य का विलास नहीं तो और क्या समझा जाए? मिस मेयो को सारे भारत में केवल गंदगी दिखाई पड़ी और कुछ नहीं। उसी की जैसी पैनी-दृष्टिवाले ये आलोचक विश्वसाहित्य में केवल भूख, नग्नता, दुख, दैन्य तलाशते और शायद देखते भी हैं और इस प्रकार विशाल प्रगतिशील परंपरा को क्रमश: दृढ़तर तथा महत्तर बनाने में सतत प्रयत्नशील हैं। रंगीन चश्मे से जो भी देखा जाएगा, रंगीन नजर आ जाएगा और रंगीन को ही यदि कोई वास्तविकता मान लेने को ठान बैठा हो तो उसे आत्म-संतोष लाभ करने देना ही उचित है। यदि ये आलोचक यह ध्यान में रखें कि दुनिया हँसिए हथौड़े तक ही सीमित नहीं है, उसका विस्तार उसके अतिरिक्त भी है तो कुछ सच्चाई का अनुभव अधिक स्पष्टता से हो सकेगा।
अब आलोचकों के उस वर्ग पर दृष्टिपात कीजिए जो सिग्मंड फ्रायड की यौनभावना के महामंत्र का एकमात्र उपासक है। उनके विचार से संसार की सारी क्रियाएन यौनभावना से परिचालित हैं। अत: साहित्य भी उस यौनभावना की अभिव्यक्ति का एक माध्यम मात्र है! ये आलोचक दिनरात अविराम रूप से मनोविज्ञान, मनोविश्लेषण आदि पावन मंत्रों का जप करने में लीन रह कर ‘सर्वं ब्रह्ममयं जगत्’ की तरह ‘सर्वं मनोविश्लेषणमयं जगत्’ की सत्यता का सोते-जागते अनुभव किया करते हैं। कभी चेतन से उपचेतन की दौड़ लगाते, कभी उपचेतन से चेतन की सतह पर लौटते और कभी अवचेतन के अतल गह्वर में डुबकी मारते। चेतन-उपचेतन-अवचेतन के चक्कर में कोल्हू के बैल की तरह परिक्रमा करते-करते परेशान! मानव-मन की गहराई में बैठकर उसके सभी व्यापार देख लेने का दावा! यौनभावना की कुंजी से मन के सारे बंद द्वार खोल देने की प्रसन्नता, और फिर काव्य की, सारे साहित्य की व्याख्या आरंभ होती है–कबीर का भावात्मक रहस्यवाद, जिसमें वह बालम को अपने घर बुलाकर ‘एकमेक है’ सेज पर सोने की इच्छा प्रकट करते हैं, अथवा सूरदास का भ्रमरगीत, या मीरा का कृष्ण के विरह में दीवानी बनकर अपने को भूल जाना, या रीतिकाल की शृंगारिक कविताएँ–सभी, केवल अतृप्तकामवासना की काव्यगत अभिव्यक्ति हैं! इस तरह सारे काव्यक्षेत्र को एक यौनभावना के हेंगे से हेंगा दिया जाता है!
मैं जो कुछ कह रहा हूँ उससे यह भ्रम उत्पन्न हो सकता है कि मैं मार्क्सवाद या फ्रायडवाद का विरोधी हूँ। मार्क्सवाद या फ्रायडवाद का क्या, मैं किसी भी ‘वाद’ का विरोधी नहीं हूँ; क्योंकि मैं जानता हूँ कि संसार का कोई भी ‘वाद’ पूर्ण नहीं है–यदि उसमें अच्छाई है तो बुराई भी अवश्य है और यदि बुराई है तो अच्छाई भी निश्चित ही होगी। केवल अच्छी या केवल बुरी वस्तुएँ संसार में अभी तक तो पैदा नहीं ही हुई हैं, आगे की बात भविष्य जाने। हाँ, किसी भी वाद या मत के सबसे बड़े विरोधी या यों कहिए कि वास्तविक शत्रु वे हैं, जो घोर बौद्धिक दासता के शिकार होकर एक उसी वाद को, जिसके वे अनुयायी होते हैं, सत्य एवं निर्दोष मान लेने का भ्रम तथा अपराध करते हैं। जिसने अपनी बुद्धि का संतुलन खो नहीं दिया है, जो गुण-दोष दोनों की सत्ता स्वीकार करता है, जो विवेक अथवा विचार से काम लेने की थोड़ी भी क्षमता रखता है, वह किसी भी वाद का विरोधी नहीं हो सकता। तो मैं मार्क्सवाद या फ्रायडवाद का विरोध नहीं करता, उनकी मखौल नहीं उड़ाता। बल्कि उनकी ओर उनके अंधानुगामियों की एकांगिता पर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ। मार्क्सवाद की दृष्टि में बाह्य जगत ही यथार्थ है, अत: वह आंतरिक व्यापारों की व्याख्या के लिए सर्वथा बाह्य व्यापारों पर निर्भर करता है। इसके प्रतिकूल फ्रायडवाद सारे बाह्य-व्यापारों को आंतरिक व्यापारों से प्रेरित, परिचालित एवं नियंत्रित मानता है। एक बाह्य जगत को प्रश्रय देता है तो दूसरा अंतरजगत को। फिर भी दोनों का दावा कि ‘एक हमीं ठीक हैं’! और इसी एकांगी दृष्टिकोण से साहित्य की सच्ची, निष्पक्ष, वास्तविक आलोचना का झूठा दम भरा जाता है! हालत है उन अंधों की जो हाथी के एक-एक अंग को हाथी मानकर अपनी समझदारी का परिचय दे रहे थे। जैसे युग और परिस्थिति के अनुसार साहित्य बदलता है वैसे ही उसकी आलोचना के सिद्धांत और साधन भी प्रत्येक युग के विभिन्न होते हैं, यह एक महज छोटी-सी बात भी इन पंडितों की समझ में नहीं आती। उदाहरणार्थ, आप प्राचीन रसवाद के सिद्धांत की कसौटी पर आधुनिक साहित्य को घसना शुरू कीजिए और देखिए कि कदम-कदम पर अव्याप्ति अथवा अतिव्याप्ति का मुकाबला करना पड़ता है या नहीं। पहले तो एक नायक का ही परंपरागत लक्षण सहस्रों स्थानों पर बाधित हो जाएगा। तब का नायक होता था–
त्यागी कृती कुलीनत: सुश्रीको
रूपयौवनोत्साही।
दक्षोऽनुरक्तलोक:
तेजो वैदग्ध्य शीलवान् नेता॥
आज के नायक की परिभाषा बनाई जाए तो कुछ ऐसी होगी :–
दीनो दलितः पतितो
बुभुक्षित: शोषितश्चापि।
शिक्षोत्साहविहीन:
श्रमिक: कृषकोऽथवा नेता॥
रस आदि की तो चर्चा ही करना व्यर्थ है। इसलिए एक युग के आदर्श के अनुसार दूसरे युग की साहित्यिक समीक्षा बहुत कुछ असंगत ही होगी। आज की दृष्टि से रीतिकालीन कविता, भले ही भद्दी बताई जाती है, पर यदि सचमुच तब के भावुक की रुचि को भी वह वैसी ही लगती तो एक-एक दोहे-सवैये पर जो अशर्फियाँ लुटाई जाती थीं वे निश्चय ही नहीं लुटाई जातीं। 200 वर्षों तक वह फूलती-फलती रही, यही इस बात का प्रमाण है कि उस काल में वह रुचिकर भी थी, रमणीय भी थी।
इन तीन प्रचलित, सामान्य आलोचनात्मक सिद्धांतों के बाद मैं कुछ उन वादों के संबंध में कहना चाहता हूँ जिनकी ओर, मेरी समझ से, आपका ध्यान इस रूप में नहीं गया होगा। इन आलोचना की प्रणालियों में सबसे पहले मैं उसकी चर्चा आवश्यक समझता हूँ जिसे मैंने ‘प्रशंसावाद’ का नाम दिया है। और जब प्रशंसा एक ‘वाद’ का रूप धारण करेगी तो उसकी अभिन्न सहचरी निंदा बिना अपना हिस्सा लिए कैसे चुप बैठ सकती है? इस तरह ‘प्रशंसावाद’ के साथ ‘निंदावाद’ अनिवार्य भाव से लगा है। इस वर्ग के आलोचक और जिनकी संख्या हिंदी के दुर्भाग्य से बहुत बड़ी है, व्यक्तिगत राग द्वेष से प्रेरित होकर कलम उठाते हैं। वे आलोचना क्या लिखेंगे, या तो विरुदावली गाते हैं या गाली देते हैं। ये लोग पहले ही ठान लेते हैं कि अमुक व्यक्ति को आसमान पर चढ़ा देना है अथवा अमुक को रसातल में ढकेल देना है। इसकी जड़ कितनी गहरी गई है इसका अनुमान तो आज से चौथाई शताब्दी से भी अधिक पूर्व देव और बिहारी को लेकर देवासुर संग्राम की तरह होने वाले उग्र संग्राम से सहज ही किया जा सकता है। आप कहेंगे कि वह आलोचना का प्रारंभिक काल था, पर आज आलोचना के बहुत कुछ तथाकथित वैज्ञानिक हो जाने पर भी उस दोष से क्या पिंड छूट पाया है? मुझे तो ऐसा लगता है कि वह व्याधि समय की प्रगति के साथ कुछ और बद्धमूल ही हुई है। आज की पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित होने वाली आलोचनाओं पर ध्यान दीजिए तो मेरे कथन के समर्थन की अपरिमित सामग्री मिल जाएगी। एक-एक व्यक्ति को लेकर या तो प्रशंसा का पुल बाँधा जा रहा है या गालियों की बौछार की जा रही है।
क्या अजीब तमाशा है? कुत्सित, सिद्धांतहीन विचारों को आलोचना का नाम दिया जा रहा है। निरंकुशता का ऐसा तांडव नृत्य? रुचि-स्वातंत्र्य का ऐसा दुरुपयोग? कृति की आलोचना के बदले व्यक्ति की आलोचना? कृति के संबंध में जब कुछ कहने को नहीं रहता तो व्यक्ति पर कीचड़ उछालना, भला-बुरा कहना, अंत में गाली-गलौज तक पर उतर आना! वैसे ही जब किसी की प्रशंसा करने लगे तो यह भूल गए कि आप उसके आलोचक हैं, चारण नहीं। इस तरह के उदाहरण दिए जाएँ तो यह लेख पुस्तक का रूप धारण कर सकता है। आपके मनोरंजन के लिए कुछ ही नमूने काफी होंगे।
आगे के उद्धरण श्रीरामविलास शर्मा द्वारा लिखित दो आलोचनाओं से हैं। पहली आलोचना का नाम है ‘स्वर्ण-किरण’ और ‘स्वर्ण-धूलि’ जिसमें पंत जी की दो कला-कृतियों की समीक्षा का प्रयास किया गया है और अक्टूबर (1948) के ‘हंस’ में प्रकाशित हैं। दूसरी आलोचना का शीर्षक है ‘कवि दिनकर’ : ‘उदय और अस्त’ जो पटने से प्रकाशित होने वाले ‘उदयन’ के मार्च (1949) के अंक में छपा है। इन दोनों आलोचनाओं को आरंभ से अंत तक पढ़ जाइए, आपको एक अक्षर भी पंत या दिनकर की अच्छाई के संबंध में नहीं मिलेगा। अच्छाई न हो, न मिले, पर क्या यह मान लिया जाए कि पंत की दोनों पुस्तकों में केवल दोष ही दोष है, गुण का नाम भी नहीं, और दिनकर का सारा साहित्य ‘प्रचार का साधन’ मात्र है? मैं कम से कम ऐसा नहीं मानता और मुझे विश्वास है कि कोई भी सहूलियत या समझ का आदमी ऐसा कहने का साहस नहीं कर सकता। फिर यह एकांगिता क्यों? ये आलोचनाएँ शुद्ध, निष्पक्ष आलोचना की दृष्टि से नहीं लिखी गयी हैं; इतना असंदिग्ध है। इनके पीछे द्वेष की प्रेरणा है, वह सैद्धांतिक हो, या व्यक्तिगत या और किसी कारण से उत्पन्न! मैं रामविलास जी को एक ठिकाने का आलोचक मानता हूँ, जो यदि चाहे तो गंभीर, सच्ची और संतुलित आलोचना लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ का छिछलापन एवं असंतुलन वस्तुत: आश्चर्यकर है और खेदजनक तो है ही। जब ऐसे लोगों की लेखनी की यह दशा है तो मानना पड़ता है कि हिंदी की आलोचना के दारुण दुर्भाग्य की अवधि निकट भविष्य में समाप्त होने वाली नहीं है।
जिन उद्धरणों की ऊपर चर्चा आई है उनमें से कुछ ये हैं–…‘हिंदुस्तान की जनता कितनी भी पिछड़ी हुई हो, वह किसी दूसरे की रोटी के सहारे नहीं जीती। हिंदुस्तान का पिछड़ा से पिछड़ा हुआ किसान पंत जी से ज्यादा दर्शन समझता है। वह ईमानदार है इसलिए रामनामी के नीचे कामशास्त्र नहीं छिपाता! और सजीव भाषा का प्रयोग तो वह इन्हें युगों तक सिखा सकता है।’
और इतना कहते-कहते अंत में आप उपसंहार करते हैं–‘स्थाई साहित्य, सुंदर साहित्य, ऐसा साहित्य, जिसे जनता युगों तक अपने हृदय में स्थान दे, कायर, अनैतिक और सिद्धांतहीन व्यक्तियों की रचना नहीं हो सकता।’
ये दोनों उद्धरण कितनी संयत और सुरुचिपूर्ण मनोवृत्ति का परिचय देते हैं? यह कृति की आलोचना है या व्यक्ति की? मैं तो रामविलास जी के ही शब्दों में थोड़ा परिवर्तन करके कहना चाहता हूँ कि–
‘स्थाई आलोचना, सुंदर आलोचना, ऐसी आलोचना जिसे जनता युगों तक अपने हृदय में स्थान दे, दोषदर्शी, संकीर्णताग्रस्त और आलोचना की आड़ में व्यक्तिक एवं अश्लील आक्षेप करने वाले व्यक्तियों की रचना नहीं हो सकती।’
इसी प्रकार दिनकर के संबंध में भी रामविलास जी के ये वाक्य दर्शनीय हैं–
“…लेकिन दिनकर किस-किसके फरमान पर कविता लिखते रहते हैं, यह क्या किसी से छिपा रह गया है? यह तटस्थता का शंखनाद अपनी साहित्यिक गुलामी छिपाने के लिए किया गया है, उस कला के रोजगार को छिपाने के लिए जो किसानों और मजदूरों में क्रांतिकारी जोश भरने के बदले पूँजीपतियों के इशारे पर कम्युनिस्ट विरोध का बॉल-डांस दिखाती रहती है।”
दिनकर किस-किस के फरमान पर कविता लिखते रहे हैं, यह तो अभी बहुतों से छिपा है; लेकिन रामविलास जी मार्क्सवाद की स्वाभाविक उपज घृणा और द्वेष के फरमान पर यह आलोचना लिख रहे हैं, यह मुझसे या इस आलोचना को आलोचक की शुद्ध दृष्टि से पढ़ने वाले किसी भी व्यक्ति से छिपा नहीं है, यह पक्का है।
दिनकर की कला पूँजीपतियों के इशारे पर कम्युनिस्ट-विरोध का बॉल-डांस दिखाती रही है, इसमें निष्पक्ष आलोचकों के लिए संदेह की बहुत काफी गुंजायश है, लेकिन रामविलास जी की यह आलोचना, घृणा के उर्वर क्षेत्र में फलने-फूलने वाले मार्क्सवाद के इशारे पर बुद्धिवाद के घोर विरोध का बॉल-डांस दिखा रही है, यह बिना किसी हिचक के कहा जा सकता है।
आगे आप फिर कहते हैं–
“मुँह से साहित्य की स्वतंत्रता घोषित की जाती है, काम से साहित्य को पूँजीवादी राजनीति का गुलाम बनाया जाता है। कहा जाता है–‘साहित्य राजनीति का अनुचर नहीं, वरन् उससे भिन्न एक स्वतंत्र देवता है।’ (‘मिट्टी की ओर’ : दिनकर) लेकिन यह स्वतंत्र देवता सरकारी मोटर पर बैठा हुआ क्यों नज़र आता है? उसका देवत्व लाउडस्पीकर से किसके रचे हुए गीत ब्रॉडकास्ट करता है? या वह अनुचर न होकर बिहार-केसरी को ही राजनीति सीखा रहा है?”
एक स्थान पर दिनकर के कथन की आलोचना करते हुए आप निर्णय देते हैं–‘लेकिन इस समन्वयवाद की असलियत क्या है? असलियत यह है कि यह न छायावाद है, न प्रगतिवाद, यह है सीधा अवसरवाद; यह है अपनी जनता से दगा और पूँजीवाद की ड्योढ़ी पर दरवानगीरी!’
मैं रामविलास जी को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जहाँ तक अवसरवाद या अपनी जनता से दग़ा अथवा पूँजीवाद की ड्योढ़ी पर दरवानगीरी का प्रश्न है, वहाँ तक इसके खासे अच्छे और अधिक उदाहरण समता के अभिमानी तथा अपने को कम्युनिस्ट घोषित करने वालों में से ही आपको मिल जाएंगे। ढूँढ़ने के लिए केवल थोड़े विवेक और तटस्थता की आवश्यकता है। और मैं तो स्पष्ट कहूँ कि आपकी यह पूरी आलोचना पढ़ जाने पर दिनकर के व्यक्तित्व के संबंध में, सही या गलत, आप जो कुछ कह रहे हैं, उसे तो अच्छी तरह समझ सका, पर दिनकर की कृतियों के संबंध में भी आपकी कोई धारणा है, यह नहीं जान सका। यदि आपके ही के कथनानुसार दिनकर का सारा साहित्य ‘प्रचार का साधन’ मात्र है तब तो उसे अवश्य निर्दोष होना चाहिए; क्योंकि मार्क्सवादी दृष्टिकोण से साहित्य का उद्देश्य, प्रचार के अतिरिक्त, और भी कुछ होता है, यह अभी लोगों को जानने को बाकी है।
आपकी दृष्टि में दिनकर का सारा साहित्य प्रचार का साधन मात्र हो सकता है, किंतु अगणित काव्य-मर्मज्ञों, सुधी समीक्षकों एवं हिंदी भाषी जनता की दृष्टि में दिनकर के साहित्य का स्थान बहुत-बहुत ऊँचा है। यदि आप इसे नहीं जानते तो मैं इसे जना देना अपना कर्तव्य समझता हूँ।
मैं इस वितंडा को अधिक बढ़ाना नहीं चाहता; क्योंकि कहने-सुनने के लिए बातों की कमी नहीं है। उपर्युक्त उद्धरणों और उनके संबंध में अपनी ओर से दो-चार शब्द कहने का लक्ष्य केवल आलोचना की एकांगिता और संकीर्णता दिखाना है। प्रगतिवाद बड़ा सुंदर शब्द है और जहाँ तक मैं समझ सका हूँ, उसका अर्थ भी बड़ा सुंदर है। उसे बदनाम करने का श्रेय ऐसी ही आलोचनाओं को है। यह दोष केवल प्रगतिवाद ही तक सीमित नहीं है, उसमें कुछ उत्कट रूप से वर्तमान भले ही हो। इस प्रकार की निंदावादी आलोचना का क्षेत्र बहुत बड़ा है।
(क्रमश:)
Image Source: Wikimedia Commons
Image in Public Domain