भारतीय संस्कृति के पुरोधा रामविलास शर्मा
- 1 April, 2015
शेयर करे close
शेयर करे close
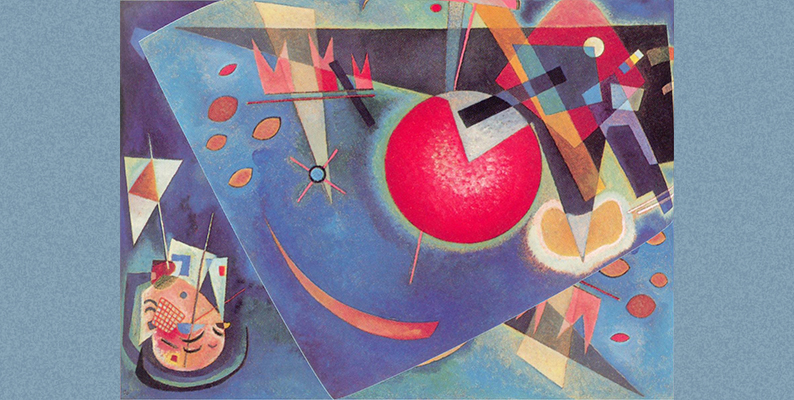
शेयर करे close
- 1 April, 2015
भारतीय संस्कृति के पुरोधा रामविलास शर्मा
रामविलास शर्मा बहुमुखी प्रतिभा के लेखक थे, जिन्होंने भाषा विज्ञान, इतिहास, संस्कृति, साहित्यालोचन जैसे क्षेत्रों में विपुल लेखन कार्य किया। यह एक सौ से अधिक किताबों के लेखक थे (शायद इसीलिए उनकी रचनावली अभी तक प्रकाशित नहीं हो सकी है) और उनकी प्रत्येक किताब के लिए उन्हें पी-एच.डी. या डी.लिट्. की उपाधि दी जा सकती है। वह 1934 से 2000 तक (66 वर्ष) निरंतर गंभीर लेखन करते रहे तथा उन्होंने अनेक विषयों पर मौलिक चिंतन-लेखन किया जिन पर वाद-विवाद-संवाद लगातार होते रहे हैं। डॉ. शर्मा ने सर्वप्रथम ‘हिंदी जाति’ की अवधारणा पेश की जिसका तात्पर्य हिंदी क्षेत्र की सामूहिक अस्मिता से था, क्योंकि हिंदी पट्टी को ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने उपेक्षित किया क्योंकि इस क्षेत्र के लोगों ने एकता का परिचय देते हुए 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम लड़ा था। मगर दुःखद है कि कुछ भारतीय भी एकांगी होकर इसे गायपट्टी (काऊबेल्ट) या ‘गोबरपट्टी’ कहते नहीं थकते। डॉ. रामविलास शर्मा ने इन दोनों आयामों को बेनकाब किया और हिंदी क्षेत्र की विविधता, बहुलता, प्रगतिशीलता तथा एकता को इतिहास सम्मत साक्ष्यों से बखूबी सिद्ध किया है। यह ‘हिंदी जाति’, जाति-पात, बिरादरी या नस्ल के अर्थ में नहीं है बल्कि हिंदी क्षेत्रीय उपराष्ट्रीयता (सब-नेशनलिटी) के अर्थ में है मगर राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद का विरोधी नहीं है। उनके शब्दों में ‘जैसे राष्ट्रीयता के बिना अंतरराष्ट्रीय का अस्तित्व संभव नहीं है, वैसे ही जातीयता के बिना राष्ट्रीयता का अस्तित्व संभव नहीं है। फिर राष्ट्र चाहे एकजातीय हो, चाहे बहुजातीय।
बहुजातीय राष्ट्र में अनेक भाषाएँ बोलने वाले, अनेक जातियों के लोग रहते हैं, मगर उनमें यह न्यूनतम चेतना हो कि वे एक राष्ट्र के नागरिक हैं। डॉ. शर्मा इसका प्रमाण महाभारत में खोजते हैं जब भीष्म पर्व में धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि यह भारत वर्ष क्या है जिसके लिए कौरव-पांडव लड़ रहे हैं। संजय विभिन्न नदियों और पहाड़ों के नाम बताते हैं और जनपदों यथा कुरु, पांचाल, शूरसेन, कोसल, उत्कल, काश्मीर, गान्धार, केरल, कर्नाटक का उल्लेख करते हैं। इसे डॉ. शर्मा भारतवर्ष का नक्शा मानते हैं। मगर मेरी समझ से डॉ. शर्मा भारतीय प्राचीन राजनैतिक व्यवस्था को जरूरत से ज्यादा खींच-तानकर प्राचीन भारत में राष्ट्र का अस्तित्व सिद्ध करते हैं जबकि राष्ट्र एक आधुनिक अवधारणा है। प्राचीनकाल और मध्यकाल में संप्रभु राष्ट्र-राज्य नहीं था, भले उसके अविकसित रूप छिटपुट रहे हों। हिंदी क्षेत्र के बिहार में मगध साम्राज्य (पाटलिपुत्र), गौतम बुद्ध की ज्ञानस्थली (बोधगया), गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली (पटना साहिब), महावीर जैन की जन्मस्थली (वैशाली), लिच्छवियों का गणतंत्र, दीदारगंज की यक्षिणी, महात्मा गाँधी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन (चंपारण) का अमूल्य योगदान भारतीय संस्कृति में रहा है। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में सारनाथ (बौद्ध), मथुरा (कृष्ण), प्रयाग (संगम), बनारस, लखनऊ (गंगा-जमुनी संस्कृति), आगरा (ताजमहल) आदि का काफी महत्त्व राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना विकसित करने में रहा है। भारत राष्ट्र के निर्माण तथा भारतीय संस्कृति के विकास में हिंदीप्रदेश की निर्णायक भूमिका को डॉ. शर्मा रेखांकित करते हैं–‘ऋग्वेद, अथर्ववेद, उपनिषद्, महाभारत, रामायण, अर्थशास्त्र की रचना यहीं हुई। यहीं कालिदास और भवभूति ने अपने ग्रंथ रचे और मौर्य तथा गुप्त साम्राज्यों की आधार भूमि यही प्रदेश था। उत्तर काल में दिल्ली, आगरा इस प्रदेश के बहुत बड़े नगर बने। ये व्यापार के बहुत बड़े केंद्र थे और सांस्कृतिक केंद्र भी। विद्यापति, कबीर, सूरदास, तुलसीदास जैसे कवि इसी क्षेत्र में हुए। इसी प्रदेश में प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का जन्म हुआ। अपने स्थापत्य सौंदर्य से संसार को चकित कर देने वाला ताजमहल इसी प्रदेश के आगरा नगर में हैं।’ (भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रवेश) उनकी हिंदी जाति की अवधारणा के पीछे एक सकारात्मक सोच है– सामंतवाद में भेदभाव और विघटन की प्रबलता होती है जबकि हिंदी जातीयता में एकीकरण एवं समावेशन होता है। इस समावेशन के सूत्रों की खोज वह इतिहास में करते हैं। ऋग्वेद के की एक महत्त्वपूर्ण घोषणा को वह उद्धृत करते हैं–‘न ऋते श्रान्तस्य सख्याय देवाः’ (4.3.11)–देवता उसी के सखा बनते हैं जो परिश्रम करता है। जाहिर है श्रम की महत्ता एवं प्रतिष्ठा ऋग्वेदकाल में थी, यह निश्चित रूप से सराहनीय है। यहाँ तब शारीरिक एवं मानसिक श्रम-विभाजन नहीं था अर्थात् समाज में भेदभाव, विषमता और विभाजन नगण्य था। अस्तु, ऋग्वेदकालीन ऋषि अपना घर बनाते थे, पुर बसाते थे, खेत नापते थे और उनके देवता पृथ्वी तथा आकाश नापते थे। इसलिए डॉ. शर्मा मानते हैं कि नापने का काम ज्यामिति के प्रारंभिक ज्ञान के बिना संभव नहीं है। इसके अलावा वह इस भ्रांति का भी खंडन करते हैं कि भारत महज ग्राम समाजों का देश है क्योंकि प्राचीनकाल में पाटलिपुत्र, काशी, मथुरा और उज्जयिनी जैसे बड़े नगर भारत में मौजूद थे। बौद्धकाल में 16 महाजनपद प्रसिद्ध थे। इसलिए उनका यह मानना सही है कि इन नगरों के कारण हमारे देश के लोग व्यापार, तीर्थ आदि के लिए एक-दूसरे से जुड़े थे तथा नगरों के कारण हिंदी का प्रसार भी संभव हुआ है।
डॉ. शर्मा ने एक महत्त्वपूर्ण बात कही है कि ‘रामायण’ (वाल्मीकि) में किसी देवता की स्तुति नहीं की गई है–‘ऐसा धर्मनिरपेक्ष काव्य शायद ही किसी और ने लिखा हो। प्रक्षिप्त अंशों में जो देव आते हैं, वे पहचाने जा सकते हैं। मुख्य घटनाक्रम का विकास किसी देवता की दखलंदाजी का मोहताज नहीं है। जीवन में दुःख आता है तो वह भी मनुष्य के कर्मों का परिणाम है; और मनुष्य उस दुःख पर विजय पाता है तो यह उसके पुरुषार्थ का परिणाम है। दुःख से निवृत्त होने के लिए वह किसी देवता से प्रार्थना नहीं करता। इस दृष्टि से रामायण अत्यंत सांसारिक और लोकवादी काव्य है।’ (‘भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश’) आगे उन्होंने यह भी रेखांकित किया है कि रामायण में मानव मात्र के लिए प्रेम है तथा वनचारी जीवों के प्रति भी प्रेम है। वाल्मीकि ने शुरू में ही लिखा है ‘जनश्च शूद्रोपि महत्त्वमीयात्’ (रामायण की कथा पढ़ने और सुनने से शूद्र जन भी महत्त्व प्राप्त करते है) तब ऐसा कवि शंबूक-वध की कल्पना कैसे कर सकता था? इसके अलावा हजारों साल तक जीना, तपस्या करना आदि असंभव प्रसंग प्रक्षिप्त अंश हैं। इसी प्रकार वैष्णव धर्म का प्रचार होने पर राम को विष्णु का अवतार बताना भी प्रक्षिप्त अंश है। डॉ. शर्मा के अनुसार रामायण में बाद में जोड़े गये प्रक्षिप्त अंशों में तीन तरह की प्रवृत्तियाँ दिखती हैं: पहली, मानुष काव्य का दैवीकरण-वैष्णव भक्तों द्वारा राम को विष्णु का अवतार बनाना तथा अनेक चमत्कारिक घटनाएँ जोड़ना। दूसरी, सांसारिक काव्य का पुरोहितीकरण-ब्राह्मणों को अति महत्त्व देना। तीसरी, काव्य का पुराणीकरण-पुराणों की नैमिषारण्य वाली धारा में कई असंभव घटनाएँ जोड़ी गईं। अस्तु, इन तीन प्रवृत्तियों को हटाने से रामायण महाकाव्य की श्रेष्ठता बढ़ जायेगी। वह यह भी मानते थे कि महाभारत की तरह रामायण इतिहास भी है क्योंकि यह मगधों और कोसलों की संघर्ष-कथा है तथा प्राचीन काल में उच्च स्तर का स्थापत्य मगधों की अमूल्य देन है।
जहाँ तक ‘महाभारत’ का सवाल है, डॉ. शर्मा का मानना है कि वहाँ दो प्रकार के धर्म हैं। पहला, लोक रीति या लोकव्यवहार में जो मान्य है, वही धर्म है। दूसरा, लोक से अधिक परलोक से जुड़ा हुआ, दैवी शक्तियों का अस्तित्व मानने वाला तथा स्वर्ग-नरक में कर्मफल पर जोर देने वाला है। दूसरे धर्म में कई उपभेद हैं : कुछ लोग इंद्र और ब्रह्मा को सबसे बड़ा देवता मानते हैं, तो दूसरे लोग ब्रह्मा, विष्णु, महेश की त्रयी स्थापित करते हैं। फिर एक ओर पुरोहितगण यज्ञ और कर्मकांड को सफलता के लिए जरूरी मानते हैं, तो दूसरी ओर भक्ति सिद्धांत शुद्ध मन से देवोपासना पर जोर देता है। डॉ. शर्मा आगे कहते हैं कि युधिष्ठिर के गणव्यवस्था वाले धर्म (जिसका विघटन हो रहा था) की जगह ‘मानवतावादी धर्म’ की स्थापना कृष्ण करते हैं जिसमें वह सांख्य, योग और वेदांत के साथ लोकायतवादी विचारधारा प्रतिष्ठित करते हैं मगर इस तर्क को मानने में कठिनाई है क्योंकि कृष्ण ने कहा है (गीता)–‘सर्वधर्माणि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज’ (सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ) इस कथन में निरंकुशता एवं व्यक्तिवाद की गंध आती है। दरअसल धर्म एक व्यक्ति नहीं बना सकता बल्कि (यह एक दीर्घकालिक सामाजिक प्रक्रिया है जो देशकाल सापेक्ष होती है तथा सामूहिकता की प्रधानता होती है) इस धर्म संबंधी स्वातंत्र्य के अलावा डॉ. शर्मा की एक और मौलिक स्थापना है कि ऋग्वेद, उपनिषद् और महाभारत में दर्शन की प्रधानता है और वेदांत हो या सांख्य, यह दर्शन मूलतः यथार्थवादी है तथा दर्शन का विकास संघबद्ध धर्म से पहले होता है। यह दर्शन अद्वैतवादी है–मनुष्य को प्रकृति का अंग समझता है तथा आत्मा-परमात्मा में भेद नहीं करता। यह दर्शन विशुद्ध विवेकवादी नहीं है, बल्कि यह कवियों की सृष्टि है (अनुभव और कल्पना दोनों का मेल)। उनके अनुसार महाभारत की प्राचीनता का आधार उसमें कर्तारूप ईश्वर का कम से कम उल्लेख होना है। उनके शब्दों में, ‘महाभारत को धर्मशास्त्र बनाने का बहुत प्रयत्न किया गया, फिर भी अपने वर्तमान रूप में उसमें दर्शन की प्रधानता है, धार्मिक अंधविश्वासों की नहीं।’ (भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश) यह स्थापना सही है यद्यपि यह भी सही है कि अधिकतर हिंदू घरों में रामायण और महाभारत को लाल कपड़े में लपेटकर पवित्र धर्मग्रंथ के रूप में पूजास्थल पर रख दिया जाता है और उसे पढ़ने-समझने की प्रवृत्ति नगण्य है। डॉ. शर्मा ‘छांदोग्य उपनिषद्’ का हवाला देते हैं जहाँ ‘धार्मिक’ शब्द का प्रयोग हुआ है–ऐसा व्यक्ति जो अध्ययन करता है, सद्गृहस्थ का जीवन जीता है, इंद्रियों को वश में रखता है, प्राणियों पर हिंसा नहीं करता, गुरु के कार्यों को पूरा करता है। वृहदारण्यक उपनिषद् में कहा गया है–‘वह जो धर्म है, निश्चय सत्य ही है।’ ‘छांदोग्य उपनिषद्’ में धर्म के तीन स्कंध (आधार स्तंभ) बताये गये हैं–पहला, यज्ञ; अध्ययन एवं दान; दूसरा, तप; तीसरा, आचार्यकुल में रहने वाला ब्रह्मचारी जो अपने शरीर को क्षीण कर देता है। मगर वह यह भी मानते हैं कि भारतीय इतिहास में वर्णव्यवस्था जहाँ अधिक परिपक्व हुई, वहाँ वर्णाश्रम धर्म के नियम कठोर बनाये गये। यों पी.वी. काणे ने कहा है कि प्राचीनकाल में यदि पुरोहिताई और दान-दक्षिणा से ब्राह्मणों की जीविका न चल सके, तो वे क्षत्रिय और वैश्य की वृत्तियाँ अपना सकते थे। सभी धर्मों यथा तीर्थों, यज्ञों एवं व्रतों पर कुलधर्म भारी पड़ता है।
डॉ. शर्मा ने यह भी विवेचना की है कि महाभारत में इतिहास की दो धाराएँ निहित हैं : विकासवादी एवं अपरिवर्तनवादी। पहली धारा के अनुसार शुरू में समाज वर्णहीन था मगर कालांतर में गुण-दोष के आधार पर वर्ण बने तथा समाज में वर्ण-संकरता मौजूद रही है। दूसरी धारा के अनुसार शुरू से ही चार वर्ण थे और उनमें ब्राह्मण एवं क्षत्रिय श्रेष्ठ थे जबकि वैश्य का स्थान तीसरा तथा शूद्र का स्थान चौथा था। जल भरी सरस्वती का उल्लेख है, ‘नदी पिबन्ति विपुलां सरस्वतीम्’, ‘सरस्वत्यरुणायाश्च संगम लोकविश्रुतम्’ ‘ततो गत्या सरस्वत्याः सागरस्य च संगमे’, ‘ततः सरस्वतीकूले समेषु मरुधन्वसु’ आदि वर्णन सरस्वती नदी के जल से भरी होने के पक्ष में हैं, तो दूसरी ओर जलहीन सरस्वती का वर्णन है जिसके आसपास की जमीन मरुभूमि बन रही है। इससे स्पष्ट है कि सामाजिक एवं प्राकृतिक कारणों से सरस्वती नदी विलुप्त हो गई।
डॉ. शर्मा ने इस भ्रांति का खंडन किया है कि प्राचीन भारत में आर्य गोरे थे और दास काले थे तथा गोरे लोग काले लोग पर शासन करते थे। उन्होंने साक्ष्यों सहित विश्लेषण किया है कि यदि ऐसा था तो राम और कृष्ण जैसे काले लोग को आर्यों ने अपना नायक दो महाकाव्यों (क्रमशः रामायण एवं महाभारत) में क्यों बनाया था? फिर अर्जुन भी काले थे। भीष्म ने महाभारत में कहा है : ‘जो अपार संकट से पार लगा दे, नौका के अभाव में डूबते हुए को नाव बनकर जो सहारा दे, वह शूद्र हो या कोई अन्य, सर्वथा सम्मान के योग्य है।’ भारतीय दर्शन में वाद-विवाद की परंपरा रही है। चरक संहिता में ‘स्थापना’ और ‘प्रतिस्थापना’ का जिक्र है तथा कौटिल्य के ‘अर्थशास्त्र’ में पूर्व पक्ष तथा उत्तरपक्ष का उल्लेख है। अर्थशास्त्र के अनुसार चारों वर्णों के लोग सेना में भर्ती हो सकते हैं। यद्यपि वहाँ ब्राह्मणों को ऊँचा स्थान दिया गया है, मगर वे पृथ्वी के देवता नहीं हैं। कुछ अपराधों के लिए वे अन्य वर्णों से अधिक दंडनीय हैं। फिर वनों की रक्षा के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान था। दो प्रकार के ऋषि थे–कुटी बनाकर रहने वाले तथा यायावर। चरक यायावर ऋषि थे और घूम-घूम कर जड़ी-बूटियों का ज्ञान प्राप्त करते थे। चरक संहिता में मूल संपदा गाँवों से प्राप्त हुई जो लोक संस्कृति का हिस्सा थी। बौद्ध एवं जैन मत की तरह वैष्णवों ने भी पशुबलि का विरोध किया। यह माना गया कि यज्ञ में देवता स्वयं आकर अपना अंश ग्रहण करते हैं। डॉ. शर्मा वासुदेवशरण अग्रवाल को उद्धृत करते हैं कि वैदिक धर्म के अनुसार एक अंगिरा सृष्टि के लिए सात अंगिरा बन गये और उसी प्रकार ईरानी धर्म की मान्यता है कि एक अहुरमज्द ने सात अमेषस्पेंद (अमृत आत्माओं) का निर्माण किया। ईरानी संस्कृति का विकास ऋग्वेद के बाद हुआ। अवेस्ता की भाषा ऋग्वेद की भाषा का रूपांतर है यद्यपि ध्वनि तंत्र में अंतर है मगर वैसा अंतर संस्कृत और प्राकृत में भी है। ईरानी धर्म में सात में से अऊहर मज्द को पहला स्थान दिया गया है जैसे वैदिक मत में अंगिरा को सात ऋषियों में पहला स्थान दिया गया है। अस्तु, डॉ. शर्मा का मत है कि भाषा तत्त्वों के साथ सांस्कृतिक तत्त्वों का भी निर्यात पश्चिम की ओर हो रहा था। सात ईरानी अमृत आत्माओं में एक अर्द वहिश्त है जिनका मूल रूप ऋत वशिष्ठ है। डॉ. शर्मा के अनुसार मूल ऋत से अर्द और मूल वशिष्ठ से वहिश्त बना है जैसे मूल असुर से अहुर, वसुमनस् से वोहूमन्, श्वेत से स्पेंद, अमृत से अमेष शब्द बने हैं। इस प्रकार डॉ. शर्मा सिद्ध करते हैं कि औपनिवेशिक सिद्धांत एवं परिपाटी के विरुद्ध व्यवहार में भारतीय संस्कृति ने ईरान के सांस्कृतिक विकास में महती योगदान दिया है।
डॉ. शर्मा इस तथ्य को बार-बार रेखांकित करते हैं कि संस्कृति सामाजिक जीवन को लगातार प्रभावित करती है तथा इतिहास-बोध संस्कृति का महत्त्वपूर्ण अंग है अर्थात् हमारी संस्कृति एक गतिशील, सामाजिक एवं ऐतिहासिक प्रक्रिया होती है। वह इस भ्रांति को खारिज करते हैं कि इस्लाम में एकरूपता थी और सारे आक्रमणकारी मुसलमान एक सामाजिक इकाई थे, क्योंकि तुर्क, ईरानी और अरब मुसलमानों की राजनैतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था में भिन्नता थी। उनके शब्दों में ‘तुर्क जब मुसलमान न बने थे, तब भी आक्रमणकारी थे, जब मुसलमान बन गये तब अपनी वही परंपरा चलाते रहे। ईरानी अपेक्षाकृत सभ्य थे, पहले उन्हें अरब मुसलमानों ने जीता, फिर तुर्क मुसलमानों ने जीता और इन तुर्कों ने आगे बढ़ते हुए अरब मुसलमानों को जीता।’ (भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश) इसके आगे वह यह भी बताते हैं कि धर्म और संस्कृति अलग-अलग चीजें हैं। तुर्कों ने भारत पर आक्रमण किया मगर वे जिस प्रदेश में बस गये, वहीं की भाषा को व्यवहार में लाने लगे। (आखिर शुद्ध संस्कृति जैसी चीज नहीं होती और भाषा निःसंदेह एक सामाजिक-सांस्कृतिक प्रक्रिया है।) दूसरी ओर तुर्की भाषा के तमाम शब्दों को हिंदी ने अपना लिया जैसे अरबी और फारसी शब्दों को सहजता से अपनाया। कुछ तुर्क ईरानियों की भाषा फारसी से काम चलाते थे मगर अधिकतर ने भारतीय भाषाओं में साहित्यिक सृजन किया : ‘बाहर से आने वाले मुसलमान (तुर्क, अरब, ईरानी, पठान) तो बहुत थोड़े थे, अधिकांश मुसलमान सिंधी, कश्मीरी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली तो यहीं के थे। धर्म बदलने से उनकी भाषा और संस्कृति बदलने वाली नहीं थी।’ मध्यकाल में बड़े पैमाने पर हिंदुओं ने इस्लाम में धर्मांतरण किया जिसके कई आंतरिक एवं बाह्य कारण थे। मेरा मानना है कि कुछ लोगों ने सत्ता के लालच में (पद, प्रतिष्ठा, धन-दौलत, खेती-बाड़ी) धर्मांतरण किया : दूसरे लोगों ने हिंदू धर्म के सोपानक्रम में निचले स्थान पर होने के कारण शोषण से मुक्ति के रूप में सामूहिक धर्मांतरण किया : तीसरे लोगों ने बाहरी दबाव एवं मजबूरी में धर्मांतरण किया क्योंकि स्थानीय शासन-प्रशासन की क्रूरता, बर्बरता एवं हिंसा की खिलाफत वे नहीं कर सके। औरंगजेब ने हिंदुओं पर ‘जजिया’ कर लगाया था और कई मुस्लिम आक्रमणकारियों ने हिंदू मंदिरों को लूटा था और हिंदू स्त्रियों को जबरन अपने ‘हरम’ में रखा था। कई हिंदू स्त्रियों ने मुस्लिम शासकों के अत्याचार से बचने के लिए ‘जौहर’ (आग में कूदकर आत्महत्या) कर लिया था।
डॉ. शर्मा इस तथ्य को करीने से रेखांकित करते हैं कि जब मध्यकाल में विदेशी आक्रमण हो रहे थे और देशी सामंत/राजा आपसी फूट तथा सैन्य शक्ति की कमी के कारण परास्त हो रहे थे, तो कई आधुनिक भारतीय भाषाएँ विकसित हो रही थीं। उदाहरणार्थ, गुजराती 12वीं सदी में पुष्पित-पल्लवित हुई और मराठी भी 12वीं सदी के उत्तरार्द्ध में विकसित हुई तथा इसके प्रथम लेखक मुकुंदराज थे। आर.सी. मजूमदार ने भाषाओं के बारे में एक ग्रंथ संपादित किया था, जिसमें बंगला, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ आदि पर एक-एक अध्याय है। मगर हिंदी या हिंदुस्तानी पर एक भी अध्याय नहीं है। इस पर डॉ. रामविलास शर्मा चिंता एवं आश्चर्य व्यक्त करते हैं। मगर उस ग्रंथ में गुजराती के बारे में लिखने वाले एच.सी. भयाणी ने लिखा है कि उद्योतन ने ‘कुवलयमाला’ में मध्य प्रदेश टक्क सिंधु, मरु, मालव, गुर्जर और लाट प्रदेशों से आने वाले व्यापारियों की विभिन्न निकालते हैं कि पुरानी हिंदी, सिंधी, गुजराती आदि भाषाओं का अस्तित्व आठवीं सदी में था और ये भाषाएँ अपभ्रंश से भिन्न थीं। फिर वह डी.सी. गांगुली के हवाले से बताते हैं कि 1021-22 ई. में जब महमूद गजनवी ने चंदेल राजा विद्याधर (कालिंजर, बुंदेलखंड) के किले को घेर लिया, तो राजा ने 303 हाथी और धन देकर समझौता किया, मगर बिना महावतों के हाथी किले के बाहर भेज दिया। मगर महमूद गजनवी के कारिंदों ने हाथियों पर काबू पा लिया। इसलिए विद्याधर ने उसकी प्रशंसा में भारतीय भाषा में एक छंद लिख भेजा जिसे पढ़कर या पढ़वाकर महमूद गजनवी खुश हुआ। डॉ. शर्मा का मानना है कि उस राजा ने बुंदेलखंडी, ब्रजभाषा या हिंदी में ही वह छंद लिखा होगा। फिर महमूद गजनवी के दरबार में बहुत से हिंदी कवि थे और उन्होंने ही उस छंद को पढ़कर महमूद गजनवी को सुनाया होगा अथवा वह स्वयं हिंदी जानता रहा होगा क्योंकि व्यापार में एक संपर्क भाषा का उपयोग होता था मगर डी.सी. गांगुली ने भारतीय भाषा कहकर हिंदी की असलियत को छिपा दिया।
यद्यपि सुनीति कुमार चटर्जी ने गोरखनाथ के पदों को पुरानी बंगला में रचा हुआ माना है–‘गोरखधंधे’ नामक पोथी में, मगर डॉ. शर्मा उनसे असहमत होकर कहते हैं कि यद्यपि इसकी भाषा बंगला है मगर वह पुरानी हिंदी का भेष बनाये है। उन्होंने पीतांबरदत्त बड़थ्वाल के हवाले से सिद्ध किया है कि श्रुति परंपरा के कारण गोरखवानी को गोरखनाथ के शिष्यों ने श्रद्धा और विश्वास के कारण नष्ट होने से बचा लिया : और दूसरे, स्मृति के कारण पुरानी रचनाओं में परिवर्तन किये गये और नये पद शिष्यों द्वारा समय-समय पर जोड़ दिये गये। इसके अलावा डॉ. बड़थ्वाल को गोरखवानी की जितनी प्रतियाँ मिली थीं, वे सभी हिंदी प्रदेश के विभिन्न स्थानों यथा पौड़ी गढ़वाल, जोधपुर, पटियाला, जयपुर, हरदोई आदि से मिली थीं। और इन सभी में पाठ भेद भी हैं। मगर क्रियापद हिंदी के हैं–‘जोगी सो जो राखै जो/जिभ्या इंद्री न करै भोग/अंजन छोड़ि निरंजन रहै/ता को गोरख जोगी कहै।’ इतना ही नहीं, दामोदर पंडित के ‘उक्ति व्यक्ति प्रकरण’ का हवाला देकर डॉ. शर्मा कहते हैं कि गोरखबानी की भाषा पुरानी अवधी है और वह 12वीं सदी की रचना है। उनके शब्दों में ‘उक्ति व्यक्ति प्रकरण’ के क्रिया रूपों में गोरखबानी के क्रियापदों और चर्यापदों (बंगला) के क्रियापदों की तुलना की जाये तो निष्कर्ष यह निकलेगा कि ग्यारहवीं, बारहवीं सदियों में अवधी के क्रियारूप दूर-दूर तक फैले हुए थे। अपभ्रंश से अवधी का जन्म नहीं हुआ वरन् प्रचलित अवधी के क्रियारूप अपभ्रंश में स्वीकार किये गये।’ (भारतीय संस्कृति एवं हिंदी प्रदेश) इसमें प्रयुक्त बोली ‘कोशली’ असल में अवधी या ‘पूर्वीया हिंदी’ है। यह ग्रंथ अवधी जानने वालों को संस्कृत सिखाने के लिए लिखा गया था। यह ग्रंथ मलिक मुहम्मद जायसी के ‘पद्मावत’ और तुलसी के ‘रामचरितमानस’ से 400 वर्ष पूर्व लिखा गया था। चौदहवीं सदी में मुल्ला दाऊद ने अवधी में एक काव्य रचना की थी जिसका नाम था ‘चंदायन’। इसके अलावा यद्यपि मुसलमानों का पवित्र ग्रंथ ‘कुरान’ अरबी भाषा में लिखा गया है, मगर अरबी भाषा को भारत में उतनी लोकप्रियता नहीं मिली। जितनी फारसी को मिली और तमाम मुस्लिम विद्वानों ने फारसी में उत्तम रचनाएँ कीं। इस प्रकार मुसलमानों की धर्म भाषा (अरबी) तथा सांस्कृतिक भाषा (फारसी) अलग-अलग रही। महमूद गजनवी के साथ फारसी भाषा-साहित्य का प्रवेश भी भारत में हुआ था। इससे स्पष्ट है कि भारत में आने से पहले अफगानिस्तान में फारसी भाषा का प्रचलन था। कुछ मुस्लिम विद्वानों यथा अजीजुद्दीन खालिद किर्मानी ने दर्शन और ज्योतिष संबंधी ग्रंथों का अनुवाद फारसी में किया (‘दलाइले फीरुजशाही’)। इसी प्रकार कालांतर में दक्षिण भारत में बहमनी राज्य के शासक अहमद शाह प्रथम के आदेश से अब्दुल्ला बिन सफी ने अश्व चिकित्सा पर लिखे संस्कृत ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया। थानेश्वर के अब्दुल अजीज शम्स ने संगीत और नृत्य पर एक संस्कृत ग्रंथ का अनुवाद फारसी में किया। फिर 17वीं सदी के पूर्वार्ध में कश्मीर के अमीर हैदर मलिक ने कल्हण की ‘राजतरंगिणी’ के आधार पर कश्मीर का इतिहास लिखा। इतना ही नहीं, लोदी शासनकाल में शेख रिजकुल्ला फारसी में मुश्तकी नाम से तथा हिंदी में ‘राजन’ नाम से कविताएँ लिखते थे। 13वीं सदी के प्रथम दशक में सुल्तान कुतुबुद्दीन कवियों को इनाम देते थे, इसलिए उन्हें ‘लाखबख्श’ कहा जाता था। डॉ. शर्मा ने रेखांकित किया है कि ‘लाख’ शब्द न तुर्की भाषा का है और न फारसी का, बल्कि हिंदी का है। अस्तु हिंदी में रचनाएँ करने वाले कवि ही सुल्तान को लाखबख्श कहते थे। फिर हिंदी में पहली मसनवी तुगलकों के शासनकाल में लिखी गई थी जिसमें लोरिक और चंदा की प्रेम कथा है। जुम्मे की नमाज के समय वह कथा लोगों को सुनाई जाती थी और वे उसे समझ लेते थे। फिर भारत में पैदा हुए अमीर खुसरों मूलतः कवि थे जिन्होंने अवधी और फारसी में संयुक्त रूप से पद्य रचनाएँ कीं। इसके अलावा उन्होंने 1291 में जलालुद्दीन खिलजी के सैनिक अभियान का वृत्तांत लिखा, 1316 में गुजरात की देवल रानी और खिज्र खाँ की प्रेम कथा लिखी–उन्होंने भारत की स्त्रियों की सुंदरता का बखान किया। फिर 1318 में उन्होंने मुबारकशाह के सैनिक अभियानों का वृत्तांत लिखा और अंततः ‘तुगलकनामा’ लिखा। अमीर खुसरो का घनिष्ठ संबंध निजामुद्दीन औलिया से था और दोनों की मजारें पास-पास (दिल्ली में) हैं। इसके अलावा राजसत्ता से प्रभावित हुए बिना 1350 ई. के करीब इसामी ने गजनी के यामिनी वंश से लेकर मुहम्मद बिन तुगलक तक का इतिहास महाकाव्य के रूप में लिखा। कश्मीर के शासक जैनुल आबिदीन के शासन (1420-1470) के दौरान जोनराज ने ‘द्वितीय राजतरंगिणी’ लिखी और उनके शिष्य श्रीवर ने ‘तृतीय राजतरंगिणी’ लिखी जिसमें 1459 से 1486 तक की घटनाओं का विवरण है। ‘राजावली पताका’ में प्राज्यभट ने कश्मीर पर अकबर का अधिकार हो जाने तक का वृत्तांत लिखा। इस प्रसंग में ए.के. मजूमदार का यह कहना सही प्रतीत होता है कि सिकंदर के शासन से पहले कश्मीर के मुसलमान बादशाह और मुसलमान जनता बहुत कट्टर नहीं थे और उनकी रानियों के नाम लक्ष्मी और शोभा जैसे होते थे तथा उन्होंने सोने का शिवलिंग स्थापित किया था। इतना ही नहीं, कश्मीर के शासक कुतुबुद्दीन ने हिंदू प्रजा के विश्वास का ख्याल करके अकाल से बचने के लिए यज्ञ करवाया था। जैनुल आबिदीन के शासन (1420-1470) के दौरान कश्मीर समृद्ध हुआ। उसकी आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में प्रगतिशील नीतियों के कारण। उल्लेखनीय है कि वह अकबर से लगभग एक शताब्दी पहले उदार एवं प्रगतिशील शासन व्यवस्था कायम किये थे। डॉ. शर्मा ने ठीक ही कहा है कि इंग्लैंड के इतिहास की अपेक्षा भारत का इतिहास उस काल में ज्यादा यथार्थपरक था तथा यद्यपि भारत में धर्म के नाम पर कई अत्याचार हुए थे मगर प्रोटेस्टेंट और रोमन कैथोलिक के बीच हुए रक्तपात-सा (जिंदा जलाने) यहाँ घटित नहीं हुआ। भारत में सूफियों-संतों का और वेदांत मतावलंबियों का उदारवादी एवं समतावादी आंदोलन मौजूद था। इसके अलावा गुरुग्रंथ साहिब में कबीर के पद, सूफियों के पद और हिंदी के अन्य प्रचलित पद मौजूद हैं। इतना ही नहीं, हरमंदिर साहब की नींव लाहौर के सूफी संत हजरत मियाँ मीर ने रखी थी। ऐसी सामाजिक सहिष्णुता की मिसाल इंग्लैंड में नहीं मिलती जहाँ किसी प्रोटेस्टेंट चर्च की बुनियाद किसी रोमन कैथोलिक पादरी ने रखी हो। मगर डॉ. शर्मा ने यह उल्लेख नहीं किया है कि बीसवीं सदी के अंतिम दो दशकों में खालिस्तान आंदोलन के दौरान गुरुग्रंथ साहिब से तमाम हिंदी शब्दों को निकालने की घृणित घटनाएँ घटीं और हिंदी की मुखालफत उग्रपंथियों द्वारा विश्वविद्यालयों के विभागों से लेकर आकाशवाणी/दूरदर्शन के कार्यालयों तक में हुई। उदाहरणार्थ, उस दौरान ‘पवित्तर’ शब्द को निकालकर ‘मुकद्दस’ शब्द गुरुग्रंथ साहिब में घुसाये गये।
डॉ. शर्मा ने एक ऐतिहासिक तथ्य रेखांकित किया है कि मुसलमान होने के पूर्व तुर्क और मंगोल लूटपाट करते थे और मुसलमान होने के बाद भी ऐसा करते रहे। ठीक उसी प्रकार ईरान के लोग मुसलमान होने से पहले नौरोज का त्योहार मनाते थे और मुसलमान होने के बाद भी मानते रहे। वह यह भी स्थापित करते हैं कि यद्यपि सामंतवाद, पूँजीवाद से पिछड़ा होता है मगर इसी दौरान साहित्य में लोकभाषाएँ प्रतिष्ठित होती हैं। उनके अनुसार तमिल, कन्नड, तेलुगु, हिंदी–प्रायः हर भाषा में चारण काव्य परंपरा पहले आती हैं, भक्ति साहित्य उसके बाद आता है। विद्यापति ने ‘कीर्तिलता’ में मैथिली और अवहट्टा (अपभ्रंश) दोनों भाषाओं में रचना की है। ‘पृथ्वीराज रासो’ (चंद वरदाई) के बारे में डॉ. शर्मा का मानना है कि उसकी आधारभूत भाषा ब्रज भाषा है मगर अवधी के बहुत से क्रियारूपों का व्यवहार ब्रज भाषा में होता था : ‘लोकभाषाओं को देशी भाषा कहा जाता था, इसलिए कि वे प्राकृत और अपभ्रंश से भिन्न थी खैर…वह यह भी मानते हैं कि राजदरबारों से कई प्रवृत्तियाँ जुड़ी थीं–चारण काव्य परंपरा, रीतिवादी धारा, पुरातन महाकाव्यों का रूपांतर, भक्ति साहित्य की रचना, साहित्य में लोकभाषा की प्रतिष्ठा। किंतु सभी प्रतिभावान कवियों को न तो राज्याश्रय मिला और न वे उसे पाना चाहते थे। जैसा कि कुंभन दास ने कहा था–‘संतन को कहाँ सीकरी सो काम/आवत जात पनहिया टूटी, बिसरि गयो हरिनाम।’ इस कथन को डॉ. शर्मा ने अपनी जिंदगी में सही मायाने में चरितार्थ किया क्योंकि उन्हें हिंदी भाषा एवं साहित्य में श्रीवृद्धि के लिए कई बड़े-बड़े पुरस्कार मिले परंतु उन्होंने हर बार पुरस्कार राशि लौटा दी और सिर्फ प्रतीकात्मक सम्मान ग्रहण किया। यह हिंदी साहित्यकारों के लिए अनुकरणीय उदाहरण है।
प्रसिद्ध भाषाविद् डॉ. सुनीति कुमार चटर्जी 14वीं-15वीं सदी को मध्यकाल मानते हैं किंतु उस समय के साहित्य को ‘नया भारतीय साहित्य’ कहते हैं, क्योंकि यह लोकभाषाओं में लिखा जा रहा था, जिसका संबंध प्रांत अथवा भाषायी क्षेत्र से था। मगर डॉ. शर्मा इसे मध्यकाल नहीं मानते क्योंकि बड़े-बड़े अंतर-जनपदीय बाजारों का निर्माण हो रहा था तथा साहित्य की नई विषय-वस्तु अंतर-प्रांतीय या अखिल भारतीय बन जाती थी। इसलिए वह इसे आधुनिक चेतना की शुरुआत मानते हैं। वह एस.के. सरस्वती एवं आर्थर पोप को उद्धृत करते हुए मानते हैं कि खिजली, तुगलक और जौनपुर के शर्की शासकों के समय हिंदू कारीगरों ने भव्य इमारतें बनायी थीं जो मुस्लिम देशों के भवनों से भिन्न थीं। अस्तु, ईरानी स्थापत्य की बहुत-सी विशिष्टताओं का जन्म भारत में हुआ था मगर उनका परिष्कार और विकास ईरान में हुआ। वह यह भी मानते हैं कि सन् 1800 ई. के पूर्व इंग्लैंड, जर्मनी और इटली में ढेर सारा साहित्य लैटिन में लिखा गया था जिसे वहाँ का जातीय साहित्य मानना चाहिए और उसी प्रकार दिल्ली के कुछ इतिहासकारों ने जो कुछ फारसी में लिखा, उसे हिंदुस्तानी संस्कृति का अंग मानना चाहिए। आर.सी. मजूमदार के अनुसार मुसलमानों के सामाजिक विचार अतिलोकतांत्रिक हैं और उनसे समता एवं बंधुत्व का सबक सीखा जा सकता है जबकि हिंदू समाज में जाति प्रथा तथा अस्पृश्यता की विषमता एवं कट्टरता जारी रखी। मगर डॉ. शर्मा इससे असहमत हैं क्योंकि जहाँ भी सामंती व्यवस्था का चलन हुआ, भूमि का केंद्रीकरण हुआ, वहाँ ऊँच-नीच का भेदभाव पैदा हुआ। भारत में सामंवाद के दीर्घजीवी होने के कारण यहाँ भेदभाव अधिक था। मगर जाति प्रथा की कट्टरता का विरोध भी सामूहिक रूप से 14वीं-15वीं सदियों में हो रहा था। मगर मजूमदार इस तथ्य को नजरअंदाज कर देते हैं। वह आर.सी. मजूमदार को सांप्रदायिक इतिहासकारों में शुमार करते हैं जो हिंदुओं और मुसलमानों को शत्रु के रूप में चित्रित करते हैं तथा अँग्रेजों को दोनों का हितैषी ठहराते हैं। डॉ. शर्मा इस प्रवृत्ति की आलोचना करते हुए कहते हैं कि भारतीय साहित्य की उपलब्धियाँ अँग्रेजों के संरक्षण के कारण नहीं, बल्कि उनसे संघर्ष के कारण हैं। उनके अनुसार भारत के मुसलमान शासक भारतीय थे और देश का पैसा देश ही में खर्च करते थे जबकि अँग्रेज यहाँ का पैसा और कच्चा माल ब्रिटेन ले जाते थे। दूसरे, मुसलमानों ने कभी इस देश को विभाजित करने की कोशिश नहीं की बल्कि यह कोशिश अँग्रेजों के शासनकाल में की गई तथा मुस्लिम संप्रदायवाद को अँग्रेजों ने बढ़ावा दिया।
यह बहुत बेबाक तरीके से कहते हैं कि भक्ति साहित्य एक ओर बौद्ध और जैन मतों के संसार-त्याग का निषेध था और दूसरी ओर चारण काव्य की रीतिवादी सीमाओं का निषेध। इसलिए इसका सामाजिक आधार ज्यादा विस्तृत था। इसमें विभिन्न निम्न जातियों की सक्रिय भागीदारी थी और स्त्रियाँ भी भक्त कवयित्री के रूप में प्रतिष्ठित थीं–विशेषकर तमिलनाडु में आण्डाल, कर्नाटक में अक्कमहादेवी (वचन), कश्मीर में ललद्यद (वाख) और हिंदीप्रदेश (राजस्थान) में मीराबाई। यद्यपि मीराबाई के पद पश्चिमी राजस्थानी में थे मगर कालांतर में गायकों ने मूल पद की भाषा का आधुनिकीकरण कर दिया। ये पद चारों धाम की यात्रा करने वालों के साथ दूर-दूर तक घूमे थे। भगवानदास तिवारी के अनुसार मीरा की प्रामाणिक पदावली के पहले पद की पहली पंक्ति है : ‘म्हांरां री गिरधर गोपाड दूसरा णा कुया।’ मगर ब्रजभाषा में उसका शाब्दिक अनुवाद इस प्रकार प्रचिलत है : ‘मेरो तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई।’ वास्तव में, ब्रजभाषा और राजस्थानी काफी निकट है तथा मीरा की भाषा ब्रजभाषा मिश्रित राजस्थानी है। ये कवयित्रियाँ अंधविश्वासों, कर्मकांडों और बाह्य आडंबरों का निरंतर विरोध करती रहीं। समूचा भक्ति आंदोलन सामंतवाद का विरोधी रहा। गोरख जैसे योगियों ने भी मंदिर-मस्जिद की संकीर्णता की आलोचना की–‘हिंदू ध्यावै देहुरा, मुसलमान मसीत/जोगी ध्यावै परमपद, जहाँ देउरा न मसीत।’
इसी प्रकार रामानंद ने कहा–‘लुंचित (जिनके बाल नुचे हों, जैन साधु), मुंचित (जिन्होंने घर-बार छोड़ दिया हो), नागा (जो वस्त्र नहीं पहनते), मौनी आदि सब बाहरी साधना में लगे हुए साधु व्यर्थ अपना जीवन खोते हैं। इसी प्रकार एकादशी और रोजा रखना, तीर्थाटन, वेद और कुरान पढ़ना, सब निष्फल होते हैं, क्योंकि पढ़ने गुनने मात्र में कुछ नहीं धरा है। सार मात्र है, हृदय का शुद्ध होना।’ विभिन्न उदाहरणों (मीरा, कबीर, तुलसी, विद्यापति, गोरख) के माध्यम से डॉ. शर्मा इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि भूतकालिक और भविष्यकालिक क्रियारूप विभिन्न हिंदी राज्यों में विकसित हो रहे थे, क्योंकि अंतर-जनपदीय व्यापार में अंतर जनपदीय भाषा या मानक (खड़ी बोली) रूपों का होना आवश्यक था। लोकभाषाएँ अपने क्षेत्र से बाहर तक प्रचलित हो रही थीं जैसे तुलसीदास ने मूलतः अवधी में काव्य-रचना की मगर ब्रजभाषा में भी की। डॉ. शर्मा के शब्दों में ‘हिंदी प्रदेश में जातीयता का विकास और अखिल भारतीय स्तर पर राष्ट्रीयता का विकास ये दोनों चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं और दोनों का ही माध्यम हिंदी है।’ (भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश)। उन्होंने प्रभाकर माचवे के हवाले से कहा है कि ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, रामदास आदि मराठी भक्त कवियों की मराठी रचनाओं के साथ कुछ फुटकर रचनाएँ हिंदी में भी मिली हैं। जैसे ज्ञानेश्वर ने 1290 ई. में लिखा–‘दुनिया त्यजकर खाक लगाई, जाकर बैठा बन मो।’ इसी प्रकार नामदेव ने लिखा (जो भूतकालिक क्रिया रूप में खड़ी बोली के प्रसार का सूचक है)–‘पांडे तुमरी गाइत्री लोधे का खेत खाती थी/लैकरि ठेका टगरी तोरी लागत लागत जाती थी।’ निःसंदेश चौहदवीं सदी में उत्तर भारत से कुछ लोग आंध्र प्रदेश में बस गये और उनके साथ हिंदी की जनपदीय भाषाएँ भी गईं तथा उन्होंने ‘दक्खिनी हिंदी’ का विकास किया। वहाँ से वह केरल और कर्नाटक गई। 17वीं और 18वीं सदियों में केरल में हिंदी को महत्त्वपूर्ण स्थान मिला था–राजकीय पत्र-व्यवहार में हिंदुस्तानी का प्रयोग होता था। उत्तर-दक्षिण के बीच व्यापार का प्रमुख माध्यम हिंदी था। केरल में हिंदी को पहले ‘गोसायि भाषा’ के रूप में जाना जाता था जो उत्तरी भारत के संतों तथा तीर्थयात्रियों द्वारा हिंदी की बोलियों के लिए व्यवहृत शब्द था।
डॉ. शर्मा ने एक ओर अकबर, शाहजहाँ और जहाँगीर को उदार पाया है हिंदुओं के प्रति, वहीं दूसरी ओर औरंगजेब क्रूर था जिसने 1680 में चित्तौड़ में 63 मंदिरों को ध्वस्त कर दिया। यों युद्ध के दौरान अकबर कभी-कभी अपने पूर्वज तुर्कों की तरह क्रूरता का परिचय देता था मगर उसका उद्देश्य मूर्तियों को तोड़ना, मंदिरों को ध्वस्त करना और इस्लाम का प्रचार करना नहीं था बल्कि वह एक व्यवस्थित साम्राज्य का निर्माता था जिसमें काफी रक्तपात हुआ मगर बाद में उद्योग, व्यापार एवं संस्कृति की उन्नति हुई। 1578 ई. में अकबर, पंजाब में झेलम के किनारे शिकार करने गया था मगर एक पेड़ के नीचे उसे विचित्र अनुभव हुआ। सो उसने आदेश निकाला कि किसी पशु-पक्षी को नहीं मारा जाए। फिर उसने फकीरों और गरीबों में काफी धन बाँट दिया। वह विभिन्न धर्मों के पुजारियों से मिलकर संवाद कायम करना चाहता था। उसने गैर मुसलमानों पर लगे जजिया कर को खत्म कर दिया था, पक्षियों को पिंजरे से मुक्त कर दिया था, शिकार खेलना बंद कर दिया था और निर्धारित दिनों को पशुवध रोक दिया (सालभर में आधे वर्ष)। उसके द्वारा चलाये गये ‘दीन इलाही’ धर्म में एकेश्वरवाद था। इसमें सर्वात्मवाद (ईश्वर से सीधा संबंध) का भी थोड़ा रंग था। उसने आदेश निकाला था कि जिन्हें जबरदस्ती मुसलमान बना दिया हो, वह अपने पुराने धर्म में वापिस जा सकता है। उनके दरबार में संगीतकार तानसेन की बंदिशें हिंदी में थीं। अकबर ने अपनी बंदूक का नाम ‘संग्राम’ रखा था, अपने बेटे मुराद का नाम ‘पहाड़ी’ रखा था। शाहजहाँ के पास दो हाथी थे–‘सुधाकर’ तथा ‘सूरजसुंदर’। दाराशिकोह जितना उदार और सहिष्णु था, उसका भाई औरंगजेब उतना ही क्रूर था तथा राजसत्ता हड़पने के लिए उसने दारा की हत्या करा दी। बंदी बनाये गये गर्मी से प्यासे शाहजहाँ ने औरंगेजब को एक पत्र लिखा था–‘हिंदुओं की तारीफ करनी चाहिए जो अपने मरे हुए संबंधियों को भी पानी देते हैं और तू मेरा बेटा अद्भुत मुसलमान है कि मुझे जीते हुए को पानी के लिए तरसा रहा है।’ इस प्रकार औरंगजेब के शासनकाल में अव्यवस्था का आलम था। यह भी ज्ञातव्य है कि मुस्लिम लोगों में एकरूपता नहीं थी। वे शिया और सुन्नी जैसे दो ध्रुवों में बँटे थे। मगर हिंदुओं में भी स्तरीकरण था (और अभी है)। इसलिए इतिहासकार जदुनाथ सरकार का यह कथन सही है कि भारत एक शांत एवं सुरक्षित राष्ट्र बनने के लिए हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों को मरना होगा और फिर जन्म लेना होगा, कठोर तपस्या और पश्चाताप करके, विवेक और विज्ञान के प्रभाव से स्वयं को शुद्ध करना होगा और नया जीवन प्राप्त करना होगा। मुस्तफा कमाल पाशा ने तुर्की में दिखा दिया है एक मुस्लिम देश धर्म-निरपेक्ष बन सकता है, अनेक पत्नियों से विवाह और गुलामों जैसा स्त्रियों का अलगाव खत्म कर सकता है, सभी धर्मों को राजनीतिक समानता प्रदान कर सकता है और मुस्लिम देश बना रह सकता है। मगर अफसोस है कि अभी तक तमाम मुस्लिम देश न तो लोकतांत्रिक हो सके हैं और न धर्म-निरपेक्ष। इसलिए मध्य-पूर्व अरब में पिछले कुछ वर्षों से तानाशाही के विरुद्ध संघर्ष चल रहे हैं और कई मुस्लिम देशों में (पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक) में तालिबानी कट्टरता महिलाओं की आजादी तथा दूसरे धर्मों की स्वायत्तता स्वीकार नहीं कर रही है।
डॉ. शर्मा ने रेखांकित किया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुँचाने के लिए पुर्तगाली, ब्रिटिश और डच कंपनियाँ समुद्री डकैती को हथियार के रूप में इस्तेमाल करती थीं। सन् 1652 में अँग्रेजों ने और 1665 में हालैंड के व्यापारियों ने सूरत से भी भीतरी नगरों तक, हुगली से आगरा तथा दिल्ली तक, माल ले जाने पर चुंगी माफ करा ली। (जबकि यह अधिकार भारतीय व्यापारियों को प्राप्त नहीं था।) यह कैसी विडंबना थी कि भारत से बाहर जाने वाले जहाजों को विदेशियों से आज्ञापत्र लेना जरूरी होता था। दूसरी ओर खेती की जमीन का पक्का बंदोबस्त लॉर्ड कार्नवालिस ने कर दिया जिससे जमींदारों ने किसानों से ज्यादा लगान एवं नाना प्रकार के नजराने वसूलने लगे। जब 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर अधिकार जमा लिया, तो (रणजीत गुहा के अनुसार) उस समय उपनिवेशवाद की तीन विशेषताएँ थीं : पहली, उपनिवेशवाद का उदय बल प्रयोग से हुआ; दूसरी, उसने जमीन की मूल उपज को औपनिवेशिक अर्थतंत्र का मूलाधार बनाया; तीसरी, उसने बल प्रयोग और शोषण को कानूनी जामा पहनाया। जाहिर है बाजार में खुली स्पर्धा से इंग्लैंड के व्यापारियों ने भारतीय व्यापारियों का मुकाबला नहीं किया। डॉ. शर्मा रणजीत गुहा से दो बातों पर अहसमत हैं : गुहा का पहला मानना है कि अँग्रेज शासक भारत की देशी भाषाओं को सीखकर जनता से सीधा संपर्क करना चाहते थे, इसलिए 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। डॉ. शर्मा का मानना है कि अँग्रेज देशी भाषाओं को बढ़ाना नहीं चाहते थे बल्कि उन्हें ‘गँवारू बोली’ (वर्नाकुलर) कहकर अपमानित करते थे। वास्तव में, अँग्रेज व्यापार और राजस्व बढ़ाने के लिए देशी भाषाएँ सीखते थे और 19वीं सदी के अंत में विलियम जोन्स ने संस्कृति कविताओं का अँग्रेजी में अनुवाद किया था और भारतीय संस्कृति के बारे में भी लिखा था। डॉ. शर्मा ने सबाल्टर्न इतिहासकारों की आलोचना की है क्योंकि वे राष्ट्र को ‘कल्पित समुदाय’ (एंडरसन की राह पर चलकर) मानते हैं, वे अँग्रेजी शासन को नवजागरण का श्रेय देते हुए भक्ति आंदोलन को नहीं देखते और पूँजीवादी राष्ट्रवाद की आलोचना करते-करते समस्त राष्ट्रवाद को भी खारिज करते हैं तथा धार्मिक मतवाद के विरोध, सामंती रूढ़ियों का विरोध तथा समाज को पुनर्गठित करने की धारणाएँ शामिल हैं।’ (भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश) सबाल्टर्न इतिहासकार यह भी गलती करते हैं कि समुदाय के लोग अपने धर्म-बिरादरी से आगे के बारे में नहीं सोचते–भाषायी और जातीय समुदाय के बारे में वे नहीं जानते। मगर यह सही नहीं है क्योंकि गाँव के लोगों ने देश के बारे में सोचकर आजादी की लड़ाई लड़ी, भाषायी अस्मिता के बारे में सोचकर शिक्षा का माध्यम हिंदी बनाने की (या अन्य क्षेत्रीय भाषा) माँग की, भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन 1950 के दशक में किया गया। इतना ही नहीं, धार्मिक संकीर्णता से हटकर सामंजस्य बनाने की बात गाँव के किसान करते रहे हैं। डॉ. शर्मा ने छपरा (बिहार) के ब्राह्मणों की राय भूदेव मुखोपाध्याय के हवाले से उद्धृत की है : ‘महाशय! मुसलमान होने से क्या होता है। मौलवी साहब का मन और आचार ऐसा पवित्र है कि हम ब्राह्मण लोग भी यदि उनका जूठा खा लें तो ऐसा सोच नहीं सकते कि हम अपवित्र हो गये।’ (सखाराम गणेश देउस्कर, ‘देश की बात’) वहीं इसका भी उल्लेख है कि पुराणों को सुनने के लिए मुसलमान लोग भी इकट्ठा होते हैं, और हिंदू लोग भी मुसलमानों के त्योहार में शरीक होते हैं। देउस्कर ने बंग-भंग की आलोचना करते हुए लिखा है : ‘बंगाली जाति की एकता कर्तारों की आँखों में गड़ रही थी…बंगालियों को अलग-अलग कर उनकी शक्ति घटा देना ही कर्तारों को अभीष्ट है।’ प्रसिद्ध इतिहासकार विपिनचंद्र ने अपनी पुस्तक ‘भारत का स्वतंत्रता संघर्ष’ में लिखा है कि भारतीय राष्ट्रीय चेतना का केंद्र था बंगाल और उसी को तोड़ने के लिए बंगाल-विभाजन 16 अक्टूबर, 1905 को किया गया। पूरे बंगाल में इसे शोक दिवस के रूप में मनाया गया, लोगों ने उपवास रखा और कलकत्ता में हड़ताल की गई। जनता ने जुलूस निकाला और जत्थों में गंगा-स्नान किया और वंदे मातरम् गाते हुए प्रदर्शन किया। स्वदेशी आंदोलन बंग-भंग विरोध में जुड़ गया था।
भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सभी भारतीयों को एकता के लिए आह्वान किया–‘परदेशी वस्तु और परदेशी भाषा का भरोसा मत करो। अपने देश में अपनी भाषा में उन्नति करो।’ कालांतर में हिंदी आंदोलन स्वदेशी आंदोलन से जुड़ गया। भारतेंदु ने ‘जातीय संगीत’ नामक लेख में ग्राम गीतों का महत्त्व रेखांकित किया, जातीय संगीत की छोटी-छोटी पुस्तकें छपे और सारे देश में, गाँव-गाँव में, प्रचलित की जाएँ। वह पुराने संस्कारों को बदलने के लिए इन गीतों को माध्यम बनाना चाहते थे। उनके अनुसार हिंदी का मुख्य विरोध अँग्रेजी से है और गौण विरोध उर्दू से क्योंकि हिंदी और उर्दू बुनियादी तौर पर एक ही भाषा है मगर फारसी और अरबी से लदी उर्दू का ही विरोध वह करते थे और चाहते थे कि बोलचाल की भाषा में देवनागरी लिपि में गद्य लिखा जाये। वह यह भी कहते थे कि अगरवाल मुख्यतः पश्चिमोत्तर प्रांत से थे जिनकी भाषा ‘खड़ी बोली अर्थात् उर्दू’ भी। उन्होंने यह भी लिखा है कि पूर्वी जनपदों यथा मिर्जापुर और बनारस में लोग ‘पुरबिया’ और ‘पद्दाही’ का भेद भूल गये हैं। इससे स्पष्ट है कि हिंदी भाषा का प्रसार चारों ओर बिना किसी संकीर्णता से हो रहा था। हिंदी क्रिया के बिना उर्दू का कोई वाक्य नहीं बनता। मगर कचहरी में प्रयुक्त उर्दू कठिन होती है, क्योंकि उसमें अरबी-फारसी के भारी-भरकम शब्द शामिल होते हैं और नोटिस या सम्मन पढ़ने के लिए उर्दू के जानकार लोग नियुक्त होते हैं। डॉ. शर्मा ने विस्तार से लिखा है कि किस तरह भाषा के सवाल पर अँग्रेजी शासन फूट डाल रहा था–1800 के बाद ब्रिटिश शासन ने शिक्षा विभाग का गठन करके हिंदी और उर्दू को दो भाषाएँ मानकर शिक्षण संस्थाओं में पाठ्य-पुस्तकें लगवाईं तथा अदालतों में अरबी-फारसी मिश्रित भाषा को प्राथमिकता दी। बालमुकुंद गुप्त ने दोनों में अनबन और मेलमिलाप के बारे में लिखा था–‘ऊपर से देखिये तो उर्दू और हिंदी में इस समय बड़ी अनबन है…पर वास्तव में उर्दू-हिंदी का बड़ा मेल है। यहाँ तक कि दोनों एक ही वस्तु कहलाने के योग्य हैं। केवल फारसीजामा पहनने से एक उर्दू कहलाती है और देवनागरी वस्त्र धारणा करने से दूसरी हिंदी।’
डॉ. रामविलास शर्मा ने निराला के साहित्य में जातीय चेतना का जिक्र किया है कि उनका बचपन बंगाल प्रांत में बीतने के कारण बंगाली प्रांतीयता के जहर ने उनमें जातीय चेतना जगाई। 1934 में निराला ने ‘सुधा’ नामक पत्रिका में ‘बगलियों की प्रांतीयता’ नामक टिप्पणी यों लिखी कि बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब आदि में प्रांतीयता का भाव है मगर संयुक्त प्रांत में नहीं है : ‘प्रांत प्रेम बुरा नहीं है, प्रांतीय तथा मातृभाषा पर गर्व होना भी स्वाभाविक है, पर प्रांत के नाम पर अन्य प्रांत वालों को पराया समझना और एक ही देश का होकर पहले प्रांत और देश तथा पहले प्रांतीय भाषा, फिर देशभाषा को सम्मान देना अनुचित है तथा निंदनीय बात है, और जो लोग ऐसा दुर्भाव पनपा रहे हैं वे अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ‘पहले बंगाल, फिर हिंदुस्तान की पुकार कुछ समय पूर्व बंगाल से बहुत सुनाई पड़ती थी पर धीरे-धीरे बंगालियों ने इसे अपनी गहरी हानि समझी।’ ज्ञातव्य है कि 1935 में हिंदी साहित्य सम्मेलन के इंदौर अधिवेशन में हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव आया जिसका निराला ने सहर्ष स्वागत किया। इस इच्छा की पूर्ति सन् 2000 में महात्मा गाँधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा के रूप में हुई। किंतु डॉ. शर्मा की मृत्यु (मई, 30, 2000) के बाद। निराला प्राथमिक से उच्च शिक्षा तक हिंदी माध्यम होने के समर्थक थे। वह साहित्य के अलावा यांत्रिकी, व्यावसायिक एवं कला की उच्च शिक्षा भी हिंदी माध्यम से चाहते थे। डॉ. शर्मा का मानना है कि जातीय प्रदेश की उन्नति के लिए कवि को जनपद जैसे सीमित क्षेत्र से शुरुआत करनी होगी मगर जनपदीयता जातीयता से, जातीयता राष्ट्रीयता से और राष्ट्रीयता मानवतावाद से अंततः जुड़ जानी है। भोजपुरी : ‘पहले जनपद, आंतरिक रूप से एकताबद्ध हों। फिर इन सब जनपदों को मिलाकर एक विशाल हिंदी भाषी राज्य बनाया जाये। इस राज्य की केंद्रीय सभा सामान्य नीति निर्धारित करेगी, प्रशासन की बुनियादी इकाइयाँ जनपद होंगे तब हिंदी प्रदेश का भरपूर सांस्कृतिक और आर्थिक विकास होगा…‘मगर आज की विकट स्थिति में ऐसा होना कठिन है।’
भारतीय संस्कृति का मूल सूत्र है : ‘एकं सद् विप्रा बहुधा वदंति।’ अर्थात् सत्य एक है जिसे विद्वान विभिन्न नाम देते हैं। वे मानते हैं कि बाल्मीकि और व्यास से लेकर रवींद्रनाथ ठाकुर, निराला और सुब्रह्मण्य भारती तक की कविताओं में अपने प्रदेश के अतिरिक्त सारे देश से प्रेम है। भारत में उपनिषदों ने समानता और बंधुत्व का संदेश रूस और फ्रांस की क्रांतियों से हजारों साल पहले दिया था। यहाँ दर्शन का विकास पहले और संघबद्ध धर्म उसके बाद आये। इसके परिणामस्वरूप यहाँ का प्रत्येक धर्म स्वयं को तर्क पर आधारित मानता है, इल्हाम पर आधारित नहीं। भारत में किसान मुख्यतः स्वाधीन थे, इसलिए यहाँ पश्चिमी देशों की तरह अर्द्धदास प्रथा का चलन नहीं था। डॉ. शर्मा जोर देकर कहते हैं कि ऋग्वेद और महाभारत की भाषा पहले लोकभाषा थी मगर कालांतर में वह संस्कृत बनी। संस्कृत नाटकों में शूद्रों और स्त्रियों को प्राकृत में बोलने का प्रावधान किया गया और अन्य पात्रों को संस्कृत में मगर बाद में योगियों, राज्याश्रित कवियों और भक्त कवियों के प्रयास से लोकभाषाएँ साहित्य का माध्यम बनीं। लोकभाषाओं के विकसित होने से राष्ट्रीय स्तर पर सांस्कृतिक एकता कायम हो सकी। वह अँग्रेजी के पटरानी बने रहने और हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं की दासियाँ बने रहने की मुखालफत करते थे मगर लिपि की बजाय भाषा को महत्त्व देते थे। उनके अनुसार 12वीं सदी से हिंदी जातीय भाषा बनी जिसमें हिंदू-मुसलमान दोनों रहे हैं और इसलिए राजसत्ता ने हमेशा उनकी एकता तथा प्रतिरोधी शक्ति को कमजोर करने की कोशिश की। उनकी स्पष्ट स्थापना थी–‘यदि प्राकृत अपभ्रंश के जाल से निकलकर जनपदीय भाषाओं की वास्तविकता पहचानी जाये तो आधुनिक भाषाओं के विकास का दूसरा मानचित्र आँखों के सामने आये।’ जाहिर है, वह लोकभाषाओं की ऐतिहासिक शक्ति पहचान गये थे और उन्हें भाषा-साहित्य की मुख्य धारा में ला रहे थे। दूसरी ओर वह विभिन्न भाषा परिवारों की गतिशीलता, परस्पर लेन-देन की प्रवृत्ति एवं उनकी सामाजिकता को बार-बार रेखांकित कर कबीले की बजाय कई कबीलों के (लंब अर्से तक) साझे तत्त्व होते हैं। उन्होंने भारोपीय भाषा जैसी आदि भाषा के अस्तित्व को खारिज किया तथा यूरोप की भाषा के निर्माण में भारतीय आर्य भाषाओं के अलावा आर्येतर भाषाओं की भूमिका को रेखांकित किया और पुराने औपनिवेशिक भाषा विज्ञान के सिद्धांतों को खारिज कर बताया कि अधिकांशतः पूरब (भारत) से पश्चिम की ओर भाषाओं का विकास हुआ। उन्होंने 1857 की क्रांति को हिंदी का पहला नवजागरण कहा, भारतेंदु युग को दूसरा, महावीर प्रसाद द्विवेदी युग को तीसरा तथा छायावाद युग एवं निराला साहित्य को चौथा नवजागरण माना। इस श्रेणीकरण पर वाद-विवाद हो सकता है (और कुछ हुए भी हैं) मगर इसमें उनकी वैचारिक संकीर्णता नहीं है, भले व्याख्या में अलग दृष्टि हो। किंतु डॉ. शर्मा आजीवन ‘दृष्टियों के जनतंत्र’ के समर्थक रहे जिसके कारण उनके कई वामपंथी मित्र उनसे असहमत भी रहे हैं। यह अकाट्य सत्य है कि वह आजीवन सामंतवाद, साम्राज्यवाद, पूँजीवाद एवं धार्मिक संकीर्णता का खुलकर विरोध करते रहे (भारतेंदु युग के साहित्य को ‘राष्ट्रीय’ कहा क्योंकि वहाँ अँग्रेजी साम्राज्यवाद की नीतियों का खंडन है) और भूमंडलीकरण को इलेक्ट्रॉनिक्स युग का पूँजीवाद माना है। उन्होंने भारतीय संस्कृति के विभिन्न आयामों, स्तरों एवं रूपों को समेकित रूप में देखा और हिंदी प्रदेश के योगदान को रेखांकित किया। इसलिए आवश्यकता है कि उनके द्वारा उठाये गये संस्कृति, भाषा, इतिहास आदि के मुद्दों पर आगे भी गंभीर शोध कार्य किये जायें।
