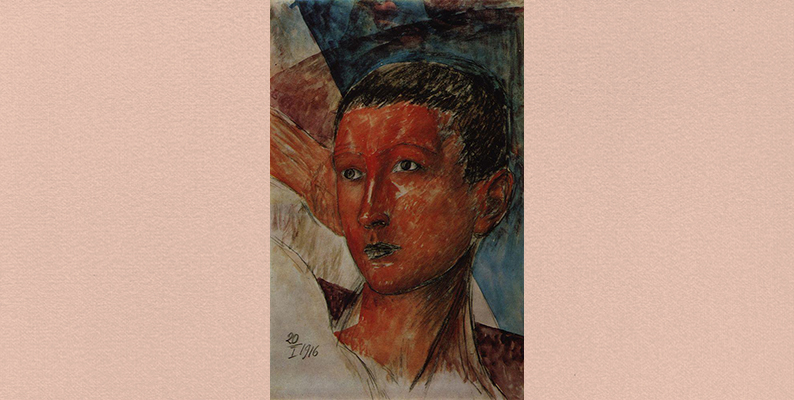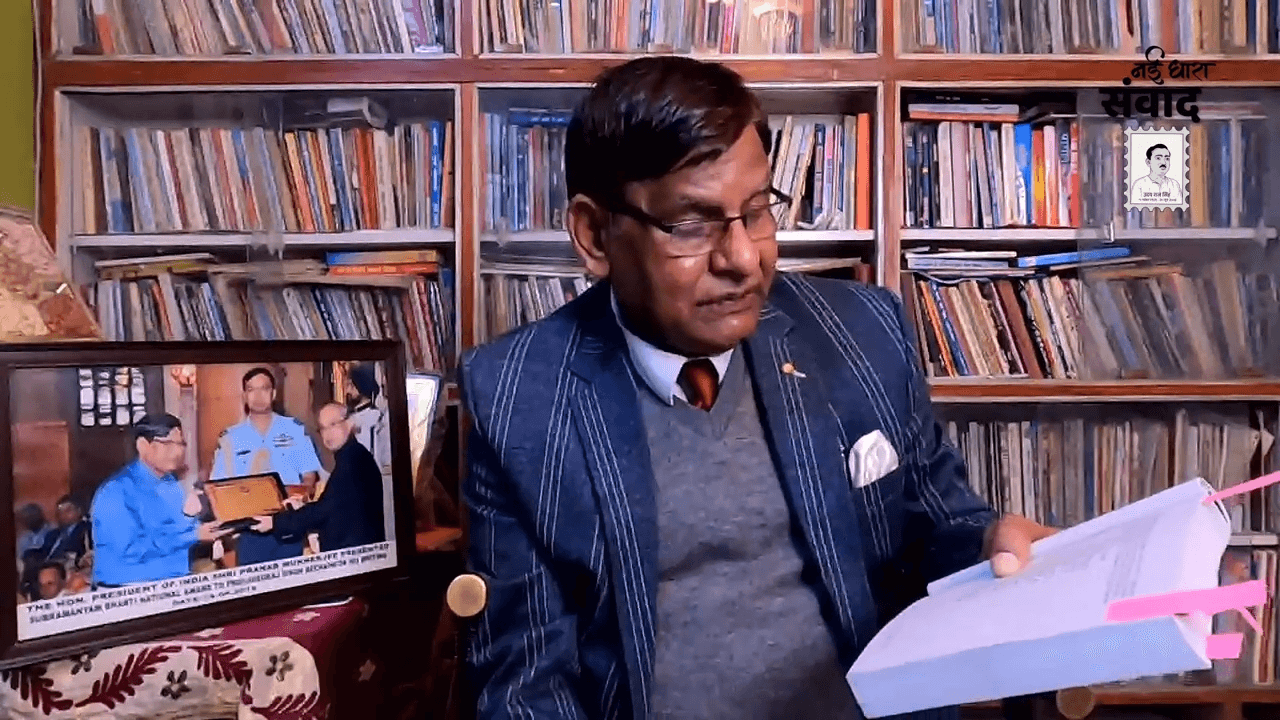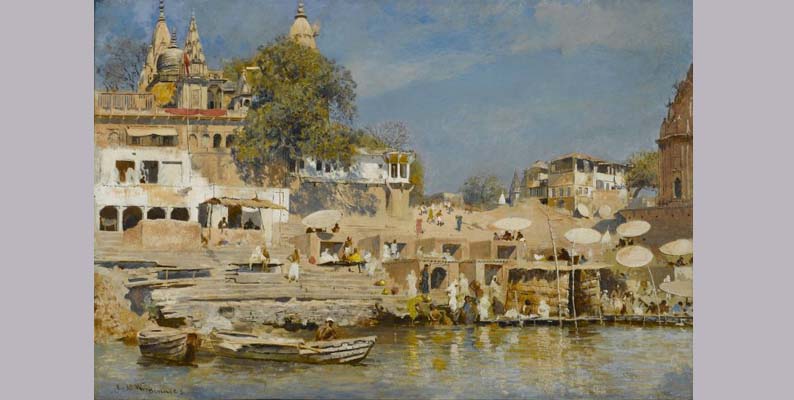कॉमरेड : जाति-भेद समस्या नहीं है…
- 1 August, 2024
शेयर करे close
शेयर करे close

शेयर करे close
- 1 August, 2024
कॉमरेड : जाति-भेद समस्या नहीं है…
भला हो उन हमारे परनाना का, जिन्होंने ‘बादी टोला’ यानी ‘बदबू टोला’ को अपना ‘चुन्नी’ नाम दिया। वे चन्दौसी ‘नगर पालिका’ में पहले साक्षर दलित प्रतिनिधि थे। बादी टोला का दरवाजा शहर से बाहर था। शहर में बदबू वाले लोग केवल ब्राह्मण, बनियों और कायस्थों की सेवार्थ प्रवेश किया करते थे। ‘बादी टोला’ दो हिस्सों को मिला कर बना था। एक हिस्से में वाल्मीकि रहते थे। दूसरे हिस्से में चमार। ये पड़ोस गाँव से पशुओं की खालें उतार कर लाते थे। उन्हें रंगते यानी बदबू दूर कर सार्वजनिक उपयोग के लायक बनाते थे। इसलिए इन्हें ‘रंगइया चमार’ भी कहा जाता था। परंतु कच्ची खालों की बदबू शहर के बनिये, ब्राह्मणों कायस्थों को बर्दाश्त नहीं होती थी।
कम्युनिस्ट आंदोलन के दौरान कुछ ऊँची जातियों के कॉमरेड कैडर निर्माण करने के उद्देश्य से इन ‘बहिष्कृत-बस्तियों’ की ओर उन्मुख हुए। इनमें मदन दीक्षित, कृष्ण दीक्षित, दूल्हा खाँ आदि प्रमुख थे। कालांतर में इन्हीं बस्तियों के अपने उन्हीं अनुभवों पर आधारित मदन दीक्षित ने ‘मोरी की ईंट’ और ‘बाहर दरवाजा’ दो उपन्यास लिखे। ‘मोरी की ईंट’ में उन्होंने ब्राह्मण पात्र से वाल्मीकि महिला के अवैध बच्चा पैदा कर सवर्ण क्रांतिकारिता का नमूना पेश किया।
‘चुन्नी’ दलित को बुरा लगता था कि लोग उनकी बस्ती को ‘बदबू-टोला’ कहते हैं। उन्होंने अँग्रेज अधिकारियों से यह नाम बदलने की गुहार लगाई। कोई नाम नहीं सूझा। ‘यह मेरा मोहल्ला है, मेरा नाम चुन्नी है, यही रख दीजिए और चल पड़ा।’ मोहल्ला खुर्जर गेट जहाँ ब्राह्मण, बनिया और कायस्थों के बीच मदन दीक्षित एडवोकेट का निवास था। शहर के बाहर का एरिया चुन्नी मोहल्ला और वाल्मीकि संजय बस्ती थी, जिसमें भंगी, चमार, धोबी, कुम्हार, मौर्य बस्तियाँ थीं। ये दोनों जुड़वाँ बच्चों की तरह एक-दूसरे से जुड़ी थीं। यहीं मैं मुन्नालाल मौर्य के साथ गुलाब देवी, जो उन दिनों काँग्रेसी कार्यकर्ता थीं, बाद में भाजपा में मंत्री बनीं, से मिला था। जब कॉ. दुबे की बेटी भावना दुबे ने एक मुस्लिम युवक से प्रेम विवाह किया तो गुलाब देवी ने उसकी पिटाई की थी। शायद ही कभी इन बस्तियों की बदहाली पर उनका ध्यान गया हो? एक दो अपवाद छोड़कर इनमें अधिसंख्य का जीवन स्तर बहुत ही निम्न था। चमारों के पास न रहने को पूरी जगह थी, न रोज़गार। न शिक्षा, न स्वास्थ्य। महिलाएँ रबड़ जलाकर खाना पकाती थीं। बच्चे स्कूल जाने की बजाय सुबह उठते ही ब्रश-डिब्बी थैले में डाल कर बूट पॉलिश करने निकल पड़ते थे। वाल्मीकि बच्चों के लिए वही झाड़ू लगाना तथा मल-मूत्र साफ करने का पुश्तैनी पेशा था। मैं इन्हीं अपने विपन्न भंगी-चमारों के बीच रह रहा था, जी रहा था। मेरी नानी, मौसी सब यहीं थीं। अँग्रेजी राज जाने और स्वराज आने का कोई सकारात्मक असर इन पर नहीं था। शिक्षा, व्यवसाय और सेवाओं पर काबिज हो केवल बनिये, ब्राह्मण और कायस्थ राज कर रहे थे। कॉमरेड शर्मा जातिविहीन समाज बनाने पर समाजवादी क्रांति घटित करने के प्रति अतिरिक्त आश्वस्त थे। सेंट्रल व स्टेट कमेटी तक के नेताओं को वे कहीं किसी होटल में नहीं, बल्कि अपनी बैठक में ठहराते थे। पंडिताइन खाँटी घरेलू महिला थीं। उनकी रसोई पर दबाव पड़ता था। वह उनके लिए खाना बनाती रहती थीं। रसोई में हाथ बँटाने का कल्चर तो कॉमरेडों में था नहीं। मुझे उनके घर की स्थिति का आभास हो जाता था। उनका मन ख़राब होना स्वाभाविक था। सो, वे चिड़चिड़ा जाती थीं।
एक बार हम ‘किसान सभा’ के प्रचार अभियान पर निकले थे। ‘नगली’ के नत्थू सिंह प्रधान हमारे साथ थे। वे दलित थे। कहा जाता है, उन्हें ग्राम-प्रधान बनाने में कॉमरेड दूल्हा ख़ाँ का विशेष योगदान था। नत्थू सिंह दूल्हा खाँ के न केवल संपर्क में थे, अपितु भूमि-संघर्ष के दौरान हिरावल दस्ता में थे। कॉमरेड शर्मा देर रात तक अध्ययन किया करते थे। बल्कि उन्होंने डिग्री कॉलेज में हिंदी के प्रवक्ता बनने के लिए प्रथम श्रेणी लाने का ऐलान कर, अध्ययन में रात-दिन एक कर दिए थे, परंतु पहली साल में मात्र उत्तीर्णांक आने से निराश होकर एम.ए. करने का इरादा छोड़ बैठे थे। उनके पास पार्टी साहित्य बड़ी मात्रा में जमा था, किंतु उन्हें अपने लिखे पर भरोसा नहीं था। एक पत्र भी लिखते तो सीधे मदन दीक्षित के घर जाते थे, उन्हें पढ़वाते, उनसे सुझाव लेते और तब ही कहीं भेज पाते थे। दीक्षित जी बड़े स्वाध्यायी और अनुभवी वकील थे। उनके छोटे भाई कृष्ण कुमार दीक्षित ‘अजय भवन’ दिल्ली से प्रकाशित होने वाले ‘मुक्ति संघर्ष’ के संपादक थे। कॉमरेड शर्मा से मेरा परिचय अनुभव की दृष्टि से सार्थक रहा। हम एक-दूसरे के काफ़ी सहयोगी रहे। कॉमरेड शर्मा मुझे तथाकथित क्रांतिकारी साहित्य पढ़वाते थे, अध्यापन के साथ-साथ किसानों-नौजवानों में काम कर रहे थे। मैंने उनके साथ दर्जनों गाँवों की पैदल यात्राएँ की थीं। वे वर्षों हमदर्द की तरह रहे। पर वे वर्ग संघर्ष स्वीकार करते थे और वर्ण-भेद को समाप्त करने के नाम से ऐसे बिदकते थे जैसे लाल वस्त्र देख कर साँड़ बिदकता है। उनका मानना था कि जाति-वर्ग के भेदभाव तो क्रांति अपने आप समाप्त कर देगी। हम कोई जाति भेद मानते ही नहीं। एक हद तक वे सही थे, अस्पृश्यता उनके यहाँ थी नहीं। भंगी, चमार किसी के भी घर खा सकते थे। अपनी थाली में खिला सकते थे। डॉ. अतीकुर्रहमान के बेटे को तो उन्होंने अपने बेटे की तरह घर पर रखकर पढ़ाया-पाला था। शुरू में उन्होंने काफी संघर्ष किया। ईमानदारी भी दिखाई। सपा में उनका राजनीतिक पतन हुआ। मंडल के बाद क्रांतिकारी आवाज के उतार में साथियों की मार्फत ऐसे आरोप मेरे कानों में आए जो मेरे लिए दुखद थे। सपा में जाकर वे अपने सिद्धांतों के खिलाफ घोर जातिवादी ब्राह्मण हो गए। बसपा पर सांप्रदायिक दल (भाजपा) से समझौते के विरोध के नाम पर वे सपा के यादवों द्वारा दलितों ख़ासकर जाटवों पर गाँव-गाँव हमले शुरू हुए तो भगवान दास दबंग अजगर के अगुआ बन गए, बल्कि सपा के जिलाध्यक्ष बन खुद सशस्त्र सुरक्षा गार्डों के साथ चलने लगे, जबकि उत्तर प्रदेश की बहुजन राजनीति के सर्वाधिक लाभार्थी ब्राह्मण होते थे। सरकार सपा की होती या बसपा की वे मलाईदार मंत्रालय कब्जा लेते थे।
उनके साथ का वह समय साक्षी है, उस वक्त के कॉमरेड शर्मा एक आदर्श चरित्र थे। दूल्हा खाँ के साये में रहते उन्हें सम्मान मिला और उनका दलित विरोधी ब्राह्मणत्व भी नियंत्रित रहा। ‘खाँ’ नहीं रहे तो कॉमरेड शर्मा भी ब्राह्मणवादी चरित्र में लौट आए। ‘मुशर्रफ अली’ ने बताया था–‘भगवान दास ने बेटी की शादी के निमंत्रण कार्ड पर सपा के राज्यस्तरीय ब्राह्मण-नेताओं के नाम आयोजक रूप में छपवा कर धन उगाही की थी।
शहरिया की पदयात्रा : कॉपरेटिव में किसानों के खिलाफ हुई धाँधलियों के विरुद्ध हम गाँव-गाँव पद यात्रा करते हुए शहरिया गाँव पहुँचे थे। वहाँ कथित उच्च जातियों के किसानों के यहाँ दावत का आयोजन हो रहा था। कॉमरेड शर्मा का भाषण सुन कर किसानों ने कहा था, बिलारी तहसील पर होने वाली सभा के लिए हम अपने गाँव से दो-दो ट्रैक्टर लेकर आएँगे और चंदा कर आपकी पूरी मदद करेंगे। दावत चल रही थी। सो, उन्होंने हमें भी खाना खाने के लिए पंगत में बैठाया। थालियों में खाना परोसा गया। मैं, कॉ. शर्मा और नत्थू सिंह प्रधान; तीनों एक पंक्ति में बैठे गर्म-गर्म पूड़ियाँ, आलू काशीफल, दही बूरा बड़े चाव से खा रहे थे। उसी वक्त एक यादव और जाट किसान ने नत्थू सिंह को पहचाना, ‘अरे! यह प्रधान तो नगलिया का चमार है। यह हमारी चौपाल में बैठ कर खाना खाएगा?… और ये दोनों भी छोटी जाति के ही होंगे। यह काला मुच्छड़ तो सौ फीसद भंगी ही होगा।’ कॉमरेड शर्मा को उसने भंगी कहा। उनका रंग साँवला था, मूँछें लंबी थीं। खादी का सफेद कुरता-धोती उनका पहनावा था। ये तो ब्राह्मण हैं, ये अछूत नहीं हैं। हमने सफाई पेश करने का प्रयास किया, परंतु किसानों का क्रोध कम नहीं हुआ। हमें खाने के आसन से अपमान के साथ उठना पड़ा।’
‘तुमलोग, अभी तुरंत गाँव से बाहर निकल जाओ।’ हम भोजन के स्थान से उठा दिए गए। शर्मा ने भी उन्हें समझाया, ‘देखो भाई मैं कॉमरेड हूँ, कोई चमार-भंगी नहीं हूँ। ब्राह्मण हूँ पर जहाँ पर मेरे साथियों का अपमान होता हो, वहाँ मैं हरगिज खाना नहीं खाऊँगा। यह जाति भेद गाँव की तरक्की और ‘किसान एकता’ के लिए अच्छा नहीं है।’ ‘देखा कॉमरेड, हमारे यहाँ किस हद तक जाति कोई समस्या नहीं है?’ वहाँ से हम बकैनिया में मौसा देवीदास जी के यहाँ पहुँचे। यह मेरे गाँव का है। वहाँ उनके भतीजे गुलाब दर्जी से मुलाकात हुई। भाभी और बेटी हमें खाना खिला रहे थे कि तभी तेज़ आँधी-तूफान आ गया, उसे थमने तक हम वहीं रुके रहे।
मैंने 1983-84 में सीजीओ कॉम्पलेक्स (जे.एन. स्टेडियम), दिल्ली में रेडियो कर्मचारी पद के लिए एक साक्षात्कार दिया था। तब मुझसे सामान्य ज्ञान के तौर पर चन्दौसी के रीजनल रेलवे ट्रेनिंग स्कूल के बारे में पूछा गया था। मैस यूनियन के साथियों के पास मैं कॉ. शर्मा के साथ मिलने जाया करता था। यदाकदा मैस के साथियों के साथ खाना भी खा लिया करता था। कॉ. चन्द्रपाल मैस यूनियन के सचिव हुआ करते थे। यूनियन साथियों की सेवा संबंधी केस में कॉमरेड उनकी कितनी और क्या मदद कर पाए, मुझे पता नहीं।
मामा अमर सिंह–‘ख़लीफा’ : मामा की देह बड़ी आकर्षक थी। उनकी शारीरिक संरचना नाना-नानी जैसी, लंबी-चौड़ी कद-काठी थी। उनका चेहरा चौड़ा, मूँछें बड़ी और पहनावा हमेशा ही एक छींट का या पट्टे का धवल कुर्ता होता था। वे मुस्लिम पठान की तरह रहते थे। उसके अलावा मैंने उन्हें कभी अन्य किसी पोशाक में नहीं देखा। चन्दौसी में ‘अप्सरा टॉकीज’, ‘लक्ष्मी टॉकीज’, ‘अजन्ता टॉकीज’ और रेलवे स्टेशन मामा के रिक्शा खींचने के ख़ास स्थान थे। उनकी गाढ़ी कमाई हिंदू बाबाओं के प्रति आस्था सेवा में निकल जाती थी। वे हर नई फिल्म देखते थे। कई अभिनेताओं से अपनी तुलना करते थे। पर स्त्री जाति से ऐसी विरक्ति थी कि कभी उन्हें कोई अभिनेत्री अच्छी लगी हो, उन्हें तारीफ करते कभी नहीं सुना। देवानन्द उनके ज़हन पर हावी थे। शिक्षा से उन्हें गहरी विरक्ति थी।
मामा की दृष्टि में सबसे वाहियात काम पढ़ना-लिखना था। शायद ही ऐसी कोई शाम हो जब वे दारू पीकर न आए हों। उनके पीने से मुझे क्या परेशानी होती, अगर वे चुपचाप आकर आराम करते, परंतु वे लगातार बोलते, गालियाँ देते रहते। पढ़ने में पूरा डिस्टर्बेंस क्रिएट करते थे, बल्कि उनकी माँग होती, ‘अगर तूने कहीं से भी खाना बनाया-खाया है तो मेरे लिए बना कर क्यों नहीं रखा?’ चन्दौसी में रहते सबसे बड़ा संकट था मेरा किसी तरह की आय का कोई जरिया न होना। मुझसे अपना ख़र्चा भी निकालना मुश्किल हो रहा था, फिर मैं मामा का पेट कैसे भरता?
खाना तो दूर चाय-नाश्ता भी नसीब नहीं था। अक्सर खाली पेट कॉलेज की ओर भागता था। कक्षाएँ समाप्त होते ही चुन्नी मोहल्ला की ओर वापस होता था। मेरा आना-जाना पैदल ही होता था, जबकि मेरे साथी छात्र-छात्राएँ रिक्शे, साइकिल या मोटरसाइकिलों से आते-जाते थे। पेट की आग खाना माँगती। विद्या की भूख थोड़ी शांत जगह चाहती, जहाँ सुकून से बैठ कर पढ़-लिख सकूँ। सड़क के दोनों ओर कहीं कड़ाही में दूध खौल रहा है, कहीं चाट-पकौड़े बिक रहे हैं। कहीं होटल पर खाना खुला है, परंतु जेब में एक पैसा नहीं तो मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है। सब कुछ अनुपलब्ध के समान था। मेरे साथी मुझे कई बार बुलाते श्यौराज आओ चाट खाते हैं। कुछ मीठा खा लो आदि। मैं जानता था दोस्ती में अदला-बदली होती है। एक बार खा लिया, तो अगली बार खिलाना भी होगा। जेब में पैसे न आज हैं, न कल होंगे। पेट में खाना नहीं हैं, भूखा हूँ, यह किसी को बता नहीं सकता था। अपनी खुद्दारी, अपना आत्मसम्मान सुरक्षित रखना था। यदि नहीं रखा होता तो मैं आज यहाँ नहीं होता। नानी के घर में एक-दो दिन को भी खाद्य-सामग्री नहीं रहती थी। यदि मैं रखता भी तो मामा नहीं रखने देता। वह खुद खाता और ज्यादा देखता तो परजीवी साधु-सड़ेलों को पकड़ लाता था। ये नागा हैं, ये ठंडे-सरी बाबा हैं। भभूत ही लपेटते हैं, इन्हें सुल्फा-चीलम बनाओ, नाश्ता कराओ। शिव-भोले के पुजारी हैं, भाँग-धतूरा पीते हैं। सेवा करो तो आशीर्वाद देते हैं।
बचपन में अम्मा के साथ जब मैं चन्दौसी के रेलवे स्टेशन के बाहर आता था तो मैं अक्सर रिक्शे वालों में मामा को ढूँढ़ा करता था। कभी-कभी मामा हमें अपने रिक्शे से नानी के घर छोड़ आते थे। वरना हम पैदल ही चल पड़ते थे। उन दिनों भी वे कभी-कभार पीते तो थे, परंतु उन्हें पीने की लत नहीं थी। जैसे-जैसे उम्र बढ़ती गई, लत भी बढ़ती गई। उन्हें जितना पढ़ना-लिखना फिजूल था, उसके ठीक उलट उतना ही प्रमुख हिंदू-बाबाओं के प्रति श्रद्धा, सेवा और समर्पण ज़रूरी था। वे बाबाओं के लिए सुलफा, भाँग और यहाँ तक कि शराब का भी इन्तज़ाम किया करते थे। बस्ती से बाहर बम्पुलस (नगर पालिका का सार्वजनिक शौचालय) से थोड़ा आगे मरघट के पास एक बाग़ था। एक दिन मैंने देखा कि वहीं नल के पास पेड़ों के बीच खड़ेश्वरी महाराज खड़े हैं। मामा उनके लिए नशे का इन्तज़ाम कर रहे हैं। वे खड़े-खड़े दारू गटक रहे हैं, मैं कुछ बोलता हूँ, तो डाँट कर भगा देते हैं। एक बार बाबा को दारू पीते किसी और ने देख लिया और बस्ती में उन्हें भोजन देने से मना कर दिया। मामा ने घर आते ही मेरे गाल पर चाँटा रसीद कर दिया, ‘बाबा का राज़ तूने ही खोला होगा।’ गुस्सा शांत होते ही कहा, ‘तू भी बाबा की सेवा कर लिया कर, मैं तुझे किसी बड़े बाबा का चेला बनवा दूँगा। आराम से तेरे खाने-पीने का इन्तज़ाम हो जाएगा। शहर के धनी घरों की बहुएँ बैठे-बिठाए खीर-पूड़ी पहुँचाएँगी। इन किताबों में आँखें फोड़ने से कुछ हासिल नहीं होगा। मेरा कहा मान, तू भी बाबा का चेला बनकर कहीं निकल जा। बैठ कर खाएगा, मौज करेगा। लोग खूब अच्छा खिलाते-पिलाते हैं। पाँव छूते हैं, सम्मान देते हैं। साधु बाबा रेलों-बसों में बिना टिकट यात्राएँ करते हैं।
मामा एक दिन अपने साथ दो-तीन बाबाओं को घर ले आए और बोले कि ‘चला जा इनके संग, 10-15 दिन में कमाना-खाना सिखा देंगे तुझे।’ केवल पेट पालने के लिए जिया जाए तो विकल्प अच्छा था। बचपन में मेरे शिक्षक प्रेमपाल सिंह यादव ने यह कह कर मेरा घर छुड़वाया था कि ‘भविष्य में हम जनसेवा के लिए संत बनेंगे’, परंतु मैं जैसे-जैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तार्किक विचारों को अपनाता गया, उतना ही अधिक दुनियादार होता चला गया। मेरे लिए कोई और दुनिया, मोक्ष, कैवल्य, निर्वाण आदि काल्पनिक और अविश्वसनीय होते चले गए।
नतीजा यह हुआ कि मामा ने मुझे ‘गंगुर्रा’ वाले मौसा जी द्वारा खरीद लिए गए नाना के घर से लात मार कर बाहर निकाल दिया। उन दिनों तेज सिंह को पाली से मेरे पास भेजा गया था कि श्यौराज की सोहबत में जा कर कुछ पढ़ाई कर ले। हाई स्कूल तक वह मेरी सलाह से और मेरा भाई होने के नाते मेरे पुराने स्कूल चिरौरी से पढ़कर आया था। चन्दौसी में रह कर वह बारहवीं करना चाहता था। उसके लिए श्री भिखारी लाल ने दो किलो घी और कनस्तर भर आटा दिया था। परंतु उसने रामकुमार की पत्नी से कहा, ‘भाभी जी, दादा (पिता) ने कहा है कि इसे श्यौराज पर ख़र्च मत करना, वो तेरा सौतेला भाई है।’
उन्होंने उसे डाँटा, इसलिए कि रामकुमार स्वयं अपनी माँ के पुनर्विवाह के समय साथ आए थे, परंतु न तो घर-ज़मीन के बँटवारे में उन्हें सौतेला समझा गया था और न उनकी शिक्षा में कोई कमी रखी गई, आख़िर रेलवे में बतौर गार्ड सर्विस में थे। शाम को उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारा भाई ऐसी-ऐसी बातें कर रहा था। उस दिन के बाद मैंने तेज सिंह से कहा कि तुम केवल अपना ख़र्चा उठाओ।
फिर भी तेज सिंह ने ‘बूढ़ी माता’ वाले मोहल्ले में एक कमरा किराये पर लिया तो मुझे भी रात गुजार लेने के लिए कह दिया। पर वह घर किसी बनिये या ब्राह्मण का था। चुन्नी मोहल्ले के बच्चे जो हमारे पास आते-जाते थे, उनके बारे में ये लोग भी जानते थे और उनके हाव-भाव-पहनावे बोलते थे कि वे चूड़े-चमारों के बच्चे हैं। तो उनका कहना था कि तुम्हें चमारों में ही जाकर रहना चाहिए। तुम उच्च हिंदुओं के घरों में किरायेदार नहीं रह सकते। उन्होंने जाति जाहिर होने के तीन-चार घंटों के दौरान हमसे कमरा खाली करा लिया था, बल्कि तुरंत ही हमारा सामान, जो बहुत कम था, घर से बाहर रखवा कर ताला लगा दिया था। एक माह का एडवांस दिया किराया भी वापस नहीं किया था। चन्दौसी में अब हम कहाँ रहते! तेज सिंह प्राइवेट पढ़ने के इरादे से अपने गाँव ‘पाली’ वापस चला गया और मैं फिर अपने मित्रों के पास या गाँव के किसानों-मजूरों की शरण में चला गया।
कॉमरेड दत्ता और कॉमरेड शर्मा दोनों नरौली इंटर कॉलेज में अध्यापक थे। दत्ता साइंस पीजीटी थे और भगवान दास टीजीटी। दत्ता ट्यूशन कर कमाई पर अधिक समय खर्च करते थे। खाली समय में ये दोनों दलित छात्रों को बरगलाया करते थे। इन्हें ब्राह्मण का नेतृत्व चाहिए था, सो एक सी.पी.आई. में तो दूसरा सी.पी.एम. में। आपसी संबंधों में कोई मधुरता नहीं। वी.के. दत्ता जनवादी लेखक संघ के नेता थे, जबकि लेखन के नाम पर उनकी हस्तलिपि ही अच्छी थी। सो, वे नारे-पोस्टर अच्छे लिखा करते थे। इसी दम पर वे जलेस के सचिव हुआ करते थे। कॉमरेड शर्मा सी.पी.आई. में थे। ये दोनों वैचारिक रूप से मार्क्सवादी थे, जातिविहीन समाज बनाने के लिए स्वयं को समर्पित क्रांतिकारी मानते थे। दत्ता की तुलना में शर्मा का आर्थिक चरित्र अच्छा था। परंतु यदि इन दोनों के जात्याभिमान के प्रतीक ब्राह्मण सूचक ‘सरनेम’ छीन लिए जाते तो दोनों आत्महत्या कर लेते–कहते, ऐसी सामाजिक क्रांति भाड़ में जाए हमसे हमारा ब्रह्मणत्व छीनना चाहे।
राकेश के नेतृत्व वाले ग्रुप ने जाति सूचक सरनेम हटा दिए थे। उन्होंने सक्सेना हटा कर ‘रफीक’ लगाया। प्रदीप कुमार शर्मा खाली ‘कुमार प्रदीप’ हो गए थे। विजयबहादुर सक्सेना ‘विजय आलम’ हो गए थे। ये हिंदू-मुस्लिम सांप्रदायिकता की दृष्टि से उठाए गए कदम थे, परंतु जातिभेदवादी वर्ण-निर्वर्ण वाले भेदभाव पर कोई असर नहीं था। वे मुस्लिम सरनेम जोड़ सकते थे। दलित का भंगी-चमार अथवा माँग-महार माला, मदगा नहीं जोड़ सकते थे यानी हिंदू-मुसलमान मिश्रित पहचान बना सकते थे। दलित के साथ नहीं बना सकते।
मैंने तथाकथित प्रगतिशीलता पर सोचा। वहाँ हिंदू-मुस्लिम भाईचारे की अच्छी कोशिश हुई है। साहित्य के इतिहास में तरक्की पसंद लेखकों की मुहिम काफी असरदार रही है। गीत-संगीत के माध्यम से सांस्कृतिक चेतना जगाई गई। भाईचारे को प्रोत्साहन मिला। ‘तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इनसान की औलाद है, इनसान बनेगा।’ ऐसी गंगा-जमुनी तहजीब भी हिंदू-मुसलमानों तक सीमित रही। तीस करोड़ ‘बहिष्कृत-भारत’ से तो इनका कोई वास्ता ही नहीं रहा।
यह साझा भाव हिंदू-मुस्लिम लेखकों की साझा मुहिम के कारण आया था। दलित वहाँ भी अछूत था। शैलेन्द्र जैसा शायर वहाँ अपनी जातीय पहचान चमार के साथ नहीं था। इसलिए उन हिंदू-मुस्लिम कवियों ने दलित बहिष्कार के साथ इनसान बनने की बात कही। यदि उन गैर-दलित कवियों में कोई मेरे जैसा दलित कवि समानता का वातावरण बना रहा होता तो ज़रूर कहता–
‘न तू ब्राह्मण बनेगा, न तू अछूत बनेगा
तू भारती है, भारती का पूत बनेगा।
तोड़ेगा सामाजिक, गुलामियों की बेड़ियाँ
समता-स्वतंत्रता का, अग्रदूत बनेगा।’
कीचड़ में मार्क्स और अम्बेडकर : जिन दिनों मैं चुन्नी मोहल्ले में गंगुर्रा वाली मौसी को दे दिए नाना के घर में रह रहा था, तब मामा अमर सिंह इसके साथ वाले कमरे में रहते थे। मौसी के कमरे की चिनाई मैंने स्वयं की थी। तब मेरे साथ के ग्रेजुएशन के छात्र-छात्राएँ जो इस मोहल्ले में थे, चकित होते थे कि देखो श्यौराज कैसे राजमिस्त्री का काम कर रहा है!
मैं गाँव से कनस्तर में दस-पंद्रह किलो आटा लेकर आया था। इस कमरे में चूल्हा था। मैं सुबह शौच को जाता तो बाग की ओर से जलावन लकड़ियाँ बीन लाता था, क्योंकि चुन्नी मोहल्ला शहर के बाहर उसी तरह अलग बसा था, जिस तरह गाँव के बाहर बहिष्कृत जातियों को दक्षिण में बसाया जाता है। यहाँ भी दलितों को शहरों के स्लम्स में रहने के लिए मजबूर किया जाता था। जब मैं खाना बनाता तो मामा के लिए भी बनाता, एक बार जब आटा खत्म हो गया तो उन्होंने कहा, ‘आटा ला और मेरे लिए रोटी बना।’ मैंने कहा, ‘मैं कहाँ से लाऊँ? मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं विद्यार्थी हूँ। रिक्शा आपकी आय का जरिया है, लेकिन मेरी आय का कोई स्रोत नहीं है।’ तो ‘चल मैं तुझे चलाना सिखाता हूँ। मैं रिक्शा कैसे चलाऊँगा मेरे तो घुटनों में गठिया-बाय का दर्द रहता है। तो तुझे पढ़ने के लिए समय और भूख शांत करने के लिए रूखा-सूखा खाना मिलना चाहिए। पर आएगा कहाँ से? तो तू पढ़ना छोड़ और कहीं कोई दूसरा काम कर या इस घर से चला जा। क्या तेरा बाप कह मरा था कि रोटी-कपड़े मिलें न मिलें, तुझे पढ़ते रहना है?’
मामा कठोर स्वर में बोला तो मैंने कहा–‘मैं कहीं चला जाऊँगा, मुझे थोड़ा वक्त दो।’ पर मामा का समाधान नहीं हुआ। मौसी-मौसा गाँव में थे। घर खाली था। फिर भी उन्हें अंदेशा हुआ कि पढ़ने वाला लड़का है। नानी-नाना का घर होने के नाते कहीं खरीदे हुए घर में अपना नाम न डलवा ले। इसलिए वे भी मुझे घर से निकाल देना चाहते थे। मौसा जी द्वारा मामा को उकसाने का यह सबसे आसान बहाना था।
मैं भूखे पेट बाहर निकला। ‘कहाँ रहूँगा? किराये पर भी यहाँ कौन मुझे घर देगा और देगा भी तो मैं किराया कहाँ से दूँगा? ‘अम्बेडकर छात्रावास’ में रह नहीं सकता। वहाँ दलित छात्र ही असहयोग करते हैं। माहौल खराब है। वहाँ पढ़ाई नहीं हो सकती।’ मेरी जेब में पैसे नहीं थे। देर रात वापस लौटा तो देखा घर के बाहर नाली के आसपास मेरी सारी कॉपी-किताबें फेंकी हुई हैं। किसने फेंकी हैं? किसी से जानने-पूछने की जरूरत नहीं थी। मामा नशे में धुत्त बैठे गालियाँ बक रहे थे, ‘यहाँ पढ़ने को रहेगा और मेरे लिए खाने का इन्तज़ाम नहीं करेगा। भाग जा यहाँ से। उठा ले जा अपनी किताबों-कॉपियों को, नहीं तो मैं इन्हें कूड़े में फेंक दूँगा।’
मैंने देखा, किताबों की शक्ल में नाली में कहीं मार्क्स पड़े थे, कहीं गाँधी जी, कहीं गोर्वाचोव, कहीं गोर्की, कहीं स्तालिन, कहीं लेनिन, तो कहीं अम्बेडकर, कहीं फुले, कहीं ‘खून के छींटे इतिहास के पन्नों पर’ पड़ी हुई थीं। कहीं ‘मधुशाला’ के रूप में हरिवंशराय बच्चन, कहीं ‘भागो नहीं दुनिया को बदलो’ में राहुल, कहीं कबीर, रैदास, तो कहीं साहिर, कहीं कैफ़ी आज़मी और कहीं निराला, कहीं मुक्तिबोध और कहीं सत्यार्थ प्रकाश के रूप में दयानन्द सरस्वती पड़े थे। किताबों की शक्ल में जिन्हें मैं वर्षों सीने से लगाए रहा, उनकी ऐसी दुर्दशा? आदत तो ऐसी थी कि सोता भी था तो कोई-न-कोई किताब छाती पर रखकर पढ़ते-पढ़ते ही नींद आती थी। वैसे भी सौ-दो सौ किताबों के अलावा मेरे पास और कुछ था भी नहीं। एक सर्वहारा के पास इतनी सारी किताबें कहाँ से आ गई थीं? इसमें सोवियत साहित्य पिछले पाँच-छह सालों में निःशुल्क ही मेरे पास आया करता था। दूसरा हरी बुक डिपो पुरानी किताबों का भी केंद्र था। मैं दु:ख भरी आँखों से बिखरी किताबों का नजारा देख रहा था। क्या करूँ, अब ये किताबें कहाँ ले जाऊँ? किताबों में कोर्स की तो थीं ही, साथ ही ढेर सारा रशियन लिट्रेचर भी था।
बराबर में रामकुमार (गार्ड) का मकान था। ननिहाल के रिश्ते से मैं उनका अंकल था, परंतु उम्र में वे मुझसे बड़े थे। मैं उन्हें भाई साहब और उनकी पत्नी को भाभी जी कहता था। वे इंग्लिश में एम.ए. थीं। किताबों की क़ीमत समझती थीं। वे मेरी अध्ययनशीलता का बड़ा सम्मान करती थीं। अतः उनकी बैठक के एक कोने में किताबें रख देने की प्रार्थना की। उन्होंने रखवा लीं और मैं मदद के लिए कॉमरेड भगवान दास शर्मा के घर गया। उन्हें किताबों की कथा बताई तो वे उसी वक्त मेरे साथ-साथ चले आए। हालाँकि यह आधी रात के बाद का वक्त था। उस समय सारी बस्ती, सारा शहर सोया हुआ था।
शर्मा रिक्शा में कुछ किताबें उठवा कर अपने घर ले गए और कुछ उसी खुली बैठक में रख दी गईं। आकर्षक रशियन काग़ज़ की कई किताबें बच्चे उठा ले गए। मैं क्या करता? पठनीय सामग्री बचा पाने की मुश्किल मेरे साथ शुरू से ही रही। यहाँ तक कि मेरे शैक्षिक दस्तावेज भी कहीं सुरक्षित रखने की जगह नहीं थी। गाँव में भी मेरे छोटे भाई की पत्नी ने एक बार मेरी किताबें रद्दी में यह कहकर बेच दी थीं कि इनसे पीछा छूटेगा तो ये कुछ काम-धंधा करेंगे। यहाँ तक कि मेरे नाम आए ढेर सारे पत्र भी उसने रद्दी कहकर निकाल दिए थे। भगवान दास के यहाँ भी हर कोने में किताबें भरी रहती थीं। फिर भी उन्होंने बैठक में बनी स्लेप पर कुछ किताबें रख दीं। कॉ. शर्मा तब तक मेरी मुसीबत में साथ थे, जब तक मैं केवल वर्ग संघर्ष की बात करता था, किंतु जब मैं दलित चेतना के साथ अस्पृश्यता का प्रश्न उठाने लगा, दलितों के प्रति होने वाले जाति-उत्पीड़न पर बोलने लगा तो मेरे दोस्त ही दुश्मन बनने लगे। यह अजीब था कि सवर्ण-कॉमरेड दलितों को जगाएँ तो क्रांतिकारी कहलाएँ और दलित खुद दलितों को जगाने लगें तो यह प्रतिक्रियावादी और संकीर्ण जातिवादी कहलाएँ। यह स्थिति केवल भगवान दास शर्मा की ही नहीं थी बल्कि बिलारी के राकेश ‘रफीक’, मुशर्रफ अली की भी थे। कॉमरेड शर्मा ने तो चन्दौसी में हुई एक आम सभा में मुझे बोलने तक नहीं दिया था कि ये अब जातियों का आंदोलन चलाते हैं, उन्हें क्रांतिकारी वर्ग संघर्ष से क्या लेना-देना?
Image: attacked a goat gray wolves-1901
Image Source : WikiArt
Artist : Zinaida Serebriakova
Image in Public Domain