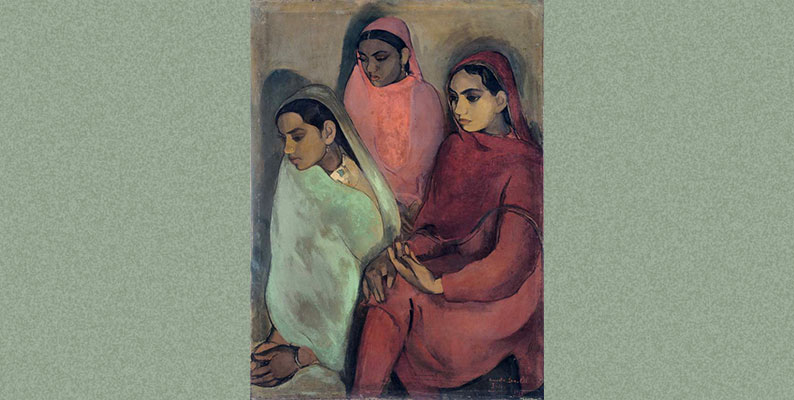दु:ख ही जीवन की कथा रही
शेयर करे close
शेयर करे close

शेयर करे close
- 1 June, 2024
दु:ख ही जीवन की कथा रही
गाँव चकमहमद, पत्रालय देसरी, जिला वैशाली (हाजीपुर), राज्य बिहार। सौ-सवा सौ घरों का गाँव। उत्तर-पूरब में घाघरा नदी जो गर्मी में सूख जाती है, पश्चिम में सड़क और दक्षिण में रेल लाइन। इसी गाँव के एक गरीब किसान इन्द्रदेव सिंह के घर 16 मार्च 1952 को प्रथम पुत्र के रूप में मेरा जन्म हुआ था, दो छोटे और भाई थे और एक छोटी बहन। कुल जमा सात जन का परिवार। तब दादा जी जीवित थे और हमारे साथ थे। जमीन कम थी–मात्र एक सौ पैंतीस डिसमल के आस-पास। उसी में ऊपरबार भी और धनहर भी। साल-भर का अनाज नहीं जुट पाता था। इसलिए दादा के समय से ही घर के लोग आसाम जाते रहते थे–कमाने के लिए। दादा जी सरदार थे–मोटिया का काम करने वाले मजदूरों का सरदार। पिता जी जहाजघाट में मुंशी थे–वैतनिक। बस, थोड़ी-सी पगार–उन दिनों गाँव में पढ़ने-लिखने का रिवाज कम था। दादा तीसरा पास थे और पिता जी सातवाँ। चाचा जी तो अँगूठा छाप थे। पिता जी अँग्रेजी भी लिख-पढ़ लेते थे। इसीलिए उन्हें जहाजघाट में मुंशी-गिरी मिली थी। दादा जी बताते थे कि शुरू-शुरू में वे पैदल ही महीना दिनों में सिलचर पहुँचते थे। सत्तू, चिउरा, भूँजा–यही सब साथ लेकर जाते थे और पैदल ही वापस भी होते थे–साल-दो साल के बाद। लोग समूह में निकलते थे–दस-पंद्रह की संख्या में। पर पिता जी के समय में रेल गाड़ी चलने लगी थी। यही कारण था कि वह सातवीं की पढ़ाई बीच में ही छोड़कर दादा जी के साथ सिलचर भाग निकले थे।
गाँव में स्कूल नहीं था। दूसरे गाँव के स्कूल में पढ़ने के लिए जाना पड़ता था। पर घाघरा नदी पर पुल नहीं था। रेल लाइन से होकर माँ-बाप अपने बच्चे को स्कूल भेजने से कतराते थे। हमारे गाँव के पश्चिमी छोर पर एक राजपुताना गाँव था। पर उस गाँव में लोग अपने बच्चे को नहीं भेजते थे क्योंकि राजपुताना के बच्चे कुरमियान के बच्चों को प्राय: मारते-पिटते रहते थे। डर से बच्चे भी उस स्कूल में जाना नहीं चाहते थे।
चाचा जी के तीन लड़के थे। तीनों हमसे बड़े थे। पर केवल बड़े भैया पढ़ते थे। उन्हीं के साथ माँ मुझे भी उस स्कूल में भेज देती थी। तब वह पाँचवीं में पढ़ते थे और मैं पहली में। घड़ी नहीं थी–जमीन में गड्ढा बनाए हुए थे। घर के छप्पर की छाया जब वहाँ पहुँच जाती थी, तो हम दोनों स्कूल को भागते थे। बस, साथ में केवल एक बोरा रहता था झोला में बैठने के लिए–किताब-कॉपी, स्लेट-पेंसिल कुछ भी नहीं। सुबह स्कूल पहुँचते ही सबसे पहले बोरा बिछाकर सामने की जमीन को गोबर से लिपना पड़ता था। जब तक प्रार्थना होती और हमलोग अपने-अपने बोरा पर आ बैठते, तब तक वह जगह सूख जाती थी। फिर तो उसी सूखी जमीन पर कोई जानकार छात्र गोरी मिट्टी से ‘अ आ इ ई उ ऊ’ लिख देता था। मैं दिनभर उसी का नकल उतारता रहता और याद करता रहता था। हाजिरी लेने के बाद ऊँची कक्षा से छुट्टी पाने पर वर्ग शिक्षक एक बार आते थे और जमीन पर बच्चों की अपनी लिखावट देखते थे और सुनते थे। शाम तक पाठ यादकर मुँह-जवानी सुना देना पड़ता था, दूसरे दिन फिर से वही प्रक्रिया शुरू होती थी–‘ए, ऐ’ की। इस तरह साल पूरा हो गया था। इस बीच मैंने हिंदी-वर्णमाला, बारह खड़ी, सौ तक गिनती और एक से बीस तक का पहाड़ा याद कर लिया था। वार्षिक परीक्षा देकर दूसरी कक्षा में चला गया था।
पर एक दिन उस वर्ग-शिक्षक ने जूता पहने पाँव से ही मुझे इतना कसके मारा था कि मैं दो ‘ढबकुनिया’ खाया था। जूते के सोल से मेरा होंठ कट गया था और खून निकल आया था। बगल के सवर्ण बच्चे खूब हँसे थे। उन पर मुझे गुस्सा भी आ गया था। दरअसल गप्पें वे सब कर रहे थे और मार मुझे लगी थी। इतने पर भी जब उस वर्ग शिक्षक का गुस्सा कम नहीं हुआ था, तब उसने फिर से मुझे पहली कक्षा में वापस कर दिया था। मेरा अपराध सिर्फ इतना था कि मैं साल के अंदर ही पहली कक्षा पास कर दूसरी में आ गया था और पिछड़ी जात का था।
यह तो बाद में, जब एक दिन डिपुटी साहब आए थे और उन्होंने पहली कक्षा के लड़कों से पूछा था, ‘इक्कीस का पहाड़ा जो सुना सकता है, वह हाथ उठाएँ।’ मैंने अपना हाथ उठा दिया था और पहाड़ा भी सुना दिया था। उन्होंने उसी समय वर्ग शिक्षक से कहा था, ‘इसे दूसरी कक्षा में भेज दो…।’ परंतु दूसरी कक्षा के वर्ग शिक्षक भी तो वे ही पंडित जी थे। मैंने दूसरे दिन से स्कूल जाना ही बंद कर दिया था। फिर तो एक दिन माँ ने गाँव के एक चाचा के साथ देसरी के प्राथमिक पाठशाला में भेज दिया था। उसी दिन उन्होंने पहली कक्षा में मेरा नाम भी लिखा दिया था। अंदाज से उन्होंने मेरी जन्म तिथि 16 मार्च 1952 लिखवा दी। तब मैं छह साल का था। मेरी पढ़ाई की शुरुआत यहीं से हुई थी। यहाँ पढ़ाई भी अच्छी होती थी और लड़के भी थे। बैठने के लिए भी बेंच, डेस्क सब थे। बहुत अच्छा लगता था, पढ़ने में मन लगता था।
सूखी मिट्टी : लहलहाती पौध–बाबू जी बराबर प्रदेश में ही रहते थे। चूँकि दादा जी थक गए थे, घर पर ही रहने लगे थे। सरदारी भी तो चली गई थी। पिता जी ने कुछ धनखेती अरज ली थी–दस कट्ठा के आसपास। खाने-भर अनाज हो जाता था, पर मेहनत बहुत करनी पड़ती थी। थका-माँदा रहने पर भी वह मुझे भोर में पढ़ने के लिए उठा देते थे। न चाहते हुए भी उसी समय लालटेन जलाकर पढ़ना पड़ जाता था। क्लास में फर्स्ट आने की शुरुआत यहीं से हुई थी।
क्लास मॉनिटर मैं ही था। दिवाल के उस पार कन्या पाठशाला थी–सातवीं कक्षा तक। एसिसमेंट का नंबर जोड़ने और प्रतिशत निकालने के लिए वहाँ जाना पड़ता था। अच्छा लगता था। पढ़ाई में बेहतर करने की प्रेरणा भी मिलती थी। यहाँ पाँचवीं तक ही कक्षाएँ थीं। फिर तो पास के हाई स्कूल में जाना पड़ गया था। कन्या पाठशाला की इन लड़कियों से मुलाकात तो आठवीं कक्षा में ही जाकर हुई थी।
1965 का समय था। तीन सेक्सन थे आठवीं में। अपने स्कूल के बच्चे सेक्सन ‘ए’ में थे जबकि दूसरे स्कूल से आनेवाले बच्चे अनुभाग ‘बी’ और ‘सी’ में। एक से बढ़कर एक लड़के थे–वज़ीफ़ा लेने वाले भी। विज्ञान शिक्षक की कमी थी, इसलिए विज्ञान विषयों की कक्षा लेने हमें दोनों अनुभागों में भी जाना पड़ता था। शिक्षक तो तीनों अनुभाग को खिड़की से देखते रहते थे। तब कक्षा में पढ़ाते समय हमलोग बहुत सतर्क रहते थे। इस तरह हमलोगों की तैयारी होती रहती थी। जब आठवीं का रिजल्ट निकला था तो, मुझे 648 अंक आए थे, जबकि दूसरे और तीसरे स्थान पर रहनेवाले को क्रमशः 619 और 616। रिजल्ट के बाद प्रधानाध्यापक मुझे खोज रहे थे, पर उस दिन तो मैं ननिहाल गया हुआ था नौवीं कक्षा की पुस्तकें लाने। हर साल वहीं से तो किताबें लाता था, तब पढ़ता था।
स्कूल में एक छोटा-सा पुस्तकालय था, अच्छी-अच्छी किताबें थीं वहाँ। मुझे लाइब्रेरियन बना दिया गया था, छुट्टी के समय चालिस मिनट के लिए मुझे वहीं ड्यूटी करनी पड़ती थी। खूब पढ़ता था मैं वहाँ, पुस्तकें भी घर ले जाया करता था। प्रसाद, प्रेमचंद, दिनकर, रेणु, शरतचन्द्र, टैगोर आदि को मैंने वहीं से जाना था। कुछ-कुछ लिखने भी लगा था। मेरे सहपाठी मुझे छायावादी कहते थे। कहते हैं, जीवन में सुख-दुःख, धूप-छाँह की तरह आते रहते हैं। सिलचर का जहाजघाट बंद हो गया था। पिता जी की नौकरी जाती रही। गाँव आ गए थे, वह खेती में लग गए थे। फलतः मुझे भी उनके साथ गृहस्थी का जुआ अपने कंधे पर लेना पड़ा था। हालाँकि एक ईंट-भट्ठा में फिर से उन्हें मुंशी की नौकरी मिल गई थी, पर वह मजा नहीं था। बँधी तनख्वाह, वह भी कम–दाल-रोटी भर। वह हर माह पैसे तो भेजते थे, पर इससे घर का खर्च नहीं चल पाता था। दादा जी गुजर गए थे। गृहस्थी की सारी बोझाई मेरे सिर आ गई थी। किसी-न-किसी तरह उसका असर मेरी पढ़ाई पर भी पड़ने लगा था। 1967-68 में जब बिहार की स्थिति अस्त-व्यस्त थी, मैट्रिक का टेस्ट देकर मैं भी आसाम चला गया था। कुछ दिनों तक भटकने के बाद मुझे भी एक चिमनी में मुंशी की नौकरी मिल गई थी।
हालाँकि मैं कमाने नहीं गया था सिलचर, बल्कि मैं तो यह देखने गया था कि आखिर ऐसी कौन-सी चीज़ है आसाम में जहाँ हमारे पूर्वज महीना दिनों तक पैदल चलकर पहुँचते थे और आज भी गाँव-घर के लोग वहाँ जा ही रहे हैं। यह तो वहाँ जाने पर पता चला था कि वहाँ मजदूर वाला काम है और देह-तोड़ मेहनत कर दो पैसा उगाहते हैं लोग। जितनी मेहनत थी उतनी कमाई भी नहीं थी। ठेला खिंचना, रिक्शा चलाना, मोटियागिरी करना, ईंट-भट्ठा में ईंट ढोना। साल-डेढ़ साल में ही बीमार पड़ जाते थे, फिर गाँव लौट जाते थे। …उन्हीं दिनों पिता जी ने 10 डिसमल का एक धनहर प्लॉट बेचने की बात पक्की कर ली थी। जमीन बेचने की शुरुआत वहीं से हुई थी। मैं गाँव लौट आया था, बोर्ड की परीक्षा जो देनी थी।
मैं सेंट-अप हो गया था। 504 नंबर आए थे। मेरे नाम के सामने लाल से राइट का चिह्न लगा था। मतलब था कि मैं बोर्ड में फर्स्ट क्लास ला सकता हूँ। प्रधानाध्यापक ने मुझे स्कूल का एक कमरा दे दिया था और वहीं रहकर बोर्ड की तैयारी करने को कहा था। जबकि मुझे तो नौका-विहार करना, चौर में नाव पर चढ़कर चिड़ियों का शिकार करना, तालाब में खिले भेट मास, कमल, काले बादल भरे आकाश में बगुलों की पंक्तियाँ आदि को देखकर कविता करने और गाँव की गरीबी को देखकर कहानी लिखने का खूब मन करता था। पर मास्टर जी स्कूल से बाहर जाने देते ही नहीं थे। मैट्रिक की परीक्षा तो मैंने किसी तरह दे दी थी, पर रसायन शास्त्र और अँग्रेजी का पेपर गड़बड़ा गया था, फिर भी 609 नंबर आए थे।
1968 का समय था। परीक्षा देने के दूसरे ही दिन से एक दवा दुकान में काम करने लगा। दवा दुकान के मालिक के बड़े भाई डॉक्टर थे। और जब रिजल्ट निकला था तो, वे (डॉक्टर) गाँव से ही अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए मुझे साथ ले गए थे। आशा बँधी भी थी कि वे मेरा नामांकन वहाँ के एक कॉलेज में करा देंगे। करा भी दिया था उन्होंने, पर वहाँ कॉलेज कहाँ था? वह तो मात्र फॉर्म और पैसा क्लेक्शन सेंटर था। पर मैं भी क्या करता, पढ़ाई छुट जाने से तो अच्छा था कि कॉलेज नामक संस्था से चिपक गया था। नहीं तो कॉलेज में पढ़ने का सपना तो कब को चूर हो गया था। परीक्षा दी–द्वितीय श्रेणी मुश्किल से आ पाई थी। मैं फिर से गाँव आ गया था अपनी किस्मत पर रोने। दरअसल गाँव के ही मेरे एक भाई थे मेरे बड़े हितैषी। डिप्लोमा होल्डर थे, बेकार थे। डॉक्टर साहब की दूसरी पत्नी ने उन्हें भी वहीं बुला लिया था। वह तो सूई लगाने और दवा देने का काम भी कर देते थे, पर मैं तो केवल बच्चों को पढ़ाता था और अपने पढ़ता था। वापस आ गया था।
मैंने आर.एन. कॉलेज में नामांकन करा लिया था। घर से ही आना-जाना करता था। दरअसल यहाँ आकर ही पढ़ाई का माहौल मिला, पढ़ाई मिली, प्राध्यापक मिले, उनका स्नेह-प्यार मिला, पुस्तकालय मिला, पुस्तकें मिलीं। पर नहीं मिला तो आर्थिक अवलंब जिसके लिए मैं लालायित था। नियति के खेल को देखने-समझने का सहुर तो मेरे में आ ही गया था। कॉलेज में था इसलिए सब कुछ भूल जाना चाहता था। गर्मी में ज्यादा परेशानी होती थी। सुबह में कोई गाड़ी नहीं थी, 10 कि.मी. पैदल चलकर चेचर में बस पकड़ना पड़ता था। फिर हाजीपुर पहुँचकर वहाँ से 5 कि.मी. पैदल चलकर कॉलेज जाना पड़ता था। आते-जाते 30 कि.मी. रोज ट्रेन में तो बिना टिकट भी चल जाता था, पर बस में पैसा देना पड़ता था। इसलिए मुझे बस की छत पर बैठना पड़ता था। जो भी पैसे देते थे, खलासी भाई रख लेता था।
पर कभी-कभी लगता था कि पढ़ाई छोड़कर कहीं काम में जुट जाऊँ। मेरा छोटा भाई और बहन दूसरे के खेत से रहर की छिम्मी तोड़कर और उसे चुक्के में सिझाकर नमक-मिर्च के साथ चटकारे लेकर खाता था, तो मेरी रुलाई फूट पड़ती थी। मेरी माँ सुंदर थी–नाम भी था सुरती। उसकी देह पर मैंने कभी अपना खरीदा नया कपड़ा नहीं देखा। नानी, मौसी, फुआ उसे कपड़े देती रहती थीं। मैं सब समझता, पर कुछ कर नहीं पाता था। हाँ, पढ़ाई के प्रति उदासीनता जरूर बढ़ सी जा रही थी।
एक दिन एक ग्राहक आया–राजपुताना का। चौर में हरबाही करनी थी–साढ़े तीन कट्ठा खेत। दो बार जोत, दो बार हेंगा। दो बज गए थे खेत में ही। जीवन का वह पहला धंधा था। 15 रुपये मिले थे–दस रुपये मेरा, पाँच रुपये अधरिया का। कभी-कभी ये रुपये ही मेरे परिवार का आर्थिक संबल होते थे। उस दिन से गाँव के हर-बेचवाओं की सूची में मेरा भी नाम चढ़ गया था। वैसे जो गाँव के हरबाहा थे, ग्राहक को तो वे ही फाँस लेते थे। मेरे यहाँ तो उसर, बंजर, उखट, ढेलवार आदि खेत का ही ग्राहक आता था, पर क्या करता विवशता थी। पैसे के कारण तो कभी-कभी अधरिया के पाँच रुपये मैं देता भी नहीं था और वह चूँकि मेरी स्थिति से अवगत थी, माँगती भी नहीं थीं।
मेरे गाँव में स्कूल नहीं था। उन्हीं दिनों मैंने अपने बथान में एक स्कूल शुरू की थी। गाँव के गरीब बच्चे आते थे और हमलोग तीन-चार लड़के मिलकर दो-ढाई घंटा रोज पढ़ाते थे। गाँव के लोग बहुत खुश थे। मैं भी खुश था कि वैसे बच्चे-बच्चियाँ जो स्कूल नहीं जा पाते थे, यहाँ पढ़ने आते थे। बच्चों की संख्या चालीस-पैंतालिस के आस-पास पहुँच गई थी। बसंत पंचमी से पढ़ाई शुरू हुई थी। किंतु भादो के आते ही गाँव में जो बाढ़ आई थी, तो लगातार तीन-तीन बार आती ही रह गई थी और सब कुछ बहाकर ले गई थी–पढ़ाई भी।
गाँव में पढ़े-लिखे लोगों का घोर संकट था। मार्ग-दर्शन भी कौन करता? एक शिक्षक के सुझाव पर तभी मैट्रिक के प्राप्तांक पर प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में मैंने आवेदन कर दिया था। मेरा नामांकन हो गया था–शिवहर कॉलेज में। पास के गाँव के एक भूमिहार परिवार के यहाँ रहने-खाने की व्यवस्था भी हो गई थी। बदले में उनके बच्चों को पढ़ा दिया करता था। कम-से-कम इतनी उम्मीद तो बन ही गई थी कि देर-सवेर शिक्षक की नौकरी मिल जाएगी। पर इसकी क्या गारंटी है कि बी.ए. करने के बाद कल जॉब पा ही लूँ। सोचा था, किसी तरह दो साल बिता लिया जाए, पर कोर्स पूरा कहाँ कर सका। बी.ए. का रिजल्ट निकला तो पास कर गया था–प्रतिष्ठा के साथ। सेकेंड डिवीजन ही आया था पर नागमणि का जो जमाना था। मैंने ट्रेनिंग छोड़ दी और एल.एस. कॉलेज, मुजफ्फरपुर में एम.ए. में अपना नामांकन करा लिया। वहीं एक छोटा-सा डेरा ले लिया था। सुबह-शाम बच्चों को पढ़ाता था, खर्चा निकल आता था। सोचा, इस तरह एम.ए. तो कर ही लूँगा, फिर देखा जाएगा। इतनी बड़ी दुनिया में कहीं-न-कहीं छोटी-मोटी नौकरी तो मिल ही जाएगी।
एक दिन पिता जी मुजफ्फरपुर आ धमके थे। एक तो इन्होंने पढ़ाई की जगह नौकरी कर लेने का सुझाव दिया था, दूसरे मेरी शादी का प्रस्ताव लेकर आए थे, लड़की का फोटो भी। वह लड़की देखकर आए थे और लड़की उन्हें और माँ को पसंद थी। वही लड़की थी जिसे मैंने भी देखा था और वह मुझे भी पसंद थी। हालाँकि मैं एम.ए. करने और नौकरी लग जाने के बाद ही शादी करने के पक्ष में था। पर विधना का विधान…। 6 जनवरी 1975 को डाक-तार विभाग में नौकरी लग गई। इससे पहले ही 16-08-1972 को शादी भी हो गई थी। धर्मशीला मेरी धर्मपत्नी बनकर मेरे घर आ भी गई। पर एम.ए. की पढ़ाई जरूर छूट गई। एम.ए. तो मैंने नौकरी ज्वाइन करने के बाद राँची विश्वविद्यालय से किया था।
अब तक खेत सब गिरवी पड़ गए थे, कुछ बिके भी थे। माँ के सारे गहने बिक गए थे। यहाँ तक कि घर के फूल के लोटा, थाली, कटोरा, गिलास आदि भी निकल गए थे। सूद पर तो पैसे थे ही जिसमें दिनों-दिन बढ़ोत्तरी होती जा रही थी जिसके लिए माँ-पिता जी को जलील भी होना पड़ रहा था।… ये सब बातें जब माँ सुनाती थीं, तो वह रोने लगती थीं। तब मेरी भी आँखें भर आती थीं। तब पत्नी समझाती–‘अब आप क्यों चिंता करते हैं? नौकरी तो लग ही गई है। धीरे-धीरे सब ठीक हो जाएगा।’ गौने आने के बाद से उसने इस घर में केवल दुःख ही देखा था, उसे झेला था, ओढ़ा-बिछाया था। लेकिन जब मैं घर से निकलने लगा था तो एक बार भी वह नहीं बोली थी कि थोड़े दिन के लिए ही नौकरी पर उसे भी साथ ले लूँ…। मैंने नौकरी ज्वाइन कर ली थी। घर वालों के सूखे-उजार जीवन में जैसे बहार आ गया हो या डूबती नाव को तिनके का सहारा मिल गया हो। किरानी की नौकरी, पगार ही कितना था–कुल जमा तीन सौ बीस के लगभग। मैंने सुबह-शाम के लिए ट्यूशन खोज लिया था। हर माह नब्बे रुपये उधर से भी आ जाते थे। ऑफिस में कुछ ओवर टाईम भी। राँची का खर्च चल जाता था। बचे पैसे हर माह घर भेज देता था, पर वहाँ की खाई तो बहुत गहरी थी।
सृजन के पथ पर : मैं विज्ञान का छात्र था, किंतु साहित्य के प्रति मेरी गहरी रुचि थी। जबकि वही दूर हो गया था। वह तो मुझे मिला एम.ए. में और फिर पीएच.डी. करते समय। प्रेमचंद, रेणु, चतुरसेन शास्त्री, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विजयदान देथा, तारा शंकर बंद्योपाध्याय, शरत् चन्द्र, चेखव, टॉलस्टाय, गोर्की आदि मेरे प्रिय लेखक हैं। ‘गोदान’, ‘मैला आँचल’, ‘वाणभट्ट की आत्मकथा’, ‘सद्गति’, ‘मुबारक बीमारी’, ‘गमी’ (प्रेमचंद), ‘उसने कहा था’ (गुलेरी), ‘विराम चिह्न’, ‘गुंडा’ (प्रसाद), ‘कहीं धूप कहीं छाया’ (बेनीपुरी), ‘माता का आँचल’ (शिवपूजन सहाय), ‘इनसान का जन्म’ (राधा कृष्ण), ‘दुविधा’ (देथा), ‘घाट बाबू’ (विमल मित्र) आदि कहानियाँ मेरे लिए आज भी महत्त्वपूर्ण हैं।
मुझ पर ‘रामायण’ और ‘महाभारत’ का विशेष प्रभाव है। राम और कृष्ण ने भगवान होते हुए भी गुरु के आश्रम में जाकर शिक्षा ग्रहण की थी और हर तरह से निपुणता प्राप्त करने के बाद ही गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया था। इसलिए इतना कुछ होने पर भी मैंने अपने को साहित्य से अलग नहीं किया था। साहित्य और इतिहास आज भी मेरे प्रिय विषय हैं। विभागीय पुस्तकालय का प्रभारी मैं ही था और हर वर्ष दस हजार के फंड का उपभोग पुस्तकों की खरीद में मैं कर लेता था। मन पसंद पुस्तकें हर वर्ष पुस्तकालय में आ जाती थीं। राँची में एक बहुत ही समृद्ध पुस्तकालय है–राज्य पुस्तकालय। मैंने अपने को उससे जोड़ रखा था। पत्र-पत्रिकाएँ तो मिल ही जाती थीं।
मेरी पहली कहानी 1981 में आई थी। एक साथ दो कहानियाँ। ‘दशकारम्भ’ (कनौज) में, ‘सुबह के इंतजार में’ तथा ‘ज्योत्स्ना’ (पटना) में ‘रवानगी’। पीएच.डी. की अब तक मेरा शोध प्रबंध भी पूरा हो गया था और उपाधि भी मिल गई थी। फिर तो कहानी-लेखन का जो क्रम चला तो मैंने उसे रुकने नहीं दिया। हाँ, मोटे उपन्यास पर काम करने से उसकी गति अवश्य ही मंद पड़ जाती है जो स्वाभाविक भी है। फिर भी अब तक मेरी डेढ़ सौ से ऊपर कहानियाँ छप चुकी हैं…।
31 मार्च 2012 को भारत संचार निगम लिमिटेड, झारखंड के परिमंडल कार्यालय से सहायक निदेशक के पद से सेवानिवृत्त भी हो चुका हूँ। संभव है, समयाभाव के कारण जो कार्य अब तक नहीं हो सका था, अब पूरा हो जाए। पर इस मुकाम पर पहुँचने के बाद अफसोस भी है कि जीवन का कीमती वक्त तो गुजर गया। छोटी-सी नौकरी जिसके लिए मैं लालायित था, मेरा परिवार लालायित था–सब कुछ निगल गई। अब जो बचा है, उसी को सहेज-समेट कर कुछ बेहतर कर लेना है।
‘वागर्थः’, ‘वर्तमान साहित्य’, ‘आजकल’, ‘कथाक्रम’, ‘नवनीत’, ‘नई धारा’, ‘दोआबा’, ‘पांडुलिपि’, ‘वैचारिकी संकलन’, ‘कथानक’, ‘कथाबिंब’, ‘पारखी’, ‘लामही’, ‘कल के लिए’, ‘परिकथा’, ‘जनसत्ता’, ‘हिन्दुस्तान’, ‘इस्पात भाषा-भारती’, ‘कुरुक्षेत्र’, ‘समाज कल्याण’, ‘पंजाब केसरी’, ‘साहिती सारिका’, ‘लोक गंगा’, ‘द संडे इंडियन’, ‘शुक्रवार’, ‘द पब्लिक एजेंडा’, ‘न्यूज इंडिया’, आदि-आदि कितनों के नाम गिनाएँ!
मैं अपने लिए आत्म-निर्णय का विशेष महत्त्व देता हूँ। अब इस मुकाम पर पहुँचकर तो और। मुझे लगता है, मेरा सबसे बड़ा मार्गदर्शक तो मेरे अंदर बैठा है।… मैं एक उदाहरण से इस आत्मार्पण को विराम देना चाहूँगा। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल की एक महत्त्वपूर्ण पुस्तक है ‘चिंतामणि’ जिसमें एक बढ़िया सा लेख है ‘सच्ची वीरता’। उस लेख में एक चित्रकार का जिक्र है जो अपने एक चित्र की दो प्रतियाँ तैयार करता है। एक दिन वह चित्रकार उस चित्र की एक प्रति को एक चौराहे पर टाँग देता है और उसमें एक नोट दे देता है कि ‘इस चित्र में पाठकों को जहाँ-जहाँ खामियाँ नजर आए, वे वहाँ-वहाँ चिह्न लगा दें।’ कहते हैं पूरा चित्र चिह्नों से भर गया था, लेकिन चित्रकार निराश नहीं हुआ। उसने चित्र की दूसरी प्रति उसी चौराहे पर लटका दी और इस बार नोट दिया–‘इस चित्र में दर्शकों को जहाँ-जहाँ खूबियाँ दिखाई दें, कृपया वहाँ-वहाँ चिह्न लगा दें।’ चित्रकार को तब और आश्चर्य हुआ, जब उसने देखा कि पूरा चित्र चिह्नों से भरा है। मैंने संक्षेप में अपने अब तक के जीवन का एक कच्चा चिट्ठा आप सब के समक्ष रख दिया है। यदि पाठक अपनी प्रतिक्रिया मुझे देने की कृपा करें तो सचमुच मुझे विशेष खुशी होगी। मेरे लेखन का सबसे बड़ा संबल पाठक ही तो होते हैं। कल भी थे, आज भी हैं और कल भी होंगे।