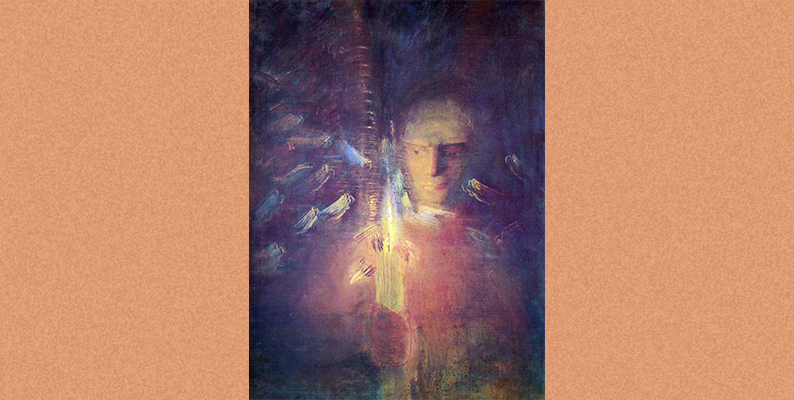मरै सो जीवै : दादू दयाल
शेयर करे close
शेयर करे close

शेयर करे close
- 1 February, 2022
मरै सो जीवै : दादू दयाल
भक्तिकाल हिंदी का स्वर्णकाल रहा है। यही समय था जब ईश्वर की सत्ता पर न केवल संदेह किया गया बल्कि उसे अस्वीकार कर दिया गया। इसी समय मनुष्यता और प्रेम की प्रतिष्ठा के लिए सबसे गंभीर प्रयास हुए। वर्ण और जाति व्यवस्था से आक्रांत इस समय में जाति, रंग और ऊँच-नीच के कारण होने वाले अत्याचार, शोषण और दमन के खिलाफ सर्वाधिक मुखर आवाज उठाई गई। अधिकांश संत कवि पिछड़ी जातियों से आए थे और उन्हें अपनी जातीय पहचान के उद्घोष से किंचित गुरेज नहीं था। कबीर खुद को जुलाहा, दादू धुनिया, सेन नाई और रैदास चमार कहने में कोई संकोच नहीं करते थे। दादू तो धुनिया के अलावा खुद को कई जगह कमीन कहने में भी संकोच नहीं करते। हिंदी साहित्य में भक्ति काल का समय भारी सामाजिक विषमता और उथल-पुथल का था। विगलित और जर्जर सामाजिक व्यवस्था में रचे-धँसे भेदभाव को इन कवियों ने जबरदस्त चुनौती दी। उस समय नीची जातियों के लोगों को पढ़ाई-लिखाई के अधिकार से वंचित रखा जाता था, इसलिए अक्सर इन सबको अनपढ़ कह देने की परंपरा-सी चल पड़ी। यह इस कारण भी हुआ क्योंकि इन कवियों ने अनुभव के आगे किताबी ज्ञान की सार्थकता को चुनौती दी। यह भी तथाकथित पढ़ी-लिखी जातियों खासकर पंडितों के खिलाफ एक तरह से उनका विद्रोह ही था। दादू के बारे में यह कहना अर्थपूर्ण नहीं होगा कि उनकी पढ़ाई-लिखाई नहीं हुई थी। भले ही इसके बहिर्साक्ष्य न हो, पर अनेक अंतर्साक्ष्य ऐसे हैं जो संकेत करते हैं कि संत परंपरा में दादू के लिए विधिवत विद्यार्जन की सुविधा जरूर संभव हुई थी। यह कहना बहुत समझदारी भरी बात नहीं है कि जो किसी स्कूल नहीं गया, उसकी पढ़ाई नहीं हुई।
दादू का जन्म 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में 1544 ई. में हुआ था। उस समय प्रायः समूचे उत्तर भारत में मुस्लिम शासकों का आधिपत्य था। कुछ स्वाधीनता प्रिय योद्धा यद्यपि हुकूमत के खिलाफ युद्ध कर रहे थे परंतु अधिकांश राजाओं, सामंतों ने लाभ-लोभ या दबाव में इस्लामी सत्ता की दासता स्वीकार कर ली थी। भारतीय समाज बहुत जर्जर अवस्था में था। आपस में ही ऊँच-नीच, जाति-पाँति या स्त्री-पुरुष के भेदभाव के कारण समाज में भारी विषमता व्याप्त थी। छोटी और नीच समझी जाने वाली जातियों पर तरह-तरह के अत्याचार हो रहे थे। उन्हें कोई आजादी नहीं थी। वह शक्तिशाली और ताकतवर लोगों की गुलामी के लिए मजबूर और अभिशप्त थे। उन्हें पढ़ने-लिखने की छूट नहीं थी। वह शास्त्रीय ग्रंथों के अध्ययन-मनन के अधिकार से वंचित थे। उन्हें मंदिरों तक में जाने की इजाजत नहीं थी। वे मनुष्य होकर भी मनुष्य की तरह जीने रहने की कल्पना नहीं कर सकते थे। स्त्रियों की दशा और भी दयनीय थी। वह भोग्या से ज्यादा कुछ नहीं थीं। ब्राह्मणों और मुल्लाओं की अपनी-अपनी दुनिया थी। अपने-अपने भगवान थे। अपनी-अपनी किताबें थीं और अपने-अपने सच। कोई किसी को सुनने या सहने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए आपस में राम और अल्लाह को लेकर द्वंद्व भी चलता रहता था, खून बहता रहता था। आक्रांताओं की हुकूमत होने से साधारण जन को अत्याचार एवं दमन का शिकार भी होना पड़ता था। ढोंगी और पाखंडी साधुओं, योगियों की जमात लोगों को झूठे बहकावे में फँसा कर मूड़ने में जुटी रहती थी। ऐसे प्रतिकूल सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य में दादू पले बढ़े। अहमदाबाद के गरीब निःसंतान दंपति लोदीराम नागर और वसीबाई ने उन्हें पाला। कहते हैं कि वे शिशु के रूप में साबरमती नदी के तट पर नागर दंपति को मिले और वहाँ से दोनों उन्हें घर ले आए। 11 वर्ष की उम्र में योगी बुड्ढन से उनकी पहली बार मुलाकात हुई और फिर 7 वर्ष बाद वे उन्हें दोबारा मिले और दादू को दीक्षा दी। अपने गुरु के बारे में उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं बताया है लेकिन दीक्षा के तुरंत बाद उन्हें काशी और पश्चिम बंगाल की यात्राओं पर चले जाने और वहाँ नाथपंथी योगियों के संपर्क में आने के प्रमाण मिलते हैं। अनुमान लगाया जाता है कि उनके गुरु बुड्ढन भी नाथ योगी संप्रदाय से जुड़े रहे होंगे और उन्हीं की प्रेरणा से दादू ने पूरब की यात्रा की होगी।
दादू को कबीर बहुत पसंद थे। वे कबीर के प्रबल प्रशंसक ही नहीं बल्कि उनके अनुवर्ती की तरह थे। उन्होंने कबीर के ही रास्ते पर चलने की ठानी, ‘जे थे कंत कबीर का सोई वर वरिहूँ।’ वे निःसंकोच कहते हैं कि उनका रास्ता वही है जो कबीर ने अपनाया। कबीर एक अक्खड़ सच्चे समाज सुधारक की तरह किसी को भी उसकी गलती पर लताड़ने में संकोच और डर नहीं दिखाते। वह बाहर जिस तीखे अंदाज में सामाजिक झूठ, पाखंड और भेदभाव को ललकारते हैं, भीतर बैठे राम को भी उतनी ही गहराई और आत्मीयता से पकड़ते हैं। ये वो राम नहीं हैं, जिनकी कुछ राजनीतिक दल जय-जयकार करते हैं, ये राम भीतर उनकी आत्मा ही है। पहले वे राम के पीछे भागते हैं फिर राम उनके पीछे। उनके निर्गुण राम और उनका निर्वैरी, निहकामता का सूत्र दादू को बहुत सुहाता है। वह कबीर की तरह हरदम लुकाठा हाथ में लिए तो नहीं फिरते पर जहाँ कड़वा सच कहना जरूरी हो जाता है, वहाँ चूकते भी नहीं। कटु बात भी वह इतनी सहजता से कह देते हैं कि सामने वाला घायल हो जाता है, बार-बार अपनी चोट सहलाता है और फिर इलाज के लिए लौटकर दादू के पास ही आ जाता है।
दादू किसी पंथ को नहीं मानते, न ही अपना पंथ बनाना चाहते हैं। वे कहते हैं, ‘भाई रे ऐसा पंथ हमारा, द्वैपखरहित पंथि गहि पूरा, अवरण एक अधारा।’ यह पंथ संप्रदाय का नहीं पथ का वाचक है। उनका रास्ता द्वैपखरहित है। इसे वे कई बार निपख भी कहते हैं। निपख यानी निष्पक्ष। दादू के समय में हिंदू-मुसलमान दोनों अपने-अपने रास्ते को सही कह कर आपस में लड़ते-झगड़ते रहते थे, इसीलिए दादू ने दोनों पक्षों से अलग रहने का निश्चय किया। उनके निपख होने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण था, वह था दोनों संप्रदायों की विचारमूढ़ता। कुछ किताबों में लिखी बातों को लेकर सांप्रदायिक दुराग्रह का परिणाम था हिंदू-मुस्लिम संघर्ष। वे इस बौद्धिक दुराग्रह से मुक्त होकर अनुभव के मार्ग पर बढ़ने की सलाह देते थे। उनका पंथ सबको स्वीकार करने को तैयार था, हिंदू हो या मुसलमान, ऊँच हो या नीच, अमीर हो या गरीब। किसी से कोई भेदभाव नहीं। इसीलिए उनके पास रज्जब, बखना और वाजिद जैसे मुस्लिम शिष्य थे तो जगन्नाथ और जगजीवन जैसे हिंदू भी। सामाजिक भेदभाव से त्रस्त नीच ‘कमीन’ जातियों के लिए भी उनके दरवाजे खुले रहते थे। इस तरह दादू ने एक सामाजिक क्रांति को जन्म दिया, सांप्रदायिक समरसता का मार्ग खोल दिया। दादू पर बहुत ज्यादा काम नहीं हुए हैं लेकिन उनके आध्यात्मिक दार्शनिक चिंतन की अनेक कोणों से समीक्षा हुई है। उनके निपख, द्वैपखरहित, मधि मारग को समझने समझाने की बहुत सारी कोशिशें हुई हैं। दादू पंथ के आचार्यों ने अपने ढंग से उन्हें महिमामंडित करने के प्रयास भी किए हैं और साहित्य के अध्येताओं और विद्वानों ने उनकी रचनाओं की प्रामाणिकता के परीक्षण के साथ ही उनके जीवन वृत्त के विश्वसनीय विस्तार को भी पकड़ने का प्रयास किया है। विदेशी विद्वानों ने भी दादू पर काम किया है लेकिन उनके प्रारंभिक अध्ययन निष्कर्षों में से अनेक अब अप्रासंगिक और निर्मूल साबित हो चुके हैं। डॉक्टर विल्सन और डॉक्टर ओर की कई स्थापनाएँ अधूरी सूचनाओं के आधार पर खड़ी होने के कारण ठुकराई जा चुकी हैं। आचार्य क्षितिमोहन सेन और परशुराम चतुर्वेदी ने यद्यपि बहुत विद्वत्तापूर्ण ढंग से दादू को समझने और उनकी रचनाओं के पाठ संपादन का काम किया है परंतु अब तमाम नई जानकारियों के परिप्रेक्ष्य में दादू के व्यक्तित्व को नए सिरे से समझने की आवश्यकता महसूस होने लगी है। संत साहित्य के विद्वान डॉक्टर गोविंद रजनीश द्वारा दो खंडों में ‘दादू समग्र’ के प्रकाशन के बाद दादू के व्यक्तित्व के अनेक ऐसे पहलुओं को नए सिरे से समझने की जरूरत महसूस की गई जो अभी तक प्रायः अज्ञात थे। रज्जब अपनी ‘सर्वंगी’ में दादू, कबीर, नामदेव और रैदास को ‘महामुनि’ कहते हैं अपने गुरु दादू को वे ‘जोग्येंद्र महामुनि’ कहते हैं। अब तक इस तथ्य के लिए तर्कों का प्रायः अभाव था कि आखिर एक सहज मार्गी साधु को उसके प्रिय शिष्य ने ‘जोगेंद्र’ क्यों कहाँ। यद्यपि दादू की रचनाओं में योग मार्ग की साधना और तद्विषयक सामग्री छिटपुट मिलती है, वह योग साधना के अनुभव की भी चर्चा करते हैं, इडा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ियों, प्राणरोध, ब्रह्मरंध्र की यात्रा, उन्मन स्थिति, पवन पथ और गगन मंडल में कोटि सूर्य के प्रकाश की बात भी करते हैं परंतु इससे कहीं ज्यादा मधि मारग, सहज साधन और प्रेम भक्ति की बात करते हैं।
कुछ साखियों या पदों को पढ़कर दादू के व्यक्तित्व के बारे में कोई राय नहीं बनाई जा सकती। वह अधूरी और भ्रांतिपूर्ण लगेगी। टुकड़ों टुकड़ों में भी वे अलग-अलग दिखाई पड़ते हैं। कहीं समग्र रूप से ईश्वरार्पित भक्तों की तरह जहाँ अगाध आस्था, समर्पण और सुमिरन के अलावा कोई और रास्ता नहीं है, जहाँ सारा खलक खुदा के खेल की तरह है और हर जीव उस खेल में एक पात्र के अलावा कुछ और नहीं। सबको राम नचा रहे हैं। उस महानट के सामने समर्पण के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। एक बार उसकी मर्जी पर छोड़ दिया तो मन खुद से निर्मल हो जाएगा, माया नष्ट हो जाएगी, ‘ब्रह्म भगति मन उपजे, तब माया भगति बिलाई। दादू निर्मल मल गया, ज्यूँ रवि तिमिर नसाई।’ कहीं विरहाकुल तड़पते प्रेमी की तरह पीड़ को आहत होकर पुकारते हुए उससे दर्शन देने की याचना करते हुए, उसकी राह देखते हुए, उसके बिना जल से बाहर कर दी गई आहत मछली की तरह, मिलन की कामना में लीन। असहनीय वियोग की मरण पीड़ा से गुजरते हुए। प्रेम में पागल तन-मन की सुधि से भी विच्छिन्न। जब सारा जग सोता है तो विरहिणी जागती और रोती है। लोक और वेद ने जो मार्ग बताए हैं, वह याद नहीं रहे। नख शिख प्रिय के विचारों की आग में जल रहा है। केवल इस उम्मीद में साँस अटकी है कि शायद कभी परम पीड़ की नजर इधर उठ जाए, ‘राम विरहिणी ह्वै रहा, विरहिणी बन गई राम। दादू बिरहा बापूरा, ऐसे कर गया काम।’ कहीं निपख मधि मार्गी की तरह दिखते हैं, इसे ही अपना सहज पथ बताते हैं। ईश्वर सब जगह है, तुम्हारे भीतर भी बाहर भी। बस यही जान लेना है। ज्यूँ का त्यूँ देखने की आदत डाल लेनी है, ‘दादू द्वैपख रहता सहज सो, सुख-दु:ख एक समान। मरे न जीवे सहज सो पूरा पद निर्वाण।’ द्वंद्वों से मुक्त होकर जो सुख और दु:ख में एक समान रहता है, समरस रहता है, वह अपने आप में स्थित रहता है। वह न जीता है, न मरता है, यही मुक्ति की स्थिति है, यही निर्वाण का पद है, यही मध्य मार्ग है। न हमें द्वंद्वों को छोड़ना है, न उन्हें पकड़ना है, न सुख मानना है, न दु:ख। खुद का कोई नाम नहीं, न किसी को साथ लेना है, न किसी के साथ जाना है, ‘मधि भाई रोवै सदा दादू मुक्ति दुआर।’ कहीं-कहीं दादू अद्वैत की महिमा गाने लगते हैं। ‘एक ही एके भया अनंद, एक ही एके भागे दंद। एक ही एके एक समान, एक ही एके पद निर्वाण।’ जरूरी है कि दादू को उनकी समग्रता में समझने की कोशिश की जाए। केवल तभी दादू की विराट दृष्टि और चेतना को समझा जा सकेगा।
गोविंद रजनीश द्वारा संपादित ‘दादू समग्र’ के दो खंडों में आने के बाद दादू के व्यक्तित्व के कुछ अब तक अज्ञात पक्षों पर रोशनी पड़ी है। खंड एक में ‘आदि बोध सिद्धांत ग्रंथ’ नामक दादू की एक लंबी रचना संकलित की गई है जो स्वयं दादू के शिष्य रज्जब द्वारा तैयार की गई एक प्राचीन पांडुलिपि के आधार पर संपादित की गई है। रजनीश लिखते हैं, ‘यह अकारण नहीं है कि रज्जब ने सर्वंगी में दादू के तत्कालीन लोक प्रचलित मूल नाम दादू जोगेंद्र का प्रयोग करते हुए उनकी योग साधना को उत्तम कोटि की मानकर उन्हें महामुनि की संज्ञा दी है। आदिबोध सिद्धांत ग्रंथ हठयोग का मूलभूत प्रतीकात्मक ग्रंथ है। इसमें हठ योग साधना के इतने प्रतीकों और क्रियात्मक साधनों का उल्लेख है कि उतने गोरखनाथ से गोपीनाथ और भरथरी तक नाथ परंपरा के किसी रचनाकार ने नहीं दिये। गोरखनाथ ने स्वयं को जोगेश्वर की संज्ञा दी तो दादू ने अपने को अवधूत जोगेंद्र की।’ इससे यह तथ्य सामने आता है कि गुरु उपदेशक बनने से पूर्व वह हठ साधना के कट्टर समर्थक और किसी नाथपंथी जोगी या साधु के शिष्य रहे होंगे। जैसे-जैसे निर्गुण मार्गी विविध साधकों से उनका संसर्ग बढ़ता गया होगा, वैसे-वैसे उनका चिंतन व्यापक और सघन होता गया होगा। यही कारण है कि नामदेव और कबीर की तरह उनके निर्गुण भाव साधना की मौलिकता के साथ परवर्ती रचनाओं में हठ योग साधना की पद्धति व प्रतीकात्मक शब्दावली प्रचुर मात्रा में अपना स्थान बनाए हुए दिखाई पड़ती है। आदिबोध सिद्धांत ग्रंथ को अगर उनकी प्रारंभिक रचना मान लिया जाए तो एक सहज प्रेम मार्गी संत के रूप में उनके व्यक्तित्व और चिंतन के उत्तरोत्तर विकास को समझा जा सकता है। योग चित्त शुद्धि का मार्ग है। गोरखनाथ एक संपूर्ण योगी थे। उन्होंने लगातार चित्त शुद्धि और कायापलट पर जोर दिया। उनकी धारणा थी कि कठिन योग साधना और प्राण रोध से चित्त निर्मल हो जाता है और निर्मल चित्त में आत्मा प्रतिबिंबित होने लगती है। निश्चित रूप से दादू ने इसी मार्ग का प्रारंभ में अनुसरण किया होगा। आदिबोध में वे केवल गोरखनाथ और उनकी परंपरा के श्रेष्ठ नाथ सिद्धों का ही उल्लेख नहीं करते हैं बल्कि गोपीनाथ, चरपटनाथ, मछंदरनाथ, भरथरी के साथ ही कपिल, पार्श्वनाथ, नेमिनाथ, रैदास, कबीर, धन्ना, पीपा, नामदेव आदि पूर्ववर्ती संतों सिद्धों का नाम भी लेते हैं। उनका मानना है कि यह सभी योग विद्या में पारंगत थे और इसी माध्यम से उच्च कोटि के संत बने थे। दादू का यह आदिबोध नाथ परंपरा से प्रभावित था। नाथ सिद्धों ने भी योग का उत्स आदिनाथ से माना है, जिनको कई जगह शंकर के नाम से वर्णित किया गया है। यह शंकर कोई योग गुरु रहे होंगे। दादू मानते हैं कि आदिबोध की ज्ञान योग परंपरा भी शंकर से ही आरंभ हुई होगी। दादू नामदेव का बार-बार नाम लेते हैं। असल में नामदेव भी उसी आदि ज्ञान परंपरा में शामिल दिखते हैं। उन्होंने नाथ योगी बिसोबा खेचर से दीक्षा ली थी। नामदेव का जिन ज्ञानदेव से अंतरंग और अभिन्न संबंध था, वे तो खुलकर अपनी गुरु परंपरा नाथ योगियों में बताते हैं। उनके अनुसार उनकी गुरु परंपरा इस प्रकार थी, आदिनाथ, मच्छिंद्रनाथ, गोरखनाथ, गैनीनाथ और निवृत्तिनाथ। नामदेव लंबे समय तक निवृत्तिनाथ और ज्ञानदेव के संपर्क में रहे। ज्ञानदेव के आग्रह पर ही वे उत्तर भारत की यात्रा पर भी आए। रज्जब ने अपने गुरु के साथ ही नामदेव, कबीर और रैदास को भी महामुनि की संज्ञा दी थी। इन तीनों का प्रभाव दादू पर स्पष्ट देखा जा सकता है। इस आदि ज्ञान की चर्चा ज्ञानेश्वर ने अपनी गीता की टीका में भी किया है। उनके अनुसार जिस आदि ज्ञान का उपदेश शंकर ने किया, वह समुद्र के किनारे रहने वाले मच्छिंद्रनाथ को भी प्राप्त हुआ और उन्होंने यह विद्या गोरखनाथ को दी। इसी के बल पर गोरख योगेश्वर के पद पर अभिषिक्त हुए। दादू को आदि ज्ञान अपनी पूरब की यात्रा के दौरान नाथ योगियों के संपर्क में आने से प्राप्त हुआ और इस साधना से ज्ञान प्राप्त कर उन्होंने स्वयं को अवधूत जोगेंद्र घोषित किया।
परवर्ती रचनाओं में योग विषयक जो भी चर्चा दादू करते हैं, उसका मूल इसी आदि बोध सिद्धांत ग्रंथ में है। उनके उत्तरवर्ती विराट सहज और निपट प्रेम पूरित व्यक्तित्व का आधार भी इसी में है। अपने साखियों और पदों में दरअसल उन्होंने इसी ज्ञान को प्रेम रस में भिगोकर व्यक्त करने का प्रयास किया है। लगता है कि उन्होंने प्रारंभ में कठोर योग साधना की, इंद्रिय नियमन, संयमित आहार विहार, कंचन-कामिनी से दूर रहकर निरंतर ब्रह्म का ध्यान, वज्रासन में बैठकर अंदर के मल को नष्ट करना, षट्चक्र भेदकर सुरति को ब्रह्मरंध्र तक ले जाना, शिवत्व की स्थिति को प्राप्त करना और इस प्रकार काल को भी जीतकर महायोग पाना कोई आसान काम नहीं है। यह सब दादू ने कर लिया और इस तरह उन्होंने अपना तन-मन निर्मल कर लिया। कहते हैं, इस तरह वे कर्म बंधन से छूट गए और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया। योग के माध्यम से आत्मसाक्षात्कार के इसी आदि बोध का विकास बाद में उनके निरंतर चिंतन के साथ हुआ। असल में यह कठिन योग कर्म, आत्मसाक्षात्कार और मुक्ति और कुछ नहीं, दादू का निजता त्यागकर सार्वजनीनता में प्रवेश करना था ताकि वे सारे जगत के लिए अपनी सेवाएँ दे सकें। यही शरीर के भीतर अखंड सत्ता का बोध है, जीवन के अस्तित्व का बोध है। वैराग्य के प्रति अनन्य समर्पण ने उनके अंदर भक्ति और प्रेम का संचार किया। भक्ति एक निर्गुण, अजर, अलेख की, जो निरावलंब होकर भी सबका अवलंबन है। यह और कुछ नहीं स्वयं पर अगाध विश्वास की परिणति है। यही से वे गोरखनाथ के समकक्ष आकर खड़े हो गए। लेकिन उन्होंने गोरख की कठोर और शुष्क साधना को प्रेम रस से सींच कर जीव जगत के लिए और सुगम पथ खोज निकाला।
दादू योग से चलकर प्रेम भक्ति के मार्ग पर पहुँच जाते हैं। योग में क्षणिक मिलन है भक्ति में निरंतर मिलन है। ‘दादू पहली आगम विरह का, पीछे प्रीति प्रकाश। प्रेम मगन लेलीन मन, जहाँ मिलन की आस।’ यह विरह प्रेम साधना में बहुत महत्त्वपूर्ण है, रोना तड़पना, तन मन की सुधि ही भुला कर पुकारना, ‘दादू विरह जगावे दर्द को, दर्द जगावे जीव, जीव जगावे प्रीती को, पंच पुकारे पीव।’ और जब पी भीतर प्रकट हो जाता है तो बस पी के प्रति प्रीति रह जाती है। यही सहज योग है। निरंतर आत्मा में स्थित रहना। दादू अपनी यात्रा में निरंतर मनन और शोधन को महत्त्व देते हैं। स्वयं की यात्रा में वह कुरान, पुरान, वेद, उपनिषद के ज्ञान का खंडन करते हैं पर यों ही नहीं शोधन के बाद, ‘चतुर वेद्या मिथ्या, सस्त्र सार कथा, अष्टादश पुराण, मध्य घृत सोधिया।’ क्या इस तरह के शोधन के लिए उचित शिक्षा-दीक्षा की आवश्यकता है या कोई अनपढ़ यह काम कर सकता है? दादू की शिक्षा-दीक्षा के बारे में विद्वानों में मतभेद है। आचार्य क्षिति मोहन सेन उन्हें अनपढ़ मानते हैं, परशुराम चतुर्वेदी भी इस बारे में प्रायः अनाश्वस्त दिखते हैं। दादू 18 से 24 साल तक पूरबी जनपदों में घूमते रहे लेकिन इस काल में वह कहाँ-कहाँ रहे, क्या-क्या किया, इस बारे में बहुत कम जानकारी है। यही समय शिक्षा-दीक्षा के लिए सर्वोत्तम समय होता है। गोविंद रजनीश दादू को अशिक्षित और अनपढ़ बताने वाले विद्वानों से असहमति जताते हैं, ‘जो लोग संतों को अशिक्षित मानकर उनकी स्वानुभूति पर जोर देते रहे हैं उनसे विशेषकर दादू के संदर्भ में सहमत नहीं हुआ जा सकता है। दादू ने व्यवस्थित रूप से शिक्षा पाई या नहीं, तथ्यों और साक्ष्यों के अभाव में निर्णयात्मक रूप से कुछ भी कहना कठिन है परंतु कबीर काव्य का तो उन्होंने गहराई से अध्ययन किया था।’ यदि दादू अनेक स्थानों पर पढ़ाई-लिखाई की जरूरत को खारिज करते हुए दिखाई पड़ते हैं, ‘पढ़े ना पावे परम गति’, ‘पढ़े न लाँघे पार’, ‘मसि कागद के आसरे क्यों छूटे संसार’, ‘केते पुस्तक पढ़ी मूये पंडित वेद पुराण’, ‘काजी कजा न जानही कागदि हाथ कतेब’ लेकिन यह सारी अभिव्यक्तियाँ इतना भर संकेत करती हैं कि बहुत किताबी ज्ञान से परमात्म तत्त्व को जानना संभव नहीं है। दादू जानते थे कि किताबों के ज्ञान के कारण ही हिंदू मुसलमान झगड़ते रहे हैं, इसीलिए वे अनुभव के ज्ञान के हिमायती थे। पढ़ने-लिखने से वाद-विवाद की परिस्थितियाँ बनती हैं और वाद-विवाद से आत्मा को जानना संभव नहीं होता। वह साधक थे, सच के समर्थक थे इसलिए यह कहना गलत होगा कि वेद पुराण और कुरान का खंडन उन्होंने उन्हें जाने बगैर ही कर दिया होगा। हालाँकि दादू का समय भी कमीन या नीची जातियों के लिए शिक्षा-दीक्षा के अनुकूल नहीं था! उन्हें वेद पुराण शास्त्र पढ़ने से वंचित रखा जाता था, लेकिन संत कवियों ने किसी भी बंदिश को स्वीकार नहीं किया। दादू ने स्वयं भी कहा है ‘ना मैं पंडित पढ़ि गुण जानो ना कुछ ज्ञान बिचार।’ इस तरह वे खुद को पंडितों की श्रेणी से अलग कर लेते हैं पर उनकी यह आत्म स्वीकृति किंचित विनम्रता का संदेश ज्यादा देती है क्योंकि अन्यत्र वे अपने को जोगी भी कहते हैं और साधक भी जो उनकी ‘जोग जुगति नाही कछु मेरे, ना मैं साधन जानो’, पंक्ति के विपरीत जान पड़ती है, जब वह कहते हैं कि ‘जैसा कंत कबीर का सो वर वरिहूँ, मनसा वाचा कर्मणा, मैं और न करिहूँ’ तो क्या कबीर को पढ़े गुने बगैर। आगे, ‘कबीर विचारा कहि गया, बहुत भाँति समझाई’, में बहुत भाँति समझाने की व्यंजना दादू के गहन अध्ययन की ओर संकेत करती है।
उनकी भाषा काव्य शैली के अध्ययन से इस बात को और बल मिलता है। छंद अलंकार बहु भाषा ज्ञान बिना पढ़े-लिखे चमत्कारिक अर्थ संपन्नता के साथ आखिर कैसे उनके काव्य में आ सकता है। दोहा, चौपाई, सोरठा, दोही, श्याम उल्लास, हरिपथ, गीता तथा छप्पय छंदों का उन्होंने एक सिद्ध कवि की तरह प्रयोग किया है। श्लोकी और फारसी बहरों का प्रयोग कोई ऐसा व्यक्ति कैसे कर सकता है जो इसका जानकार न हो। गुजराती, हिंदी, पंजाबी, राजस्थानी और उर्दू फारसी के शब्दों का बहुलता से प्रयोग उनकी बहु भाषा विज्ञता को दर्शाता है। काव्य के अलंकार गुण से वह पूरी तरह परिचित लगते हैं। वाक्यों, शब्दों, पंक्तियों की पुनरावृति से शब्दालंकार और नाद सौंदर्य का अद्भुत सृजन उनकी रचनाओं में दिखाई पड़ता है। पुनरुक्ति से भी वे सफलतापूर्वक सौंदर्य का सर्जन करते हैं। ‘आदि है अंत है, अंत है आदि है’, ‘रमन हवन हवन रमन’, ‘धर्म का कर्म का, कर्म का धर्म का’ जैसे प्रयोगों की उनके यहाँ भरमार है। छंद अलंकार और भाषा के यह असाधारण रूप अनायास इनकी रचनाओं में आ गए होंगे, यह स्वीकार करना सहज नहीं लगता। इससे लगता है कि भाषा और काव्य कला के विविध पक्षों पर उनका अधिकार था। निश्चित रूप से हमारे पास इस बात का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है कि दादू की विधिवत शिक्षा-दीक्षा हुई थी या नहीं, उन्होंने या उनके शिष्यों ने कहीं इस बारे में कोई संकेत नहीं किया है लेकिन उनकी रचनाओं में यहाँ वहाँ जो संकेत मिलते हैं उनसे यह धारणा बलवती होती है की उनकी पढ़ाई-लिखाई जरूर हुई थी। संभव है अपनी काशी यात्रा के दौरान वहीं रहकर उन्होंने विद्वानों के साहचर्य में शिक्षा पाई हो क्योंकि जब सुंदर दास की पढ़ाई की बात आती है तो दादू स्वयं उन्हें काशी भेजना पसंद करते हैं, इसलिए कि उन्हें पहले से ही मालूम था कि काशी विद्वानों और आचार्यों की नगरी है। यह कहना तर्कसंगत होगा कि उन्होंने वेद, पुराण, कुरान, उपनिषद सबका पारायण किया होगा और तभी वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे होंगे कि केवल इन्हें पढ़कर ज्ञान नहीं हो सकता, उसके लिए साधना का मार्ग अपनाना पड़ेगा।
दादू कबीर के साथ ही अपनी समूची पूर्व संत परंपरा से परिचित दिखाई पड़ते है। वे नामदेव, रैदास, धन्ना, पीपा, सेन सभी की चर्चा करते हैं। बहुत साधारण तरीके से नहीं असाधारण तरीके से। लगता है कि वे इन सब के साहित्य से पूर्णरूपेण परिचित हैं। नाथ संप्रदाय के सभी सिद्धों का आदर पूर्वक नाम लेते हैं, गोरखनाथ, मच्छिंद्रनाथ, गोपीचंद, भरथरी के हठयोग के अनुभव और चित्त शोधन, कायापलट के तौर तरीके भी उन्हें मालूम हैं। वे न केवल उनसे प्रभावित हैं बल्कि उनकी योग साधना में पारंगत भी। इस रास्ते पर वह बहुत दूर तक जाते हैं और जैसे गोरखनाथ स्वयं को जोगेश्वर कहते हैं, वैसे ही दादू स्वयं को अवधूत जोगेंद्र कहने में संकोच नहीं करते। ईसा मूसा से लेकर भारत की तमाम पुरा कथाएँ भी उन्हें अपनी बात कहने का माध्यम प्रदान करती है। वह ध्रुव, प्रहलाद, सनकादिक की तो चर्चा करते ही हैं, सांख्य के प्रणेता कपिल, पार्श्वनाथ, नेमिनाथ समेत 24 जैन तीर्थंकरों का भी उल्लेख करते हैं। उन्हें 84 सिद्धों के बारे में पता है। वे कुरान से चलकर चार वेद, 18 पुराण, स्मृति ग्रंथों, बावन उपनिषद् तक की बात करते हैं। उन्हें भारतीय दर्शन के सभी षट संप्रदायों का ज्ञान है। किसी भी एक व्यक्ति को साहित्य, इतिहास और दर्शन की इतनी जानकारी केवल सुनी सुनाई बातों से ही हो सकती है यह कहना अव्यावहारिक लगता है। बिना विधिवत पढ़ाई के बिना अध्ययन के यह संभव नहीं है। दादू पंडितों और पाखंडियों के विरोधी जान पड़ते हैं, वेद की भी आलोचना करते हैं और कुरान की भी। शायद उनके विरोध का असल मकसद उसकी अज्ञान की निर्धनता का प्रतिपादन करना है। लगभग सभी संत कवियों ने अनुभव के मार्ग में किताबी ज्ञान को बाधक बताया है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए दादू उस सीमा तक चले जाते हैं, जहाँ लगने लगता है कि वे पढ़ने-लिखने को भी व्यर्थ मानते हैं लेकिन उनकी रचनाओं में अनेक स्थानों पर अनेक अभिव्यक्तियाँ बताती हैं कि वे पढ़ाई-लिखाई के विरोधी नहीं थे। यह बातें केवल दादू का यह मंतव्य स्पष्ट करती हैं कि ढेर सारा पुस्तकीय ज्ञान एकत्र कर लेने से तत्त्वज्ञान नहीं हो सकता। वे जानते थे कि पढ़ने का एक अनिवार्य परिणाम है, वाद विवाद और इससे असली रास्ते से भटक जाने की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं।
आचार्य क्षितिमोहन सेन दादू को अनपढ़ कहते हैं वहीं यह भी स्वीकार करते हैं कि ‘सर्वंगी’ और ‘गुणगंजनामा’ दोनों संकलन उनके जीवनकाल में ही तैयार हो गए थे और दादू ने उन्हें सुन भी लिया था। यह तथ्य अगर सही है तो यह सेन की अपनी संकल्पना का खंडन कर देता है कि दादू की पढ़ाई-लिखाई नहीं हुई थी। दादू को अगर पढ़ाई-लिखाई से कोई दिक्कत होती या परेशानी होती तो वे अपने उपदेशों को संकलित कराने में इतनी दिलचस्पी क्यों लेते। सच तो यह है कि वे चाहते रहे होंगे कि उनकी रचनाएँ यथासंभव शुद्ध रूप में संकलित की जाए ताकि लोग पढ़ कर उनका लाभ उठा सकें। सबसे महत्त्वपूर्ण तथ्य जो ध्यान देने योग्य है वह यह है कि उचित शिक्षा-दीक्षा के लिए दादू ने स्वयं अपने शिष्य सुंदर दास को विद्या अध्ययन के लिए काशी भेजा था, रज्जब और जगजीवन 11 वर्ष के बालक सुंदर को वहाँ ले गए थे। यह दृष्टि किसी ऐसे व्यक्ति की नहीं हो सकती, जिसकी पढ़ाई-लिखाई में रुचि न हो। विद्या अध्ययन के महत्त्व को वही जान सकता है जो स्वयं विधिवत गुरुओं के सानिध्य में रहकर अध्ययन कर चुका हो। अगर साधना और स्वानुभूति जन्य ज्ञान में पढ़ने लिखने का कोई योगदान नहीं हो सकता है तो फिर सुंदर दास को काशी भेजकर उनका समय नष्ट करने कि दादू को क्या जरूरत थी। इतना ही नहीं दादू को अपने वे शिष्य विशेष प्रिय थे जो प्रतिभाशाली और पढ़े-लिखे थे। कौन नहीं जानता कि रज्जब दास, जगजीवन और जगन्नाथ पर दादू का अत्यधिक स्नेह था। वे तीनों ही पढ़े-लिखे थे। सर्वंगी और गुणगंजनामा इन्हीं के प्रयासों का परिणाम थीं। दादू की रचनाओं में जो अंतर साक्ष्य निहित हैं वह इस पर प्रबल संदेह के पर्याप्त आधार प्रदान करते हैं कि दादू अनपढ़ थे। स्पष्ट रूप से काव्य शिल्प से लेकर इतिहास शास्त्र और दर्शन विषयक उनकी जानकारी इस तर्क को मजबूत आधार प्रदान करती है कि दादू की गंभीर शिक्षा-दीक्षा जरूर हुई थी। यह विषय अध्ययन की और संभावनाएँ समेटे हुए हो सकता है।
Image : Medieval Ornament no. -1.-Conventional leaves and flowers from illuminated manuscript
Image Source : WikiArt
Artist :Owen Jones
Image in Public Domain