हिंदी का नया आख्यान साहित्य और मनोविश्लेषण
- 1 August, 1953
शेयर करे close
शेयर करे close
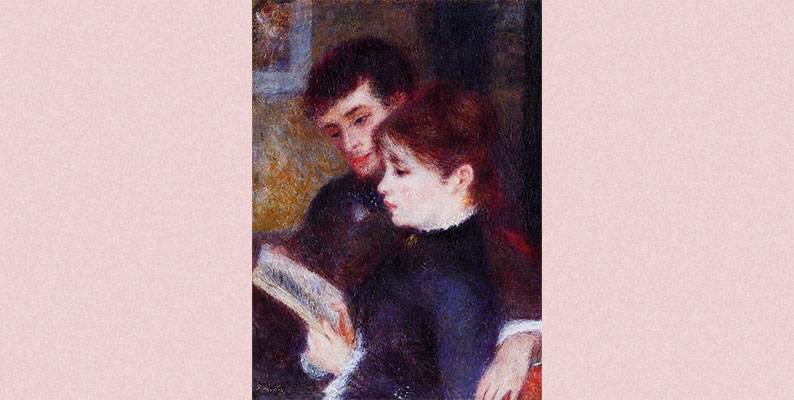
शेयर करे close
- 1 August, 1953
हिंदी का नया आख्यान साहित्य और मनोविश्लेषण
साहित्य और कला जीवन-वास्तव को मूर्त और वैविध्यपूर्ण ढंग से प्रतिबिंबित करती है। जीवन-वास्तव के अंतर्गत व्यक्ति का संपूर्ण अंतर्बाह्य जीवन आ जाता है। कला का यह सामान्य धर्म रहा है। आदिकाल से श्रेष्ठ कलाकार वस्तुन्मुखी रहे हैं, या कहें कि वस्तुन्मुखी कलाकार ही महानता प्राप्त कर सके हैं। उन्होंने समाज-वास्तव के साथ ही साथ अंगांगिरूप में मनुष्य के मनोवैज्ञानिक सत्य को भी प्रतिबिंबित किया है। आख्यान साहित्य में विशेष रूप से श्रेष्ठ कलाकारों ने अपने युग और समाज की इतिहास निर्दिष्ट केंद्रीय समस्याओं का कलात्मक उद्घाटन किया है और साथ ही उन समस्याओं से जूझने वाले पात्रों की विशिष्ट मानसिक प्रतिक्रयाओं का भी गहरा और मार्मिक चित्रण किया है। जीवन-वास्तव के ये दोनों पक्ष हैं। मानव-जीवन के इस संपूर्ण अंतर और बाह्य सत्य को प्रतिबिंबित कर के ही कोई रचना कलाकृति बनती है और मानव-जीवन में निहित संभावनाओं को उद्घाटित कर पाती है। सार्थक और सर्वजन-संवेद्य होती है। कला की इस यथार्थवादी परंपरा का सम्यक् विकास कर के ही डिकंस, हार्डी, बाल्जक, टॉल्स्टोय, तुर्गनेव, रवींद्रनाथ, शरत्, प्रेमचंद आदि कलाकारों की श्रेणी में आ सके हैं।
किंतु फ्रायड ने कला की इस परंपरागत यथार्थवादी परंपरा को उलट कर एक मनोवैज्ञानिक सौंदर्य सिद्धांत की स्थापना की। उसके अनुसार कला एक विक्षिप्त और विक्षुब्ध मानस की उपज है। कलाकार एक अभिशप्त व्यक्ति है जो प्रवृत्ति से ही अंतर्मुखी होता है। वह समाज में अपना सामंजस्य पाने में असमर्थ रहता है, इसलिए यथार्थ से पलायन करके वह अपने कल्पनालोक में शरण लेता है। वह यश, प्रभुता, धन और स्त्रियों का प्रेम पाना चाहता है, किंतु उसके पास साधन नहीं होते। साधारण विक्षिप्त तो इन काम्य वस्तुओं के दिवास्वप्न देखकर ही परितुष्ट हो रहता है, पर कलाकार का अंत:कोष इतना विपन्न और रिक्त नहीं होता। वह अपने दिवास्वप्नों को मूर्त अभिव्यक्ति देना जानता है। वह उनका उदात्तीकरण कर लेता है जिसके पीछे व्यक्ति स्वर छिप जाता है और ये दिवास्वप्न सबके लिए सुखदाई बन जाते हैं। फ्रायड के अनुसार कल्पना-जगत से पुन: यथार्थजगत की ओर लौटने का पथ ही कला है। कला जीवन-वास्तव को नहीं, बल्कि व्यक्ति के दिवा-स्वपनों को ही प्रतिबिंबित करती है। कलाकार में कुछ ऐसी रहस्यशक्ति होती है जो व्यक्ति मानस की इन प्रतिक्रियाओं को ऐसा आकर्षक रूप प्रदान कर देती है कि वे चाहे कितनी असामाजिक और अनैतिक क्यों न हों, उनमें सौंदर्य का गुण पैदा हो जाता है और उसके रसास्वादन से व्यक्तियों के अहं के बीच की दीवारें ढह जाती हैं। सब के अहं एक सामूहिक अहं के रूप में संहत हो जाते हैं, मानसिक तनाव ढीले पड़ जाते हैं और पाठकों या द्रष्टाओं को एक उच्चकोटि का सुख प्राप्त होता है। लेखक को अपनी जगह यश, प्रभुता, धन और स्त्री-प्रेम का लाभ हो जाता है। यह तो हुआ कला-सर्जन की प्रक्रिया का फ्रायडीय विश्लेषण।
किंतु इससे अधिक महत्त्वपूर्ण फ्रायड का मनोविश्लेषण का सिद्धांत है। वह व्यक्ति की चेतना के तीन स्तर स्वीकार करता है। पहला स्तर ‘इड’ (Id) का है जो हमारे व्यक्तित्व का निगूढ़ और अज्ञात जवी क्षेत्र है। यह नकारात्मक, अराजक, उच्छृंखल आवेगों का खौलता कुंड है। नियम, तर्क और विचार से शून्य, काल-देश की मर्यादाओं से अनभिज्ञ, अपरिवर्तनीय सत्यासत्य और पाप-पुण्य की नैतिक धारणाओं से उदासीन यह स्तर केवल आदिम शक्ति का चिरंतन स्रोत है। केवल ‘सुख सिद्धांत’ ही इसका निर्देशक है। दूसरा स्तर ‘अहं’ का है जो सुख-सिद्धांत को त्याग कर ‘यथार्थ’ सिद्धांत को अपनाता है। अर्थात् वह सामाजिक है। विचार, स्मृति और अनुभव की मध्यस्थता से वह संगठन, नियम, संयम आदि का परिपालन करता है और सत्य-असत्य का भेद करने में समर्थ है। तीसरा स्तर ‘सुपर-ईगो’ (Super-Ego) का है। सुपर-ईगो, आत्म-निरीक्षण, अंत:करण, नैतिक धारणाओं, सामाजिक आदर्शवाद एवं जीवन की उच्चतर अभिलाषाएँ लेकर पूर्णता की ओर उन्मुख व्यक्ति की चेष्टाओं का प्रतीक है। किंतु प्रत्येक व्यक्ति की चेतना सुपर-ईगो के आत्मत्यागी, समाजोन्मुखी धरातल तक ऊँची नहीं उठ पाती। क्योंकि चेतना का ऐसा उदात्त संस्कार तभी संभव है जब व्यक्ति पूर्ण-रूप से अपने सामाजिक जीवन में सामंजस्य पा जाए। प्राय: होता यह है कि बाल्यकाल की क्षुधा-काम की अन्य-वृत्तियाँ सामाजिक वर्जनाओं से कुंठित होकर व्यक्ति की चेतना के विकास को किसी मध्यस्तर पर ही जड़ीभूत कर देती हैं, जिससे ‘ओडापस कामप्लेक्स’ अर्थात पिता के प्रति शत्रुभाव; स्वरति अर्थात अपने शरीर के प्रति मोह या हीनभावना जैसी अनेक मानसिक विकृतियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। फ्रायड का मनोविश्लेषण-शास्त्र व्यक्ति की मानसिक विकृतियों के अध्ययन और निराकरण की एक मनोवैज्ञानिक चिकित्सा-प्रणाली है। इसकी वैज्ञानिकता के बारे में विद्वानों में गंभीर मतभेद है। जीवन की वास्तविकता केवल इतनी ही नहीं है। मानसिक दृष्टि से स्वस्थ और पूर्णत: विकसित व्यक्ति भी आज के वर्ग समाज में पूर्ण सामंजस्य पाने और अपनी क्षमताओं का विकास करने में असमर्थ हैं। वस्तुत: इस असामंजस्य की जड़ें अधिक गहरी हैं, और उनका मनोवैज्ञानिक निदान ही पर्याप्त नहीं है।
इस व्यापक तथ्य की अवहेलना करके अनेक उपन्यासकारों ने फ्रायडीय मनोविश्लेषण को ही ध्रुव सत्य मान लिया है। वे अपनी रचनाओं में वास्तविकता को प्रतिबिंबित न करके व्यक्तिमानस की वासनाजनित कुंठाओं को ही रूपायित करते हैं। एक प्रकार से ये रचनाएँ फ्रायडीय मनोविज्ञान के कथा-रूप में दृष्टांत उपस्थित करती हैं। उनमें ऐसे अभिशप्त पात्रों का चित्रण किया जाता है जो आत्मनिष्ठ, असामाजिक और अनैतिक हैं। इस प्रवृत्ति को तार्किक औचित्य प्रदान करने के लिए कहा जाता है कि कला के क्रमिक विकास की दृष्टि से नये उपन्यासों में वृत्त और चरित्र-चित्रण के स्थान पर लेखक का दृष्टिकोण ही अधिक महत्त्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि जीवन की जटिलता बढ़ गई है और विज्ञान की ईजादों और युद्धों की विभीषिकाओं ने जीवन के प्रति मनुष्य में अनास्था और अनिश्चितता की भावना भर दी है। नए आख्यानों में मानव-उद्योग और नियति का संघर्ष महत्त्वपूर्ण नहीं रहा, क्योंकि व्यक्ति का मानस ही एक परिस्थिति बन गया है जहाँ वासनाओं और विचारों का संघर्ष अविराम जारी है। व्यक्तिमानस का यह अंतर्द्वंद्व ही नए उपन्यासों की विषयवस्तु है। इसे चित्रित करने में ही कला की सार्थकता है। इसीलिए नए-नए उपन्यासों में प्रतिनिधि मानव-चरित्रों (टाइप्स) के स्थान पर विशिष्ट व्यक्तियों की विशिष्ट मानसिक प्रतिक्रियाओं का ही चित्रण होता है। पुराने ढंग के उपन्यासों में यदि समाज-विश्लेषण होता है तो आधुनिक उपन्यासों में व्यक्ति का मनोविश्लेषण होता है। यह नए-पुराने का भेद वस्तुत: कृत्रिम है और यह सारा तर्क फ्रायड के कल्पना-जन्य दिवास्वप्नों को प्रतिबिंबित करने वाले कला-सिद्धांत का ही रूपांतर मात्र है। इससे स्पष्ट है कि यदि जीवन-वास्तव को रूपायित करने का प्रश्न ही न रहे तो लेखक अनिवार्यत: रूप और टेकनीक के माध्यम से स्वयं अपने ही जीवन वृत्त को लेकर मनोविश्लेषण में प्रवृत्त होंगे और अपने प्रतिरूप पात्रों के प्रति मोहासक्त होकर उसके अहंकारी, दायित्वहीन, अनैतिक और स्वेच्छाचारी आचरण को उनकी अभिशप्त आत्मा का परिणाम सिद्ध करके उन्हें अतिरिक्त महिमा से मंडित करेंगे। हिंदी के नए आख्यान साहित्य में जहाँ मनोविश्लेषण है, वहाँ यह प्रवृत्ति भी है और आत्मचरितात्मक उपन्यासों की संख्या बढ़ती जा रही है।
‘शेखर : एक जीवनी’ इस परंपरा का पहला उपन्यास है। अज्ञेय ने शेखर को जन्मजात विद्रोही के रूप में चित्रित किया है। वह आरंभ से ही संस्थाओं के प्रति, स्वयं अपने व्यक्तित्व के प्रति विद्रोही है। वह ‘ऐतादृश्य’ मात्र का विरोधी है। उसकी विद्रोह-भावना को उदात्त जीवन दर्शन का आधार देने की चेष्टा की गई है। इस विद्रोह को निर्माण का पर्याय बताया गया है। किंतु यदि मनोविश्लेषण शास्त्र की दृष्टि से देखें तो शेखर एक ऐसा अभिशप्त व्यक्ति है जिसकी चेतना ‘इड’ (Id) और ‘अहं’ के स्तरों के बीच में ही कहीं जड़ीभूत हो गई है। ‘सुपर ईगो’ (Super-ego) का मानवीय विवेक तो उसे छू भी नहीं गया। इसीलिए अपने आचरण में वह इतना अनुदात्त, कृतघ्न, स्वार्थी, नृशंस और परपीड़क है। उसके जीवन मंी अनेक लड़कियाँ आती हैं, लेकिन समाज की नैतिक मर्यादाओं के कारण उसे अपनी काम-वृत्तियों का दमन करना पड़ता है। उसका आहत अहंकार इससे और भी उद्धत और असहिष्णु बनता जाता है। और जब उसकी मौसेरी बहन शशि उसके प्रति अपनी आसक्ति के कारण पति द्वारा परित्यक्त होकर उसकी शरण में आती है तो शेखर उसे अपनी सहानुभूति नहीं देता। वह शशि को अपनी अहंतृप्ति का साधन बनाता है। शशि अपना सब कुछ समर्पण करके भी शेखर से उपेक्षा और पीड़ा ही पाती है। फिर भी लेखक अपनी तटस्थता छोड़कर शेखर के नृशंस व्यवहार को भी औचित्य और सहानुभूति देता गया है। वस्तुत: यही शेखर अज्ञेय के दूसरे उपन्यास ‘नदी के द्वीप’ में भुवन के नाम से सामने आता है। भुवन क्रांतिकारी और विद्रोही नहीं है। वह एक वैज्ञानिक है। किंतु वह भी शेखर की ही तरह असामान्य प्रतिभा का अनुत्तरदायी और आत्मनिष्ठ नायक है। उसके संपर्क में आने वाले सभी उसे देवता मानकर अपनी श्रद्धा का नैवेद्य चढ़ाते हैं। वह जैसे पाने का ही अधिकारी है, बदले में देने का उत्तरदायित्व न उसे मान्य है और न कोई उससे इसकी आशा रखता है। रेखा और गौरा उसके प्रति समर्पित होती हैं और भुवन अपनी वासना-तृप्ति के लिए पहले रेखा, फिर उसे त्याग कर गौरा के प्रति समर्पित होता है। अपनी प्रेमिकाओं से प्रेम के स्वीकार या तिरस्कार के बीच भुवन ज्यों का त्यों बना रहता है, अंतरात्मा का उसमें विकास नहीं हुआ कि वह उसे कभी धिक्कारे। इस प्रकार हम देखते हैं कि इन उपन्यासों में भी पात्र एक विशेष साँचे मंह ढले-ढलाए ही सामने आते हैं। आदि से अंत तक वे इस साँचे का अतिक्रमण नहीं कर पाते। घटनाएँ और परिस्थितियाँ उनके चारित्रिक विकास में सहायक नहीं होतीं। वस्तुत: उनकी संयोजना इन साँचों के भीतर पात्रों की मानसिक प्रतिक्रियाओं का प्रकृत चित्रण करने की सुविधा प्रदान करने के लिए ही की गई है। किंतु जहाँ साँचों का प्रयोग हो वहाँ रचना में क्या सामाजिक सत्य और क्या मनोवैज्ञानिक सत्य, दोनों में से कोई भी प्रवेश नहीं पा सकता।
इलाचंद्र जोशी के उपन्यासों में भी कुंठाग्रस्त पात्रों के रुग्ण मानस को औचित्य प्रदान करके उनके जघन्य और असामाजिक कृत्यों को महिमा-मंडित करने का प्रयत्न है। ‘संन्यासी’, ‘पर्दे की रानी’ और ‘प्रेत और छाया’, आदि उपन्यासों में पाठकों को ऐसे ही पात्रों का चित्रण मिलता है। जोशी जी के पात्र हीन-भावना, मातृरति, स्वरति आदि मानसिक विकृतियों के शिकार होते हैं। इस अवस्था में वे नैतिक मर्यादाओं का उल्लंघन करके पूर्ण स्वच्छंदता से अपने पाशविक और हिंस्र रूप में समस्त मानवीय संबंधों को ठुकराते हुए केवल अपनी स्वार्थसिद्धि और भद्र और अभद्र नारियों के साथ काम तृप्ति करते फिरते हैं। उदाहरण के लिए ‘प्रेत और छाया’ का नायक पारसनाथ पिता के यह कहने पर कि वह उनका अवैध पुत्र है, विक्षिप्त हो उठता है। अपनी माँ के दुराचरण की बात जानकर वह समस्त स्त्री जाति के सतीत्व पर ही संदेह नहीं करने लगता, बल्कि अपने संपर्क में आने वाली प्रत्येक स्त्री का सतीत्व हरण करता फिरता है। इसमें उसे एक पाशविक आनंद आता है। किंतु अंत में उसे ज्यों ही पता चलता है कि पिता ने झूठ बोला था, और उसकी माँ तो साध्वी थी, त्यों ही वह आत्मग्लानि से भरकर एक वेश्या से विवाह कर लेता है, और सद्गृहस्थ बन जाता है। ऐसे मनोवैज्ञानिक तिलिस्म उनके अन्य उपन्यासों में भी मिलते हैं।
हिंदी के अन्य उपन्यासकारों में अज्ञेय और इलाचंद्र जोशी की तरह इतने सीधे ढंग से मनोविश्लेषण की प्रवृत्ति नहीं दिखाई देती। किंतु वैसे फ्रायडवादी न होते हुए भी फ्रायड के सिद्धांतों से न्यूनाधिक प्रभाव तो अनेक लेखकों ने ग्रहण किया है। इनमें से दो तरह के प्रभाव विशेष रूप से नए आख्यानों में लक्षित हुए हैं। कुछ लेखकों के मन में फ्रायड के मनोविश्लेषण शास्त्र ने यह धारणा बैठा दी है कि मनुष्य स्वभावत: स्वार्थी, क्षुद्र और अवसरवादी है। यह ऊँचे-ऊँचे आदर्शों और नैतिक मूल्यों का आडंबर केवल इस क्षुद्रता और स्वार्थपरता को छिपाने के लिए है। वस्तुत: सभी वर्गों के प्राणी इन आदर्शों की आड़ में अपने वर्गगत नहीं बल्कि व्यक्तिगत स्वार्थों की ही सिद्धि चाहते हैं। उनकी कृतियों में वर्तमान समाज की खोखली नैतिकता का पर्दाफाश तो होता है, किंतु साथ ही मनुष्य का सत्य, उसकी उच्चतर मानवीय विकास-संभावनाओं का सत्य भी छिप जाता है, और पढ़कर मन में एक अनास्था, विरक्ति और अनास्था की भावना पैदा होती है। भगवतीचरण वर्मा के उपन्यास ‘तीन वर्ष’, ‘टेढ़े-मेढ़े रास्ते’ और ‘आखिरी दाँव’ में, उपेंद्रनाथ अश्क के नवीनतम उपन्यास ‘गर्म राख’ में और एक सीमा तक डॉ. देवराज के उपन्यास ‘पथ की खोज’ में मनुष्य प्राय: इसी रूप में चित्रित हुआ है।
इनके अतिरिक्त कुछ लेखकों पर मनोविश्लेष शास्त्र का यह प्रभाव भी पड़ा है कि मानसिक आघात से जिस तरह व्यक्ति विक्षिप्त होकर पतित, हिंस्र और असामाजिक बन सकता है, उसी तरह यह भी संभव है कि उसका मानवीय विवेक जागृत हो जाए और वह चेतना के उदात्तीकरण द्वारा अपनी काम-वासनाओं को दबाकर देशभक्त और आत्मत्यागी बनकर निश्छल मन से जन-सेवा में लग जाए। यद्यपि काम-वासनाएँ अंतत: दबाई नहीं जा सकतीं, किसी न किसी रूप में उभर कर सामने आती रहती हैं, और व्यक्ति चाहे उन्हें पुन: दबा ले जाए, लेकिन निरंतर की आत्मपीड़ा से उसे मुक्ति कहाँ है, फिर भी उनको दबाकर उदात्त मानव बनना ही श्याघ्य है। उदयशंकर भट्ट के उपन्यास ‘नये मोड़’ का डॉ. शेफाली का आदर्श-चरित्र इस विचार-सूत्र के आधार पर ही निर्मित हुआ है।
अंत में नए आख्यानों में मनोविश्लेषण की प्रवृत्ति का मूल्य कूटने की यदि हम चेष्टा करें तो इस परिणाम पर पहुँचेंगे कि उससे चरित्र-चित्रण में यांत्रिकता और एकांगिता आ गई है। वस्तुत: यथातथ्यवाद का ही यह मनोवैज्ञानिक रूप है। यशपाल और जैनेंद्र जैसे समर्थ कलाकार आज भी अपने-अपने ढंग से जीवन-वास्तव को समग्र रूप में प्रतिबिंबित करने में सचेष्ट हैं। उनकी कृतियों में समाज-सत्य और व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक-सत्य को अंगांगिरूप में ग्रहण किया जाता है। किंतु मनोविश्लेषण की प्रवृत्ति समाज-सत्य का तिरस्कार करके केवल साँचों में ढले-ढलाए व्यक्ति पात्रों को ही चित्रित करती है, जिससे मनोवैज्ञानिक सत्य भी एकांगी और विकृत हो जाता है। और ये रचनाएँ सर्वजन संवेद्य कलाकृति की ऊँचाई नहीं छू पातीं। मानव-जीवन की पुनीतता और संभावनाओं की उपेक्षा करके कला अपने धर्म से च्युत ही हो सकती है।
Original Image: Reading Couple Edmond Renoir and Marguerite Legrand
Image Source: WikiArt
Artist: Pierre Auguste Renoir
Image in Public Domain
This is a Modified version of the Original Artwork

