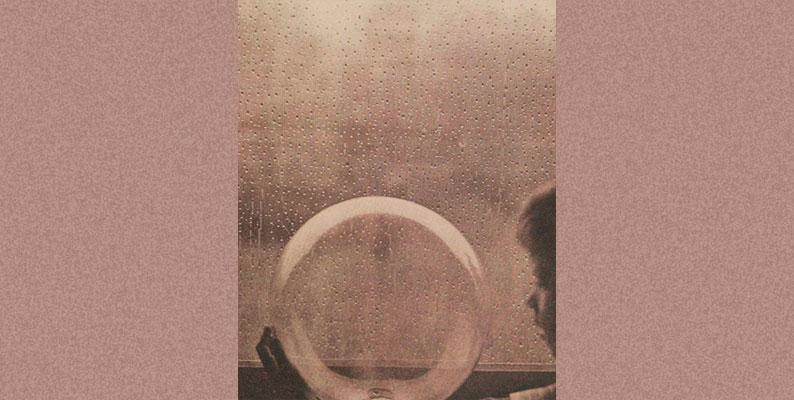रामदरश मिश्र–भारतीय ग्राम्य संस्कृति के कवि
- 1 August, 2020
शेयर करे close
शेयर करे close

शेयर करे close
- 1 August, 2020
रामदरश मिश्र–भारतीय ग्राम्य संस्कृति के कवि
रामदरश मिश्र ऐसी कविता के कवि हैं, जो हृदय का केवल गहरा स्पर्श न करे, बल्कि हृत्तंत्री को देर तक झनझना दे, विचारों को उद्बुद्ध कर दे, जगा दे, पाठक को सहभावन कराने के साथ-साथ स्थितियों का मूल्यांकन भी करा दे। उनकी सर्जकीय संवेदना में करुणा, विडंबना और मानवीयता को उद्घाटित करने की पक्षधरता है। वह सतही यथार्थ की जगह अर्थान्वेषी यथार्थ के सर्जक साहित्यकार हैं। साहित्य, समाज और जीवन से संयुक्त रहने के बावजूद वह साहित्य की शिविरद्वंद्वी से सर्वथा विलग रहे हैं। उनकी रचना में स्वदेश, समकाल और लोगों की गहरी पहचान और परख है। उनके लघु गीतों में कवि-दृष्टि का उन्मेष अपने शिखर पर है। उनके गीतों में कहन शैली की ऐसी बुनावट, भावानुभूति का ऐसा आत्मसातीकरण तथा उसके बीच संवादी सुरों की ऐसी सटीक सार्थकता अन्यत्र देखने को नहीं मिल पाती है। उनकी गीतात्मक प्रवृत्तियों में अनोखी बिंबोद्भावन की क्षमता है। अपने गीतों में वैयक्तिक राग और प्रकृति राग का वितान तानने वाले मिश्र जी गीत विधा की प्रकृति को जब सामाजिक, राजनीतिक विडंबनात्मक संत्रासों की निगूढ़ता देते है, तब वे युगचेता महान गीतकार बन जाते हैं। उनकी अभिधेयात्मकता व्यंजना में अंतरित हो जाती है। साहित्योद्यान की सभी विधियों में अपनी सर्जना के ऐसे सुमन खिलाने वाले मिश्र जी को ऐसी अनेकशः खूबियाँ उनके पाठकों को स्मरणीय हैं। वह गालिब, निराला और प्रसाद की तरह ‘गंजी नए मानी’ (कठिन भावबोध) के अनेकार्थों के कवि नहीं होकर भी अपनी कविताओं के सहजपन में सहज से असहज उद्गार तक की अर्थमूँजों को बड़ी सहजता से सहेज कर संपुटित कर देते हैं। यह सहजता उनके जीवन और सर्जन-दोनों का बीजतत्व है।
आज याद आता है कि रामदरश मिश्र का नाम उनकी कविताओं को पढ़ते-पढ़ते और उनसे प्रभावित होते-होते आज से 55 वर्ष पूर्व मेरे दिल-दिमाग पर छा चुका था। 1964 का वर्ष था। मैं नया-नया प्राध्यापक नियुक्त हुआ था। हिंदी की सभी साप्ताहिक, मासिक और त्रैमासिक पत्रिकाएँ नियमित रूप में खरीदता और पढ़ता था। उन दिनों कोई भी ऐसी प्रमुख पत्रिका नहीं थी, जिसमें रामदरश मिश्र नहीं छप रहे हों। उनके गीत और कविताएँ प्रायः छपती रहती थीं जो बार-बार पढ़े जाने के लिए मुझे आमंत्रित करती थीं और मेरे मन-मस्तिष्क में व्याप्त हो जाती थीं। गेयता, प्रभविष्णुता और काव्यलय से अर्थलय तक की मानसिक-यात्रा कराने की शक्ति-क्षमता उनकी कविताओं की विशेषता थी। ‘धर्मयुग’ हो या साप्ताहिक हिंदुस्तान’,‘कादम्बिनी’ हो या ‘ज्ञानोदय’, हर साप्ताहिक और मासिक पत्र-पत्रिका में अनेक छपी कविताओं के बीच उनकी कविता अपने को अन्य सबसे अलग गाती थी और पाठकों को खींचती थी। उस समय मुझे उनके कवि होने के अतिरिक्त इस बात की जानकारी नहीं थी कि रामदरश मिश्र अन्य किन-किन विधाओं में लेखन करते हैं और न ही यह जानकारी थी कि वे दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक हैं। पर कुछ समय बाद ही मुझे कथा-साहित्य के अनुशीलन से पता चला कि वे उपन्यासकार भी हैं और कहानीकार भी। मैं इस बात से ज्यादा प्रभावित था कि किस निर्बाध गति से वे अपना कविकर्म कर रहे हैं और कितना अधिक प्रकाशित हो रहे हैं। समय बीतता गया। फिर ‘पानी के प्राचीर’ उपन्यास को लेकर उनकी प्रसिद्धि हुई और वे ग्राम्य और आंचलिक कथाकार के रूप में माने जाने लगे। फिर उनकी दूसरी पुस्तक आई ‘जल टूटता हुआ’। ये दोनों नाम उनके उपन्यासों में भी उनकी काव्य-संवेदना को अभिव्यक्त करने वाले थे। मुझे लगा कि जल-तत्त्व है। यह उनकी कविता में भी देखने-गुनने को मिल जाता था। नदी, बाढ़ और बरसात से भरा है उनका साहित्य।
‘नदी
बड़े भोर सारस केंकारे
नदिया तीर बुलाए’
का आकर्षण देखें…।
उन्हीं दिनों मैं नई कहानी की प्रयोगधर्मिता पर अपना शोध-कार्य संपन्न कर रहा था। मैं उनकी कुछ कहानियों को लेना चाहता था, पर यह बात मेरी समझ से बाहर थी कि मैं नई कहानी आंदोलन से उन्हें किस तरह जोड़ूँ। उस समय मुझे पहली बार इस बात का भान हुआ कि रामदरश मिश्र एक ऐसे कथाकार हैं जो किसी आंदोलन या किसी वाद या शिविर के कथाकार नहीं हैं। वे एक ऐसे मुक्त कथाकार हैं, जिनके यहाँ परिवार, समाज, देश और युगबोध सभी मिल जाएँगे। पर किसी ठप्पे के तहत आप उनका विवेचन नहीं कर सकते। अतएव उनकी कहानियों से प्रभावित होने के बावजूद मैं उनका उपयोग अपने शोधकर्म में नहीं कर पाया। तभी मुझे यह भी पता चला कि प्रकृति के जल-तत्त्व के साथ बचपन और कैशोर्य की सघन स्मृतियों के कारण उनका गहरा आत्मीय लगाव है। पानी को देखने की दोनों दृष्टियाँ उनके पास थीं–पानी के उभार की और पानी के बिखराव की।
एक लंबा समय बीत गया। मैं अपनी अध्यापकीय वृत्ति में रमता गया। दैनिक कार्यभार इतना था कि उससे मुक्त नहीं हो पाता था। अनेक परिषदों के दायित्व भी मेरे साथ जुड़े थे। हाँ, जब-जब उनकी कोई औपन्यासिक नई कृति आती थी, तब-तब मैं उन्हें पढ़ता और रामदरश जी को सराहा करता था। पर बहुत चाहकर भी तब मैं न उनसे पत्र-सरोकार बना सका और न उन पर कुछ लिखने का अवसर ही निकाल सका। 1977 का साल था। मैं भागलपुर विश्वविद्यालय सेवा से गुरु नानकदेव विश्वविद्यालय के हिंदी-विभाग में रीडर बनकर आ गया था। तभी एक दिन उस वर्षांत में मेरे विभागीय प्रोफेसर और अध्यक्ष डॉ. रमेश कुन्तल मेघ ने अपने कमरे में बुलाकर मेरा उनसे परिचय कराया। मेरे सामने डॉ. रामदरश मिश्र थे, जो विभाग में किसी की मौखिकी संपन्न कराने आए थे। लंच का समय हो रहा था, सो मेघ जी डॉ. रामदरश मिश्र को अपने साथ अपने घर लंच कराने ले गए। इस पहली और छोटी-सी मुलाकात में मैंने पाया कि रामदरश जी शांत-संयत और हँसमुख थे। तब पाँच-छह वाक्यों में उनसे मेरी जो संक्षिप्त बातचीत हुई, उससे उनकी शालीनता और आत्मीयता का भी आभास हुआ।
रामदरश मिश्र जी से मेरी दूसरी मुलाकात इसके एक वर्ष बाद हुई। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला में एम.ए. की उत्तर-पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए कई विश्वविद्यालयों से लोगों को बुलाया गया था। उनके आमंत्रण पर मैं अमृतसर से पहली बार शिमला पहुँचा था और अतिथि-भवन में ठहरा था। वहीं मुझे रात में ‘डिनर’ के समय डॉ. रामदरश मिश्र जी सपत्नीक मिले। हमलोग ने साथ-साथ भोजन किया। जब हमलोग अपने-अपने कमरों में जाने के लिए पहली मंजिल की सीढ़ियाँ चढ़ने लगे तब मैंने उनसे सहज भाव से पूछा कि आप किस कमरे में हैं? उन्होंने अपने कमरे की जो संख्या बताई वह कमरा मेरे कमरे के बगल वाला कमरा निकला। अब हमलोग परस्पर पार्श्ववर्ती थे। दूसरे दिन नाश्ते के समय हमलोग ने साथ-साथ विश्वविद्यालय-कार्यालय जाने का कार्यक्रम बनाया, क्योंकि कार्यालय के निर्दिष्ट होने के बावजूद हमें यह पता नहीं था कि वह भवन कहाँ पर है और हमें किस तरह वहाँ पहुँचना है। विश्वविद्यालय का अतिथि-भवन पहाड़ की निचाई पर स्थित है और विश्वविद्यालय का वह कार्यालय उससे ऊँचाई पर। सो हमलोग अतिथि-भवन से नीचे उतरकर एक साथ ठीक दस बजे ढ़ालवे से चलते हुए ऊँचाई की ओर बढ़ने लगे। मैं मिश्र जी से सत्रह वर्ष छोटा हूँ। फिर भी हम दोनों की साँस चढ़ने लगी। हमने अपनी गति धीमी की और अगल-बगल की रमणीक वृक्ष-मालाओं को पीछे छोड़ते हुए धीरे-धीरे विश्वविद्यालय के केंद्रीय-भवन तक पहुँच गए। वहाँ अपने गंतव्य स्थल के बारे में जो भी मिला, उससे पूछताछ की। फिर सीढ़ियाँ चढ़ते हुए हम उस विशाल प्रशाल में पहुँच गए, जहाँ उत्तर-पुस्तिकाएँ जाँची जानी थीं। हमने अपना-अपना काम शुरू किया। बीच-बीच में चाय बिस्किट लेने का प्रबंध था। लंच के लिए हम पुनः लौट कर अतिथि-भवन गए और वहाँ से पुनः चढ़ाई चढ़कर उस विशाल प्रशाल में लौट आए। न जाने क्यों और कैसे उस दिन एक ही समय हम दोनों के मुँह से सहसा यह वाक्य निकला कि यह काम बड़ा उबाऊ है और हमें सात-आठ दिन यहाँ रहना है। कैसे चलेगा?
उससे अगले दिन संध्या समय हम दोनों ने शिमला के मॉल-रोड जाने का कार्यक्रम बनाया। हम चाह रहे थे कि हमें विश्वविद्यालय की गाड़ी की सुविधा मिल जाए पर यह संभव नहीं था, क्योंकि वहाँ बीसियों लोग भिन्न-भिन्न विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों से पधारे हुए थे। अतएव हमने संध्या समय बस से ही माल रोड जाने का कार्यक्रम बनाया। हम अतिथि-भवन लौटे तो भाभी जी तैयार बैठी थीं। हमलोग ने डायनिंग हॉल में आकर चाय बनवा कर पी। फिर धीरे-धीरे ऊँचाई चढ़ते हुए हम परिसर के पोस्ट-ऑफिस की बिल्डिंग के पास पहुँचे। वहीं पर बस-अड्डा था। हमलोग ने वहाँ से पहली छूटने वाली बस ली और उससे मॉल-रोड शिमला पहुँच गए। मॉल-रोड पर तो हमें पैदल ही चलना था, इसलिए हमलोग थोड़ा-बहुत ही चले-फिरे। फिर उस ऊँचाई से एक जगह नीचे की ओर उन्मुख हुए, क्योंकि नीचे बाजार था और भाभी जी को कुछ घरेलू उपयोगी चीजें तथा शॉल आदि की खरीद करनी थी। इस खरीदारी के क्रम में समय खिसकता गया और संध्या के सात बज गए। अँधेरा घिर आया था। हमलोग उस स्थान पर पहुँचे, जहाँ से बालूगंज होते हुए यूनिवर्सिटी तक मिनी बस जाती थी। पर वहाँ उस समय न कोई जाने वाली बस थी और न तत्काल उसके आने की कोई संभावना थी। हमें बताया गया कि जब गई हुई बस लौटकर आएगी, तभी यहाँ से जाना संभव हो सकेगा। ऊपर-नीचे करते हुए हम तीनों थक चुके थे। पर वहाँ नजदीक में बैठने की न कोई जगह थी और न कोई व्यवस्था ही। हमलोग रेलिंग पकड़कर नीचे की ओर देखने लगे। नीचे सारा शिमला शहर और उसका रेलवे स्टेशन बत्तियों से जगमगा रहा था। सुदूर नीचे स्थलीय अंतराल पर बल्ब दीये की तरह टिमटिमा रहे थे। हम तीनों ही पहाड़ की चढ़ाई और यातायात की कुव्यवस्था से बुरी तरह प्रभावित थे। हमारे दो दिनों के अनुभव का निचोड़ यह चिंता थी कि शिमला में हमारे सात-आठ दिन कैसे कटेंगे? मिश्र जी दिल्ली जैसे शहर से आए थे जहाँ मिनट-मिनट पर यातायात के साधन और वाहन उपलब्ध हैं। यद्यपि तब तक अमृतसर में रहते हुए मेरा साल भी पूरा नहीं हुआ था, पर मेरा अनुभव भी यही था कि वहाँ ऑटो और रिक्शे जी.टी. रोड पर हर पाँच-सात मिनट में सुलभ थे। पर हम तो कभी भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी रही उस शिमला में उपस्थित थे जहाँ यातायात का कष्ट हमें त्रासद प्रतीत हो रहा था। अंततः हम तीनों के मुँह से यही निकला कि हमलोग समतल मैदान के रहने वाले हैं, पहाड़ हम सबके लिए एक-दो दिन घूमने-फिरने के लिए तो ठीक है, पर यहाँ हमारे सात-आठ दिन कैसे कटेंगे? खैर! हमें कोई एक घंटे बाद एक मिनी बस मिली और हमलोग विश्वविद्यालय-परिसर में आ गए। फिर वहाँ से खरीदे हुए सामान को उठाया। कुछ ऊपर चढ़ते और नीचे ढालवें से उतरते हुए हम विश्वविद्यालय के अतिथि-भवन पहुँचे और वहाँ सीधे डाइनिंग रूम में आ धमके, क्योंकि हम में इतना धीरज शेष नहीं रह गया था कि हम सीधे ऊपर अपने-अपने कमरों में जाएँ और फिर वहाँ से फ्रेश होकर हम नीचे खाने की मेज तक आएँ। थकान ने हमारे धीरज का मानो चीरहरण कर डाला था। उस रात हमलोग खाकर सीधे अपने-अपने कमरे में गए और सो गए। फिर तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे और सातवें दिन विश्वविद्यालय-व्यवस्था का वहीं एकरस रूटीन कार्यक्रम रहा। बीच-बीच में इस एकरसता को भंग करने वाली कुछ इतर चर्चाएँ चलती रहीं। कुछ उत्तर-पुस्तिकाओं में अमान्य तौर पर लिखे हुए अंशों को एक-दूसरे के पास जाकर बाँचने-सुनाने और हँसने-हँसाने का प्रयत्न करने का कार्यक्रम चलता रहा।
शिमला में रहते हुए मिश्र जी और भाभी जी के साथ हमारी आत्मीयता बढ़ी। मिश्र जी की कविताओं को उनके मुख से सुनने के अवसर मिलते रहे। उस औपचारिक कार्यक्रम में एक अनौपचारिक आत्मीय भाव हमारे अपने-अपने कक्षों में परस्पर एक-दूसरे का स्वागत करने को सदैव तत्पर था। वहीं मुझे पता चला कि भाभी जी हिंदी की एम.ए. हैं और उन दिनों वह अपनी पीएच.डी. के लेखन में व्यस्त भी थीं। उनके रहने से हमारे बीच पारिवारिक बोध विकसित हुआ। हफ्ता पूरा होने पर हमलोग सात दिनों की दिहाड़ी और यात्रा-भत्ता का चेक लेकर अपने-अपने गंतव्य शहर लौट आए। इसके बाद हम दोनों के बीच आत्मीय और अकादमिक दोनों प्रकार के संबध प्रगाढ़तर होते गए। मैंने उनकी कविता पुस्तक ‘कंधे पर सूरज’ की समीक्षा की, जो ‘आलोचना’ त्रैमासिक में प्रकाशित हुई। उसके बाद शायद ही उनकी कोई ऐसी महत्त्वपूर्ण पुस्तक रही हो, जिस पर मैंने समीक्षा लेख नहीं लिखा हो। दिल्ली में आई बाढ़ पर उनकी प्रकाशित पुस्तक ‘आकाश की छत’ पर मैंने लंबा समीक्षात्मक लेख लिखा, ‘दूसरा घर’ उपन्यास पर भी लिखा। उनकी ‘परिवार’ नामक उपन्यासिका पर भी लिखा। उनकी आत्मकथा के दूसरे खंड की मैंने विस्तृत समीक्षा की। कविताओं में ‘आम के पत्ते’, ‘आग हँसती है’ तथा अन्य कई पुस्तकों पर भी आलेख लिखे।
रामदरश जी की कवि-दृष्टि की गहरी परख आज भी बेजोड़ है। वह अपनी सर्जनात्मकता में विश्व-दृष्टि के चश्मे से झाँक-ताक कर कविता नहीं लिखते। उनकी संवेदित दृष्टि उनके मर्म के तंतु-जाल को झंकृत कर देती हैं इसके साथ ही उनकी कवि-दृष्टि काल, स्थल, स्थिति, लोग उनकी करुणा, विडंबना, संत्रास, भय और सन्नाटे को अर्थवान करने लग जाती है। यह अर्थ सीधे दिल से टकराता और विवेक को झकझोरता है। इसीलिए मैं उन्हें सामान्य-सी घटना तक में कविता को साधने और बाँधने वाला अकेला और अद्वितीय कवि मानता हूँ। वे यह नहीं कहते कि सन्नाटा बुनता हूँ, पर उनका कवि-धर्म यही करता है। उनकी इस पहचान और परख को प्रायः जनवादी कवि-अलोचक नहीं जानते-मानते हैं। रामदरश जी की जिजीविषा साहित्य से अनुप्राणित और साहित्य में ही निहित है। वही उनकी पिपासा है, वही उनकी रिरंसा (रमणेच्छा) है और वही उनकी सिसृक्षा है। वे प्रकृति और पर्यावरण तथा ग्राम्य भारतीय संस्कृति के कवि हैं, मानसिक विकृति के नहीं, जैसा आज प्रायः समकालीनों में देखने-पढ़ने को मिलता है। उनकी वाणी में अब भी वही आकर्षण है। आँखों में वही दृष्टि की उत्सुकता है। काया थोड़ी क्षीण पड़ी है। गर्दन थोड़ी झुकी है, पर मेरुदंड पूर्ववत तना है, बहुत सारे संघर्ष के राज को पचाये। वैसे ही रामदरश जी की कविताएँ भी अपनी सहजता में सीधी गोताखोरी के लिए पाठकों को न्योतती हैं। ठीक वैसे ही जैसे प्रेमचंद की कहानियाँ सहज होकर भी पाठकों को गोताखोरी के लिए आमंत्रित करती है। मिश्र जी अपने-अपने देखे, सुने और भोगे यथार्थ को कला-सत्य बना देते हैं।
आपातकाल के दौरान उनके द्वारा लिखी एक कविता ‘वसंत’ ने मुझे झकझोर दिया था।
‘कोयल से मैंने कहा–गाओ
कुछ सन्नाटा कटे
वह चुप रही
मैंने कहा–मेरे पास आओ
कुछ सन्नाटा कटे
वह डाल पर बैठी रही
मैंने कहा–
अच्छा सुनो, मैं ही गाता हूँ।
उसने सहमी निगाहों से चारों ओर देखा–
और एकाएक उड़ गई…’
इस कविता का शीर्षक है ‘वसंत’ और कविता में छाया है सन्नाटा। वसंत अनेकविध मुखरता का परासंदेशी शब्द (Hypogramic word) है। वसंत रूप, रस, गंध, स्पर्श, नाद-सबकी मुखरता है। यह कविता निराला के ‘भरा हर्ष वन के मन, नवोत्कर्ष छाया’–वाले वसंत की वासंती कविता नहीं है। यहाँ तो सन्नाटा-ही-सन्नाटा है। यहाँ कोयल की पंचम तान को कौन कहे, कोयल निःशब्द, मूक-मौन है। वह गाने के आग्रह को ठुकरा कर चुप रह जाती है। कवि उसे अपने समीप बुलाना चाहता है, पर वह इसे भी नहीं स्वीकारती और डाल पर यथावत् बैठी रहती है। कोयल की इस चुप्पी और स्थिरता की यथास्थिति में अंततः कवि उसे श्रोता की भूमिका में आने का आग्रह करता है और कहता है कि मैं ही गाता हूँ, तुम सुनो। पर वह सहमी नजरों से चारों ओर देखती और उड़ जाती है। वह द्रष्टा भाव, भोक्ता भाव और साक्षी भाव-तीनों में से किसी भी भूमिका-निर्वाह को नहीं स्वीकारती और उड़ कर पलायन कर जाती है। कविता में ‘वसंत’ कवि का बीज शब्द (key word) है और ‘सन्नाटा’ तथा ‘सहमी निगाह’ प्रतिपाद्य शब्द (Theme word) हैं। ‘वसंत’, ‘आपातकाल (Emergency) बन जाता है और ‘वसंतोत्सव’ ‘अनुशासन पर्व’ में बदल जाता है। स्मरणीय है कि विनोबा ने आपात काल को ‘अनुशासन पर्व’ की संज्ञा दी थी। लोकमानस में प्रजा के बीच सन्नाटा है, सहमे-सहमे रहने की आशंकित स्थिति है। जन-मानस की अभिव्यक्ति प्रतिबंधित हैं, पर सत्ताधारियों के यहाँ वसंतोत्सव है। ‘आपातकाल’ पर दुष्यंत ने गजलें लिखीं, धर्मवीर भारती ने ‘मुनादी’ कविता लिखी। पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के छिनने, सन्नाटा छा जाने और सहमे-सहमे रहने जैसी त्रासद-व्यंजना जैसी इस कविता में हुई है, वैसी मुझे अन्यत्र कहीं भी देखने को नहीं मिली। यहाँ सत्ता का बुना हुआ सन्नाटा है, कवि-दृष्टि का बुना हुआ सन्नाटा (मैं सन्नाटा बुनता हूँ) नहीं है। कहना न होगा कि यह कविता रामदरश मिश्र को एक महान कवि बना देती है। यह बहुत महत्त्वपूर्ण है कि यह कविता कालांकितता (Datedness) से उत्पन्न होकर भी कालातीतता (Beyojnd the time limit) का स्पर्श कर उठती है। इस कविता में कवि का पूरा स्वदेश, स्वदेश के लोग और उसका समकाल–तीनों ही मुखर हुए हैं। अपनी इस कविता में कवि की भागीदारी द्रष्टा, भोक्ता और स्रष्टा–तीनों की है।
Image Source : Nayi Dhara Archives