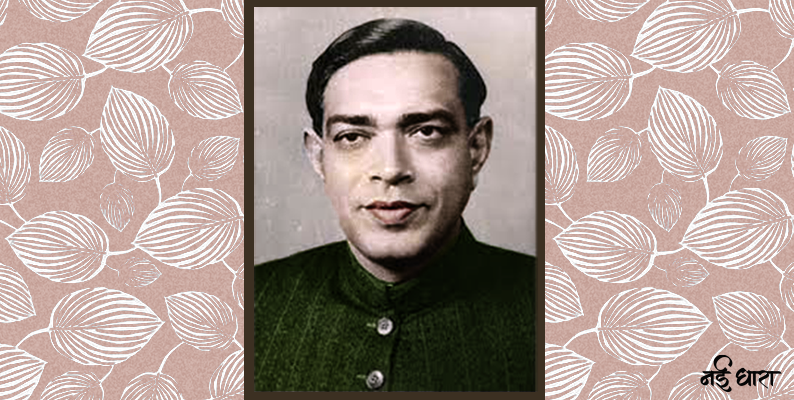वंदे मातरम्
- 1 February, 2016
शेयर करे close
शेयर करे close

शेयर करे close
- 1 February, 2016
वंदे मातरम्
वे दिन : वे लोग
मेरी माँ अन्नपूर्णा सिन्हा भारतीय आंदोलन से एक अटूट हिस्से की तरह संबद्ध रही थीं। जब अनामिका जी ने मुझे मेरी माँ से सुनी आजादी की बातें कलमबद्ध करने के लिए कहा तो उस पल लगा कि उन बातों को शब्दों के फंदों में कैसे डाल पाऊँगी, क्योंकि वे तो हवा की तरह हैं, सूरज की रोशनी तथा बारिश की बूँदों जैसी हैं। लेकिन जब लिखने बैठी तो आजादी के किस्से के बहाने क्या था जो बीते समय को पकड़ा गया। घर में माँ का अनुशासन था। अलस्सुबह उठना, सितार बजाना, दुर्गा सप्तशती के श्लोक याद करना, स्कूल जाना, पढ़ना आदि। लेकिन रात में हम छह भाई-बहन माँ के आसपास जमा हो जाते और तब उनके हृदय की अतल गहराई में छिपी बहुत-सी सीपियाँ खुलती, तो खुलतीं कहानी की जादुई दुनिया। वह आजादी की कहानी ठीक उसी तरह सुनातीं, जिस तरह रामायण और महाभारत की कहानियाँ। आज जब लिखने बैठी तो परत दर परत उतरने पर मेरे भीतर वे समय मानो आज भी जीवित हैं। बरसों बीतने पर भी वे आत्मीय अनुभूतियों के क्षण ज्यों के त्यों बने हुए हैं। यहाँ यादों की एक पूरी बस्ती है। वे लम्हें, वे पल बचकाने नहीं हैं, अत्यंत गंभीर एवं अर्थपूर्ण हैं।
मेरी माँ की कही आजादी की कहानी शुरू होती थी 16वीं शताब्दी से और खत्म होती थी 15 अगस्त 1947 को। सोलहवीं शताब्दी में अँग्रेज व्यापार करने भारत आये। 150 साल तक व्यापार करते-करते उन्होंने बेहद चतुराई से भारत को अपनी मुट्ठी में कर लिया। पहली बार 1757 में पलासी युद्ध में उन्हें देश से निकलने की चेतावनी मिली। पलासी में अँग्रेज जीत गए किंतु देशवासियों ने हार नहीं मानी। वे लगातार अपने असंतोष का इजहार करते रहे। 1764 में बक्सर युद्ध में भी हम पराजित हुए, पर आजाद होने की तीव्र कामना बनी रही। अपने-अपने स्तर पर संथाल बगावत, संन्यासी विद्रोह, भील विद्रोह, वहारी विद्रोह होते रहे। इसके बाद हुआ 1857 का विद्रोह। इस विद्रोह में मात्र सिपाही नहीं लड़े–इस युद्ध में झाँसी की रानी के साथ राजे-रजवाड़े, जमींदार, मौलवी, विद्वान सभी शामिल हुए। पूरे देश में आग लगी थी। इसी समय हिंदुस्तान में नया जागरण फैला, समाज में नव-संस्कार की लहर फैली। यह पूरा दौर आँखों पर से पर्दे हटाने का, दिमागी जाले साफ करने का, अपने कुसंस्कारों के दाग-धब्बे मिटाने का दौर था। हिंदू और मुसलमान दोनों ही समाज में ऐसे लोग पैदा हुए जो अपने समाज की अंदरूनी खामियों पर तार्किक दृष्टि से विचार करने लगे एवं उसमें सुधार की संभावनाएँ टटोलने लगे। राजा राममोहन राय, देवेंद्रनाथ ठाकुर, ईश्वरचंद विद्यासागर, गोविंद रानाडे, ज्योतिबा फूले, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, बंकिम चट्टोपाध्याय आदि समाज सुधारकों ने उसे एक व्यवस्थित आंदोलन देने का काम किया। इनका सामाजिक दर्शन क्रांतिकारी था। विवेकानंद ने अपने एक भाषण में कहा था, ‘ध्यान रखो कि राष्ट्र झोपड़ियों में रहता है। किसान, जूते बनाने वाले, गंदगी ढ़ोने वाले वर्ग में तुम से कहीं ज़्यादा काम करने और स्वावलंबन की क्षमता है। ये लोग युग-युग से चुपचाप काम करते रहे हैं। वे ही हैं, जो देश के समस्त संपदा के उत्पादक हैं। फिर भी उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। ऐसा दिन शीघ्र आने वाला है जब उनका दर्जा तुम से ऊपर होगा।’ नये भारत का यह काल जितना प्रखर था, उतना ही चुनौतीपूर्ण। वह पूरा युग सीखने-सिखाने की एक बेहद रोमांचक कथा है। 1905 से 1919 के दौर में भारतीय राजनीति में अँग्रेजों ने सांप्रदायिकता का जहर घोलने का सक्रिय प्रयास किया। इसी से 1905 में बंग-भंग हुआ। 1906 में मुस्लिम हितों का प्रतिनिधित्व करने वाली नई पार्टी-मुस्लिम लीग अस्तित्व में आईं। मुस्लिम लीग की स्थापना के समय राष्ट्रवादी काँग्रेस मुसलमान मुहम्मद अली जिन्ना और शायर मुहम्मद इकबाल जैसे लोगों ने इसका सख्त विरोध किया। पर इस दल की अगुवायी सर आशा खान ने की। ये इस्माइली खोजों के धार्मिक गुरु थे। इस तरह मुस्लिम अलगाववाद की 1906 में बुनियाद रखी गई। लेकिन इसी के साथ स्वदेशी एवं बहिष्कार का एक व्यापक आंदोलन दावानल की तरह सारे देश में फैल रहा था। अब तक काँग्रेस नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गया था। गरम दल का नेतृत्व करने वाले नेता थे–बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय एवं विपिनचंद्र पाल। तब लाल, बाल, पाल से ये मशहूर थे। ये तीनों सक्रिय संघर्ष कर लंबी सजा भुगत चुके थे। बाल गंगाधर तिलक ने देश को पहली बार नारा दिया, ‘स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा।’
उधर नरम दल का नेतृत्व कर रहे थे–फिरोज शाह मेहता, गोपालकृष्ण गोखले, डॉ. रासबिहारी घोष। ये लोग सरकार के साथ सहयोग का मार्ग अपनाकर धीमी गति से संसदीय लोकतंत्र की दिशा में बढ़ने के हिमायती थे। 1905 के सूरत काँग्रेस अधिवेशन में गरम दल एवं नरम दल बुरी तरह आपस में उलझ गए। विवाद में पड़कर काँग्रेस टूटने लगा। इसी समय जनवरी 1915 में गाँधी जी भारत आये। इस अति सामान्य व्यक्ति में ऐसा कुछ नहीं था जो उसे राजनेता बना देता लेकिन उनमें तड़पती क्रांति तथा अखंड शांति का अद्भुत समन्वय था। उन्होंने दो सौ साल से ज़्यादा समय से चले आ रहे स्वतंत्रता संग्राम के सारभूत तत्वों की विरासत के साथ अपना आंदोलन शुरू किया। भारतीय राजनीति के मंच पर इनके आने के बाद न तो काँग्रेस वैसी रहीं, न देश, न स्वतंत्रता की लड़ाई का स्वरूप वैसा रह गया।
मेरी माँ अन्नपूर्णा के दादा भगवतीचरण वर्मा ने सन् 1880 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से कानून में स्नात्तक की डिग्री हासिल की थी। वे उत्तरी बिहार के मुजफ्फरपुर शहर में सरकारी वकील थे और वहाँ के जाने माने जमींदार थे। उनके पुत्र श्यामाचरण वर्मा ने भी 1910 में वकालत शुरू किया और शीघ्र ही उनकी गिनती वहाँ के श्रेष्ठ वकीलों में होने लगी। उस समय लोगों के मन में शंका थी की भारत को स्वराज योग्य होने में समय लगेगा, किंतु श्यामाचरण जैसे न जाने कितने देश भक्तों ने माना कि भारत आज ही स्वराज्य के लिए तैयार हैं। वे अपने पिता के सरकारी वकील होने का विरोध करने लगे और स्वयं राष्ट्रीयता की ओर आकर्षित होने लगे।
धीरे-धीरे वह कचहरी की बजाय खादी भंडार जाने लगे। वहाँ काँग्रेस सेवादल का दफ्तर था। वहाँ गाँधी द्वारा निकाली पत्रिका ‘हरिजन’ पढ़ने लगे। कोट पतलून छोड़ खद्दर का धोती-कुरता पहनने लगे। पिता के बहुत मना करने पर भी उन्होंने वकालत छोड़ दी। बहुत दिनों तक लोग उनके पास मुकदमें की पैरवी लेकर आते रहें पर वे ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आंदोलन में व्यस्त हो गए। ठीक इसी समय पंडित मोती लाल नेहरू, पंडित मदनमोहन मालवीय ने वकालत छोड़ा, सुभाषचंद्र बोस ने अपनी आई.सी.एस. की नौकरी छोड़ी। श्यामाचरण के पिता का निधन हो गया था। छोटे भाई रमाचरण ने पूरी तरह अपना जीवन प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में लगा दिया। छोटी बहन शारदा देवी बाल विधवा थीं। भाइयों के साथ रहती थीं। वे नवजागरण की पत्रिका निकाला करती थीं। बाद में बिहार विधान परिषद् की सदस्य बनीं। दूसरी बहन शैल कुमारी की शादी छपरा के बैरिस्टर शिवनाथ जी से हुई थी। वे कहानी कविताएँ लिखा करती थीं। सन् 1925 में उन्होंने ‘उमा सुंदरी’ नाम से एक उपन्यास लिखा था। सन् 1916 में श्यामा चरण के एक मित्र साबरमती गए थे। गाँधी से उनका पहला संपर्क उन्हीं के मित्र के माध्यम से हुआ था। तब गाँधी का वहाँ आश्रम नहीं बना था। कस्तूरबा जी एक कोठरी में खाना बनाती थीं। एक-दो स्थानीय लड़के उनकी मदद करते थे। गाँधी सबको साथ बैठा कर खिलाते थे।
श्यामा चरण अक्सर किसी काम से या बहन से मिलने छपरा जाया करते थें। वहाँ वे अपने बहनोई के जरिये ब्रजकिशोर जी से परिचित हुए। 1915-16 के आस-पास की बात हैं। वे छपरा गए थे। वहाँ वे ब्रजकिशोर जी से मिलने गए। उनके पास चम्पारण से एक किसान आया था राजकुमार शुक्ल। वे चम्पारण में नील की खेती करने वालों के जुल्म से परेशान थे। उनकी तरह दूसरे खेतीहर भी जुल्म के शिकार थे।
राजकुमार शुक्ल को कहीं से पता चला था कि गाँधी जी ने दक्षिण अफ्रिका में भारतीय बंधुआ मजदूरों के लिए संघर्ष किया था, उन्हें बराबरी का हक़ दिलाया था। उन्होंने ब्रज किशोर प्रसाद ने अपना दुखड़ा सुनाकर कहा कि वे काँग्रेस के सम्मेलन में नील खेतीहरों की समस्या के बारे गाँधी को बताये। ब्रज किशोर बाबू से वचन लेने के बाद ही वे वहाँ से गए। फिर ब्रज किशोर बाबू के सतत प्रयास से सन् 1917 में गाँधी चम्पारण आये। चम्पारण सत्याग्रह गाँधी का देश का पहला सत्याग्रह था। इसका श्रेय ब्रज किशोर बाबू एवं राजकुमार शुक्ल को जाता है। श्यामा चरण वर्मा इस सारे प्रसंग में परोक्ष रूप से जुड़े हुए थे। देश के भविष्य को लेकर अनेक सपने उनके मन को आंदोलित कर रहे थे। 1919 में रॉलेट एक्ट आया। उसके विरुद्ध फिर आंदोलन हुआ। 1919 में ही बैसाखी के दिन जालियाँवाला बाग में जनरल डायर ने बहुत बड़ी सभा में गोलियाँ बरसा दी। सब जगह इसकी बहुत आलोचना हुई।
1921 में पंजाब दमन के बाद और स्वराज के प्रश्न पर गाँधी के नेतृत्व में अहिंसात्मक असहयोग आंदोन हुआ। इसी समय इंग्लैण्ड के युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आये। पूरे देश में बंद का आह्वान किया गया। अक्टूबर 1921 में श्यामा चरण प्रांत काँग्रेस कमिटी के काम से दक्षिण बिहार के दुमका शहर गए थे। बंद का आह्वान होते ही उन्होंने वहाँ से टीन बाजार में जनसभाएँ की। उनका ओजस्वी भाषण सुनकर भारत माता की जय जयकार होने लगी। एक का साहस दूसरे में फैलने लगा। सबमें बलिदान की चेतना जाग गई। किसी की आँखों में डर नहीं। बेकसूरों को मारा जा रहा था पर वे दबने वाले नहीं थे। सिपाही निर्ममता से उन पर टूट पड़े। गिरफ्तारियाँ हुईं। श्यामा चरण को भी गिरफ्तार कर लिया गया।
वर्मा जी को तीन महीने की सजा हुई। वे प्रथम श्रेणी के राजनीतिक बंदी थे। जेल में भी उन्हें घर जैसी सुविधा मिलती। लेकिन उन्हें अपने स्वयंसेवकों का ध्यान था। वे तीसरी श्रेणी में आ गए। उनसे जेल अधिकारी ने कहा, ‘तीसरे दर्जे के कैदियों के साथ रहेंगे तो काम भी वहीं करना पड़ेगा।’
उन्होंने कहा, ‘कोई हर्ज नहीं, मुझे मंजूर है, मुझे रियायत नहीं चाहिए।’
अधिकारी ने उन्हें हर तरह से बताना चाहा कि वहाँ मुश्किलें बहुत हैं लेकिन उन्होंने अपनी राय नहीं बदली। वे तीसरे दर्जे में आ गए।
1923 में उन्होंने एक पुस्तक लिखा, ‘माई एक्सपीरियेंस इन जेल’। इस पुस्तक का संशोधन उनके परिचित राजेन्द्र प्रसाद ने किया था। बाद में वे भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। उसी वर्ष वह पुस्तक कलकत्ता के प्रसिद्ध समाचार पत्र अमृत बाजार पत्रिका में धारावाहिक रूप से प्रकाशित हुई। उन दिनों पत्रिका के संपादक शिशिर कुमार घोष थे। ब्रिटिश राज के तत्कालीन उप-राज्यपाल उनसे अप्रसन्न रहते थे। वर्मा जी 1923-24 में काँग्रेस टिकट से विजयी रहें। सेंट्रल असेंबली में वे एक प्रखर वक्ता के रूप में जाने जाते थे। सन् 1929 में भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली हॉल में जब बम फेंका था वे वहाँ मौजूद थे। उस दहकते अतीत के साक्षी थे। माँ से वे वाकया मैंने कितनी बार सुना था। भगत सिंह ने अँग्रेजी हुकूमत के हर अमानवीय अत्याचार का डटकर मुकाबला किया था। आजीवन कारावास, काले पानी की सजा भुगती। देश के लिए प्राणों की भी परवाह नहीं की। 9 अगस्त 1925 को काकोरी में डकैती डाली गई। उसमें राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, लाहिड़ी, मुकुंदी लाल, आशफाकउल्ला, मन्मथनाथ, शचीन्द्र नाथ, बनवारी लाल, मुरारी लाल, कुंदन लाल का दल गठित हुआ। सरकारी खजाना लेकर जब गाड़ी लखनऊ के लिए चली तो काकोरी में गाड़ी रोक ली गई। खजाने से भरा संदूक उतारा गया। क्रांतिकारी गोलियाँ चलाते रहे। संदूक तोड़कर थैलियाँ निकाली गई, उनका गठरी बनाया गया। बिस्मिल ने लखनऊ पहुँचकर सारा धन कहीं छिपा दिया। दल के सभी लोग इधर-उधर हो गए।
माँ ने बताया कि दूसरे दिन अखबार इसकी खबर से भरा था। बाद में ये सब गिरफ्तार हुए। जिस समय काकोरी केस लखनऊ में चल रहा था उस समय उनके अभियुक्तों को छुड़ाने को एक विशेष योजना लेकर भगत सिंह लखनऊ आये थे। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। इस पर बिस्मिल का एक मशहूर गज़ल था–
‘मिट गया जब मिटने वाला फिर सलाम आया तो क्या
दिल की बर्बादी के बाद उनका पयाम आया तो क्या।’
1927 में अप्रैल के इनका फैसला आया। लाहिड़ी एवं अशफाकउल्ला खाँ को फाँसी की सजा मिली और बाकियों को 4 से 14 वर्ष तक का कारावास। इसकी देश में तीखी प्रतिक्रिया हुई। मुस्लिम समाज से आने के बावजूद अशफाकउल्ला खाँ ने मौत को बहादुरी से स्वीकार किया। देशभक्ति का उनका अपना ज़ज्बा था। आखिरी वक्त जब वे चलने लगे तो इन पंक्तियों में कहा–
‘कुछ आरजू नहीं है, है आरजू तो ये है
रख दे कोई जरा-सी, खाके वतन कफन में।’
इन लोगों का लक्ष्य था देश में समाजवाद की स्थापना। शोषणहीन समाज, साम्राज्यवाद का सारी दुनिया में खात्मा। यह काम इंकलाब के जरिये ही पूरा हो सकता था। प्रसंगवश माँ से सुना एक बात यहाँ बता दें। भगत सिंह हमेशा ‘इंकलाब जिंदाबाद’ कहा करते थे। किसी ने उनसे पूछा कि आप ‘वंदे मातरम’ की जगह ‘इंकलाब जिंदाबाद’ क्यों कहते है, उन्होंने जवाब दिया, ‘माँ की वंदना करने का अधिकार तो आपको तब होगा जब माँ के बंधन तक पहुँचने का आपको अधिकार होगा। जब तक माँ विदेशियों के कब्ज़े में है, तब तक पहला कदम है माँ को बंधन से मुक्त कराना। वंदना तो उसके बाद होगी। मुक्त कराने का काम केवल माँ की वंदना करने से नहीं होगा, बल्कि इंकलाब के रास्ते पर चलकर ही संभव होगा।’
श्यामा चरण के चार बच्चे थे–दो लड़के और दो ही लड़कियाँ। पत्नी कुसुम का निधन हो चुका था। बच्चों से उनको स्नेह था, पर अपने कामकाजों से अवकाश काम मिलता। लेकिन बच्चों की शिक्षा का पूरा इंतजाम था। यों घर-परिवार भी आजादी की कामना के रंग में रंगा था। इन चारों भाई-बहनों को गहने कपड़े का शौक नहीं था, न ही अपनी हैसियत बढ़ाकर दिखाने की धुन। कोई भी राष्ट्रीय आंदोलन हो उसकी पूरी जानकारी घर वालों को होती थी। किसी भी हालत में सांप्रदायिकता और छुआछूत को स्थान नहीं दिया जाता था। उनका नैतिक आचरण अध्यात्म एवं धर्म से जुड़ा हुआ था। घर में सामवेद का पाठ होता था। सभी खादी पहनते थे और नित्य चर्खा से सूत कातते थे। चर्खा कातते समय उनकी भावना रहती–‘चर्खा से जमीं को हमतो चर्ख गूँजा देंगे।’
सबसे बड़ी अन्नपूर्णा स्वदेशी आंदोलन एवं बॉयकाट नाम के लेखों का संग्रह कर रही थीं। वे ‘चाँद’ और ‘हरिजन’ पत्रिकाएँ पढ़ती थीं। असहयोग आंदोलन के कारण स्कूल कॉलेज की औपचारिक शिक्षा उन्हें नहीं मिली थीं किंतु पढ़ी लिखी खूब थीं। लेख, कहानी, कविताएँ लिखा करती थीं। उनकी छोटी बहन ललिता ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से एम.ए. किया था। दोनों भाइयों का असमय निधन हो गया था। अन्नपूर्णा व्यक्तित्व संपन्न तेजस्वी लड़की थीं। एक बार की बात है, वे दस-बारह साल की थी। गाँधी जी मुजफ्फरपुर आए। अन्नपूर्णा ने अपने हाथों से काता सूत की माला उनको पहनाई। वे बहुत खुश हुए और उनको अपने पास बैठा लिये। तभी बापू से मिलने उनकी हमउम्र लड़कियाँ आईं। उस दिन वे सभी खादी के कपड़ों में थीं। उन्हें खादी के कपड़ों में देखकर अन्नपूर्णा ने कहा, ‘बापू आज आपको दिखाने के लिए ये खादी पहने हुए हैं नहीं तो रोज मेरे खादी के कपड़ों को मोटिया-मोटिया कहकर चिढ़ाती हैं।’ वहाँ बैठे सभी लोग बच्ची की स्पष्टवादिता पर मुरकुरा दिये। बापू ने कहा, ‘चलो एक ही दिन के लिए, कम से कम खद्दर पहना तो। अब ये तय है कि ये तुम्हारे खद्दर को कभी मोटिया नहीं कह पाएँगी।’
अन्नपूर्णा ने आठ वर्ष की उम्र से खद्दर पहनना शुरू किया और आजीवन खद्दर पहनती रहीं। हमारे घर के पर्दे, चादर, तौलिया आदि खद्दर के हुआ करते थे। हम यहीं जानते थे कि खद्दर का जड़ सत्य और अहिंसा में है। खादी जीवन मूल्यों का प्रतीक है, जबकि मिल का कपड़ा केवल भौतिक मूल्य प्रकट करता है।
आजादी की लड़ाई के दौर में भारतवासियों की भावनाओं को जाग्रत करने का काम किया आजादी के तरानों ने। इस समय का साहित्य सामूहिकता का, विस्मृति के विरुद्ध स्मृति का बिखराव के विरुद्ध लगाव था, जमाखोरी एवं अमानवीय तंत्र के विरुद्ध मानवता का, देश प्रेम का, उन्नत जीवन की आशा-अभिलाषा का था। उन दिनों सैकड़ों हजारों गीत देश की हवाओं में गूँजते थे। उनमें ओज़ और तरन्नुम ऐसा होता था कि लोग विदेशी वस्त्रों की होली जलाने को खुद-ब-खुद प्रेरित हो जाते थे। माँ से सुना उस लोक गायन की दो पंक्तियाँ आज भी मुझे याद है।
‘जरा भारत की दौलत बचाओ पिया, मुझे खादी की चादर उढ़ाओ पिया।’
घर-घर में अनगिनत तराने लिखे, जा रहे थे–‘दुखिया किसान हम हैं, भारत के रहने वाले, दाने बिना तरसते न्यामत परसने वो।’
घर का कोई एक सदस्य गीत रचता, बाद में दूसरे लोग उनमें कुछ शब्दों का परिवर्तन-संशोधन कर देते। इनमें गेयता तत्त्व प्रधान रहता था। ये स्वाभाविक रूप से सामाजिक होते थे, अपने आस-पास के अनुभव, आकांक्षा, दुःख-दर्द इनके प्राण तत्त्व होते थे। इनमें अपनी मिठास होती थी–
‘धन्य-धन्य झाँसी की रानी
धन्य-धन्य वह पानी
धन्य-धन्य वह दुर्ग जिससे
दुर्गा सम प्रगटी लक्ष्मी रानी।’
ऐसे अनगिनत लोक साहित्य रचे गए। मैंन सुना है कि बुंदेलखंड और कुमांऊनी-गढ़वाली क्षेत्रों में उन गीतों को अब भी सुना जा सकता है। 1930-1940 के दौरान लगभग हर कस्बे में देशभक्त कवि होते थे। इनके कई तराने तो ऐसे थे जिन्हें अँग्रेजी हुकूमत ने डर के मारे जब्त कर लिया। ऐसा ही एक जब्तशुदा गीत जो लगभग–1923-33 के दौरान लिखा गया था, मेरी बड़ी बहन मोदी ने मुझे दिया था–‘दे दे मुझे तू जालिम, मेरा ये आशियाना,/आरामगाह मेरी, मेरा बहिश्तखाना’।
इन गीतों को लिखने वालों का कोई अता-पता न मिलता। पर स्थानीय लोग इन्हें अपना मसीहा मानते थे। अपने घर में छिपाकर उनको पूरी सुरक्षा देते थे। अँग्रेजी सरकार और सिपाही की नजरों से दूर रखते थे। कुँवर चंद्रप्रताप, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, अशफाकउल्ला खाँ, दिनेश, चकोर, अजीज साहब, कुरबान साहब, अख्तर शीरानी जैसे सैकड़ों गीतकार थे–
‘बाँध ले बिस्तर फिरंगी, राज अब जाने को है
जुल्म काफी कर चुके, पब्लिक बिगड़ जाने को है।’
संघर्षशील कवि लगातार गोरी हुकूमत के खिलाफ संघर्षशील रहे। वे सरकार को चुनौती दे रहे थे, उनके डर से ब्रिटीश सिंहासन डोल रहा था–
‘खुशी है हो गया महबूब का दीदार फांसी से
हो जाएँगे आजाद हम जालिम अँग्रेजों से।’
तब यह भावना बह रही थी कि जो देश के लिए बलिदान करें वह पूजनीय है। शहीद, फौज, जालिम की हथकड़ी, लंदन का तख्त, स्वदेशी, ख्वाहिश, वतन, दिवाने आदि लफ्जों से सराबोर उन तरानों में ऐसा जादू था जो घर वालों के देश पर बलिदान हो जाने के बाद भी उनका हौसला बनाये रखने की ताकत देता था। इनको लिखने वाले हिंदू और मुसलमान दोनों थे। वे हमारी अनमोल विरासत थे। हम चाहते तो इस अमूल्य मौखिक परंपरा को बचा सकते थे। लेकिन आजादी मिलते ही हम देश के नवनिर्माण के कार्य में इतने व्यस्त हो गए कि बीते जमाने की उस मूलभूत प्रेरणा को भूलने लगे। आजादी की लड़ाई में उनका एक पूरा सैलाब उमड़ा था। जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने देश लड़ाई लड़ी, उनके मन में वंदे मातरम् की भावना थीं।
भारत के स्वाधीनता आंदोलन में समाचार पत्रों ने बहुत महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी। देश में मराठा, केसरी, इंडियन मिरर, नेशन हिंदुस्तानी, ट्रीब्यून, हिंदू एवं क्रेसेंट आदि प्रमुख समाचार पत्र थे। इनके उदय के बाद ही ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज आदि की स्थापना हुई। इन संगठनों ने अपने आदर्श के प्रचार-प्रसार के लिए पत्र-पत्रिकाओं को जरूरी समझा। इस कारण राजा राममोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, केशवचंद्र सेन, देवेंद्रनाथ ठाकुर, स्वामी दयानंद सरस्वती, श्रद्धानंद, गोविंद रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले आदि ने भी समाचार पत्रों की या तो स्थापना की या उनमें सहयोग दिया। इनका ऐसा प्रभाव था कि बहुत-सी चीजें जो पहले नहीं दिखती थीं, वे दिखने लगीं। बहुत से रागात्मक संबंध जो सोये हुए थे वे जाग गए। इस संदर्भ में भारतेंदु हरिश्चन्द्र का नाम उल्लेखित है। 1850 से 1885 अपने जीवन के 35 वर्ष के जीवनकाल में उन्होंने हिंदी प्रदेश में अपूर्व वैचारिक क्रांति ला दी थी। उन्होंने स्वयं भी कई पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन किया तथा इनके प्रकाशन के लिए लोगों को प्रेरणा दी। उनके प्रयास से लाहौर में ‘ज्ञान प्रदायिनी’, वृंदावन से ‘भारतेंदु’ और कानपुर से ‘ब्राह्मण’ का प्रकाशन हुआ। इनके प्रथम अंक में ही ब्रिटीश शासन की आलोचना शुरू हो गई।
भारतेंदु हरिश्चंद्र औनरेरी मजिस्ट्रेट थे और काशी के प्रसिद्ध रईस थे। देश में शायद वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ऑनरेरी मजिस्ट्रेट का पद छोड़ा। उस समय असहयोग आंदोलन की कल्पना भी नहीं की गई थी। आजादी की लड़ाई में पंडित गंगाधर तिलक का ‘केसरी’, कलकत्ता से छपने वाला ‘वंदे मातरम्’, पंजाब का ‘वंदेमातरम्’ इलाहाबाद से निकलने वाला ‘अभ्युदय’ एवं ‘लीडर’ ने प्रमुख भूमिका निभायी थीं।’ हिंदी के अनेक लेखकों को उस जमाने में जेल यात्रा करनी पड़ी। गणेशशंकर विद्यार्थी, पालीवाल जी, रामवृक्ष बेनीपुरी। रामवृक्ष बेनीपुरी का एक उपन्यास ‘कैदी की पत्नी’ हमारे घर में था। यह स्वतंत्रता संग्राम पर आधारित था–खासकर सन् 1942 का काल। रामवृक्ष बेनीपुरी एवं रामधारी सिंह दिनकर का हमारे घर आना-जाना था। रामधारी सिंह दिनकर मेरे पिता सच्चिदानंद सिन्हा के मित्र थे। 1937 में मेरे पिता मधुबनी (बिहार) में मुंसिफ थे, और रामधारी सिंह रजिस्ट्री ऑफिस के सब रजिस्ट्रार थे। दोनों का सरकारी बंगला अगल-बगल था। दिनकर की एक कविता मेरे पिता जी की डायरी में मिली थी–‘कलम, आज उनकी जय बोल’।
देशभक्ति, खादी, चर्खा स्वराज का पाठ पढ़ते हुए अन्नपूर्णा बड़ी हो रही थीं। सन् 1933 में उनकी शादी राँची के एक अभिजात्य परिवार में सच्चिदानंद सिन्हा से हुई। उस समय सच्चिदानंद कानून की पढ़ाई कर रहे थे। राँची छोटानागपुर के पठार पर बसा एक सुंदर शहर है। यहाँ की प्राकृतिक छंटा अत्यंत मनोरम है। यहाँ आकर अन्नपूर्णा का परिचय समाज से हुआ। ये सादगी से रहने वाले ईमानदार लोग थे। यहाँ के बिरसा मुंडा ने 18वीं शताब्दी के अंत में अँग्रेजी सत्ता एवं स्थानीय दमनकर्ताओं के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति की थीं। वे आदिवासी समाज को गरीबी एवं अंधविश्वास से निकालकर शिक्षित एवं स्वस्थ बनाना चाहते थे। उन्होंने अपनी क्रांति का नाम दिया उलगुलान। 1900 में जेल में उनकी मृत्यु हो गई। मरने से पहले उन्होंने अपने अनुयायियों से कहा–‘अब मेरा मरण है, पर उलगुलान को मत मरने देना।’ इसके बाद 1914 में उरांव जनजाति के ताना भगत आंदोलन हुआ। यह बिरसा मंडा की क्रांति की तरह सशस्त्र नहीं था, यह पूर्णतः अहिंसक था। बाद में इसके अधिकांश नेता अपने सदस्यों के साथ काँग्रेस में शामिल हो गए। राँची काँग्रेस कमिटी हमारे घर से कुछ ही फासले पर थी। माँ के साथ कभी-कभी मैं भी वहाँ जाया करती थी। वहाँ इन ताना भगतों से मिली थी। काँग्रेस में आने के बाद भी ये ताना भगत नाम से अपनी पहचान बनाये हुए थे। ये सब सफेद कपड़ों में होते थे और देखने में साधु जैसे लगते थे।
अन्नपूर्णा को स्वच्छता, निर्भीकता, निष्पक्षता विरासत में मिले थे। उन्होंने स्वयं पर आग्रह किया, किसी का अनुकरण नहीं किया। वह किसी भी अन्याय के विरोध में खड़ी होने की ताकत रखती थीं। वह जिसके साथ रहती थीं, उसको शक्ति की बोध करातीं थीं। सन् 1934 की बात है। गाँधी जी राँची आये थे। बिड़ला हाउस में ठहरे थे। अन्नपूर्णा उनसे मिलना चाहती थीं। उनके सचिव अन्नपूर्णा के पिता श्यामाचरण वर्मा को जानते थे। माँ को उनसे मिलने का समय मिल गया। वह अपने हाथ से काता सूत की माला लेकर निकलीं। बाहर आईं तो देखा कि जिस गाड़ी से उन्हें बिड़ला हाउस जाना था उसकी खिड़कियों में पर्दे लग रहे हैं। उन्होंने पर्दा लगाने से मना कर दिया। घर में हंगामा मच गया। लेकिन वह तो बापू से मिलने जा रही थीं जो खुद पर्दा-प्रथा के सख्त खिलाफ थे। बापू के पास जाकर जैसे ही माला उनको दिया वे उनको तुरंत पहचान गए। उन्होंने अन्नपूर्णा को औरतों को चर्खा, करघा और हैंडलूम सिखाने को कहा। उसके बाद उन्होंने राँची में काम शुरू किया–स्वतंत्रता आंदोलन को गति एवं ऊर्जा देना, पर्दा प्रथा समाप्त करना, घर-घर जाकर अभिभावकों को लड़कियों को स्कूल भेजने के लिए सहमत कराना, प्रौढ़ शिक्षा के लिए रात्रि पाठशाला की व्यवस्था करना, राँची विमेन्स कॉलेज खुलवाने के लिए श्रम करना। इन सब के लिए उन्हें कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा। उनके लिए बाधाएँ थीं, विरोध था पर वे उम्मीद लेकर चलती थीं। उनकी ये संघर्षशील व्यक्तित्व अचानक नहीं बने थे। उनके पिछले जीवन से ही इमर्ज किये थे। इन सबसे न जाने वह कितने अंतरंग स्तरों पर जुड़ी हुई थीं। उनमें अपने समय को समझने की दृष्टि थी। उस दृष्टि से वह बाहर ही नहीं भीतर भी देखती थीं। यह उनकी संवेदना का विस्तार था जो उन्हें आत्मीयता का भाव देता था।
उन दिनों मेरे पिता सच्चिदानंद सिन्हा पटना में जज थे। औरों की तरह इनमें भी आक्रोश बढ़ता गया, उनमें एक अलग तरह का जोश व्याप्त हो गया। वे नौकरी छोड़कर आंदोलन में शामिल होना चाहते थे। उसी समय माँ गाँधी जी से मिलीं। उनसे पिता के मन की बात बताई। तब मेरे माता-पिता पर चार बच्चों को पालने की जिम्मेदारी भी थी। गाँधी जी ने माँ को सलाह दी कि पति को नौकरी में बना रहने दो। लेकिन तुम दोनों किसी सरकारी समारोह में मत जाना। यही बात दिनकर जी के साथ भी हुई। वे भी अपनी सरकारी नौकरी छोड़ना चाहते थे, किंतु उन पर एक बहुत बड़े परिवार की जिम्मेदारी थी। उनको अर्थाभाव से सामना करना उनको उचित नहीं लगा। मेरे पिता और दिनकर जी आजीवन मित्र रहें। माँ, जी-जान से आंदोलन से जुड़ गईं। वह घर के लोगों के साथ प्रभात फेरी, जुलूस, भाषण पूरे दमखम से करतीं। अपने आस-पास बच्चों को राम प्रसाद बिस्मिल की कविता ‘सरफरोशी की तमन्ना’ याद करवातीं। एक बार वह कविता फिर से दुहरा दूँ–
‘सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है
देखना है ज़ोर कितना बाजु-ए-कातिल में है।’
मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद साफ हो गई कि सरकार किसी सम्मानजनक समझौते के लिए तैयार नहीं। गाँधी ने ‘करो या मरो’ का नारा दिया। उन्होंने जेल में इक्कीस दिन का उपवास शुरू कर दिया। सरकार गाँधी पर दबाव डाल रही थी कि ‘भारत छोड़ो आंदोलन’ में हुई हिंसा की भर्त्सना करें, लेकिन उनका कहना था कि आंदोलन की इस हिंसा के लिए सरकार ही जिम्मेदार हैं। गाँधी जी के रिहाई के बाद दो मुख्य मुद्दे थे, सरकारी कार्रवाइयों की भर्त्सना करना और शहीदों का गौरव गान करना। इससे लोग भयमुक्त होने लगे। इसी समय काँग्रेसी समाजवादियों की एक नई पीढ़ी आ रह थी। जय प्रकाश, आचार्य नरेन्द्र देव, अच्युत पटवर्धन, राममनोहर लोहिया, अरूणा आसफअली। जय प्रकाश नारायण का हमारे चाचा राधाकृष्ण सहाय से गहरी मित्रता थी। वे हमारे घर आया-जाया करते थे। कभी-कभी वे अपनी सभा एवं हमारे श्रद्धानंद रोड स्थित ‘बलदेव भवन’ में किया करते थे। माँ ने आखिर बहुत परिश्रम के बाद ‘महिला चर्खा मंदिर’ की स्थापना की। उनको बरसों का सपना पूरा हुआ। गाँधी जी के कहे मुताबिक औरतों को चर्खा, करघा और हैंडलूम चलाने की शिक्षा दी जाने लगीं। पाँचवीं तक बच्चों को मुफ्त पढ़ाया जाता था। वहाँ प्रौढ़ शिक्षा की भी व्यवस्था थी। माँ इस संस्था को हम छह भाई-बहनों से ज्यादा प्यार करती थीं।
उन महिलाओं और बच्चों को पढ़ाना, उनके दुःख दर्द में शामिल होना हम भाई-बहनों की दिनचर्चा में शामिल था। मेरा तो जन्म एवं पालन-पोषण उसी जगह हुआ। वहाँ उन लोगों के आंसू और आक्रोश की प्रत्यक्ष अनुभूति ही मेरा यथार्थ ज्ञान है। बाद में इन्हीं को आधार बनाकर मैंने कई रचनाएँ की। अन्नपूर्णा अंधकार से प्रकाश की ओर जाने वाली महिला थीं। उनसे यही जाना कि जीवन में थोड़ा-सा भी प्रकाश बहुत से अँधेरे को नष्ट कर देता है। 1940 के दशक में वह लिखा करती थीं। ‘माया’, ‘कल्याण’, ‘सरिता’, ‘धर्मयुग’ में उनकी रचनाएँ छपती थीं। अपनी बातों की पुष्टि के लिए रामायण की पंक्तियाँ उनके मुहावरे थे। मेरे पिता भी उद्भट विद्वान थे। मेरा घर मेरा विद्यापीठ था। किताबों की पूरी दूनिया थी। प्रेमचंद, शरतचंद्र, टैगोर, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, माखनलाल चतुर्वेदी, सोहनलाल द्विवेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सुब्रमण्यम भारती, मैथिलीशरण गुप्त के साथ ही शेक्सपीयर, रूडयार्ड किपलिंग, सॉमरसेट मॉम, वर्ड्सवर्थ, शेली, कीट्स आदि की रचनाओं से हमारा परिचय किशोरावस्था में हो चुका था।
बाद में अन्नपूर्णा राँची नगरपालिका की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। बीस वर्षों तक इस पद पर रहीं। वे राँची नगर की सफाई, खासकर पार्कों की सफाई पर विशेष ध्यान देती थीं। वह पूरे शहर की सफाई इस तरह करवाती थीं, जैसे कोई गृहिणी अपने घर का। अँगुलियों पर गिनाने पर राँची में बिरसा मुंडा के बाद अन्नपूर्णा सिन्हा का नाम आना चाहिए/जगहों की भी अपनी धड़कन होती है। इन धड़कनों में वह हमेशा मौजूद रहेंगी। इन कारणों से उनको बहुत से हक मिल गए थे। उन्हें जो भी कहना होता स्पष्ट रूप से कहतीं। साथ ही वह सद्गृहस्थ भी थीं। उन्हीं से सीखा कि गृहस्थी और घर के बाहर किया जाने वाला सत्कर्म एक-दूसरे के पूरक होते हैं, विरोधी नहीं। वह अपने अंतिम समय तक पढ़ती रहीं। पढ़कर वे पुस्तक का मूल्यांकन करतीं, उस पर अपने विचार व्यक्त करतीं। वे सरल, निष्कपट और सुनहरे स्वप्न देखने वाली महिला थीं।
उस साम्राज्यवादी गोरी हुकूमत ने अन्याय एवं अत्याचार की सारी सीमाएँ लाँघ दी, लेकिन अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाईं। आखिरकार 15 अगस्त 1947 का दिन आ गया। माँ मुजफ्फरपुर में थी। पिता जी वहीं सब जज थे। उस दिन सुबह से बादल छाये थे। शाम तक बारिश होने लगी। वह जागते रहने वाली रात थी। अर्द्धरात्रि में बारह का घंटा बजते ही ब्रिटिश साम्राज्य का यूनियन जैक दिल्ली के लाल किले से उतरा और भारत का तिरंगा झंडा फहराने लगा। जब जवाहर लाल नेहरू ने देश की आजादी का ऐलान किया तो उनकी आवाज भारतवासियों के दिल में उतर गई। कितने शहीद हुए, कितनों ने कुर्बानियाँ दी, उस दिन का सपना देखते हुए जब हिंदुस्तान आजाद होगा। वह दिन आ गया। चारों ओर देश भक्ति के गीत बज रहे थे–
‘विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊँचा रहे हमारा,
शान न इसकी जाने पाये, चाहे जान भले ही जाए…’
इसके कवि श्यामलाल पार्षद को कोई जानता हो या न हो इस झंडागीत को पूरा देश जानता है।
ये सब कहते हुए माँ के चेहरे पर एक खास तरह की आश्वस्ति का भाव उपस्थित होता, जो उनके सौम्य मुस्कान में घुलता हुआ उस गौरवशाली अतीत की स्मृतियों में विलीन हो जाता। वे बातें अब नहीं रहीं। धीरे-धीरे जमाना बदलता गया। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं होता। परिवर्तन समय की आवश्यकता है। वर्तमान हमारे निकट होता है कि हम उसके प्रति आलोचनात्मक रूख अपना लेते हैं। वही जब बीत जाता है तब अधिक गौरवपूर्ण मालूम होता है। अपने युग से असंतोष स्वास्थ्य का लक्षण हैं, वरना हम आत्मतृष्ट हो जाएँगे तो नया सृजन कैसे करेंगे। लेकिन बलिदानों की परंपरा हमारी विकास यात्रा को हमेशा रौशन करेगी, प्रेरणा देगी, वंदे मातरम्!
Image :By the Canal, Venice
Image Source : WikiArt
Artist :Marcus Stone
Image in Public Domain