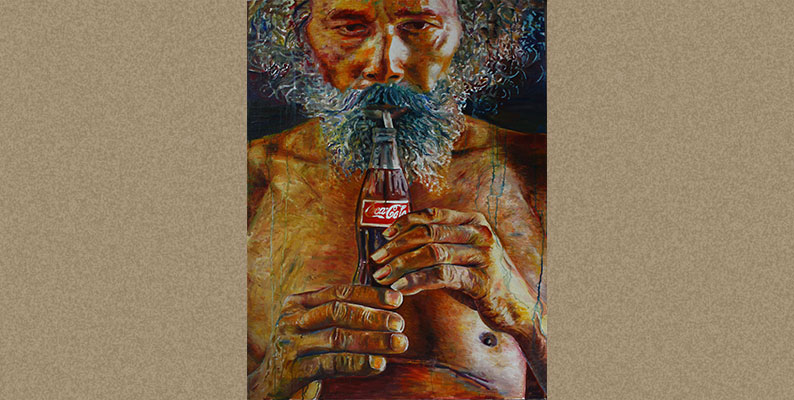रामदरश मिश्र के आरंभिक उपन्यास
शेयर करे close
शेयर करे close

शेयर करे close
- 1 October, 2023
रामदरश मिश्र के आरंभिक उपन्यास
रामदरश मिश्र की औपन्यासिक यात्रा सुदीर्घ और वैविध्यपूर्ण है। यदि उनकी केंद्रीय लेखन विधा के बारे में बातचीत की जाए तो यह कहना होगा जितने अच्छे वह कवि हैं, उतने ही बड़े कथाकार और उपन्यासकार हैं। ‘पानी के प्राचीर’ से लेकर ‘एक था कलाकार’ तक उन्होंने जिस शिद्दत से उपन्यासों की रचना की है वह काबिले गौर है। जिस समय वे उपन्यासों की दुनिया में आए, उस समय आंचलिक उपन्यासों की धूम थी। उसमें भी आज़ादी के बाद के मोहभंग को लेकर आंचलिक किस्सागोई को बड़े फलक पर रखने वाले उपन्यास ‘मैला आँचल’ के कारण रेणु चर्चा में थे। रामदरश जी के उपन्यास संसार में हम प्रवेश करें तो देखते हैं कि ‘पानी के प्राचीर’ की आंचलिकता हमें छूती है तो ‘जल टूटता हुआ’ में यथार्थ जीवन के प्रतिबिंब हमें विचलित करते हैं। ‘अपने लोग’ सामाजिक अंतर विरोधों की गाथा है तो ‘सूखता हुआ तालाब’ मानवीय प्रतिश्रुतियों का विन्यास। ‘रात का सफर’ मानवीय यातना की गाथा और उससे उबरने की दास्तान है तो ‘बिना दरवाजे का मकान’ शहर में रह रही कामवालियों की मार्मिक दास्तान। ‘दूसरा घर’ में गुजरात का आत्मीय परिवेश और पूर्वांचलियों का दर्द समाहित है तो उस मिट्टी की आभा और ऊष्मा भी जिसके ताप में उत्तप्त होकर जीवन की एक भरी-पूरी कहानी लिखी जाती है। ‘थकी हुई सुबह’ में एक अकेली स्त्री के जीवन संघर्ष को जिस तरह से लेखक हमारे सामने रखता है उसे हम गाँव के बदलते स्त्री चरित्र के रूप में इस उपन्यास की नायिका में उभरता हुआ देख सकते हैं। ‘बीस बरस’ बदलते हुए गाँव की गाथा है तो आधुनिकता के तमाम छद्म के बावजूद गाँव आज भी तमाम बुनियादी अभाव में जीने के लिए किस तरह तरस रहे हैं इस बात की तस्दीक भी यह उपन्यास करता है और इस बीच गाँव में करवट लेने वाली नई संवेदनात्मक आधुनिकता भी इसके माध्यम से सामने आती है। अपने उत्तर जीवन में उन्होंने कई छोटे और अपनी पत्नी और पुत्र हेमंत की याद में भी उपन्यास लिखे हैं। औपन्यासिक कथा के आयाम की दृष्टि से वे बेशक लघु उपन्यासों की श्रेणी में परिगणित हों, और उपन्यास कला की दृष्टि से थोड़े कमतर हों लेकिन उपन्यास के माध्यम से उन्होंने जिस तरह से निरंतर बदलते ग्रामीण यथार्थ और आधुनिक भारत की विडंबना और शहरी आधुनिकता के छद्म को उजागर किया है, वह अपने आप में उल्लेखनीय है, उनकी अथक जिजीविषा और रचना सक्रियता का साक्ष्य तो है ही।
‘पानी के प्राचीर’ रामदरश मिश्र का पहला उपन्यास है, जो 1961 में आया। उसके लिखने के पीछे ‘मैला आँचल’ जैसे आंचलिक उपन्यासों की सबल प्रेरणा रही है। यदि रेणु की कथा भूमि फारबिसगंज, बिहार का इलाका रहा है तो रामदरश मिश्र के लिए राप्ती और गोर्रा नदियों से घिरा एक ऐसा पूर्वांचल है जहाँ आज़ादी के लिए संघर्ष करते गाँव और वहाँ की उजाड़ स्थितियाँ हैं। गाँव को अपनी किस्सागोई का माध्यम बनाने वाले कई कथाकार हैं। प्रेमचंद, रेणु, विवेकी राय इत्यादि इसी कोटि के कथाकार हैं। रामदरश मिश्र अपनी किस्सागोई के लिए गाँव के मौजूदा और बदलते यथार्थ को उपन्यास की विषय-वस्तु बनाते हैं। आज़ादी का मोहभंग ‘मैला आँचल’ में भी है और ‘पानी के प्राचीर’ में भी। कहा जाए तो बिहार और उत्तर प्रदेश के ग्रामीणों के संघर्ष में कोई बहुत ज्यादा अंतर भी नहीं है।
इस उपन्यास पर लिखते हुए प्रभाकर माचवे मानते हैं कि ‘बलचनमा’ और ‘मैला आँचल’ की तरह इसका विज्ञापन नहीं हुआ, पर यह एक तगड़ी कलाकृति है। ‘पानी के प्राचीर’ की कहानी में पांडेपुर गाँव के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले संघर्ष और इस संघर्ष से और छोटे-मोटे परिवर्तनों से गुजरते हुए गाँव हैं। एक तरफ राप्ती और गोर्रा नदियों की हाहाकारी बाढ़ है, दूसरी तरफ गाँव में विभिन्न संप्रदाय और चरित्र अपनी-अपनी तरह से पानी के प्राचीर की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। पांडेपुर गाँव भी अन्य गाँवों की तरह ही अंधविश्वास, शोषण, ऊँच-नीच, नए-पुराने मूल्यों के संघर्ष, बाढ़ से गुजरते कछार के दुख-दर्द का केंद्र है। बाढ़ में गाँव के लोगों की फसलें डूब जाती हैं और इससे पैदा अभाव और आर्थिक किल्लत में गाँव वालों को जिंदगी बितानी पड़ती है। इस उपन्यास में अनेक पात्र हैं जो बहुत ही जीवंत हैं। जिन्होंने गाँव में कभी जीवन बिताया है, वे जानते हैं कि होली में किस तरह शरारती लोग गाँव-घर की लकड़ी या खटिया-मचिया उठाकर होलिका के हवाले कर देते हैं। रामदीन जैसे सत्याग्रही की झोपड़ी को जब लोग आग के हवाले कर उनकी चारपाई को होलिका पर डाल देते हैं तो जैसे वे ठान लेते हैं कि हम तो अब यही जलेंगे। इससे बढ़िया चिता कहाँ मिलेगी।
पांडेपुर की कहानी गरीबी और अभावों से संघर्ष की कहानी है, किसानों के संघर्ष की कहानी है, फसल के डूबने की कहानी है, राजनीतिक रूप से घायल लोगों के शोषण की कहानी है। इसमें गाँव का भी टीसुन ‘भज लो रामचंद्र का नाम’ कहकर भीख माँगता है तो कल्लू पांडे और रघु बड़े महात्मा का वेश धारण करके जनता को ठग रहे हैं। लेकिन टीसुन जहाँ गाली खाता है वहीं कन्नू पांडे को आदर और सम्मान सब कुछ मिलता है। इसी गाँव का नीरू दुख-दर्द से निराश नजर आता है। नीरू का जीवन भी संघर्ष भरा है। पांडेपुर गाँव के भीतर छोटी-बड़ी जातियों में यौन संबंधों को लेकर अनेक तरह की चर्चाएँ व्याप्त हैं। कहीं स्वेच्छा से, कहीं आर्थिक विवशता वश। यूँ तो ऊँच-नीच में पूरा गाँव ही विभाजित है, लेकिन बिंदिया चमारिन को लेकर उच्च जातियों में भी वही ललक है। पूरा गाँव उसके पीछे पागल है। वह इस विडंबना पर धिक्कारती हुई कहती है, इन छोकरों और बूढ़े बैलों की आसक्ति केवल मेरी देह के लिए है। अँधेरे में उसे चूस कर यह बामन लोग उजाले में पंडित बने घूमेंगे और उसकी छाया से भी बचने की कोशिश करेंगे। किस तरह इन्हें सच्चाइयों का एक पूरा परिदृश्य ही पांडेपुर में नजर आता है, जहाँ औरतें भी शरीर हैं कि एक दूसरे की पोल खोलने में लगी हैं। इस तरह गाँव जो कभी सदाशयता और सामाजिकता का केंद्र था, बदल रहा है, मूल्य टूट रहे हैं। पंचायत के मुखिया और सरपंच ने पुलिस को अपने गिरोह का अंग बना रखा है। पांडेपुर के मुखिया कुबेर पांडे पुलिस के दलाल बन जाते हैं और अपने ही गाँव के लोगों को हवालात में भिजवाने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ते। राजनीतिक चेतना से अनुप्राणित पांडेपुर में देखता हूँ, कुछ लोग गाँधीवादी प्रकृति के लोग भी हैं जो जुलूस निकालकर गाँव में अँग्रेजों के खिलाफ जागरण की मुहिम चलाते हैं, जिसमें ग्राम भटौली के नेता गनपति हरिजन नेता फेकू, निर्बल तेली, दधिबल यादव और विक्रमगढ़ हैं जो एक तरह की सुराजी चेतना का प्रचार-प्रसार कर रहे हैं। नीरू भी इसी चेतना का प्रसारक बना हुआ है जिसके भीतर राष्ट्रीय चेतना आंदोलित है। लेकिन जमींदार लोग प्रतिक्रियावादी शक्तियों के मुखिया हैं जो अँग्रेजों से मिलकर आम जनता का शोषण करने में लगे हैं, लेकिन कहीं-न-कहीं गाँधी जी का आंदोलन इसी तरह गाँव-कस्बों में फैल रहा है कि लोग गाँधी जी के कथन को याद कर कहते हैं कि ‘सुराज मिलने पर कोई भूखा नहीं रहेगा’ लेकिन राजनीतिक चेतना जगाने के बावजूद फेकू जैसे लोग बहुत असहाय जीवन जीते हैं। वे आए दिन जमींदारों से पिटते और मुखिया से अपमानित होते रहते हैं।
‘पानी के प्राचीर’ की भाषा में अचूक किस्सागोई है। गाँव का बहूकोणीय यथार्थ है। अनेक चरित्र अपनी तरह-तरह की भंगिमा से इस किस्सागोई को जीवंत बनाते हैं। बाढ़ के दृश्य को बहुत जीवंतता से लेखक ने प्रस्तुत किया है, क्योंकि इस विभीषिका से वह गुजर चुका है। यह उसके अनुभव की कथा है। जहाँ तक आंचलिकता का सवाल है, रेणु के ‘मैला आँचल’ की राह पर चलता हुआ यह उपन्यास पूर्वांचल के कछार की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक हालात का जायज़ा लेता हुआ एक ऐसा उपन्यास बन गया है जहाँ आज़ादी के पूर्व और आज़ादी के बाद का सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्ष हमारे सामने आता है। आज़ादी के सच्चे नायक और गाँधी में विश्वास करने वाली पीढ़ी यहाँ है तो अँग्रेजों के दलाल बने जमींदारों और अँग्रेजी राज मैं चापलूसी के जरिये और आज़ादी आने पर आज़ादी के प्रतिफल की लूट-खसोट में शामिल लोग भी हैं। इस तरह एक गाँव के भीतर यथार्थ की अनेक परतों को उघारता उपन्यास अपने दौर का एक बड़ा उपन्यास बन गया है और पहला उपन्यास होने के बावजूद रामदरश मिश्र जी की कीर्ति में चार चाँद लगाने वाला उपन्यास सिद्ध हुआ है।
इसी परिपेक्ष्य का एक बड़ा उपन्यास ‘जल टूटता हुआ’ भी है जो कि आज़ादी के बाद के मोहभंग का जीता-जागता चित्रण है। यह उपन्यास भी कहा जाए तो ‘पानी के प्राचीर’ की तरह आंचलिक और उसका पूरक उपन्यास है जो उसी तरह बाढ़ की भयावहता के बीच गाँव-जवार की स्थितियों को रेखांकित करता है। उसकी आंचलिक विशेषताओं के साथ उस परिदृश्य को एक बार फिर उपन्यास के पन्नों पर जीवंत करता है। हिंदी में प्रेमचंद के बाद किसान, मजदूर और ग्रामीण जीवन पर जो उपन्यास लिखे गए उनमें ‘सती मैया का चौरा’ और ‘बीज’ जैसे उपन्यास हैं तो ‘अलग-अलग वैतरणी’ और ‘सोना माटी’ जैसे उपन्यास भी। रामदरश मिश्र के उपन्यास इसी तरह पूर्वांचल की दुरवस्था का जायज़ा लेने वाले उपन्यास हैं; ‘जल टूटता हुआ’ जिनमें प्रमुख है। आज़ादी के बाद गाँव-देहात को अगर समझना है, किसानों के मध्य वर्ग को समझना है, गरीब किसानों की हालत का जायज़ा लेना है, शिक्षा, बेरोजगारी, गरीबी, छुआछूत, ऊँच-नीच, घात-प्रतिघात का जायज़ा लेना है, या आज़ादी के बाद पूर्वांचल के गाँव की तस्वीर देखनी है, उनका सामाजिक, आर्थिक यथार्थ कैसे बदला है, कैसे सब कुछ बदल जाने का वजूद किसानों का जीवन बदहाल है, बदलाव की बयार बहने और आज़ादी मिलने के बावजूद आज़ादी का प्रतिफल लोगों तक नहीं पहुँचा, इसका जायज़ा लेना हो तो ‘जल टूटता हुआ’ एक बेहतरीन उपन्यास है। इस उपन्यास में मास्टर सुगन का कथन है जो वे 15 अगस्त के समारोह से लौटते हुए कहते हैं, ‘इतने साल हो गए आज़ादी मिले। यह अभागी जिंदगी टस-से-मस नहीं हुई। यही वह दौर है जब धूमिल लिख रहे थे–
‘आज़ादी क्या तीन थके हुए रंगों का नाम है
जिसे एक पहिया ढोता है
या इसका कोई और मतलब होता है?’
इस दौर का साहित्य मोहभंग का साहित्य है जिसे साठोत्तर लेखन कहा जाता है। साठोत्तर मोहभंग की छाया रामदरश मिश्र के प्रारंभिक दोनों उपन्यासों पर है। यही मोहभंग ‘मैला आँचल’ की कथावस्तु में भी है।
लोग सोचते थे कि आज़ादी के बाद स्वराज्य स्थापित होगा, भूमिहीनों को जमीन मिलेगी, बाढ़ में डूबी धरती को कोई समाधान मिलेगा, लेकिन इसी उपन्यास का एक चरित्र रामकुमार कहता है–‘सरकार ने क्या किया। आज भी बेगार जारी है, मजदूरों को मजदूरी नहीं, पेट भर खाने को अन्न नहीं, बच्चों को शिक्षा नहीं, हरिजनों को जमीन नहीं, दस गुना लगान…यही है आज़ादी का मतलब?’ आज़ादी के बाद जमींदारों का जो चरित्र सामने आया वह बहुत ही आश्चर्यजनक था। कहते हैं जमींदार जो अँग्रेजों के दौर में गरीबों और किसानों के शोषक थे, काँग्रेस के खिलाफ अँग्रेजी राज के दलाल थे, आज़ादी के बाद जब सत्ता काँग्रेस के हाथ आई तो वे रातों-रात काँग्रेसी बन बैठे और आज़ादी की तमाम योजनाओं में हिस्सेदार बने। विधायक बने, सांसद और मंत्री बने। अपना दबदबा कायम रखा। इस तरह जो राजनीतिक परिवर्तन गाँव में आया उसके कुफल भी सामने आए। खद्दर पहनने वालों का चरित्र सामने आया। इस विडंबना को ‘जल टूटता हुआ’ जैसा उपन्यास एक सबल स्वर देता है। ‘जल टूटता हुआ’ बारिश से बाँध टूटने का ही एक मार्मिक रूपक है जो इस उपन्यास के शीर्षक से ही व्यक्त होता है। बारिश से चूते घरों की क्या हालत होती है यह वंशी तिवारी के घर से पता चलता है जहाँ सभी जगह पानी चू रहा है। न चूल्हा बचा है, न राशन पानी महफ़ूज़। आज आज़ादी के 75 सालों के बावजूद जिस तरह हमारे समय में बाढ़ आपदाएँ हैं, जिस तरह हमारे यहाँ आज सांप्रदायिकता सिर उठा कर बोल रही है, उस लिहाज से आज़ादी के तुरंत बाद का समय भी उसी तरह की लूट-खसोट और अराजकता का रहा है और इस दृष्टि से उस समय का समाज भी अपनी तरह से कम खतरनाक नहीं रहा है। इस लिहाज से इस ऐतिहासिक विडंबना को लेखक ने जिस तरह अपनी उपन्यासों में उसे सहेजा है वह अपने आप में एक मिसाल है। ‘जल टूटता हुआ’, ‘पानी के प्राचीर’ की तरह ही एक महत्वपूर्ण उपन्यास है जो कि अगर हम कहें तो अपनी भाषा-शैली और अपने संवादों के कारण आंचलिकता के वैशिष्ट्य में समाहित होता है। राजनीति धीरे-धीरे गाँव को किस तरह आच्छादित करती रही हैं इसे देखना हो तो ग्रामीण पृष्ठभूमि के ऐसे उपन्यासों में देखा जा सकता है। रामदरश जी ने ऐसा कोई कोना नहीं छोड़ा है शोषण का, लाभ-लोभ का, ऊँच-नीच का, छद्म राजनीति का, छद्म यथार्थ का, छद्म आदर्श का जिस पर उनका ध्यान न गया हो। कुछ सकारात्मक पहलू भी इसमें हैं। तभी प्रसिद्ध आलोचक वेद प्रकाश अमिताभ यह मानते हैं कि ‘यह उपन्यास ग्रामीण जीवन का व्यापक श्वेत पत्र है।’
रामदरश जी के अन्य उपन्यासों में ‘बीच का समय’, ‘आकाश की छत’ यह दो महत्वपूर्ण उपन्यास है, लेकिन इससे अलग एक उपन्यास और है ‘अपने लोग’ जो रामदरश जी के बेहतरीन कुछ उपन्यासों में गिना जाता है। गाँव के प्रति नॉस्टैल्जिक किस्म की भावुकता भी रामदरश मिश्र के अंदर है और रही है लेकिन इसी उपन्यास में एक जगह ‘अपने लोग’ के मुख्य चरित्र प्रमोद को लगता है कि भावुकता उसकी जिंदगी की शक्ति है। जहाँ तक आज के गाँव की स्थिति है, कहना न होगा कि गाँव अब नर्क हो गए हैं। हर आदमी एक दूसरे से कटा-कटा सा दिखता है। ‘अपने लोग’ के केंद्र में गोरखपुर जैसा शहर है। हालाँकि इसी उपन्यास का एक पात्र प्रमोद गोरखपुर को भिखारियों और कोढ़ियों का देश कहता है जहाँ वैचारिक और राजनीतिक प्रदूषण मनुष्यता को पीड़ित कर रहे हैं। यह हाल किसी एक शहर की न होकर पूरे देश की है। लेकिन यही पात्र जब एक जगह कहता है कि ‘सेवा यही है कि तुम पास थोड़ी देर बैठो और इस एहसास को मरने न दो कि आत्मीयता कहीं जीवित है’ तो लगता है कहीं-न-कहीं उस वक्त की पीढ़ी में मूल्यों से टकराने की एक शक्ति थी। ‘अपने लोग’ के प्रमोद को देखें तो जैसे लगता है उपन्यासकार के व्यक्तित्व की छाया उसमें दिखाई देती है। वह खुद को मार्क्सवादी भी कहता है लेकिन बाहर एक नए शहर में अध्यापक के रूप में आया है तो वहाँ की गुंडई के विरुद्ध, खराब व्यवस्था के प्रति, कवि सम्मेलन इत्यादि में उमेश जैसे प्रतिभाशाली कवि के साथ की जाती ज्यादती को लेकर वह आहत होता है और जहाँ कहीं आवश्यकता पड़ती है वह उसकी सहायता करता है। कहा जाय तो ये सच्चे अर्थों में वही मार्क्सवादी हैं, वरना मार्क्सवाद का लेबल लगाने वाले कितने हैं जो केवल फैशनपरस्त मार्क्सवादी हैं। यहाँ तक कि वह अपने बेटे से भी कहता है कि ‘तुम एक सच्चे मार्क्सवादी बनो, किताबी मार्क्सवादी नहीं।’ ‘अपने लोग’ एक तरह से एक व्यापक युगबोध की कथा है। तत्कालीन व्यवस्था और लचर जीवन समाज और उसके अर्थतंत्र की कथा है।
‘अपने लोग’ का समर्थ नायक प्रमोद है जो यह बख़ूबी जानता है कि इस शहर और गाँव की राजनीति एक और क्या खराबी पैदा की है जहाँ जनता को सारे दल फुटबॉल की तरह किक मारते हैं। वह कई जगह निराश भी होता है लेकिन अपने आप में एक मूल्यवान संभावना बनकर उपस्थित होता है। वह जानता है कि जिस दिन इस संभावना को सही नेतृत्व और दिशा मिल जाएगी, बेहतरीन परिवर्तन समाज में आ सकेगा। प्रमोद के वैचारिक उच्च आदर्श उसी तक सीमित नहीं है बल्कि पवन और उसकी नई पीढ़ी तक यह विचारधारा इन्हें नए सपने और बदलाव के सपने देखने के लिए बाध्य करती है। पवन को गोरखपुर शहर और उसके लोग अच्छे लगते हैं। बहुत सारे सवालों के साथ इस उपन्यास में रागात्मक क्षण भी हैं जो बिलाल और मंजरी, उमेश और माधवी, के लाल और इमरतिया के माध्यम से प्रकट हुए हैं। लेकिन इस उपन्यास का एक त्रासद प्रसंग उमेश का है जो कि इस व्यवस्था में पागल होता है। प्रमोद की चिंता उमेश को लेकर बहुत सघन है। इस समाज में कुछ पुरातन पंथी जैसे लोग भी हैं जो शास्त्र और वेद के हवाले से रूढ़ परंपराओं के अनुसरण करने तक सीमित हैं। लेकिन इस रूढ़ और प्रतिक्रियावादी सोच का विरोध उपन्यास में सर्वत्र हुआ है। इस उपन्यास का अंत कुछ आकस्मिक जरूर है लेकिन इंकलाब जिंदाबाद जैसे नारों के साथ जब मजदूर सम्मुख खड़े होते हैं तो लगता है कि प्रमोद जैसे लोगों का सपना अप्रासंगिक नहीं है। कहीं-न-कहीं बदलाव की बयार ऐसे शहरों में बह रही है।
‘सूखा हुआ तालाब’ के कथ्य में कहीं-न-कहीं ‘जल टूटता हुआ’ की छाया भी नजर आती है। एक बार फिर गाँव को अपने उपन्यास के केंद्र में रामदरश जी ने रखा है, लेकिन यहाँ भी देव प्रकाश को गाँव से पलायन करना पड़ता है जो इस बात का संकेत है–गाँव से धीरे-धीरे उन सारी शक्तियों का पलायन हो रहा है, जो गाँव को एक दिशा दे सकती थीं। रोजी-रोटी के चलते गाँव बौद्धिक मेघा से विपन्न नजर आते हैं। लेकिन आज की स्थिति में भी इसका कोई उपचार नहीं है। सारी स्थितियाँ, सारे विकास शहर केंद्रित होकर रह गए हैं। छोटे कस्बों और नगरों की कोई औकात नहीं रह गई है कि वे लोगों को उनकी योग्यता के अनुरूप काम दे सकें और सरकार की विकास योजनाओं का लाभ जन-जन को मिल सके। ‘सूखता हुआ तालाब’ का शीर्षक ही इस अवसाद और निराशा का सूचक है।
रामदरश जी के कुछ अच्छे उपन्यासों में ‘दूसरा घर’ की गणना भी होती है। यह संभवत तब की रचना है जब रामदरश जी दिल्ली आ चुके थे और उस दूसरे घर की उन्हें याद ज्यादा ही सताती थी जहाँ उन्हें बहुत आत्मीय प्रेम मिला, उनके संघर्ष को शक्ति मिली, उनकी कल्पना को प्रशस्त व्योम मिला तो कुछ दुखदाई प्रसंग भी उनके जीवन में रहे। गुजरात में बिताए हुए लगभग 8 वर्षों की इस कथा में हमारे समय का शिक्षा तंत्र है और एक तरह से गुजरात उनका ‘दूसरा घर’ भी है लेकिन जिन परिस्थितियों में मिश्र जी ने गुजरात छोड़ा था, लगभग बुरी हालात में इस उपन्यास का नायक डॉ. गौतम गुजरात से विदा होता है। बहुत योग्य अध्यापक है वह, लेकिन उसे तमाम तरह की त्रासदियों का शिकार होना पड़ता है जो शिक्षा तंत्र की व्याधियों की उपज है। लेकिन डॉ. गौतम में एक तरह का विद्रोही तेवर है जो इस खराब व्यवस्था को स्वीकार नहीं करता।
हालाँकि यह उपन्यास केवल शिक्षा जगत की समस्याओं पर ही आधारित नहीं है, बल्कि उत्तर भारतीय कर्मठ नागरिकों के जीवन पर भी आधारित है जो रोजी-रोटी के निमित्त गुजरात में आ बसे हैं। गाजीपुर, जौनपुर, देवरिया, गोरखपुर आदि जिलों से आए हुए प्रवासी नागरिक जो गुजरात में एक तरह की आत्मीयता और जीविका की तलाश में आए हुए हैं। जाहिर है कि इस उपन्यास के नायक के रूप में वे लोगों के बीच आत्मीयता महसूस करते हैं लेकिन वह जानते हैं यहाँ भी जमींदार-मजदूर, सवर्ण-अवर्ण, ऊँच-नीच का भेद है। यहाँ भी झोपड़-पट्टियाँ हैं, यहाँ भी निम्न स्तर का जीवन यापन करते मजदूर हैं, जो संगठित नहीं हैं। हाल के बरसों में हिंदू और मुसलमान को लेकर जिस तरह सांप्रदायिक तनाव व्याप्त रहा है इसकी छाया ‘दूसरा घर’ में भी है लेकिन फिर भी ऐसे समय असलम और रहमतुल्ला जैसे लोगों का होना आश्वस्त करता है की नफरत की दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं।
जैसा कि उनके प्रारंभिक दो उपन्यासों में आंचलिक शब्दावली की मौजूदगी है, इस उपन्यास में उससे भरसक बचा गया है। इस उपन्यास में डॉ. गौतम, रहमान, शंकर, कमलेश और विनोद सभी की यह समस्या है कि वे इस नई जगह पर अपने पाँव कैसे टिकाएँ। अहमदाबाद की मजदूर बस्तियों के जीवन की झलक भी उपन्यास में है, लेकिन एक तरह से यह उपन्यास विस्थापित लोगों की कहानी भी है जहाँ अनैतिक आचरण में लिप्त गंगाराम शास्त्री जैसे लोग फल-फूल रहे हैं जो शिक्षा संस्थानों के संचालक हैं, अनेक स्त्रियों के साथ अनैतिक संबंध है, स्त्रियों के चीरहरण में कुशल हैं, स्थानीय नेताओं के संपर्क में है और येन केन प्रकारेण चुनाव लड़ कर वे राज्य के शिक्षा मंत्री भी बन जाते हैं। इस उपन्यास का पात्र शंकर इस बात से दुखी होता है कि क्या विडंबना है कि ‘शास्त्री जी जैसे लोग हर जगह धक्का मारकर अपनी जगह बना लेते हैं और पत्थर के ऊपर भी झंडा गाड़ देते हैं और डॉक्टर गौतम जैसे लोग विस्थापित होने के लिए अभिशप्त हैं।’
सच कहा जाए तो इस उपन्यास के केंद्र में रामदरश जी खुद हैं जो डॉ. गौतम के रूप में नजर आते हैं, जहाँ उन्हें अपने अस्तित्व के लिए, अपनी नौकरी के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। एक कॉलेज से उन्हें अपने आपको अलग करना पड़ा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा यह गुजरात अहमदाबाद और नवसारी की कथा भी है, जहाँ रामदरश मिश्र जी को बहुत स्नेह मिला। रघुवीर चौधरी जैसे शिष्य मिले और अन्य शिष्यों की बड़ी लंबी कतार रही है जिसकी चर्चा करते हुए आज भी वे ऐसे लोगों को नहीं भूल पाते। ‘दूसरा घर’ जहाँ उपन्यासकार का भी दूसरा घर है, डॉ. गौतम का भी दूसरा घर है; वहीं पर इस दूसरे घर में अपमानकारी अनेक स्थितियाँ भी रही हैं जिनसे रामदरश जी को स्वयं और इस उपन्यास के नायक गौतम को भी बार-बार गुजरना पड़ा है। उपन्यास परवासियों के दर्द से भरा हुआ भी है। इस तरह यह पराई पीड़ा का नहीं, आत्मपीड़ा का दस्तावेज भी है।
Image : After Rain, at Băneasa
Image Source : WikiArt
Artist : Stefan Luchian
Image in Public Domain