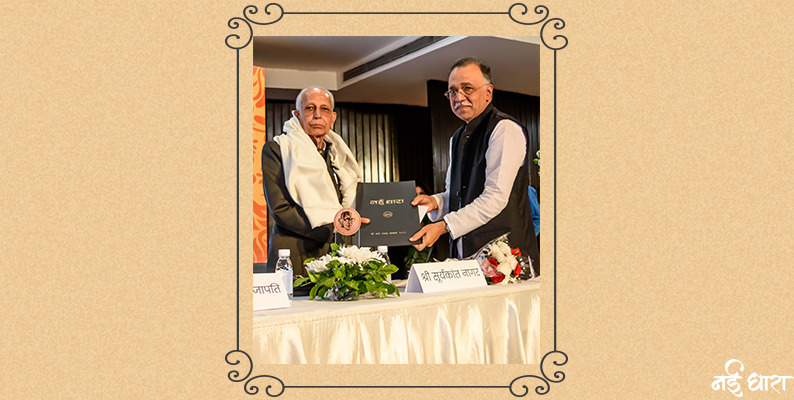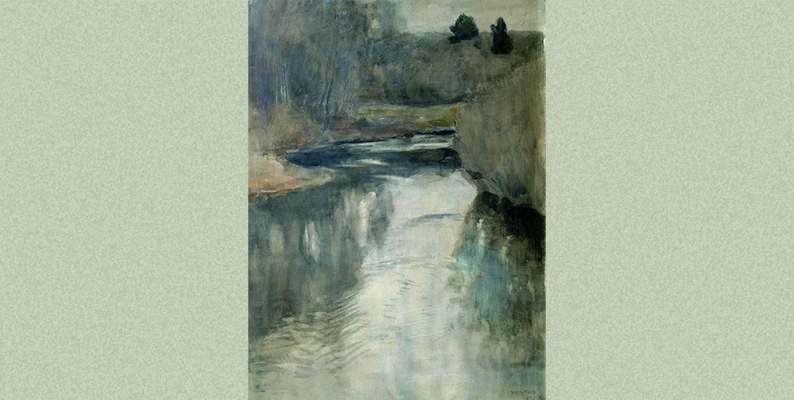एक अन्वेषी कवि की काव्य दृष्टि – ‘अज्ञेय’
- 10 April, 2025
शेयर करे close
शेयर करे close
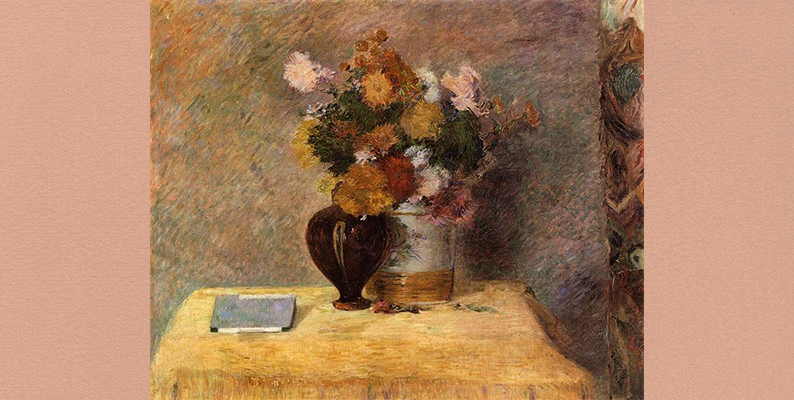
शेयर करे close
- 10 April, 2025
एक अन्वेषी कवि की काव्य दृष्टि – ‘अज्ञेय’
अज्ञेय जी से केवल एक बार भेंट हुई थी। चालीस वर्ष पूर्व जब वे इंदौर आए थे। निरंजन जमींदार के आवास पर। एयरपोर्ट से (उन दिनों गिनती की ही फ्लाइट थीं) लाने का दायित्व इंदौर नगर निगम के सहायक आयुक्त के.सी. जैन को सौंपा गया था। जैन साहब ने बताया था कि रास्तेभर अज्ञेय जी ने कोई बातचीत नहीं की। बाद में हमलोगों ने भी महसूस किया कि वे अंतर्मुखी हैं। बहुत कम संवाद करते हैं। आत्म केंद्रित साहित्यकार थे। बाहरी-सामाजिक गतिविधियों के रुपायन में उनकी रुचि नहीं थी। मेरा उनसे असल परिचय तो ‘दिनमान’ के संपादक के रूप में था। ‘दिनमान’ मेरी अत्यंत प्रिय पत्रिका थी। अज्ञेय की संपादन दृष्टि और कौशल से बहुत प्रभावित था। राजनीति, कला, फिल्म, साहित्य और समीक्षा का इतना उत्तम गठजोड़ होता था कि दिल-दिमाग डूबा रहता था। कला के प्रति रुझान पैदा करने का श्रेय साहित्य और कला को समर्पित दिनमान के पृष्ठों को है। दिल्ली में होने वाले नाटकों की समीक्षा में मेरी विशेष दिलचस्पी होती थी, क्योंकि एन.एस.डी. के समाचारों के अलावा, ‘दिनमान’ में ओम शिवपुरी और सुधा शिवपुरी की नाट्य प्रस्तुतियों की समीक्षाएँ छपती थीं। ‘दिनमान’ के तमाम अंक मैंने सहेज कर रखे थे, जो पिछले दिनों ही निकाले। राजनीतिक के समाचारों की ‘दिनमान’ में छपी समीक्षात्मक टिप्पणियों को पढ़ते रहने का लाभ यह हुआ कि वर्ष 1971 में लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में काँग्रेस की हार के कारणों को तलाशने के लिए ‘नई दुनिया’ द्वारा आमंत्रित लेखों में मेरे लेख को सर्वश्रेष्ठ माना गया।
इसके बाद अज्ञेय के साहित्य को पढ़ने के प्रति रुचि बढ़ती गई। उनके उपन्यास ‘शेखर एक जीवनी’, ‘नदी के द्वीप’, ‘अपने-अपने अजनबी’ और संपूर्ण कहानियों का दूसरा खंड तो पढ़ा ही, उनकी काव्य-कृतियों का आस्वाद भी लिया। उनकी प्रारंभिक रचनाओं के बाद तार सप्तकों के संपादक ने उन्हें विशेष प्रतिष्ठा दिलाई। इनमें हिंदी कविता की साहित्यिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के अतिरिक्त नई कविता की सामर्थ्य को भी रेखांकित किया गया। माना जाता है कि चौथा सप्तक तुलनात्मक रूप से अज्ञेय का कमजोर चुनाव था, जिसमें कुछ हाशिये के कवि शामिल हैं। पता नहीं किन पूर्वाग्रहों की वजह से संकलन में नागार्जुन, त्रिलोचन, श्रीकांत वर्मा जैसे कविगण नजरअंदाज कर दिए गए!
अज्ञेय की एक लंबी (चौदह पृष्ठों में समायी) कविता ‘असाध्य वीणा’ है। यह जून 1961 में अल्मोड़ा में लिखी गई थी। यह कथा आधारित काव्य रचना है। माना जाता है कि यह चीन और जापान की एक लोक कथा पर आधारित है। यह एक तरु की कथा है। ऋषितुल्य इस देव वृक्ष ने वीणा के रूप में जन्म लिया है। वीणा में बसी है वृक्ष की आत्मा। न वह वृक्ष साधारण था न उससे निर्मित वीणा और न उसमें अंतर्निहित संगीत ही साधारण था। सोए हुए संगीत को जगाना ‘साधना’ का काम है। असाधारण साहस का काम। वीणा सोई हुई है पर नींद में भी उसे अपने साधक की प्रतीक्षा है। उसे पता है कि सोया हुआ संगीत उनकी निजी संपत्ति नहीं है। वह सामाजिक है। वह उन लोगों से नहीं बजेगी जो दुनियादारी के जंजाल में फँसे हैं। दरअसल, कविता में जिस वीणा का वर्णन किया गया है, वह केवल वीणा नहीं है, एक प्रतीक है। कविता कवि के व्यापक जीवनानुभवों का संकेत देती है।
डॉ. करुणा गुप्ता ने अपनी पुस्तक (सप्तक) में कई बातों का खुलासा किया है। उनके अनुसार अज्ञेय को धर्मवीर भारती की रुमानियत तो पसंद थी, किंतु वे दुष्यंत कुमार की ताकत न पहचान सके। ‘गीत फरोश’ के कवि भवानी मिश्र को उन्होंने सही पहचाना। अज्ञेय अन्वेषी कवि थे। एक स्थान पर उन्होंने लिखा है–‘प्रयोग कोई वाद नहीं है, हम वादी नहीं रहे, न हैं! न प्रयोग अपने आप में दृष्ट या साध्य है। ठीक इसी तरह कविता का भी कोई वाद नहीं है।’ वे आगे कहते हैं–‘मैं लिखता इसलिए हूँ कि मेरे पास सांस्कृतिक परंपरा और संवेदना है। सांस्कृतिक परंपरा और आंतरिक संवेदना के अभाव में कोई रचनाकार सृजनरत नहीं होता। अपने व्यक्तित्व को पहचानने तथा उसके परिमार्जन, परिष्कर के लिए सहायक माध्यम साहित्य है।’
अज्ञेय हिंदी कविता में प्रयोगवादी नूतन काव्य धारा के प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। द्विवेदी युग की अतिइतिवृत्तात्मकता की प्रतिक्रिया-स्वरूप छायावाद का जन्म हुआ। फिर छायावाद का विरोध हुआ और कल्पना के मनोजगत के स्थान पर यथार्थ चित्रण को महत्त्व दिया गया। इस काव्य के स्थान पर प्रयोगवादी कविता अस्तित्व में आई। सन् 1943 में अज्ञेय द्वारा संपादित ‘तार सप्तक’ प्रकाश में आया। इन संकलनों में सम्मिलित कवियों मसलन, मुक्तिबोध, रामविलास शर्मा, भारतभूषण अग्रवाल, शमशेर बहादुर सिंह, रघुवीर सहाय और बाद के संकलन में केदारनाथ सिंह, कुँवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना अदि की कविताओं से हमें नई कविता के ध्येय और भाव-बोध का पता चलता है। इसमें पुरानी परंपराओं को नकार कर प्रयोग को ही काव्य जीवन में माना गया। कविता के जन-जीवन से जोड़ा गया। नए प्रतीकों और बिंबों के माध्यम से काव्य में विशिष्टिकरण की प्रतिस्थापना हुई। इसका संपूर्ण श्रेय अज्ञेय को है।
अन्य महत्त्वपूर्ण रचनाकारों की भाँति अज्ञेय की रचनाओं के केंद्र में मनुष्य है, किंतु साथ ही वे रचना में अविष्कार करते चलते हैं–नए शब्दों का, नए शिल्प का, विचारों का और मनुष्य के राग-विराग का। उन्होंने एक नई काव्य भाषा को रचा। बाहरी सामाजिक गतिविधियों के रूपायन में उनकी अधिक रुचि नहीं थी। वे समाज की बात कम, संस्कृति की ज्यादा करते रहे हैं। वैसे विज्ञान, इतिहास, पुराण, धर्म, दर्शन आदि के गहन अध्ययन से उनका रचना संसार व्यापक हुआ। ‘तारसप्तक’ की भूमिका में उन्होंने लिखा है–‘कवि का काव्य उसकी आवाज का सत्य है। यह सत्य व्यक्तिबद्ध नहीं है, व्यापक है और सत्य जितना व्यापक होगा, काव्य उतना ही उत्कर्षकारी होगा।’
अज्ञेय की काव्य-दृष्टि, रचना-प्रक्रिया, जीवन-दर्शन, आलोचना-कर्म आदि को ठीक से समझने में उनकी डायरियाँ सर्वाधिक सहायक हैं, किंतु खेद कि इस ओर समुचित ध्यान नहीं दिया गया। डायरियों का न तो ठीक से अध्ययन किया गया न मूल्यांकन। उनकी चार डायरियाँ ‘भवन्ती’, ‘अंतरा’, ‘शाश्वती’ और ‘शेष’ अज्ञेय के सरोकारों से परिचित कराने के सशक्त माध्यम हैं। स्वयं अज्ञेय के अनुसार डायरियों की टीपें अंतःप्रक्रियाएँ हैं। चंद्रकांत वांदिवडेकर के शब्दों में ये अंतः प्रक्रियाएँ अनवरत सृजनकर्मी की मानसिक लीलाएँ हैं, जिनमें रस का स्रोत है। मानस मुकुल दास इन्हें लेखक का जर्नल या बेतारीख डायरियाँ कहते हैं। स्वयं अज्ञेय कहते हैं अपनी रचनाओं को रूपक में बाँधते हुए कि भवन्ती (प्रथम डायरी) रचना-यात्रा की लॉग-बुक है। लेखक का अंतर्मन ‘यान या नौका’ के कंट्रोल पैनल या एंजिन रूप के समान है जो यात्रा को दिशा को शोधता है। निर्धारित लक्ष्य पर आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत रहता है। वस्तुतः अज्ञेय अपने पाठकों को अपने ‘सागर रथ पर अनुधावन’ करने के लिए आमंत्रित करते हैं। डायरियों के अध्ययन से समझा जा सकता है कि कवि के चिंतन की दिशा क्या है? कवि की कला-दृष्टि क्या है? वे कौन से सरोकार हैं जो उनके सर्जनात्मक संघर्ष को धारदार बनाते हैं? डायरियों से कवि का सृजनशील व्यक्तित्व सामने आता है। लेखक के नाते अज्ञेय अपनी रचना-यात्रा को काफ़ी अकेली मानते हैं, लेकिन क्या रचनाकार सचमुच अकेला होता है? अनुभव के भोगते हुए और उस पर चिंतन करते हुए भले ही वह अकेला हो, लेकिन रचना अपने प्रकाशन के साथ ही सार्वजनिक, सार्वलौकिक और सार्वभौमिक हो जाती है, विशेषतः जब वह निजी न होकर समष्टिगत होती है–एक बड़े वर्ग की बन कर उसे अपना हिस्सेदार बना लेती है। वस्तुतः पाठक लेखक का सहयात्री है। वैसे भी रचना के दौरान कहीं-न-कहीं, एक हद तक पाठक, लेखक के भाव-बोध में होता ही है। भवन्ती में 1964 से 1970 तक की, अंतरा में 1970-79 तक की, शास्वती में 1975 से 79 तक की, शेषा में 1980-87 तक की रचनाओं के बारे में टीपें, अतःप्रक्रियाएँ हैं। उल्लेखनीय है कि भवन्ती और अंतरा में किस्सागोई, चुहुलबाजी, छेड़छाड़ भी है। वजह सिर्फ यह कि डायरियों का गंभीर चिंतन पाठकों के लिए बोझिल न हो जाए, संप्रेषणीयता बनी रहे।
अज्ञेय पर पाश्चात्य कवियों का प्रभाव रहा है। इलियट, सार्त्र, कमिंग्स आदि का प्रभाव उनकी काव्य-कृतियों में देखा जा सकता है। इलियट के काव्य का तो अज्ञेय पर सर्वाधिक प्रभाव रहा। अज्ञेय बाहरी प्रभाव से इनकार भी नहीं करते। उनका मानना है कि सर्वथा मौलिक विचार कोई विरला ही लाता है। विभिन्न युगों और क्षेत्रों के लेखकों-चिंतकों से अंशतः या पूर्णतः प्रभावित होते ही हैं। विचारों के इस स्वायत्त जगत से अज्ञेय ने बहुत कुछ पाया है और उसे धीरे-धीरे पचाया है। इनके बाद अपनी कसौटी पर कसकर उसे परखा है। बाहरी प्रभाव की स्वभाविकता को स्वीकार करते हुए उन्होंने लिखा है–‘बंद घर में प्रकाश पूर्व या पश्चिम किसी निश्चित दिशा में आता है पर खुले आकार में वह सभी ओर समाए रहता है। इसी में उसका आकाश-तत्व है। उस खुले आकाश को अपनी बाँहों में भर सके, यह लेखक का स्वप्न रहा है।’
इलियट के काव्य में प्रतीकों की भरमार है। अज्ञेय को भी प्रतीकों के प्रयोग से परहेज नहीं था। उनके प्रतीक नए और प्रभावशाली हैं। इलियट की तरह अज्ञेय ने भी नए शब्दों, मुहावरों आदि का प्रयोग किया। उनका भरोसा, भाषा को नया रूप देने में रहा है। इलियट का काव्य दुरूह है और अज्ञेय की बाद की कविताओं का रचनाविधान भी दुरूह है। वैचारिकता, अलग जीवन-दृष्टि, विशिष्ट भाषा और उसमें संस्कृतनिष्ठ, तत्सम, आध्यात्मिक, देशज और नूतन शब्दों के प्रयोग और अन्योक्ति के कारण कई स्थलों पर अज्ञेय का काव्य दुरूह और भाषा क्लिष्ट हो गई। पर सब जगह ऐसा नहीं है। उनकी आरंभिक कविताएँ सहज हैं। यदि समझ विकसित न हो और संदर्भों का ज्ञान हो तो सामान्य पाठक के लिए उनके भावों की तह तक जाना मुश्किल हो सकता है। उदाहरण के लिए ये पंक्तियाँ देखिए–
‘मेरे चेहरे में बागड़िया के झोपड़े से झाँकता है एकलव्य
द्रोणाचार्य अभिसंधि करते हैं
मुनियों की ब्याजहीन आँखों में
पोण्य राजहंसमाला नीर-झीर करती है
लाख-लाख मछलियाँ पेटियाँ उलटकर दम तोड़ देती हैं
मेरे चेहरे से भोले बालकों की भवितव्य का विश्वास है।’
लेकिन इस पर दूसरे ढंग से भी विचार करने की आवश्यकता है। जब तक कुछ नया नहीं होगा, प्रयोग नहीं होगा, अलग से कुछ न होगा तो रचनाकार विशिष्ट कैसे होगा! वह लकीर का फकीर बना रहा तो सामान्य और उसमें क्या अंतर रह जाएगा। यदि आज वह प्रतिष्ठित है तो सिर्फ इसलिए कि उसने साहित्य जगत को कुछ खास दिया है–सामान्य से हटकर। प्रयोग से ही नई राहें खुलती हैं। इसलिए केवल दुरूह कहकर हम अज्ञेय को छोटा नहीं कर सकते। इलियट ने अपने काव्य में निराशा, घुटन, अकर्मण्यता, उदासी आदि का चित्रण करते हुए अपनी ‘वेस्टलैंड’ कविता में ऐसे जीवन दर्शन का चित्रण किया है, जिसमें मानवद्रोही तत्व हैं। अज्ञेय के काव्य में भी हताशा, खिन्नता, अपरूप को देखा जा सकता है।
अज्ञेय की अनेक रचनाओं में प्रेमानुभूति की अभिव्यक्ति हुई है। ऐसी कतिपय प्रारंभिक रचनाओं में छायावादी प्रवृतियाँ हैं तो बाद की कविताओं में प्रयोगवाद और अस्तित्ववाद की। उनकी प्रेमानुभूति में स्त्री के आकर्षण-विकर्षण, प्रेम के उद्भव, प्रेम का स्वरूप और प्रेम के विकास को रेखांकित किया गया है। ‘अग्रदूत’, ‘चिंता’, ‘इत्यलम’ जैसे प्रारंभिक काव्य-संग्रहों में छायावादी संस्कार देखे जा सकते हैं। प्रेम की अनिवार्यता को इन पंक्तियों में अनुभव किया जा सकता है–
‘भर दिया प्रथम उसमें
कर दिया फिर प्यार वर्जित
तन बने अंधे पतंगे
हो चुका जब दीप निर्मित।’
‘पलकों का काँपना’ कविता में प्रेम की उत्कृष्ट भावाभिव्यक्ति हुई है–
‘और सब समय बराबर है
बस उतना क्षण अपना
तुम्हारी पलकों का कँपना!’
प्यार के जन्म के बारे में कवि सजग है–
‘कितनी निर्ब्याज अजटिल होती है स्थितियाँ
जिनमें
प्यार जन्म लेता है।’
‘कस्वालिम का झरना’ कविता में प्रेम और प्रकृति की यह उक्ति दृष्टव्य है–
‘विचारों की ओर
सुरसुराता, सरकता
झरने का पानी
अरे जा चुप नहीं रहा जाता तो
चाहे जिससे कह दे जा
सारी कहानी
पतझर ने कब ढंक दी है
धरा की गोद सी वह ढाल जहाँ
हमने की थी मनमानी।’
डॉ. माचवे के अनुसार अज्ञेय की कविता में छायावादी अतींद्रिय प्रेम और प्रगतिवादी मांसल भौतिक प्रणय को नकारकर एक नया आयाम दिया गया है। अज्ञेय के अनुसार प्रेम केवल एक क्षणानुभूति है और बाद में स्मृति। ‘असाध्य वीणा’, उनकी उच्चकोटि की लंबी कविता है। कवि ने चीनी मूल की दो लड़कियों के आत्म-द्वंद्व की कथा को सार्वजनिक बनाकर प्रस्तुत किया है।
कवि ने प्रकृति के नए-पुराने उपकरणों को लेकर सुंदर-सजीव बिंबों की योजना की है। कुछ बिंब तो इतने प्रभावी हैं कि वस्तु या भाव का चित्र सजीव हो उठता है। प्रगति के मानवीकरण के रूप में उन्होंने भव्य चित्र अंकित किए हैं। प्रकृति उनके काव्य में विभिन्न रूपों में प्रकट हुई है। प्रकृति के साथ कवि का पूर्ण तादाम्य है। प्रकृति-वर्णन में भारतीय परंपरा का सौंदर्य है। बौद्धिकता के साथ काव्य में सूक्ष्म निरीक्षण और कल्पना का लालित्य है।
बहरहाल, अज्ञेय हमारे समय के अत्यंत महत्त्वपूर्ण और प्रतिभा-संपन्न कवि रहे हैं। वे अपनी रचनाओं में भाषा को बहुत महत्त्व देते थे। गद्य और पद्य दोनों में भाषा को लेकर उन्होंने प्रयोग किए। उपन्यास ‘शेखर : एक जीवनी’ में उनकी भाषा की उत्कृष्टता देखी जा सकती है। भाषा का जैसा उछाल वहाँ है, वैसा कम ही देखने को मिलता है। अपनी रचनाओं में वे स्मृति और युक्ति का आलोक जगाते हैं। उन्होंने श्रुति परंपरा से बहुत कुछ सीखा है। अज्ञेय के कालजयी व्यक्तित्व की अनदेखी नहीं की जा सकती। हालाँकि कुछ ने अज्ञेय को कमतर आँककर उनके विरोध की संगठित साजिश की थी। वस्तुतः वे एक बड़े काव्य शिल्पी थे। उनका शिल्प रेअर था। वे जानते थे कि जीवन-शिल्प को जाने बिना रचना-शिल्प की बात करना व्यर्थ है। कला और जीवन को अलग-अलग करके नहीं देखा जा सकता।
Image name: Flowers and Japanese book
Image Source: WikiArt
Artist: Paul Gauguin
This image is in public domain.