गँवई मन का सहज कवि
शेयर करे close
शेयर करे close
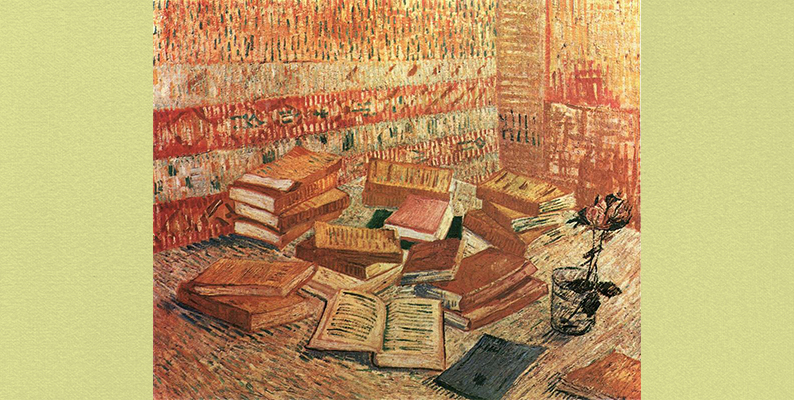
शेयर करे close
- 1 June, 2019
गँवई मन का सहज कवि
एक रचनाकार को जानने व समझने का सबसे सशक्त माध्यम बनती है, उसकी रचना। एक पाठक के रूप में जब हम किसी रचना से जुड़ने का प्रयास करते हैं तो अपनी रुचि, संस्कार और देखने के मूल्य के आधार पर उस कृति और उसके रचनाकार के बारे में अपनी एक अलग राय कायम करने लगते हैं। इसी क्रम में जब त्रिलोचन और उनकी कविताओं को पढ़कर समझने की कोशिश की तो एक मोटी समझ बनी और वह यह कि त्रिलोचन ‘गँवई मन के सहज कवि’ हैं और उनकी रचनात्मकता में इस ‘गँवई मन’ और उसकी ‘सहजता’ की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। ‘गँवई मन’ से हमारा तात्पर्य है, लोकजीवन से संपृक्त मन। भाव में भी और भाषा में भी। जब भी हम त्रिलोचन की कविताओं के नजदीक हों तो पाएँगे कि ‘जनपदीय तत्व’–उस जनपद का कवि हूँ। उनकी कविताओं के रेशे-रेशे में व्याप्त है। इसकी सहजता का यही मूल आधार है। विश्वनाथ त्रिपाठी के अनुसार ‘लोक’ जटिल संदर्भों का सहज रूप होता है। याद कीजिए चंद्रगहना से लौटते वक्त केदारनाथ अग्रवाल ने क्या कहा था, ‘देख आया चंद्रगहना। …दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। (फूल नहीं रंग बोलते हैं, पृ.-18)। यानी नगरों में व्यापार होता है, प्रेम नहीं। प्रेम की प्रिय भूमि का आगार तो ‘लोक’ ही है। जीवन अपने नैसर्गिक रूप में ही हमें यहीं मिलता है। त्रिलोचन का मन इसी लोक में रमा है।
लोकजीवन से जुड़ाव का यह आशय नहीं कि यह कवि जीवन और साहित्य में ‘पश्चिम की आधुनिक अवधारणा’ की चुनौतियों से अनजान था। ऐसा बिल्कुल नहीं है। त्रिलोचन की कविताओं में अगर गँवई जीवन का परिदृश्य है तो शहरी जीवन की आहट भी है। गाँव और शहर के बीच का द्वंद्व भी है। ‘आदमी की गंध’ शीर्षक कविता में त्रिलोचन ने गाँव और शहरी जीवन के बदलते परिदृश्य का बड़ा ही सटीक चित्र खींचा है।
त्रिलोचन की आधुनिकता और उसके महत्त्व को विस्तार से समझाते हुए केदारनाथ सिंह जी ने लिखा, ‘त्रिलोचन एक खास अर्थ में आधुनिक हैं और सबसे आश्चर्यजनक बात तो यह है कि वह आधुनिकता के सारे प्रचलित साँचों को अस्वीकार करते हुए भी आधुनिक हैं। वे आज की हिंदी कविता में उस धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो आधुनिकता के सारे शोर-शराबे के बीच हिंदी-भाषा और हिंदी-जाति की चेतना की गहरी जड़ों को सींचती हुई चुपचाप बहती रही है। …पिछले तीन चार दशकों की हिंदी कविता के पूरे विकास को देखें तो पाएँगे कि उसमें से समानांतर प्रवृत्तियाँ एक साथ सक्रिय रही हैं। पहली वह जो पश्चिम की आधुनिक कविता की बहुत सी बातों को स्वीकार करते हुए धीरे-धीरे अपने रूपाकार में ज्यादा नागरिक और अपनी प्रकृति में ज्यादा सार्वभौम होती गई। दूसरी वह जो हर कीमत पर अपने खास भारतीय मिज़ाज को बनाए रखने के लिए अपनी ठोस जमीन और ठेठ भाषा में लगातार जुड़ी रही है। त्रिलोचन की कविता का संबंध दूसरी प्रवृत्ति से है। नागार्जुन और केदारनाथ अग्रवाल की बहुत सी कविताएँ भी इसी के अंतर्गत आती हैं। समकालीन कविता के बहुरंगी आंदोलनों के बीच इस दूसरी प्रवृत्ति की ऐतिहासिक भूमिका कई बार आलोचकों की दृष्टि से ओझल हो गई है।’ चूँकि त्रिलोचन कभी किसी साहित्यिक आंदोलन के केंद्र में नहीं रहे और दूसरी तरफ ‘प्रगति’ और ‘प्रयोग’ के सारे प्रचलित साँचों को अस्वीकार करके अपनी कविता का शास्त्र गढ़ा था, जिसकी उनको भारी कीमत चुकानी पड़ी।
त्रिलोचन की कविता में ‘ऐसा क्या है जो इनके लिए भी असुविधाजनक और उनके लिए भी’ जानने के लिए हमें उनकी कुछ एक कविताओं को उदाहरण स्वरूप देख लेना चाहिए। त्रिलोचन की एक कविता है, ‘सब्जीवाली बुढ़िया।’
‘मेथी और पालक की दो हरी-हरी गट्ठियाँ
लहसुन और प्याज की चार-ख्सा पोटियाँ
बुढ़िया पूछ रही थी ग्राहक से ले लो
यह सब ले लो कुल पचास पैसे में
ग्राहक बोला–जो कुछ लेना था ले चुका
यह सब क्या करूँगा
रखने की चीज नहीं
बुढ़िया ने साँस ली और कहा–दिन हैं ये ठंड के
ले लो तो मैं भी घर जाऊँ
ग्राहक ने सुना नहीं और दाम चुकाकर चला गया
मैं पास वाले से गोभी ले रहा था
बुढ़िया से मैंने कहा–अम्मा, सारी चीजें
इकट्ठे बाँधकर मुझको दे दीजिए
बुढ़िया असीसती हुई चली गई।’
इस कविता को पढ़कर ऐसा लगता है जैसे एक सब्जी बेचने वाली बुढ़िया और उसके ग्राहक के बीच हुई बातचीत के विवरण को यहाँ प्रस्तुत भर कर दिया गया हो। एक ऐसी आँखों देखी स्थिति का विवरण जिसमें स्वयं कवि भी सम्मिलित है। लेकिन सवाल वही कि यह एक स्थिति का चित्रण भर है, इसमें कवि की कविताई कहाँ है? इसका सटीक जवाब देते हुए विश्वनाथ त्रिपाठी ने अपने एक लेख में बताया कि, बुढ़िया ने साँस ली और कहा–‘दिन हैं यह ठंड के’–यह केंद्रीय पंक्ति है। स्थिति ही दारुण है। उसे किसी प्रकार से काव्यात्मक बनाने की जरूरत नहीं। जरूरत देखने-सुनने और पाठक-श्रोता को दिखाने-सुनाने की है। इसमें ज्यादा कुछ करना कविता की हत्या करना है।
‘उसकी बातें जो कानों में पड़ी
उसको अनसुना कर नहीं पाया मैं।’
अनसुना न कर पाना कविता में सौंदर्य और उसका आधार नवता लाता है। बुढ़िया की विवशता, उसकी व्यथा को एक ने समझा ओर दूसरे ने नहीं। समाज में दूसरों की चिंता, व्यथा विवशता को न समझने वालों की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ‘व्यक्ति केंद्रिता’ कवि की चिंता और व्यथा का कारण है।
ऐसी ही पीड़ा और व्यथा से संपृक्त कवि की एक दूसरी कविता है, ‘रैनबसेरा’। कविता के केंद्र में हैं परमानंद। जूनियर हाईस्कूल में प्रिंसिपल और कवि के परिचित। समस्या यह कि शहर में आए कई दिन हो गए लेकिन उनके रहने की कोई व्यवस्था नहीं। उनका कोई स्थाई ठिकाना नहीं, जहाँ जगह मिली वहीं रात काट ली। उनकी यह व्यथा कवि की व्यथा का कारण बन जाती है। अपने किसी परिचित को चाहकर भी अपने यहाँ रुकने के लिए न कह पाने की व्यथा।
‘कमरा एक और रहने वाले तीन। पत्नी, बच्चा और मैं। चौथे की गुंजाइश यहाँ नहीं। मेरी अनकही चिंता। मेरी विधा बना दी।’ इसी क्रम में हम त्रिलोचन की कविता ‘जीवन का एक लघु प्रसंग’ देख सकते हैं। बचपने की बात है। लड़का (कवि) अपनी बुआ से नई किताबों के लिए पैसे माँगता है।
स्कूल जाने का समय हो गया है। बहुत व्यग्र बुआ के पास खड़ा-खड़ा मैं। उससे किताबें नई लेने के लिए पैसे माँग रहा था। बुआ ने कहा–‘किसी लड़के से माँग लो न, तुमसे जो आगे पढ़ता रहा हो।’
मैंने चिढ़कर कहा–‘बुआ, वे किताबें अब बदल गईं।’
बुआ ने पूछा–‘क्यों?’
‘क्या जानूँ!’–मैंने कहा।
अर्ध स्वगत बुआ बोलीं–‘सभी पैसे कमा रहे हैं।’
बुआ और लड़के के बीच की इस बतचीत में दो पंक्तियाँ ऐसी हैं, जो हमारा ध्यान अपनी तरफ खींचती हैं। पहली, ‘वे किताबें अब बदल गईं’ और दूसरी पंक्ति, ‘सभी पैसे कमा रहे हैं।’ शिक्षा और पूँजी का यह धालमेल त्रिलोचन बहुत पहले ही समझ चुके थे। सीधे सरल वाक्यों द्वारा गहरी-से-गहरी बात कह देना ही त्रिलोचन की कला है।
ऐसे ही न जाने कितने छोटे-छोटे, अनछुए, अनदेखे जीवन-प्रसंगों को त्रिलोचन ने कविता का रूप दे दिया। ‘नगई महरा’, ‘ओरई केवट’, ‘अवतरिया’, ‘चंपा काले-काले अच्छर नहीं चीन्हती’, ‘चित्रा जाम्बोरकर’, ‘आरर डाल’ जैसी न जाने कितनी ही कविताओं में त्रिलोचन ने हमें जीवन की एक अलग ही धूपछाँही और उसके विविध रंगों से हमारा परिचय कराया। सब कुछ इतने चुपचाप और सहन तरीके से होता है कि अगर आप जाग्रत न रहें तो आप स्वयं को कविता में बँधे जीवन की लय से जोड़ नहीं पाएँगे और तब कविता आपको रूखी, खुश्क, उबाऊ और सपाट लगेगी। आप इसे कविता कहने में भी संकोच करेंगे। आपके अंदर यह भाव जग सकता है कि ‘छोड़ो, इसमें क्या है।’ इसका जवाब स्वयं त्रिलोचन ने देते हुए लिखा।
‘इसमें क्या है, मेरे और आपके दिल की धड़कन है, कहना चाहें तो कविता कह लें। इसकी धारा में बहना चाहें तो बह लें। देख सकेंगे यहाँ धूपछाही झिलमिल की आभा। …जो रसज्ञ हैं, इसे उन्हीं के लिए लिखा है। जो अजीर्बग्रस्त हैं, कहेंगे इसमें क्या है।’ जीवन के अमूल्य अनुभवों का खजाना है, त्रिलोचन की कविता। त्रिलोचन ‘सहज सुंदर’ के कवि हैं और उनकी कविता ‘जीवन में संघर्ष की प्रेरणा देने से कहीं ज्यादा हमें जीवन के सौंदर्य का बोध’ कराती है। इसीलिए आप पाएँगे कि उनकी कविता ‘नैतिकता’ और ‘ईमानदारी’ को एक कसौटी के रूप में देखती है और मात्र ‘सफलता’ का कवि-दृष्टि में कोई मूल्य नहीं। वह गहरे अर्थों में ‘मानवीय चरित्र के उन्नयन (नैतिक और सांस्कृतिक) की कविता’ है। इसीलिए कवि ‘जीवन-संदेश’ का वाहक (कभी-कभी) बन पड़ता है।
यह देखकर आश्चर्य होता है कि एक कवि जिसके जीवन और साहित्य में इतना संघर्ष हो, जिसने दुत्कारों, अपमानों, उपेक्षाओं का दंश झेला हो, वह और उसकी कविता इतनी सहज और सुंदर कैसे हो सकती है? अपने जीवन में आए संघर्ष को कवि ने इन शब्दों में बाँधने की कोशिश की है–
‘वही त्रिलोचन है वह–जिसके तन पर गंदे
कपड़े हैं
कपड़े भी कैसे–फटे-लटे हैं
यह भी फैशन है, फैशन से कटे-कटे हैं
कौन कह सकेगा इसका यह जीवन चंदे
पर अवलंबित है
चलाना तो देखो इसका
उठा हुआ सिर, चौड़ छाती, लंबी बाँहे,
सधे कदम, तेजी, वे टेढ़ी-मेढ़ी राहें
मानो डर से सिकुड़ रही हैं, …कौन बताएँ
क्या हलचल है इसके रुँधे-रुँधाए जी में
कभी नहीं देखा है इसको चलते धीमे
धुन का पक्का है, जो चेते वही चिताएँ।’
यह त्रिलोचन के जीवन का वह सत्य है, जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। उनका अपना भोगा हुआ यथार्थ। लेकिन जीवन में आया यह संघर्ष और उससे उपजा दर्द उन्हें तोड़ नहीं पाता। उनकी प्रगतिशीलता इस बात में है कि वे उन अनुभूतियों को स्वस्थ रूप ग्रहण करते हैं,
‘आभारी हूँ मैं पथ के सारे आघातों का
मिट्टी जिनसे बज्र बनी उन फुटपाथों का।’
उन्हें जीवन में व्याप्त संघर्षों से कोई शिकायत नहीं,
‘हार नहीं मैं जीते जी मानूँगा
और लड़ूँगा उत्पातों में।’
यह अपराजेय भाव ही उनमें दारुण अभाव के बावजूद उन्हें अनथक जीवन-संघर्ष से दो-दो हाथ करने के लिए प्रेरित करता है। रामविलास जी ने लिखा, ‘भूख, उपवास और बेरोज़गारी पर जैसी अनुभूति-तीव्रता त्रिलोचन की कविताओं में है वैसी अन्य कसी प्रगतिशील कवि में नहीं। लगभग वैसी ही अनुभूति जैसी तुलसी और निराला की आत्मकथात्मक पंक्तियों में है। ऐसी पंक्तियों में ट्रैजिक औदात्य है, नैतिक दृढ़ता से भंडित मानवीय गरिमा है।’ त्रिलोचन की कविताओं में आया दु:ख और अवसाद का अवसान निराशा या मायूसी में न होकर करुणा में होता है। यह वह दर्द नहीं जो हमें व्यक्ति और समाज से काट देता है बल्कि यह दर्द हमें दूसरों से जोड़ता है, हमारी आत्मा को प्रसार देता है। इसीलिए जब ‘दर्द जो आया तो दिल में उसे जगह दे दी।’
अब सवाल यह उठता है कि त्रिलोचन की कविताओं में आया दु:ख और अवसाद का अवसान क्यों करुणा में होता है? क्यों उनके जीवन का अनथक संघर्ष उन्हें अंदर से तोड़ नहीं पाता? क्यों वह उनकी आत्मा के प्रसार का कारण बन जाता है? कोई व्यक्ति कैसे इतनी उपेक्षा, अपमान झेलने के बाद भी सहज, सरल रह सकता है। इन सारे सवालों का जवाब देते हुए विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने लिखा, ‘उस जनपद का कवि हूँ जो भूखा–दु:ख है, नंगा है, अनजान है, कला–नहीं जानता। कैसी होती है क्या है, वह नहीं मानता, फतवा कुछ भी दे सकती है। …वह उदासीन बिलकुल अपने से, अपने समाज से है; दुनिया को सपने से अलग नहीं मानता।’ का भाव ही मूलतः सहजता का भी आधार है। अहंकार व्यक्ति को अकेला बनाकर पृथक करता है। जीवन से प्रेम करनेवाला अकेला होकर भी मन में लोगों से जुड़ा रहता है। जब मन में यह भाव रहता है कि ‘दु:खी सिर्फ मैं नहीं हूँ–देश काल में दु:ख भी असीम है तब उसका दु:ख भी व्यापक होकर सहज, आडंबरहीन हो जाता है। तब दु:ख बजता, खड़खड़ाता नहीं–रचनाशील होता है।’ सुख हो या दु:ख उसके प्रसार में ही जीवन का सार है। प्रसाद जी ने श्रद्धा से कहलवाया,
‘औरों को हँसता देख, मनु हँसो और सुख पाओ
अपने सुख को विस्तृत कर लो सबको सुखी बनाओ।’
त्रिलोचन ने भी यही किया,
‘और
जब पीड़ा बढ़ जाती है
बेहिसाब
तब
जाने-अनजाने लोगों में
जाता हूँ
उनका हो जाता हूँ
हँसता-हँसाता हूँ।’
त्रिलोचन का किसानी-मन प्रकृति में खूब रमा है। प्रकृति अगर त्रिलोचन के यहाँ किसान-जीवन का अभिन्न अंग बनकर आई है तो उसका स्वतंत्र और आकर्षक सौंदर्य भी यहाँ चित्रित है। खेती की शोभा और जीवन की स्मृति का आधार प्रकृति ही है।
‘गेहूँ, जौ के ऊपर सरसों की रंगीनी
छाई है, पछुआ आ-आकर इसे झुलाती
है, तेल सी बसी लहरें कुछ भीनी-भीनी
नाक में समा जाती है, सप्रेम बुलाती है
मानो यह झुक-झुककर
समीप ही लेटी
मटर खिलखिलाती है, फूलभरा आँचल है,
लगी किचोई है, अब भी धीमी की पेटी
नहीं भरी है, बात हवा से करती है, बल है
कहीं नहीं इसके उभार में।’
वर्षा, बादल, धूप, प्रकृति के वे उपादान हैं जिन पर किसानों का जीवन निर्भर रहता है। त्रिलोचन ने अपनी कविताओं में इन सबके विविध चित्र आँके हैं। भादों की रात का यह दृश्य देखिए।
‘भरी रात भादों की…पथ…लपका वह कौंधा। दीप्ति भर उठी आँखों में इतनी, फिर हम-तुम। कुछ भी पकड़ सके न डीठ से, छाया चौंधा। …रिमझिम रिमझिम-छक् छक् छक्…सर् सर् सर् सर्। चम-चम चमके-धमाके धन के, उत्स निशि भर।’ भादों की रात से अलग एक दृश्य है। आठ पहर की टिप्-टिप् का, ‘सड़क भींग गई है। पेड़ों के पत्तों से बूँदें। गिरती है टप्-टप्, हवा सरसराती है। चिड़ियाँ समेटे पंख यहाँ-वहाँ बैठी हैं। ऐसे लोग आते हैं जाते हैं। जो काम टाल नहीं सकते। किसी तरह।’ शब्द-संयोजन के विवेक से कवि ने इन दृश्यों को जीवंत बना दिया है। वर्षा के दो भिन्न चित्र। दोनों की भाषिक-संरचना दृश्य के अनुरूप। इन कविताओं को पढ़कर जो बात बिल्कुल साफ है, वह यह कि त्रिलोचन केवल प्रकृति के रूप पर नहीं बल्कि उसके प्रभाव के अंकन में भी बेजोड़ हैं। इसलिए उनका प्रकृतिपरक चित्रण कहीं भी ‘मानवीय-संदर्भों’ से कटा हुआ नहीं है। त्रिलोचन की इसी कला पर मुग्ध हैं नामवर जी। उन्होंने लिखा, ‘इस चित्र में न बिंब है, न प्रतीक। रंगा भेजी भी नहीं। हैं तो कूँची के करतब। प्रकृति का अलंकार नहीं। बस एक अनुभव। एक ऐसा अनुभव जिसमें प्रकृति मनुष्य से अलग नहीं है। जीवन के प्रेमी त्रिलोचन प्रकृति में भी जीवन ही देखते हैं, बल्कि प्रकृति में उसकी दृष्टि वहीं जाती है जहाँ जीवन दिखता है। वस्तुतः त्रिलोचन के काव्य का एक बड़ा भाग जीवन का महोत्सव है।’ प्रगतिशील कवियों का प्राकृतिक-संसार रूप, रस गंध, ध्वनि का समृद्ध संसार है। प्राकृतिक-चित्रों का यह सूक्ष्म अंकन प्रकृति के प्रति उनकी आत्मीयता (प्रेम) को दर्शाता है। यहाँ केवल प्रकृति में मानव-जीवन का सहज स्वभाविक चित्र ही नहीं बल्कि उस पर प्रगतिशील सामाजिक विचारधारा की छाप भी है, जो मनुष्य को जीवन में कर्म और संघर्ष के लिए प्रेरित करती है। ‘बादलों ने हलकी अँगड़ाई ली। एक ओर चमक जरा बढ़ गई। हवा नए अँखुओं से यों ही बतियाती है। उनका सिर हिलता है। फूल खिलखिलाते हैं।’ यहाँ भी यह काम त्रिलोचन बड़े ही संयत और सहज तरीके से करते हैं।
कविता में ‘शब्द’ के महत्त्व को रेखांकित करते हुए अज्ञेय ने लिखा कि कविता सबसे पहले शब्द है और अंत में भी यही बात बचती है कि कविता शब्द है। इससे स्पष्ट है कि अज्ञेय के यहाँ शब्द का क्या महत्त्व है। प्रगतिशील कविता में त्रिलोचन एक ऐसे कवि हैं जो यथार्थवादी धारा का समर्थन करते हुए भी शब्द की सत्ता को महत्त्व देते हैं। लेकिन त्रिलोचन और अज्ञेय (प्रयोगवाद, नई कविता) के काव्य-व्यापार में शब्द के महत्त्व के अर्थ में एक मूलभूत अंतर झलकता है। अज्ञेय के लिए शब्द की सार्थकता, ‘शब्द के परिष्कार’ या ‘प्रयोग की विशिष्टता’ में है, जबकि त्रिलोचन के लिए शब्द का अर्थ है, ‘जीवन से घनिष्ठ साक्षात्कार’। एक के लिए शब्द ‘मोह’ है तो दूसरे के लिए ‘लगाव’। लगाव क्यों? क्योंकि, ‘शब्दकार, इन शब्दों में जीवन होता है। ये भी चलते-फिरते बात करते हैं। तोष, रोष–जब जैसे भावों से भरते हैं। तब वैसे ही अर्थों का व्यंजन होता है। शब्दों में भी हाड़, मांस है, जीवन धरकार–वे भी जीवधारियों के स्वर-यंत्र सँभाले। स्फुट, अस्फुट दो धाराओं में प्रवहमान हैं। रात और दिन–धावा पृथ्वी में विचरण कर। झलकाते हैं दुनिया के सब खेल निराले।’
त्रिलोचन ने अपनी कविताओं के लिए सॉनेट का रास्ता चुना। ‘सॉनेट’ एक विजातीय छंद है। इस विजातीय छंद में अपने सारे अनुभव और अध्ययन को तपाकर उसे भारतीय रूप देकर प्रस्तुत करना त्रिलोचन के कवि सामर्थ्य को दर्शाता है। यानी अंतर्वस्तु भारतीय पर उसका रूप-विधान यूरोपीय। त्रिलोचन ने इसके लिए काफ़ी आलोचना भी झेली। लेकिन अपनी जिद के आगे उन्होंने किसी की नहीं सुनी। शायद उनके शास्त्रीय (कवि) व्यक्तित्व के स्वभाव के यह काफ़ी करीब था। अनुभूति का अतिरेक (अनुभूति का आपका रूप) उन्हें नहीं भाता। सॉनेट की शक्ति और सीमाओं को पहचानकर ही इस कवि ने उसका प्रयोग किया।
‘इस सॉनेट का रास्ता चौड़ा अधिक नहीं है
कसे-कसाए भाव अनूठे
ऐसे आएँ जैसे किला आगरा में जो नग है,
दिखलाता है पूरे ताजमहल को
गए रहे, एकान्विति हो।’
त्रिलोचन ने बड़ी विनम्रता के साथ यह स्वीकार किया कि यह ‘चीज किराये की है’ और उन्होंने ‘झूठे ठाट-बाट बाँधे हैं।’ इस विश्वास के साथ कि उन्होंने जो भी किया वह गलत नहीं। इसीलिए लिखा कि, ‘लड़ता हुआ समाज, नई आशा-अभिलाषा, नए चित्र के साथ नई देता हूँ भाषा।’
त्रिलोचन ने अपनी कविताओं के लिए ‘सॉनेट’ जैसे विजातीय छंद का चुनाव ही क्यों किया, इसका जवाब देते हुए राजेश जोशी ने लिखा, ‘लय की गति का धीमा होना, सॉनेट का खास गुण है। गंभीरता, विचारशील भाव, अनुभूति की गहन एकाग्रता और कसी हुई भाषा के साथ ही चौदह पंक्तियों का अनुशासन, ये सारी बातें जो एक सॉनेट की विशिष्टता हैं, त्रिलोचन की मनोभूमि के लिए बहुत अनुकूल थीं। आवेगों की अभिव्यक्ति का संयमित ढंग और स्वर की तटस्थता वाली अपनी काव्य-मानसिकता क कारण ही सॉनेट जैसे विदेशी काव्य रूप ने त्रिलोचन जैसे ठेठ भारतीय किसानी मन के कवि को आकर्षित किया होगा। अष्टपदी में लय का अनुशासन और षटपदी में लय की स्वतंत्रता के द्वैत ने त्रिलोचन के अपने स्वभाव को लुभाया होगा। पूरा सॉनेट रोला के भाषिक अनुशासन में ढाला है। रोला छंद की अपनी लय में ढलकर त्रिलोचन के सॉनेट ने पूरी तरह हिंदी के जातीय स्वरूप को ग्रहण कर लिया है।’ त्रिलोचन पूरा प्रयास करते हैं कि अपनी बात को ‘पूर्ण वाक्य’ में कहें। ‘अरूद्धांत वाक्य-रचना-निर्वाह’ के कारण भावों की इकाइयाँ एक पंक्ति से खींचकर दूसरी पंक्ति तक पहुँच जाती है। त्रिलोचन ने संगीत की समानांतर इकाइयों की जगह यतियों की विविधता का सौंदर्य पैदा किया है, जिसकी वजह से उनकी कविता ‘विशिष्ट वाचन पद्धति’ की माँग करती है। अन्यथा आप कविता को पढ़कर बहुत आनंदित न होंगे। यही वजह है कि उनकी कविता को ‘भागते हुए तीव्र अहसासों के क्षण में पकड़ पाना’ आसान नहीं। इसके लिए आपके पास थोड़ा समय और धैर्य होना चाहिए। तभी आप कवि की कही हुई बात तक पहुँच पाने में सफल होंगे, अन्यथा नहीं। त्रिलोचन ने इसी कीमत पर यह रास्ता चुना।
त्रिलोचन के पूरे कवि-व्यक्तित्व को देखते हुए परमानंद श्रीवास्तव ने बिल्कुल सही बात कही है कि, ‘हिंदी कविता में उनके ढंग का दूसरा कवि नहीं। वे सच्चे कवियों में हैं, जिनके द्वारा अंकित साधारण वस्तुएँ भी मन को लीन करने वाली होती है।’ अपने प्रति उपेक्षा, अपमान, प्रवंचना को देखते हुए त्रिलोचन ने कभी स्वयं के बारे में लिखा था कि, ‘नहीं हूँ किसी का भी प्रिय कवि मैं’ लेकिन बीते समय (तथाकथित आधुनिकतावाद की आँधी के थमने के बाद) के साथ इस ‘गँवई मन के सहज कवि’ की धारणा गलत सिद्ध हुई और उसकी सादगी, सहजता आज हमारे जीवन-मूल्य के साथ-साथ काव्य-मूल्य के रूप में भी प्रतिष्ठित हो चुके हैं।
