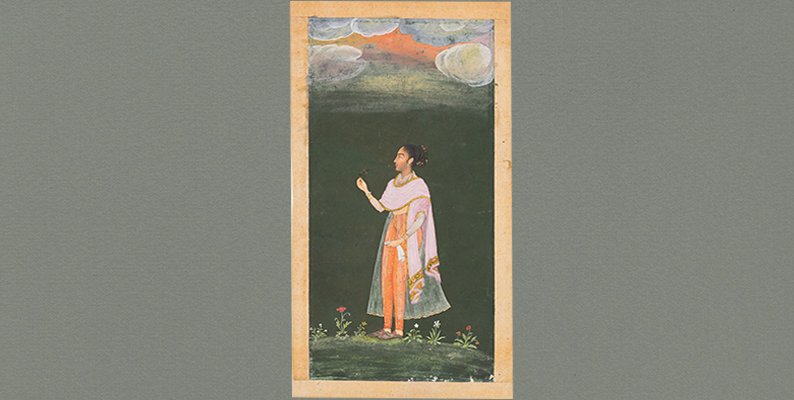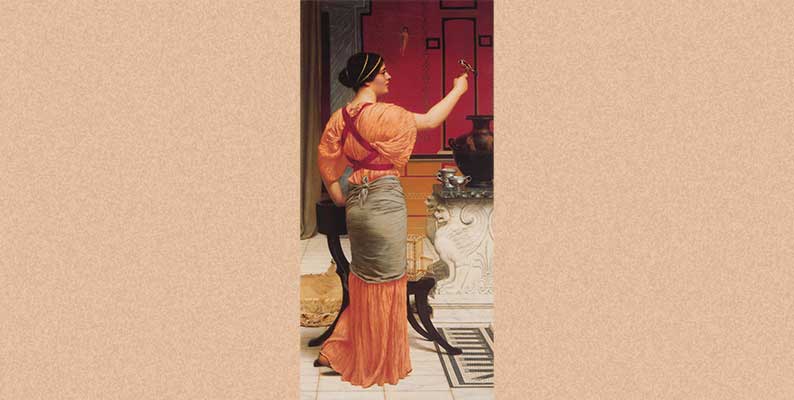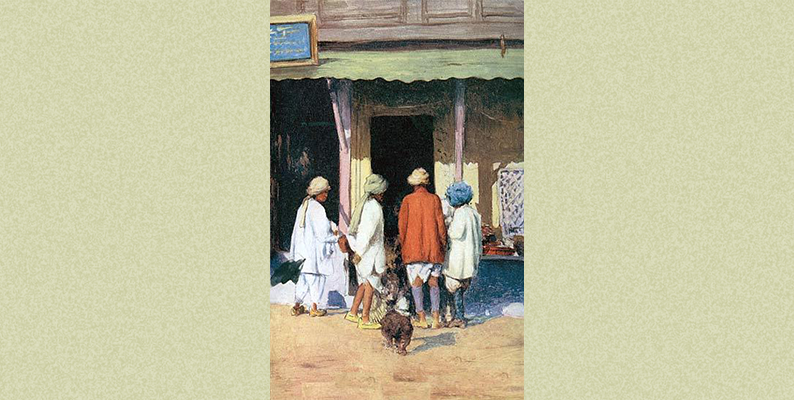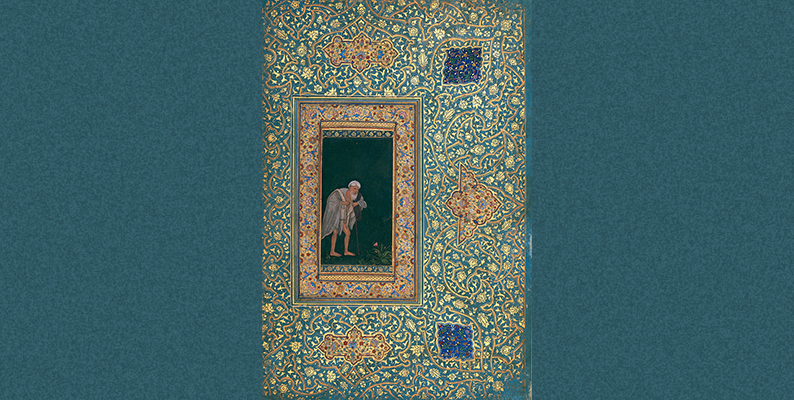मेरा बचपन मेरा जीवन
- 1 April, 2019
शेयर करे close
शेयर करे close

शेयर करे close
- 1 April, 2019
मेरा बचपन मेरा जीवन
बचपन अच्छा हो या बुरा, अनुकूल हो या प्रतिकूल, प्रभावशाली हो या प्रभावहीन, भुलाए नहीं भुलता। संसार में घुल जाता है। मानसिकता बन जाता है। अक्सर नहीं लेकिन कभी-कभी नियति भी निर्धारित करता है। हम प्रामाणिक तौर पर नहीं कह सकते कि हमारा बचपन अक्षरसः ऐसा ही था। बचपन में स्मृतियों को सँजोने की क्षमता और तमीज इतनी विकसित नहीं होती है कि सब कुछ सिलसिलेवार याद रहे। हम अपने बचपन को अपनी स्मरण शक्ति से कम परिजनों के द्वारा अक्सर दोहराई जाती बातों से अधिक जानते हैं। परिपक्व उम्र में भी हम सब कुछ सिलसिलेवार याद नहीं रख पाते क्योंकि विस्मरण का आक्रमण होने लगता है। इसलिए गीता पर हाथ रख कर नहीं कह सकते जो कहेंगे, सच कहेंगे, सच के सिवाय कुछ नहीं कहेंगे।
मेरा बचपन। कोई उतार-चढ़ाव नहीं। थ्रिल नहीं।
निषेध और नियंत्रण से गुजरा सीमित बचपन।
पाँच बहन दो भाइयों में मैं तीसरी संतान। मुझसे आठ साल बड़ी जीजी। ढाई साल बड़ी मँझली। उन दिनों चाइल्ड डेथ रेट बहुत था पर हम सात चमत्कारिक रूप से तंदुरुस्त थे। हमारे आस-पास दो-तीन बच्चों वाले छोटे परिवार सिर्फ वही थे जिनमें वंशधर आ चुके थे। वंशधर की प्रतीक्षा वाले परिवार हमारी तरह बड़े थे। मेरी अनपढ़ अम्मा (अब काम चलाऊ उठना-बैठना करते हुए वयोवृद्व हैं) संताप कहा करतीं–‘दाई (दादी) के तेरह बच्चों में तुम्हारे बाबू जी ही बचे। शंका बनी रही हमारे साथ भी यह न हो जाए। दाई का कठोर आदेश था लड़का न हुआ तो वंश खत्म। घर में हमारी एक्कौ न चलती। दाई भक्त बाबू जी हमारे पच्छ में कबहूँ एक्कौ आखर नहीं बोलते…। हम जानते हैं, तुमलोग को साधन-सुविधा नहीं दे पाए। बाबू जी की कम तनखाह (उन दिनों जज को अल्प तनख्वाह मिलती थी। आज इतनी अधिक है कि अम्मा तीस-पैंतीस हज़ार रुपिया फेमिल पेंशन पा रही हैं)। बाबू जी आधी तनखाह दाई, बाबा (नेत्रहीन), कक्का-काकी (निःसंतान) के लिए रीवा (पैतृक नगर) पठा देते हैं। उनकी ईमानदारी का तो तुमलोग जानती हो। दीवाली पर कोई मिठाई-फटाका देने आए तो लाल-पीले होकर लौटा देते हैं…।’ आज के दौर में ऐसे ईमानदार अधिकारी काल्पनिक लग सकते हैं पर स्वर्गीय बाबू जी इतने ईमानदार थे कि सरकार बिना माँगे वेतन न देती तो न माँगते। दीपावली पर आई मिठाइयाँ, मेवे, उपहार बैरंग लौटा देते। त्योहार का हमारा आनन्द चौपट होता है तो हो। अम्मा जोड़-तोड़ से गृहस्थी चलाती थीं।
लड़कियों की तादाद देख उग्र होती जा रही थीं। उन्होंने मेरे जन्म से पहले ज्योतिष को घर बुलाया (भ्रूण परीक्षण अस्तित्व में नहीं था अन्यथा करातीं) ज्योतिष ने शर्तिया पुत्र होने का प्रिडिक्शन बता कर ठग लिया। मैं लड़का नहीं थी। प्रिडिक्शन के असर से मेरी आवाज जरूर लड़कों जैसी मोटी हो गई। आवाज के कारण दाई मुझे गरबैठी (बैठे गले वाली) पुकारतीं। पुत्र जन्म सुनकर खाना खा रही काकी के हाथ से कौर छूट गया था। घर में जैसे मारकेश लगा हो। संयुक्त कुल को आगे ले जाने वाले अकेले बाबू जी। लग रही है लड़कियों की पाँत। जावद (निमाड़) में जन्मी मुझसे तीन साल छोटी चौथी बहन। अम्मा निपूती घोषित कर दी गई। जीजी डिंड पुकार कर रोई। मुझे मँझली से रोने का कारण ज्ञात हुआ–‘हमारा भाई कभी नहीं होगा। हमलोग इस साल भी बाबू जी को राखी बाँधेंगे।’
मुझे तब लगता था, आज भी लगता है मँझली (जब डेढ़ वर्ष की थी मोती झीरा (टायफाइड) हुआ जिससे पोलियोग्रस्त हो गया। पोलियो प्रभावित होने से उसका विवाह न हो सका। वह सरकारी पाठशाला में अध्यापिका हैं।) परिस्थितियों को मुझसे बेहतर समझती है। उसका निर्णयात्मक हौसला प्रबल है। पोलियो के कारण अम्मा-बाबू जी उसके प्रति संवेदनशील रहते थे। हमलोगों की जिद का अर्थ न था पर उसकी जिद कभी-कभी मान ली जाती। मेरा मानना है अभिन्न परिस्थिति से गुजर कर भी प्रत्येक व्यक्ति की अवधारणा, सोच, साहस भिन्न होता है। मैं आज भी जिद्दी होकर फैसले नहीं कर पाती। मुझे भाई नहीं होगा वाली बात अफसोस करने जैसी नहीं लगी थी–‘बाबू जी का राखी बाँध देंगे। एक रुपिया मिलेगा।’
बाबू जी राखी बँधाई के एक रुपिया देते थे। अम्मा ने अपनी हस्तकला का बेहतरीन उपयोग कर हम बहनों के लिए बारीक रेगीन मोतियों से छोटे-छोटे बटुआ (पर्स) बनाए थे। बटुओं में पड़ी पर्ची बटुओं को नामजद करती। मेरी पर्ची में लिखा था–सुषमा की रकम। बटुये और रकम कहाँ गई मालूम नहीं। माह अंत में आर्थिक आपदा की भेंट चढ़ गई होगी। जावद में श्रीनाथ (वह अब गणित का प्राध्यापक है) ने जन्म लेकर अम्मा को निपूती के कलंक से मुक्ति दिलाई। हम बहनें उत्फुल्ल। राखी बँधवाने वाला आखिर आ ही गया। जावद बहुत छोटी जगह थी। न्यायप्रियता और ईमानदारी के कारण बाबू जी की प्रतिष्ठा थी। घर में बधाई के स्वर भर गए। मध्य प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री वीरेन्द्र कुमार सखलेचा उन दिनों जावद में वकालत करते थे। वे भी बधाई देने आए। जावद में जीजी और मँझली पाठशाला जाती थीं। पाँच साल से कम होने के कारण मुझे प्रवेश नहीं मिल रहा था। मैं घर का बना सूती बस्ता टाँगे जाती और मँझली की कक्षा (तीसरी) में बैठ जाती। अध्यापक ने अंततः मेरा नाम पहले दर्जे में लिख लिया। मैं कक्षाएँ पास करती गई। अब अठारह साल के विद्यार्थी स्कूल पास करते हैं। मैं अठारह में विज्ञान स्नातक हो गई थी। मैं और मँझली अक्सर स्कूल में बस्ता भूल आते। जो दूसरे दिन यथास्थान टाट पट्टी में मिल जाते। स्कूल के आखिरी दिन भी छोड़ आए। ग्रीष्मावकाश शुरू हो गया। इसी बीच सुदूर सारंगगढ़ (छत्तीसगढ़ की तहसील) तबादला हो गया। जब्त बस्ते नहीं मिल सके।
अरमानों से जन्मा श्रीनाथ दस माह का। निमाड़ से छत्तीसगढ़ की लंबी यात्रा। भरी बरसात! उन दिनों ग्लोबल वार्मिंग का आतंक नहीं था। बरसात का अर्थ था चौमास। अम्मा शिथिल थीं–‘बरसात में कैसे जाएँगे? श्रीनाथ बीमार हो जाएगा।’
बाबू जी ने न कभी स्थानान्तरण स्थगित कराया, न कभी अच्छी जगह पाने का प्रयास किया। बोले–‘भगवान का नाम लो और चलो।’
उन दिनों यातायात के बहुत साधन नहीं थे। रीवा को तो अभी दस-पंद्रह साल पहले रेल सुविधा मिली है। सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग की कठिन यात्रा।
हहराती महा नदी और मान नदी को नाव से पार किया गया। तट पर फिसलन। जीजी फिसल कर नदी में गिर गई। उसने किनारे की लंबी-मजबूत घास को बुद्धिमानी से पकड़ कर बाबू जी को पुकारा। मल्लाहों ने उसे बाहर निकाला।
सारंगगढ़–फिरंगी काल के दो बड़े बँगले। एक में हम रहते। दूसरे में पी.डब्ल्यू.डी. के दो छोटे बच्चों वाले अभियंता। सामने के विशाल मैदान में बंजारों के दो तंबू थे। बड़े तंबू में माता-पिता, दो लड़कियाँ और एक लड़का रहता था। दूसरे में बड़ा लड़का, बहू, उनका छोटा बच्चा। रात में हमलोग सामूहिक रूप से पढ़ने बैठाए जाते, बंजारे खेलते, हँसते, रस्सी पर अभ्यास करते। पोथी में मेरा चित्त न लगता। वे आजाद खेल रहे हैं, मैं पहाड़े रट रही हूँ। अनिवार्यता कष्टप्रद होती है। वर्जनाएँ लुभाती हैं। मुझे उनकी स्वतंत्रता दिखती थी। अभाव नहीं दिखते थे। एक बार मूसलाधार पानी में दोनों तंबू गिर गए। बंजारा परिवार का मुखिया बाबू जी के पास सहारा माँगने आया–‘मालिक, रातभर रहने दो। छोटा बच्चा पानी में मर जाएगा।’
अम्मा को बैदू (अर्दली) ने बताया था सारंगगढ़ में टोना-टोटका बहुत होता है। ये बंजारे पता नहीं कौन से जंतर-मंतर जानते हैं। अम्मा सशंकित थीं पर बाबू जी ने गेस्ट रूम में उन्हें जगह दे दी। सुबह पानी रुक गया। बंजारे तंबू ठीक करने लगे। हाट वाले दिन मुखिया बड़ा तरबूज लाया। अम्मा नहीं ले रही थीं पर वह रख कर चला गया।
‘आप मदद न करते तो बच्चा मर जाता।’
इस प्रसंग पर मैंने ‘देवता’ कहानी लिखी जो ‘वसुधा’ में प्रकाशित हुई।
समर्थ उपकार न चुकाएँ, असमर्थ चुकाना जानते हैं। अभियंता जीप से अक्सर जिला रायगढ़ जाते। अच्छे वस्त्र, केले आदि लाते। सारंगगढ़ में न रेडीमेड वस्त्र मिलते थे न केले। अच्छे वस्त्रों में सजे उनके बच्चे केले के छिलके बाहर फेंक कर शायद संकेत देते थे–इसे रहन-सहन कहते हैं। संकेत समझ जीजी अम्मा से कहती–‘जिंदगी तो ये लोग जी रहे हैं। अम्मा मेरे पास एक भी रेडीमेड ड्रेस नहीं है।’
अम्मा शिथिल हो जातीं–‘बाबू जी सुनेंगे तो डपट देंगे। हमें भी, तुम्हें भी।’
बाबू जी की कठोर चितवन हमलोगों को शिव का तीसरा नेत्र लगती थी। वे अदालत की तरह घर में भी सख्त न्यायाधीश होते थे। घर में लड़कियाँ हैं वे शायद इस बोध से कभी नहीं छूट पाए। लड़कियाँ गलत राह न पकड़ लें इसलिए वे नियंत्रण की डिग्री बढ़ाते गए। लड़कों के मायाजाल से पृथक रखने के लिए हम बहनों को कन्या शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ाया। जहाँ कन्या शैक्षणिक संस्थान नहीं थे, सह शिक्षा में पढ़ाया (अक्सर कहते तुमलोगों को कुछ दूँ न दूँ, पढ़ने का पूरा अवसर दूँगा) लेकिन न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भागीदारी करने दी, न देखने जाने दिया। एक माह में मात्र एक मूवी देखने की छूट दी। मूवी को पहले कचहरी का कोई क्लर्क देखता फिर बाबू जी को सूचित करता बच्चों के देखने लायक है। कोई अमर्यादित दृश्य नहीं है। फिल्मों में तब दो फूलों के मिलन से सुहाग रात संपन्न हो जाती थी, लेकिन बाबू जी डरे रहते थे लड़कियाँ बिगड़ जाएँगी। आज के बच्चे कंप्यूटर, मोबाइल, टी.वी. में क्या-क्या देखकर पंडित बन रहे हैं। न माता-पिता रोक पा रहे हैं, न बच्चे रुक रहे हैं। दंड देने का बाबू जी का तरीका विचित्र था। मारते-पिटते नहीं थे। हमारे शौक पर रोक लगा देते थे। मैं सागर विश्वविद्यालय से बी.एससी. द्वितीय वर्ष कर रही थी। पिछले साल दो बहनों के रिजल्ट बिगड़ गए। बाबू जी ने कहा, ‘फिल्म का असर है। आज फिल्म बंद।’
बहुचर्चित फिल्म ‘शोले’ सागर में छह माह लगी रही पर हमलोग नहीं देख सके। हमलोग रिकार्ड तोड़ लोकप्रियता प्राप्त बिनाका गीत माला सुनने के लिए भी स्वतंत्र नहीं थे। रेडियो का मतलब था–समाचार। घर में बहुत पुराने जमाने का बहुत बड़ा रेडियो था। रेडियो छूने की पात्रता बाबू जी और जीजी को थी। हमारे छुने से चौपट हो जाने का रिस्क। मुझे उसकी लाल सुई मुश्किल से दिखाई दी। जब मैं ग्यारहवीं में थी तब थर्मामीटर की पारे की चमकती लकीर दिखाई दी। अब डिजिटल तापमापी है। बीप से तापक्रम जान लो।
बाबू जी के कठोर नियंत्रण के फलस्वरूप प्रेम शब्द मुझे अनैतिक लगने लगा। मैंने इतनी कहानियाँ लिखीं, एक उल्लेखनीय प्रेम कथा नहीं लिख पाई। जो लिखी उनमें प्रेम का परिणाम नकारात्मक रहा।
सारंगगढ़ में मात्र दो विद्यालय (लड़कों वाले) थे। प्राथमिक विद्यालय मेरे घर के समीप, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दूर था। उस आदिवासी बहुल इलाके में लड़कियों को शिक्षित नहीं किया जाता था। अधिकारियों की लड़कियाँ, लड़कों के स्कूल में पढ़तीं। मेरी कक्षा में मैं और फरहत कुल जमा दो लड़कियाँ थीं। मैं और फरहत प्राथमिक विद्यालय में थे। नौंवीं या दसवीं में अध्ययनरत जीजी तालाब वाली रोड से बड़े स्कूल जाती। तब हमलोग एकांत पथ में अकेले आते-जाते थे। आज आठ-दस माह की बच्ची के लिए कोई पातकी घात लगाए रहता है। स्कूल से लौट कर जीजी, अम्मा से बोली–‘अम्मा तालाब के पास गुंडे बैठते हैं।’
अम्मा ने सतर्क किया, ‘उनकी ओर न देखा करो।’
मँझली आरंभ से प्रयोगधर्मी रही है। स्कूल से लौटते हुए मुझसे बोली–‘आज तालाब के रास्ते से घर जाएँगे।’
‘क्यों?’
‘गुंडे देखेंगे।’
‘कैसे पहचानेंगे?’
‘उनके सिर पर दो सींग होती हैं।’
मेड़ पर लड़कों का समूह बैठा था। अलबत्ता गुंडे न दिखे। मँझली हैरत में–‘जीजी पता नहीं क्या देख लेती है। एक भी गुंडा न दिखा।’
घर पर अम्मा ने विलंब का कारण पूछा। मँझली ने तत्काल विवेक का परिचय दिया। ‘छोटे रास्ते में कीचड़ था। तालाब की तरफ से आना पड़ा।’
‘वहाँ गुंडे बैठते हैं।’
‘अम्मा वे गुंडे नहीं लड़के हैं। किसी के सिर पर सींग नहीं थी।’
‘वे लड़के ही गुंडे हैं। इनसान के सिर पर सींग नहीं होती।’
मुझे लगता है यही स्थितियाँ, यही भ्रम, यही जिज्ञासा बच्चों को स्थितियों पर सोचने का अभ्यास कराती है। मैं सोचने लगी थी यह है तो क्यों है? यह नहीं है तो क्यों नहीं है? कुछ जिज्ञासाएँ, कुछ भय शाश्वत होते हैं। आम बच्चों की तरह मुझे भी अँधेरे में भय लगता था। सारंगगढ़ में एक टॉकीज थी। खुले आसमान के नीचे पर्दा (स्क्रीन) लगा था। दर्शक अपने घर से बोरी-फट्टे लाकर भूमि पर बैठते थे। अधिकारियों के लिए दर्शकों के पीछे बेंच और कुर्सियाँ लगाई जातीं। जीजी को मूवी का चाव था। अम्मा हम बहनों को सिनेमा दिखाने ले गईं। श्रीनाथ घर में बाबू जी के साथ सो गया था। अँधेरा होते ही मैं और छोटी बहन सिसक-सिसक के रोने लगीं। अग्नि दृश्य देख कर मुझे लगा घर में आग लग गई है। बाबू जी और श्रीनाथ लपटों से घिरे हैं। हम दोनों के कारण सब मध्यांतर में लौट आए। मैं दंग थी। घर में आग नहीं लगी थी। प्रसंग जान कर अम्मा ने मुझसे कहा–‘तुम्हारे कभी अकल नहीं आएगी।’
मुझे नहीं आएगी तो अम्मा को कौन सी आ गई थी। उन्हें बिल्कुल ध्यान नहीं था चाय पत्ती खत्म है। रात में एक अधिकारी बाबू जी से मिलने आ गए। चाय की माँग हुई। बैदू घर चला गया था। बाबू जी के तीसरे नेत्र से अम्मा खौफ खाती थीं। अम्मा ने पीछे के दरवाजे से मुझे और मँझली को पास वाली चाय की गुमटी भेजा।
‘वह चाय पत्ती नहीं चाय बेचता है पर दो प्याले के लायक चाय पत्ती दे देगा।’
मँझली बोली, ‘अम्मा डर लगेगा।’
अम्मा खड़ी होकर हमें देखती रहीं। गुमटी में मेरे स्कूल के प्राचार्य मिल गए। वे कभी-कभी बाबू जी से मिलने आते थे। उन्होंने छिलके वाली गरम मूँगफली खरीद कर मुझे दे दी। अनायास हस्तगत हुई मूँगफली का अपार आनन्द था। लगभग भागते हुए हम दोनों घर आए। मूँगफली देखकर बाबू जी का तीसरा नेत्र खुल गया–‘प्रिंसिपल से क्यों ली? भूखों मरती हो? नाक कटाती हो…और जी तुम। होश नहीं रहता घर में क्या है क्या नहीं? लड़कियों को रात में भेजा। इतनी लापरवाही। प्रिंसिपल के सामने बेइज्जती हो गई…।’
बाबू जी का क्रोध सदा की तरह अम्मा पर केंद्रित हो गया था। उनकी राय में हमारी प्रत्येक हरकत में अम्मा का हाथ होना संभावित था। मूँगफली के लिए मिली दुत्कार, दीपावली पर आए उपहार, मिठाई, फटाके बैरंग लौटाए जाने के अफसोस ने दर्द बहुत दिया पर स्वाभिमानी बना दिया। मैं आज भी थोड़े में संतोष कर लेती हूँ। जो नहीं है उसका अफसोस नहीं करती।
लेकिन श्रीनाथ को लेकर अम्मा बहुत सोच करती थीं। उसे बड़ी माता निकली। उसका चेहरा देख कर रुलाई आती। हम बहनें उसे बहलाने का प्रयास करते वह खुजली और दर्द से तड़पता था। नीम की पत्तीदार टहनी से हवा करती अम्मा ट्रॉमाटाइज्ड। एक बार ऊँची कुर्सी से गिर कर पसर गया। अम्मा ट्रॉमाटाइज्ड–‘तुमलोग एक भाई को नहीं सँभाल सकती? यह एक और आ गई है (पाँचवी बहन सारंगगढ़ में जन्मी)। इसको देखें कि श्रीनाथ को देखें। श्रीनाथ को कुछ हो गया दाई हमको जीने न देंगी। दाई भक्त बाबू जी हमारे पच्छ में एक आखर न कहेंगे…।’
अम्मा मुझे अबूझ पहेली लगतीं। हमलोग दिनभर भारी श्रीनाथ को गोद में टाँगे फिरते हैं। मैदान में खेलते कम इसकी चौकसी अधिक करते हैं कि कंकड़-पत्थर बीन कर न खा ले। लेकिन आम्मा आरोप लगाती हैं। अम्मा का असमंजस अब समझ में आता है। वे श्रीनाथ की माँ थीं। उस पर पहला अधिकार उनका था पर दाई के लिए वे कुल को वंशधर देने वाली साधन मात्र थीं। वंशधर को क्षति पहुँचती है तो साफ तौर पर अम्मा गुनहगार। इक्कीसवीं सदी के खत्म होते दूसरे दशक में भी स्त्रियाँ ऐसे असमंजस से सौ प्रतिशत मुक्त नहीं हैं। तभी तो कन्या भ्रूण हत्या के मामले थम नहीं रहे हैं। वैसे मैं स्वीकार करती हूँ अम्मा-बाबू जी ने लड़के-लड़की में भेद नहीं किया। खाने-पहनने-शिक्षा के अवसर एक समान मिले। सिविल लाइंस के बच्चों की तरह हम बहनों के जन्म दिवस धूम-धाम से नहीं मनाए गए तो भाइयों के भी नहीं मनाए गए। फुलौरी वाली कढ़ी और गुलगुले बताते थे घर में किसी का जन्म दिवस है।
सारंगगढ़ में कक्का का तार पहुँचा था–बाबा नहीं रहे। उन दिनों सूचना-समाचार के लिए चिट्ठी-पत्री, तार जैसे माध्यम थे। आवागमन के सीमित साधन। पूरा परिवार ले जाना संभव न था। तार पाते ही बाबू जी ट्रक में बैठ कर रायगढ़, वहाँ से बस, ट्रेन पता नहीं किस साधन से रीवा गए। अम्मा को नींद न आती–‘तुम्हारे बाबू जी, रीवा कैसे पहुँचे होंगे कुछ पता नहीं। तेरही करके लौटेंगे, कब लौटेंगे, कुछ पता नहीं। न ढंग का घर-दुआर (रीवा में) है, न खेती-वाड़ी। बस तनखाह का सहारा। हे देवी-महारानी नेकी-कुसल रखना…।’
यह भय सदा हम सभी के साथ चला। बाबू जी को असमय कुछ हो गया तो हमलोग गहरी खंदक में जा गिरेंगे। मैंने तीसरी कक्षा उत्तीर्ण की। इंदौर के लिए तबादला हो गया। यहाँ कई न्यायाधीश। न अर्दली न बँगला। जेल रोड के एम.टी.एच. कंपाउंड में एलॉट हुए जाफरी वाले छोटे मकान को पहले वाले जज छोड़ नहीं रहे थे कि उनका अविवाहित भाई दो माह बाद होने वाली प्रतियोगी परीक्षा में बैठने के लिए मित्रों के साथ कंबाइंड तैयारी कर रहा है। मकान दो माह के बाद खाली करेंगे। मुझे याद नहीं वह कोचिंग थी या कंबाइंड स्टडी। संकोचवश मकान के लिए कार्रवाई न कर बाबू जी परिवार को लेकर सस्ते होटल में टिके रहे। जज ने प्रस्ताव दिया। वे भाई का भार बाबू जी पर डालना चाहते थे। ‘पांडे जी, आप यहाँ शिफ्ट हो जाएँ। बैठक दो माह के लिए मेरे भाई को दे दें।’
बाबू जी को लड़कियों वाले घर में युवक को रखना उचित नहीं लग रहा था पर होटल का खर्च अधिक था। एम.टी.एच. कंपाउंड के ठीक सामने रोड क्रॉस करने पर कचहरी थी। सारंगगढ़ की भाँति साइकिल से नहीं जाना पड़ेगा। उस बहुत पतले युवक का नाम मुझे याद नहीं है। हमलोग उसे चाचा कहते थे। वह दो वक्त के भोजन, चाय के साथ दो माह बैठक में रहा। वह वस्तुतः सभ्य था। मित्रों को कभी घर नहीं लाया। पूरा दिन गायब रहता। संकोचवश चार रोटी से अधिक न खाता। प्रातः नहा-धोकर एक बाल्टी पानी बैठक में रख लेता। अम्मा से बोला–‘आपके पास रहने-खाने में मुझे शर्म आती है। मेरे माता-पिता नहीं हैं। भाभी पराई हैं पर भैया से न हुआ, मेरा अलग रहने का कुछ इंतजाम कर देते। आपको कष्ट दे रहा हूँ। भगवान से प्रर्थना कीजिए यह परीक्षा पास कर अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊँ।’
आज सोचता हूँ अभाव वह था जो बंजारे या यह लड़का झेल रहा था। मेरा बचपन अभाव में बीता पर प्रतिष्ठा और सुविधाएँ बहुत थीं। आज बाबू जी पर गर्व होता है। कई-कई जिम्मेदारियों के बावजूद उन्होंने मूँगफली पर तीसरा नेत्र खोल लिया था। ये जज, भाई की अलग व्यवस्था करने में अव्यावहारिक कृपणता दिखा रहे थे। एक अपरिचित परिवार पर अनुज का भार डालते हुए संकोच हुआ न अनुज फिक्र।
रौनक वाला शहर इंदौर। केले ही केले। रेडीमेड वस्त्र, मिठाइयों की सजी दुकानें। रौनक हमारे लिए नहीं थीं। हमारा रहन-सहन अपरिवर्तनीय रहा। यहाँ जन्मे सबसे छोटे भाई गुड्डू और श्रीनाथ के लिए एक-दो बार रेडीमेड कपड़े आए पर पक्षपात की तरह नहीं। सिलाई मशीन पर हमारे लिबास अम्मा निपुणता से सिलतीं। लड़कों के शर्ट-पैंट नहीं सिल पाती थीं। बाबू जी और भाइयों के कपड़े दर्जी से सिलाए जाते। ठीक बगल में दो बेटियों, एक बेटे वाले रेलवे मजिस्ट्रेट रहते थे। स्तर बताता था ऊपरी कमाई करते हैं। वह परिवार अच्छे वस्त्र पहनता। ब्रेड-बटर (इंदौर की पाप्युलर ब्रेड बहुत प्रसिद्व थी) का नाश्ता करता। मूवी, मेला, पार्क जाता। एक बार उनकी बेटी विद्या (मेरी हमउम्र) ने मुझे अपनी रेडीमेड फ्रॉक दी। बाबू जी का तीसरा नेत्र खुल गया। ‘किसकी फ्रॉक पहने हो?’
‘विद्या की।’
‘कहा, नाक न कटाओ पर मानती नहीं। अभी वापस करो। मेरे पास दो जोड़ी कपड़े हैं (काले कोट, सफेद कमीज-पतलून के अतिरिक्त) तो दूसरे से माँग कर पहनूँ? पढ़ाई में ध्यान दो। सब कुछ मिलेगा।’ कहकर बाबू जी ने अम्मा को लपेटे में लिया। ‘देखती नहीं लड़कियाँ क्या सीख रही हैं? गलत रास्ते भटकाते हैं…।’
बाबू जी कचहरी चले गए। कॉलेज गोइंग जीजी ने अम्मा के समक्ष उपद्रव किया।
बाबू जी घूस न लेकर, जैसे हमारे ऊपर एहसान कर रहे हैं। इतना बड़ा परिवार। दाई-बाबा नहीं रहे पर रीवा भेजने में कमी नहीं करते। जानते हैं कक्का चार लपाड़ियों को घर में घुसेड़ कर जुआ खेलते हैं। भाँग घोटते हैं। कक्का की चालाकी देखो तीन पन्ने की चिट्ठी लिख कर घर में नल फिटिंग, बिजली फिटिंग, मरम्मत कराने के बहाने अधिक पैसा माँगते हैं। बाबू जी भेजते हैं। अम्मा हमलोग रीवा गए तो थे। न नल लगा, न बिजली। बाबू जी ने नहीं पूछा कक्का ने पैसा कहाँ फूँक दिया, लेकिन मुझे कॉलेज ट्रिप में माण्डू नहीं जाने दिया। लड़कियाँ बन-ठन कर कॉलेज आती हैं। मेरे पास चार जोड़ी कपड़े। जी ललकता है अम्मा…।’
अम्मा सांत्वना ही दे सकती थीं, ‘तभी कहती हूँ खूब पढ़ो। जिंदगी बनाओ।’
मुझे जीजी की मुद्रा कातर लगती। इच्छा होती जादू वाली सुपारी मुझे मिल जाए तो मैं सबके अरमान पूरे कर दूँ।
एम.टी.एस. कंपाउंड में एक पुस्तकालय था। पुस्तकालय के टोपीधारी भाईजी अच्छे स्वभाव के थे। मैं अक्सर पुस्तकालय जाती। परी, जादूगर, राजा, रानी वाली बाल कहानियों को पढ़कर कल्पना में डूब जाती। मुझे कहानी ख़ास पसंद थी–परी ने दुःखी बच्ची को जादुई सुपारी देकर कहा, ‘सुपारी को मुँह में रख लेने से तुम किसी को दिखाई नहीं दोगी, पर तुम सब कुछ देखती रहोगी।’ बच्ची ने सुपारी के जादू से लोगों से जम कर बदला लिया। मैं सोचती वह सुपारी मुझे मिल जाए तो दुकानों से झोला भर केले, कपड़े, मिठाई चुरा लाऊँ। पैसे चुरा कर जीजी को माण्डू भेजूँ। उस लड़की का पता लगाऊँ जिसने मेहनत से बनाई मेरी सूत की मोटी लच्छी को मेरे बस्ते से चुरा लिया था। स्कूल में हमें तकली से सूत कातना सिखाया जाता था। तकली की ऊपरी हुकदार नोक में रूई की पोनी फँसा कर तकली घुमाते हुए मैं बहुत बारीक सूत कातती थी। सूत को अटेरन में लपेट कर बनाई गई मोटी लच्छी पर शिक्षिका से शाबासी मिली थी लेकिन चोरी हो गई।
इदौर में मैंने चार, पाँच, छह कक्षाएँ पास की। बाबू जी प्रोन्नत (एडीशनल डिस्ट्रिक्ट जज) होकर तबादले पर टीकमगढ़ आ गए। अब ईमानदारी का उल्लेख हो न हो, तब होता था। ईमानदारी, सटीक न्याय के फलस्वरूप बाबू जी को प्रमोशन जल्दी मिले। ग्यारह साल जिला व सत्र न्यायाधीश रहे। सेवानिवृत्ति के बाद दो साल के लिए लोकायुक्त फिर चार साल के लिए कनज्यूमर फोरम के चेयरपरसन बनाए गए। 1975-76 के दौर में जिन डाकुओं ने आत्मसमर्पण किया था उनके लिए सागर (म.प्र.) में स्पेशल जेल कोर्ट बनाई गई थी। बाबू जी को वहाँ भेजा गया। पूरन सिंह जिसे सब पूजा बब्बा कहते थे सहित कई डाकुओं ने बाबू जी के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर जेल में अपने बीहड़ स्वभाव में काफी सुधार किया।
छोटा जिला टीकमगढ़। अच्छा मकान। कुक सहित कई अर्दली।
बगल में दक्षिण भारतीय बड़े इंजीनियर (पी.डब्ल्यू.डी. के ई.ई.) रहते थे। मुझसे दो वर्ष छोटे इकलौते पूत की हिंदी सुधारने के लिए नंदन, चम्पक, पराग, धर्मयुग आदि पत्रिकाएँ मँगाते। वह न पढ़ता। मेरी पढ़ने में लगन थी। मैं उससे माँग कर अक्षर-अक्षर बाँच डालती। सोचती हूँ उन्हीं दिनों निहायत गुप्त तरीके से मेरे भीतर रचनाकार तैयार हो रहा था। निबंध प्रतियोगिता में हर बार प्रथम आती। बाबू जी के नियंत्रण में बोलने का अभ्यास न हुआ, अतः भाषण प्रतियोगिता में भागीदारी नहीं की। आज भी किसी साहित्यिक-सांस्कृतिक कार्यक्रम में बोलती हूँ तो बेचैनी होती है।
टीकमगढ़ में हम बहनें टीन एज की ओर अग्रसर थे। बाबू जी ने चौकसी बढ़ा दी। हम सिविल लाइंस के मैदान में शाम को खेलने न जा सके इसलिए युक्तिपूर्वक एक वृद्ध ट्यूटर नियुक्त कर दिया जो सरे शाम हमलोगों को सामूहिक रूप से बैठा कर हिंदी, अँग्रेजी, संस्कृत पढ़ाने लगे। बाबू जी का जोर था भाषाओं का सम्यक ज्ञान होना चाहिए।
टीकमगढ़ की दीवाली थी। एक व्यक्ति बड़े झोलों में मिठाइयाँ, नमकीन, फटाके और एक कैरम बोर्ड लिए आया। अम्मा ने स्वीकार नहीं किया।
‘मेरे सेठ इस बँगले में हर साल दीवाली का सामान भेजते हैं।’
कहकर वह झोले छोड़कर रफू चक्कर हो गया। अम्मा को राह नहीं। झोले कहाँ ठिकाने लगाएँ? बाबू जी जान लेंगे तो आरोप तय है–तुमने सख्ती से मना नहीं किया होगा। बाबू जी के कचहरी जाने के उपरांत कैरम खेला जाता। मिठाई खाई जाती। फटाके फूटते। ई.ई. का पूत हँसता।
‘दिन में फटाके फोड़ते हो। कितने बेवकूफ हो।’
श्रीनाथ कहता, ‘बेवकूफ नहीं चतुर हैं। रात में बाबू जी नहीं फोड़ने देंगे।’
टीकमगढ़ में मैं सात, आठ, नौ कक्षा पास करते हुए बचपन ऊबडूब।
हैरानी होती है। बाबू जी की अवधारणा पता नहीं कब मेरी अवधारणा बन गई। उनकी ईमानदारी ने संतोष करना सिखा दिया। नियंत्रण ने अंतर्मुखी बना दिया। जहाँ ब्याह दिया हम बहनें अपने हाथ की लकीरें लिए चली गईं। किराये के छोटे घर में गृहस्थी बसाई। बरसों संघर्ष किया। प्रत्येक बहन के विवाह में बाबू जी का जी.पी.एफ., अम्मा की साड़ियों वाली पेटी खाली होती रहीं, फिर भी उचित दहेज न लाने की कटुता सही। आज जरूरतें पूरी हो रही हैं। ठीक-ठीक खा-पहन रही हूँ। जब बाबू जी को याद करते हुए कोई कहता है–ऐसा ईमानदार, कर्मठ, न्यायप्रिय जज नहीं देखा तब मेरा मस्तक ऐसा उन्नत हो जाता है मानो वे मेरी ही बदौलत अपनी धुर ईमानदारी पर अडिग रह पाए!
Image name: Children by the sea
Image Source: WikiArt
Artist: Charles Atamian
This image is in public domain