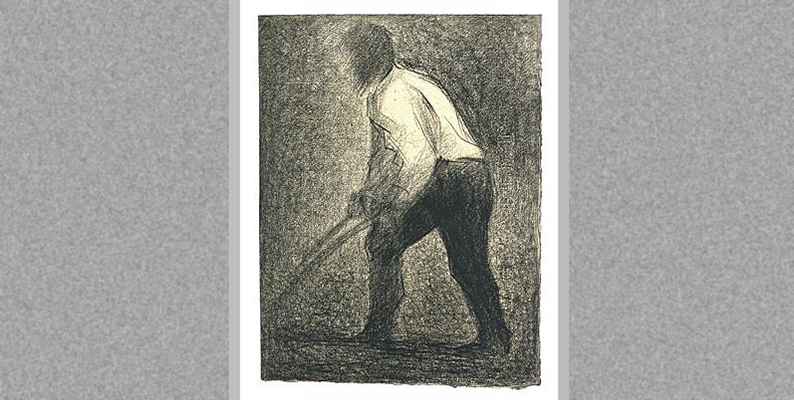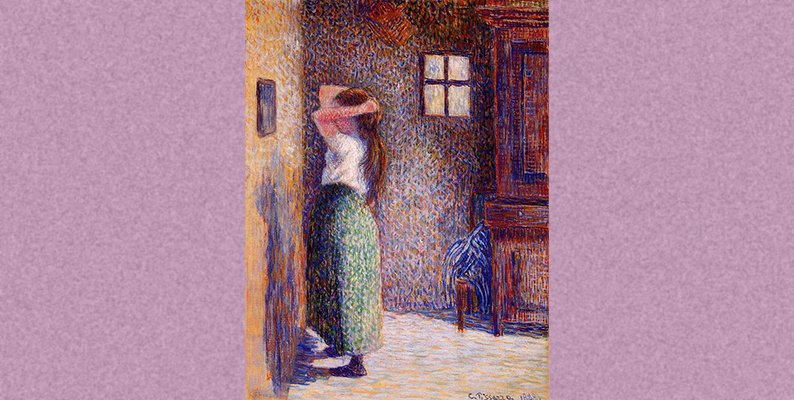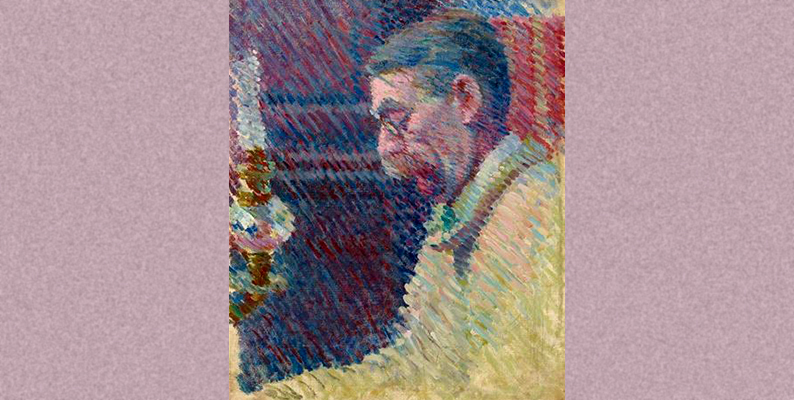मैं और मेरा कविता कर्म
- 1 December, 2023
शेयर करे close
शेयर करे close

शेयर करे close
- 1 December, 2023
मैं और मेरा कविता कर्म
मेरे लिए अपने कविता कर्म पर बोलना आसान भी है और कठिन भी। आसान इसलिए क्योंकि मैं जो अपने जीवन, समाज, देश, परिवेश और अपने आसपास देखता हूँ, सुनता हूँ, महसूस करता हूँ, उससे संवेदित होता हूँ और फिर उससे जो विचार पैदा होते हैं वही तो मेरी कविताओं में छनकर आते हैं। कवि-लेखक का उनकी रचनाओं से अधिक असली परिचय भला और क्या हो सकता है। औरों की तो मैं नहीं जानता लेकिन मेरा असली परिचय तो मेरी कविताएँ ही हैं।
मैंने कविताएँ कब से लिखनी शुरू की, यह ठीक-ठीक बताने में मैं असमर्थ हूँ। लेकिन यह बताने में मुझे कोई संकोच नहीं कि मेरे मानस और चेतना का निर्माण कविता लिखने से बहुत पहले ही हो चुका था। मैंने जीवन में सबसे पहले आत्मसम्मान, सामाजिक न्याय, अस्तित्व और गरिमा का बोध हासिल किया। और ये सब कुछ उस गाँव में हुआ जहाँ मेरा भी जन्म हुआ और जिसको अम्बेडकर ने नरक का द्वार कहा है। मैट्रिकुलेशन तक मैंने गाँव में ही रहकर पढ़ाई-लिखाई की। हमारा गाँव जो 8-10 हज़ार लोगों की आबादी वाला गाँव है अन्याय और अपमान की हाल-फिलहाल तक चीन से भी लंबी दीवार खड़ा कर रखा था। गाँव के दलित-पिछड़े किसी ब्राह्मण को उनके नाम से संबोधित नहीं कर सकते थे। अगर किसी ने संबोधित कर दिया तो उसकी शामत आ जाती। आप गाँव के उस पुल पर नहीं बैठ सकते थे जिस पर ब्राह्मण बैठे होते थे। अगर आप अनजाने में बैठ गए तो आपकी चमड़ी उधेड़ दी जाती थी। आप कितने भी अमीर, विद्वान और लोकप्रिय क्यों नहीं हों, अगर आप किसी ब्राह्मण के यहाँ खाना खाते हैं तो आपको अपना जूठा पत्तल खुद उठाना पड़ेगा। आपकी छोटी-सी चूक पर भी स्कूल के गुरुजी आपके कान तब तक उमेठते जब तक कि वे लाल नहीं हो जाते और चमड़े नहीं छिल जाते। ऐसी-ऐसी हकीकतों की लंबी फेहरिश्त है जिनसे मेरा सामना होता, तो मेरी चूलें हिल जातीं। मुझे अपने होने पर ग्लानि होती। मैं अपने अस्तित्व की खोज करने लग जाता। आत्मसम्मान और सामाजिक न्याय के लिए मैं तड़प उठता।
गाँव की सामाजिक स्थितियों की और लोगों पर क्या असर होता, ये तो मैं नहीं जानता लेकिन मैं विचलित हो जाता और विद्रोह कर उठता। हो सकता है कि इसका कारण मेरी संवेदनशीलता हो। गाँव के सामाजिक वातावरण से मुझे धीरे-धीरे विरक्ति होने लगी और मैंने सार्वजनिक जगहों पर आना-जाना लगभग बंद-सा कर दिया। अभी भी गाँव जाता हूँ तो उन्हीं लोगों से मिलने की इच्छा होती है जो मेरा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपमान नहीं करें। नहीं तो मैं अपने घर में कैद होना ज्यादा मुनासिब समझता हूँ। आखिर दुनिया के सारे प्रपंच और कारोबार के केंद्र में सम्मान ही तो है। दुनिया की सारी लड़ाइयाँ सम्मान के लिए ही तो लड़ी गई हैं। बगैर सम्मान के न तो आप आत्मविश्वास प्राप्त कर सकते हैं और न ही कुछ करने के लिए साहस या उत्साह बटोर सकते हैं।
गाँव के दलितों-पिछड़ों के साथ अपमान, अन्याय में 90 के दशक से ब्रेक लगना शुरू हुआ और चुनौतियाँ दोनों तरफ से मिलनी शुरू हुईं। मेरे परिवार की थोड़ी बेहतर आर्थिक स्थिति और शिक्षा ने इसमें बहुत ही कारगर भूमिका का निर्वहण किया। गाँव के प्रभु वर्ग को सबसे पहली चुनौती मेरे पिता जी से मिली। जिनकी चतुराई और बुद्धिमता ने उनकी मनमानी पर रोक लगाने का काम शुरू किया। उन्होंने गरीब-गुरबों को उनकी ताकत का अहसास कराया और उन्हें संगठित किया। अब लड़ाई आर-पार की होने लगी। हरेक गैर-बराबरी का प्रतिकार किया जाने लगा। सामाजिक अन्याय के शिकार लोगों की चेतना जागने लगी। उनमें धीरे-धीरे आत्मबल आने लगा, जिससे हरेक क्षेत्र में उनमें आगे बढ़ने की भूख जगी। इन्हीं स्थितियों-परिस्थितियों के बीच मैं बड़ा होता रहा और छोटी-सी-छोटी घटनाओं को भी भूलाना मेरे लिए असंभव होता रहा।
मैंने ‘जाति’ पर सबसे ज्यादा यदि कविताएँ लिखी हैं तो उसके पीछे उपर्युक्त घटनाएँ और दुर्घटनाएँ ही परोक्ष रूप से काम करती रही हैं। मेरा अतीत यदि कुछ और होता तो कभी भी जाति मेरा प्रिय विषय नहीं होती। वैसे भी बगैर जाति के आप न तो भारत की कल्पना कर सकते हैं और न ही साँस ले सकते हैं। आप दिल्ली तो छोडि़ए, उज्जैन भी बगैर जाति के नहीं जा सकते। दिल्ली तो वैसे भी सबसे बड़ी जातिवादी जगह हो चुकी है। भारत का अंत भी जाति ही करेगी। इसने बुद्ध और अम्बेडकर का आविष्कार वैसे नहीं किया। यह मनु से पहले से ही सबसे बड़ी समस्या रही है। मनु ने तो गैर-बराबरी को सिर्फ संहिताबद्ध किया। लेकिन प्रभु वर्ग सदैव यही कहता रहा कि जाति तो कब का खत्म हो चुकी। यदि वह ऐसा नहीं कहेगा, तब फिर उनके विशेषाधिकार पर आँच आ सकती है। विडंबना देखिए, जाति के सवाल को अभी भी इग्नोर कर दिया जाता है। दलित साहित्य और प्रेमचंद को यदि छोड़ दिया जाए, तो पूरा द्विज साहित्य इस सवाल की उपेक्षा करते लिखा हुआ मिलेगा। आज तो हम और भी भयंकर दौर से गुजर रहे हैं। दिल्ली में तो दलित, पिछड़ा और मुसलमान के नाम का उच्चारण करने से भी लोग डरने लगे हैं। क्या पता, उन्हें कब सलाखों के पीछे धकेल दिया जाए। ऐसे हालात मुझे जाति पर लिखने के लिए और प्रेरित करते हैं। मेरी फितरत अभाव को दूर करने की रही है। लोग इस सवाल से जितना मुँह मोड़ेंगे, मैं इस सवाल को और जोर से उठाता रहूँगा। मैंने तय किया है कि जाति को लक्ष्य करके इतनी कविताएँ लिखूँगा कि समकालीन कविता की मुख्य प्रवृत्ति के तौर पर कालांतर में उसकी पहचान की जाने लगे।
जातियों पर लिखने के कारण कई लोग मुझे दलित कवि समझने लगते हैं। उन्होंने यह मान लिया है कि जातियों पर लिखने का काम दलित ही कर सकते हैं। जबकि ऐसी बात नहीं है। कबीर, प्रेमचंद, रेणु, नागार्जुन दलित नहीं थे लेकिन उन्होंने जातियों पर लिखा। सिर्फ दलित जातियों पर ही नहीं बल्कि सभी जातियों पर लिखा। मेरी कविताओं की भी पड़ताल करते हुए कोई यह नहीं कह सकता कि मैंने किसी ख़ास समुदाय की जातियों या ख़ास जाति पर ही लिखा है। कास्ट डिस्कोर्स की परिधि में सिर्फ दलित जातियाँ ही नहीं आती हैं बल्कि ओबीसी जातियाँ भी आती हैं, जिनकी आबादी दो-तिहाई से भी अधिक आँकी जा रही है। अब तो कास्ट डिस्कोर्स की परिधि में पसमांदा मुसलमान भी आने लगे हैं। दलित, ओबीसी, पसमांदा मुसलमानों की तो छोडि़ए मैंने तो द्विज जातियों पर भी कविताएँ लिखी हैं। उनकी अस्मिता और हक की बात की है। उत्तर भारत की तो छोडि़ए, मैंने दक्षिण भारत की जातियों पर भी लिखा है। वरिष्ठ आलोचक-प्राध्यापक कमलेश वर्मा मेरे काव्य-संग्रह ‘किस-किस से लड़ोगे’ पर टिप्पणी करते हुए कहते हैं–‘जाति समस्या पर सबसे ज्यादा कबीर ने लिखा है। लेकिन पहली बार सबसे ज्यादा 60 से ज्यादा जातियों का उल्लेख पंकज चौधरी की कविताओं में मिलता है।’
मेरे कास्ट डिस्कोर्स के अंतर्गत यदि चमार, दुसाध, डोम, हलखोर, मुसहर, धोबी, पासी आदि आते हैं, तो उसमें हज्जाम, बढ़ई, कहार, कुम्हार, मल्लाह, कानू, धानुक, तेली, कलबार, कुशवाहा, यादव आदि भी आते हैं। उपर्युक्त जितनी भी जातियों का मैंने उल्लेख किया है, सबकी सामाजिक स्थिति कमोबेश एक समान है। सबको सामाजिक न्याय और सम्मान की दरकार है। ये जातियाँ कितनी भी अमीर क्यों न हो जाएँ, इन्हें वो मान-सम्मान कभी नहीं मिलता, जो दूसरी जातियों को सहज ही मिल जाता है। मुझे इस बात की तसल्ली है कि मैं दलित साहित्य का भी विस्तार कर रहा हूँ और तथाकथित मुख्यधारा के साहित्य का भी। मेरी कविताओं में आदिवासी भी हैं, मुसलमान भी और द्विज भी हैं।
समकालीन कविता के बहुलांश को मैं बकवास मानता हूँ। वहाँ देश की 80-85 फीसदी जनता की कथा गायब है। ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन दलित-बहुजन की बेटियाँ जलाई नहीं जातीं। उनकी बहू-बेटियों का बलात्कार नहीं होता। अमानवीयता, भेदभाव, शोषण आज भी दलित-बहुजन की नियति बनकर रह गई है। इतना कुछ होने के बाद भी स्वनामधन्य कवियों के मुखारबिंद से आपको यही सुनने को मिलेगा कि ‘जाति’ कहाँ है? जाति तो कब का खत्म हो गई। आखिर ये किस प्रगतिशीलता और जनवाद का बुझौवल बुझाते रहते हैं? इनकी कविताओं का यदि आप गंभीरता से अध्ययन करेंगे, तो पाएँगे कि इनकी कई कविताओं में दलित-बहुजन नायकों के प्रति कटूक्तियाँ और घृणा व्यक्त की गई हैं। गरीब-गुरबों के आंदोलनों का मज़ाक और उपहास उड़ाया गया है। ऐसे ही दलित साहित्य और कास्ट डिस्कोर्स के साहित्य की महती जरूरत नहीं महसूस की गई।
मेरे कविता कर्म की मोटा-मोटी मूल चिंता यही है। मेरा कवि दिन-रात इसी चिंता में जलता-गलता रहता है। जाति की चिंता इतनी बड़ी है कि उसने और चिंताओं को ग्रस लिया है। यह चिंता उन सबको खा लेती है जिनको जाति का लाभ नहीं मिलता। भारत को सुंदर और बेहतर बनाने के लिए हर एक को इस समस्या का समाधान पहले करना होगा।
(5 नवंबर, 2023 को नई दिल्ली में ‘नई धारा रचना सम्मान’ अर्पण समारोह में दिए गए वक्तव्य।)