प्रसाद की ‘कामायनी’
- 1 February, 2016
शेयर करे close
शेयर करे close
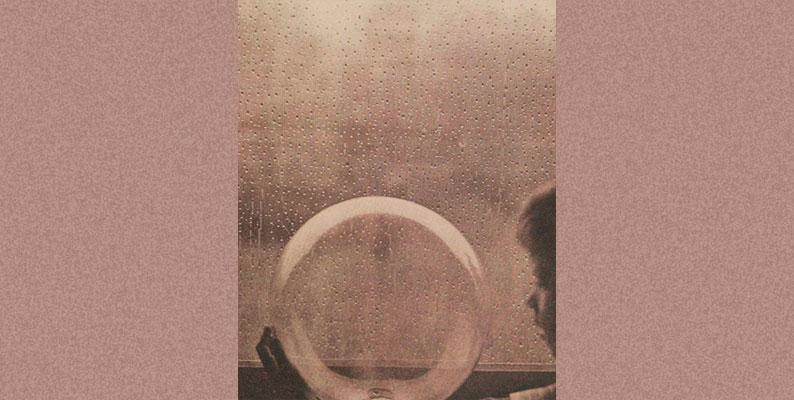
शेयर करे close
- 1 February, 2016
प्रसाद की ‘कामायनी’
मानवाधिकार का नहीं, मानव-प्रत्यभिज्ञा का काव्य
‘कामायनी’ भारतीय औपनिषदिक जीवन-मूल्य पर आधारित काव्यकृति है। कामायनीकार ने इसके निरूपण के लिए समरसतावादी ‘प्रत्यभिज्ञा’ दर्शन को आधार बनाया है। वस्तुतः यह एक आद्य मिथक की ऐसी पुनस्सर्जना है, जिसमें समस्याएँ तो बाह्य भौतिक संसार में फैली हैं, पर उसका समाधान अभ्यंतर की प्रगुणात्मक सिद्धि में निहित है। व्यक्ति का यह आंतर परिष्कार ही स्थायी समाधान देने वाला है। व्यक्ति की मानसिकता के इस परिष्करण से ही समाज-कल्याण और व्यापक लोकहित संभव है। अतः ‘कामायनी’ में मनु भौगोलिक हिमालय (‘अस्ति उत्तरस्यां दिशि देवतात्मा नगाधिराजः हिमालयः’) मात्र की यात्रा नहीं करते। उसके कहीं विपरीत यह आंतरिक हिमालय के ऊर्ध्वारोहन की यात्रा करते हैं। यही व्यक्ति को वह स्थायी समत्व-दृष्टि प्राप्त हो पाती है, जिससे व्यक्ति समाज और लोक का कल्याण हो सके। इस आंतर अर्थ-गह्वर (Semantic Enclave) में प्रवेश नहीं कर पाने के कारण ही ‘कामायनी’ के आलोचकों ने ‘कामायनी’ में निरुपित जीवन-दर्शन को ‘पलायनवादी’ मान लिया है। पर वस्तुस्थिति इसके ठीक विपरीत है।
औपनिषदिक जीवन-मूल्य कहीं से भी सांसारिक समस्याओं से भागने और भगाने वाला जीवन-मूल्य नहीं है, बल्कि यह आत्मशोधन और लोकहित हेतु ‘आत्मज्ञान’ उपलब्ध करने का व्यक्ति-परिष्कारक प्रवृत्तिमार्गी जीवन-मूल्य है। इसी से समानता की अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है। इसीलिए ‘ईशावास्योपनिषद्’ में ‘आत्मज्ञान’ प्राप्त करने हेतु तत्पर नहीं होने और इस दिशा में नहीं बढ़ने वाले अथवा इससे विमुख रहने वाले को ‘आत्महंता’ कहा गया है। ‘कामायनी’ में अंततः श्रद्धा मनु को ‘आत्महंता’ होने से बचाती है और उसे ‘आत्मज्ञान’ उपलब्ध कराने में मार्ग-दर्शिका बनती है, जिससे उसका अंत:करण; मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, मलरहित, परिष्कृत हो सके और उसे सामाजिक समत्व एवं पूर्ण समत्व की दृष्टि और सिद्धि प्राप्त हो सके। वस्तुत ‘कामायनी-रजोगुण से सतोगुण (फ्रायड-निरूपित इदम्/ID, अहम/Ego से सुप्राहम् Super Ego) के गंतव्य तक, ‘पितृयान’ से ‘देवयान’ के गंतव्य तक, ‘विवाह’ से ‘उद्वाह’ के गंतव्य तक, ‘कवित्व’ से ऋषित्व’ के गंतव्य तक, भेदबुद्धि से समत्व बुद्धि के गंतव्य और ‘सकामता’ से ‘आप्तकामता’ के गंतव्य तक की सर्जकीय-भावकीय यात्रा संपन्न करने-कराने वाला एक अद्वितीय भारतीय महाकाव्य है।
इस यात्रा का सहयात्री बनकर गंतव्य प्राप्त कर लेने वाले पाठक, आलोचक को यह प्रतीति सहज ही हो जाती है कि कामायनीकार अपनी इस कृति में व्यक्ति के आभ्यन्तर परिष्कार, सामाजिक समत्व और लोक-कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। पर वह अपनी इस प्रतिबद्धता का स्वीकरण-प्रतिबिंबन और अपनी प्रवृत्तिमार्गी समाधान बाहरी संसार में प्रति-संघर्ष के द्वारा नहीं दर्शा कर ‘अंत:करण’ के परिवर्तन और शुद्धिकरण के द्वारा प्राप्त और प्रस्तुत करता है, जिसका मूलाधार भारतीय संस्कृति और दर्शन है। यदि यह उसका अभीष्ट नहीं होता, तो वह अपनी काव्यकृति में सांसारिक स्वार्थमय छीनाझपटी, अबाधित अधिकार और काम-सुख भोगने की सजग, स्पृही हठधर्मिता, संघर्ष-प्रति संघर्ष हिंसा, प्रतिहिंसा आदि का इतने विस्तार से निरूपण-चित्रण नहीं करता। यह संसार की न केवल समकालीन, अपितु सनातन और शाश्वत समस्या का निरूपण है, जिसका स्थायी समाधान मनुष्य के अभ्यंतर में उसकी मानसिकता को रूपांतरित-गुणांतरित कर निर्दिष्ट किया गया है। इस गुणांतरण से वह समाज के लिए भेद-बुद्धि त्याग कर कहीं अधिक उपयोगी सिद्ध हो पाता है। ‘कामायनी’ को उसके इस पूरे परिप्रेक्ष्य और उसकी कथ्य-संरचना के साकल्य में देखने की अपेक्षा रही है और, जिसकी उपेक्षा प्रायः हिंदी के कवि-आलोचकों ने लगातार की है। इसका एक बड़ा कारण उपनिषद् और भारतीय दर्शन-विरोधी उनकी पूर्वग्रस्त धारणा रही है। वे या तो राजा राममोहन राय की तरह आधुनिकता की झोंक में भारतीय दर्शन को व्यर्थ, निरुपयोगी और निस्सार समझने वाले रहे हैं या जवाहरलाल नेहरू की तरह पश्चिमी ज्ञान-विज्ञान की मोहांधता में भारतीय ज्ञान को पिछड़ापन का प्रपंची खजाना मानने वाले रहे हैं, अथवा तथाकथित आधुनिक भारतीय बुद्धिजीवी की तरह अभ्यंतर; आत्माद्ध की उपेक्षा कर बाह्य (देह) को ही एकमात्र सत्य मानने वाले रहे है तथा मार्क्सवाद और मार्क्सवादी समाधान को ही क्रमशः एक मात्रा सार्थक विचारधारा और एकमात्र उपयुक्त समाधान मानने वाले सर्जक-आलोचक रहे हैं।
‘कामायनी’ में ‘आत्मवादिता’ और ‘दकह्वादिता’ के बीच तथा ‘भारतीय संस्कृति’ और ‘पाश्चात्य संस्कृति’ के बीच तनाव देखने को मिलता है। ‘कामायनी’ की समस्या का समाधान इसी द्वंद्वात्मकता का परिणाम है। ‘कामायनी’ देव संस्कृति बनाम आज की पाश्चात्य संस्कृति, जो एक संतुलनहीन, घोर अतिरेकी संस्कृति है, को ही वैश्विक दुःख का मूल कारण मानती है। इसके केंद्र में मनुष्य की निर्बाध स्वच्छंद ‘इच्छा’ (Desire) और मनुष्य का निरनुशासित ‘अंत:करण’; मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार सक्रिय रहता है। प्रसाद ने इससे मुक्ति का शाश्वत उपाय बनाम समाधान भारतीय संस्कृति के आधार पर निर्दिष्ट किया है। ‘कामायानी’ का आरंभ जिस देव संस्कृति के ध्वंस से होता है और कुछ अंतराल के बाद पुनः उसी दिशा में ‘कामायनी’ की कथा का विकास होने लगता है, वह बाहर-बाहर सुख को तलाशने वाली आज की भोगवादी पाश्चात्य संस्कृति ही है। इसके केंद्र में निर्बाध अधिकार-सुख की पिपासा है। यह प्यास कंचन और कामिनी के अनवरत भोग से भी नहीं बुझती है। पर ‘निर्वेद’ सर्ग के बाद श्रद्धा मनु को इस संस्कृति के मोह से मुक्त कर जिस दिशा में ले चलती है, वह विशुद्ध भारतीय संस्कृति में स्वीकृत ‘अभ्यंतर’ की दिशा है।
आज से 107 वर्ष पूर्व और ‘कामायनी’ के रचनाकाल से 27 वर्ष पूर्व महात्मा गाँधी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ‘हिंद स्वराज’ में पाश्चात्य भौतिकतावादी सभ्यता को ‘चांडाल सभ्यता’ कहा था। उन्होंने लिखा था कि ‘इस सभ्यता की सही पहचान तो यह है कि लोग बाहरी खोजों में और शरीर के सुख में धन्यता-सार्थकता और पुरुषार्थ मानते हैं। यही नहीं, उन्होंने अपने अख़बार ‘यंग इंडिया’ के 11.08.1927 के अंक में लिखा था कि ‘भारत का भविष्य उस रक्त-रंजित मार्ग पर नहीं है, जिस पर चलते-चलते पश्चिम अब खुद थक गया है…भारत के सामने इस समय अपनी आत्मा को खोने का खतरा उपस्थित है और यह संभव नहीं है कि अपनी आत्मा को खोकर वह जीवित रह सके।’ उन्होंने अपने ‘हिंद नवजीवन’ के अंक में लिखा था कि ‘शारीरिक सुख-सुविधाओं की सतत खोज और उनकी संख्या में तेजी से हो रही वृद्धि ऐसा ही एक दोष है और मैं साहसपूर्वक यह घोषणा करता हूँ कि जिन सुख-सुविधाओं के वे (यूरोपीय) गुलाम बनते आ रहे हैं, उनके बोझ से यदि उन्हें कुचल नहीं जाना है, तो यूरोपीय लोगों को अपना दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा।… यदि मैं निश्चयपूर्वक जानता हूँ कि भारत के लिए इस सुनहले मृग के पीछे दौड़ने का अर्थ आत्मनाश के सिवा और कुछ न होगा।’ इसी प्रकार उनका यह अभिमत भी ‘कामायनी’ के संदर्भ में द्रष्टव्य और स्मरणीय है–‘मेरा पूरा विश्वास है कि भारत के पास पूरी दुनिया के लिए एक संदेश है।’ (यंग इंडिया, 6.8.1925) प्रसाद जी ने स्वयं भारतीय संस्कृति और भारतीय दर्शन की गोताखोरी की थी। उन्हें इनका तलान्वेषी गहन बोध था। इसके अतिरिक्त उस युग में भारतीयता के संदर्भ में महात्मा गाँधी जो भी लिख-बोल रहे थे उससे प्रसाद की अपनी मान्यता भी सम्पुष्ट होती दीखती है। ‘कामायनी’ में उन्होंने पूरे विश्व के कल्याण के लिए जैसे भारतीय संस्कृति और दर्शन का वही संदेश प्रस्तत किया है। प्रसाद की जीवन-दृष्टि राजाराम मोहन राय, मानवेंद्रनाथ राय और जवाहरलाल नेहरू की पाश्चात्य जीवन-दृष्टि से मेल नहीं खाती है। वह तो महर्षि अरविंद, कवींद्र रवींद्रनाथ ठाकुर और महात्मा गाँधी की भारतीय जीवन-दृष्टि की सहचरी है। ‘कामायनी’ में श्रद्धा और मनु के माध्यम से सनातन मानव-जीवन के, जिसमें आज का मानव-जीवन भी सहज समाविष्ट है, पारस्परिक संघर्ष, अतिचार, हिंसा-प्रतिहिंसा, अधिकार-प्रमत्तता आदि में मुक्ति के लिए प्रसाद द्वारा सुझाये गये समाधान का मूल्यांकन उपर्युक्त विवेचन के संदर्भ में ही किया जाना चाहिए।
‘कामायनी’ में यदि भारतीय ज्ञान की तप-साधना है, तो उसका लक्ष्य वैयक्तिक मुक्ति नहीं है, जैसा पंत और दिनकर मान लेते हैं। यहाँ योग-साधना उस ‘निवेश’ के रूप में प्रस्तुत और प्रस्तावित है, जिसका निर्गत लोक-कल्याण और लोक-अभ्युदय है। जैसा आचार्य क्षितिमोहन सेन का मानना है, ‘भारतीय ज्ञान की तपस्या कोई व्यक्तिगत सुख-समृद्धि की तपस्या नहीं है। वह सबके अभ्युदय के लिए हैं।’ ‘कामायनी’ उसी को चरितार्थ करती है।
मुक्तिबोध ने ‘कामायनी’ पर जितने भी आरोप किये हैं, वह सब केवल इसलिए कि ‘कामायनी’ में निरूपित समाधान मार्क्सवाद या कि साम्यवाद पर क्यों नहीं आधारित है। मुक्तिबोध की दृष्टि में आज की जागतिक समस्याओं का समाधान आंतरिक नहीं, बाहरी संघर्ष और क्रांति का समाधान है। वह अहिंसक नहीं हिंसक समाधान है। पर प्रसाद ऐसे आरोपित समाधान के पक्षधर नहीं हैं। उनका विश्वास मानसिकता के आमूलचूल सतोगुणी परिवर्तन पर बल देता है। यहाँ मार्क्सवाद अपनी विफलता के कारण स्वतः खारिज हो जाता है। विवेकानंद की मान्यता है कि ‘सामान्यवादी सिद्धांतों का आधार आध्यात्मिक ही होना चाहिए।’ (विवेकानंद साहित्य, खंड-4, पृष्ठ-252) पर वर्तमान साम्यवाद इससे विरहित है। यही नहीं, विवेकानंद यह भी मानते हैं कि ‘कोई भी समाजवादी संस्था, जो धर्म पर अथवा मनुष्य के भीतर के शुभ पर आधारित न हो, स्थायी नहीं हो सकती।’ (वही, खंड-4, पृष्ठ-243) विवेकानंद के साथ-साथ महात्मा गाँधी भी वर्तमान मार्क्सवाद को नकारते हैं, ‘पाश्चात्य समाजवाद या साम्यवाद उचित नहीं है। उसमें हिंसा का रंग चढ़ा हुआ है।’ (गाँधी वाङ्मय, खंड-58, पृष्ठ-227) और फिर ‘रूसी ढंग का जबर्दस्ती थोपा गया समाजवाद भारत को कभी स्वीकार न होगा।’ (वही, खंड-64, पृष्ठ-348) कारण यह है कि यह तथाकथित समाधान स्वतः समस्याएँ उत्पन्न करने लगता है। इसका जो एकमात्र समाधान वर्ग-संघर्ष है, वह नितांत एकांगी और अस्थायी है। आज के जीवन की बहुत सारी समस्याओं तक इसकी पहुँच भी नहीं हो पाती है। पर ‘कामायनी’ में प्रसाद ने भारतीय संस्कृति, अध्यात्म और दर्शन के द्वारा ‘प्रत्यभिज्ञा’ की आत्म-पहचान (Self Recognition) के द्वारा मानसिकता का जो रूपांतरित सतोगुणी विकास दिखाया है, वह मनुष्य के जीवन-जगत् की समस्याओं का शाश्वत और सनातन समाधान है, जहाँ समस्याएँ निर्बीज और निर्मूल हो कर मिट जाती हैं। इसी दृष्टि से श्रद्धा मनु को ‘स्पर्श दीक्षा’ देती है और फिर मनु लोक को ‘दीप्त दीप दीक्षा’ प्रदान करते हैं। ‘कामायनी’ में निरूपित यह आंतरिक समाधान पूरे लोक को संकीर्ण मानसिकता और पक्षधरता से मुक्त करने वाला सिद्ध होता है।
‘कामायनी’ जिस भारतीय संस्कृति पर आधारित काव्य-कृति है, उस संस्कृति के स्वरूप को भी सम्यक् रूप में समझना अपेक्षित है। स्वयं प्रसाद ने अपने ‘काव्य और कला तथा अन्य निबंध’ नामक पुस्तक में इस पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि ‘यह संस्कृति विश्ववाद की विरोधिनी नहीं’ क्योंकि इसका उपयोग तो मानव-समाज में, आरंभिक प्राणित्व-धर्म में सीमित मनोभावों को सदा प्रशस्त और विकासोन्मुख बनाने के लिए होता है।’ (‘काव्य और कला’, पृष्ठ-28) साथ ही यह भी कि ‘संस्कृति का सामूहिक चेतनता से, मानसिक शील और शिष्टाचारों से, मनोभावों से मौलिक संबंध है।’ (पूर्ववत्) इस दृष्टि से ‘कामायनी’ इसमें विश्ववाद की संपोषिका सिद्ध होती है–‘विजयिनी मानवता हो जाए।’ मनु का शीलगत विकास प्रसाद की संस्कृति-परक मान्यता का दर्पण है। मनु का आरंभिक शील प्राथमिक प्राणित्व-धर्म के इर्द-गिर्द ही सक्रिय रहता है। पर ‘कामायनी’ के उत्तरार्ध में मनु का यही शल लोक-कल्याण की दृष्टि से प्रशस्त और विकसित होता है। उसके मनोभाव रूपांतरित होते हैं और मानसिकता लोक-कल्याण के लिए समर्पित होती है। प्रसाद ने अपने इसी आलेख में आगे लिखा है कि ‘हमारे ज्ञान-प्रतीक दुर्बल नहीं है।’ (पूर्ववत्, पृष्ठ-31) ‘कामायनी’ में इसी भारतीय ज्ञान-प्रतीक का साभिप्राय निरूपण देखने को मिलता है, जहाँ प्राचीन दर्शन और उसके पारिभाषिकों में यगु-सापेक्ष अर्थ-बोध की साभिप्रायित प्राण-प्रतिष्ठा हुई है। ‘कामायनी’ प्रसाद की काव्य-दृष्टि का सार्थक प्रतिफलन और उन्मीलित विस्तरण है। प्रसाद का मत है कि ‘भारतीय विचारधारा ज्ञानात्म्क होने के कारण मूर्त और अमूर्त का भेद हटाते हुए बाह्य और अभ्यंतर का एकीकरण करने का प्रयत्न करती है।’
‘कामायनी’ में बाह्य और अभ्यंतर का यह काम्य एकीकरण सार्थक हुआ है। यहाँ मूल में, अभिप्रेरक रूप में अभ्यंतर की स्थिति दिखाई गई है और बाह्य को उससे परिचालित-संचालित माना गया है। तभी यह एकीकरण लोकहित में उपस्थित हो पाता है। श्रद्धा ‘मानव’ को इड़ा को सौंपती है। ‘मानव’ में श्रद्धा का अभ्यंतर निवसित है। उसे श्रद्धा इड़ा से बाह्य ज्ञान प्राप्त करने को कहती है, ‘राष्ट्रनीति’ देखने को कहती है और शासक के रूप में भ्रांति फैलाने से रोकती है। श्रद्धा ‘मानव’ से कहती है–
‘वह तर्कमयी तू श्रद्धामय
तू मननशील कर कर्म अभय,
इसका तू सब संताप निचय
हर ले, हो मानव-भाग्य उदय,
सबकी समरसता का प्रचार,
मेरे सुत, सुन माँ की पुकार!’
(कामायनी’, दर्शन सर्ग) श्रद्धा का ‘अंत:करण (मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार) शुद्ध और सतोगुणी है। वह मनु के इस ‘अंत:करण’ को, उसके अभ्यंतर को बदलना चाहती है, उसे शुद्ध और सतोगुणी बनाना चाहती है। पर मनु श्रद्धा का आग्रह नहीं मानता और उसे अपने आचरण में अनुपालित नहीं करता है। तब श्रद्धा ठोकरें खाये हुए आहत मनु में ‘शक्तिपात’ करती है, उसे स्पर्श-दीक्षा देती है और मनु श्रद्धा के मार्ग-दर्शन में योग-साधना के द्वारा अपने ‘अंत:करण’ की शुद्ध और सतोगुणी उपलब्धि प्राप्त करता है। यहाँ श्रद्धा के प्रयत्न अभ्यंतर से जुड़े हैं। इड़ा भी मनु को परिवर्तित, परिष्कृत करना चाहती है, उसके रजोगुणी व्यक्तित्व की स्वच्छंदता को नियंत्रित करने का आग्रह करती है। उसे आत्मानुशासन में और नियम-व्यवस्था में रहने को कहती है। इड़ा मनु से कहती है–
‘लोक सुखी हो आश्रम ले यदि उस छाया में,
प्राण-सदृश तो रमो राष्ट्र की इस काया में!’
यही नहीं, वह मनु को स्वार्थ की ‘क्षितिज-पटी’ को उठा कर लोक-कल्याण हेतु उसे लोक के आंतर विश्व (ब्रह्मांड-विवर) में बढ़ने का भी आग्रह करती है। पर मनु इन सारे आग्रहों को ठुकरा देता है–
‘तुम कहती हो विश्व एक लय है, मैं उसमें
लीन हो चलूँ, किंतु धरा है क्या सुख इसमें!’
इड़ा का यह सारा आग्रह बाहर से होता है। इसका स्वरूप बाह्य है और मनु के प्रति श्रद्धा का उत्तरवर्ती आग्रह आंतरिक है। अतः श्रद्धा और इड़ा भाव और बुद्धि के साथ-साथ ‘आंतर’ और ‘बाह्य को भी प्रतीकित करते हैं। श्रद्धा ‘मानव’ के शील में इसी अभ्यंतर और ‘बाह्य’ का एकीकरण चाहती है, जिससे ‘मानव अपने अंत:करण की सतोगुणी मानसिकता से अभिप्रेरित होकर लोक-कल्याणार्थ अपेक्षित रजोगुणी (बाह्य कर्मपरक) व्यापार संपादित करे।
प्रसाद के लिए ‘काव्य आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति है, जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है। वह एक श्रेयमयी प्रेय रचनात्मक ज्ञान-धारा है। वह निस्संदेह प्राणमयी और सत्य के उभय लक्षण प्रेम और श्रेय दोनों से परिपूर्ण होती है। …आत्मा की मननशक्ति की वह असाधारण अवस्था, जो श्रेय सत्य को उसके भूल चारुत्व में सहसा ग्रहण कर लेती है, काव्य में संकल्पात्मक मूल अनुभूति कही जा सकती है।’ (पूर्ववत्, पृष्ठ 37-38) काव्य-विषयक कामायनीकार की इस मान्यता के आलोक में यदि ‘कामायनी’ का परीक्षण करें, तो यह मान्यता ‘कामायनी’ में पूरी तरह प्रतिफलित और निरूपित दीखती है। पूरी ‘कामायनी’ आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति है, जिसका संबंध किसी विकल्प से बैठाया नहीं जा सकता। दूसरे शब्दों में इसमें प्रतिपादित संकल्पात्मकता को किसी विकल्प से प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता। ‘कामायनी’ के कवि-आलोचकों का ध्यान प्रसाद की काव्य-विषयक मान्यताओं की ओर नहीं जा सकता है और न ही वे इन मान्यताओं के प्रतिफल को ‘कामायनी’ में निरूपित साभिप्रायित देख पाये हैं। इसलिए उनमें कई ‘कामायनी’ की संकल्पात्मक अनुभूति से परिणामित समाधान की जगह कोई दूसरा विकल्पात्मक समाधान माँगते दीखते हैं और कोई-कोई तो नितांत पूर्वग्रही रूप में बिना ‘कामायनी’ की संकल्पात्मक अनुभूति के लयात्मक तारतम्य को समझे बिना अपना विकल्पात्मक परामर्श तक दे जाता है। कहना न होगा कि यह सारा दुराग्रह असंगत और बेमानी है। प्रसाद की काव्य दृष्टि के अनुरूप ‘कामायनी’ की दूसरी विशेषता आत्मा की मनन शक्ति की उस असाधारण अवस्था में निहित है, जहाँ ‘प्रेय’ के साथ-साथ ‘श्रेय’ का निरूपण मूल चारुत्व के साथ उसकी सोद्देश्यता को निर्दिष्ट करता है। कहना न होगा कि इस काव्यकृति की महत्ता ‘प्रेय’ के साथ-साथ ‘श्रेय’ की स्थापना से व्यक्तिनिष्ठता की जगह लोकार्पितता की संकल्पात्मकता से कहीं अधिक मार्गदर्शी स्थायिता प्राप्त कर लेती है। इस ओर भी ‘कामायनी’ के आलोचकों का ध्यान नहीं जा पाया है। प्रसाद मानते हैं कि काव्य में ‘व्यक्ति द्वारा प्रकट हुई आत्मानुभूति सामूहिक या समष्टि-भाव से विस्तार करने का प्रयत्न करती है।’ (पूर्ववत्, पृष्ठ-42) ‘कामायनी’ इसका श्रेष्ठ निदर्शन है।
प्रसाद मानते हैं कि ‘श्रोता, पाठक और दर्शकों के हृदय में कविकृत मानसी प्रतिभा की अनुभूति होती है’…। पर प्रसाद की ‘कामायनी’ पर जिन कवि-आलोचकों ने सीधे आरोप-पर-आरोप किये हैं, उनके विषय में यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि उन्हें ‘कामायनी’ में ‘कविकृत मानसी प्रतिभा’ की कहीं कोई अनुभूति नहीं हो पायी है। यदि यह अनुभूति उन्हें हुई होती, इसका साधारणीकरण उन्हें हुआ होता, तो इस तरह वे आरोप नहीं कर पाते। प्रसाद काव्य-विषयक विमर्श करते हुए यह भी स्वीकार करते हैं कि ‘व्यंजना वस्तुतः अनुभूतिमयी प्रतिभा का स्वयं परिणाम है।’ (पूर्ववत्, पृष्ठ-43) यहाँ यह प्रतिभा कारयित्री भी है और भावयित्री भी। पाठकों में इस भावयित्री प्रतिभा के बल पर ही व्यंजना की पहचान-परख होती है। पर ‘कामायनी’ के कवि-आलोचकों में इस भावयित्री प्रतिभा का भी अभाव दीखता है, जिससे उन्हें ‘कामायनी’ में सुविन्यस्त व्यंजना की पहचान नहीं हो पाती है। इस प्रकार ‘कामायनी’ के मूल्यांकन का एक सुदृढ़ आधार प्रसाद का काव्य-विषयक विमर्श सिद्ध होता है, जिस ओर अब तक ‘कामायनी’ के आलाचकों का ध्यान नहीं जा सके है।
‘कामायनी’ में ‘व्यक्ति’ और ‘संस्था (Institution) के बीच भी तनाव की स्थिति है। यह तनाव पूरी ‘कामायनी’ में परिव्याप्त है। पूर्वार्ध में ‘व्यक्ति’ और ‘परिवार’ नामक निर्मित हो रही संस्था के बीच तनाव है, तो उत्तरार्ध के आरंभ में ‘व्यक्ति’ और निर्मित हो चुके ‘समाज’ के बीच तनाव है। इसका मूल कारण है व्यक्ति की घोर अहम्मन्य उच्चशृंखल ‘इच्छा’ (Desire)। यह वही ‘इच्छा’ है जिसे आज उत्तर-आधुनिकता के केंद्र में माना जाता है। पर मूलतः यह प्राक्तन (Primordal) मानव को परिचालित करने वाली उच्चशृंखल ‘इच्छा’ है, जिससे मनु का पूरा व्यक्तित्व परिचालित है। मनु श्रद्धा के साथ संबंध-बंध (Live in relationship) में रहता है। ‘विवाह’ नामक संस्था अभी बनी नहीं है। मनु और श्रद्धा जब मनु से मिलती है तब वह उसे ‘वेदनामय’ और ‘कलांत’ देखती है। वह उसे जीवन-संदेश देती है–
‘दुःख के डर से तुम अज्ञात
जटिलताओं का कर अनुमान,
काम से झिझक रहे हो आज,
भविष्य से बन कर अनजान
…काम मंगल से मंडित श्रेय
सर्ग, इच्छा का है परिणाम,
तिरस्कृत कर उसको तुम भूल
बनाते हो असफल भवधाम!’
इस प्रकार श्रद्धा मनु को जीवन के प्रति अभिप्रेरित करती है। यहाँ उसके द्वारा व्यवहृत ‘काम’ ‘LIBIDO’ के अर्थ में, ‘जिजीविषा की ऊर्जा’ के अर्थ में प्रयुक्त है, यौनकर्म या Sex के अर्थ में नहीं। यहीं श्रद्धा मनु की सहचरी बनती है, सहयोगिनी बनती है। वह अपना प्रस्ताव रखती है और निर्णय भी सुना देती है–
‘दब रहे हो अपने ही बोझ
खोजते भी न कहीं अवलंब
तुम्हारा सहचर बन कर क्या न
उऋण होऊँ न बिना विलंब
समर्पण लो सेवा का सार
सजह संमृति का यह पतवार,
आज से यह जीवन उत्सर्ग
इसी पदतल में विगत् विकार
दया, माया, ममता लो आज
मधुरिमा लो, अगाध विश्वास;
हमारा हृदय-रत्न निधि स्वच्छ
तुम्हारे लिए खुला है पास!’
यह श्रद्धा का मनु के प्रति समर्पण है। ‘श्रद्धा’ सर्ग के इस संदर्भ के बाद ‘वासना’ सर्ग में मनु श्रद्धा के प्रति अपना समर्पण निवेदित करता है–
‘आज ले लो चेतना का यह समर्पण दान
विश्वरानी, सुंदरी नारी, हृदय की मान।’
इसी ‘संबंध-बंध’ (Live in relationship) में मनु श्रद्धा से संभोग करता है–
‘और एक फिर व्याकुल चुंबन
रक्त खौलता जिसे,
शीतल प्राण धधक उठता है।
तृषा-तृप्ति के मिस से
दो काठों की संधि बीच
उस निभृत गुफा में अपने,
अग्नि-शिक्षा बुझ गई,
जागने पर जैसे सुख-सपने।’
और श्रद्धा गर्भवती होती है। ‘ईर्ष्या’ संर्ग में वह अपनी संतान के आगमन की पूरी तैयारी करती है। ‘परिवार’ जैसी संस्था निर्मित-विकसित होती दीखती है। पर श्रद्धा के हृदय में संचित हो रहे वात्सल्य पर मनु प्रश्न उठाता है–
‘यह संचित क्यों हो रहा स्नेह
किस पर इतनी हो सानुराग?’
उसे दोनों के बीच कोई तीसरा नहीं चाहिए, संतान भी नहीं। उसका अहम्मन्य स्वार्थ, इसे सहन नहीं कर सकता। सो वह श्रद्धा से कहता है–
‘यह जीवन का वरदान,
मुझे दे दो रानी अपना दुलार!
केवल मेरी ही चित्त का
तब चित्त वहन कर रहे भार!’
श्रद्धा अपनी नई गृहस्थी की योजना को उसे विस्तार से सुनाती-समझाती है। पर मनु का अहंकार इसे सहन नहीं कर पाता और वह कहता है–
‘यह जलन नहीं सह सकता मैं
चाहिए मुझे मेरा ममत्व,
इस पंचभूत की रचना में
मैं रमण करूँ बस एक तत्त्व!
यह द्वैत अरे यह द्विविधा तो है प्रेम बाँटने का प्रकार!
भिक्षुक मैं? ना, यह कभी नहीं
मैं लौटा लूँगा निज विचार!…भूले-से कभी निहारोगी
कर आकर्षणमय हास एक,
मायाविनि! मैं न उसे लूँगा। वरदान समझ कर जानु टेक।’
और मनु अपनी इस निर्मित-विकसित हो रही ‘परिवार’ नाम की संस्था को तोड़कर, छोड़कर चला जाता है–
‘लो चला आज मैं छोड़ यहीं
संचित संवेदन-भार-पुंज,
मुझको काँटे ही मिलें धन्य!
हो सफल तुम्हें ही कुसुम-कुंज!’
कह ‘ज्वलनशील अंतर लेकर मनु चले गये,
था शून्य प्रांत,
रुक जा, सुन ले ओ निर्मोही!’
इस प्रकार मनु ‘परिवार’ नामक संस्था को अपनी निजी उच्चशृंखल कामेच्छा और अहम्मन्यता के कारण तोड़ देता है और श्रद्धा को ऐसी दुरवस्था में उसे अकेली छोड़ कर चला जाता है। इसमें उसका वह पुरुष-आधिपत्य सिर उठाकर बोलता है, जिससे कालांतर में पितृसत्तात्मक परिवार और समाज निर्मित होते हैं। ‘कामायनी’ में वर्ग-संघर्ष नहीं है। अतः उसके आलोचकों को ‘वर्ग-संघर्ष’ की जगह ‘कामायनी’ की इस मूल समस्या को देखना और उस पर विचार करना चाहिए था, जो प्राक्तन मनुष्य और एक बहुत विकसित और समृद्ध सभ्यता के अवशेष मनु से आज तक पुरुष के मानस में यथावत् विद्यमान है। हमारी विकसित सभ्यता ने उस पर केवल आवरण डालने का प्रयास किया है। इस पर समस्या की दृष्टि से इसके अनुरूप युक्तियुक्त, सम्यक् समाधान भी चाहिए। क्या पुरुष की इस अहम्मन्य उच्चशृंखल ‘इच्छा’ के परिणामवश आज हमारे समकाल में भी परित्यकताएँ देखने को नहीं मिलती हैं? यदि मिलती हैं, तो उसका कोई समाधान हमारे समाज या प्रशासन-तंत्र ने निकाला है क्या? सिवा इस बाह्य विधान के कि पुरुष आज के संविधान के तहत ऐसी परित्यक्ताओं के भरण-पोषण के लिए एकमुश्त या माहवार निर्धारित की गई राशि उसे दे दे। पर क्या इससे समस्या मिटती है?
मनु सामाजिक संस्था को भी तोड़ता है। वह श्रद्धा को छोड़कर चला जाता है, तब ‘इंड़ा’ सर्ग में स्वयं उसका आत्मरूप और प्रतिरूप स्वीकारता है–
‘मैं तो अबाध गति मख्त सदृश हूँ
चाह रहा अपने मन की।’
‘पागल मैं, किस पर सदय रहा?
क्या मैंने ममता ली न तोड़!
किस पर उदारता से रीझा,
किससे न लगा दी कड़ी होड़?’
‘मनु तुम श्रद्धा को गये भूल!
…जो क्षण बीता सुख-साधन में उनको ही वास्तव लिया मान
वासना तृप्ति ही स्वर्ग बनी, यह उल्टी मति का व्यर्थ ज्ञान
तुम भूल गये पुरुषत्व-मोह में कुछ सत्ता है नारी की
समरसता है संबंध बनी अधिकार और अधिकारी की!’
‘इंड़ा’ सर्ग में ‘इंड़ा’ के आगमन के पूर्व कथित ये पंक्तियाँ मनु की इच्छा-केंद्रित अहम्मन्यता और वासनामयता को दर्शाती हैं। यही नहीं, मनु का प्रतिबिंब मनु को श्रद्धा और उसके बीच के संबंध की टूटन के कारण को भी बता-समझा देता है–
‘मनु उसने तो कर दिया दान!
वह हृदय प्रणय से पूर्ण सरल, जिसमें जीवन का भरा मान
जिसमें चेतनता ही केवल निज शांति-प्रभा से ज्योतिमान
पर तुमने तो पाया सदैव उसकी सुंदर जड़ देह-मात्रा!
सौंदर्य-जलधि से भर लाये केवल तुम अपना गरल-पात्र!
तुम अति अबोध, अपनी अपूर्णता को न स्वयं तुम समझ सके
परिणय जिसको पूरा करता उससे तुम अपने-आप रुके।
‘कुछ मेरा हो’ यह राग-भाव
संकुचित पूर्णता है अजान!’
पर क्या मनु इंड़ा से मिलने के बाद इससे कुछ सीख ले पाता है और ऐसी स्थिति पुनः उपस्थित न हो, इससे अपने-आपको बचा पाता है? स्पष्ट ही नहीं!
मनु को इड़ा मिलती है। दोनों का पारस्परिक परिचय होता है। इड़ा बताती है कि वह उजड़ा सारस्वत प्रदेश ही मेरा देश था। अब तक मैं इस आशा से ही यहाँ पड़ी हूँ कि यहाँ नगर बसेगा और मेरे दिन फिरेंगे। मनु इसका दायित्व स्वीकारता है। इड़ा उसकी कर्म-सहचरी बनती है, उसे मार्ग सुझाती है। नगर बसता है, समाज बनता है। सभ्यता निर्मित होती है। नियम बनते हैं। श्रम-विभाजन होता है। पर मनु स्वयं नियम मानने से इनकार कर देता है। यहाँ पुनः उसकी अहम्मन्यता और उच्चशृंखल ‘इच्छा’ सिर उठाती है। वह अपनी कामांधता में अकरणीय के लिए मानो दृढ़ता से तन जाता है। मनु सोचता है–
‘जो मेरी है सृष्टि, उसी से भीत रहूँ मैं!
क्या अधिकार नहीं कि कभी अविनीत रहूँ ‘मैं?
…इड़ा नियम-परतंत्र चाहती मुझे बनाना,
निर्बाधित अधिकार उसी ने एक न माना!’
‘मैं चिर बंधनहीन मृत्यु-सीमा उल्लंघन–
करता सतत चलूँगा, यह मेरा है दृढ़ प्रण!
महानाश की सृष्टि बीच जो क्षण हो अपना,
चेतना की तुष्ट वही, फिर सब है सपना!’
इड़ा उसे समझाती है–
‘किंतु नियामक नियम न माने,
तो फिर सब कुछ नष्ट हुआ-सा निश्चय जाने!
…आह! प्रजापति यह न हुआ है, कभी न होगा।
निर्बाधित अधिकार आज तक किसने भोगा?’
पर मनु इड़ा को उत्तर देता है–
‘इड़े, मुझे यह वस्तु चाहिए, जो मैं चाहूँ।
तुम पर हो अधिकार प्रजापति न तो वृथा हूँ।’
इड़ा उसे पुनः समझाती है–
‘मैंने जो मनु किया उसे मत यों कह भूलो
तुमको केंद्र बना कर अनहित किया न मैंने।
मैंने इस बिखरी विभूति पर तुमको स्वामी,
सहज बनाया, तुम अब जिसके अंतर्यामी
किंतु आज अपराध हमारा अलग खड़ा है
‘हाँ’ में ‘हाँ’ न मिलाऊँ तो अपराध बड़ा है।’
इसके पूर्व ‘स्वप्न’ सर्ग में भी मनु की कामांध हठधर्मिता दिखाई गई है। इड़ा को कामायनीकार ने ‘मनु की सतत सफलता की उदय बिजयिनी तारा’ कहा है। यहाँ ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि जैसे मनु श्रद्धा के साथ ‘संबंध-बंध’ (Live in Relationship) में बँधा था, उसने एक गृहस्थी बसा ली थी वैसा कुछ भी इड़ा के साथ नहीं था। इड़ा उसकी कर्म-सहचरी-मात्र थी। वह अपने को मनु की प्रजा मानती है। यह भी स्मरण दिलाती है कि प्रज्ञा आत्मजा होती है। पर मनु अपने अधिकारी होने के मद में, अपनी उच्चशृंखल कामांधता में इड़ा जैसी अधिकृत सहयोगिनी प्रज्ञा पर ‘अतिचार’ करता है, उसका ‘बलात्कार’ करता है, उसका ‘रेप’ कर डालता है। उसकी सोच गंदी हो उठती है–
‘मैं शासक, मैं चिर स्वतंत्रा, तुम भी मेरा–
हो अधिकार असीम, सफल हो जीवन मेरा।’
और इसी सोच के वशीभूत वह ‘बलात्कार’ कर बैठता है–
‘किंतु आज तुम बंदी हो मेरी बाँहों में
मेरी छाती में, फिर सब डूबा आहों में
सिंहद्वार अरराया जनता भीतर आई
मेरी रानी! उसने चीत्कार मचायी।
अपनी दुर्बलता में मनु तक हाँफ रहे थे।
स्खलन-विकंपित पद वे अब भी काँप रहे थे।’
कहना होगा कि यहाँ मनु अपनी हठधर्मी कामांध व्यक्तिवादिता में इड़ा को ‘घर्षिता’ बना, समाज के नियम-विधान को तोड़ते हुए वस्तुतः ‘समाज’ नामक संस्था को ही तोड़ डालते हैं। जैसे श्रद्धा मनु के साथ संबंध-बंध ही रहती हुई थी, उसकी इस रजोगुणी व्यक्तिवादी अहम्मन्यता और कामांधता को बाहर से बार-बार समझाने और लोक कल्याण की ओर उन्मुख करने का संदेशात्मक प्रबोध देती है, पर उसे बदल नहीं पाती है, उसे सतोगुणी नहीं बना पाती है और ‘परित्यक्ता’ होकर उसकी कुटिसत अहम्मन्यता का दुष्परिणाम स्वतः झेलती है, वैसे ही इड़ा भी उसकी कर्म सहयोगिनी-मात्र के नाते उसके व्यक्तिवाद रमोण्डणी अधिकार-मद और उसके घोर अहंकार को लोकोन्मुख नहीं करवा पाती है और उसके कामांध ‘बलात्कार’ का शिकार होने से अपने-आपको बचा तक नहीं पाती है। इस आलोक में ‘कामायनी’ की मूल समस्या व्यक्ति के अधिकार-मद, घोर अहंकार, कामांध वासना-लोलुप कुसंस्कार और नारी को पीड़ित करने वाले पुरुषत्व वादी दृष्टिकोण की समस्या है। यह समस्या जितनी किसी प्राक्तन मनुष्य, की है उतनी ही आज के सभ्य मनुष्य की भी। इस दृष्टि से यह एक सनातन समस्या है, जिससे आज भी ‘परिवार’ और ‘समाज’ दग्ध हो रहा है। यह समस्या यद्यपि ऊपर से बाहरी प्रतीत होती है, पर मूलतः यह मनुष्य के ‘अंत:करण’ (मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार) से जुड़ी मानसिक समस्या है। इसीलिए कामायनीकार ने इसका आंतर समाधान सुझाया है, जिससे मनुष्य ‘रजोगुण’ से अभिप्रेरित होकर ही अपेक्षित ‘रजोगुणी’ (सांसारिक) कर्म-संपादन कर सके। हमारे अद्यतन अति सभ्य समाज में भी परित्यक्ता नारियाँ हैं। आज भी अधिकारी पुरुष कार्यालयों में तथा अन्यत्र भी अधिकृत नारी से ‘बलात्कार’ तक करते हैं। यही नहीं, ‘नारी’ को भोग्या और शरीर-मात्र मानने वाला हमारा पुरुष-वर्ग यत्र, तत्र, सर्वत्र कुमारिकाओं, विवाहिताओं और वृद्धाओं तक से ‘सामूहिक बलात्कार’ तक करता है, उनसे ‘गैंगरेप’ करता है। आज इन सबको रोकने के सभी बाहरी उपाय-कानून, अदालती दंड-विधान, आरक्षी-व्यवस्था-तंम विषम सिद्ध हो रहे हैं। क्या ‘कामायनी’ के समाधान से हमें इस पुरुष-वर्ग की मानसिकता को परिवर्तित करने, उसे ‘सतोगुणी’ बनाने के लिए अपेक्षित सीख लेने की आवश्यकता नहीं है और यदि है, तो किस तरह? क्या प्राथमिक शिक्षा में बुनियादी मूल्य-वादी नैतिक शिक्षा को सिद्धांत और व्यवहार दोनों रूपों में लागू कर या योग-साधना द्वारा ‘सहस्रार’ को सिद्ध कर यह मानसिकता बदली जा सकती है? वस्तुतः यही कामायनीकार की सच्ची भविष्य दृष्टि है। ‘कामायनी’ में जो संघर्ष दिखलाया गया है, वह इसी ‘बलात्कार’ की प्रतिक्रिया में उभरता है और उस शीर्ष पर जा पहुँचता है, जिसके लिए कामायनीकार ने लिखा है–‘रक्त नदी की बाढ़ फैलती थी उस भू पर!’ इसे किसी भी प्रकार से आज के आर्थिक वर्ग-संघर्ष से नहीं जोड़ा जाना चाहिए, जिससे साम्यवाद के तथाकथित बाहरी समाधान की अपेक्षा हो। प्रसाद की ‘कामायनी’ का न तो यह प्रतिपाद्य है और न ही ‘कामायनी’ इस दृष्टि से अधीतव्य है।
‘कामायनी’ एक और समस्या से हमें रु-ब-रु कराती है। इड़ा ने अपनी सामाजिक संरचना और व्यवस्था के लिए मनु से नियमों का विधान करवाया था। नियमों का यह विधान सभी पर लागू होता है। पर नियमों का निर्माता मनु स्वयं इसे अनुपालित करने, इसे मानने से इनकार कर देता है–
‘मैं नियमों के लिए बुद्धि-बल से प्रयत्न कर,
इनको कर एकत्र चलाता नियम बनाकर
किंतु स्वयं भी क्या वह सब-कुछ मान चलूँ मैं,
तनिक न मैं स्वच्छंद, स्वर्ण-सा सदा गलूँ मैं?
जो मेरी है सृष्टि उसी से भीत रहूँ मैं?
क्या अधिकार नहीं कि कभी अविनीत रहूँ मैं?
…इड़ा नियम-परतंत्र चाहती मुझे बनाना
निर्बाधित अधिकार उसी ने एक न माना!
…मैं चिर बंधनहीन मृत्यु-सीमा उल्लंघन–,
करता सतत चलूँगा, यह मेरा है दृढ़ प्रण।’
क्या आज हमारे समकाल में आम आदमी के साथ-साथ नियम-निर्माता तक नियमों को तोड़ते हुए उनकी धज्जियाँ उड़ाते हुए आपराधिक कर्मों में संलग्न नहीं दीखते? इन्हें पुलिस पकड़ती है। न्यायालय इन्हें दंड-संहिता के तहत सजा सुनाता है। पर न तो नियमोच्छेदन, नियमोल्लंघन रुकता है और न आपराधिक कर्म ही रुकते हैं। क्या ‘कामायनी’ का ‘मानव’ श्रद्धा और इड़ा के संस्कारों से समन्वित होकर इस दिशा में हमारा कोई मार्ग-दर्शन नहीं करता है? ‘कामायनी’ की कथावस्तु में कहीं भी ‘वर्ग-संघर्ष’ नहीं है। अतः यह उसका प्रतिपाद्य भी नहीं है। आश्चर्य तो तब होता है जब ‘कामायनी’ के आलोचक इसमें ‘वर्ग-संघर्ष’ देख लेते हैं और उसके समाधान हेतु साम्यवादी समाधान की वकालत भी करने लगते हैं। वस्तुतः ‘कामायनी’ के ‘सघर्ष सर्ग में प्रज्ञा न तो वर्गचेतना और वर्गगत विषम खाई को ध्यान में रखकर मनु से संघर्ष करने हेतु आ उपस्थित होती है और न आरंभ में उसमें मनु के प्रति किसी प्रकार का विद्रोह-भाव ही होता है। वह तो प्रकृति के उपद्रव से घबड़ा कर, भीत होकर मनु के पास अपने रक्षार्थ उपस्थित होती है, उनसे शरण माँगने आती है।
‘स्वप्न’ सर्ग में मनु जैसे ही इड़ा का आलिंगन करता है और इड़ा भय-क्रंदन करती है, वैसे ही पृथ्वी काँपती है, आकाश में रुद्र-हुंकार होता है, आत्मजा प्रज्ञा पर मनु का यह पाप उसके लिए शाप बन जाता है। देव-क्रोध से प्रकृति त्रस्त होती है। प्रज्ञा आश्रय पाने के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए व्याकुल हो उठती है। पर मनु का शासन इससे प्रज्ञा की रक्षा नहीं कर पाता है। प्रसाद ने लिखा है–
‘आश्रय पाने को सब व्याकुल, स्वयं कलुष में मनु संदिग्ध,
फिर कुछ होगा यही समझ कर वसुधा का थर-थर कँपित!
काँप रहे थे प्रलयमयी क्रीड़ा में सब आशंकित जंतु,
अपनी-अपनी पड़ी सभी को, छिन्न स्नेह का कोम तंतु,
आज कहाँ वह शासन था, जो रक्षा का था भर लिये,
इड़ा क्रोध-लज्जा से भर कर बाहर निकल चली थी किंतु!’
प्रजा मनु के पास इसी उद्देश्य से आती है, पर यहाँ वह इड़ा के साथ मनु का जो अतिचार देखती है, उसे वह सहन नहीं कर पाती है–
‘नियमन एक झुकाव दबा-सा, टूटे या ऊपर उठ जाय!
प्रजा आज कुछ और सोचती, अब तक जो अविरुद्ध रही!’
अब तक मनु के अविरुद्ध रहने वाली प्रजा आज पहली बार अन्यथा-भाव से भर उठती है। मनु अपना द्वार अंदर से बंद कर लेते हैं और उसे देखकर प्रकृति-प्रकोप से आश्रय पाने की दृष्टि से मनु के पास पहुँची प्रजा त्रस्त-स्रस्त धैर्यहीन हो उठती है–
‘द्वार बाद लख प्रजा त्रस्त सी, कैसे मन फिर धैर्य धरे।’
इसी संदर्भ में प्रसाद ने पहली बार ‘वर्गों की खाई’ शब्दों का प्रयोग किया है। मनु की निस्सीम अभिलाषा, उड़ान भरने की इच्छा, नीचे नहीं मुड़ने (जुड़ने) की असीम आशाएँ, अधिकारी और अधिकृत का विभाजन–इन सबने ही वर्ग की खाई पैदा की, जहाँ जुड़ने की, पारस्परिक सामंजस्य की कोई उम्मीद शेष नहीं रही–
‘वह विज्ञानमयी अभिलाषा, पंख लगाकर उड़ने की,
जीवन की असीम आशाएँ, कभी न नीचे मुड़ने की,
अधिकारों की सृष्टि और उनकी वह मोहमयी माया,
वर्गों की खाई बन फैली, कभी नहीं जो जुड़ने की!’
यहाँ ‘वर्गगत खाई’ शासक और शासित के बीच की दूरी को निर्दिष्ट करती है। प्रजा तो यहाँ शरण माँगती, आश्रय पाने की आशा से आती है, जिससे प्रकृति-प्रकोप से मनु उसकी रक्षा कर सके–
‘भौतिक विप्लव देख विकल वे थे घबराये
राजशरण में त्रण प्राप्त करने को आये!’
‘किंतु मिला अपमान और व्यवहार बुरा था,
मनस्ताप से सबके भीतर रोष भरा था
क्षुब्ध निखरते वदन इड़ा का पीला-पीला,
उधर प्रकृति की रुकी नहीं थी तांडव-लीला।’
पर यहाँ आते ही प्रज्ञा इड़ा पर मनु के द्वारा किये गये दुराचार का प्रत्यक्ष कर क्रुद्ध हो उठती है। पहले मनु को उन्हें अपने प्रतिकूल समझ कर उन पर शस्त्र प्रहार करता है। फिर आत्मरक्षा में प्रजा भी उनसे भिड़ जाती है। अतः इस संघर्ष को अर्थ-केंद्रित वर्ग-संघर्ष समझना इस संघर्ष की भ्रांत व्याख्या है, अपितु इसकी दुर्व्याख्या है। ऐसे आलोचक ‘संघर्ष’ सर्ग के प्रथम चरण की परवर्ती दो पंक्तियों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं–
‘भौतिक विप्लव देख विकल्प वे थे घबरायें
राज-शरण में त्राण प्राप्त करने को आये।’
यही नहीं, इड़ा भी मनु से कहती है–
‘प्रजा क्षुब्ध हो शरण माँगती उधर खड़ी है,
प्रकृति सतत आतंक विकम्पित घड़ी-घड़ी है।’
ध्यातव्य यह भी है कि मनु के यहाँ शास्त्र-सम्मत रूप में कहीं भी ‘वर्ग-विभाजन’ नहीं है, हर कहीं ‘वर्ण-विभाजन’ का ही उल्लेख है। ‘कामायनी’ में भी मनु कहता है–
‘चार वर्ग बन गये बँटा श्रम उनका अपना,
शरण-यंत्र बन चले न जिनका देखा सपना।’
इस तरह यहाँ कर्म-श्रम-आधारित वर्ण-विभाजन का उल्लेख है। मनु आगे चल कर पुनः कहते हैं–‘मैंने ही श्रम-भाग किये, फिर वर्ग बनाया।’ यहाँ भी विभाजन श्रम-आधारित ही है। मनु ने जिसे ‘वर्ग’ कहा है, वह मूलतः वर्ण ही है। प्रजा मनु से कहती है कि तुमने हमें योग-क्षेम से अधिक प्रकृति को लूटना, उसका शोषण करना सिखलाया। हममें इसका लोभ भर दिया, हमें लोभी बना दिया। तुमने यंत्र आविष्कृत किये, उन्हें परिचालित किया और हम सबकी प्रकृति मानवी शक्ति छीन ली। तुमने पर्यावरण-विरोधी सभ्यता को जन्म दिया, कोलाहल फैलाया और शांति का शोषण किया और हमारी प्रकृत जीवनी-शक्ति जर्जर कर डाली प्रज्ञा यहीं नहीं रुकती, वह आगे कहती है–
‘और इड़ा पर यह क्या अत्याचार किया है?
इसलिए तू हम सबके बल यहाँ जिया है?
आज वंदिनी मेरी रानी इड़ा यहाँ है?
ओ यायावर/अब तेरा निस्तार कहाँ है?’
इस प्रकार ‘संघर्ष’ सर्ग के संघर्ष का मूल कारण यहाँ स्पष्ट हो जाता है और यह भी पता चल जाता है कि यह संघर्ष ‘अर्थ-केंद्रित साम्यवादी वर्ग-संघर्ष’ नहीं है। इड़ा-केंद्रित इस संघर्ष का आरंभ भी पहले प्रजा नहीं करती, बल्कि मनु ही करता है–
‘यों कह मनु ने अपना भीषण अस्त्र सँभाला
देव ‘आग’ ने उगली त्योंही अपनी ज्वाला।
‘रक्तोन्मद मनु का न हाथ अब भी रुकता था,
प्रजा-पक्ष का भी न किंतु साहस झुकता था।’
इस संघर्ष में दैवी शक्ति भी ज्वाला उगलती है, प्रकृति भी निरंतर अपना प्रकोप दिखाती चलती है। स्मरणीय है कि इस चल रहे संघर्ष के बीच में इड़ा संघर्ष रोकने का आग्रह करती है–‘इड़ा अभी कहती जाती थी,
‘बस रोको रण–
भीषण जन-संहार आप ही तो होता है,
ओ पागल प्राणी तू क्यों जीवन खोता है
क्यों इतना आतंक ठहर जा ओ गर्वीले
जीने दे सबको, फिर तू भी सुख से जी ले।’
पर इड़ा की इस पुकार को न प्रज्ञा सुन पाती है और न मनु इस पर ध्यान दे पाता है।
‘कामायनी’ के प्रतिपाद्य के ऊपर निर्दिष्ट संदर्भों से यह स्पष्ट हो जाता है कि मनु की मानसिकता को मानव-कल्याण और लोक-हित की दिशा में रूपांतरित करने का बाह्य प्रयत्न, श्रद्धा और इड़ा- दोनों ही नारियाँ अपने-अपने दृष्टिकोण और ढंग से करती हैं। पर मनु पर इनका ऐसा कोई भी प्रभाव नहीं पड़ पाता है, जिससे वह इसे आत्मसात् और अपनी मानसिकता को काम्य दिशा में रूपांतरित कर सके, क्योंकि उसका रजोगुणी चित्त इस जीवन-दर्शन को ही अस्वीकार कर देता है। फलतः मनु इसका दुष्परिणाम भी भोगता है। इसीलिए मनुष्य की सांसारिक समस्याओं के समाधान हेतु श्रद्धा द्वारा अनुभूत संकल्पना के सिद्ध आंतरिक अनुभवीकरण और आत्मसातीकरण के लिए ‘मानव-प्रत्यभिज्ञान’ का माध्यम अपेक्षित हो उठता है।
हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि प्रसाद जीवन जगत् के गंभीर पर्यवेक्षण और चिंतन से संपन्न सर्जक रहे हैं और ‘कामायनी’ उनकी एक गंभीर काव्य-सर्जना है। यहाँ उनकी कवि-दृष्टि एक ओर भारतीय ज्ञान-दृष्टि और जीवन-दृष्टि से संबल प्राप्त करती है, तो दूसरी ओर वह अपनी अंतर्गर्भी सम्यक् व्याख्या के आधार पर विश्व-दृष्टि बनने की क्षमता भी रखती है। यहीं ‘कामायनी’ ‘मानवाधिकार’ की आत्मचेतना जगाने वाली ‘मानव-प्रत्यभिज्ञा’ का काव्य बन जाती है। मानव-प्रत्यभिज्ञा जीव और जीव में, मनुष्य और मनुष्य में ‘अद्वयता’, ‘अद्वैत’ और ‘अभेद’ को मानती है। मनुष्य को उपलब्ध होने वाला यह आंतरिक ‘आत्मज्ञान’ ही ‘मानव-प्रत्यभिज्ञा’ है, जिससे संघर्ष और हिंसा से मुक्त ‘समरसता’ और ‘समानता’ संभव है।
‘कामायनी’ में जिस ‘प्रत्यभिज्ञा’ या ‘सामरस्यवादी’ दर्शन की बात की गई है, वह सिद्धांततः और स्वरूपतः अद्वैतवादी है–‘The school of Pratyabhijna or self recognition represents the highest point of the development of the non-dual philosophical thought in Kashmir Shaiva tradition.’ (Dialogue, Editor B.B., Oct-Dec, 2014, page-196).
कश्मीरी शैव दर्शन का यह एक विशिष्ट प्रकार है। पर प्रसाद की विशेषता यह है कि उन्होंने ‘कामायनी’ में इस दर्शन की पुनस्सर्जना की है। इसे वहाँ पूर्व प्रतिपादित यथारूप में नहीं प्रस्तुत कर लोकहित में जागतिक धरातल पर प्रतिष्ठित किया गया है। ‘अद्वैत’ की व्याख्या दो रूपों में संभव है। इसकी पहली व्याख्या ऊर्ध्वाधर संबंध (Vertical relation) पर टिकी हुई है। इसे अंशी-अंश संबंध भी कह सकते हैं। परंपरा से प्रायः इसे ही निरूपित और व्याख्यायित किया जाता रहा है। यहाँ ब्रह्म और जीव के बीच ‘अद्वैत’ की बात की जाती है। ब्रह्म उच्च स्थित है, तो जीव अवस्थित। ब्रह्म व्यापक और विराट् है, तो जीव सीमित और लघुतर। ब्रह्म अंशी है, तो जीव अंश। ब्रह्म अविनश्वर हैं, तो जीव नश्वर। पर इन दोनों सत्ताओं में अद्वैत और अभेद है। ये दोनों मूलतः एक ही हैं, दो नहीं हैं। ब्रह्म ही जीव में व्याप्त है। ‘अद्वैत’ का यह निरूपण और विवेचन परम्परित रूप में प्रतिष्ठित है। साथ ही आध्यात्मिक है। पर जागतिक धरातल पर ‘अद्वैत’ की एक दूसरी निरूपणात्मक व्याख्या भी है। वह है जीव और जीव के बीच ‘अभेद’ और ‘अद्वैत’ की अनुभूति और प्रतीति, क्योंकि लोक में द्वयता है–‘द्वयता में लगी निरंतर ही वर्णों की करती रहे वृष्टि।’ यही नहीं, ‘भेद-बुद्धि निर्मम ममता की/समझ, ही होगी।’ ‘प्रत्यभिज्ञा का अर्थ है आत्मज्ञान की उपलब्धि। यह ज्ञान हो जाना कि जो ‘अन्य’ है वही ‘मैं’ हूँ और जो ‘मैं’ हूँ वही ‘अन्य’ है,कहीं कोई द्वयता नहीं है, भेद-बुद्धि नहीं है, यही ‘प्रत्यभिज्ञा’ है। मुझ में और अन्यों में कोई भेद नहीं, कोई अंतर नहीं, कोई द्वैत नहीं, यही अद्वैतवादी ‘प्रत्यभिज्ञा’ है। ‘द्वयता का जो भाव सदा मन में भरता है’–उससे यह ‘प्रत्यभिज्ञा’ मुक्ति देती है। अतः यह ‘अद्वैत’ की स्थिति का ही आत्मबोध है। प्रसाद का वैशिष्ट्य यह है कि उन्होंने परम्परित अर्थ वाले मुक्तिकामी ‘प्रत्यभिज्ञा’ दर्शन के ‘अद्वैत’ को लोकहितकारी रूप में सांसारिक धरातल पर अनुप्रयुक्त किया है। इस तरह उसे नयी पहचान की सार्थकता और चरितार्थता प्रदान की है। उन्होंने संसार के कल्याण के लिए इसकी दिशा मोड़ दी है। कामायनीकार ने ‘कामायनी’ में इसी ‘समरसता’ की प्रतिष्ठा की है।
‘तुम भूल गये पुरुषत्व-मोह से कुछ सत्ता है नारी की
समरसता है संबंध बनी अधिकार और अधिकारी की।’
प्रसाद ने ‘समरसता’ का यह प्रयोग बिल्कुल लौकिक और यथार्थ धरातल पर किया है।
जो आलोचक ‘लोक’ या सांसारिक लोगों का मुद्दा उठाकर ‘कामायनी’ में प्रतिपादित जीवन-दर्शन पर यह आरोप करते हैं कि यह ‘पलायनवादी’ और ‘संन्यासमूलक’ जीवन-दर्शन है, वहाँ आधुनिक समाधान नहीं है, उन्हें ‘प्रत्यभिज्ञा’ के इस रुपान्तरित निरुपण को देखना और समझना चाहिए कि आखिर किस तरह का सांसारिक समस्याओं का संघर्षरहित, शांतिपूर्ण, समाधान देने में सक्षम है। इस सोद्देश्य कथ्य की अंतर्धारा ‘कामायनी’ में–‘कल्याणभूमि यह लोक’ में–अपनी साकल्यपूर्णता (Wholeness) में परिव्याप्त है, चाहे संदर्भ श्रद्धा का हो या इड़ा का। इस तरह ‘कामायनी’ के काव्य-संदेश को, उसे मूल प्रतिपाद्य को और उसकी संकल्पित सोद्देश्यता को नहीं समझ पाना आलोचकों के अपने-अपने काव्य-विवेक और जीवन-विवेक की सीमा और उसकी ऋणात्मकता बन जाता है।
जो बात आज ‘मानवाधिकार’ (Human right) से नहीं बन पा रही है, उसे कामायनीकार ने ‘कामायनी’ में ‘मानव-प्रत्यभिज्ञा’ से स्थापित किया है। ‘मानवाधिकार’ की संकल्पना बाहरी है, पर ‘मानव-प्रत्यभिज्ञा’ की संकल्पना आंतरिक है जो मनुष्य को तमोगुण-रजोगुण से सतोगुण की ओर उन्मुख करती है। ‘कामायनी’ में ‘मानवाधिकार बनाम ‘मानव-प्रत्यभिज्ञा’ का तनाव है। द्रष्टव्य है कि वहाँ ‘मानवाधिकार’ के भाव से भरकर ही श्रद्धा मनु को (‘कर्म’ सर्ग में) कहती है कि
‘अपने में सब-कुछ भर कैसे
व्यक्ति विकास करेगा
यह एकांत स्वार्थ भीषण है
अपना नारा करेगा।’
पर मनु पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बाद में चलकर मनु यद्यपि श्रद्धा से यह कहता है कि
‘वही करूँगा जो कहती हो
सत्य, अकेला सुख क्या’,
पर इसे वह अपने कर्म में कभी आचरित नहीं कर पाता है। वह तो यह श्रद्धा से महज इसलिए कहता है, क्योंकि उसे श्रद्धा को सोमपान कराना है–
‘श्रद्धा! पी लो इसे बुद्धि के
बंधन को जो खोले।’
यही नहीं, जीव-रक्षा की दृष्टि से भी वह मनु से आग्रह करती है–
‘वे प्राणी जो बचे हुए हैं
इस अचला धरती के
उनके कुछ अधिकार नहीं क्या
वे सब ही हैं फीके? मनु!
क्या यही तुम्हारी होगी उज्ज्वल नव मानवता
जिसमें सब-कुछ ले लेना हो
हंत! बची क्या शवता?’
‘ईर्ष्या’ सर्ग में वह पुनः मनु से तर्कपूर्ण आग्रह करती है–
‘पर जो निरीह जी कर भी कुछ
उपकारी होने में समर्थ,
वे क्यों न जिएँ, उपयोगी बन
इसका मैं समझ सकी न अर्थ।
…ये द्रोह न करने के स्थल हैं
जो पाले जा सकते सहे तु
पशु से यदि हम कुछ ऊँचे हैं
तो भव-जलनिधि में बने सेतु।’
इस तरह श्रद्धा मनु को सीमित मानवाधिकार के साथ-साथ व्यापक मानव-कर्त्तव्य का भी प्रबोध देती है, जिसका क्षेत्र नितांत सांसारिक है। पर मनु जब अपनी मानसिकता में इसे गृहीत और आधारित नहीं कर पाता है, तभी इसके लिए ‘मानव-प्रत्यभिज्ञा’ की निंदात्मक अपेक्षा सामने आती है।
‘मानवाधिकार’ में प्रचलित लोगों को एकता में बाँधने वाले रूप का आग्रह भी ‘संघर्ष’ सर्ग में दिखता है–
‘वे विस्मृत पहचान रहे से एक-एक को
होते सतत समीप मिलाते हैं अनेक को।’
साथ ही
‘कितने जब से भर कर
इनका चक्र चलाया
अलग-अलग थे
एक हुई पर इनकी छाया।’
फिर यह कामना करना कि ‘लोक सुखी हो आश्रम ले यदि इस छाया में।’ पर यह सभी व्यर्थ सिद्ध होते हैं। मनु पर इसका कहीं कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसीलिए मनु की मानसिकता का आंतरिक परिवर्तन अनिवार्य निदान बन कर सामने आता है। प्रसाद ने दर्शन, रहस्य और आनंद सर्ग की योजना इसी दृष्टि से की है। इन सर्गों की सार्थकता इसी दृष्टि से है। इसके लिए प्रसाद को अद्वैतवादी ‘प्रत्यभिज्ञा’ दर्शन सर्वाधिक उपयुक्त लगा है। इससे मानव को आत्म-प्रत्यभिज्ञान प्राप्त करना, उसे उपलब्ध करना संभव है। इसके लिए योग-साधना अपेक्षित होती है। पर प्रसाद ने इस कृच्छ प्रक्रिया को सरलीकृत किया है और मनु में श्रद्धा के द्वारा ‘शक्तिपात’ करवाया है। यह गम्य है। केवल अपने परिणाम के द्वारा, श्रद्धा द्वारा मनु को विभिन्न लोकों की आंतरिक यात्रा कराने और दर्शन कराने के द्वारा स्पष्ट हो पाता है। यदि श्रद्धा के द्वारा यह शंतिपात हीं किया गया होता, तो यह आंतरिक यात्रा संभव नहीं हो पाती। पर प्रसाद ने इसकी सोद्देश्यता की दिशा में परिवर्तन कर समाधान को युगानुकूल कर किया है। ‘अद्वैत’ की यह सार्थकता और साभिप्रायता पूरी तरह आधुनिक है। इसकी सोद्देश्यता समष्टिपरक है। यहाँ व्यक्ति की मुक्ति-सकामता नहीं हैं, अपितु समरसता-भरी लोक की पारस्परिक अभिन्नता और अभेदता अभीष्ट है। यही ‘कामायनी’ का मूल प्रतिपाद्य है। विडंबना यह है कि ‘कामायनी’ में प्रतिपादित इस बीज-प्रोक्ति (Key Discourse) की ओर सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर और गजानन माधव मुक्तिबोध तक की दृष्टि नहीं जा पाई है। फलतः वे सब कामायनी को समझने में असमर्थ सिद्ध हुए हैं। यह सच है कि कोई भी महान रचना या काव्यकृति पाठकों-आलोचकों के लिए चुनौती बन जाती है। ‘कामायनी’ इस चुनौती का प्रत्यक्ष प्रमाण है। इस तरह ‘कामायनी’ मानवाधिकार की विफलता को दिखाने वाली ‘मानव-प्रत्यभिज्ञा’ का लौकिक महाकाव्य बन जाती है।
Image : Drops of Rain
Image Source : WikiArt
Artist : Clarence White
Image in Public Domain

