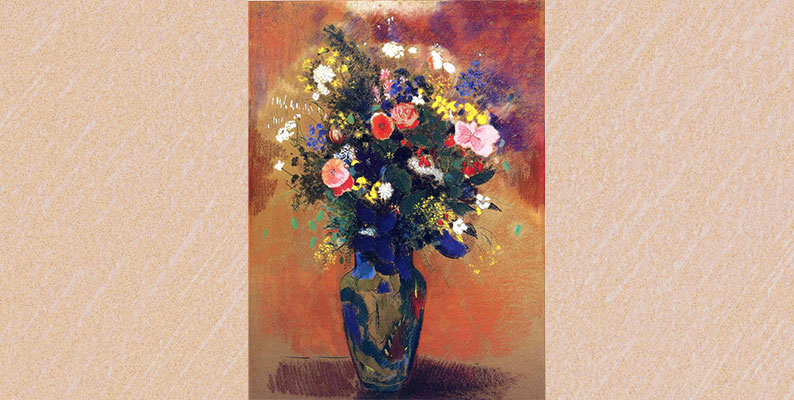महादेवी की कविता
- 1 April, 1951
शेयर करे close
शेयर करे close

शेयर करे close
- 1 April, 1951
महादेवी की कविता
‘नीहार’ की उदासी, खीझा और झुँझलाहट ‘दीपशिखा’ तक पहुँचते-पहुँचते दूर हो गई है और उसमें परिस्थिति का सर्वोच्च आस्वाद, अभाव का आत्मसंतोष प्रकाशित हो उठा है। ‘दीपशिखा’ के आगे किस मनोराज्य की भूमि कवयित्री देखना चाहती है, यह भविष्य के गर्भ में है।
छायावाद-युग ने महादेवी को जन्म दिया और महादेवी ने छायावाद को जीवन। प्रगतिवाद (साम्यवाद) के नारे से प्रभावित हो जब छायावाद के मान्य कवियों ने अपनी आँखें पोंछ कर भीतर से बाहर झाँकना प्रारंभ कर दिया और अनंत की ओर से दृष्टि फेर कर मार्क्स पर उसे केंद्रित कर दिया तब भी महादेवी की आँखें भींगती रहीं, हृदय सिहरन भरता रहा, ओठों की ओट में आहें सोती रहीं और मन ‘किसी निष्ठुर’ की आरती उतारता ही रहा। दूसरे शब्दों में वे अखंड भाव से अंतर्मुखी बनी रहीं।
छायावाद के उन्नायक पंत ने ‘रूपाभ’ की प्रथम संख्या में उसका विरोध करते हुए लिखा था “इस युग की कविता स्वप्नों में नहीं पल सकती। उसकी जड़ों को अपनी पाषाण सामग्री धारण करने के लिए कठोर धरती का आश्रय लेना पड़ रहा है।” भगवती चरण वर्मा ने प्रगतिवाद के युग में छायावाद की दीपशिखा सँजोने वाली कवयित्री की ‘विशाल भारत’ में निर्दय भर्त्सना की थी, उनके भावैक्य और पलायन-प्रवृत्ति को प्रतिगामिनी कहा था। फिर भी महादेवी छायावाद की वकालत करती ही रहीं–“मनुष्य की वासना को बिना स्पर्श किए हुए जीवन और प्रकृति में सौंदर्य को समस्त सजीव वैभव के साथ चित्रित करने वाली उस युग (छायावाद) की अनेक कृतियाँ किसी भी साहित्य को सम्मानित कर सकती हैं।…उसने जीवन के इतिवृत्तात्मक यथार्थ चित्र नहीं दिए क्योंकि वह स्थूल से उत्पन्न सूक्ष्म सौंदर्यसत्ता की प्रतिक्रिया थी। अप्रत्यक्ष स्थूल के प्रति उपेक्षित यथार्थ की नहीं जो आज की वस्तु है।”[i] कल्पना परान्मुखियों से भी उन्होंने कहा–“जीवन की समष्टि में सूक्ष्म से इतने भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि वह तो स्थूल से बाहर कहीं अस्तित्व ही नहीं रखता। अपने व्यक्त सत्य के साथ मनुष्य जो है और अपने अव्यक्त सत्य के साथ वह जो कुछ होने की भावना कर सकता है वही उसका स्थूल और सूक्ष्म है! और यदि इनका ठीक संतुलन हो सके तो हमें एक परिपूर्ण मानव ही मिलेगा।”[ii] जिस भीतर-बाहर के संतुलन की यह बात महादेवी ने सन् 1940 में कही थी, उसी को दस वर्ष बाद पंत ने प्रगतिवाद से मुख मोड़कर ‘उत्तरा’ में उद्घोषित किया है।[iii] पंत के बाहर से भीतर लौटने की भविष्यवाणी जो महादेवी ने की थी–“हमें निष्क्रिय बुद्धिवाद और स्पंदनहीन वस्तुवाद के लंबे पथ को पार कर कदाचित फिर चिर संवेदन रूप सष्क्रिय भावना में जीवन के परमाणु खोजने होंगे, ऐसी मेरी व्यक्तिगत धारणा है।”[iv] आज तो पंत ही नहीं, निराला, अज्ञेय, राहुल आदि अनेक प्रगतिवाद के क्षेत्र से विमुख हो चुके हैं।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत है–“छायावादी कहे जानेवाले कवियों में महादेवी जी ही रहस्यवाद के भीतर रही हैं…अज्ञात प्रियतम के लिए वेदना ही इनके हृदय का भाव-केंद्र है जिससे अनेक प्रकार की भावनाएँ छूट-छूट कर झलक मारती रहती हैं।”
प्रश्न यह है कि महादेवी की भावनाओं की ‘झलकें’ क्या रहस्यवाद की सीमा के अंदर परिगणित की जा सकती हैं? और क्या महादेवी का रहस्यवाद कबीर, जायसी, मीरा की परंपरा है? इन प्रश्नों का उत्तर देने के पूर्व संक्षेप में रहस्यवाद और छायावाद की सीमा समझ लेनी होगी। आ. शुक्ल जी इन दो शब्दों को इस प्रकार समझाते हैं–“छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए, एक तो रहस्यवाद के अर्थ में जहाँ उसका संबंध काव्य-वस्तु से होता है अर्थात् जहाँ कवि उस अनंत और अज्ञात प्रिय को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है…छायावाद शब्द का दूसरा प्रयोग काव्य-शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में है। छायावाद का सामान्यत: अर्थ हुआ, प्रस्तुत के स्थान पर उसकी व्यंजना करने वाली छाया के रूप में अप्रस्तुत का कथन। इस शैली के भीतर किसी वस्तु या विषय का वर्णन किया जा सकता है।” (हिंदी साहित्य का इतिहास) ‘काव्य में रहस्यवाद’ में वे पुन: छायावाद का अर्थ स्पष्ट करना चाहते हैं–“जो छायावाद प्रचलित है वह वेदांत के पुराने प्रतिबिंबवाद का रूप है। यह प्रतिबिंबवाद सूफियों के यहाँ से होता हुआ यूरोप में गया जहाँ कुछ दिनों पीछे प्रतीकवाद से संश्लिष्ट होकर धीरे-धीरे बंग साहित्य के एक कोने में आ निकला और नवीनता की धारणा उत्पन्न करने के लिए छायावाद कहा जाने लगा। यह काव्यगत रहस्यवाद के लिए गृहीत दार्शनिक सिद्धांत का द्योतक शब्द है।” (पृ. 142-43)
आचार्य छायावाद और रहस्यवाद को एक मानते हैं और शैली विशेष भी। इससे विवेचना के क्षेत्र में यदि हम उन्हीं का शब्द प्रयुक्त करें तो ‘गड़बड़झाला’ हो जाने की संभावना हो गई है। विषय सुलझने की अपेक्षा अधिक उलझ गया है। महादेवी ने ‘यामा’ की भूमिका में इन ‘वादों’ की चर्चा करते हुए कहा है कि–“प्रकृति के लघु तृण और महान वृक्ष, कोमल कलियाँ और कठोर शिलाएँ अस्थिर जल और स्थिर पर्वत, नीड़ अंधकार और उज्ज्वल विद्युत-रेखा मानव की लघु विशालता, कोमल कठोरता, चंचलता, निश्चलता और मोहज्ञान का प्रतिबिंब न होकर, एक ही विराट से उत्पन्न सहोदर हैं। जब प्रकृति की अनेकरूपता में, परिवर्तनशील विभिन्नता में ऐसा तारतम्य खोजने का प्रयास किया जिसका एक छोर किसी असीम चेतना और दूसरा उसके ससीम हृदय में समाया हुआ था, तब प्रकृति का एक-एक अंश अलौकिक व्यक्तित्व लेकर जाग उठा। परंतु इस संबंध में मानव हृदय की सारी प्यास न बुझ सकी क्योंकि मानवीय संबंधों में जब तक अनुरागजनित आत्मविसर्जन का भाव नहीं घुल जाता तब तक वे सरस नहीं बन पाते और जब तक यह मधुरता सीमातीत नहीं हो जाती तब तक हृदय का अभाव दूर नहीं होता। इसी से इस अनेकरूपता के कारण पर एक मधुर व्यक्तित्व का आरोपण कर उसके निकट आत्मनिवेदन कर देना, इस काव्य (छायावाद) का दूसरा सोपान बना जिसे रहस्यमय रूप के कारण ही रहस्यवाद का नाम दिया गया है।”
महादेवी ने भी छायावाद और रहस्यवाद को एक दूसरे का पर्याय मान लिया है। परंतु छायावाद युग की रचनाओं का विश्लेषण कर लेने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि ये दो शब्द भिन्न अर्थों के द्योतक हैं। छायावाद के काव्य में अंतर्मुखी प्रवृत्ति प्रधान है। उसके लिए परोक्ष सत्ता के प्रकाशन की अनिवार्यता नहीं है। उसमें व्यक्ति की कोई भी अभाव-जनित अंतर्व्यथा झलक मार सकती है, बाह्य प्रकृति के प्रति आसक्ति भी सरस हो सकती है। मानव या प्रकृति के अंतर्बाह्य सौंदर्य के प्रति रागात्मक संबंध स्थापित करने के आयास की लक्षणात्मक अभिव्यंजना छायावाद की सीमा है और हृदय की व्यक्त जगत् के प्रति जिज्ञासा और उसमें अंतर्हित सूक्ष्म सत्य का आतुरतामय अन्वेषण रहस्यवाद की निकटता है। व्यक्त जगत में साधक की हृदय-भूमि भी सम्मिलित है। तात्पर्य यह कि सभी अंतर्मुखी की रचनाएँ लाक्षणिक अभिव्यक्ति के साथ छायावादी कहला सकती हैं! पर सभी छायावादी रचनाएँ रहस्यवादी नहीं हो सकतीं। रहस्यवादी रचनाओं में अव्यक्त सत्य या सूक्ष्म के प्रति ललक अनिवार्य है और वह अव्यक्त सत्य निर्गुण ब्रह्म का पर्याय होना चाहिए। ब्रह्म के सगुण रूप की अभिव्यक्ति में रहस्य कहाँ है? यह बात सत्य है कि निगुण ब्रह्म सगुण सत्ता लेकर ही काव्य में उतरता है क्योंकि भावना शून्य के आलंबन पर ठहर नहीं सकती।
जब महादेवी की रचना में समीक्षक रहस्यवाद पाते हैं तब संभवत: वे उनकी रचनाओं के शाब्दिक अर्थ तक अपने को सीमित रखते हैं। महादेवी ने रहस्यवाद की साधनात्मक अनुभूति को स्पर्श किया है यह संदिग्ध है। यह हमारा ही संदेह नहीं है, उनको रहस्यवादी कहने वाले आचार्य शुक्ल जी को भी कहना पड़ा है “वेदना को लेकर जो अनुभूतियाँ उन्होंने रखी हैं वे कहाँ तक वास्तविक हैं और कहाँ तक अनुभूतियों की रमणीय कल्पना, यह नहीं कहा जा सकता।” दीपशिखा की भूमिका में स्वयं महादेवी ने स्वीकार किया है–“यह आत्मानुभूत ज्ञान आत्मा के संस्कार और व्यक्तिगत साधना पर इतना निर्भर है कि इसकी पूर्ण प्राप्ति और सफल अभिव्यक्ति सबके लिए सहज नहीं है।” ज्ञान से जो दार्शनिक सत्य उपलब्ध हो सकता है वह हृदय के माध्यम से ही अनुभव किया जाता है, तभी रहस्यवाद की सृष्टि होती है। इसमें संदेह नहीं, महादेवी में निर्गुण संतों की वाणी का स्वर ध्वनित होता है पर ध्वनि में उनकी जीवन-साधना की अनुभूति का कितना अंश है, यह स्पष्ट नहीं हो पाता। कबीर कहते हैं–
“सुनु सखि पिऊ महिं जीऊ बसे,
जिऊ महिं बसे कि पीऊ।”
यह अत्मा-परमात्मा का ऐक्य महादेवी के जीवन में साध्य हो सका है, यह हम नहीं जानते। निर्गुणी संत अपने में सृष्टि और सृष्टि में अपने को कल्पना से नहीं, हृदय की ज्योति जगाकर देखते थे।
संतों के हृदय में उस सूक्ष्म की सघन संवेदना हुई थी। हक्सले बाह्य मन और बुद्धि के परे एक और व्यक्ति का, जिसे वह थर्ड थिंग कहता है, इसी तीसरी वस्तु या शक्ति के द्वारा निर्गुण ब्रह्म का साक्षात्कार संभव मानता है! प्राचीन द्रष्टा ऋषि इस वृत्ति के अस्तित्व की बराबर घोषणा करते आए जिसे वे साक्षात् ज्ञान, अनुभव ज्ञान या आसन्न अनुभूति के नाम से पुकारते हैं। बुद्धि के क्षेत्र को नीचे छोड़ कर निर्गुणी संतों ने अनुभूति के इसी राज्य में प्रविष्ट होने का दावा किया है। यहीं उन्हें परम सत्ता का साक्षात्कार हुआ है। यह बात सत्य है कि अपनी अलौकिक अनुभूतियों को समझाने के लिए उन्हें स्थूल उपकरणों और लौकिक भाषा का आश्रय लेना पड़ा है।
संतों की वाणी में जो अनुभूत सत्य बार-बार प्रतिध्वनित हुआ है, वह सार रूप में इस प्रकार है–परमात्मा और आत्मा की पृथक् सत्ता नहीं है, परमात्मा आत्मा में ही समाया हुआ है। अतएव उसकी खोज बहिर्वृत्ति से नहीं, अंतर्वृत्ति से संभव है।
महादेवी के काव्य में हम परोक्ष सत्ता की साक्षात् अनुभूति में विश्वास करने में इसलिए झिझकते हैं कि उसमें मध्ययुगीन संतों के समान सघन एकस्वरता–सहज एकतानता–नहीं है। उसमें कभी अद्वैत के प्रति ललक झलकती है, कभी द्वैत के प्रति कामना उमड़ती है और कभी स्थूल के प्रति राग सजग हो उठता है।[v] उनमें प्रेमतत्व का प्राधान्य होने से उन्हें सूफिनी कहने का भी साहस किया जाता है। पर सूफियों की भी आध्यात्मिक श्रेणियाँ और परंपराएँ हैं। महादेवी के काव्य में उनकी खोज करना उनमें सहज प्रकाशित प्रेमतत्व को भी अग्राह्य बनाना है। उनके काव्य को सूफियों से प्रभावित कहना भी उनका उपहास करना है।
महादेवी को मीरा की परंपरा में बतलाना भी इसी प्रकार कलाकार महादेवी को हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में “युगों पीछे फेंक देना है।” मीरा की भक्ति साधनामूलक थी, महादेवी का काव्य-साधना कलामूलक है। उनका तथाकथित ‘सूक्ष्म प्रिय’ क्या मीरा के ‘जोगी’ का पर्याय हो सकता है?
उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि महादेवी की रचनाएँ निर्गुणी संतों की एक लक्ष्योन्मुख सघन अनुभूति और उनके साधन-मार्ग परंपरा की नहीं है। उनके काव्य में व्यक्त ‘सूक्ष्म’ को कल्पना की सुंदर सृष्टि मानते हुए भी हम उनकी काव्य-प्रेरणा की सजीव यथार्थता में अविश्वास नहीं करना चाहते। उसे हम जीवन की क्रूर विषम परिस्थितियों से विचलित और विकंपित मानते हैं। जगत के अशोभन स्थूल सत्य के साथ सामंजस्य न हो सकने के कारण उनका भावुक मन आघात खा-खा कर अंतर्मुखी हो गया है और वहीं अपनी अभिरुचि की स्वप्निल प्रतिभा के साथ क्रीड़ा करने लगा है। कभी उनके साथ मिलन-सुख अनुभव करता है, कभी स्त्रियों-चित मान, अभिसार, शृंगार आदि का अभिनय करता है। परंतु ज्यों ही उसमें यह मान जागृत होता है कि स्वप्निल प्रतिभा से स्थूल मिलन असंभव है, वह विरह की वास्तविक स्थिति में आकर विकल हो जाता है। कवयित्री के काव्य की प्रेरणा ‘दीपशिखा’ की इन दो पंक्तियों में मुखरित हो उठी है–
“मैं कण-कण में डाल रही अलि
आँसू के मिस प्यार किसी का,
मैं पलकों में पाल रही हूँ,
यह सपना सुकुमार किसी का है॥”
सारी कविताओं का प्रेरणा-सूत्र इनमें है। इसी बात को एक स्त्री आलोचिका श्रीमती शचीरानी गुर्टू ने बहुत स्पष्ट शब्दों में यों व्यक्त किया है–“यौवन के तूफानी क्षणों में जब उनका अल्हड़ हृदय किसी प्रणयी के स्वागत को मचल रहा था और जीवन गगन के रक्ताभ पटल पर स्नेह-ज्योत्स्ना छिटकी पड़ रही थी, तभी अकस्मात विफल प्रेम की धूप खिलखिला पड़ी और पुलकते प्राणों की धूमिलता में अस्पष्ट रेखाएँ-सी अंकित कर गई। आत्म-संयम का व्रत लेकर उन्होंने जिस लौकिक प्रेम को ठुकरा कर पीड़ा को गले लगाया, वह कालांतर में आंतरिक शीतलता से स्नान होकर बहुत कुछ निखर तो गई किंतु उनके हठीले मन का उससे कभी लगाव न छूटा और वे उसे निरंतर कलेजे से चिपकाए रखने की मानो हठ पकड़ बैठीं।”
महादेवी ने कभी बहुत पहले गाया था–“विसर्जन ही है कर्णाधार; वही पहुँचा देगा उस पार।” यह तो स्पष्ट है कि महादेवी के इस विसर्जन में उल्लास नहीं, वेदना है, पर अपनी अभावजनित वेदना को छिपाने का उन्होंने सतत प्रयत्न किया है। ‘रश्मि’ की भूमिका में उन्होंने लिखा है–“संसार साधारणत: जिसे दु:ख और अभाव के नाम से जानता है, वह मेरे पास नहीं। जीवन में मुझे बहुत दुलार, बहुत आदर, सब कुछ मिला है, उस पर पार्थिव दु:ख की छाया नहीं पड़ी! कदाचित् वह उसी की प्रतिक्रिया है कि वेदना मुझे इतनी मधुर लगने लगी।” पर अपने ही कथन का मानो प्रतिवाद करती हुई वह एक स्थान पर लिखती हैं–“समता के धरातल पर सुख-दुख का मुक्त आदान-प्रदान यदि मित्रता की परिभाषा मानी जाए तो मेरे पास मित्र का अभाव है।” सुख-दुख में समभागी होनेवाले मित्र का अभाव क्या जीवन का कम उत्पीड़न है? ‘आधुनिक कवि’ की भूमिका में हम फिर पढ़ते हैं–“हृदय में तो निराशा के लिए कोई स्पर्श ही नहीं पाती, केवल एक गंभीर करुणा की छाया देखती हूँ।” निराशा इसलिए नहीं है कि महादेवी ने अपने अभाव से समझौता कर लिया। आशा तभी तक रहती है जब तक परिस्थिति में सुधार की संभावना होती है। एक बार इस संभावना के नष्ट हो जाने पर मन निराशा की ओर नहीं बढ़ता, पर वह आशान्वित होकर हर्ष से परिपूरित भी नहीं हो पाता। वह अपने अभाव को बिसूरता रहता है, उस पर चिंतन-मनन करता रहता है। कभी-कभी यह भी कल्पना कर वह अपने को सुखी मानने का यत्न करता है कि मैं निराश नहीं हूँ, प्रसन्न हूँ। पर यह कल्पित उल्लास का झोंका क्षणिक ही रहता है। उसके हटते ही मन अपने दु:ख को नगण्य नहीं मानता। महादेवी की ‘यामा’ की भूमिका में यही मनोवृत्ति बोल रही है–“दुख मेरे निकट जीवन का ऐसा काव्य है जो सारे संसार को एक सूत्र में बाँध रखने की क्षमता रखता है। हमारा एक बूँद आँसू भी जीवन को अधिक मधुर उर्वर बनाए बिना नहीं रहता।” मनुष्य सुख को अकेला भोगना चाहता है, परंतु दु:ख को सब को बाँट कर। विश्व-जीवन में अपने जीवन को, विश्व-वेदना में अपनी वेदना को इस प्रकार मिला देना जिस प्रकार जल का एक बिंदु समुद्र में मिल जाता है, कवि का मोक्ष है।
महादेवी को दु:ख का वह रूप प्रिय है जो मनुष्य के संवेदनशील हृदय को सारे संसार के एक अविच्छिन बंधन में बाँध देता है और उसका वह रूप भी काल और सीमा के बंधन में पड़े हुए असीम चेतन का क्रंदन है। दूसरे शब्दों में व्यष्टि और समष्टि दोनों का दु:ख उन्हें प्रिय है। हम महादेवी को कलाकार कवयित्री मानते हैं। यदि उनकी कविता को किसी वाद से ही बाँधना हो तो उसे दु:खवाद से अभिहित कर सकते हैं। उन्होंने स्वयं अपने जीवन को दु:ख या पीड़ा से सिक्त कहा है–
“चिंता क्या है हे निर्मम
बुझ जाए दीपक मेरा
हो जाएगा तेरा ही
पीड़ा का राज्य अँधेरा॥”
गद्य की भाषा में भी वे कहती हैं–“बचपन में ही भगवान बुद्ध के प्रति एक भक्तिमय अनुराग होने के कारण उनके संसार को दु:खात्मक समझने वाले दर्शन से मेरा असमय ही परिचय हो गया। अवश्य ही इस दु:खवाद को मेरे लिए नया जन्म लेना पड़ा। फिर भी उसमें नये जन्म के संस्कार विद्यमान हैं।” इसका यह आशय हुआ कि महादेवी ने बुद्ध की संसार को देखने की दृष्टि ग्रहण की है। बुद्ध भगवान ने दु:ख को शाश्वत सत्य माना है। वे कहते हैं कि संसार में दु:ख की सत्ता ठोस और स्थूल है। परंतु कवयित्री बौद्धों के संघात या नैराश्यवाद में विश्वास नहीं करती। अर्थात् वे आत्मा की वास्तविक सत्ता से इंकार नहीं करतीं परंतु बौद्धों के ‘संतानवाद’ में बहुत अंश तक विश्वास करती हैं। संतानवाद में आत्मा और जगत को अनित्य माना जाता है। महादेवी आत्मा को नित्य मानती हैं, उसके अमरत्व में आस्था रखती हैं परंतु क्षण-क्षण परिवर्तित दिखाई देनेवाले जगत की क्षणभंगुरता को बौद्धमत के समान ही स्वीकार करती हैं। यह सत्य है कि आत्मा का अमरत्व तब तक कायम रहता है जब तक वह परमात्मा में लीन होकर मुक्ति लाभ नहीं कर लेती। वे कहती हैं–
“जब असीम से हो जाएगा
मेरी लघु सीमा का मेल
देखोगे तब देव! अमरता
खेलेगी मिटने का खेल”
‘निर्वाण’ हो जाने के बाद आत्मा-परमात्मा नामक दो तत्व कहाँ रह जाते हैं? संसार में पदार्थों का नहीं, उनके रूप का नाश होता–
“स्निग्ध अपना जीवन कर क्षार
दीप करता आलोक प्रसार
जलाकर मृत पिंडों में प्राण
बीज करता असंख्य निर्माण,
सृष्टि का है यह अमिट विधान
एक मिटने में सौ वरदान।
मृत्यु को उन्होंने जीवन का चरम विकास कहा है। उनका विश्वास है कि यदि जीवन शाश्वत हो जाए तो वह ह्रासोन्मुख हो जाता है। अतएव विकास के लिए मृत्यु को उन्होंने आवश्यक माना है। मृत्यु से जीवन का सर्वदा लोप नहीं हो जाता। उसकी एक स्थूल शृंखला-मात्र विच्छिन्न हो जाती है।
अपने दु:ख की प्रतिच्छाया समस्त सृष्टि में देखने की वृत्ति हिंदी काव्य में नई नहीं है। ऊपर के विवेचन से सिद्ध है कि महादेवी का काव्य व्यक्तिगत मानसिक संघर्ष, अभाव और बुद्ध के दु:खवाद से प्रभावित है। दु:ख को उन्होंने ‘मधुर भाव’ के रूप में स्वीकार किया है। उसमें उनकी प्रेयसी की भूमिका है जो परोक्ष प्रिय के लिए अहर्निश आतुर होती रहती है। प्रिय और प्रियतम की इस कल्पित आँख मिचौनी से उनका काव्य क्रीड़ामय हो उठा है। वे कहती हैं–
“प्रिय चिरंतन है सजन
क्षण-क्षण नवीन सुहागिनी मैं।”
जब उनकी पलकें लज्जानत होना सीख ही रही थीं तभी उनमें किसी अज्ञात की प्रेम-पीड़ा हँस उठी थी–
“इन ललचाई पलकों पर
पहरा जब था व्रीडा का।
साम्राज्य मुझे दे डाला
उस चितवन ने पीड़ा का।”
तब से आजतक उनकी पीड़ा का अंत नहीं हुआ, उनकी विरह-निशा का अंत नहीं हुआ। वे कहती हैं–
“अलि! विरह के पंथ में
मैं तो न इति अथ मानती री।”
इसीलिए उनका जीवन विरह का जलजात बन गया है। जिसकी ‘चितवन’ ने उन्हें ‘पीड़ा का राज्य’ दे जीवन को झकझोर डाला है, उससे उनकी मनुहार है–
“जो तुम्हारा हो सके
लीला कमल यह आज
खिल उठे निरुपम तुम्हारी
देख स्मिति का प्रात॥”
कभी-कभी उनका भ्रांत मन यह भी कल्पना कर लेता है कि वे जिसे खोज रही हैं, वह उनके हृदय में ही है–
“गूँजता उर में न जाने
दूर के संगीत-सा क्या!
आज खो निजको मुझे
खोया मिला विपरीत-सा क्या?
क्या नहा आई विरह-निशि
मिलन मधु दिन के उदय में?
कौन तुम मेरे हृदय में?”
पर उसी क्षण जैसे उन्हें अपनी वास्तविकता का भान होता है। वे पुन: अपने को अभावमय अनुभव करने लगती हैं तथा अपनी स्थिति से संतुष्ट होना चाहती हैं–
“एक करुणा अभाव में
चिरतृप्ति का संसार निर्मित।”
उन्हें अपनी कसक में माधुर्य अनुभव होने लगा है। एक ही गीत में अनुभूति की विपरीत झलकों से जान पड़ता है कि वे लिखना कुछ चाहती हैं पर बेसुधमना होने के कारण कुछ और ही लिख जाती हैं। उनके गीतों में इस प्रकार की भाव विषमता का यह अर्थ हो सकता है कि या तो वे एक कल्पना के पश्चात् दूसरी कल्पना की चिंतना में व्यस्त रहती हैं या उनका मन ही भूला-भूला-सा भटकता रहता है।
अपने कल्पित प्रिय की कभी वे प्रतीक्षा करती हैं (‘जो तुम आ जाते एक बार’) और कभी उसे अपनी दशा दिखलाकर करुणा से आर्द्र करना चाहती हैं–“यह सजल मुख देख लेते, यह करुण मुख देख लेते”। उसे सपनों में बाँधने की आकांक्षा भी रह-रहकर आकुल हो उठती है और एकांत मिलन की, अभिसार की साध भी सिहर उठती है। फिर भी उनका अभिमान आँसुओं की राह से बिलकुल गल नहीं गया। अपने प्रिय में अपना अस्तित्व मिटाना उन्हें सह्य नहीं है–
“सखि! मधुर निजत्व दे
कैसे मिलूँ अभिमानिनी मैं?”
‘रत्नाकर’ की गोपियों की भी यही वृत्ति है। उनका विश्वास है कि अगर ससीम असीम में मिल जाएगा तो असीम का उससे तो कुछ उत्कर्ष न होगा प्रत्युत ‘ससीम’ ही बर्बाद हो जाएगा–
“जैहे बन विगरि न वारिधिता वारिधि की
बूँदता बिलैहै बूँद विवस बिचारी की!”
अलौकिक प्रिय के साथ प्रेम की यथा संभव समस्त क्रीड़ाओं का प्रदर्शन उनकी रचनाओं में बिखरा हुआ है। उनका कथन है कि उन्होंने सृष्टि के भीतर ही अपने प्रिय को पहचान लिया है। तभी वे आश्वस्त होकर कहती हैं–
“जो न प्रिय पहचानती।
कल्पयुग व्यापी विरह को
एक सिहरन में सँभाले,
शून्यता भर तरल मोती
से मधुर सुध दीप बाले,
क्यों किसी के आगमन के
शकुन स्पंदन में मनाती?”
वे उनके उन्मन संदेश भी जानती हैं, इसीलिए नयनों में पावस और प्राणों में चातक बसाती हैं। परंतु कवयित्री अपनी विरह-साधना का अंत नहीं चाहती। प्रतीक्षा-रस में उसकी अटूट ममता है–
“इस अचल क्षितिज रेखा से
तुम रहो निकट जीवन के
पर तुम्हें पकड़ पाने के
सारे प्रयत्न हो फीके।
तुम हो प्रभात की चितवन
मैं विधुर निशा बन जाऊँ।
काटूँ वियोग-पल रीते
संयोग समय छिप जाऊँ।”
ब्राउनिंग के समान वे भी अतृप्ति को जीवन मानती हैं। इसलिए उनके काव्य में विरह और मिलन की समानांतर निकटता लक्षित होती है।
महादेवी के काव्य में प्रकृति से परिचय पाना शहराती ड्राइंग रूम के फर्श पर वनप्रांगण की हरी दूब को खोजने के समान अप्राकृत प्रयत्न है। वे मानव-मन की हैं। बाह्य सृष्टि को काव्य में चित्रित करना उनका काम नहीं है। वे तो सिंगारना प्रकृति से ही अपना शृंगार कराती हैं–
“रंजित कर दे ये शिथिल चरण
ले नव अशोक का अरुण राग
मेरे यौवन को आज मधुर
ला रजनीगंधा का पराग
यूथी की मीलित कलियों से
अलि! दे मेरी कबरी सँवार।”
उन्होंने फूलों के नाम सुन रखे हैं; पढ़े भी हैं पर कौन फूल कब कहाँ खिलता है, उसकी चिंता उन्हें नहीं रही। हरसिंगार, शेफाली दुपहरिया का फूल भिन्न-भिन्न नहीं, एक ही है। इसे जानने का भी उन्हें अवकाश कहाँ? प्रकृति उनके काव्य को अलंकृत करने का कार्य अधिक करती है और उनकी भावनाओं की पृष्टभूमि बनाती है, स्वयं काव्य नहीं! उनके काव्य में तारक, ओस, बिजली, बादल आदि की बड़ी महिमा है। वे बार-बार गीतों में भिन्न-भिन्न प्रतीकों और नामों में झलक उठते हैं। वास्तव में प्रकृति में उन्होंने अपनी ही आशा-निराशा, आकांक्षा और उत्कंठा के चित्र आरोपित किए हैं। वे कभी-कभी स्वयं विराट रूप धारण कर विराट की मिलन-उत्कंठा से प्रकृति के उपकरणों को अपने शृंगार का साधन बनाती हैं–
“शशि के दर्पण में देख-देख
मैंने सुलझाए तिमिर केश।”
प्रकृति में मन के न रमने के कारण वह महादेवी के काव्य में पूरी तरह से बिंबित नहीं हो पाई। फिर भी आश्चर्य है कि वे सृष्टि के कण-कण को पहचानने का दावा करती हैं। इसीलिए हमारा संदेह दृढ़ होता है कि महादेवी का काव्य कल्पना की सुंदर सृष्टि है। अनुभूति के साथ उनकी अभिव्यक्ति का बहुत कम तारतम्य है।
गीतकर्त्री की दृष्टि से महादेवी को प्रसाद और निराला के बीच की शृंखला कहा जाता है। प्रसाद के गीतों में भाव प्रवणता, निराला के गीतों में चिंतन और महादेवी के गीतों में दोनों का समावेश है। निराला के गीत स्वर-ताल की शास्त्रीय मर्यादा के साथ प्राय: चलते हैं। प्रसाद और महादेवी के गीतों में संगीत शास्त्र का कोई बंधन नहीं है। निराला में शब्दों के ह्रस्व दीर्घ के विकार कम पाए जाते हैं, प्रसाद में अधिक, पर महादेवी में प्रसाद से कम, परंतु निराला से अधिक मिलते हैं। निराला में भावों को अन्विति के साथ गीत पूर्ण होता है। प्रसाद में भी प्राय: भाव विच्छिन्न नहीं हो पाता। पर महादेवी के गीतों में भावों की विच्छिन्नता पाई जाती है। उनका एक गीत प्राय: एक ही भाव की पूर्ण परिणति नहीं होता। उसमें कई भाव झलक उठते हैं।
छायावादी युग की काव्यकला महादेवी में पूर्ण वैभव के साथ दिखाई देती है। शब्द की अभिधाक्ति का वहाँ ज़रा भी सम्मान नहीं है। लक्षणा, प्रतीक और व्यंजना से वह ओतप्रोत है। कवयित्री प्रतीकों के प्रयोग में बहुत स्वच्छंद है। एक प्रतीक एक ही अर्थ में सब जगह प्रयुक्त नहीं होता। कभी-कभी भिन्न-भिन्न स्थलों पर संदर्भ के अनुसार बहुत भिन्न अर्थ देता है, इसी से काव्य प्राय: दुर्बोध हो जाता है। प्रसाद और पंत के समान वचन, लिंग आदि के प्रयोगों में वह व्याकरण के नियमों से बँधना नहीं चाहतीं।
अभी तक रचनाकाल की दृष्टि से महादेवी के निम्न कविता-संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं–
(1) नीहार (2) रश्मि (3) नीरजा (4) सांध्य गीत (5) नीहार, रश्मि, नीरजा और सांध्यगीत का सम्मिलित रूप यामा (6) दीपशिखा। इन संग्रहों की प्रारंभिक रचनाओं में संभवत: आयु के अनुसार भाव-विगोपन की प्रवृत्ति रही है पर क्रमश: ‘दीपशिखा’ तक पहुँचते-पहुँचते इनका हृदय खुल-सा गया है और अभिव्यक्ति बहुत कुछ स्पष्ट हो गई है। ‘नीहार’ की उदासी, खीझ और झुँझलाहट ‘दीपशिखा’ तक पहुँचते-पहुँचते दूर हो गई है और उसमें परिस्थिति का सर्वोच्च आस्वाद, अभाव का आत्मसंतोष प्रकाशित हो उठा है। ‘दीपशिखा’ के आगे किस मनोराज्य की भूमि कवयित्री देखना चाहती है, यह भविष्य के गर्भ में है।
संदर्भ
[i] आधुनिक कवि–भूमिका
[ii] वही
[iii] “मैं बाहर के साथ भीतर की क्रांति का भी पक्षपाती हूँ”…(उत्तरा पृ. सं. 26)
[iv] आधुनिक कवि
[v] अद्वैत का स्वर 1 ‘बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ।’
2 ‘मधुर राग तू मैं स्वर संगम, चित्र तू मैं रेखा क्रम।’
द्वैत की भावना–
‘तुम सो जाओ मैं गाऊँ
मुझे साते युग बीते
तुम को यों लोरी गाते
अब आओ मैं पलकों में
स्वप्नों से सेज बिछाऊँ।’
स्थूल के प्रति राग–
‘कह दे माँ क्या देखूँ।
देखूँ खिलती कलियाँ या प्यासे सूखे अधरों को
या मुरझाई पलकों से झरते आँसू कण देखूँ।’
Image Source: Wikimedia Commons
Image in Public Domain