नई समीक्षा पर मार्क्स और फ्रायड का प्रभाव
- 1 April, 1951
शेयर करे close
शेयर करे close
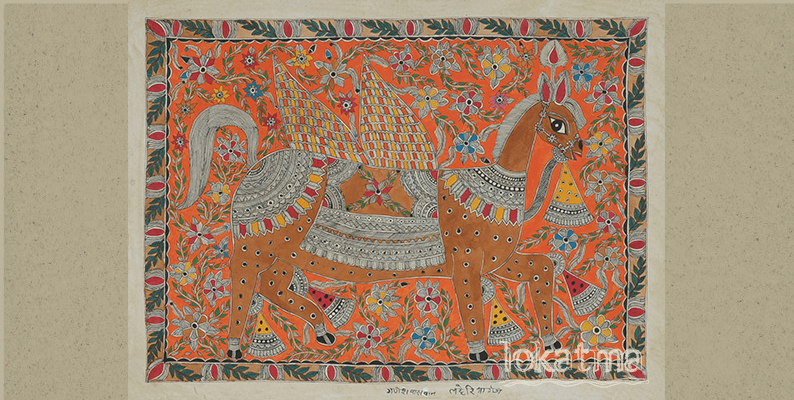
शेयर करे close
- 1 April, 1951
नई समीक्षा पर मार्क्स और फ्रायड का प्रभाव
“साहित्य और कला के इस व्यापक और क्रमागत स्वरूप को हम किसी नवीन मतवाद के आग्रह से सहसा छोड़ नहीं देंगे। परंतु इन दोनों मतों का उपयोग और उनकी सहायता हम अपनी काव्य-धारणाओं के निर्माण में अवश्य लेना चाहेंगे।”
मार्क्स का सिद्धांत साहित्य में जिस प्रकार प्रयुक्त हो रहा है, उसे साहित्यिक प्राय: प्रगतिवाद के नाम से पुकारते हैं। यह तो स्पष्ट है कि मार्क्स का यह सिद्धांत सामाजिक जीवन से संबंध रखता है, कला-विवेचन से नहीं। किंतु वर्ग-संघर्ष के आधार पर उसने जिस समाजतंत्र का निरूपण किया, वह भविष्य का इतना सुंदर स्वप्न था कि स्वभावत: पूर्वकाल की सारी सामाजिक और सांस्कृतिक योजनाएँ उसके सामने फीकी जान पड़ीं। जब तक संसार में यह वर्ग-रहित समाज स्थापित नहीं हो जाता और जब तक उसके साथ ही अनिवार्य रूप से आने वाली पुरुष और नारी की पूर्ण आर्थिक और वैयक्तिक स्वतंत्रता प्रतिष्ठित नहीं हो जाती, तब तक सच्चे सांस्कृतिक उत्थान का युग कभी आया था या आ सकता है, यह अपने हृदय से कोई भी प्रगतिवादी नहीं मानता। प्राचीन साहित्य और धर्म आदि को वे इसी दृष्टि से देखें तो इसमंस आश्चर्य ही क्या! उनकी निगाह में वर्गवादी युग की सारी सृष्टि ही मूलत: दूषित है। इस भयानक एकांगी दृष्टि से देखने पर अब तक साहित्य में कुछ भी सुंदर नहीं दीख पड़ता। जिनकी कुछ कलात्मक अभिरुचि है, वे यदि प्राचीन काव्य में कहीं कुछ सौंदर्य देखते भी हैं, तो हठात् उन्हें उस समाज की याद आ जाती है जो वर्गवादी समाज था। वे विवश होकर उसकी ओर से मुँह फेर लेते हैं, अथवा ऐसी नुक्ताचीनी करते हैं जिसे सच्ची काव्य-समीक्षा में कोई स्थान नहीं मिलना चाहिए। सच्चे अर्थ में ये ही लोग प्रगतिवादी हैं, और इनकी सारी सांस्कृतिक आशाएँ भविष्य में अटकी हैं। इसलिए ये एक विवादग्रस्त जीवन-सिद्धांत को काव्य-कसौटी बना लेने की अक्षम्य गलती करते हैं। काव्य का क्षेत्र भावों और मानव के चिर दिन की अनुभूतियों और कल्पनाओं का क्षेत्र है और बाह्य-जगत के आर्थिक या सैद्धांतिक विभेदों के रहते हुए भी मनुष्य मनुष्य है, उसके आदर्श और उसकी मानवीयता सभी सभ्य युगों में एक-सी ही ऊँची रह सकती है और साहित्य में वही आदर्श और वही मानव स्वभाव प्रतिफलित हुआ करता है, यह मानने को आज का प्रगतिवादी तैयार नहीं। मार्क्स से भी अधिक ये मार्क्स के प्रगतिवादी अनुयायी कला के प्रति ऐसी भ्रांत धारणाएँ बनाए हुए हैं। यदि ये जान-बूझकर प्रचारात्मक नहीं हैं, तो मार्क्सवादियों का यह काव्य-कला-विरोधी सिद्धांत और धारणा आश्चर्यजनक ही कही जाएगी। मैं यह नहीं कहता कि सभी प्रगतिवादियों की यही धारणा है, पर प्राय: इस तरह के विचार आए दिन देखने-सुनने में आते हैं।
मार्क्सवादी सामाजिक-आार्थिक सिद्धांत का जब काव्य अथवा साहित्य में प्रयोग किया जाता है, तब उसकी स्थिति बहुत कुछ असंगत और असाध्य-सी हो जाती है। अत्यंत स्थूल रूप में मार्क्स-मतवादी पक्ष यह है कि साहित्य और कलाएँ या तो वर्गहीन समाज की सृष्टि हैं, या वे वर्गवादी समाज की सृष्टि हैं। समाजवाद की प्रतिष्ठा के पूर्व का संपूर्ण साहित्य वर्गवादी या पूँजीवादी साहित्य है, अतएव वह मूलत: दूषित है। केवल वह साहित्य श्रेष्ठ और स्वागतयोग्य है जिस पर पूँजीवादी समाज-व्यवस्था की छाया नहीं पड़ी। मार्क्सवादियों की यह उपपत्ति सभी दृष्टियों से थोथी और सारहीन सिद्ध होती है। पहली आपत्ति तो यही है कि समाजवादी साहित्य और पूँजीवादी साहित्य के दो कठघरे बनाकर मानव समाज की संपूर्ण भावनात्मक और सांस्कृतिक संपत्ति को एक या दूसरे में बंद कर दिया गया है। इसमें साहित्यिक वस्तु के विवेचन का रंचमात्र भी प्रयास नहीं। पहला कटघरा दूषित और अपवित्र है, दूसरा कठघरा पूज्य और पवित्र। मानव के सामूहिक श्रौर सांस्कृतिक विकास के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। वाल्मीकि, व्यास, होमर, दांते, मिल्टन, शेक्सपियर, कालिदास, भवभूति, सूर, तुलसी आदि मानव संस्कृति के महान उन्नायकों की महती जीवन-कल्पना, मानव-स्वभाव-दर्शन और अनुभूतियों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। यह कहना व्यर्थ है कि ये पूँजीवादी युग के कवि थे। रहे हों ये किसी युग के कवि, पर देखना यह है कि मानव-चरित्र और मानव भावना का कितना व्यापक, समुन्नत और प्रभावशाली निर्देश इन महाकवियों ने किया है। जो सिद्धांत इन्हें पूँजीवादी युग का कवि कहकर टालता है, वह स्वत: अपनी असाहित्यिकता का इजहार करता है और अपनी अयोग्यता का प्रमाण देता है।
कुछ मार्क्सवादी साहित्य-विवेचक इतने असाहित्यिक न होने के कारण अपने सिद्धांत का प्रयोग एक दूसरे रूप में करते हैं। वे कवि, कलाकार अथवा साहित्यिक की व्यक्तिगत स्थिति और मनोभावना का आधार लेकर यह देखना चाहते हैं कि कौन-सा कवि आर्थिक दृष्टि से संपन्न था, उच्च वर्ग का था और कौन-सा कवि विपन्न और दरिद्र था। जो कवि दरिद्र और निम्न वर्ग का रहा हो वही प्रगतिशील और समुन्नत कवि माना जाएगा। यह कसौटी भी अनोखी है। इसमें यह पहले ही मान लिया जाता है कि गरीब लेखक ही क्रांतिकारी हो सकता है। यह निर्णय मानव-स्वभाव और चरित्र की कितनी भोंड़ी और नि:सार रूपरेखा प्रस्तुत करता है, यह समझने की बात है। कोई संपन्न और उच्च कुलशील कवि समाज के दीन दुखी अंग के प्रति अपनी कल्पना दौड़ा ही नहीं सकता, न उनके प्रति मानसिक सहानुभूति रख सकता है। दूसरी बात यह है कि क्रांतिकारी और प्रगतिशील होने के लिए दरिद्रता और समाज के नैतिक और सांस्कृतिक आदर्शों के प्रति अनास्था और विद्रोह अनिवार्य गुण हैं। चाहे उनकी रचनाएँ कितनी ही साधारण या सामान्य क्यों न हों!
इन दोनों प्रवादों की मूलभूत असाहित्यिकता इतनी स्पष्ट है कि इनका समर्थन करने के लिए मार्क्सवादियों में भी अधिक उत्साह नहीं दिखाई देता। इसके बदले वे एक तीसरे सिद्धांत की आड़ लेने लगे हैं। वर्गवाद के आधार पर सामाजिक विकास का विवरण देते हुए वे युग-विशेष की वर्गीय स्थिति का निरूपण करते हैं और उसी स्थिति-विशेष की भूमिका पर उस युग-विशेष के कवियों और साहित्यिकों की कृतियों का मूल्य निर्धारण करना चाहते हैं। उनकी दृष्टि में समय-विशेष की वर्गीय स्थिति ही वास्तविकता है, और उस वास्तविकता की नींव पर ही उस युग की कला-कृतियों और साहित्यिक-सृष्टियों का भवन बना करता है। वर्ग-संघर्ष के ऐतिहासिक विकास-क्रम में वे किसी कवि को ले लेते हैं और उसके काव्य का विवेचन करते हुए यह दिखाने का प्रयत्न करते हैं कि वर्ग-संघर्ष की तत्कालीन स्थिति की ही उपज उस कवि की कविता है। किसी युग-विशेष की एक नपी-तुली वर्गीय स्थिति का निरूपण करना स्वत: एक संदिग्ध कार्य है, फिर उस नपी-तुली स्थिति के अंतर्गत किसी कवि की भावना-कल्पना और उसकी काव्य-शक्ति की नाप-जोख करना कितना विवादास्पद कार्य होगा, यह आसानी से समझा जा सकता है। इस कठिनाई को समझकर और इसकी मूलवर्तिनी त्रुटियों की जानकारी रखने के कारण ये मार्क्सवादी साहित्य-समीक्षक इस संबंध में कई प्रकार के हथकंडे काम में लाते हैं। वे कहते तो यह हैं कि युग-विशेष की वर्ग संघर्ष संबंधी स्थिति की वास्तविक भूमि पर ही उस युग के कवि का कल्पना-भवन खड़ा होता है, पर अनुशीलन करते हुए वे पहले कवि की साहित्यिक विशेषताओं को ज्यों का त्यों मान लेते हैं और तब उन विशेषताओं का उस तथाकथित युग-स्थिति से कार्य-कारण संबंध स्थापित करने का प्रयास करते हैं। स्पष्ट ही यह एक उल्टा और तर्कहीन क्रम है। प्राय: इस प्रकार के समीक्षक किसी कवि विशेष के संबंध में स्थापित साहित्यिक मान्यताओं को–उसके साहित्यिक उत्कर्ष को–मानकर आगे बढ़ते हैं, जिसमें उनके सिद्धांत पर लोगों की आस्था बनी रहे। पर यह उपक्रम भी कितना छिछला और सारहीन है! यह तो कार्य संबंधी साहित्यिक मानदंड को प्रकांतर से स्वीकार करने का ‘मार्क्सवादी तरीका’ ही हो जाता है। समय-विशेष की स्थिति को ‘सत्य’ मानकर उस समय के काव्य को उस ‘सत्य’ के आसपास बुना हुआ कल्पना-जाल मानना, और फिर उन दोनों के अनिवार्य संबंध को सिद्ध करने के लिए उक्त काव्य की मनमानी व्याख्या करना–और साथ ही साहित्य-क्षेत्र में फैली हुई उस कवि के संबंध की साहित्यिक धारणाओं को अपनाते रहना, ये सब स्पष्टत: मार्क्सवादी साहित्य निर्देश की ऐसी खामियाँ हैं जिनको समझने के लिए थोड़ी-सी समझदारी भी पर्याप्त है।
यही कारण है कि मार्क्सवाद की यह साहित्यिक मान्यता अब तक प्रौढ़ और परिपुष्ट रूप में साहित्यिक समाज के सम्मुख नहीं रखी जा सकी। इस आधार को लेकर चलने वाले समीक्षकों में परस्पर इतनी अधिक मतभिन्नता रहती है–किसी भी कार्य की वर्ग-भावना या वर्गीय प्रतिक्रिया का आकलन करने में इतने भिन्न मत हुआ करते हैं कि केवल इस बात से ही सिद्धांत का कच्चापन स्पष्ट हो जाता है। दूसरी बात यह है कि यह सिद्धांत अपने पैरों पर खड़ा होने में असमर्थ है और बिना साहित्यिक विवेचकों के निर्णय का पीछा पकड़े यह चल ही नहीं पाता। कल्पना की भूमि में रमने वाले स्वतंत्र कवियों और साहित्यिकों को वर्गवाद की खूँटी में बाँधने का प्रयत्न करना बुद्धिमानी की बात नहीं है। इसलिए इस सिद्धांत के हिमायतियों को पग-पग पर दूसरों के मतों के साथ समझौता करना पड़ता है, जिससे कि उनकी स्थिति सदैव अस्पष्ट और अनिर्णीत बनी रहती है।
वर्गवाद के इस सामाजिक या वर्गीय ‘सत्य’ से नितांत भिन्न और उसकी प्रतिक्रिया में फ्रायड तथा अन्य मनोविश्लेषणवेत्ताओं का एक नया मत भी चल पड़ा है, उसके आधार पर साहित्यिक समीक्षा संबंधी नई चर्चा होने लगी है। मार्क्सवादी वर्ग सत्य या सामूहिक सत्य के स्थान पर ये मनोविश्लेषक व्यक्ति की निजी चेतना को–चेतना क्यों अंतश्चेतना को–उसके व्यक्तित्व का चरम सत्य मानते हैं और काव्य-साहित्य में उस अंतश्चेतना की अभिव्यक्ति को प्रमुख तत्त्व ठहराते हैं। व्यक्ति की चेतना या अंतश्चेतना के निर्माण में सामाजिक अथवा सामूहिक स्थितियाँ योग देती है, परंतु कवि की अंतश्चेतना ही अंतत: वह स्वतंत्र और मौलिक सत्ता है जो उसके काव्य-निर्माण के लिए उत्तरदायी है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जहाँ एक ओर मार्क्सवादी सामाजिक स्थिति (वह भी वर्गीय स्थिति) को सत्य मानकर कवि-कल्पना को उसकी छाया या प्रतिबिंब मानते हैं, वहाँ दूसरी ओर मनोविश्लेषणवादी सामाजिक गतिविधि या स्थिति से काव्य का संबंध न मानकर व्यक्ति की ऐकांतिक अंतश्चेतना को काव्य की प्रेरक और विधायक ठहराते हैं। स्पष्ट है कि दोनों मत अपने मूल दृष्टिकोण में एक दूसरे के विपरीत और विरोधी हैं।
अंतश्चेतनावादी मत यह है कि काव्य की सत्ता अत्यंत एकांतिक और मनोमयी है। व्यक्ति की चेतना पर पड़ने वाले सामाजिक प्रभाव और संस्कार काव्य के लिए उपादेय नहीं होते–सामाजिक परिस्थितियाँ, समस्याएँ और प्रश्न तो काव्य के लिए भी दूरवर्ती वस्तुएँ हैं। काव्य और कलाओं की उद्भावना कवि के अंतरंग व्यक्तित्व या अंतश्चेतना से होती है–ठीक वैसे ही जैसे स्वप्नों का सृजन व्यक्ति की जागरूक चेतना नहीं करती, उसकी अंतवर्ती सत्ता स्वप्नों का सृजन करती है। कव्य भी एक स्वप्न ही है। कल्पना-व्यापार भी स्वप्न-प्रक्रिया ही है। जिस प्रकार स्वप्न में अनेक प्रतीक और मूर्त स्वरूप अंतश्चेतना की सृष्टि बनकर विचरण करते हैं, उसी प्रकार काव्य की कल्पनाएँ और प्रतीक-विधान भी अंतश्चेतना की ही उपज होते हैं। यदि उनका निर्माण कवि की अंतवर्ती चेतना नहीं करती, तो वे कल्पनाएँ और वे अप्रस्तुत मूर्त-विधान सच्चे काव्य के उपादान न होकर कृत्रिम कविता की सृष्टि करेंगे। इस प्रकार मनोविश्लेषणवादी साहित्यिक मत अंतश्चेतना के द्वारा उद्भूत प्रतीकों और कल्पना-रूपों को ही वास्तविक काव्य का आधार मानता है।
हमारी चिर दिन से चली आती हुई साहित्यिक धारणा और साहित्यिक विधियों के अनुसार ये दोनों ही–मार्क्सवादी और अंतश्चेतनावादी–दृष्टिकोण और मत एकांगी हैं। अधिक से अधिक ये साहित्य की दो धाराओं–उद्देश्य-प्रधान सामाजिक धारा और व्यक्तिमूलक ऐकांतिक धारा–के प्रेरणा सूत्रों का आभास देती हैं। परंतु ये साहित्य की प्रशस्त उद्भावना और विकास भूमि का परिचय नहीं देतीं और साहित्यिक वैशिष्ट्य के आधारों का आकलन नहीं करतीं। मार्क्सवादी मत को मान लेने पर कवि-कल्पना और काव्य की प्रसार-सीमा वर्ग-संघर्ष की स्थिति-विशेष से ही संबद्ध और उसी से परिचालित माननी पड़ेगी और दूसरी ओर मनोविश्लेषक मत के अनुसार काव्य को केवल स्वप्न का स्वरूप मानना पड़ेगा। ये दोनों मत परस्पर विरोधी तो हैं ही, स्पष्टत: अतिवादी भी हैं। कुछ विशेष प्रकार के काव्य ही इन निर्देशों की सीमा में जा सकेंगे। अधिकांश काव्य और श्रेष्ठ काव्य इन प्रतिबंधों और निर्देशों से बाहर ही रह जाएगा। आज तक जिसे हम सांस्कृतिक और भावात्मक दृष्टियों से श्रेष्ठ काव्य मानते आए हैं, उसमें सामाजिक और वैयक्तिक दोनों ही दृष्टियों का समाहार होता रहा है और फिर भी वह सामाजिक और वैयक्तिक सीमाओं से परे मानव की संपूर्ण अंतर्बाह्य सत्ता से संबद्ध और उसकी उच्चतम भाव-भूमिका की पूर्ति और समाधान करने वाला सिद्ध हुआ है। साहित्य और कला के इस व्यापार और क्रमगत स्वरूप को हम किसी नवीन मतवाद के आग्रह से सहसा छोड़ नहीं देंगे। परंतु इन दोनों मतों का उपयोग और उनकी सहायता हम अपनी काव्य-धारणाओं के निर्माण में अवश्य लेना चाहेंगे। हमें यह भी समझ लेना चाहिए कि ये दोनों ही काव्यवाद साहित्य के प्रेरणा-सूत्रों और उनके स्वरूप को ही इंगित करते हैं, वे काव्य और कलाओं के वैशिष्ट्य और उनकी तुलनात्मक विशेषताओं का निरूपण नहीं करते। उसके लिए तो हमें अपने साहित्यिक मानदंडों और परंपराओं का ही आश्रित रहना पड़ेगा। नए मतों और सिद्धांतों की चकाचौंध में पड़कर हम साहित्य की परंपरा में गृहीत विवेचन-पद्धति और साहित्य की मूल्यांकन-संबंधी साहित्यिक विधियों को छोड़ दें, यह उचित नहीं। नए मत और सिद्धांत साहित्य-समीक्षा को किस सीमा तक और किस विशेष दिशा में नया प्रकाश प्रदान करते हैं, यह बिना समझे, इन नए वादों को साहित्य-समीक्षा का एकमात्र आधार और उपादान मान लेना ऐसा भ्रामक निर्णय है जिसे किसी भी सभ्यताभिमानी देश की साहित्यिक परंपरा स्वीकार नहीं कर सकती।
Image Courtesy: LOKATMA Folk Art Boutique
©Lokatma

