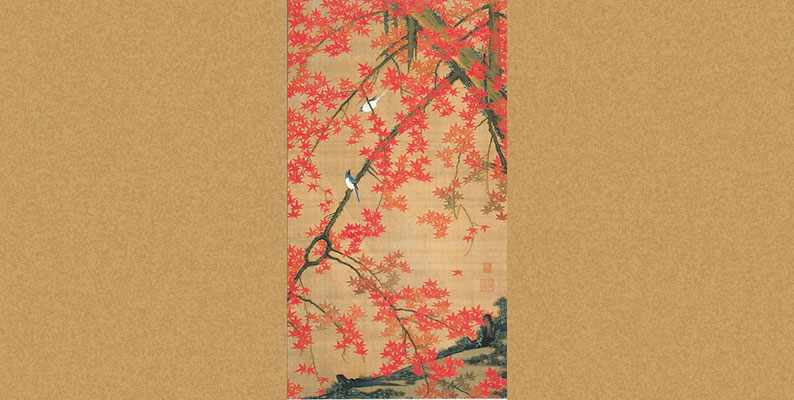राष्ट्रभाषा का स्वरूप
- 1 September, 1951
शेयर करे close
शेयर करे close

शेयर करे close
- 1 September, 1951
राष्ट्रभाषा का स्वरूप
हिंदी राष्ट्रभाषा के पद पर आसीन हो गई। जो लोग किसी और भाषा को राष्ट्रभाषा के पद पर बैठाना चाहते थे उनके सपने टूट गए। पर साथ ही साथ हिंदी की जिम्मेदारियाँ भी बढ़ गईं। अब वह सारे भारत के लोगों की भाषा बन गई है। इसलिए उसके स्वरूप के बारे में आज सोचने-समझने की बड़ी आवश्यकता है।
भाषा का एक रूप तो वह होता है जो सरकारी टकसाल में गढ़ा जाता है। भारतीय सरकार की टकसाल के साँचे कैसे हैं इसका छोटा-सा और विशिष्ट उदाहरण है रेडियो के बदले आकाशवाणी का प्रयोग। जिस मनोवृत्ति का यह परिचायक है, उससे भाषा और देश का कितना हित हो सकता है यह सहज कल्पना की चीज है।
दूसरी ओर भाषा का स्वरूप जनता भी निर्धारित करती है। सरकार द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने के बहुत पहले जनता ने हिंदी को राष्ट्रभाषा मान लिया था। कलकत्ता, बंबई जैसे बड़े शहरों में, जहाँ हर प्रादेशिक भाषा के लोग मौजूद रहते, हिंदी में ही परस्पर विचारों का आदान-प्रदान होता। हाँ, उस हिंदी का स्वरूप कुछ ऐसा था और है कि किताबी हिंदी से उसकी तुलना नहीं की जा सकती। सरकार ने अपने टकसाल में चाहे जैसी भी भाषा ढालनी शुरू की हो, जनता तो अपना काम कर रही है। और जनता के इस काम के पीछे कोई पोंगापंथी दलील नहीं है। वह सिर्फ अपनी सहूलियत के लिए ऐसा करती है। तुर्रा यह कि सरकार के ये सारे कारनामे भी जनता की ही दुहाई देकर किए जा रहे हैं।
किताबी हिंदी और इस तरह की ‘चालू हिंदी’ में पहले ही से एक खाई चली आती थी। बीच-बीच में ऐसे व्यक्ति भी साहित्य के क्षेत्र में आए जिन्होंने उसे पाटने की कोशिश की, जैसे विद्यापति और तुलसीदास। इसीलिए आज भी उनकी कृतियों की लोकप्रियता तथा जन-जीवन पर गहरे प्रभाव को हम बढ़ता हुआ ही पाते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से वह खाई गहरी होती जा रही है। जो सरकारी हिंदी हमारे ऊपर लादी जा रही है वह न तो अहिंदी भाषी क्षेत्रों के लिए नई है बल्कि हिंदी-भाषी क्षेत्रों के लिए भी। जिस पलायनवादी और भूतकाल की ओर मुड़कर देखने वाली नीति का सर्वत्र परिचय आज मिलता है, भाषा-संबंधी नीति भी उसी की उपज है। भूत पर हमें नाज हो सकता है, वह हमारी विरासत हो सकता है, लेकिन वह हमारा लक्ष्य नहीं हो सकता।
इस ‘चालू हिंदी’ के कुछ नमूने यहाँ पेश किए जाते हैं। एक बंगाली सज्जन जिन्होंने कभी हिंदुस्तानी नहीं सीखी, मगर बिहारियों के संसर्ग से जो हिंदुस्तानी बोल लेते हैं, बाइबिल के एक किस्से को इस प्रकार बयान करते हैं–
“एक आदमी का दू ठो लेड़का था। उससे छोटा लेड़का उसका बाप को बोला–‘बाबा हमारा विषय (संपत्ति का हिस्सा हमको दे दीजिये।’ ओही बात सुनके उसको बाबा दोनों लेड़का को दो भाग बटवारा करके दे दिया था। उसको थोड़ा बाद छोटा लेड़का उसको विषय का हिस्सा एक साथ करके दूर देस चला गिया था और उस देश में बदखियाली करके सब विषय खरच कर दिया।”
इसी कथा को एक अनपढ़ बिहारी यों कहेगा–
“एक आदमी को दो लड़का रहा। छोटका बाप से कहा कि हमारा हिस्सा तुम दे दो। बाप लड़कवन का हिस्सा बाँट दिया। फिर छोटा लड़का अपना सब कुछ लेकर परदेस चला गिया, और वहाँ नवाबी से सब उड़ा दिया।”1
आखिर ये नमूने किस बात की ओर संकेत करते हैं? कम से कम इतना तो स्पष्ट है कि रेडियो का ‘आकाशवाणी’ अनुवाद जिस दिशा की ओर संकेत करता है, उसके विपरीत इनका संकेत है। जनता की भाषा, उसके हृदय की भाषा बनने के लिए हिंदी को इन विकृतियों की प्रेरणा का आदर करना पड़ेगा। उसे अपना व्याकरण इतना सरल बनाना होगा कि वह हर किसी को सहज ग्राह्य हो सके। एक जमाना था कि व्याकरण की छोटी-से-छोटी बात पर पत्रिकाओं के पन्ने रंगे जाते थे। अब वह जमाना आया है कि व्याकरण के उन बंधनों को काट फेंकना होगा। तभी हिंदी जनमन की भाषा हो सकेगी। वरना लादी जाने पर वह बोझ ही बनेगी, मन की वाणी नहीं। यह खतरा और भी गहरा इसलिए है कि वर्तमान परिस्थिति में स्थानीय प्रादेशिक भाषाओं का अस्तित्व रहेगा ही। फिर जनता हिंदी में क्यों दिलचस्पी लेगी? उसे राजभाषा समझ कर, सरकारी कामों में उसका उपयोग भले ही होता रहे पर अहिंदी भाषी क्षेत्र में कोई भी ऐसा नहीं रहेगा जो सरकारी हिंदी को आपस की बोलचाल की भाषा बना सके।
डॉ. सुनीतिकुमार चाटुर्ज्या ने अपनी किताब ऋतंभरा में इस प्रश्न पर विस्तार पूर्वक विचार किया है और उन्होंने चालू हिंदी के व्याकरण-स्वरूप एक नमूने का व्याकरण भी पेश किया है। वह कलकत्ते, बंबई इत्यादि शहरों के बाजारों में बोली जाने वाली जनता की हिंदी की विकृतियों का नियमबद्ध स्वरूप है। उस व्याकरण के कुछ नियम यों हैं–
- शब्द रूप–
लिंग-भेद प्रकृति के अनुसार–पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और क्लीवलिंग। स्त्रीलिंग वाले शब्द के विशेषण तथा क्रिया के लिए विशेष प्रत्यय ‘ई’ का प्रयोग नहीं होता। जैसे “एक राजा का एक बेटी था। वह बड़ा खूबसूरत था।”
- सर्वनाम–
‘मैं’ ‘तू’ का प्रयोग नहीं होता।
- धातुरूप–
वचन और लिंग में पार्थक्य नहीं होता।
यह नहीं कहा जा सकता कि हिंदी को सरल करने के लिए व्याकरण में ऐसी ही तरमीमें होनी चाहिए और इस व्याकरण में जो तरमीमें नहीं दी गई हैं उनका कोई स्थान नहीं। जनता ने जिस दिशा की ओर संकेत किया है उसी दिशा में यह एक अगला कदम है। भाषाविदों की एक सक्रिय गोष्ठी इस काम को आगे बढ़ा सकती है। अगर इस दिशा को नजरअंदाज किया गया तो हिंदी के दुर्दिन आने वाले हैं और विद्यापति तथा तुलसीदास की परंपरा मिटने वाली है। साहित्य में ऐसा ग्रहण लगने वाला है कि सशक्त साहित्य का सूर्य कभी नहीं चमकेगा।
इसी दुर्नीति का प्रयोग कर पिछली काँग्रेसी सरकारों ने तामिलनाड और बंगाल के बहुत सारे लोगों को हिंदी विरोधी बना दिया था। अब वैसा विरोध तो संभव नहीं क्योंकि केंद्रीय सरकार की छत्रछाया में सारा काम हो रहा है, पर हृदय के कबूल करने की बात तो नहीं हो सकती। सर पर लद जाएगा, तो लोग ढो लेंगे, बस इतना ही।
भाषा के स्वरूप के साथ लिपि का प्रश्न भी जुड़ा है। और अगर भाषा के स्वरूप को सरल करने की बात मान ली जाय, तो लिपि को भी सरल करने की बात स्वत: सामने आ जाती है। गाँधी जी ने इस दिशा में थोड़ी कोशिश की थी और उनके चेले-चाटी आज भी उस परिपाटी को चला रहे हैं। पर क्या एक वही उपाय है, अन्य कोई उपाय नहीं? लिपि संबंधी किसी सुझाव की बात को ध्यान में लाते ही रोमन लिपि का प्रश्न स्वयं आ खड़ा होता है।
देवनागरी लिपि में कुछ इतनी जटिलता है कि बहुत मौकों पर उलझन उठ खड़ी होती है, खास कर नौसिखुए के लिए। ‘नई धारा’ के जून वाले अंक में ‘लौह लेखक : लौह लेखनी’ शीर्षक लेख उसका अच्छा उदाहरण है। हाँ, देवनागरी लिपि के बारे में भारतीय संस्कृति की परंपरा, भारतीयता, राष्ट्रीय गौरव इत्यादि बातें कही जा सकती हैं। कही भी जाती हैं। लेकिन यह दलील कितनी थोथी है इसकी कल्पना भी सहज ही की जा सकती है। सिर्फ एक पोशाक की ही बात को देख लीजिए! कितने परिवर्तन हुए। हमने अपनी जरूरत के अनुसार विदेशियों के कपड़े तक अपना लिए। लेकिन उससे क्या बिगड़ गया। इतना ही क्यों, हमने मूँछ-दाढ़ी का फैशन भी विदेशियों के अनुकूल कर लिया। पर क्या इतने से ही हम अ-भारतीय हो गए। हाँ, अंधानुकरण की बात जरूर हास्यास्पद है। जैसे चौके में खाना हो तो सूट पहन कर खाना। लेकिन मशीन पर काम करते समय हमें ‘हाफ पैंट और हाफ कमीज’ में ज्यादा सहूलियत होती है, तो धोती-कुरता हम क्यों पहनें? कोई पहनता भी है? फिर तो मोटर और रेलगाड़ी छोड़ कर हमें रथ की बात करनी चाहिए।
साथ ही रोमन लिपि को ज्यों का त्यों अपनाया नहीं जा सकता। यह मानी हुई बात है कि देवनागरी की वर्णमाला उच्चारण की दृष्टि से काफी अच्छी है। उसमें तरमीमों की गुंजाइश जरूर है पर मूलत: वह काफी अच्छी है। इसलिए हम अपनी वर्णमाला को कायम रखते हुए, उसमें थोड़ा-बहुत हेर-फेर कर लिपि को रोमन बना सकते हैं। ऐसी ही लिपि को ‘भारत रोमक’ नाम देकर डॉ. सुनीतिकुमार चाटुर्ज्या ने उसकी सिफारिश की है। उन्होंने तो यहाँ तक भविष्यवाणी की है कि हमें चाहे जितना अरुचिकर मालूम हो, वह दिन आएगा जब भारत की सभी भाषाएँ स्वेच्छा से रोमन लिपि को मान लेंगी।2 और डॉक्टर साहब की भविष्यवाणी सत्य सिद्ध होगी इसमें हमें भी संदेह नहीं। प्रश्न तो इतना ही है कि अगर हमने समय की गति को समझ कर आने वाले युग की तैयारी में हाथ बँटाया तो भविष्य हमारी दाद देगा वरना हमारे नाम पर आने वाली पीढ़ी रोएगी और हमें कोसेगी।
इस सिलसिले में एक मजेदार बात याद हो आई। वैज्ञानिक माप-जोख के लिए अँग्रेजी पैमाने चले आते थे। जैसे लंबाई की माप के लिए फुट, वजन की माप के लिए पौउंड और समय की माप के लिए सेकेंड। पीछे चल कर वैज्ञानिकों को इस प्रणाली में कई दोष नजर आए और उन लोगों ने काफी समझ-बूझकर माप के नए पैमाने बनाए जिसे फ्रेंच प्रणाली या वैज्ञानिक प्रणाली कहते हैं। इस प्रणाली में लंबाई की माप ‘सेंटीमीटर’, वजन की माप ‘ग्राम’ और समय की माप के लिए सेकेंड उपयुक्त होता है। अँग्रेज वैज्ञानिकों ने हठ में जितनी भी किताबें लिखीं अपनी माप की प्रणाली में। आज भी वह प्रणाली इंगलैंड में चलती ही है। पर सारे विज्ञान जगत ने उस प्रणाली को ठुकरा दिया है और धीरे-धीरे अँग्रेज वैज्ञानिकों को भी यह बात समझ में आने लगी है।
क्या हिंदी के हमारे कर्ताधर्ता भी वैसे ही हठ के चंगुल में फँस गए हैं। व्यक्तिगत या दलगत हठ के नाम पर राष्ट्र की प्रगति को रोक रखना कितनी खतरनाक बात है यह किसी से छिपा नहीं। अभी भी समय है। भूल सुधार के लिए कभी देर नहीं होती।
1. डॉ. सुनीतिकुमार चाटुर्ज्या: ऋतंभरा, पृ. 36
2. ऋतंभरा, पृ. 60
Image: Vase of flowers
Image Source: WikiArt
Artist: Paul Gauguin
Image in Public Domain