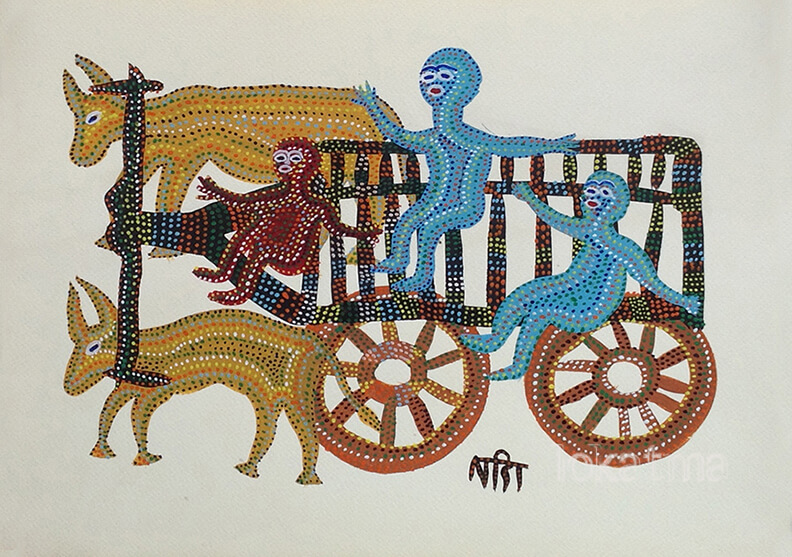वैज्ञानिक संपादन की एक छटा
- 1 August, 1953
शेयर करे close
शेयर करे close

शेयर करे close
- 1 August, 1953
वैज्ञानिक संपादन की एक छटा
वैज्ञानिक संपादन के विषय में कुछ कहने से लाभ नहीं, उसका रूप भर दिखा देना किसी ‘अकादमी’ का काम है। सो उत्तर प्रदेश की ‘हिंदुस्तानी एकेडेमी’ के वैज्ञानिक संपादन का एक नमूना है ‘जायसी ग्रंथावली’ का ‘प्रामाणिक संस्करण’। उसके ‘अधिकारी विद्वान’ डॉ. माताप्रसाद गुप्त का कथन है–
“(3) ग्रियर्सन में ‘अरगाना’ शब्द निम्नलिखित स्थल पर आया है–
जावँत अहहिं सकल अरगाना। साँबर लेहु दूरि है जाना। (128’2) ‘अरगाना’ के स्थान पर ‘अरकाना’ पाठ होने के संबंध में शुक्ल जी का प्रमाण ‘अरकाने-दौलत’ उसकी व्युत्पत्ति पर आधारित है। ‘अरकाना’ पाठ और उसकी ‘अरकाने-दौलत’ व्युत्पत्ति दोनों शुक्ल जी को उक्त कानपुरवाले संस्करण से मिले हैं, यद्यपि शुक्ल जी ने यह लिखा नहीं है–उसमें मूल में पाठ ‘अरकाना’ तथा अनुवाद में ‘अरकाने दौलत’ दिए हुए हैं।
किंतु भाषा की संभावनाओं की ओर उनका ध्यान नहीं गया–‘अरकाना’ का ‘भाषा’ में ‘अरगाना’ और ‘अरगाना’ का ‘उरगाना’ या ‘ओरगाना’ हुआ होना स्वाभाविक है, यथा शोक से ‘निसोगा’ (42’7), (58’8), ‘अनेक’ से ‘अनेग’ (37’3) ‘बिकसै’ से ‘बिगसै’ (326’8)। ‘पदमावत’ में यह शब्द अन्यत्र इसी रूप में आया भी है। एक स्थान पर है–
राघवचेतन चेतन महा। आई ‘ओरगि’ राजा के रहा। (446’4) ‘ओरगि’ शब्द की इस व्युत्पत्ति को न समझ कर शुक्ल जी ने वहाँ पाठ दिया है–
आऊ सरि राजा के रहा।
यद्यपि नवलकिशोर प्रेस, और कानपुर वाली उक्त प्रतियों में पाठ ‘ओरकि’ था–जो ‘ओरगि’ का ही उर्दू लिपि की विशेषताओं के कारण विकृत पाठ है।” (भूमिका, पृष्ठ-112)
डॉ. गुप्त के इस कथन का किसी ‘विज्ञान’ से नाता क्या? लिपि-विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो उर्दू लिपि में ‘क’ और ‘ग’ के निश्चित संकेत हैं। उसमें कभी ‘क’ को ‘ग’ अथवा ‘ग’ को ‘क’ नहीं पढ़ा जा सकता। हाँ, अरबी लिपि में अवश्य ही ‘ग’ का अपना कोई संकेत नहीं। कारण यह उसकी अपनी ध्वनि नहीं। और भाषा-विज्ञान की दृष्टि से विचारा जाए तो प्रत्यक्ष हो कि डॉ. गुप्त के उदाहरणानुसार तो ‘अरकाना’ का अरगाना हो गया, पर उसने कभी ‘उरगाना’ या ‘ओरगाना’ सिद्ध नहीं हुआ, तो भी इनमें फेर रहा ‘अ’, ‘उ’ और ‘ओ’ का ही न? किंतु नहीं। डॉ. गुप्त के ‘विज्ञान’ को इतने से ही संतोष कहाँ? नहीं, उनको तो ‘ओरगि’ में भी यही ‘अरकाना’ दिखाई देता है। पता नहीं, डॉ. गुप्त के यहाँ इसका अर्थ क्या है और कैसे उन्होंने ‘ओरगाना’ और ‘ओरगि’ को एक कर दिया। स्मरण रहे डॉ. गुप्त का ही यह भी विचार है–
“26’3 छप्पन कोटि कटक कर साजा। सबै छत्रपति ‘ओरगन्ह’ राजा।
‘ओरगन्ह’<‘अरकान’ [-ए-दौलत] (तुलना 099’9)” (पृ.-30) तुलना भी कर लीजिए। 99-9 है–
अष्टौ कुरी नाग ओरगाने भै केसन्हि के बाँद।
और यहाँ भी आपकी व्याख्या है–
“ओरगाने<अरकान [-ए-दौलत] (तुलना. 26’3)” (वही, पृ.-32) ‘ओरगि’, ‘ओरगन्ह’ एवं ‘ओरगाने’ को दृष्टि में रख कर देखें यह कि वास्तव में इनका रहस्य क्या और क्या है इनका लागत वस्तुत: इस ‘अरकान [-ए-दौलत]’ से। क्या केवल ‘अरकान’ का कुछ अर्थ नहीं? अच्छा होगा, यहीं इतना और भी जान लें कि इस प्रामाणिक संस्करण का 457’3 है–
छत्तिस लाख ओरगन्ह असवारा। बीस सहस हस्ती दरबारा। तथा इसी का 613’4 है–
छत्तिस लाख तुरै जेहिं छाजहिं। बीस सहस हस्ती दर गाजहिं। तो क्या ‘छत्तिस लाख ओरगन्ह असवारा’ और ‘छत्तिस लाख तुरै जेहिं छाजहिं’ में कोई भेद नहीं? स्मरण रहे डॉ. गुप्त की साखी है कि द्वि. 4, 5 अर्थात् कानपुर और नवलकिशोर प्रेस के स्थान पर ‘तुरक (या तुरग)’ जो है सर्वथा 613’4 के मेल में।
अपनी ओर से क्या कहें? कवि का ही कथन है इस प्रामाणिक संस्करण में–
राघौ चेतन कीन्ह पयाना। ढीली नगर जाइ नियराना।
जाइ साहि के बार पहूँचा। देखा राज जगत पर ऊँचा।
छत्तिस लाख ओरगन्ह असवारा। बीस सहस हस्ती दरबारा।
जाँवत तपै जगत महँ भानू। ताँवत राज करै सुलतानू।
चहूँ खंड के राजा आवहिं। होइ अस मर्द जोहारि न पावहिं।
मन तिवानि के राघौ झूरा। नहिं उबारु जिय कादर पूरा।
जहाँ झुराहिं दिहें सिर छाता। तहाँ हमार को चालै बाता।
अरध उरध नहिं सूझै लाखन्ह उमरा मीर।
अब खुर खेह जाब मिलि आइ परे तेहि भीर।।457।।
पता नहीं डॉ. गुप्त ‘छत्तिस लाख ओरगन्ह असवारा’ का अर्थ क्या लगाते हैं और क्या समझते हैं ‘लाखन्ह उमरा मीर’ को। परंतु जो अति स्पष्ट है वह यह है कि डॉ. गुप्त की दृष्टि में ‘ओरगन्ह’ है ‘अरकान [-ए-दौलत]’। किंतु यह ‘अरकान [-ए-दौलत]’ क्या है? कौन कहे? वैज्ञानिक संपादन से इसका नाता क्या? परंतु 613.4 तो ‘ओरगन्ह’ और ‘तुरग’ को एक ही कर रहा है न? कासत–
बादिल कोरि जसोवै माया। आइ गहे बादिल के पाया।
बादिल राय मोर तूँ बारा। का जानसि कस होइ जुझारा।
पातसाहि पुहुमीपति राजा। सनमुख होइ न हमीरहिं छाजा।
छत्तिस लाख तुरै जेहिं छाजहिं। बीस सहस हस्ती दर गाजहिं।
अलाउद्दीन के लिए यह ‘छत्तिस लाख’ कुछ महत्त्व का है न? ‘बीस सहस हस्ती’ के साथ ‘छत्तिस लाख सुरगन्ह’ का ही मेल है न? फिर भी डॉ. गुप्त इसका विचार नहीं करते और एक ‘अरकान’ से न जाने क्या-क्या काम लेते हैं?
डॉ. माता प्रसाद गुप्त के ‘प्रामाणिक संस्करण’ की दिव्यता तो देखिए। भूमिका में आप ही लिखते हैं कि–
‘नवलकिशोर’ प्रेस, और कानपुरवाली उक्त प्रतियों में पाठ ‘ओरकि’ था किंतु स्वयं मूल में इस पाठ-भेद का निर्देश नहीं करते। देखिए उनका है न प्रामाणिक संस्करण यही–
[446]
राघौ चेतनि चेतनि1 महा2। आइ ओरँगि राजा के3 रहा।
अर्थात् मूल में ‘ओरँगि’ का पाठ सर्वत्र है और यदि कहीं पाठ-भेद है तो ‘चेतनि’, ‘महा’ और ‘के’ में। परंतु वस्तुस्थिति यह है कि भूमिका का ‘ओरगि’ यहाँ मूल में ‘ओरँगि’ हो गया है। क्योंकि जिज्ञासा कौन करे? परंतु कुछ विचारने से आप ही पता होगा कि हो न हो कहीं यह ‘ओरक’ ‘ओलक’ का रूपांतर न हो। कारण–
रानी चली छड़ावै राजहि आपु होइ तेहि ओल।
बत्तिस सहस सँग तुरिअ खिंचावहि सोरह से चंडोल।।622।।
तो फिर ‘ओल’ का अर्थ क्या? अपनी ओर से क्या कहें? ‘हिंदी-शब्दसागर’ का अवतरण है–
“ओल-संज्ञा पुं. [सं.] सूरन, जिमीकंद।
वि. गीला। ओदा।
संज्ञा स्त्री [सं. कोड] (1) गोद। (2) आड़। ओट। (3) शरण, पनाह।
उ.–सूरदास ताको डर काको हरि गिरिवर के ओलै।–सूर। (4) किसी वस्तु वा प्राणी का किसी दूसरे के पास जमानत में उस समय तक के लिए रहना जब तक उस दूसरे व्यक्ति को कुछ रुपया न दिया जाए वा उसकी कोई शर्त न पूरी की जाए। जमानत। उ.–टीपू ने अपने दोनों लड़कों को ओल में लार्ड कार्नवालिस के पास भेज दिया।–शिवप्रसाद।”
तो क्या ‘ओरक’ यह ‘ओलक’ नहीं और ‘ओरग’ तथा ‘ओरगाना’ का इससे लगाव नहीं? कहिए रहस्य क्या है ‘अरकान [-ए-दौलत]’ का?
जो हो, डॉ. गुप्त ही का यह भी कथन है–
“दूसरे स्थान पर है–
अष्टौ कुरी नाग ओरगाने भै केसन्हि के बाँद। (99’9)
‘ओरगाने’ के स्थान पर नवलकिशोर प्रेस वाले में पाठ ‘उरके’ था, कानपुर वाले में ‘अरुझे’ था, और ग्रियर्सन में ‘सब’ पाठ स्वीकृत किया गया था। कदाचित् कानपुर वाले संस्करण का ही अनुसरण करते हुए शुक्ल जी ने भी पाठ ‘अरुझे’ दिया। किंतु यदि ग्रियर्सन द्वारा दिए हुए पाठांतरों पर उन्होंने ध्यान दिया होता, तो उन्हें ज्ञात होता कि प्र. 1 तथा तृ. 1 के अतिरिक्त उनकी सभी प्रतियों में इसके स्थान पर ‘उरगाने’ ‘उरगानेउ’ ‘ओरगाएन’ ‘अउरँगे’ पाठ है। ग्रियर्सन ने स्वत: इस स्थल पर कदाचित् ‘ओरगाने’ शब्द से अपरिचित होने के कारण–प्रतियों के बहुमत एवं आधार-प्रति विषयक अपने दोनों सिद्धांतों का उल्लंघन किया था। शुक्ल जी शब्द से तो परिचित थे, किंतु उन्होंने कदाचित् ग्रियर्सन के संस्करण में दिए हुए पाठांतरों पर कोई ध्यान नहीं दिया, अन्यथा कदाचित् वे भी ‘ओरगाने’ पाठ ही स्वीकार करते।” (भूमिका, पृ.–112’3)
‘ग्रियर्सन’ और ‘शुक्ल’ ने क्या किया की जानकारी के लिए यदि ‘जायसी-ग्रंथावली’ का ‘प्रामाणिक संस्करण’ निकला है तो डॉ. माताप्रसाद गुप्त की भूमिका और भी विचारणीय है और ‘हिंदुस्तानी एकेडेमी’ के लोगों से खुल कर पूछ लेना है कि आखिर उत्तर प्रदेश की सरकार को इसकी आवश्यकता क्या पड़ी कि आप लोगों ने ऐसा दिव्य डौल डाला। और यदि सचमुच इसका उद्देश्य वैज्ञानिक ढंग से जायसी के प्रकृत पाठ तक पहुँचना है तो उसका यह रूप क्यों? हम और कुछ नहीं, एकेडेमी के ‘मंत्री तथा कोषाध्यक्ष’ डॉ. धीरेंद्र वर्मा जी से जानना चाहते हैं कि वस्तुत: माजरा क्या है जो जायसी का ऐसा प्रामाणिक पाठ निकल रहा है जिसका पता डॉ. गुप्त को छोड़ कर कदाचित् किसी को नहीं है। यदि किसी को है तो आप ही बताने का कष्ट करें कि उसका नामधेय क्या है। उससे यह जन तो पूछ देखे कि वास्तव में ‘पदमावत’ में ‘अरकान [-ए-दौलत]’ का रहस्य क्या है और कितने हैं उसमें इसके रूप। कहने को तो डॉ. गुप्त कहते हैं कि ‘नवलकिशोर प्रेस वाले में पाठ ‘उरके’ था’ किंतु टिप्पणी में देते हैं उसका पाठ ‘नाग सब डरि कै।’ तो क्या इसका अर्थ यह समझा जाए कि वास्तव में इसका पाठ है ‘नवलकिशोर प्रेस वाले में’–
अष्टौ कुरी नाग सब डरि कै
अन्यथा इस वैज्ञानिक संपादन का मर्म क्या? स्मरण रहे, मूल का पाठ है–
अस्टौ कुरी नाग ओरगाने भै केसन्हि के बाँद।
और यही ‘नवलकिशोर प्रेस वाले में’ है इस रूप में–
अश्टौ कुली नाग सब डरि कै भै केस के बाँद।
‘अश्टौ’, ‘अष्टौ’ तथा ‘अस्टौ’ में किसे मूल माना जाए का महत्त्व डॉ. गुप्त के यहाँ न हो, पर पाठ तो उसका मनमाना नहीं। ‘भूमिका’ और ‘मूल’ में इतना भेद क्यों? क्या डॉ. गुप्त की सारी शक्ति ‘भूमिका’ में जुटी थी और संपादन का कार्य उनकी छाया में चल रहा था? अन्यथा इस ‘अष्टौ’ और ‘अस्टौ’ तथा ‘उर के’ और ‘डरि कै’ का रहस्य क्या? यदि ‘डर कै’ पाठ होता तो प्रेस की भूल कही जा सकती थी; किंतु ‘डरि कै’ के कारण यह संपादन का प्रमाद निकला न?
डॉ. माताप्रसाद गुप्त की संपादन-कला के विषय में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। बात तो अभी उनके वैज्ञानिक संपादन की ही है न? अतएव लीजिए फिर उसी ‘अरकान (-ए-दौलत)’ को। इस ‘अरकान’ के कितने रूप ‘पदमावत’ में मिलते हैं, इसे कौन कहे? परंतु इतना तो कोई भी धड़ल्ले से कह सकता है कि डॉ. गुप्त का प्रामाणिक पाठ है–
छप्पन कोटि कटक दर साजा। सबै छत्रपति ओरँगन्ह राजा। (26’3) जबकि इसी का भूमिका-पाठ है–
छप्पन कोटि कटक दर साजा। सबै छत्रपति ‘ओरगन्ह’ राजा।
‘अरकान’ से ‘ओरँगन्ह’ और ‘ओरगन्ह’ कैसे बना, इसका पता नहीं। परंतु देखना यह है कि डॉ. गुप्त का वैज्ञानिक संपादन इस ‘अरकान’ को समझता क्या है। हम भूमिका में देख चुके हैं कि ‘ओरगि’ को भी डॉ. गुप्त ‘अरकान’ ही समझते हैं और मूल में उसका पाठ ‘ओरँगि’ कर देते हैं। तो क्या ‘ओरँगा’ भी ‘अरकान’ नहीं? देखिए डॉ. गुप्त का प्रामाणिक पाठ है–
जानहुं बेधि साहि कै राखा। गढ़ भा गरुर फुलाएँ पाँखा।
औरँगा केरि कठिन है जाता। तौ पै लहै होइ मुख राता।
पीठि देहिं नहिं बानन्हि लागे। चाँपत जाहिं पगहिं पग आगे।
चारि पहर दिन बीता। गढ़ न टूट तस बाँक।
गरुव होत पै आवै। दिन-दिन टाँकहि टाँक।। (524-5-9)
पाठ-भेद की दृष्टि से देखा जाए तो डॉ. गुप्त का ‘प्रामाणिक संस्करण’ बताता है कि (द्वि. 5) अर्थात् ‘नवलकिशोर प्रेस वाले में’ ‘जानहुँ’ के स्थान पर ‘बान’ है और है दोहे का प्रथम चरण यह–
चारि पहर दिन जूझ भा।
परंतु तथ्य है कुछ और ही। उसका पाठ है–
बान बेद साही कै राखा। गढ़भा गरुर फुलावै पाँखा।
ओरगा केरि कठिन है बाता। तो पै लहैं होइ मुख राता।
पीठि देहिं तेहि बानन्ह लागैं। चाँपत जाहिं पगहिं पग आगैं।
चारि पहर दिन जूझ भा गढ़ न टूट तस बाँक।
गरुव होत पै आवै दिन दिन नाँकहि नाँक।।
‘ओरगा’ और ‘ओरँगा’ में भेद नहीं किया तो कोई बात नहीं, पर ‘बाता’ और ‘जाता’ की उपेक्षा क्यों की गई? और ‘नाँकहि नाँक’ को इतना नगण्य क्यों समझा गया कि पाठ-भेद में उसका उल्लेख भी न हुआ। ‘टाँकहि टाँक’ से तो वह कहीं अधिक सुबोध था न? हम जानना चाहते हैं कि डॉ. गुप्त अथवा प्रयाग की हिंदुस्तानी एकेडेमी का ‘वैज्ञानिक संपादन’ किस पद्धति पर चलता है जो इस प्रकार का गड़बड़झाला भी ‘प्रामाणिक’ बन जाता है। पाठक भली-भाँति समझ लें कि यह ‘ओरगा’ और कुछ नहीं, ‘गरुड़’ का विपक्षी ‘उरग’ है। डॉ. गुप्त इसे अरकान समझा करें। बोध के अभाव में विज्ञान?
Original Image: The Attributes of the Sciences
Image Source: WikiArt
Artist: Jean Baptiste Simeon Chardin
Image in Public Domain
This is a Modified version of the Original Artwork