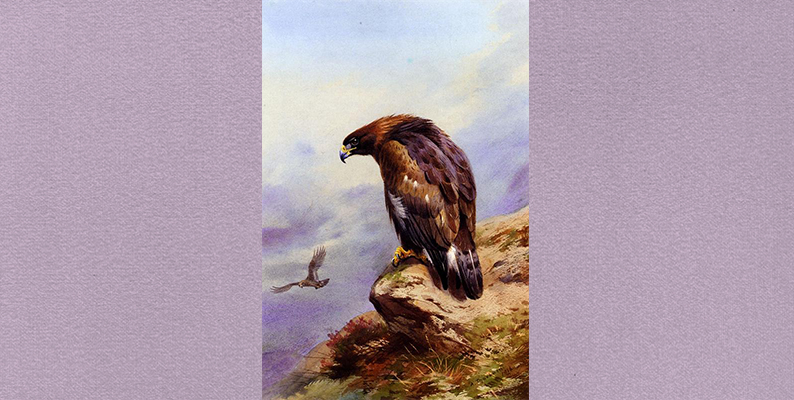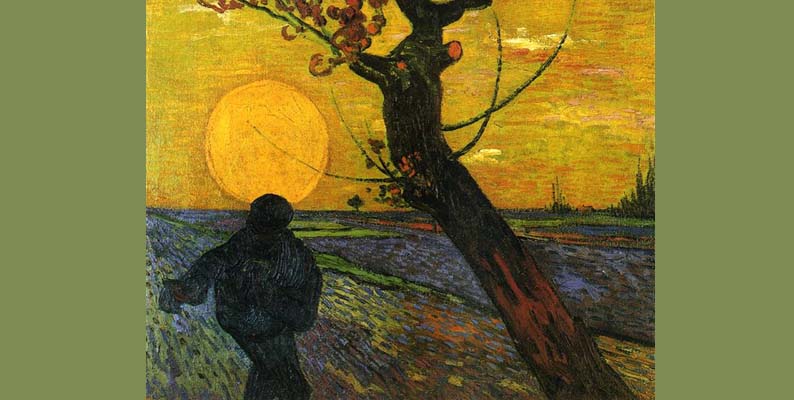पंडित विद्यानिवास मिश्र के ललित निबंध
शेयर करे close
शेयर करे close

शेयर करे close
- 1 December, 2016
पंडित विद्यानिवास मिश्र के ललित निबंध
ललित निबंध का प्रसंग आते ही मेरे सामने पद्मभूषण पंडित विद्यानिवास मिश्र की निर्मल छवि उभर आती है। क्या दिव्य व्यक्तित्व की आभा थी उनमें! बोलते तो उनकी जुबान से पूरबी की संस्कृति झरने लगती और लिखते तो जैसे उनके अथाह ज्ञान का सोता देसी संस्कृति में घुल-मिलकर असंख्य प्राणियों के तप्त हृदय को संतृप्त कर देता! पहली बार उनसे वर्ष 1988 में अपने गुरु आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा के सौजन्य से पटना स्थित उनके ही निवास पर मिला था। घंटों उनके साथ रहने का अवसर मिला। उनकी बोली-बानी, आचार-व्यवहार की छाप अब तक मेरे मानस पर अंकित है। दूसरी बार, जब वे ‘नवभारत टाइम्स’ के प्रधान संपादक होकर दिल्ली रहने लगे, तब उनके दफ्तर में ही मिला था। तब कुछ पल का ही उनका साहचर्य मिला, लेकिन उसकी आत्मीयता आज तक मुझे भिंगोती है। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी से कभी मिला नहीं, केवल उन्हें जी भर पढ़ा भर है; लेकिन प्रो. नामवर सिंह, डॉ. विश्वनाथ त्रिपाठी आदि के लेखन से उनकी जो छवि मेरे मानस में अंकित हुई, उसे पंडित विद्यानिवास मिश्र में ही मूर्त रूप में देखता आया। बोली, भाषा, व्यवहार, वेशभूषा आदि हर रूप में जैसे वे द्विवेदी जी के ही प्रतिरूप थे। ललित निबंध लेखन में तो वे थे ही! आखिर थे तो वे दोनों ही पुरबिया ही न! वहाँ की लोक-संस्कृति में रचे-सने! अब पूरबी संस्कृति को जानने-समझने की उत्कंठा हो, तो उनके ललित निबंधों का रस तो ग्रहण करना ही पड़ेगा!
ललित निबंध के लेखन में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। उनके निबंधों में पांडित्य, धर्म, दर्शन, इतिहास, पुरातत्त्व, भाषा-विज्ञान आदि से लेकर मानवतावादी दृष्टिकोण तक की प्रधानता है। कहना चाहिए कि उनके आलोचनात्मक व्यक्तित्व और सर्जन मन का संगम ही ललित निबंध है। आगे चलकर उनकी इसी परंपरा को समृद्ध करते हुए पंडित विद्यानिवास मिश्र ललित निबंधकार रूप में प्रतिष्ठित हुए। यों भी उनका सम्मोहक व्यक्तित्व कवि, आलोचक, अनुवादक, संपादक, भाषाविज्ञानी आदि से समन्वित है। वे वेद, पुराण, उपनिषद्, शास्त्र, धर्म के साथ-साथ लोकजीवन, लोक-संस्कृति तथा लोकशास्त्र के भी अद्भुत ज्ञाता रहे। संस्कृत, पालि, प्राकृत, फ्रेंच, अँग्रेजी, फारसी आदि भाषाओं पर तो उनका अधिकार विलक्षण रूप में रहा। केवल ललित निबंध की ही बात करें तो ‘छितवन की छाँह’, ‘तमाल के झरोखे से’, ‘गाँव का मन’, ‘मेरे राम का मुकुट भींग रहा है’, ‘वसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं’, ‘परंपरा बंधन नहीं’, ‘शेफाली झर रही है’, ‘तुम चंदन हम पानी’, ‘आँगन का पंछी’, ‘बंजारा मन’ जैसी अनगिनत पुस्तकें उन्होंने हिंदी जगत को दीं, जिनसे गुजर कर भारतीय ज्ञान, संस्कृति और उसकी आत्मा को समझा जा सकता है। उनके निबंधों में विचार या घटना विशेष की विविध संदर्भों में रम्य प्रस्तुति, प्राकृतिक सौंदर्य की छवियों का अंकन, अवधी प्रभावित भोजपुरी बोली-बानी के उदाहरण की प्रस्तुति से पाठकों में आत्मीयता का भाव उत्पन्न करना आदि ऐसी विशेषताएँ हैं, जो मन-प्राणों को मोह लेती हैं। अपने पांडित्य का उपयोग तो वे विषय को साफ एवं प्रामाणिक करने के निमित्त ही करते हैं।
इधर हिंदी संसार में कथेतर गद्य की खासी चर्चा चल रही है। मेरे सामने कथेतर गद्य में पंडित विद्यानिवास मिश्र की पुस्तक ‘छितवन की छाँह’ है, जिसके ललित निबंधों के ब्याज से उनकी निबंध कला के वैशिष्ट्य पर चर्चा होगी, किंतु उसके पूर्व ललित निबंध की तात्विकियों पर थोड़ी-सी चर्चा अपेक्षित होगी। अन्य आधुनिक विधाओं की तरह हिंदी में ललित निबंध का सूत्रपात भी भारतेंदु काल से ही आरंभ माना जाता है। तब बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी, बालमुकुंद गुप्त, सरदार पूर्ण सिंह, पद्म सिंह शर्मा आदि ने ललित निबंध की भावात्मक कला को विकसित किया। विद्वानों का मानना है कि ललित निबंध निजता और सामूहिकता के मंथन से निकले चिंतन एवं लालित्य की ऐसी रम्य रचना है, जिसमें व्यक्ति की अंतश्चेतना से लेकर सांस्कृतिक परिदृश्य तक के विस्तार को प्रभावित करने का कलात्मक सौष्ठव है। स्वयं पंडित विद्यानिवास मिश्र ने इस विधा पर विचार करते हुए एक जगह लिखा है कि ‘ललित निबंध में मोहकता स्मृतियों के ताने-बाने से उतनी नहीं आती, जितनी आती है शब्दों की चित्रमयता से और भावों की सरसता से, आरोही-अवरोही सरसता से; जबकि व्यक्ति व्यंजक निबंधों में स्मृतियों का ताना-बाना विशेष मतलब रखता है। और ये स्मृतियाँ अपनी होते हुए भी दूसरों में घुली हुई अपनेपन की होती हैं। व्यक्तिव्यंजक निबंध में भाव विचारमय होने के लिए प्रस्तुत होते हैं, जबकि शब्द आत्मीय संवाद स्थापित करने के लिए।’ आगे वे लिखते हैं कि ललित निबंध लिखने के लिए मुक्त निबंधक फक्कड़पन होना आवश्यक है। निस्संग फक्कड़पन के साथ-साथ आसपास के जीवन में गहरी संपृक्ति होनी आवश्यक है। पंडित जी के ललित निबंध विषयक इन विचारों के आलोक में इस विधा के प्रमुख तत्त्व होंगे–लालित्य, विषय-विस्तार, रागात्मकता, स्वच्छंदता, सांस्कृतिकता, वैयक्तिकता, ललित शैली आदि।
‘छितवन की छाँह’ में सतरह निबंध हैं–‘छितवन की छाँह’, ‘हरसिंगार’, ‘गऊचोरी’, ‘साँझभई’, ‘वसंत न आवै’, जमुना के तीरे-तीरे’, ‘चंद्रमा मनसो जातः’, ‘साँची कहौं व्रजराज तुम्हें रतिराज किधौ रितुराज कियौ है’, ‘प्यारे हरिचंद की कहानी रहि जायगी’, ‘धनवा पियर भइलें मनवा पियर भइले’, ‘सखा धर्ममय अस रथ जाके’, ‘दिया टिमटिमा रहा है’, ‘तांडव देवि भूयादभीष्ट्यै च नः’, ‘टिकोरा’, ‘होरहा’, ‘आहो आहो संज्ञा गोंसाईंनि’ और ‘घने नीम तरु तले’। इन निबंधों में अधिकांशतः भावात्मक हैं, जिनमें ग्रामीण चेतना और उनकी संस्कृति के दर्शन सहज रूप में हो जाते हैं और शैली में भी एक प्रकार की आत्मीयता उत्पन्न हो जाती है। पंडित विद्यानिवास मिश्र के इसी प्रकार के निबंधों में पांडित्य और सहजता के अनूठे मेल को लक्षित करते हुए स.ही.वा. अज्ञेय ने टिप्पणी की है कि ‘सर्जनातमक गद्य के रचयिताओं में विद्यानिवास मिश्र अग्रगण्य हैं। उन्होंने संस्कृत साहित्य को मथकर उसका नवनीत चखा है और लोकवाणी की गोरण गंध से सदा स्फूर्ति भी पाते रहे हैं। ललित निबंध वह लिखते हैं तो लालित्य के किसी मोह से नहीं; इसलिए कि गहरी, तीखी, आमंत्रण या चुनौती भरी बातें भी वह एक वेलाग और निर्द्वेष नहीं बल्कि कौतुकभरी सहजता से कह जाते हैं।’ हालाँकि अज्ञेय की यह टिप्पणी पंडित जी की निबंध-पुस्तक ‘मेरे राम का मुकुट भींग रहा है’ के फ्लैप पर उस संकलन के निबंधों के संदर्भ में है, किंतु टिप्पणी का विस्तार उनके तमाम निबंधों के भाव-संबंध में देखा जा सकता है।
‘छितवन की छाँह’ का पहला ही निबंध ग्रंथ-शीर्षक पर है, जिसमें अत्यंत भावपूर्ण शैली में छितवन की प्रकृति, उसके गुण-दोष तथा प्रभाव की चर्चा की गई है। लेखक अपने छात्र जीवन से चौथेपन की अवस्था तक छितवन से भावात्मक रूप से जुड़ा रहा। बावजूद इसके कि ‘लोक में छितवन के बारे में प्रसिद्धि है कि इसकी छाया में जाते ही आदमी के सब पुण्य खत्म हो जाते हैं, इसलिए इसे कोई लगाता नहीं’, लेखक छितवन की मादकता के प्रभाव में आसक्त रहता है। बतौर लेखक ‘यह छितवन साक्षी है मेरी प्रीति का, मेरी प्रीति के प्रथम उत्सर्ग का और उसकी प्रथम प्राप्ति का। मेरे कुसुमित यौवन के दूसरे मोड़ पर का यह साक्षी, अब तक न जाने कितने प्रणय-कलहों के तपन के बीच, न जाने कितने विकृत जीवन की दुर्गंधियों के बीच और न जाने कितनी विरसताओं के बीच स्नेह की समरसता का संबल देता रहता है। तब से न जाने कितनी बार दीये में स्नेह भरा गया होगा, पर जीवनदीप की अखंड ज्योति की प्रेरणा मुझे मिली है, इस दूसरे छितवन की छाया से।’ ग्राम्य गंध में पगा लेखक का जीवन चाहे महानगरों की उन्नत सुख-सुविधाओं में विकसित होता रहा हो, लेकिन उनके मन-प्राणों की ऊर्जा ग्राम्य-संस्कृतियों से ही मिलती रही है; इसलिए वर्जनाओं अथवा नकारात्मक मान्यताओं के बावजूद वे हर उन चीजों का साहचर्य पाना चाहते हैं, जिनसे उनके छुटपन की स्मृतियाँ जुड़ी हुई हैं। वे मुक्त मन कहते हैं कि ‘छितवन की छाँह’ हमें मिलती है मधुमास की नई संध्या में और वह फिर मिलती है कुआर की उमसी दोपहरी में। वह यौवन के चढ़ाव और उतार का मापदंड है।’ इसी ‘मापदंड’ की स्मृति-गंध से लेखक रस विमुग्ध होता रहा है। उनकी एकांत मान्यता है कि छितवन का आनंद वही ले सकता है जो उसकी प्रकृति से प्रेम करता है। जो छितवन की प्रकृति से प्रेम नहीं करता, उसके लिए तो वह मरघट का पेड़ है। इसलिए वे साफ-साफ कहते हैं कि ‘…रही बात घर-घर घाट-घाट छितवन के पेड़ लगाने की, उसकी सलाह न दूँगा, क्योंकि सबका मन एक-सा नहीं होता और सब अपने जीवन के साथ इतना बड़ा जुआ खेलने को तैयार नहीं मिलते। जहाँ मरघट होगा, वहाँ छितवन का पेड़ मिलेगा ही, चिता की चिरायँध गंध का प्रतिकार देने के लिए और मरघट न होगा तो मनुष्य सियार और कुत्ता बन जाएगा। छितवन देने के लिए किसी वन महोत्सव की अपेक्षा नहीं, वर मरघट का शृंगार है। वह मिट्टी के शरीर का उत्कर्ष है और शरीर के मिट्टी में मिल जाने पर उसका एकमात्र अवशेष। जाहिर है कि ऐसे छितवन की छाँह में सुख-सुकून उसी को मिल सकता है, जो उसकी प्रकृति से प्रेम की दीवानगी रखता है। ‘छितवन की छाँह’ में स्मृति की स्वच्छंदता की रागात्मक शैली में प्रस्तुति के द्वारा छितवन के नैसर्गिक सौंदर्य को उद्भाषित किया गया है।
पुस्तक की भूमिका में लेखक ने छितवन के सौंदर्य को रेखांकित करते हुए लिखा भी है कि ‘गंध-साधना, मैं बार-बार करता हूँ, सबसे चरम और कठिन साधना है। इस गंध-साधना का नंदन वन यही छितवन है, जो जितना ही दूर रहता है, उतना ही मादक; जितना ही समीप, उतना ही सामान्य और निर्विशेष। …छितवन पार्थिव शरीर के यौवन का प्रतीक है, उसकी समस्त मादकता का, उसकी सामूहिक चेतना का, उसके निश्शेष आत्मसमर्पण का और उसके निश्चल और शुभ्र अनुराग का। छितवन की छाँह में अतृप्ति की तृप्ति है, अरति की रति है और अथ की इति।’ छितवन में सौंदर्य का जो लालित्य लेखक को दृष्टिगोचर हुआ, कदाचित वही ‘हरसिंगार’ में भी, क्योंकि ‘हरसिंगार है शिव के भालेंदु का जावकमय शृंगार।’ जैसे छितवन की छाँह मादक है, वैसे ही ‘हरसिंगार की ढुरन पाकर उत्कंठा और तीव्र हो जाती है, मान और बलवान हो जाता है और दर्द और नशीला।’ कहते हैं हरसिंगार में प्रतिदान की भावना होती है। अपने सौष्ठव से वह हर चाहने वाले को सम्मोहित करता है। आखिर वह प्रकृति का शृंगार जो ठहरा! कहते हैं, जब किसी का प्रेम खो जाता है, तब हरसिंगार की छाँह में ही आकर वह अपनी राह पा जाता है। एक से निराश होकर वह बहु का आशाप्रद हो जाता है। इस तरह एकोन्मुख प्रेम की मृत्यु की बहून्मुख प्रसाद का जीवन देना, यही हरसिंगार का संदेश है और जीवन के नीरव निशीथ में, विरह के अनंत अंधकार में और निराशा की विराट निःशब्दता में धीरज के ललौहें फूल बरसाना ही उसका काम है। हरसिंगार के बहुविध भाव-संसार को यहाँ लेखक ने अपनी रम्य शैली में प्रस्तुत किया है। कभी-कभी मैं सोचता हूँ कि क्या साहित्य केवल शब्दों में भाव-संसार का खुलना-खिलना ही है अथवा और कुछ भी है? विद्यानिवास मिश्र के इन निबंधों को पढ़ते हुए मेरी यह धारणा पुष्ट होती है कि साहित्य आज भी अंततः और तत्त्वतः भाषा की साधना है, जो अभिव्यक्ति के कौशल को समृद्ध करता है। इस उक्ति के विनियोग के लिए ‘गऊचोरी’ निबंध की चर्चा की जा सकती है।
कभी-कभी सामान्य बतकही से भी असामान्य किस्से निकलने लगते हैं, ऐसा ‘गऊचोरी’ को पढ़ते हुए लगा। एक बार जब बाढ़ उतार पर थी, तो नाव से अपने गाँव जाते हुए यों ही बतकही के लिए लेखक ने माझी से पूछा–‘कह सहती, गाँव-गड़ा के हालचाल कइसन बा?’ जवाब में पता चला कि इन दिनों गाँव-जवार में गाय की चोरी बहुत हो रही है। फिर इस गऊचोरी के ब्याज से लेखक ने गाय-चोरी के अलावे भूमि चोरी, राज्य चोरी, साहित्य चोरी तथा आँख या इंद्रिय चोरी की ऐसी तार्किक गाथा बुनी कि उसके विश्लेषण-सौंदर्य पर कौन न मुग्ध हो जाय! लेखक के अनुसार गऊचोरी का ही विकसित रूप है भूमि की चोरी, जिसके जनक पटवारी होते हैं। कहावत है कि सोने की चिड़ियाँ को हलाल करने के लिए अँग्रेजों ने ही पटवारी प्रथा चलाई। भूमि चोरी का ही विस्तार है राज्य चोरी। बकौल लेखक ‘पटवारी जो छोटे पैमाने पर हमारे गाँव में करता है, वही विराट पैमाने पर कर रहे हैं बड़े-बड़े स्वनामधन्य राजनीतिज्ञ। काश्मीर और कोरिया को चोरों की छीना-झपटी में श्मशान बना डालने वाली नीति क्या उससे कम श्लाघ्य है? हाँ, दंड दोनों नहीं पाते। पटवारी के पास शासन का कवच है और राजनीतिज्ञ के पास सिद्धांत का कवच है।’ तो इसी भूमि और राज्य चोरी की तरह उसकी अगली कड़ी में है साहित्य की चोरी, जहाँ रचना से लेकर पुस्तक तैयार करने का कुटीर उद्योग चलता है। साहित्य में चोरों के कई वर्ग होते हैं। पहले वर्ग में नवसिखुआ ग्रेजुएट आते हैं जो आदेश मिलने पर अपने हरबा-हथियारों से न जाने कितने वागी-मंदिरों में सेंध लगा-लगाकर माल इकट्ठा कर लेते हैं, जबकि दूसरे वर्ग में श्री हितैषी जी आते हैं जो अपनी अलग प्रतिभा का चमत्कार दिखाते हैं। ये अपनी आलोचना के कुछ बंधे लच्छे यहाँ-वहाँ जोड़ देते हैं और बस साहित्य के आगे ‘कुसुम, सुमन, सौरभी, पराश, चंद्रिका, कमल, प्रकाश, आलोक और किरण जैसा कोई एक शब्द जोड़कर साहित्य के विकास में अभिनव श्रीवृद्धि करने का सुयश कमा लेते हैं।’ साहित्य चोरी का तीसरा वर्ग है प्रकाशक, जो प्रायः इन पहले दो चोरों का भी गला काटने वाले होते हैं। साहित्य चोरी का चौथा वर्ग दलाल और पाँचवाँ वर्ग पाठ्य पुस्तक समिति है। लेखक के अनुसार ‘हाँ, इस गऊचोरी को सभ्य संसार बड़ी आदर दृष्टि से देखता है, जो जितना ही चोरी करता है, वह उतना ही पंडित और विद्वान समझा जाता है। बिना इस चोरी की कला में प्रवीण हुए किसी साहित्यकार को इतिहास में स्थान नहीं मिलता, कारण यह कि तत्कालीन इतिहास को लिखवाने वाले भी इन चोरों के भाई-बंधु ही होते हैं, जो छद्म रूप से इस व्यवसाय को प्रोत्साहन देते हैं, वैसे ही जैसे गाँव की पुलिस, हलका के कानूनगो या अंतरराष्ट्रीय दार्शनिक अपने-अपने क्षेत्रों में चोरियों को बढ़ावा देते हैं।’
पाँचवीं गऊ है आँख या इंद्रिय, जिसकी चोरी युगों-युगों से होती आई है। इस पाँचवीं चोरी की व्यवस्था करने वाले सांसारिक भाषा में ‘चित्तचोर’ कहे जाते हैं। जितने भी गऊचोर हैं, उसमें सबसे सांघातिक चित्तचोर ही माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि ‘बैल चोरी चले जाने पर गरीब की खेती खड़ी हो सकती है, जमीन की चोरी चले जाने पर बेवा की जिंदगी बसर हो सकती है, राज्य छिन जाने पर राष्ट्र जी सकता है और अपनी कृति की चोरी के बाद साहित्यकार में भी प्राण-शक्ति बची रह सकती है, पर चित्त चुरा लिया गया तो प्राण नहीं रहते।’ यह पाँचवीं चोरी सबसे अधिक दुर्दांत होती है, इसलिए लेखक का मानना है कि ‘चार गऊचोरियों को मूर्ख लोगों के लिए छोड़ दिया जा सकता है, पर यह जो पाँचवी सिद्ध चोरी है, उसके लिए कोई देवी-देवता ही पूजना चाहिए और इसके देवी-देवता हैं राधाकृष्ण।’ इस ललित निबंध की रचना इतनी रम्य शैली में हुई है कि उसके प्रवाह में बहते चले जाने का अपना ही आनंद है। पंडित जी के इन ललित निबंधों में विषय-दृष्टि, भाव-भंगिमा और स्वर, इन सबका सहज और प्रौढ़ समन्वय है। भाषा-शैली सहज ग्राह्य है, जिसका जीवंत उदाहरण के रूप में ‘गऊचोरी’ को देखा जाना चाहिए। पंडित जी के निबंध प्रायः संस्मरणात्मक ही होते हैं।
‘साँझ भई’ में जीवन-यौवन की संध्या का व्यंजनामूलक आख्यान है, तो ‘बसंत आवै’ में बिछोह का मधुर क्रंदन। ये दोनों ही निबंध मन की आकुलता को स्मृत्याभास से संतृप्त करते हैं। एक में ‘सर्वे बभूवुस्ते तृर्ष्णी वयांसीव दिनात्यये’ (अर्थात दिन डूबने पर जैसे पंछी शांत हो जाते हैं, वैसे ही सब लोगों ने मौन गह लिया।) का भाव-संसार है, तो दूसरे में ‘प्रीतम मोंहि जो दरसावै’ के दर्शन की कामना ललक के साथ की गई है। इसी तरह ‘जमुना तीरे-तीरे’ में यमुना किनारे फैले करील वन के ब्याज से जीवन में प्रेम के सौंदर्य की व्याप्ति की भाव-तरंगें हैं जो विकट क्षणों में भी मन को सुकून देता है। यमुना तटों पर फैले जीवन के विस्तार में कुछ स्मृतियाँ ऐसी भी हैं जो थकान में भी ताजगी की मधुरता प्रदान करती है और जिससे जीवन का महमह कटूक्तियों को विस्मृत कर देता है; तभी तो लेखक मानता है कि जीवन की ‘इस थकान में भी जमुना के तीरे चलते रहने का अपने आप क्रम बना हुआ है। वह कम नहीं है। यों तो अपने नसीब के नाम पर कल्पना करना मानव स्वभाव है, उसके लिए मैं क्या करुँ?’ व्यंजना ब्याज से यह निबंध संताप को सुकून में बदलता है, मसलन लेखक का यह कहना कि ‘सुना है कि यमुना और यमराज में भाई-बहन का नाता है, शुभ-अशुभ और विधि-निषेध की थप्-थप्, इसलिए इस धारा में एक क्षण भी बंद नहीं होती, भाई इनके लेखा-जोखा के ठेकेदार जो ठहरे!’
पुस्तक में ‘टिकोरा’, ‘होरहा’, ‘घने नीम तरु तले’ जैसे निबंध भी हैं, जो स्वच्छंद मन के प्रकृति-संस्कृति विचरण की शृंगार गाथा बताते हैं। टिकोरे का शृंगार और होरहा के स्वाद पर किसका मन न मचल उठे, ऐसी मादकता इन निबंधों में है। ‘काँची अमिया न तुरिहऽ बलमु काँची अमिया’ जैसे पूरबी गीत के बोल से मन के तार रसाल कानन की किन स्मृति-वीथिकाओं से जुड़ जाए, कोई नहीं जानता। लेखक का मन उसमें रचा-बसा, इसलिए ‘कानन जोगू’ पंडित जी के लिए ‘यह नए वर्ष का उदय है और मधुमास का चरम उत्कर्ष’ भी। टिकोरे ऋतु-संस्कृति के जागने का पर्व है पंडित जी के लिए, इसलिए देसी संस्कृति की धूम में उनका क्लांत मन भी खिल उठता है। होरहा की सुगंध भी ऐसी ही होती है। होली के साथ ही होरहा का भी समय शुरू होता है, जब डंठल-पत्ती समेत बूट को भूनकर और छील-छालकर नए अधपके चने का बिना नमक-मिर्च के आस्वादन के साथ होरी-होरहा की संगति पूरे गाँव को मदमस्त कर देती है। लेखक ने इसका बड़ा रमणीय चित्रण किया है। गाँव में नीम, महुवा आदि के पेड़ अपने नैसर्गिक सौंदर्य से लोगों को लुभाते हैं। पंडित जी का मन भी नीम पर फिदा रहता है। क्यों भला! ‘अब सोचिये, नीम में क्या मिलता है, गंध असह्य, स्वाद असह्य, यहाँ तक कि कुसुमित नीम का रूप भी असह्य, चारों ओर सफेद बुंदियाँ छिटकी हुई, पत्तियाँ इतनी दूर-दूर कटी-कटी कि पेड़ की जड़ बिचारी ओट के लिए तरसती रहती है। इसलिए आम में फसल न आए, महुवे में कूँचे न लगे, गुलाब में कली न आए और मधुमास सूना चला जाए, पर नीम बराबर फूलेगा, बराबर फरेगा और इतना फरेगा कि अकुला देगा, इतना बेशर्म कि वह कट जाने पर भी इसकी लकड़ी में घुन न फटकेगा। यदि कहीं नीम की शहतीर लग गई हो तो वर्षा होते ही जो आकूल दुर्गंधि व्याप्ति है तो प्राण औंतियापात हो उठते हैं। पर हाय रे नियति का विधान कि घर-घर बिना जतन सेवा के नीम धरती की छाती का स्नेह छीन कर खड़ा मिलेगा।’
पंडित जी के नीम प्रेम के कई कारण हैं। उनमें एक कारण है ‘नीम तो सुनता हूँ लगता भर तीता है, पर अपने परिणाम में मधुर होता है, पर इसके प्रतिरूप मानव जगत का सप्ततिक्त तो आदि से अंत तक एकरस है’ ब्याजस्तुति भाव से ‘नीम की वंदना’ करते हुए लेखक मानता है कि इस कडुवी दुनिया का ईलाज नीम के पास ही है। एक अन्य निबंध ‘धनवा पियर भइलें मनवा पियर भइले’ में खाद्य समस्या के ब्याज से राजनीति और साहित्य की विरूपता पर टिप्पणी की गई है। देश में ग्रामों का विकास हुआ नहीं, क्योंकि ग्राम के देवता पाँच-पाँच सालों पर ही ग्राम की फेरी लगाते हैं। ऐसे में ‘हंस पानी छोड़ देता है, उच्च वर्गीय साहित्यकार भी नीरस पानी साधारण लोगों के लिए छोड़ देता है, सरोवर के कमलों पर जीने वाला हंस इतनी दया तो दिखाता है; परंतु आकाश के मेघ और धरती के ‘परजन्य’ जनता के शासक तो धरती का मधु उगाहकर और धरती का दूध उगाहकर पानी का एक बूँद भी नहीं देना चाहते। वे अपना संचित संभार निभृत कोनों में चोरी-चोरी लुटाते रहते हैं। इसी में उसकी ‘परजन्यता’ सिद्ध होती है। धान पियराये या मन पियराये, इससे उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। उसके आसपास मोर नाचते रहते हैं, वे उसी में आत्मविभोर रहते हैं, उन्हें कुररी का विलाप सुनाई नहीं पड़ता।’ ग्राम्य जीवन का रूप तत्त्व कोई हो, उसके प्रति वाह्य संसार का प्रतिकूल रूख लेखक के मन को पीड़ित करता है, जिससे लोकपक्ष की संस्कृति की संरक्षा में वह सन्नद्ध हो जाता है। प्रकृति ग्राम की हो, लोक की, रितु की, पर्व की, संस्कृति की या फिर जन सामान्य की, सबकी संरक्षा एवं समृद्धि से ही लेखक ऊर्जा ग्रहण करता है, क्योंकि उसी की छाँह में वह पल्लवित-पुष्पित हुआ। अपने एक निबंध ‘साँची कहौं व्रजराज तुम्हें रतिराज किधौ रितुराज कियौ है’ में लेखक रति, रितु और रितुराज के अंतर्संबंधों पर अपने भाव विस्तार के क्रम में निष्कर्षतः लिखता है कि ‘वसंत और कला के बीच कौन-सा संबंध हो और उसका स्वरूप कैसा हो, इसका विचार करने के लिए भी कला के ऐसे विकास की आवश्यकता है जो वसंत की कृपा दान मात्र पर अवलंबित न होकर अपने वितान से वसंत को भी छतनार बनाने की क्षमता रखता हो, अन्यथा बसंत की इतरान में कला विहँस न सकेगी, वह नीचे दुबकी रहेगी और संस्कृति का प्रवाह रुद्ध हो जाएगा; वह कुर्द हो जाएगा, जहाँ से उबरने का कोई मार्ग न रहेगा।’
‘वसंत न आवै’, ‘चंद्रमा मनसो जातः’, ‘प्यारे हरिचंद की कहानी रहि जाएगी’, ‘सखा धर्ममय अस रथ जाके’, ‘दिया टिमटिमा रहा है’, ‘तांडवं देवि भूयादभीष्ट्यै च नः’ जैसे चारू निबंधों में भी रितु, रीति, रति, पर्व, धर्म आदि के सौंदर्य के ब्याज से सामाजिक सरोकार का प्रति संसार रचा गया है। धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक जीवन मूल्यों का प्रवाह ऐसे ही प्रीति संसार से प्रवाहित होता है। अपने निबंधों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की भाव परंपरा को समृद्ध करने वाले पंडित विद्यानिवास मिश्र विषय-विस्तार की रागात्मक स्वच्छंदता की ऐसी सांस्कृतिकता की गाथा रचते हैं, जो अनूठी ललित शैली से सम्मोहित कर लेती है। पंडित जी प्रायः संस्मरणात्मक शैली में ही निबंध रचते हैं, जिसमें ग्रामीण संस्कृति के भी दर्शन हो जाते हैं और उनकी शैली से एक प्रकार की आत्मीयता उत्पन्न हो जाती है। उनके निबंधों में कहीं भी पांडित्य प्रदर्शन नहीं, बल्कि उसके स्पर्श से वर्ण्य विषय सामाजार्थिक पक्ष ही विश्लेषित होते हैं, जो पाठकों के दृष्टिकोण को उन्नत ही करते हैं। नगण्य से नगण्य विषय भी उनकी अनूठी शैली से जीवंत हो उठते हैं, क्योंकि उनके निबंधों में भाषा-भूगोल की लोक संस्कृति पाठकों से बोलती-बतियाती नजर आने लगती है।
ललित निबंध में प्रायः शैली को ही प्रमुखता दी जाती है, इतना कि कभी-कभी वर्ण्य विषय पर शैली तन कर खड़ी हो जाती है। इससे उसका चमत्कार तो प्रभावित करता है, किंतु विषय का सौष्ठव क्षीण पड़ जाता है। पंडित विद्यानिवास मिश्र के निबंधों में शैली, भाषा, शिल्प आदि का शृंगार तो है, पर विषय का सौंदर्य चमक उठने तक ही। आलोचकों का ध्यान इनकी अनूठी शैली के चमत्कार की ओर ही अधिक गया है। ‘छितवन की छाँह’ के ‘आभार’ में पंडित जी ने लिखा भी है ‘शैली को मैं साधन मानता हूँ, साध्य नहीं।’ इसी तरह अपनी निबंध-भाषा के बारे में भी उन्होंने स्पष्ट किया है कि ‘संस्कृत में जमकर अँग्रेजी का स्तन्यपान किया है, पर मुझे छाँव मिली है भोजपुरी के धानी आँचर में, सो इनसे मेरा अविलग भाव है।’ इसी तरह अपने निबंध लेखन के प्रेरक स्रोतों का स्मरण करते हुए उन्होंने लिखा है कि ‘निबंध कला में मुझे सबसे अधिक प्रेरणा दो फक्कड़ों से मिली है, वे हैं भैया साहब पंडित श्रीनारायण चतुर्वेदी और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी।’ यही नहीं, अपने भाषा एवं साहित्य संस्कार के गठन में प्रेरक स्रोतों का उल्लेख करते हुए पंडित जी कहते हैं कि ‘संस्कृत के पठन-पाठन की ही मेरे कुल में परंपरा रही है पर मैं रुद्री के ‘गणनांत्वा’ के आगे न जा सका और ए.बी.सी.डी. लिखने लगा। यूनिवर्सिटी में पहुँचते-पहुँचते संस्कृत अध्ययन की ओर मेरा प्रत्यावर्तन हुआ और तभी एक ओर राबर्ट लुई, स्टीवेंसन, टामस डिक्वेंसी, चार्ल्स लैम्ब और स्विफ्ट की कलमनवीसी से प्रभावित हुआ। दूसरी ओर वाणभट्ट, भवभूति एवं अभिनव गुप्त पादाचार्य की भाषा-शक्ति का भक्त बना। मेरी तबीयत भी गुलेरी, पूर्ण सिंह, माधव मिश्र और बालमुकुंद गुप्त की डगर पर चलने के लिए मचलने लगी और कागद-स्याही का मैंने काफी दुरुपयोग किया भी। भाषाडंबर के पचीसों ठाठ बाँधे और उधेड़ दिए। …साहित्य का अधकचरा अध्ययन, मित्रों का प्रोत्साहन, पूरबी का स्नेहांचल-वीजन और अपना बेकार जीवन, मेरे मध्यवित्तीय निबंधों को यही दाय मिला है।’ इन समस्त तथ्यों से पंडित विद्यानिवास मिश्र के साहित्य-जीवन का गठन ही नहीं, उनके ललित निबंधों के रचाव का भी बोध होता है।
14 जनवरी, 1926 ई. की गोरखपुर (उ.प्र.) के एक गाँव पकड़ीडीहा में जन्में पंडित विद्यानिवास मिश्र का निबंध लेखन 1956 ई. से ही आरंभ हो गया था, लेकिन उनके पहले ललित निबंधों का संग्रह ‘छितवन की छाँह’ 1976 ई. में प्रकाशित हुआ। इस संग्रह के निबंधों पर स्वाभाविक रूप में संस्कृत का प्रभाव अधिक है किंतु इससे रसोत्पादन में कहीं बाधा खड़ी नहीं होती। किसानी जीवन और कारीगरी संस्कृति की अंत:सलिला जीवनधारा को फिर से अपने निबंधों द्वारा प्रतिष्ठापित करने में उन्हें अद्भुत सफलता मिली। कहना चाहिए कि उनके ललित निबंध का लोकतंत्र भारतीय समाज के किसानी-कारीगरी संस्कृति के पल्लवन से ही ऊर्जा ग्रहण करता है और जिसमें सामान्य जन के लिए करुणा, न्याय और प्रतिरोध का संग्राम है। लोकरंगों से अपने ललित निबंधों में आत्मीयता का सघन भाव उत्पन्न करने वाले चितेरा लेखक पंडित विद्यानिवास मिश्र का आकस्मिक निधन 14 फरवरी, 2005 ई. को एक कार दुर्घटना में क्या हुआ, मानो ललित निबंध से ‘ललित’ फुर्र हो गया!