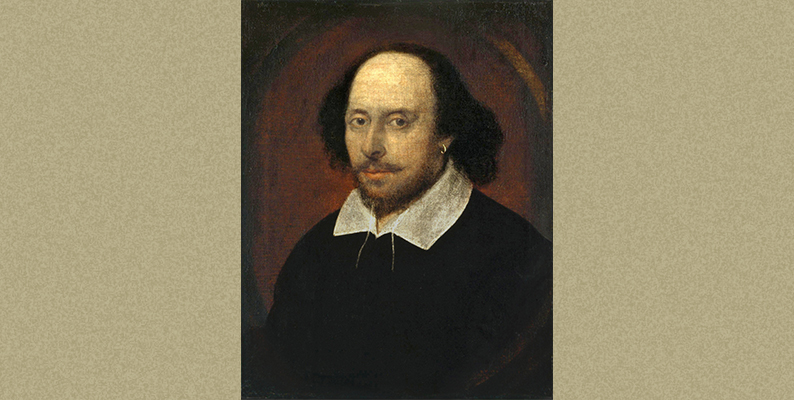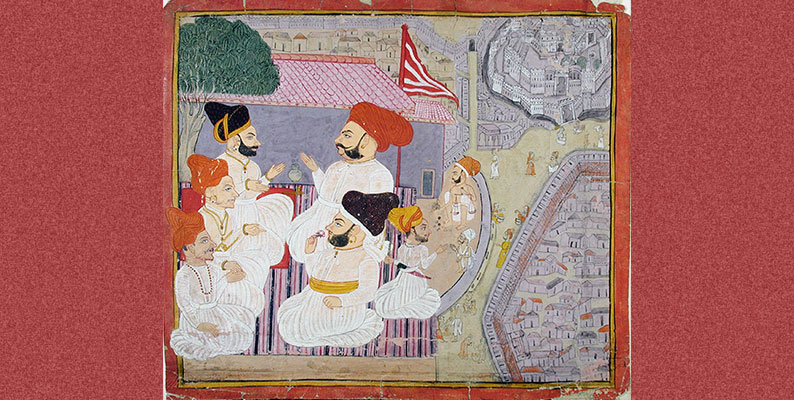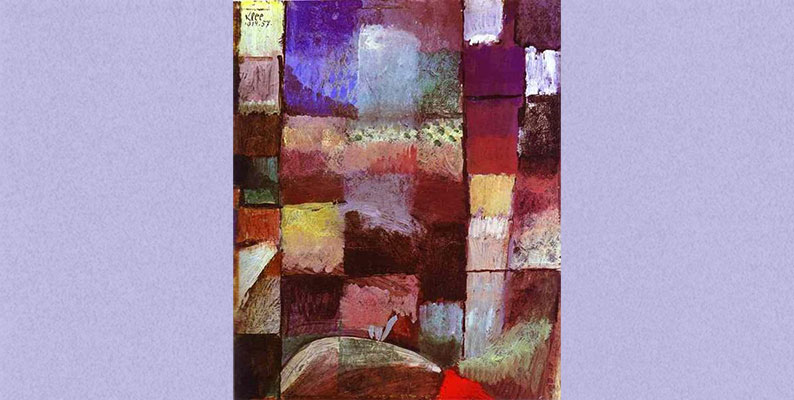पत्रकार या मजदूर!
- 1 January, 1954
शेयर करे close
शेयर करे close

शेयर करे close
- 1 January, 1954
पत्रकार या मजदूर!
पत्रकारों पर मजदूरों के लिए बनाए गए कानून लागू हैं या नहीं, यह एक प्रश्न उठा है। मजदूरों के लिए जो कानून बने हैं, वे उन्हें कुछ सुरक्षाएँ और सुविधाएँ देते हैं–वे बिना कारण के हटाए नहीं जा सकते, ऐसा करने पर उनकी क्षतिपूर्ति करनी पड़ेगी, उनके वेतन और तरक्की के बारे में भी कुछ निश्चितता लानी होगी, उनके रहने-सहने के संबंध में कुछ खास व्यवस्थाएँ करनी होंगी, आदि आदि! आज का पत्रकार इन सुरक्षाओं और सुविधाओं से वंचित है। अत: वह चाहता है, उसे भी मजदूरों के लिए बनाए गए कानून के दायरे में ले लिया जाए। किंतु उसके कुछ ऐसे भाईबंद भी हैं, जो अपने को मजदूर समझे जाने में अपनी तौहीनी समझते हैं। कहाँ समाज का नेता, संसार का ज्ञानदाता बनने का दावा और कहाँ अपने को मजदूर कहलवाने के लिए हो-हल्ला! अत: वे इस आंदोलन का विरोध कर रहे हैं। सुरक्षा के लिए वे भी कानून चाहते हैं, किंतु ज़रा अपने पद के अनुरूप। वे चाहते हैं मीठा भी हो, मुरमुर भी हो! ऐसे लोगों में विशेषत: प्रधान संपादकों का दल है, जिन्हें अच्छे वेतन मिलते हैं, जिनकी अखबार-मालिकों से अच्छी साँठगाँठ रहती है। इसी तरह पत्रकारों के अपने ही घर में द्वंद्व चल रहा है। जिनसे यथार्थ झगड़ा है, यानी अखबार-मालिक, वे तो अलग बैठे हैं–यहाँ ‘राड़-सी मची है नटराज के तबेले में!’ भाँग के नसे में शंकर सोये हैं, साँप फुँकार रहे हैं, एक-दूसरे को निगलने को व्याकुल हैं! एक ऐसा मामला अभी हाईकोर्ट में आया था। एक पत्रकार को तंग किया जाने लगा, उसने मुकद्दमा दायर किया, हाइकोर्ट से वह मुकद्दमा हार गया। फिर क्या था, प्रधान संपादक ने इसमें अपनी विजय समझी। एक पूरी पुस्तक ही निकाल दी गई! अब उस पत्रकार ने संपादक महोदय पर मानहानि की नालिश ठोक दी है। इस मुकद्दमे का क्या हश्र होगा, कौन जीतता है, कौन हारता है,–सब कुछ विचाराधीन है। किंतु जो कोई भी पत्रकारिता से संबंध रखता है, उसके लिए यह अजीब दृश्य है कि पत्रकार-पत्रकार के बीच ही कुश्ती मची हो!
पक्ष और विपक्ष में!
बहुत से देशों में पत्रकारों को मजदूर-कानून के दायरे में मान लिया गया है। मजदूर वह है जो एक निश्चित रकम के पारिश्रमिक पर, दूसरे के औजार पर दूसरे के लिए, मेहनत करता है! उसका अधिकार न तो उस औजार पर होता है और न उसके नफा-नुकसान से ही उसका कुछ लेना-पावना होता है। आज का पत्रकार भी तो ऐसा ही है। न प्रेस पर उसका अधिकार, न हानि-लाभ से उसका सरोकार। निश्चित वेतन पर वह खटता है। अत: वह मजदूर नहीं तो क्या है? रही पद-मर्यादा की बात! सो, जब पेट में भूख खाँव-खाँव कर रही हो, तो पद-मर्यादा को लेकर कोई चाटेगा? यदि आज पत्रकार अपनी पद-मर्यादा भूल कर अपने को मजदूर कहलाने के लिए आगे बढ़ता है, तो इसके दोषी वे लोग हैं, जिन्होंने उसे ऐसी स्थिति में ला दिया है। किंतु, दूसरी ओर से तर्क पेश किया जाता है, कारखाने के मैनेजरों या इंजीनियरों की शुमार मजदूरों में नहीं की जाती, फिर पत्रकारों को क्यों उस श्रेणी में लिया जाए? कंपोजीटर, प्रेसमैन आदि ही उस श्रेणी में लिए जा सकते हैं! एक तीसरा दल ऐसा है, जो चाहता है, पत्रकारों के लिए एक अलग कानून ही बनाया जाए। यह दल मानता है कि पत्रकारों पर जुल्म होते हैं, उनकी रक्षा की जानी चाहिए, किंतु उन्हें मजदूर की सतह पर नहीं उतारना चाहिए। भारत-सरकार ने जो प्रेस कमीशन बनाई है, वह इन बातों पर भी ग़ौर करेगी। देखना है, वह किस निर्णय पर पहुँचती है। निस्संदेह यह प्रश्न इस समय एक ज्वलंत प्रश्न हो गया है और अतिशीघ्र इसका समाधान खोजना ही पड़ेगा! कुछ अखबारों के मालिकों ने ऐसी स्थिति ला दी है कि इसे अब अधिक दिनों के लिए टाला नहीं जा सकता।
लेखक और आलोचक!
असफल लेखक ही आलोचक बन जाता है, जिन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने ऐसा मान लिया कि आलोचक लेखक नहीं है। आलोचक स्वयं लेखक है और यदि लेखक से मतलब स्वतंत्र रचनाकार से है, तो यह भी दावे के साथ कहा जा सकता है कि आलोचना भी एक प्रकार की स्वतंत्र रचना है! यों ऐसा लेखक भी हो सकता है जो स्वतंत्र रचना के नाम पर साहित्यिक उठाईगिरी करता हो और ऐसे आलोचकों की भी कमी नहीं कि जिनकी आलोचना का मूलोद्देश्य झूठी प्रशंसा या द्वेषपूर्ण निंदा है। न तो वह लेखक है और न ऐसे लोगों को आलोचक कहा जाना चाहिए। हाँ, हिंदी के लिए यह दुर्भाग्य की बात है कि उसमें ऐसे आलोचकों की कमी है, जो ऐसी चीजें प्रस्तुत करते हों, जिन्हें स्वतंत्र रचना कहलाने का गौरव प्राप्त हो सके। जबसे कॉलेजों में हिंदी-साहित्य की पढ़ाई बढ़ी है, तब से आलोचकों की संख्या बहुत बढ़ गई है। प्रश्न-पत्रों के उत्तर के लिए कॉलेज के विद्यार्थी सस्ती और कामचलाऊ आलोचना-पुस्तकों पर टूटते हैं। अभी उस दिन एक ऐसे सज्जन से भेंट हुई जिनकी रचना-प्रतिभा के हम सदा कायल रहे हैं। उन्होंने बताया, एक तो कॉलेज में पढ़ाने से उन्हें फुर्सत नहीं मिलती; दूसरे स्वतंत्र निबंध या कहानी लिखने की अपेक्षा आलोचना लिखना आसान पड़ता है और वह तुरंत पैसे भी दिलाता है! पत्र-पत्रिकाओं के संपादकों का भी अनुभव है कि धीरे-धीरे स्वतंत्र रचनाकारों की संख्या घटती जा रही है और आलोचकों की संख्या में बेहद वृद्धि हो रही है! कभी यह हिसाब लगाया जाए कि प्रसाद, प्रेमचंद या पंत, महादेवी की पुस्तकों की कितनी बिक्री हुई या हो रही है और उनकी पुस्तकों पर लिखी उलूल-जलूल आलोचना-पुस्तकों की कितनी, तो अचरज ज़रूर होगा! यह स्थिति अवश्य ही चिंतनीय है। सबसे बुरी स्थिति आलोचना में यह आई है कि आलोचकों के अपने-अपने गुट हैं और जब कभी वे आलोचना लिखने लगते हैं, अपने उस दायरे से वे बाहर झाँकने का कष्ट नहीं उठाते। यह प्रवृत्ति बड़े-बड़े आलोचकों में भी देखी गई है। नतीजा यह है कि जो लोग उनके गुट से अलग हैं, कितनी भी अच्छी चीज क्यों न लिखें, उनका नामोल्लेख भी नहीं किया जाएगा। यदि कोई ऐसा आलोचक पाठ्य-पुस्तकों का निर्णायक भी बन गया, तब तो महान अनर्थ हो जाता है! वह कितने लेखकों के भाग्य का ही वारा-न्यारा नहीं कर देता; विद्यार्थियों को साहित्य का एकांगी ज्ञान प्राप्त करने को बाध्य करके उनके साथ भी महा अन्याय करता है। हम चाहते हैं, हमारे समर्थ साहित्य-महारथियों का ध्यान इस ओर अवश्य आकृष्ट होना चाहिए।
नाटक और अभिनेता!
हिंदी में नाटकों की कमी है या अभिनेताओं की? नाटक का अर्थ ही होता है कि उसका अभिनय हो। जो नाटक अभिनय योग्य नहीं, उसे नाटक ही क्यों कहा जाए? लेखक अपनी किसी पुस्तक पर, जिसमें उसने वार्तालाप को माध्यम अपनाया है, नाटक लिख देता है और हम भी मान लेते हैं, वह नाटक है! यह गलत बात है। तब तो सुकरात के सारे वार्तालाप नाटक बन जायँगे? नाटक के लिए यह आवश्यक शर्त है कि उसे रंगमंच पर उतारा जा सके। किंतु, इसके लिए भी एक शर्त है कि इसके लिए योग्य अभिनेता उपलब्ध हों। नाटक ऊँचाई पर जा नहीं सकता, जब तक कि ऊँचे दर्जे के अभिनेता नहीं मिलें। इधर देश में जो सांस्कृतिक जागरण आया है, अब नाटकों की ओर लोगों का ध्यान बढ़ता जा रहा है। इस सिनेमा के युग में भी पृथ्वीराज के नाटकों को देखने के लिए भीड़ बनी रहती है! किंतु, क्या यह सचमुच दुर्भाग्य की बात नहीं है कि अब तक किसी साहित्यिक नाटक को पृथ्वीराज द्वारा अभिनीत होने का सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ? यह नहीं कि वह ऐसा नहीं चाहते हैं, किंतु उनका क्षोभ यह है कि हिंदी के ऐसे नाटक उन्हें मिले नहीं! अत: उन्हें स्वयं नाटक लिखवाना पड़ता है, जो अभिनय की दृष्टि से बहुत ही अच्छे होते हैं, किंतु साहित्यिक दृष्टि से उनकी कोई क़ीमत ही नहीं है। यह तो पृथ्वीराज का जादू है जो उन नाटकों को चमका देता है! लेकिन, हमारा ध्यान सिर्फ पृथ्वीराज पर नहीं है। पृथ्वीराज तो देश में एक ही हैं। परंतु, अब तो गाँव-गाँव में लोग नाटक खेलने का आयोजन करने लगे हैं। क्या हम उनके योग्य भी नाटक लिख पाए हैं? वे प्राय: बँगला नाटकों के अनुवाद पर टूटते हैं या पारसी-थियेटर के तर्ज पर लिखे गए बाजारू नाटकों पर! इसमें दोष सिर्फ उनका ही नहीं है, हमारा भी है। जब कभी कोई उत्साही संस्था साहित्यिक नाटकों को लेती है, कमाल कर दिखलाती है। अभी उस दिन आर्यकन्या-विद्यालय की लड़कियों ने ‘अंबपाली’ का इतना सफल अभिनय किया कि श्री जगदीशचंद्र माथुर ऐसे नाटक और अभिनय के पारखी मुग्ध हो रहे! लड़कियों के इस उत्साह को देखकर माथुर साहब ने माना कि हिंदी रंगमंच के सुनहले दिन आ रहे हैं! वह दिन निकटतम हो सके, इसके लिए आवश्यक है कि हर नाटककार नाटक लिखते समय अभिनेता की कठिनाई पर भी ध्यान रखे! जब तक अच्छे नाटक अच्छे अभिनेता के हाथ में नहीं आवेंगे, दोनों का स्वर्ण-संयोग नहीं होगा, हिंदी का नाटक-साहित्य पिछड़ा ही रहेगा!
कूप-जल या बहता नीर!
डॉक्टर बलदेवप्रसाद मिश्र मध्यप्रदेश के एक ऐसे रत्न हैं जिनपर हिंदी को अभिमान होना चाहिए। अभी उन्होंने एक लेख में राष्ट्रभाषा हिंदी के रूप पर विचार प्रगट किया है। उनका कहना है, जनसाधारण जिसे चला दे, वही भाषा है, वह विशेषज्ञों की समिति में गढ़ी नहीं जा सकती, यदि गढ़ भी लीजिए, तो उसे आप चला नहीं पायँगे। भाषा ‘कूप-जल’ नहीं, वह तो ‘बहता नीर’ है। आपने बतलाया है, ‘हिंदोस्तानी’ नाम से जो चीज गढ़ी गई, वह चल नहीं पाई। क्यों? राजबल ही नहीं, राष्ट्रपिता की सारी शक्ति भी उसके साथ थी। लेकिन ‘हिंदोस्तानी’ तो मरी, वह एक नई प्रतिक्रिया छोड़ गई। अब लोगों ने संस्कृत पर ज्यादा जोर देना शुरू कर दिया है और उसके आधार पर नए-नए शब्द गढ़े जा रहे हैं। किंतु, क्या ये शब्द चल पाएँगे? मिश्र जी की राय है, हिंदी केवल संस्कृत के व्याकरण अथवा संस्कृत के कोश का आधार लेकर नहीं चली है। वह देशज एवं द्रविड़ भाषाओं से भी प्रभावित है, अत: यह वास्तविक रूप में राष्ट्रभाषा है। यों जो लोग उसे संस्कृत के कोल्हू में बाँधना चाहते हैं, वे उसके इस व्यापक रूप को नष्ट करना चाहते हैं! यह भाषा तो चलेगी नहीं ही; हिंदी के लिए महा अनर्थ कर जाएगी। इन पंक्तियों का लेखक उस दिन एक जिला-बोर्ड के दफ्तर में गया था। उसके हेड कर्ल्क ने बताया, उसे रघुवीरी कोश के आधार पर ही सूचनाएँ निकालने को बाध्य किया जाता है, जहाँ ‘नीलाम’ ऐसे आम फहम शब्द के लिए ऐसा संस्कृत शब्द रख दिया गया है कि बार-बार वह याद करना चाहता है, किंतु याद रख नहीं पाता! क्या यह हिंदी के साथ खेलवाड़ नहीं है? मिश्र जी की यह चेतावनी हिंदी-संसार को सदा स्मरण रखनी है–“बहते नीर की धारा को एकदम उलटना असंभव कार्य है। उसकी विशिष्ट प्रकृति उसी की होकर रहेगी। उसके बहाव की प्रवृत्ति को नहीं पहचानना उसके वास्तविक लाभ से अपने को वंचित रखना है। चतुर किसान वही है जो उसकी विशिष्ट शक्ति और उसके बहाव का विचार रखता हुआ, उसका यत्रतत्र संशोधन करता जाता है जिससे वह विविध क्षेत्रों को अच्छी तरह हरा-भरा करती चले।”
रघुवीरी कोश को दफनाओ!
यह प्रसन्नता की बात है कि रघुवीरी कोश की निरर्थकता के विरोध में वहीं से आवाज उठ रही है, जहाँ उसका जन्म हुआ! हम स्पष्ट कहना चाहते हैं, मध्यप्रदेश की सरकार ने अपने हिंदी-प्रेम के झोंके में एक ऐसे अनर्थ का बीज बोया है, चिसका कड़वा फल एक दिन हिंदी को बुरी तरह भोगना पड़ेगा। चूँकि एक सरकार की मातहत वह कोश तैयार किया गया, अत: स्वभावत: ही प्रादेशिक सरकारें उसे प्रामाणिक मान कर उसी के आधार पर अपने कामकाज चलाने की कोशिश कर रही हैं। इस तरह सारे देश में एक अजीब सरकारी भाषा की सृष्टि होती जा रही है। अब समय आ गया है कि हम मध्यप्रदेश की सरकार से साग्रह निवेदन करें कि वह इस कोश को वापस कर ले, उसे रद्द किए जाने की घोषणा करे। श्री राहुल जी की देखरेख में हिंदी-साहित्य-सम्मेलन ने एक राजनीतिक कोश तैयार कराया है, वह इस कोश से कहीं उत्तम है! जब तक कोई सर्वसम्मत कोश तैयार नहीं हो जाता; तब तक उनके इस कोश से ही काम चालाना चाहिए। रघुवीरी कोश जितना जल्द दफना दिया जाए, उतना ही अधिक हिंदी का कल्याण होगा।
Image: Wood seller and his wife – Sivites (Saivites), leaf from Bound Collection of 20 Miniatures Depicting Village Life
Image Source: Wikimedia Commons
Image in Public Domain