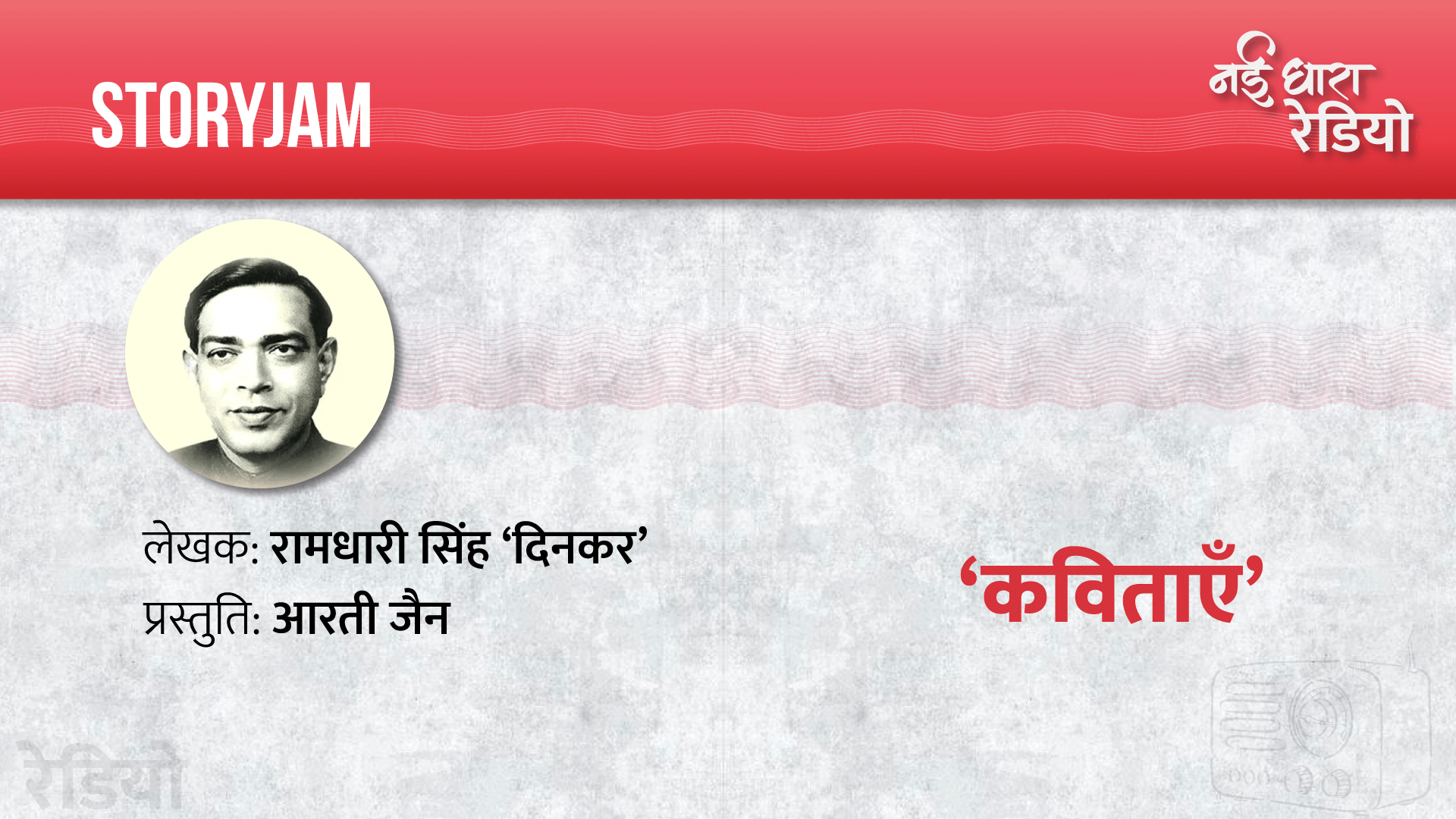भारतीय गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति
- 1 April, 1950
शेयर करे close
शेयर करे close

शेयर करे close
- 1 April, 1950
भारतीय गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति
“मैं हिंदी-साहित्य सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन में ही सम्मिलित हुआ था। यही नहीं, बल्कि हिंदी-साहित्य-सम्मलेन जैसी कोई संस्था कायम की जाए, इसके लिए मैंने थोड़ा-बहुत आंदोलन भी चलाया था और इसके लिए पत्रों में लेख भी लिखे थे।”
बिहार में हमारी पीढ़ी के लोग भारतीय गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति देशरत्न डॉ. राजेंद्र प्रसाद जी के सुयश की कहानियाँ सुनते-सुनते पले और बढ़कर जवान हुए हैं। प्रांत के जीवन पर ज्यों-ज्यों वे छाते गए, त्यों-त्यों उनकी छाया हम सभी लोगों की जिंदगी पर पड़ती गई और हम सभी लोग मन की निर्मलता के समय छोटे-छोटे राजेंद्र प्रसाद बनने की कामना से उद्वेलित रहे हैं। व्यवहार में मनुष्य क्या बन पाता है, सबसे बड़ी बात तो यही है; किंतु, मन की कामना भी विशेषता रखती है; क्योंकि यह कामना हमारे जीवन की दिशा निर्धारित करती है तथा हमें व्यक्ति विशेष का अनुगमन करने को भी प्रेरित करती है। पहले राजेंद्र बाबू हमारे मनों में आए और तब उन्होंने हमें अपने पीछे लगा लिया। फिर बहुत-सी जिज्ञासाओं का समाधान भी हमें उनके व्यक्तित्व में मिला। देशभक्त कैसा होता है? मन ने कहा, राजेंद्र प्रसाद के समान। गाँधीजी का अनुसरण कैसे करना चाहिए? आँखों ने कहा–जैसे राजेंद्र प्रसाद कर रहे हैं। एक यह भी शंका थी कि उस युग में उच्च से उच्च कोटि की बौद्धिकता को लेकर भी निपट देहातियों के बीच अपने को कैसे खपाया जा सकता है? उस विचित्र शंका का भी उचित समाधान हमें राजेंद्र बाबू के ही व्यक्तित्व में मिला। अब तो श्रद्धा इतनी घनी हो गई है कि लोग उनका नाम न लेकर उन्हें सिर्फ ‘बाबू’ कहकर पुकारते हैं। बाबू के सान्निध्य में मैं प्रथम-प्रथम सन् 1935 में आया जिस साल बाबू भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। उसी दिन मैंने उन्हें अपनी कविताएँ भी सुनाईं। मैंने देखा कि कविताओं की कई कंडिकाएँ सुनते उनकी आत्मा आंदोलित हो गई और उनकी आँखों से आँसू निकल आए। अवश्य ही, यह विचलन कविता की बेधकता की अपेक्षा उनकी देशभक्ति-संबंधी स्वानुभूति का ही परिणाम रहा होगा, किंतु जिस आदर और मनोयोग के साथ उन्होंने मेरी तुकबंदी को सुना, उससे मुझे बड़ा ही उत्साह मिला और तब से मैं बराबर, अवसर मिलने पर, उन्हें अपनी रचनाएँ सुनाता रहा हूँ।
बाबू के साहित्यिक व्यक्तित्व से लिपटने का एक कारण यह भी था कि हिंदी-प्रांतों के चोटी के राजनीतिज्ञों में टंडनजी को छोड़कर वे ही एक ऐसे राजनीतिज्ञ थे जो हिंदी भाषा और साहित्य की उन्नति और विकास को देश के सर्वांगीण विकास से मिलाकर देखते थे और जिन्हें यह जानने की इच्छा थी कि हिंदी में कहाँ क्या हो रहा है? उनका साहित्यानुराग केवल अखिल-भारतीय हिंदी-साहित्य-सम्मलेन अथवा प्रांतीय सम्मेलनों के सभापतित्व तक ही सीमित नहीं रहा है, बल्कि वे लेखकों और कवियों के वैयक्तिक संपर्क में भी रहे हैं और जब तब उन्होंने सभा-सम्मेलनों का भी साथ दिया है।
कहते हैं, सर तेज बहादुर सप्रू और जस्टिस सुलेमान–जैसे बड़े आदमी भी जब मुशायरों में जाते थे, तब वे वहाँ काफी देर तक बैठकर कविताओं का रस लेते थे और इस प्रकार आयोजकों को यह महसूस करने का मौका देते थे कि वे जिस काम को कर रहे हैं वह बड़ा ही ऊँचा सांस्कृतिक काम है। किंतु, लगभग चार सौ साहित्य-सम्मेलनों और कवि-सम्मेलनों में भाग लेने के बाद भी दुर्भाग्यवश मैं यह नहीं कह सकता कि हिंदी-प्रांतों के तगड़े लोग साहित्य या कवि सम्मेलनों के सांस्कृतिक महत्त्व से जरा भी प्रभावित हैं अथवा उन्होंने कभी भी व्यक्तित्व के आलोक से साहित्य-सम्मेलनों की शोभा बढ़ाई है। हाँ, पूज्यवर राजेंद्र बाबू इसके अपवाद जरूर हैं, क्योंकि उन्हें मैंने साहित्य-सम्मलेन ही नहीं, कवि-सम्मेलनों में भी यदा कदा सम्मिलित होते देखा है और वे जब भी वहाँ गए हैं, उन्होंने सभी तरह के कवियों की रचनाओं को एक समान धीरता और मनोयोग से सुना है।
हिंदी में राजनीति और साहित्य के बीच एक खाई है जो दिन-दिन चौड़ी होती जा रही है। राजनीति के लोग साहित्य को उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं, मानों यह कोई चीज़ ही नहीं हो, मानों साहित्य की उपेक्षा से उनका या देश का नुकसान नहीं होता हो! किंतु, साहित्य बलवान् तो है ही, और उसके झरने में पानी पीना अगर आपके लिए ग्लानि की बात है, तो इसका यह अर्थ नहीं है कि उसका पानी सड़ रहा है और लोग उसे पी नहीं रहे हैं।
राजेंद्र बाबू की यह एक बहुत बड़ी विशेषता है कि वे साहित्य-रचना को भी देश के नवनिर्माण का अंग मानते हैं और साहित्यिकों को समुचित आदर देकर वे साहित्य के प्रति अपनी आस्था प्रकट करते हैं। अन्य नेताओं के समान अंग्रेजी के प्रगाढ़ पंडित होते हुए भी वे आरंभ से ही हिंदी के प्रबल समर्थक और अनुरागी रहे हैं। आज से कोई तीस वर्ष पूर्व उन्होंने पटना में ‘देश’ नामक हिंदी साप्ताहिक की स्थापना की थी और तब से भाषा के प्रश्न पर सुझाव देकर, साहित्य-सम्मेलनों का सभापतित्व करके तथा ग्रंथों की रचना के द्वारा वे हिंदी भाषा और साहित्य की सेवा करते ही आ रहे हैं। उनकी लिखी–1. ‘चंपारन में गाँधीजी’ 2. ‘संस्कृत का अध्ययन’ 3. ‘आत्मकथा’ और 4. ‘बापू के कदमों में’–ये चार पुस्तकें हिंदी की अक्षय निधि हैं। विधान-परिषद की समाप्ति पर अपना विचार प्रकट करते हुए उन्होंने अपनी जिन दो वेदनाओं का जिक्र किया, उनमें से एक यही थी कि भारतीय गणतंत्र का विधान मौलिक रूप से हिंदी में नहीं लिखा जा सका!
उनकी अन्य हिंदी-सेवाओं की तरह उनके इस वेधक वाक्य ने भी हिंदी भाषी जनता का ध्यान उनकी ओर आकर्षित किया और तब से कितने ही लोग अपने-आपसे आँख चुराए हुए यह सोच रहे हैं कि हमने अबोहर-सम्मलेन के समय जिसको हिंदी-विरोधी कहा था, क्या यह वही पुरुष है?
राजेंद्र बाबू का साहित्यिक व्यक्तित्व जनता से छिपा नहीं है, फिर भी, एक दिन, उनके राष्ट्रपति हो जाने के बाद, मैंने जानबूझकर उनसे इसलिए मुलाकात की कि इस संबंध की कुछ और हल्की-फुल्की बातें जनता को मालूम हो जाएँ।
ऐसा संयोग कि मैं और सुप्रसिद्ध समाजवादी चिंतक श्री फूलन प्रसाद जी वर्मा साथ ही बुलाए गए। जब फूलन जी दो चार मिनट तक बातें कर चुके, तब मैंने यह कहते हुए अपना काम शुरू किया– “बाबू! आज मैं आपका साहित्यिक इंटरव्यू लेने आया हूँ और सारे प्रश्न मैंने पहले से ही लिख रखे हैं।”
बाबू ने चौंक कर कहा–“साहित्यिक इंटरव्यू के क्या मानी? मैं कोई साहित्यिक थोड़े ही हूँ!”
मैंने कहा–“आप ऐसा ही समझें, किंतु हमारा आग्रह भी तो कोई वस्तु है।” और मैंने झट पहला प्रश्न कर दिया–“आप अखिल भारतीय हिंदी-साहित्य-सम्मलेन में पहले-पहल कब सम्मिलित हुए थे?”
बाबू बोले–“पहले ही अधिवेशन में। यही नहीं, बल्कि, हिंदी-साहित्य-सम्मलेन जैसी कोई संस्था कायम की जाए, इसके लिए मैंने थोड़ा-बहुत आंदोलन भी चलाया था और उसके लिए पत्रों में लेख भी लिखे थे। किंतु अब याद नहीं कि वे लेख कहाँ छपे थे। मुझमें यह विचार बंगीय साहित्य- परिषद को देखकर उठा था जो संस्था उन दिनों काफी कार्यशील थी।”
मैंने दूसरा प्रश्न यह पूछा कि जब आप छात्र थे उस समय हिंदी में किन कवियों की कविताएँ आदर से पढ़ी जाती थीं।
राजेंद्र बाबू ने कहा–“हिंदी में उस समय भारतेंदु बाबू की रचनाओं की धूम थी और उनकी कविताओं के आगे बहुतों के दोहे-सवैये फीके पड़ रहे थे। अपने छात्र जीवन में हमलोग देवी प्रसाद ‘पूर्ण’ और श्रीधर पाठक जी की कविताओं को भी बड़े ही चाव से पढ़ते थे। आगे चलकर नवयुवक कवि श्री मैथिलीशरण जी आए और उनकी रचनाएँ भी आरंभ से ही लोकप्रियता प्राप्त करने लगीं।”
मैंने फिर पूछा कि हिंदी के प्राचीन कवियों में आपको अधिक प्रिय कौन लोग रहे हैं।
उन्होंने आशानुरूप उत्तर दिया–“तुलसीदासजी पर शुरू में ही जो भक्ति बैठी, वह आज भी ज्यों की त्यों है, बल्कि, दिन-दिन उनकी कविता मेरे लिए नवीन होती गई है। उनके सिवा, सूरदास की कविताओं से भी मैं विह्वल हो जाता हूँ तथा वे मेरे हृदय को बड़े जोर से छूती हैं। इन दोनों के बाद मीरा और कबीर का स्थान आता है। तब भी तुलसीदास की रचनाएँ मैंने सबसे पहले पढ़ी थीं और आज भी उन्हें पढ़ता रहता हूँ।”
विषय का दायरा बढ़ाने के उद्देश्य से मैंने सवाल किया कि अँग्रेजी और उर्दू के किन कवियों पर आपका विशेष स्नेह है।
वे बोले–“मैंने इन कवियों का विधिवत् अध्ययन नहीं किया है; जहाँ-तहाँ से कुछ थोड़ा-बहुत देख-भर गया हूँ। तो भी उर्दू के कवि मियाँ नजीर अकबराबादी की कई चीजें मुझे बेहद पसंद हैं।”
छायावादी आंदोलन पर पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि मैंने उस आंदोलन की चर्चा दूर से ही सुनी थी; नज़दीक से उसे देखने या समझने का मौका मुझे नहीं मिला। अतएव, उसके संबंध में मैं अपना कोई मत नहीं दे सकता।
हिंदी और उर्दू के जीवित समकालीन कवियों के संबंध में जिज्ञासा करने पर उन्होंने कहा कि नाम तो मैंने कइयों के सुने हैं और उनकी छिटपुट रचनाएँ भी देखी हैं, किंतु, उनके संग्रह-विशेष को ठीक से देखने का मुझे अवसर नहीं मिला। हाँ, बाबू मैथिलीशरण जी गुप्त की ‘भारत-भारती’ की याद मुझमें अब भी बनी है।
मैंने फिर पूछा कि आपने हिंदी में सबसे पहले क्या लिखा था?
उन्होंने कहा–“सबसे पहले मैंने कुछ स्फुट लेख लिखे थे जो उस समय के कई पत्रों में प्रकाशित हुए थे। बिहारी-छात्र-सम्मलेन की ओर से हमलोग ‘यंग बिहार’ नामक एक मासिक पत्र निकाला करते थे जिसमें हिंदी और अंग्रेजी की मिली-जुली रचनाएँ प्रकाशित होती थीं। संभवतः, मेरा पहला हिंदी-लेख ‘यंग बिहार’ में ही छपा था। किंतु, ठीक से नहीं कह सकता कि मेरा पहला लेख कहाँ छपा–क्योंकि उन्हीं दिनों मैं पंडित पद्मसिंह जी शर्मा के ‘भारतोदय’ और पंडित जीवानंद जी शर्मा की ‘कमला’ में भी लेख लिखने लगा था। पंडित पद्मसिंह जी शर्मा का ‘भारतोदय’ ज्वालापुर-महाविद्यालय से निकलता था और ‘कमला’ कलकत्ता से। पीछे चलकर ‘कमला’ भागलपुर से निकलने लगी।”
अब बात राजेंद्र बाबू की आत्मकथा के बारे में चली। यह तो मैं जानता ही था कि ‘आत्मकथा’ की रचना के समय राजेंद्र बाबू के पास न तो कोई डायरी थी और न चिट्ठियों की फाइल; न अख़बारों की कतरन थी और न कांग्रेस की प्रस्ताव पुस्तिका। ‘आत्मकथा’ में एक तरह से भारतवर्ष के चालीस वर्षों का राजनीतिक इतिहास ही लिपिबद्ध हुआ है, किंतु, इस विशालकाय ग्रंथ को उन्होंने सिर्फ अपनी स्मृति से ही लिख डाला। लेकिन, मुझे यह जानकर और भी आश्चर्य हुआ कि कोई 1500 पृष्ठों की विशाल पांडुलिपि उन्होंने अपने ही हाथों से तैयार की; कहीं भी कोई डिक्टेशन नहीं दिया। यह भी उनकी धीरता और अध्यवसाय का एक ज्वलंत उदाहरण है।
फिर, मानो, मुझे आश्चर्य-चकित देख कर उन्होंने कहा–“लेकिन, ‘बापू के कदमों’ का एक पृष्ठ भी मैंने अपने हाथ से नहीं लिखा है। उसकी पांडुलिपि सिर्फ डिक्टेशन से तैयार हुई है।”
मेरा एक प्रश्न था–“आप कब लिखते हैं? दिन में या रात में?”
उन्होंने कहा, “कोई ठीक नहीं। जब समय मिल जाता है, कुछ लिख लेता हूँ।”
मेरे यह पूछने पर कि आप पेंसिल से लिखना पसंद करते हैं या कलम से, बाबू ने कहा कि पेंसिल से तो भरसक मैं लिखता ही नहीं। मैं जो कुछ भी लिखता हूँ, कलम से ही लिखता हूँ।
मेरा एक सवाल यह भी था कि अपनी चारों पुस्तकों में से खुद आपको कौन पसंद है।
उन्होंने कहा–“लिखने के बाद मुझे पुस्तकों को पढ़ने का अवकाश नहीं मिला है। यह तो आप लोग ही बता सकते हैं कि कौन किताब कैसी हुई है।”
मैंने निवेदन किया–“आत्मकथा विशाल है। किंतु, ‘बापू के कदमों में’ महान है और वह जनता को कहीं अधिक प्रभावित करेगा।” मेरा अंतिम प्रश्न था कि आगे आप क्या लिखने का विचार कर रहे हैं।
बाबू बोले–“अभी तो कोई योजना सामने नहीं है।”
प्रसंगवश, फूलन जी ने बाबू के सामने ही उनकी शैली की सरलता की चर्चा छेड़ दी और मुझे कहा कि जेल में राजेंद्र बाबू ने अपनी शैली की व्याख्या करते हुए कहा था कि मैं न तो संस्कृत का पंडित हूँ और न फारसी का विद्वान्; ऐसी हालत में मैं जो कुछ लिखूँगा वह आसान छोड़ कर और क्या होगा। इस विनयशीलता पर चकित होना व्यर्थ है, क्योंकि यह तो राजेंद्र बाबू की गिनी-चुनी विशेषताओं में से एक है।
जब हम बाहर निकले, फूलन जी ने एक बात कही। जेल में जब ‘आत्मकथा’ समाप्तप्राय थी, एक दिन राजेंद्र बाबू ने फूलन जी से पूछा कि तुम्हें यह रचना कैसी लगती है? फूलन जी ने कहा कि यह एक संयमी योद्धा की जीवनी है, किंतु, इसमें कला के गुणों का अभाव है।
मेरे एक और मित्र (पं. शांतिप्रिय जी द्विवेदी) ने एक दिन बातों के सिलसिले में मुझसे कहा था–“राजेंद्र बाबू की आत्मकथा गाँव की नदी बन कर आई है। वह गाँव वालों की आवश्यकता को पूरी करती हुई बहती जा रही है, किंतु, उसमें उद्वेग का अभाव है।”
सच ही, कला में उद्वेग का अभाव नहीं होता। कला का जन्म ही उद्वेग से होता है कलाकृति का एक सौंदर्य उसके चढ़ाव-उतार का भी सौंदर्य है।
किंतु, क्या राजेंद्र बाबू कभी उद्वेग से होकर नहीं गुज़रे हैं? फिर उनकी रचना में उद्वेग अनुपस्थित क्यों है?
श्री फूलन जी ने इसका राज़ खोला–कला के उत्कर्ष की एक शर्त यह भी है कि कलाकार आंतरिक द्वंद्व से होकर गुज़रे। किसी भी बड़े काम के सामने आने पर मनुष्य एक प्रकार के संकट में पड़ जाता है। उस संकट की वेदना भोगने से कलाकार की कृति में विह्वलता उत्पन्न होती है जो सभी महान कलाओं की जान है। किंतु, राजेंद्र बाबू संकटों को पार करते हुए भी उनकी टीस से अपरिचित रहे हैं। वर्षा में जो आर्द्रता, जाड़े में जो ठंडक और गर्मी में जो ताप है उसे तितिक्षु नहीं जानता; क्योंकि उसका मन नियंत्रित और चर्म कड़ा होता है। राजेंद्र बाबू जब संकटों का मुकाबला करने निकले थे तब अपनी नाव जला कर निकले थे, जिसका परिणाम यह हुआ कि विपत्तियाँ उनके भीतर वह दर्द नहीं जगा सकीं जो तितिक्षावस्था से नीचे की सतह पर काम करने वाले कलाकारों में पैदा होता है। यही कारण है कि उनकी वाणी तितिक्षुओं की वाणी के सामान विश्रब्ध और सीधी-सादी है तथा उसमें कलाकारिता के चढ़ाव-उतार का अभाव है।
यहाँ वर्ड्सवर्थ की याद आती है। उसके बारे में मैथ्यू आर्नाल्ड ने लिखा है कि जगह-जगह ऐसा मालूम होता है, मानों प्रकृति ने वर्ड्सवर्थ के हाथ से कलम छीन ली हो और वह खुद कविता लिखने लगी हो। मगर, जब वर्ड्सवर्थ प्रकृति के हाथ में कलम नहीं देना चाहता तब वह बहुत अच्छा नहीं लिखता है।
यानी आत्मविस्मृति की शीतलता में पहुँच कर वर्ड्सवर्थ जो कुछ भी लिखता है, वह बिना चढ़ाव-उतार के भी सुंदर है।
Image Courtesy: LOKATMA Folk Art Boutique
©Lokatma