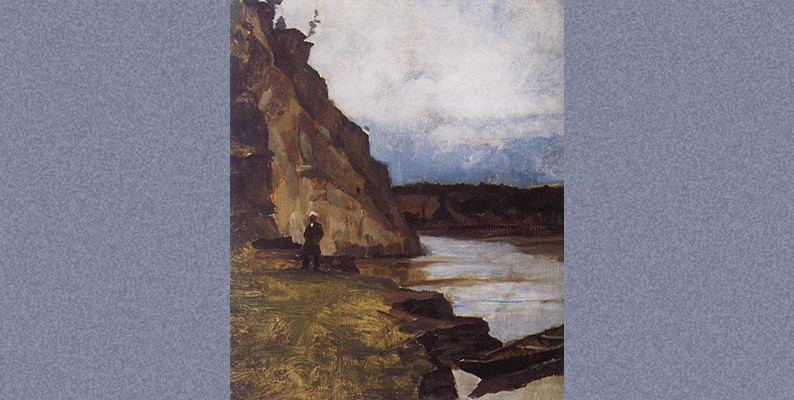साहित्य केवल बुद्धि से नहीं रचा जाता
- 1 December, 2016
शेयर करे close
शेयर करे close

शेयर करे close
- 1 December, 2016
साहित्य केवल बुद्धि से नहीं रचा जाता
आपका पूरा नाम?
अब पूरा नाम कहाँ! अब तो जो सिमट कर रह गया है, उसे ही पूरा नाम कहिए, यानी अमरेंद्र। मुझे याद है, मैंने कभी भी अपना नाम अमरेंद्र कुमार सिन्हा नहीं लिखा। अमरेंद्र कुमार सिन्हा से डॉ. अमरेंद्र होने की भी एक कहानी है। कविताएँ लिखनी शुरू की, तो अपना उपनाम रखा ‘घायल’। वर्षों तक ‘घायल’ ही रहा, अमरेंद्र कुमार ‘घायल’। फिर घायल हटा, तो कुमार भी हट गया। यह ‘कुमार’ कथाकार कमलेश्वर के कहने पर हटाया था, जब मैं समांतर कथा-आंदोलन से जुड़ा। बाद में साहित्यकार आनंद शंकर माधवन ने कहा, अमरेंद्र तो बहुत छोटा नाम लगता है, अच्छा होगा कि तुम अपना नाम अमरेंद्र ‘अमर’ कर लो। एकाध बार लिखा भी, इस नाम से छपा भी। फिर इस उपनाम को भी छोड़ दिया और पी.एच.डी. करने के बाद मैं डॉ. अमरेंद्र हो गया। वैसे मैं आपको यह भी बता दूँ कि मेरे छद्म नाम भी कई हैं–डॉ. निर्दलीय के नाम से अगर समीक्षाएँ करता था, तो डॉ. अक्स के नाम से अनुवाद भी करता रहा और श्रीज्ञान संभूति के नाम से भी कुछ लिख लिया।
आप कब पैदा हुए?
इसका उत्तर देना बड़ा कठिन लगता है। बस ऐसा ही समझिए कि एक बार पिता जी ने एक आवेदन पत्र पर मेरे जन्म की तारीख 5 जनवरी 1949 लिख दी, और उसे ही सच मान लिया। लेकिन माँ से जो बातें मैंने सुनी हैं उससे मेरे जन्म का महीना जनवरी नहीं, मार्च का मध्य या आरंभ रहा होगा। माँ ने बताया था कि जब मेरा जन्म हुआ, उस समय गाँव के मेरे घर के छप्परों पर सिर्फ पके हुए कुम्हड़े ही बिछे दिखाई देते थे पुआल नहीं। साफ है, वह वसंत का समय रहा होगा। जहाँ तक सन्, ई. का सवाल है, वह सन् 1949 ही सही लगता है।
आपने कहीं नौकरी की?
मन ही नहीं लगा, नौकरी में। डुमरामा के महाशय द्वारिकानाथ उच्च विद्यालय में पिता जी शिक्षक थे। उस समय स्कूल के सचिव और शिक्षा पदाधिकारी ही सब कुछ हुआ करते थे, उसी स्कूल का मैं शिक्षक भी बन गया। पिता जी ने चाहा कि कहीं दूसरी नौकरी कर लूँ। उस समय बोकारो स्टील प्लांट का बहुत बोलबाला था, और उसी में कार्यरत थे मेरे चाचा अनंत कुमार सिन्हा। उनका बोलबाला भी कम नहीं था। पिता जी ने उन्हीं के पास भेज दिया, उन्होंने आनन-फानन में आरंभिक काम करवा दिया और बताया कि हफ्ते भर बाद एक छोटी-सी परीक्षा होगी, टंकण कला में दक्षता की, लेकिन उसकी चिंता नहीं करनी है। मैं बोकारो से बाँका लौटा। रास्ता भर सोचता आया कि इस क्लर्क की जिंदगी में तो मेरा जीवन गया ही समझो। सो आते ही घर में पिता जी से कह दिया, ‘चाचा ने कहा है, वैकेंसी निकलेगी, तो सूचित करूँगा।’ पिता जी ने आगे पूछताछ नहीं की। मुझे आनेवाले बंधन की विपत्ति से मुक्ति मिल गई थी। और आखिर में एक नौकरी मिल गई, मेरे मन के बिल्कुल अनुकूल, एक नए महाविद्यालय में हिंदी व्याख्याता के रूप में मैं ले लिया गया, जहाँ वेतन तो नहीं था, लेकिन इसके बाद सब कुछ था, जो किसी सरकारपोषित महाविद्यालय में भी शायद ही मिले। तब इस कॉलेज का कोई अपना भवन भी नहीं था, लेकिन वहाँ के शिक्षकों डॉ. उमेश राय, शशिभूषण सिंह खड़गाहा, प्रमोद चट्टोपाध्याय, चक्रधर प्रसाद सिंह, अवधेश सिंह, अभय सिन्हा, धनंजय मिश्र रत्नेश्वर प्रसाद चौधरी के आत्मीय सहयोग और गंभीर विषयों पर वाद-विवाद-संवाद ने कभी किसी चीज की कमी का अनुभव ही नहीं होने दिया। हमलोग के जो सचिव थे, सोना बाबू, यानी तेगबहादुर सिंह, उन्होंने कभी अपने व्यवहार से यह अनुभव ही नहीं होने दिया, कि वह सबलपुर स्टेट के जमींदार हैं। मुझे और क्या चाहिए था। यही कारण है कि भागलपुर के एक महाविद्यालय में जब हिंदी व्याख्याता की जरूरत हुई और मेरे गुरुदेव डॉ. शिवनंदन प्रसाद (अलवर्ट अली कृष्ण) ने आवेदन दे देने का आदेश यह कहते हुए दिया कि मैंने तुम्हारे बारे में एक्सपर्ट को बता दिया है, सब ठीक हो जाएगा, फिर भी मैंने कोई कोशिश नहीं की। सच तो यही है कि सी.एन.डी. महाविद्यालय में आने के बहुत पूर्व से ही मुझे मंदार क्षेत्र बहुत प्रिय था। बौंसी में साहित्यकार प्रो. कृष्ण किंकर सिंह थे, आनंद शंकर माधवन थे, प्राणमोहन प्राण थे, महाविद्यालय में आया, तो बौंसी में नए साहित्यकारों का मंडल बना। द्विजेंद्र राष्ट्रभाषा परिषद बनी, मैं उसका अध्यक्ष था, और प्राण जी उसके महासचिव। ‘समय’ पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ। अनूप जी उसके संपादक बने। विजय सिंह, मिथिलेश झा, कालिकानंदन झा, विमल चंद्र दास जैसे साहित्यकार सामने आए। पन्ना दा के सहयोग ने उत्साह के झेलम को गंगा-गोदावरी बना दिया था। हरगानवी साहब, आप सोच भी नहीं सकते कि कोई वेतन के बिना शिक्षा और संस्कृति का महादान इस महाआर्थिक युग में करेगा, लेकिन हमलोग ने किया है। आप अगर इसे नौकरी करना कहेंगे, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं।
आपकी पसंद की भाषा क्या है?
वह तो हिंदी ही है, लेकिन इसकी कमियों को भी पसंद करता हूँ, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं अनुशासन को पसंद करता हूँ लेकिन जब आप अनुशासन को ही सब कुछ मान लेते हैं, तब दिक्कत होती है। फिर अनुशासन में भी अगर एकरूपता नहीं हो, तो और दिक्कत। मैं यह हिंदी के व्याकरण के संबंध में कह रहा हूँ। यहाँ तालव्य ‘श’ और मूर्धन्य ‘ष’ के प्रयोग की ही जटिलता नहीं है, लिंग-प्रयोग की भी जटिलता है। मुझे स्कूली शिक्षा के क्रम में एक शिक्षक ने बताया था कि न के पूर्व य या र आए, तो ‘न’ हमेशा मूर्धन्य ‘ण’ होगा, लेकिन मैं पूछता हूँ, जब कन की जगह कण ही लिखा जाए, तब कौन-सा व्याकरण काम कर रहा है। मैंने बाद में यह प्रश्न किया था, तो शिक्षक ने बताया था कि पश्चिम प्रांतों में कन को लोग कण बोलते हैं। अब सोचिए कि भाषा पर व्याकरण का अनुशासन होगा कि क्षेत्र के लोगों का? अगर ऐसा ही है, तो बिहार के लोग जैसा बोलते हैं, वैसा ही व्याकरण क्यों न बने। हिंदी में संस्कृत के, अरबी, फारसी के ढेरों शब्द हैं, जब हमने उन शब्दों को लिया है, तो उनके लिंगों को भी वैसा ही क्यों न रहने दिया गया, मुझे लगता है कि हिंदी को सरल बनाने की अभी और जरूरत है। जब हमने यह माना कि हिंदी में मूर्धन्य ‘ष’ का उच्चारण लुप्त हो गया है, तो इसे वर्णमाला में बनाए रखने की क्या जरूरत। इसे, ‘ष’ को बनाए रखने के लिए व्याकरण बनाना पड़ा है, और हिंदी सीखनेवालों के लिए यह बोझिल है। जब ‘ऋ’ का उच्चारण ‘रि’ की तरह होता है तो ‘रि’ ही लिखने को आप क्यों नहीं प्रोत्साहित करते हैं। ऋतु को रितु ही लिखते बोलते हैं। इधर उर्दू का भी अरबी-फारसीकरण होने लगा है, तो उनलोग के लिए उर्दू सीखना कठिन हो गया है, जो हिंदी परिवेश में पले-बढ़े हैं। मेरी हिंदी-उर्दू में रचनाएँ हैं, लेकिन मेरी हिंदी वह हिंदी-उर्दू है, जो काया और आत्मा से एक है, अंतर करने के लिए बस साड़ी या बुरका पहनाने की जरूरत है, मेरा मतलब लिपि से है। और लिपि का अंतर भाषा को अलग नहीं सिद्ध कर सकता।
आपने लिखना कब और कैसे शुरू किया?
निश्चित रूप से वह 1967 या 68 का वर्ष होगा, जब मैंने लिखना शुरू किया। इसके पहले का मुझे स्मरण नहीं आ रहा। तब मैं भागलपुर से बाँका चला आया था, 1969 में बाँका से एक मासिक पत्रिका ‘चंद्रकिरण’ का प्रकाशन शुरू हुआ। संपादक थे, सदानंद सिंह और प्रकाशक थे बाबा भारती। बाबा भारती का मूल नाम था, चंद्रकिशोर सिंह, पर उपनाम रख लिया था, बाबा भारती, और वह इसी उपनाम से विख्यात भी थे। सुदर्शन की कहानी ‘हार की जीत’ के बाबा भारती की तरह सहृदय थे, लेकिन वक्त पड़ने पर खड़गसिंह भी बन जाते थे। साहित्यकार खुशीलाल मंजर जब उनके चरित्र की कहानी सुनाते हैं, तो इनकी आँखें खिल जाती हैं। यह मैंने बहुत बाद में जाना था कि साईकिल से ही बाबा भारती शांतिनिकेतन तक पहुँच गए थे, बोलपुर बंगाल। तो बाबा भारती ने ‘चंद्रकिरण’ का प्रकाशन शुरू किया था। इसके प्रवेशांक में मेरी कविता छपी थी और दूसरे अंक में विमल विद्रोही की कहानी ‘बंधन’। विद्रोही ही आगे चलकर अनिरुद्ध प्रसाद विमल हो गए। ‘चंद्रकिरण’ का दूसरा अंक नवंबर-दिसंबर 1969 में प्रकाशित है। स्पष्ट है कि इसका प्रवेशांक अक्टूबर 1969 में ही प्रकाशित हुआ होगा। इस प्रवेशांक में जो मेरी कविता छपी थी उसका शीर्षक था ‘ओ बापू नाविक तू आ।’ कविता तो याद नहीं, लेकिन यह कविता सवैया छंद में थी, इतना मुझे याद है। आरंभ में जो कविताएँ की, वे वार्णिक छंद में ही थीं। यह मेरे लिए आसान भी था। गुरु-लघु अक्षरों को जान गया था, इसी से सवैया, कवित्त और पंचदशाक्षर छंद में मुक्तक लिखना शुरू किया था।
हिंदी में व्यंग्य का कैसा भविष्य देखते हैं?
बहुत अच्छा भविष्य नहीं कहा जा सकता। व्यंग्य के प्रति जो प्रतिबद्धता हरिशंकर परसाई, शरद जोशी, के.पी. सक्सेना, डॉ. श्यामसुंदर घोष, डॉ. बालेन्दु शेखर तिवारी में दिखाई पड़ी या है, वैसी प्रतिबद्धता अब मुझे दिखाई नहीं पड़ती। बहुत दिनों तक मेरे पास ‘व्यंग्यम’ नाम की एक पत्रिका आती रही, नहीं कह सकता कि वह निकलती भी है या नहीं। अभी हाल में ही बालेन्दुशेखर तिवारी के दो व्यंग्य संग्रह आए हैं, एक तो कविताओं का संग्रह है ‘प्रणाम सर’ और दूसरा व्यंग्य लेखों का संकलन ‘भारत दुर्दशा का चित्रहार’। इन दोनों संग्रहों को पढ़कर यही लगा कि व्यंग्य की धार अभी सूखी नहीं है लेकिन परसाई और कमला प्रसाद बेखबर के नहीं रहने से इस धारा का वेग तो घटा ही है। बेखबर जी ने व्यंग्य को मजबूती देने के लिए जिस तरह से नाटक, कविता, कथा का सृजन किया, वह कभी भुलाया नहीं जा सकता और जिस तरह से डॉ. श्यामसुंदर घोष ने व्यंग्य साहित्य को स्थापित करने के लिए लगातार लेखन किया, वैसी सक्रियता भी अब नहीं दिखती। सभी पुराने व्यंग्यकार शिथिल पड़ रहे हैं, और नए व्यंग्यकार दूर-दूर तक नहीं दिखते। इधर फेसबुक पर मुन्ना पांडेय और ब्रजेंद्र गर्ग के दोहे व्यंग्य के भविष्य के प्रति आश्वस्त तो करते हैं, लेकिन इनकी संख्या ही कितनी है!
अगर आप से कहा जाए कि 1900 से 2015 के बीच की 25 हिंदी कहानियों का चयन करें, तो वे कहानियाँ कौन-कौन-सी होंगी?
यह काम बहुत कठिन है, कारण कि 1900 से 2015 के बीच जितने कथाकार हुए उनमें 25 कथाकारों को चुनना ही कठिन है; कहानियों की बात तो छोड़ दीजिए। मैं जब अपने आसपास के कहानीकारों की ओर देखता हूँ, तो यह देखकर आश्चर्य होता है कि हिंदी कथा साहित्य के इतिहास में इनके नाम भी कहीं नहीं मिलते। इसका अर्थ यह नहीं कि इनकी कहानियाँ राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, मन्नू भंडारी, उषा प्रियंवदा या भीष्म साहनी से कम हैं, बात यह है कि इन कहानीकारों की पकड़ न तो महानगर की पत्रिकाओं पर है, और न कथालोचकों या इतिहास लेखकों पर। इससे इनकी कहानियों के बारे में तो क्या, इन कहानीकारों के बारे में भी कथालोचकों को पता नहीं। नहीं तो क्या कारण है कि डॉ. शीतल अवस्थी, डॉ. मृदुला शुक्ला, डॉ. निरूपमा राय, श्रीकेशव, कांता सुधाकर, सदाशिव सुगंध, शिव कुमार शिव, अनिरुद्ध प्रसाद विमल, रंजन, सुरेंद्र प्रसाद यादव जैसे कई कहानीकारों की कहानियाँ कथा साहित्य के इतिहास में कहीं दर्ज नहीं मिलतीं, न इनके नाम। लेकिन इससे क्या होता है। अगर सौ, सवा सौ वर्षो के बीच की कहानियों में से मुझे 25 कहानियाँ ही चुननी हो, तो ये कहानियाँ होगी (अँगुली पर गिनते हुए कहते हैं) गुलेरी की कहानी ‘उसने कहा था’, प्रेमचंद की ‘शतरंज के खिलाड़ी’, प्रसाद की ‘आकाशदीप’, जैनेंद्र की ‘नीलम देश की राजकन्या’ उग्र जी की ‘गंगा’, यशपाल की ‘दूसरी नाक’, अज्ञेय की ‘शरणदाता, मोहन राकेश की ‘मलवे का मालिश’, धर्मवीर भारती की ‘बंद गली का आखरी मकान’ मन्नू भंडारी की ‘यही सच है’, निर्मल वर्मा की ‘परिंदे’ कमलेश्वर की ‘राजा निरवंशिया’, भैरव प्रसाद गुप्त की ‘कंठी’, डॉ. मधुकर गंगाधर की ‘बरगद’, ज्ञानरंजन की ‘घंटा’ जसवंत सिंह विरदी की ‘माँ को लिखा पत्र’, श्रीकेशव की ‘सबसे बड़ा झूठ’ डॉ. मृदुला शुक्ला की ‘कहानी एक बुरी लड़की की’, अनिरुद्ध प्रसाद विमल की ‘करवट’, सदाशिव सुगंध की ‘ज्ञानसिंह’, सुधा ओम ढ़ीगरा की ‘आग में गर्मी कम क्यों है’, सुरेंद्र प्रसाद यादव की ‘मगरी’, शिव कुमार शिव की ‘चलावा’, रंजन की ‘तो सलाम मेरे दोस्तो’ और डॉ. आभा पूर्वे की ‘चंदन जल न जाए’।
पहले के साहित्य और आज के साहित्य में अंतर?
है, जितना पहले के आदमी और आज के आदमी में है। पहले व्यक्ति के पास संवेदना की सबसे बड़ी संपत्ति थी, वह आज के मनुष्य में भी वैसा ही है, ऐसा मैं नहीं कह सकता। बचपन में देखा है, मेरे घर की बगल में एक सौ वर्ष के एक आदमी ने जब अपनी देह छोड़ी, तो गाँव भर के लोग उस घर के बाहर आ जुटे थे। आज वह स्थिति नहीं रह गई है, कंधा देने के लिए दस-पंद्रह बुलाने पर जुट जाएँ, तो बहुत। समय बहुत बदल गया है। आदमी ने समस्याओं में अपने को उलझा लिया है। संवेदना ने जीवन का साथ छोड़ दिया है। जटिलताएँ उभर आई हैं और इन नई परिस्थितियों का साहित्य पर भी अच्छा खासा प्रभाव पड़ा है। जो सरलता ‘पंच परमेश्वर’ में थीं, ‘वह जिंदगी और जोंक’ में नहीं है। बात सिर्फ कथानक की नहीं है, आधुनिक जीवन की जटिलताओं ने अभिव्यक्ति के शिल्प पर भी अच्छा खासा प्रभाव छोड़ा है। आप सुदर्शन की कहानी ‘हार की जीत’ राजा राधिकारमण प्रसाद सिंह की कहानी ‘दरिद्रनारायण’ के शिल्प की तलाश, कमलेश्वर की कहानी ‘राजा निरवंशिया’ या शिवकुमार शिव की ‘चलावा’ कहानी में नहीं ढूँढ़ सकते। ये बदलाव कथा तक ही नहीं, कविता तक पसरा हुआ है। नतीजा यह हुआ कि संवेदना से साहित्य का संबंध छूट रहा है, विचार का बोझ साहित्य के माथे पर थोप दिया गया है। सिर्फ बुद्धि से क्या साहित्य को चलाया जा सकता है? हम क्यों नहीं सोचते कि श्यामसुंदर घोष की काव्य कृति ‘अरण्यायन’ पाठकों पर जितना प्रभाव छोड़ती है, वह ‘असाध्यवीणा’ नहीं। किसी के कहने से क्या होता है कि ‘कामायनी’ का महत्त्व इसलिए है कि वह पाठ्यक्रम में शामिल है।
पत्रिकाओं में छपी समीक्षा का संबंध क्या केवल तारीफ से होता है?
पत्रिकाओं में छपनेवाली पुस्तक-समीक्षा विज्ञापन के अतिरिक्त कुछ विशेष होती भी नहीं है और विज्ञापन से आप समीक्षा की कितनी अपेक्षा कर सकते हैं। यह तो कुछ वैसा ही होगा कि टीवी पर वस्तुओं की खूबियों को बताने वाले विज्ञापन पर हम पूरी तरह भरोसा करें और बिना खोजबीन किए, उन वस्तुओं का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। कभी ऐसी पुस्तक-समीक्षाओं का अपना महत्त्व रहा होगा, जब जीवन की व्यस्तताओं को देखते हुए रिव्यु का प्रचलन साहित्य के पाठकों की जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए आरंभ हुआ होगा, जिसमें पुस्तक के कथ्य और शैली के साथ उसकी सजावट-कसावट के आकर्षण को संकेत में समझाने का प्रयास समीक्षक करते होंगे। अब यह सब उद्देश्य कहीं हासिये पर है। जहाँ संपर्क ही ऐसी समीक्षा का आधार बन गया हो, रागद्वेष ईट और गारे का काम करे, तब ऐसी समीक्षा से पाठकों का क्या भला होने वाला है। वैसे इस भीड़ में कभी-कभी अच्छी पुस्तक-समीक्षा भी मिल जाती है। अब इतनी पुस्तकें छप रही हैं, कि सभी की समीक्षाएँ संभव नहीं, और समीक्षकों पर समीक्षाओं के लिए दवाब भी बना रहता है, नतीजा यह होता है कि समीक्षक पुस्तक को पढ़ते नहीं, सूँघते भर हैं और सूँघने से पुस्तक के बारे में क्या ज्ञान हो सकता है। आज लेखक लिखते भले गाँव पर हैं, रहते हैं महानगरों में और समीक्षकों से जो चाहे लिखवा लेते हैं, और समीक्षकों को भी तो लेखकों के बीच ही रहना है, पाठकों के हित-अनहित से क्या लेना-देना। अधिकांश समीक्षक उन पुस्तकों की ही समीक्षा करना चाहते हैं, जो बाजार में खपने योग्य हैं, और फिर उनकी तारीफ में उम्दा से उम्दा कसीदे पढ़ देते हैं। और क्या?
आपने अंगिका भाषा में एक छोटी-सी पुस्तक लिखी, नाम है ‘गजल रो पिंगल’। इस पिंगल शास्त्र में आपने उर्दू के कई छंदों को हिंदी के छंद से अलग नहीं माना है। आखिर उर्दू और हिंदी में कुछ तो अंतर होगा और अगर है, तो यह कैसे है?
राही मासूम रजा ने कभी ‘धर्मयुग’ के एक अंक में लिखा था कि गजल की जन्मभूमि भारत है और दोहे से इसका विकास है। जब गजल की बात उठती है, तो न जाने क्यों राही मासूम रजा के वक्तव्य को जानबूझ कर अनदेखा कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ बात है छंद विधान की, तो देखिए, उर्दू में जितने भी साधारण यानी मुफरिद बहरें हैं, वे संस्कृत के ‘गण’ से बने छंदों से अलग नहीं हैं। चार मफाईलुन से बनने वाले हजज को ही लें, तो हिंदी में यही छंद यगण के अंत में एक गुरु रख दें और इसे चार बार घुमाएँ, तो उर्दू में जिसे रमल कहते हैं, वही छंद होगा। इनसे अलग हम उर्दू के बहर कामिल को ही लें, इसमें मुतफाइलन की चार आवृत्ति होती है। हिंदी में यही तगण के अंत में एक गुरु के जोड़ने से हो जाता है। उर्दू के हजज और वाफर में क्या भेद है, मुझे मालूम नहीं, हिंदी में दोनों का निर्माण एक-सा है। जहाँ उर्दू के बहर मतकारब का प्रश्न है, वह तो हिंदी के ‘यगण’ गण से कुछ भी भिन्न नहीं और न मतदारक यानी चार फाइलुन कभी संस्कृत गण से अलग कुछ लगता है। मुझे तो लगता है कि हिंदी और उर्दू छंदों में जो कुछ भिन्नता है, वह नामों को लेकर है, चौपाई। आप भी जानते हैं कि उर्दू में इसी छंद का बहुत बड़ा नाम है, वह है मतदारक मस्मन मक्तूअ। अगर नामों के अंतर को मिटा दिया जाए, तो मुझे लगता है, हिंदी-उर्दू का भेद भी बहुत कुछ मिट जाएगा। यहाँ मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि संस्कृत में लघु-गुरु के अनुशासन का विशेष ख्याल रखा जाता है लेकिन संस्कृत का वर्णिक छंद जब हिंदी में मात्रिक रूप धारण करके आता है, तब यहाँ गुरु का रूप बदला हुआ भी मिलता है। कहने का मतलब है कि यहाँ दो लघु मिलकर एक गुरु का रूप ले लेते हैं, यही बात हम उर्दू के छंदों में भी स्पष्टता के साथ देख सकते हैं।
हिंदी में सॉनेट के सबसे बड़े कवि त्रिलोचन समझे जाते हैं। उसका सॉनेट संग्रह ‘उस जनपद का कवि हूँ’ बहुत लोकप्रिय हुआ है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, इसके बाद ‘साधो सुर का देश’ ही हिंदी का दूसरा ऐसा सॉनेट संग्रह है, जिसमें 127 सॉनेट सिर्फ हिंदी के ही हैं। ‘उस जनपद का कवि हूँ’ और ‘साधो सुर का देश’ में कोई विषयगत या रूपगत भेद?
मैं सिर्फ अपने सॉनेट की बात करूँगा। ‘साधो सुर का देश’ के अधिकांश सॉनेटों का स्वर व्यंग्य का है, बाद में करुणा का। लेकिन इन्हीं स्वरों के बीच एक ऐसा भी स्वर है, जो आशा और विश्वास का भी है, जो बाद में लिखे गए सॉनेटों का स्वर है। जहाँ तक रूप की बात है, इस पर पहले भी मैं कह चुका हूँ। एक बात और जो बताना चाहूँगा, वह यह कि मैं अपने सॉनेटों में पादांतर प्रवाहिता से बचता रहा हूँ। एक पंक्ति दूसरी में जा कर समाप्त हो, यह हिंदी छंदशास्त्र से अनुमोदित नहीं, फिर भी प्रसाद जैसे कवि की कविताओं में पादांतरवाद ही पंक्तियाँ हैं। त्रिलोचन के सॉनेटों में भी यह बात देख सकते हैं। ‘साधो सुर का देश’ में यह एकाध कहीं दिख जाय तो दिख जाय, इसे शैली के रूप में स्वीकार नहीं किया है।
आपने काव्य-सृजन भी शुरू किया तो बंधे हुए छंदो से, उसमें भी वार्णिक छंदों से, जो पूरी तरह लघु-गुरु के नियमों से बंधे हुए हों, फिर आप मुक्त छंद की ओर कैसे आ गए। ‘जनतंत्र का विक्रमशिला’ की कविताएँ छंदबद्ध नहीं हैं और इसके बाद आप फिर छंदों की ओर लौट आए, अगर छिटपुट उदाहरणों को छोड़ दें, तो क्या मैं समझूँ आपको मुक्त छंद से कोई लगाव नहीं, जबकि आज की अधिकांश कविताएँ मुक्त ही होती हैं, छंदबद्ध कम। इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे?
मुक्त छंद की कविताओं के प्रति मेरा आकर्षण कभी नहीं रहा। जिस समय मैं ‘जनतंत्र का विक्रमशिला’ की कविताओं को लिख रहा था, उसी समय मैंने चंद्रशेखर आजाद पर एक प्रबंध काव्य की रचना की थी, जो छंदबद्ध था। ‘जनतंत्र का विक्रमशिला’ की कविताएँ ‘आपातकाल’ में रची गई थीं। जब निश्चिंत होकर रचनाएँ रचना संभव ही नहीं था। गोष्ठियों में देश की स्थितियों के बारे में बताना भी था, तब यही संभव था कि मुक्त छंद की रचना की जाय, जो विचारों से पूर्ण काव्य की भाषा से गठित हों। आपातकाल के बाद मैंने मुक्त छंद की कविताओं से मुक्ति ले ली, भले ही आज का युग मुक्त छंद की कविताओं का क्यों न रहें। हरगानवी साहब, आज मुक्त छंद के पक्ष में बहुत दलीलें दी गई हैं, जैसे कि कविता में भावों की लय होना ही पर्याप्त है, छंदों की लय का नहीं। छंद तो पुराने जमाने की चीज हो गई, जब मुद्रण कला का विकास नहीं हुआ था, तब कविता याद हो सके, इसलिए छंदबद्ध होती थी, अब तो लोग पढ़ते हैं, किसी से सुनते नहीं। अब ऐसे विद्वानों को कौन समझाएँ कि तब कविताएँ छंद के कारण कंठस्थ रहती थीं कि कागज की बर्बादी नहीं होती थी, कम किताबें छपती थीं, तो वृक्ष कम कटते थे, ये जब से कविताएँ पढ़ने की चीज हो गई हैं, वृक्षों का बहुत नुकसान हुआ है। मैं पूछता हूँ, कविता में कहानी नहीं है क्या, नाटक नहीं है क्या, उपन्यास नहीं है क्या? रामचरितमानस क्या है, उपन्यास ही तो है। आज भी गाँव में ऐसे लोग मिल जाएँगे, जिन्हें पूरी रामायण याद है। मैं तो कहूँगा कि गद्य की जगह छंदबद्ध काव्य को बचाने की पहल हो और जो मुक्त छंद के समर्थकों की भीड़ जम गई है, उनके असली मकसद को उजागर करना चाहिए। सच पूछिए तो मुझे इस छंदहीनता में आज के परिवेश में टूटते मूल्यों की छाया ही नजर आती है।
एक सवाल जो आजकल खूब आम है, आप बताएँ कि क्या हिंदी नवजागरण, औपनिवेशिक मानसिकता के विरुद्ध हमारे बौद्धिक संघर्ष और मुक्ति-कामना का द्योतक है?
यह बात बहुत हद तक सही है। लेकिन इसे सीधे-सीधे स्वीकार कर लेना ठीक नहीं होगा। हिंदी के आधुनिक काल में जो नवजागरण के स्वर सुनाई पड़ते हैं, उसके मूल में बदली हुई परिस्थितियाँ भी थीं। एक तो इस पर मध्यकाल के संत काव्य का प्रभाव काम कर रहा था और इसी तरह अँग्रेजों की वैज्ञानिक संस्कृति और सभ्यता का भी दबाव था। अँग्रेजों की आधुनिक आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक, औद्योगिक व्यवस्थाओं ने भारतीयों को प्रभावित ही नहीं किया था, बल्कि यह सोचने के लिए बाध्य भी, कि उनकी बुरी स्थितियों के कारण क्या हैं। तब उनका ध्यान उन मध्यकालीन संत कवियों पर विशेष रूप से गया, जो समाज में फैली दूषित परंपराओं और अमानवीय सामाजिक व्यवस्थाओं पर लगातार प्रहार कर रहे थे। हिंदी साहित्य में जिस नवजागरण की चर्चा बार-बार उठाई जाती है, उसका एक छोर उन्हीं मध्यकालीन संत कवियों के काव्य से बँधा हुआ था और दूसरा छोर औपनिवेशिक व्यवस्था से मुक्ति की छटपटाहट से जुड़ा हुआ था। उस युग के साहित्यकार देश और देशवासियों की दुर्दशा से आहत हो ही रहे थे, सिर्फ समाज सुधारक ही नहीं हो रहे थे, और इसके लिए जिम्मेदार अँग्रेजों के विरुद्ध हिंदी में एक खास तरह की राष्ट्रीय चेतना का विकास हो चला था। यह चेतना भारतेंदु से लेकर निराला, प्रसाद तक में मुखर-अमुखर रूप में उजागर हो रही थी।
Image: The Popular Educator Illustration 6 Holding the Pen.png
Image Source: Wikimedia Commons
Image in Public Domain
Note : This is a Modified version of the Original Artwork