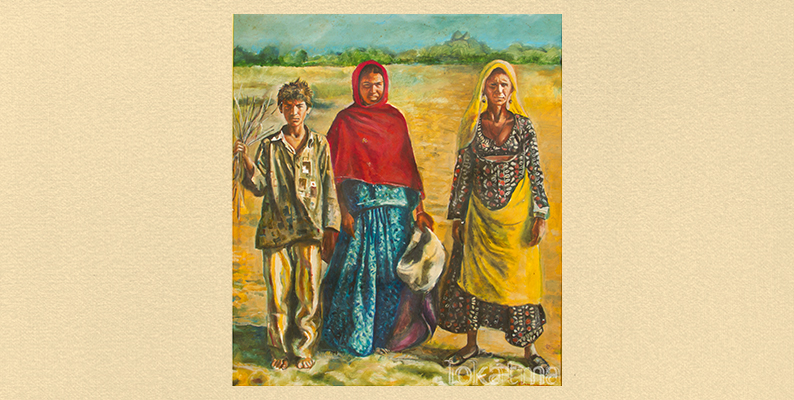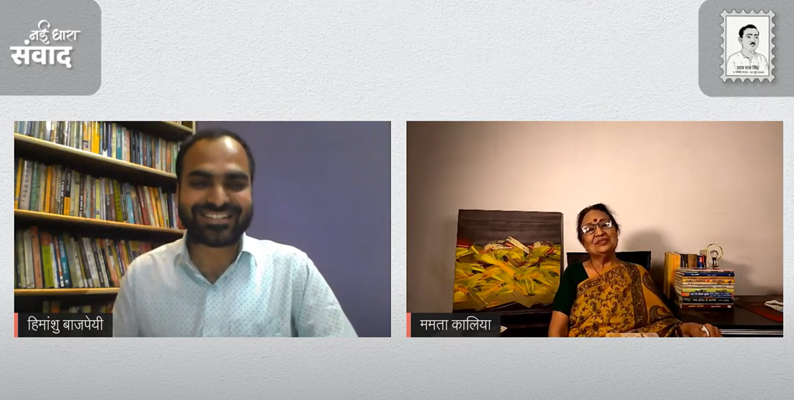नई धारा संवाद : कवि अशोक वाजपेयी
- 1 February, 2022
शेयर करे close
शेयर करे close

शेयर करे close
- 1 February, 2022
नई धारा संवाद : कवि अशोक वाजपेयी
‘कविता लिखना अपने आप में सामाजिक हस्तक्षेप है’
नई धारा संवाद की इस कड़ी में आप सब का स्वागत है और नई धारा संवाद का ये दूसरा संस्करण है। पहले संस्करण को आपलोग ने बहुत प्यार किया, बहुत शौक से सुना। अब जो ये जो दूसरा संस्करण है इसमें भी हम अपने रचनाकार से उनके रचना कर्म के बारे में जानेंगे। उनसे उनका रचना पाठ सुनेंगे।
यहाँ हम अपने समय के प्रसिद्ध लेखक अशोक वाजपेयी से संवाद करेंगे, जो कवि तो हैं ही, कलाविद हैं, प्रशासक हैं, बहुत अच्छा सोचते हैं, और जो एक पूरा कलाओं का संसार है उस पर उनकी गहरी नजर रहती है और इसीलिए जब उनसे बात होती है तो न सिर्फ कविता पर, न सिर्फ गद्य पर, न सिर्फ विविध कलाओं पर बल्कि कला अपने आप में जो संवेदना पैदा करती है हम उसके करीब जाते हैं। अशोक जी की 1941 में पैदाइश हुई, दुर्ग में। सागर यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ाई की। उसके बाद उनका एक लंबा अनुभव है आईएएस के तौर पर। लेकिन ये उनका जो परिचय है आज हम उस हवाले से नहीं मिल रहे हैं। आज जो उनका रचनाकर्म है उसके बारे में बात करने के लिए। खासतौर पर उनकी जो कविताएँ हैं। जैसे कुछ मुझे बहुत पसंद है हम उन पर बात करने के लिए उनसे जुड़े हैं। और आखिर के हिस्से में आपलोग जो ये एपिसोड देख रहे हैं ऑनलाइन। आप भी अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। और कोशिश की जाएगी कि कुछ सवाल हम अशोक जी से पूछें उनमें से।
मैं सोचता हूँ कि आपसे मैं सिर्फ बुनियादी सवाल कुछ पूछूँगा जिसमें मेरी भी दिलचस्पी है और मुझे लगता है सुननेवालों की भी दिलचस्पी उन सवालों को आपसे उनका जवाब सुनने में होगी। मैं बहुत बेसिक सवाल पूछता हूँ कि आपके नजदीक कविता क्या है?
देखिए, इसके जितने कवि होंगे उतने उत्तर हो सकते हैं। हरेक का उत्तर ठीक भी होगा लेकिन जरूरी नहीं है कि दूसरे पर लागू हो। मैं अपनी बात कबीर की एक पंक्ति का सहारा लेकर करना चाहूँगा। कबीर ने कहा है–‘ताते अंधचिनहार मैं चिन्हा’, उससे यानी शब्द से मैंने जो अनचिन्हा था उसे चिन्हा। तो मैं ये कहूँगा कि मेरी कविता कोशिश रही है उसको चिन्हने की जो अक्सर अनचिन्हा चला जाता है। यानी कविता के कई काम होते हैं जो एक साथ करती है–एक काम है आसपास को दर्ज करना जो हो रहा है वो। दूसरा होता है उसका काम कि जो दी हुई सच्चाई है उसी को अंतिम सच्चाई न मानकर वैकल्पिक सच्चाई के बारे में भी सोचना। यानी सपना देखना। तो वो सच्चाई भी देखती है, सपना भी देखती है। और सिर्फ देखती नहीं है, उसको भाषा में चरितार्थ करती है, और सोचती है। कविता एक साथ कल्पना की भी विधा है, स्वप्न की भी विधा है, यथार्थ की भी विधा है और विचार की भी विधा है। अब ये आदर्श रूप है कविता का। मेरी कविता इस आदर्श पर कितनी खरी उतरती है ये काम दूसरों का है। मैं इस पर फैसला नहीं कर सकता, मैं अपनी कविता का खुद पारखी नहीं हो सकता।
ऐसी क्या चीज है जो कविता को उत्पन्न कर देती है और क्या चीज है जो जब नहीं होती है तो कविता नहीं होती है। यानी मैं ये पूछता हूँ कि जितने लोग कविता लिख रहे हैं या जितने कवि हैं क्या वो सब कविता को रच पा रहे हैं? मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या चीज या किस चीज के होने से कविता कविता हो जाती है या कविता कविता नहीं होती है?
देखिए एक तो ये है कि कविता तरह-तरह की होगी यानी एक तरह की कविता, जिस तरह की कविता मैं लिखता हूँ वो मेरे मित्र और बंधु विनोद कुमार शुक्ल वैसे नहीं लिखते। जिस तरह से विनोद कुमार शुक्ल लिखते हैं वैसे मसलन अभी दिवंगत हुए मंगलेश डबराल नहीं लिखते थे। तो ये अलग-अलग हरेक की शैली होती है, हरेक का मुहावरा होता है, एक बात। लेकिन कोई भी कविता जो टिकाऊ होने का दावा करे या जिसको टिकाऊ होने की आकांक्षा हो वो मेरे वक्तव्य से कविता नहीं बनती। ऐसे वक्त आते हैं और हमारा ऐसा वक्त है दुर्भाग्य से जिसमें सीधे-सीधे कहना जरूरी हो जाता है। यानी सपाट बयानी लेकर, शुद्ध अविधा। लेकिन कविता में अंतरध्वनियाँ होती हैं, व्यंजना होती हैं, वो हर बात सीधे-सीधे नहीं कहती है। कविता का सच वैसे भी अधूरा सच होता है। उसमें जब आप थोड़ा-सा अपना सच मिलाएँगे तब वो सच पूरा होगा। इसीलिए एक कविता की सतरह व्याख्याएँ हो सकती हैं क्योंकि सतरह पाठक उसमें अपना अलग-अलग सच मिलाएँगे। अब मुश्किल क्या है कि ज्यादातर कविता हर समय में, छायावाद में आपको याद होगा चार हजार से अधिक कवि रहे होंगे। बचे साढ़े चार तो बाकी कहाँ खो गए। तो ये हर समय में होता है, हर समय में बहुत खराब कविता लिखी जाती है। बहुत कविता लिखी जाती है जो कविता के नाम पर तो लिखी जाती है पर होती कविता नहीं है। क्योंकि उसमें कोई टिकाऊपन, कोई अप्रत्याशित कुछ ऐसा होता नहीं है। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि आज जो कविता लिखी जा रही है उसमें अच्छी कविता भी है और हमेशा की तरह बहुत खराब कविता भी है। अपनी खराबी को पहचानना भी बड़ा मुश्किल होता है। जो लोग आत्मरत होते हैं, आत्ममुग्ध होते हैं वो चाहे राजनेता हों, जो कि जिनका तो अब एक लहेड़ा ही पैदा हो गया है वो अपना सच न तो जानते हैं, न अपनी खराबी पहचानते हैं। और इसलिए कबाड़ा करते रहते हैं तो राजनीत का भी कबाड़ा करते है, कविता का भी कबाड़ा करते हैं।
कई बार हम ये सुनते हैं कि जो हमारे समय में हो रहा है यानी कि जैसा समाज है और जो राजनीति है तो हमें उसकी ध्वनियाँ कविता में लानी चाहिए, अगर कोई सोशल इश्यू है, या कोई पॉलीटिकल प्रॉब्लम है, कई बार कई कवि नहीं लाते हैं तो उनकी बहुत आलोचना करते हैं कि ये तो समय कुछ और है और ये कुछ और कविता लिख रहे हैं, प्रेम की कविता लिख रहे हैं। तो आपका इस पर क्या विचार है? क्या कविता के लिए अनिवार्य बाध्यता है कि हम जिस समय में हों उसकी सामाजिक, राजनैतिक ध्वनियाँ हमारी कविता में आएँ ही। और अगर नहीं आती हैं तो क्या कवि कोई अपराध करता है या नहीं करता है?
देखिए, आज दो तरह के समय हैं बल्कि तीन तरह के समय हैं। एक तो समय है जो आपका समय है जिसमें आप, आपके पूरा पड़ोस में, आपके जीवन में, आपके रोजमर्रा की सच्चाई में, आपके समाज में क्या हो रहा है। ये एक समय है। दूसरा समय है जो आपके स्मृति में है। यानी वो समय जो बीत चुका। लेकिन इसमें गालिब भी थे, मीर भी थे, तुलसीदास भी थे, सूरदास भी थे, निराला भी थे और मुक्तिबोध भी थे। जो समय बीत चुका है। ये भी कविता का ही समय है। इसका दबाव आज की कविता पर पड़ता है। और तीसरा समय है जो कविता स्वयं बनाती है। यानी ये हुए समय और उत्तराधिकृत समय दोनों से अपने को बावस्ता रखते हुए भी वो एक अलग समय रचने की कोशिश करती है। इस समय को रचने में अनेक आवाजें होती हैं, अनेक दबाव होते हैं, अनेक तनाव होते हैं। किसी कवि को एक आधार पर न तो माना जा सकता है, न खारिज किया जा सकता है कि उसने अपने समय को कैसे दर्ज किया। क्योंकि दर्ज करना सिर्फ विधा में दर्ज करना नहीं है। ये कोई रजिस्टर नहीं है जिसमें आप लिख दें कि मेरी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो रजिस्टर बनाए घूम रहे हैं और दूसरे लोग के नाम उसमें दाखिल खारिज करते रहते हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे ऐसे, शमशेर बहादुर सिंह जैसा कवि, सौंदर्य का कवि, सौंदर्य के लिए संघर्ष करने वाला कवि। तो क्या सौंदर्य का संघर्ष कोई कम संघर्ष है। उन्होंने राजनैतिक कविताएँ भी लिखीं, और ज्यादातर खराब लिखीं, वो अलग बात है। लेकिन क्या ये सही होगा कहना कि उनके सौंदर्य के संघर्ष को हम नजरअंदाज कर दें। उसको कूड़ेदान में फेंक दें, ये सही नहीं होगा। आप अंतरध्वनियों को, देखिए क्या होता है–कविता में, कविता थोड़ी तो शब्दों में होती है, बहुत सारी शब्दों के बीच की चुप्पियों में होती है। और उन चुप्पियों को भी समझ पाना, सुन पाना असली रसिक का काम है। और उसके लिए भी एक दीक्षा की जरूरत होती है। मतलब आप, जैसे शास्त्रीय संगीत है उसको सुनने के लिए आप फिल्मी गाने की तरह की रसिकता नहीं काम में ला सकते, फौरन आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। तो ये बात ध्यान में रखने की है। किसी भी कवि को इस आधार पर जाँचा नहीं जा सकता कि उसने अपने समय को सीधे-सीधे कितना दर्ज किया।
एक कविता हम सुन लेते हैं, क्योंकि बातें तो कविता पर हो रही है। लेकिन जब कविता सामने होगी तो बेहतर बात हो पाएगी। मेरी एक बहुत पसंदीदा कविता है, पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि ‘वो थोड़ा-सा आदमी’ वो कविता मुझे बहुत पसंद है। अगर आप वो सुना पाएँ और वो कविता भी इन्हीं सारे मूल्यों की बात करती है।
थोड़ा-सा
अगर बच सकेगा
तो वही बचेगा
हम सब में थोड़ा-सा आदमी
जो रौब के सामने नहीं गिड़गिड़ाता
अपने बच्चे के नंबर बढ़वाने नहीं जाता मास्टर के घर
जो रास्ते पर पड़े घायल को सब काम छोड़कर
सबसे पहले अस्पताल पहुँचाने का जतन करता है
जो अपने सामने हुई वारदात की गवाही देने से नहीं हिचकिचाता–
वही थोड़ा-सा आदमी
जो धोखा खाता है पर प्रेम करने से नहीं चूकता
जो अपनी बेटी के अच्छे शौक के लिए
दूसरे बच्चों को थिगड़े पहनने पर मजबूर नहीं करता
जो दूध में पानी मिलाने से हिचकता है,
जो अपनी चुपड़ी खाते हुए दूसरे की सूखी के बारे में सोचता है
वही थोड़ा-सा आदमी
जो बूढ़ों के पास बैठने से नहीं ऊबता
जो अपने घर को चीजों का गोदाम बनने से बचाता है
जो दु:ख को अर्जी में बदलने की मजबूरी पर दुखी होता है
और दुनिया को नरक बना देने के लिए दूसरों को ही नहीं कोसता
वही थोड़ा-सा आदमी जिसे खबर है कि
वृक्ष अपनी पत्तियों से गाता है अहरह एक हरा गान
आकाश लिखता है नक्षत्रों की झिलमिल में एक दीप्त वाक्य
पक्षी आँगन में बिखेर जाते हैं एक अज्ञात व्याकरण
वही थोड़ा-सा आदमी
अगर बच सका तो वही बचेगा।
आप देखें, इस कविता के बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहिए, अपनी कविता के बारे में तो खासकर नहीं। लेकिन बहरहाल इसमें, देखेंगे बहुत देर तक तो कविता जो है तथाकथित सामाजिक सच्चाइयों से घिरी हुई है। फिर एकाएक वो एक दूसरा मोड़ लेती है। हमारे यहाँ शास्त्र में अवचारित का रमणीय सुख यानी जो आपने सोचा नहीं है वो एकाएक प्रकट हो जाए, तो ये अप्रत्याशित का रमणीय क्या है कि आप वृक्ष, पक्षी, आकाश, आँगन इधर चले जाते हैं और जिस आदमी को वो सब सामाजिक सच्चाइयाँ उसको ये प्राकृतिक सच्चाइयाँ भी जानना, उनसे भी रू-ब-रू होना जरूरी है। तभी वो आदमी जितना थोड़ा-सा है उसकी आदमीयत बनी ही रहे। तो ये इसमें सामाजिक सच्चाई से नहीं होगा, ये इस दूसरी सच्चाई से भी होगा। मतलब कविता का वो ये करने की कोशिश कर रही है कितनी सफल, कितनी विफल होगी हम क्या जानें।
सर, मैं ये कह रहा था कि कविता जो है आप तक कैसे आई, या आप कविता की तरफ कैसे आए? अगर उस पसमंजर पर कुछ बात कर पाएँ, या बता पाएँ कि कैसे कविता आपके अंदर आई?
देखिए कविता कैसे आई, ये तो मुझे ठीक-ठीक पता नहीं है कब आ गई ससुरी। लेकिन जब मैं बहुत छोटा था, मैं अपने को अकाल परिपक्व व्यक्ति कहता हूँ, अब तो खैर परिपक्व भी बहुत हो गया लेकिन उस समय तो अकाल परिपक्व था। मैं सीधे ‘धर्मयुग’ और ‘ज्ञानोदय’, ‘युगचेतना’, ‘कल्पना’, ‘कृति’ इन पत्रिकाओं में जो साहित्यिक पत्रिकाएँ थीं, मैं उस समय अपने छात्र होने को छुपाता था, कहीं किसी को पता चल जाए कि बी.ए. फर्स्ट ईयर का छात्र है और कविता इतनी लिख रहा है तो कुछ गड़बड़ न हो जाए, तो बहरहाल। लेकिन हुआ ये था कि मेरी बचपन से, मैं अपने पिता का सबसे, मतलब माता-पिता का सबसे बड़ी संतान था। सबसे बड़ी जो संतान होती है वो हमेशा अकेली होती है क्योंकि दूसरों से उसकी दूरी कुछ ज्यादा ही हो जाती है। तो बड़ा मुझे शब्दों से खेलना कुछ सुहाने लगा, और हमारे एक अध्यापक थे उन्होंने मुझे अज्ञेय और दूसरे कवियों, ‘शेखर एक जीवनी’ वगैरह पढ़ने पर, साहित्य या ‘कल्पना’ जैसी पत्रिका देखने को दिए। उनका जब तबादला हुआ, वो जाने लगे तो उन्होंने मुझसे कहा देखो तुम्हारा परिवार तो प्रशासकों का है। (मेरे पिता विश्वविद्यालय में प्रशासक थे, मेरे नाना प्रशासक थे, मेरे मामा प्रशासक थे।) आना तो तुमको भारतीय प्रशासन सेवा में चाहिए, पर मरना कवि की तरह। तो अब पहला हिस्सा तो मैंने पूरा कर दिया। अब दूसरा तो बड़ा कठिन है। लेकिन बहरहाल फिर भी कोशिश करता रहता हूँ। मैंने अपने परिवार को लेकर भी बहुत कविताएँ लिखी हैं।
सर, मैंने जो लिखकर रखी थी एक कविता सुनने के लिए, सुनना चाहूँगा आपसे, वो कविता है–‘जब हम प्यार करते हैं’, और फिर मैं उस कविता के बाद कविता और प्रेम में क्या संबंध है? चूँकि आप वो कवि हैं जिनकी प्रेम की कविताएँ बड़ी अलग तरीके से उन्होंने अपनी जगह बनाई, तो मैं आपको इस विषय पर सुनना चाहता हूँ कि आप इसको कैसे देखते हैं? पहले अगर आप वो कविता सुना पाए!
असल में वो बहुत पुरानी कविता है। 1960 की कविता है। पहले पहले प्रेम की कविता है।
प्यार करते हुए सूर्य स्मरण
जब मेरे ओठों पर तुम्हारे ओठों की परछाइयाँ झुक आती हैं
और मेरी उँगलियाँ तुम्हारी उँगलियों की धूप में तपने लगती हैं
अब सिर्फ आँखें हैं कि प्रतिक्षा करती हैं मेरे लौटने की
उन दिनों में जब मैं नहीं जानता था कि दो हथेलियों के बीच
एक कुसुम होता है–सूर्य कुसुम
जब अँधेरे दरवाजे पर खड़े होकर तुम एक गीत अपने कंधों
से मेरी ओर उड़ा देती हो और मैं एक पेड़ की तरह खड़ा रहता हूँ
तब सिर्फ आँखें ही प्रतिक्षा करती हैं मेरे लौटने की
उन दिनों में जब मैं नहीं जानता था दो चेहरों के बीच
एक नदी होती है–सूर्य नदी
जब तुम मेरी बाँहों में साँझ रंग सी डूब जाती हो और मैं
जब बिंदुओं सा उभर आता हूँ तब सिर्फ आँखें हैं
जो सिर्फ प्रतीक्षा करती हैं मेरे लौटने की
उन दिनों में मैं नहीं जानता था दो देहों के बीच
एक आकाश होता है–सूर्य आकाश।
इस कविता की एक दिलचस्प कहानी है–मैं तब बी.ए. अंतिम वर्ष का छात्र था जब ये कविता लिखी थी, और उन दिनों ‘ज्ञानोदय’ कलकत्ते से निकलती थी और प्रतिष्ठित पत्रिका थी। तो ये कविता मैंने वहाँ भेजी। उन दिनों ‘ज्ञानोदय’ में कुछ प्रसिद्ध कवियों के स-वक्तव्य कविताएँ छप रही थीं। उसमें कुँवर नारायण, केदार नाथ सिंह, शमशेर बहादुर सिंह, वो हमारे प्रतिष्ठित कवि थे। एकाएक उनके संपादक का पत्र आया कि हम इसको स-व्याख्या कविता वाले सीरीज में छापेंगे। तो हमारी पहली, मतलब उन्नीस बरस में हमने स-व्याख्या लिखी। जब मैंने प्रेम की कविताएँ लिखी थीं तो हिंदी में कुछ ऐसा वातावरण बन गया था, सामाजिक यथार्थ इत्यादि के, आतंक में। निजता की कोई खास जगह नहीं रह गई थी और प्रेम निजता का सबसे सघन और उत्कट इजहार होता है। तो मैंने प्रेम कविताएँ लिखीं और उन प्रेम कविताओं को मैंने संस्कृत की परंपरा में सोचने की कोशिश की। अगर आप संस्कृत का प्रेमकाव्य देखें खासकर जो गीत काव्य है तो उसमें ये पता नहीं चलेगा कि, कौन है, कहाँ है, यानी उसमें वो सारे चिह्न मिटा दिए गए हैं और शुद्ध शृंगार है। और शृंगार बाद में वो रीतिकाव्य वगैरह में शृंगार को सह्य बनाने के लिए कृष्ण-राधा का आख्यान ले लिया गया है। लेकिन हमारी भारतीय शृंगार की परंपरा संसार की महान शृंगार परंपराओं में एक है। और सिर्फ संस्कृत में ही नहीं, संस्कृत में प्राकृत में, अपभ्रंश में और गीतिकाव्य में। इन सब में महान प्रेम कविता लिखी गई, अद्भुत प्रेम कविता लिखी गईं। लेकिन हमारे यहाँ सामाजिकता का ऐसा घटाटोप छाया, तब मुझे लगा कि इस घटाटोप में प्रतिपक्ष प्रेम कविता ही हो यानी निजता ही होगी। तो मैंने बूझकर और अगर आप थोड़ी सी जगह बनाएँ, उसमें देखें तो पृथ्वी, ब्रह्मांड, नदी, पर्वत, चट्टान ये जो उपादान हैं जिनका मैंने सहारा लिया है, उनसे कोई इस बात पर नहीं पहुँच सकता कि ये किसके बारे में लिखी गई हैं। यानी ये जो आसानी से फलाने के बारे में लिखी गई है, ठिकाने के बारे में लिखी गई है, ये सब चिह्न उसमें से गायब हैं। वह एक तरह से प्रेम कविता में अपनी जगह बना रहा है, बिना किसी इतिहास या भूगोल की चिंता किए, और उस उत्कटता को, जब आप प्रेम करते हैं तो ये थोड़े सोचते हैं कि हम कहाँ बीसवीं सदी के फलाने, उसमें हैं जिसमें भयानक। और आज आप प्रेम कविता लिखेंगे तो जो किसान संघर्ष चल रहा है उसको ध्यान में रख कर लिखेंगे या कि उसको भी प्रेम कविता में बदल सकते हैं क्या, यानी हुनर जो है, आपके कौशल में है।
मैं यही पूछना चाह रहा था कि जैसे जिस सामाजिकता के आधिक्य का और माहौल का आपने जिक्र किया, उस दौर में जब आपने प्रेम कविता लिखनी शुरू की, अभी भी हम ये देखते हैं कि उसको लेकर एक लाउडनेस तो है। वो जो कन्सर्न और वो हम सब अपने, जो हमारा साहित्यिक परिवेश है उसमें ये बातें सुनते हैं लेकिन आपको लगता है कि जो इस वक्त के कवि हैं, खास तौर पर जिसे हम मुख्य धारा की कविता या साहित्य की कविता मानते हैं; वो क्या कोई हस्तक्षेप कर पा रही है, इस दौर के तमाम सामाजिक, राजनैतिक आंदोलनों में, या कुछ बदल पा रही है जमीन पर, आपको लगता है ऐसा?
देखिए, ये ऐसा हस्तक्षेप करना और कुछ बदल पाना ये कविता का काम नहीं है। हो सकता है कभी कविता बड़ी कविता होगी वो वैसा कर पाए। लेकिन अगर आप, इस समय हिंदी प्रदेश, हिंदी भाषा-भाषी अंचल सबसे अधिक सांप्रदायिक, सबसे अधिक धर्मांध, हिंसा, हत्या, बलात्कार की मानसिकता से सबसे अधिक ग्रस्त, सबसे अधिक घृणा और भेदभाव में यकीन करनेवाला अंचल बन चुका है। इस अंचल में कबीर, रैदास, तुलसीदास, सूरदास इतने बड़े-बड़े कवि हुए हैं। गालिब, मीर इन कवियों का कोई प्रभाव बाकी नहीं। इनमें से किसी कवि को आप धर्मांधता, सांप्रदायिकता, हिंसा, हत्या, बलात्कार के पक्ष में उद्धृत नहीं कर सकते। हिंदी और उर्दू साहित्य की जो परंपरा है पिछले चार सौ, पाँच सौ वर्ष की वो परंपरा से इस समय हिंदी समाज पूरी तरह से विपथगामी हो चुका है। जब तुलसीदास और कबीर का प्रभाव नहीं बचा तो हम जैसे दुमछल्लों का कहाँ से बचेगा। इतने बड़े-बड़े कवि जो मान्य हैं जिनकी चौपाइयाँ आज भी लोग दोहराते हैं और इनके दोहे, लेकिन एक विचित्र किस्म का पाखंड पैदा हो गया है कि ये भी करते रहो, रामचरितमानस भी पढ़ते रहो, और बगल के मुसलमान को अगर मौका मिले तो छुरा भी मार दो। तो ये जो मानसिकता है, ये साहित्य ने एक जमाने में वो भूमिका संभवतः निभाई थी। लेकिन ऐसे वक्त आते हैं जब साहित्य वो भूमिका नहीं निभा सकता, निभा पाता एक बात। दूसरी बात कि हमको अपनी सच्चाई पर जिद करके अड़े रहना होता है। वो सच्चाई लोकप्रिय है या नहीं है, लोकप्रिय तो आजकल सारे हत्यारे बहुत लोकप्रिय हैं, वो तो सत्तारूढ़ हैं। इसलिए लोकप्रिय हैं, या इसको हमारे अध्यापक लोग अपने निंदनीय शोध ग्रंथों में शामिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इन सब कि चिंता किसी सच्चे कवि को नहीं होगी। कविता लिखना अपने आप में एक सामाजिक हस्तक्षेप है। उसको अलग से हस्तक्षेप करने के लिए प्रेरित करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसी कविता होती है और उसकी जरूरत भी होती है जो सीधे-सीधे लोगों को संबोधित करे और उनको भी सकर्मकता की ओर ले जाए। लेकिन बहरहाल मैं ऐसा कवि नहीं हूँ, लेकिन ऐसे कवि जो हैं मैं उनकी अवमानना भी नहीं करता। लेकिन जब कविता विरोधी समय हो। इससे अधिक कविता विरोधी समय क्या होगा जो आज है। उस समय कविता पर जिद करके अड़े रहना, अपनी शर्तों पर अड़े रहना, अकेले पड़ने से न घबड़ाना, ये भी एक साहसिक कर्म है।
सर, ये बात उस दौर में बहुत अहम हो जाती है जब हम ये देखें कि हमारा समाज है वो कविता से कटा हुआ है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कविता को पढ़नेवाले या कवियों को जाननेवाले जैसे कविता को जानना चाहिए और जैसे कवि को जानना चाहिए समाज में उस तरह की चेतना तो नहीं है। मतलब जो लोग कविताएँ पढ़ते हैं, जैसे आप तो इतने स्वीकृत कवि भी हैं, साहित्यिक संसार में लोकप्रिय भी हैं अपनी तरह से, लेकिन फिर भी हम देखें कि जिस तरह से कविता हमारे समाज में होनी चाहिए, किसी भी समाज में होनी चाहिए वैसे कविता नहीं है, तो ये अवस्था मायूसी न पैदा करे इसके लिए आपसी वो बात बहुत अहम है कि हमें कविता पर अड़े रहना चाहिए।
मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि कविता में रुचि जो है वो अपने आप पैदा नहीं होती है। जैसे कविता पेड़ों पर नहीं लगी होती है कि आप जाकर पत्तियों की तरह चुनकर ले आएँ। ठीक उसी तरह से रुचि को भी विकसित करने की, बनाने की जरूरत होती है। मुझमें ही कविता की रुचि कैसे आई–एक छोटे शहर में सरकारी स्कूल में पढ़ता हुआ एक तेरह बरस का लड़का, उसको एक अध्यापक कहता है कि इस समय ‘कल्पना’ नाम की पत्रिका निकल रही है जो जिला पुस्तकालय में है उसको पढ़ो। मेरा जब राजापुर गरहेवा में उपनयन संस्कार होता है तो मुझे वो पुस्तकों का एक पैकेट भेजता है उपहार के रूप में, जिसमें ‘हरी घास पर क्षण भर’ अज्ञेय का कविता संग्रह, पंत जी का दो कविता संग्रह, रवींद्रनाथ का ‘गीतांजलि’ का अँग्रेजी अनुवाद और ‘शेखर एक जीवनी’ के दो भाग हैं। ये था अध्यापक का काम। देखें, आप कि मुझे कहाँ से प्रेरित किया उन्होंने। तो ये शिक्षा संस्थाएँ, शिक्षक इनका काम है कि ये रुचि बनाएँ। दूसरी तरह ये इस कदर इस रुचि को भ्रष्ट करते हैं, सबने ये फैला रखा है कि कविता तो सिर्फ भावोच्छवास का मामला है, क्योंकि कविता में बुद्धि की कोई जरूरत नहीं है। अरे तुलसीदास जैसा बड़ा कवि बिना बुद्धि के संभव है! प्रसाद और निराला जैसे बड़े कवि क्या बिना बुद्धि के संभव हैं। कबीर का ‘द्रोह’ क्या बिना बुद्धि के संभव है। तो कविता का काम नहीं होता, कविता के लिए जैसे कवि को व्यक्त करना पड़ता है, वैसे ही रसिक को भी करना पड़ेगा। आप गालिब और मीर की कविता बिना उस परंपरा को समझे, जाने, देखे उसे कैसे जान लेंगे। और गालिब ने सीधे-सीधे अपने समय के बारे में कविता नहीं लिखी, लेकिन जाहिर है गालिब में वो समय बोलता है, वो मीर में भी बोलता है, वो निराला में और मैथिलीशरण गुप्त सब में बोलता है। लेकिन उस समय को पहचानने की जरूरत है। वो सीधा-सीधा समय नहीं है।
हम बात कर रहे थे कि किस तरह से साहित्यिक रुचियाँ भ्रष्ट की गईं। चूँकि आप एक प्रशासक भी रहे हैं, आईएएस अधिकारी भी रहे हैं और आपका एक करिश्मा भारत भवन के तौर पर सामने आया था एक जमाने में और आज भी वो कायम है। आपको क्या लगता है कि हमारे यहाँ चूँकि प्रशासन की बहुत महत्त्वपूर्ण भूमिका है, वो एक पावर है उसके पास तो वह किसी तरह की भूमिका निभाता है या विफल हो जाता है उसमें। अपने उस अनुभव के बारे में आपसे जानना चाह रहा हूँ।
प्रशासन और राजनीति दोनों में इस समय शिक्षा का एक बहुत उपक्रमनात्मक रूप ही रूढ़ हो गया है। साहित्य पढ़ने से क्या होता है, नौकरी नहीं मिलती, इस तरह के बहुत सारी बातें आप सुनेंगे, और स्वतः शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे रोजगार मिले। हमलोग जब पढ़ते थे, हमने जब साहित्य पढ़ना, मैं तो साइंस का विद्यार्थी था, और आपको लगता होगा कि मैं फटीचर हूँ। मैं साइंस में यूनिवर्सिटी में टॉप किया और फिर ये तय किया कि मैं तो बी.ए. करूँगा। मैंने बी.ए. में फिर टॉप किया। फिर तय किया कि मैं अँग्रेजी साहित्य में एम.ए. करूँगा तो मैं दिल्ली आया। तो ये अवसर मिले जो छात्र, सब छात्र साहित्य पढ़ने लग जाएँगे ऐसा तो जरूरी नहीं है। लेकिन स्कूल के स्तर पर हमारी हिंदी की शिक्षा का जो अंधकूप है वो स्कूल है। और अगर आप बच्चों से पूछें कि उनके सबसे खराब अध्यापक कौन से हैं तो उनमें से ज्यादातर अपने हिंदी अध्यापक या अध्यापिका का नाम लेगा। जिन्होंने भाषा में रस लेने की, भाषा को सुख पाने की, उसमें जो स्वाभाविक छंदमयता है उसमें उसको समझ पाने की सारी, कोई इच्छा ही नहीं दिखती, कोई क्षमता ही नहीं विकसित करते। तो ये प्रशासन का काम है कि वो ऐसी शैक्षणिक नीति भी बनाए। हमने कोशिश की थी कि उस जमाने में, मसलन मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ–हमारे समाज में बड़ी लोकसंपदा है, हमने ये तय किया, मैं लोकशिक्षण संचालक था, और हमारे लगभग तीन लाख अध्यापक, मध्यप्रदेश में उस समय और उसमें से कम से कम एक लाख अध्यापक स्कूलों में थे। मैंने कहा हर स्कूल का अध्यापक अपने आसपास के दो लोकगीत जमा करे, जिस बोली में है उसमें लिख दे, उसका हिंदी में भावार्थ लिखे। तो अगर एक लाख शिक्षकों ने ये किया होता तो दो लाख लोकगीत एकत्र हुए होते। अब हुआ ये कि मेरा उस समय वहाँ जो हमारे मंत्री थे वो संघी थे तो उनसे बात बनती नहीं थी। मूर्ख भी थे जैसे कि अकसर संघी होते ही हैं। उन्होंने हटा दिया मुझे, तो मैं हट गया। फिर ये योजना धरी रह गई। फिर मैंने पुस्तकें खरीद कीं। पुस्तक खरीद की शुरुआत मैंने ही की थी, लेकिन जब उसमें ही भ्रष्टाचार होने लगा तो मैंने उसको बंद कर दिया और विज्ञान की प्रयोगशालाओं के लिए वो सारी राशि दे दी। पर डेढ़-दो करोड़ की पुस्तकें खरीदी गई थीं ताकि अध्यापकों का भी तो बौद्धिक उन्नयन हो, वो भी तो जानें कि इस समय क्या हो रहा है साहित्य में। तो ये सब बहुत सारे ऐसे निर्णय हैं जो की जा सकती थी।
आम तौर पर हमारा जो मंत्रालय है या जो डिपार्टमेंट है साहित्य संस्कृति का, उसमें जैसे कि आईएएस जाते हैं प्रशासक बन के। अब आईएएस आप जैसा हो तब तो ठीक है। उसकी एक रुचि है, वो समझता है, परंपरा को भी जानता है, खुद भी कवि है, साहित्यकार है। लेकिन आमतौर पर सारे आईएएस के साथ तो ये मुमकिन नहीं है या सारे राजनेताओं के साथ ये मुमकिन नहीं है कि वो दिलचस्पी रखते हों साहित्य या संस्कृति में, लेकिन अब वो ये जिम्मेदारी सँभाल लेते हैं। हमें लगता है कि उसका तो बड़ा खराब असर पड़ता होगा, इसीलिए शायद ये जो इदारे बने हुए हैं वो उस तरह का रोल नहीं निभा पा रहे हैं।
देखिए हिंदी भाषी अंचल में सांस्कृतिक संस्थाएँ चाहें वो गैरसरकारी हों, चाहे सरकारी हों, जैसे–नागरीप्रचारिणी सभा, हिंदी साहित्य सम्मेलन ये सब निजी पहल पर बने थे। ये गैर सरकारी इदारें थीं। वो सब नष्ट हो गए–उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान और बाकी राज्यों में भी कुल मिलाकर हालत यही है। क्योंकि संस्कृति का काम हास्य का काम समझा जाता है। हम तो हास्य के ही प्रशासक थे। हमने तो हास्य को ही अपने केंद्र में रखा था। हमने कोई आकांक्षा नहीं की थी कि हमको वाणिज्य उभार मिल जाए या ऐसा कोई बड़ा उभार मिल जाए जिससे हम बहुत बड़े तानाशाह बन जाएँ या बहुत बड़े नौकरशाह बन जाएँ। हमने अपने लिए चुना ही ये था। अब ये तो इस पर निर्भर करता है कि क्या हमारा ऐसा मध्यवर्ग पैदा हो गया है जिसको अपनी संस्कृति की न तो समझ है, न चिंता है। अगर ऐसा मध्यवर्ग अंततः बन गया है तो फिर किसी तरह की उम्मीद करना, अपवाद होंगे इधर-उधर।
सर, आपके लिए अनेक सवाल आ रहे हैं। एक सवाल संजय पटेल जी का है। वो ये कह रहे हैं कि नई कविता को जितना अच्छा आप पढ़ते हैं, उतना अन्यत्र सुनाई नहीं देता है, क्या नई कविता की जन कविता न होने का कारण ये भी है कि वो अच्छी पढ़ी, यानी की सुनाई नहीं जाती।
देखिए, हमने ये प्रयोग किया था, मध्य प्रदेश में। मैंने कम से कम कविता पाठ के सौ से अधिक आयोजन किए। बहुत सारे शहरों में किए–इंदौर में, उज्जैन में, सागर में, जबलपुर में, रायपुर में, बिलासपुर में। और ये जो तथाकथित नई कविता वाले लोग हैं इन्हीं को भेजा पढ़ने, और इसके बहुत अच्छे परिणाम सामने आए। एक बार जब आप कविता कवि के मुख से सुनते हैं तो उससे फर्क पड़ता है। क्योंकि ऐसी कई अर्थ-छवियाँ और अंतरध्वनियाँ आपके मन में उभरती हैं, जो सिर्फ पढ़ने से नहीं होती, वो तो जड़-विजलित सा है, इसलिए ये प्रयोग न ठीक है। देखिए जन कविता तो एक व्यर्थ का मुहावरा है। जनकवि तो वो होते थे एक जमाने में और अक्सर लोकप्रिय कवि। हिंदी में कविता, अच्छी कविता और खराब कविता के बीच वैसा ही विभाजन हो गया है जैसे शास्त्रीय संगीत और फिल्मी संगीत के बीच। तो अच्छी कविता समझने की, अच्छी कविता के पास जाने की एक जुगत तो ये है कि आपको वो सुनाई दे। शायद इन माध्यमों का एक उपयोग ये भी हो रहा होगा कि उससे कुछ लोग की रुचि जाग रही होगी, मैं जानता नहीं हूँ कि ऐसा हो रहा है कि नहीं, लेकिन ऐसी अटकल लगाना अच्छा लगेगा। दूसरी तरफ बहुत सारी खराब कविता हर जमाने में लिखी गई है तो इसी जमाने में कैसे सारी कविता अच्छी लिखी जाएगी?
संवाद का विडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक करें : https://www.youtube.com/live/ulPiLtf76T4?feature=shared