प्रभाकर माचवे
शेयर करे close
शेयर करे close
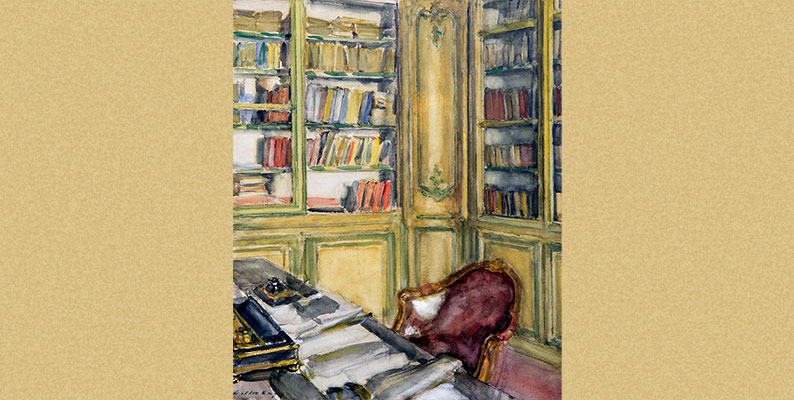
शेयर करे close
- 1 August, 1953
प्रभाकर माचवे
विनयनगर
9-5-53
प्रिय ललित सहगल जी,
क्षमा करें! रेडियो के काम से सहसा मुझे शनिवार-रविवार को वृंदावन जाना पड़ रहा है। कृपया मंगलवार तारीख 12 मई को सुबह जितनी जल्दी आ सकें, आ जाइए!
आपका
प्रभाकर माचवे
× × × ×
मंगलवार 12 मई को सुबह 7 बजे ही मैं उनके घर पहुँच गया। श्रीमती माचवे जी ने मुझे बैठने को कहा और स्वयं उन्हें बुलाने अंदर चली गईं।
कमरे में दाईं ओर पुस्तकों से भरी एक आलमारी रखी हुई थी। दरवाजे के ठीक सामने एक दरी पर हिंदी की पच्चीसों पत्रिकाएँ और कुछ मराठी, अँग्रेजी तथा फ्रेंच पत्र-पत्रिकाओं के मई के अंक बिखरे पड़े थे। उनके आने तक मैं पत्र-पत्रिकाओं में उलझा रहा, सामने एक छोटा-सा पुस्तकों का रैक था जिसमें उनके दो लघु-उपन्यास ‘परंतु’ और ‘एकतारा’ भी करीने से रखे हुए थे।
थोड़ी देर में ही उन्होंने हाथ में चाय के प्याले लिए कमरे में प्रवेश किया। अभिवादन के बाद हम चार-पाँच मिनट तक चायपान में मग्न रहे। इतने में एक और सज्जन भी आ गए। हमारी बातचीत शुरू होने वाली ही थी कि साहित्य-रत्न की एक छात्रा, जो आकृति से दक्षिण की लगती थीं, अंदर आईं और कुछ देर तक ‘अज्ञेय’ के ‘नदी के द्वीप’ पर बातचीत चलती रही…
और आखिर हमारी बातचीत शुरू हो ही गई :
“माचवे जी, आपके साहित्यिक क्षेत्र में प्रवेश करने की क्या पृष्ठभूमि है?” मैंने पहला प्रश्न किया।
“पृष्ठ-भूमि?” माचवे जी ने अपने आप प्रश्न को दुहराया और फिर कहना शुरू किया, “जब मैं विद्यार्थी ही था, मैंने साहित्यिक-क्षेत्र में प्रवेश किया। घर में मेरे बड़े भाई मराठी छंद-शास्त्र के जानकार थे। उन्हीं से मैंने छंद-शास्त्र का ज्ञान बहुत बचपन में यानी 12 वर्ष की आयु में प्राप्त किया। सन् 33 में श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी ने ‘कर्मवीर’ में लगभग 6 पंक्तियों की मेरी कविता को स्थान दिया…”
वह अभी पूरा उत्तर दे भी न पाए थे कि मैंने बीच में ही प्रश्न किया, “तो इस हिसाब से आपकी वही कविता सर्वप्रथम प्रकाश में आई?”
“हाँ,” वह बोले, “हिंदी में लिखना कविता से ही आरंभ हुआ था। ब्रजभाषा भी बहुत अच्छी लगती थी। बाद में सन् 36 में प्रेमचंद जी ने मराठी से हिंदी में अनुवाद करने तथा मराठी कृतियों की आलोचना करने का परामर्श दिया। इंदौर क्रिश्चिचयन कॉलेज में जब मैं बी.ए. में ही था, प्रथम कहानियाँ ‘मोमबत्ती’ और ‘दानिश’ के नाम से छपीं…”
मैंने तुरंत ही प्रश्न किया, “प्रारंभ में आपने, संभवत:, मराठी में ही लिखा-पढ़ा होगा, फिर आप हिंदी-साहित्य में किन बातों से प्रभावित होकर मुड़े?”
“मेरा तमाम वातावरण ही हिंदी का था। रतलाम के हाई स्कूल में मैट्रिक तक हिंदी पढ़ी। मालवा हिंदी प्रांत है। इसी कारण से हिंदी में स्वाभाविक रुचि पैदा हुई। उधर मैंने इंदौर से विशारद किया। मराठी तो, सहगल जी, मातृ-भाषा है।”
देश-विदेश के किन-किन लेखकों का उन पर प्रभाव पड़ा और कौन-कौन से लेखक उनको क्यों अच्छे लगे?–इस विषय पर उन्होंने बताया, “वैसे तो बहुत लेखकों को मैंने पढ़ा है। आप यूँ चलिए–मैट्रिक तक तो मैं शब्द-माधुर्य से प्रभावित था। इसी कारण से प्रसाद, पंत नाद-मधुरता के कारण मुझे प्रिय थे। इंटर में आकर गुरुदेव रवींद्रनाथ ठाकुर का पूरा साहित्य पढ़ा। इसके लिए बंगला भी पढ़ी। उन्हीं दिनों मराठी के उपन्यास भी बहुत पढ़े। कई दिनों तक जर्मन दार्शनिक नीट्ज्शे का कायल था।
“आगरा आकर उर्दू-फारसी कविता पढ़ने का शौक लगा। 37 में उन्नीस वर्ष की आयु में आगरा विश्वविद्यालय से दर्शन में एम.ए. किया। उत्तीर्ण छात्रों में मेरा प्रथम स्थान था। बर्नार्ड शॉ से मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। निबंधों में बहुत रुचि है। धीरे-धीरे सब ललित कलाओं में रुचि पैदा हो गई। संगीत, चित्र, स्थापत्य, शिल्पकला आदि में बड़ा शौक था। ‘साहित्य में ललित कला भाव’ पर तो एक प्रबंध सन्’ 35 के मराठी साहित्य सम्मेलन में पढ़ा था मैंने…”
उनका कहना जारी था, “अमलनेर की फिलॉसॉफिकल रिसर्च इंस्टिट्यूट में सौंदर्य-शास्त्र पर डॉक्टरेट करने के विचार से और पढ़ा भी, मगर फिर विचार बदल गया। बाद में मैंने मजदूरों में काम किया और ‘संघर्ष’ (लखनऊ) में दर्जनों कहानियाँ लिखीं। तब से ही समाजवाद की ओर मैं आकृष्ट हो गया। मनोविज्ञान का तो मैं अध्यापक था ही। अनेक भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करने में भी मेरा हृदय बड़ा रमता था। इसीलिए उत्तर भारत की प्राय: सारी भाषाएँ, यथा–हिंदी, मराठी, बंगाली, गुजराती और उनकी माताएँ संस्कृत, मागधी, पाली आदि सीखीं। इस प्रकार किसी एक लेखक विशेष का ही मुझ पर प्रभाव पड़ा हो–यह मैं नहीं कह सकता।”
इतने में उनके सुपुत्र उनकी गोदी में आकर चढ़ गए। वह उसे मराठी में ही कुछ कहते रहे जिसे मैंने ऐसा समझा–“भई, मैं उनकी बातों का उत्तर दे रहा हूँ, तुम जाओ और खेलो!”
मैंने पूछा, “आपके प्रकाशित साहित्य पर अधिकांश आलोचकों की क्या राय है?”
“किसी ने आलोचना ही नहीं की,” उन्होंने तुरंत उत्तर दिया, फिर जरा रुककर धीरे-धीरे कहना आरंभ किया, “हाँ, ‘तार सप्तक’ और ‘संगीनों का साया’ पुस्तकों की अच्छी आलोचना हुई। ‘संगीनों का साया’ तो प्रगतिशील पुस्तक थी, इसलिए पत्र-पत्रिकाओं में इसकी खूब चर्चा रही। शमशेर बहादुर सिंह ने ‘तार सप्तक’ में मेरी कविताओं पर एक जगह आलोचना करते लिखा है, ‘अब बहुत है।’ नंददुलारे वाजपेयी और डॉ. नगेंद्र ने एक कविता की कुछ पंक्तियों का उद्धरण देकर लिखा है, ‘यह भी कोई कविता है?’ सन् 48 में ‘तार सप्तक’ के बाद राहुल जी के साथ 6 महीने तक मैंने 16,000 शब्दों का शासन-शब्द-कोश तैयार कराने में काम किया। आठ प्रांतों में घूमा–तब शब्दों से काफी माथा-पच्ची की।”
बातचीत में विराम-चिह्न कहीं नहीं लगा।
“आपके साहित्य-प्रकाशन का उद्देश्य क्या है?”
माचवे जी बोले, “पत्र-पत्रिका में जब लोग लेख माँगते हैं, तब लिख देता हूँ। मन से जो लिखा, उसको प्रकाशन नहीं मिला। जैसे मेरी 500 अच्छी कविताएँ, 200 कहानियाँ, 60 नाटक और 50 ललित-निबंध पुस्तकाकार अभी तक नहीं छपे। पत्र-पत्रिकाओं में छपकर बिखरे हुए हैं।”
“क्या आप अपने को शत-प्रतिशत साहित्यिक समझते हैं?”
तत्क्षण उत्तर मिला, “बिल्कुल नहीं। अपने को साहित्यिक बता कर परेड करना मेरा उद्देश्य नहीं।”
“आपकी दृष्टि से साहित्य का क्या उद्देश्य है?”
“इस विषय पर मैं एक बार पहले भी अपने विचार प्रकट कर चुका हूँ। वे ऐसे थे–व्यक्ति की मानसिक रूढ़ियों से, समाज की जड़-धारणाओं से और राष्ट्र की अर्थ-दासता से मुक्ति ही साहित्य का उद्देश्य है। इसलिए साहित्य केवल कला के लिए कला या रस के लिए रसवाद नहीं हो सकता। वह व्यक्ति के मन का विलास नहीं, उसका सामाजिक दायित्व भी है।”
“जब आपने लिखना आरंभ किया था–उन प्रारंभिक दिनों की पत्र-पत्रिकाओं, विचारधाराओं और मान्यताओं में आज कितना अंतर आ पाया है?” मैंने पूछा!
“बहुत ज्यादा अंतर है। तब साहित्य के प्रति लोगों में ईमानदारी और पवित्रता थी। आज लेखक, संपादक और प्रकाशक सभी व्यापारी हो गए हैं। दो-चार पत्रिकाएँ ही ऐसी नजर में आती हैं जिनमें लगता है कि लेखक जागरूक हैं। बाकी पत्रिकाएँ तो सस्ती भूख को मिटाने की एकमात्र साधन हैं। मजा तो यह है कि सरस्वती, विशाल भारत जैसी उच्च पत्रिकाएँ भी आज उस स्टैंडर्ड की नहीं रहीं।”
समय काफ़ी हो गया था। माचवे जी को रेडियो भी जाना था। अत: बातचीत को बिना किसी गत्यवरोध के चलाये जाना अनिवार्य हो गया।
“आपके दृष्टिकोण से साहित्य में यथार्थ और कल्पना का क्या महत्त्व है?”
वह बोले, “यथार्थ का एक इतिहास है। पहले इसमें केवल हूबहू यथार्थ (Photographic realism) होता था जिसमें सूक्ष्म से सूक्ष्मतर चीजों का वर्णन होता था। फिर प्रकृतिवादी यथार्थवाद (Natural realism) आया जिसके लेखकों में फ्रांस के मोपासाँ और बाल्जाक आदि थे। तीसरी मंजिल थी सामाजिक यथार्थ (Social realism) की और चौथी है अतियथार्थवाद की। अतियथार्थवाद में लेखक केवल बाहर ही की नहीं, अंदर-बाहर की चीजों को एक साथ छूता है!
“यहाँ मुझे उर्दू की एक पंक्ति याद आ गई। वह यों है–‘कुछ ख्वाब है, कुछ अस्ल है, कुछ तर्जे अदा भी’। केवल यथार्थ ही साहित्य नहीं कहला सकता। इसलिए उसमें कल्पना का योग भी जरूरी है। बार-बार जिस साहित्य को पढ़ने की इच्छा हो, वही साहित्य नवोन्मेषशाली साहित्य है।”
“राजनीति और साहित्य में साम्य का क्या महत्त्व है?”
संक्षिप्त-सा उत्तर मिला, “राजनीति कभी भी साहित्य की परवाह नहीं करती। इस तरह राजनीति और साहित्य में साम्य का कुछ अधिक महत्त्व नहीं है। पश्चिम में, हाँ, कुछ ऐसा साम्य अवश्य अधिक दृष्टिगोचर होता है।”
“प्रतीकवाद, प्रयोगवाद और प्रगतिवाद के विषय में आपका क्या अभिमत है?”
“प्रतीकवाद और प्रयोगवाद कोई अलग-अलग चीजें नहीं। यूरोप में अवश्य थीं। 43 में ‘तार सप्तक’ निकला। यह प्रयोगवाद का आरंभ था। ‘दूसरा सप्तक’ ‘तार सप्तक’ से कुछ हल्का है। प्रयोगवाद का भविष्य उज्ज्वल है। प्रगतिवाद का आरंभ तो अच्छे ढंग से हुआ था, लेकिन इन प्रगतिवादी लेखकों में से कुछ फिल्म में चले गए। इन्होंने फिल्म में तो कुछ लिखा और साहित्य में कुछ और।” यहाँ उन्होंने शब्दों पर जोर देते हुए कहा, “कला में सबसे पहले संस्कृति का पतन दृष्टिगोचर हो जाता है।”
“आप किन क्षणों में रची हुई रचना को श्रेष्ठ मानते हैं?”
माचवे जी ने कहा, “अनुभूति और अभिव्यक्ति का सामंजस्य ही वे क्षण हैं, जब श्रेष्ठ रचना रची जाती है।”
हमारी बातचीत समाप्ति के स्तर पर ही थी।
मैंने पूछा, “साहित्य के प्राचीन मान-मूल्यों और स्थापनाओं का वर्तमान साहित्य में क्या कुछ मूल्य है?”
“इसका उत्तर इलियट के शब्दों में ठीक होगा–क्षण और युग का सत्य जिस बिंदु पर आकर मिलता है, वही सर्वोत्कृष्ट साहित्य का उत्स है।”
इतने में माचवे जी को बाजार से कुछ लाने का आदेश मिला। चलते-चलते मैंने पूछा, “लघु-उपन्यास प्रकाशित कराने का आपका क्या उद्देश्य है।”
वह बोले, “मैं अभी तक प्रकाशन के लिए किसी प्रकाशक के पास नहीं गया हूँ। प्रकाशक आ गया, सहज भाव से ले गया। मैं यह समझता हूँ कि बड़े-बड़े उपन्यासों की जगह जनता में लघु-उपन्यासों की माँग अधिक है। पश्चिम में भी ऐसा है। इसीलिए लघु-उपन्यास मुझे पसंद हैं। जैसे–डॉ. देवराज का लंबा उपन्यास ‘पथ की खोज’ है–बहुत कम लोग को धीरज होगा कि उसे पूरा पढ़ जाएँ, और फिर भई, यह तो व्यक्तिगत रुचि की बात है।”
हम घर से बाहर आ गए थे। बातचीत तो समाप्त हो ही चुकी थी। माचवे जी मुझे ‘बस-स्टैंड’ तक छोड़ने आए। संयोग से ‘बस’ उसी समय मिल गई और मैं उनको धन्यवाद देता हुआ ‘बस’ पर चढ़ गया।
Original Image: ibrary-at-Chateau-du-Breau
Image Source: WikiArt
Artist: Walter Gay WikiAr
Image in Public Domain
This is a Modified version of the Original Artwork