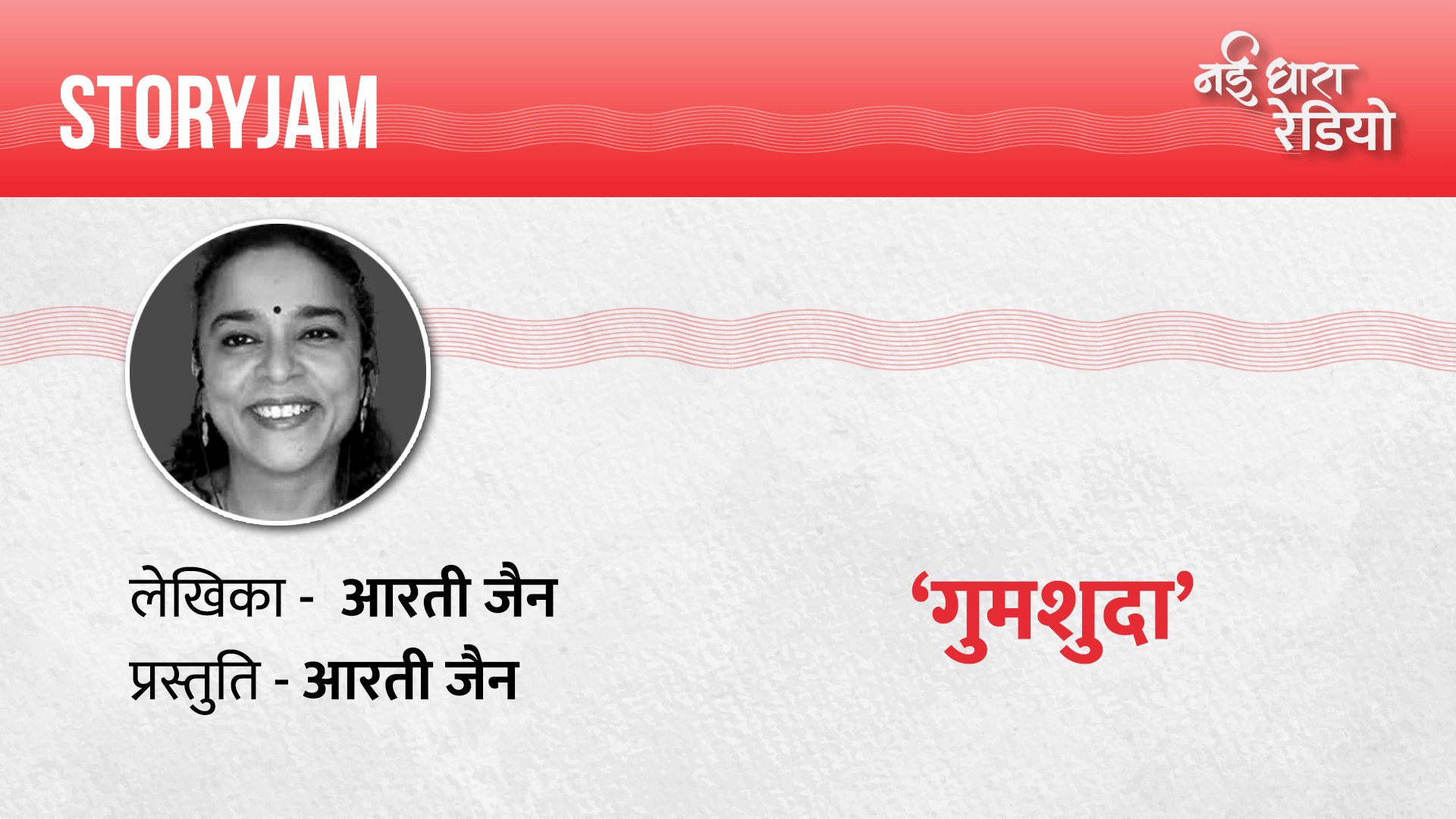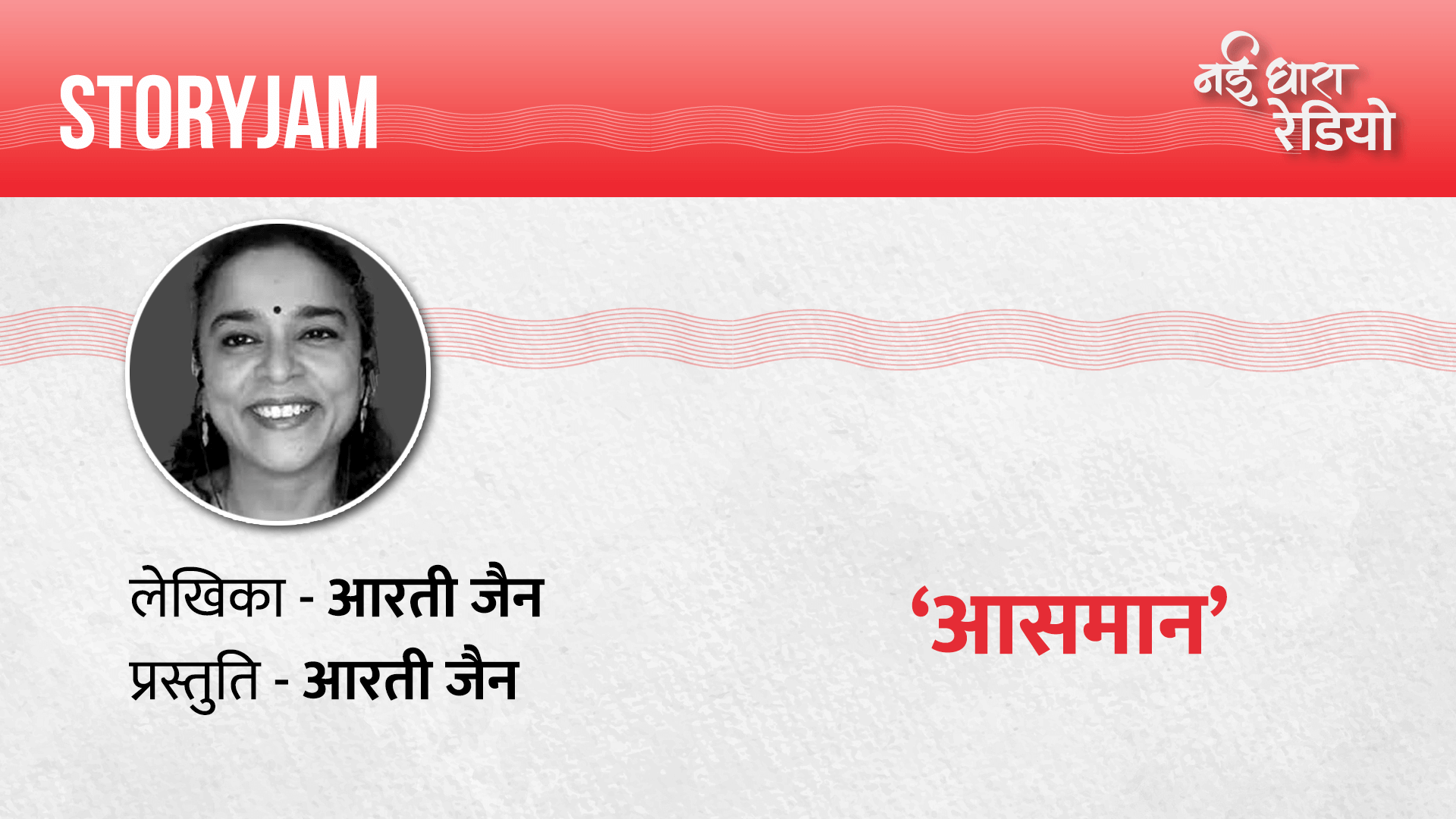नई धारा संवाद : सूर्यबाला (कथा-लेखिका)
शेयर करे close
शेयर करे close

शेयर करे close
- 1 October, 2021
नई धारा संवाद : सूर्यबाला (कथा-लेखिका)
(व्यंग्य बहुत सकारात्मक विधा है)
कथा साहित्य और समकालीन व्यंग्य में एक जाना-माना नाम है डॉ. सूर्यबाला का। अपने छह उपन्यास, पंद्रह कथा-संग्रह और चार व्यंग्य-संग्रह में सूर्यबाला जी ने अलग-अलग रूप से मध्यवर्ग के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पक्षों को दर्शाया है। अपनी रचनाओं और उनकी विविधताओं के लिए वह जानी गईं। आज इसी पर हम उनसे चर्चा करेंगे और साथ ही सुनेंगे उन्हीं के द्वारा उनकी कुछ रचनाओं का पाठ।
सबसे पहला प्रश्न मैं आपसे यही करना चाहती हूँ, आपका जन्म हुआ वाराणसी में जो लेखन और विद्या की एक प्रमुख नगरी है, और यहीं से आपने भी अपने लेखन की यात्रा शुरू की तो अपने बचपन के बारे में और लेखन की शुरुआत के बारे में कुछ बताइए।
बचपन तो बहुत अच्छा था आरती, अभी भी नहीं लगता कि वह बचपन बीता हुआ है और इतने वर्ष हो गए, लेकिन आपको बताऊँ कि मेरा बचपन, मेरी पीढ़ी की जो स्त्रियाँ हैं या मेरी पीढ़ी के जो लोग हैं उनसे काफी अलग रहा है। इस तरह अलग रहा है, उसमें एक तो हम थे मध्यवर्गीय, पिता शिक्षा अधिकारी थे उस समय, लेकिन वे बहुत शौकीन थे, बहुत जिंदादिल थे, बहुत शंजिदे थे और हर कुछ इंज्वाय करने वाले थे, मतलब हारमोनियम बजाते, बाँसुरी भी बजाते थे और आपको ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि हमारे आँगन में एक फव्वारा हुआ करता था। आपने आजतक किसी मध्यवर्गीय परिवार के आँगन में ऊँचा-सा लंबा फव्वारा नहीं देखा होगा, और फव्वारे के नीचे रंग-बिरंगी मछलियाँ तैरती होती थीं, चारों तरफ सबसे अच्छे प्रोटन लगे होते थे। तो इसके बीच में हम चार बहनें थीं और हमें बड़े लाड़-प्यार में पाला जाता था। माँ-पिता के बीच में बहुत अच्छी हारमनी थी, और हमें कभी भी ये नहीं कहा गया कि चार बेटियाँ। सोचिए उस जमाने की, चार बहनें बड़ी-छोटी बच्चियाँ, कि तुम्हें दूसरे घर जाना है, चूल्हा-चौका, रोटी बनाना सीख लो या कढ़ाई-सिलाई-फराई सीख लो या पराये घर का कोई खौफ नहीं। तो बड़ा अच्छा सा बचपन था और आपको एक बात बताऊँ, पिता शेरो-शायरी भी करते थे। अभी भी एक लाइन मुझे याद है–उठो हिंदवालों हुआ है सबेरा, तो ऐसे बचपन के बीच हम मध्यवर्गीय शहजादियों की तरह पाले गए, लेकिन ये बचपन थोड़े छोटा ही रहा, सचमुच छोटा बचपन रहा, अचानक हमारे सिर से उस पिता का साया उठ गया। बसंतपंचमी की एक रात पिता नहीं रहे और आप सोचिए कि बयालीस वर्ष की मेरी माँ, चार बड़ी-छोटी बच्चियों और एक ढाई वर्ष के बेटे के साथ उस फव्वारे और मछली वाले घर में अकेली खड़ी थी जैसे कहर टूटता है, जैसे बिजली गिरती है। उसके बाद, मुझे याद है मैं छठवीं क्लास में थी, तो छठवीं क्लास से लेकर मेरे विवाह तक क्योंकि बहनों की तो एक-एक दो-दो वर्ष में शादियाँ हो गईं, सबसे ज्यादा लंबा समय मैंने अपनी माँ और छोटी बहन और भाई के साथ, वो संघर्ष इतने कम समय में नहीं बाँटा जा सकता। आरती बस एक ही बात बताऊँगी कि हमारा वो संघर्ष भी अलग किस्म का था। जानती हैं इस तरह का कि हम शहर के इतने सम्मानित परिवार से थे कि हमारे पास चरम अभाव आता चला गया, साल दर साल पास हो के समाप्त होते गए। मेरी कई कहानियों में अनायास आ गया है कि पासबुकें खाली हो गईं, और कोई चाचा-मामा, कोई नहीं था हमें देखने वाला, तो उसमें उस स्थिति में भी हम अपने आप को, हम अपने अभाव नहीं दिखा सकते थे लोगों को, सबसे बड़ी आयरनी, सबसे बड़ी विडंबना ये थी कि हमें सबके सामने खुश रहने और संपन्न होने का ही अभिनय करना होता था, क्योंकि मेरी माँ को था कि हम उसी तरह, उसी शान के साथ जियेंगे, जी रहे हैं। लोगों को ये भ्रम देकर कि जिस तरह हमारे पिता के समय में हम रहा करते थे।
सचमुच बहुत, बहुत संघर्षशील रहा आपका बचपन। मैंने ये भी सुना है कि छठी क्लास तक आप स्कूल गई नहीं थीं तो उसके पीछे क्या किस्सा है।
हाँ, अच्छा हुआ आप मुझे इधर ले आईं उस दुःख से। यहाँ क्या था कि हमने कहा न कि हमारे पाता-पिता, वो बहुत ज्यादा बच्चों की भावनाओं का, बच्चों का खयाल किया करते थे। ऐसी निगरानी, रखवाली करते थे जैसे, तो मैं जब छोटी थी उन दिनों, पिता के ट्रांसफर होते रहते थे, कहीं छह महीने किसी शहर में, किसी शहर में एक साल। तो वो ऐसे देखने के लिए कि देखिए बच्चों को अच्छा लगता है, स्कूल ले जाओ, देखिए मन लगता है कि नहीं इसका। पहले बच्चे का मन लगना चाहिए, तो जब भेजा और मैं जरा नाक चढ़ाते हुए घर आ गई। क्या बेटा कैसा लगा, नहीं अच्छा लगा, छोड़ो। तो ऐसे कर-कर के एक दो शहरों में जहाँ-जहाँ तबादले हुए, भेजे गए। फिर अंत में जब हम वाराणसी आकर बस गए। तब यहाँ, तबतक मैं छठी में जाने लायक हो गई थी, थी तो चौथी-पाँचवीं लायक, लेकिन पिता शिक्षा अधिकारी थे तो उन्होंने बड़ी बहन से कहा, जाकर अपने प्रिंसिपल से कह देना कि इसका छठी में नाम लिख लें। मुझे अभी तक याद है। मेरी लंबाई, हुलिया देख के प्रधानाध्यापिका ने मेरी बहन को ऐसे देखा और कहा, ‘छठी में! किसने पढ़ाया, तुमने या पिता जी ने।’ तो बहन को समझ आई, उसने कहा–‘पिता जी ने।’ ठीक है बेटा लिख लेती हूँ। तो बहन ने ये भी कहा–कि पिता जी ने ये भी कहा है कि नहीं चलेगी तो पाँचवीं और चौथी में कर दीजिए। लेकिन एक चीज बड़ी अच्छी थी कि मुझे, ये मैं बता दूँ यहाँ कि क्यों, मुझे पढ़ाई कभी मुश्किल नहीं लगी। छठी में गई, क्योंकि पिता शिक्षा अधिकारी थे तो घर में ढेर-सी नई-नई किताबें चारों तरफ फैली रहती थीं। और वो इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, साहित्य, कविता, कहानी मुझे जो मन आता था वो मैं पढ़ती थी और जब मन आता था तब पढ़ती थी। जब मैं छठवीं में गई तो इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र सब आता था। परेशानी होती थी सिर्फ गणित और सिलाई में।
तो आप शायद हमारे यहाँ की सबसे पहली होम स्कूल जिसे आजकल कहते हैं न होम स्कूल बालिका रही होंगी। अच्छा थोड़ा और आगे बढ़ते हैं फिर आपकी पहली कहानी जो थी वह ‘सारिका’ में प्रकाशित हुई और उसका भी एक बड़ा दिलचस्प-सा किस्सा है कि वो कहानी आपने भेजी नहीं थीं, उसको एक बार हमारे श्रोताओं को सुनाइये कि कैसे वह कहानी छपी?
अरे ये एक लंबा फ्लैश बैक है, मैं बताती हूँ तुम्हें। एक तो यही कि बचपन से हमने कहा कि पिता लिखते थे, शेरो-शायरी करते थे तो मैं सुनती थी, तो खैर पिता के कारण छठवीं में मेरा एडमिशन हुआ और पिता नहीं रहे थे। तो सुना तो था ही, सारे अपने संस्कार थे, रुचियाँ थीं तो मैं भी लिखती थी। एक बार ऐसे ही बचपन में एक कविता लिख ली थी, जब मैं थी करीब आठ-नौ वर्ष की। तो एक कविता लिख ली। बहनों ने कहा अरे इसने तो कविता लिख ली, तो वह कविता ऐसे ही कहीं बाल-साहित्य में छप गई। फिर मैंने देखा कि वाराणसी से एक समाचार पत्र निकलता था ‘आज’। तो ‘आज’ के बाल-संसद में मैं लिखने लगी। ये मैं बचपन की बात बता रही हूँ। बचपन की लिखते हुए फिर, मतलब वहाँ थे जो भैयाजी बनारसी और बेढब बनारसी, उस समय के बहुत बड़े व्यंग्यकार, वो संपादक थे ‘आज’ के साहित्यिक परिशिष्ट के। उन्होंने देखा कि बिना पिता की बेटी है और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तो तुम्हारे घर के पास ही रहता हूँ, मुझे तुम अपनी रचनाएँ ‘आज’ के लिए हमेशा दे दिया करो। उनको देती थी और दस रुपये पारिश्रमिक कहानियों के आते थे। सबसे अच्छा तो वह लगता था कि मैं माँ के यज्ञ में कोई समिधा दे रही हूँ जैसे। मैं बी.ए. में थी तभी मुझे गुप्त जी ने, फिर संपादक जी ने मुझे वयस्क परिशिष्ट पर, वयस्क पृष्ठों पर छापना शुरू कर दिया था, तो मैं ‘आज’ की लेखिका हो गई थी। लेकिन जब तक मैं ‘आज’ की लेखिका हुई, तब तक मैंने एम.ए. कर लिया था। फिर पीएच.डी. में मैं इनरोल हो गई थी और मेरा विवाह हो गया। विवाह हो गया तो सारा लिखना-पढ़ना जैसे होता है स्त्रियों का सब छूट गया था और मैं बिलकुल भूल गई थी। मतलब मैं सोचती भी नहीं कि लिखना है मुझे या कुछ करना है। पति मेरे मर्चेंट नेवी में थे तो विदेश की यात्राएँ की खूब और उसके बाद बच्चों के साथ गृहस्थी बसा ली। पूरे सात-आठ वर्षों तक मैंने कुछ नहीं लिखा था, भूल गई थी। ‘आज’ को भी भूल गई थी। मतलब लिखती रहती थी इधर-उधर, कोई महत्त्वाकांक्षा, लेखिका बनना, रचनाकार बनना ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा कुछ नहीं सोचा और पीएच.डी. कर चुकी थी। एम.ए. पीएच.डी. करके तीन बच्चों की माँ खुश-खुश। लेकिन, घर में ‘धर्मयुग’, ‘साप्ताहिक हिंदुस्तान’, ‘कादंबिनी’, ‘नवनीत’ सारी पत्रिकाएँ लेती थी, क्योंकि हिंदी की छात्रा थी, साहित्य की। एक दिन ‘सारिका’ में एक कहानी पढ़ी, प्रेम कहानी। प्रेम कहानी की नायिका का नाम था–सुरबाला। बहुत अच्छी कहानी थी। एक लंबी प्रतिक्रिया लिखी। कमलेश्वर जी के पास वह प्रतिक्रिया पहुँची। वह एक व्यंग्यमय प्रतिक्रिया थी और लिखकर मैं भूल गई, बिलकुल भूल गई भेजकर। एक महीने बाद मेरे पास पत्र आता है कमलेश्वर जी के हाथों का लिखा, कि–आपकी रचना देखी, इसमें निहित व्यंग्य को देखा, और मुझे लगा कि यदि आप नियमित रूप से लिखें तो हिंदी को आपसे बहुत अच्छी रचनाएँ मिल सकती हैं, आप लिखिए और अपनी कुछ रचनाएँ मुझे पढ़ने के लिए भिजवाइये, मतलब आप सीधे ‘सारिका’ में छपने के लिए मत भेजने लगिए खुश होकर।
फिर भी प्रोत्साहन और वह भी कमलेश्वर जी के द्वारा, आपके रचनाकर्म को तो जैसे पंख लग गए होंगे।
हाँ, वही तो! कमलेश्वर जी का और वो भी एक अलेखिका। बचपन में ‘आज’ में लिखा था बस, तो वो दिन और आज का दिन। उसके बाद मैंने इधर-उधर ढूँढ़ा, इधर-उधर की पुरानी-धुरानी। जैसे मुझे कोई जादू की छड़ी हाथ लग गई हो। वही जो कहते हैं न ‘अप दीपो भव’ ये रास्ता रोशनी, टॉर्च जला दी हो किसी ने, और मैंने एक-दो कहानियाँ फेयर की। एक कहानी याद है ‘जीजी’ और एक कहानी ‘गौरा गुणवंती’। और मैंने कमलेश्वर जी के पास दोनों भेज दी। उन्होंने ‘जीजी’ तुरंत और ‘गौरा गुणवंती’ चार-पाँच अंकों बाद प्रकाशित कर दिये। तो ‘सारिका’ में महिला कथाकार अंक, हिंदी की शीर्ष पत्रिका, में सूर्यबाला आ गईं।
अरे वाह, और फिर कैसी अद्भुत यात्रा रही। मैं सोच रही थी कि आपकी कहानियों का कैनवस जो है, इतना विस्तृत है, इतना विविध है कि आपकी कहानियों का किरदार हर तबके के विदेश में, देश में, शहरों में, गाँव में, उनके मानवीय भाव तरह-तरह के। मुझे लगता है आपकी दो कहानियों में शिल्प में इतना अंतर है कि कई बार तो लगता है कि एक ही लेखक की कहानी कैसे हो सकती है। तो कुछ अपनी रचना प्रक्रिया के बारे में बताइये कि कैसे कहानी आपके मन में उठती है और आप कैसे उसे लिखती हैं?
मैं बिलकुल सच बोलती हूँ, इसे मेरा दंभ न समझना। मैं कहानियाँ कभी ढ़ूँढ़ने नहीं जाती। बहुत लोग को सुनती हूँ कि इस पर लिखना चाहा। इस पर लिखने की योजना बनाई, यहाँ गई वो एक बड़ी अच्छी बात है। वो लोग योजना बनाकर, प्वाइंट्स बनाकर। मैंने उपन्यास तक की कभी योजना, प्वाइंट्स, अध्याय कुछ नहीं बनाया, और कहानियाँ खुद मेरे पास आती हैं चलकर। मेरे पास आती हैं, मेरे अंदर, मेरे अनजाने वो बैठी रहती हैं, अंदर मेरे रचती-बसती रहती हैं मेरे अनजाने। ये शायद इस तरह होता है–हम सभी लेखकों का। मेरे लिए कुछ अलग नहीं, कि हम कोई बहुत मार्मिक, कोई व्यक्ति, कोई शब्द, कोई वाक्य, तुम तो खुद लिखती हो और पूछ रही हो, तो कोई शब्द, कोई वाक्य, कोई घटना, कोई चरित्र, कोई व्यक्ति अचानक अनायास इतना डिस्टर्व कर जाता है, इतना मन के अंदर घुस जाता है कि वह निकलता नहीं है। तो कभी तो हम तुरंत लिखने बैठ जाते हैं। समय सुविधा एक स्त्री के पास जितनी रही, और कभी रहने देते हैं।
आपकी कहानी, आपके लेखन पर थोड़ी और चर्चा करते हैं। आपकी पीढ़ी की बहुत कम महिलाएँ हैं जो हास्य-व्यंग्य के लिए जानी गई हों। आपका नाम प्रमुख है बल्कि मैं कहूँगी कि मैंने और किसी का नाम आपकी पीढ़ी में सुना नहीं हास्य-लेखन में। तो ऐसा क्यों? पहली बात तो ये कि क्या हम महिलाओं में ‘सेंस ऑफ ह्यूमर’ नहीं, ऐसा तो नहीं है। और दूसरा क्या ऐसा कि महिला लेखकों से खास किस्म के लेखन की अपेक्षा की जाती है और उसमें हास्य-व्यंग्य कहीं फिट नहीं होता उस अपेक्षा में ऐसा है क्या? तो आप कैसे व्यंग्य लिखने लगीं?
जैसे कहानियाँ लिखने लगी। ये भी बता दूँ तुमसे, ये प्रश्न मुझसे हर हफ्ते, हर पंद्रह दिन पर तो जरूर इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आप महिला होकर व्यंग्य लिखती हैं। तो जैसे महिला होकर व्यंग्य लिखना, मतलब मुझे लगता है कि शायद बहुत क्षुद्र विधा मान ली गई थी उन दशकों में। शूद्र विधा कहा था परसाई जी तक ने, तो शायद इसीलिए महिलाओं ने सोचा हो कि ये उसे कुछ स्तरीय, मतलब चीज समझी नहीं गई, विधा व्यंग्य को कभी वह दर्जा मिला नहीं। तो इसलिए, या शायद ऐसा था कि भई ये क्या है, व्यंग्य को कोई हास्य के साथ ले आता था। जबकि हास्य और व्यंग्य में बहुत अंतर है। हास्य तो निरुद्देश्य होता है, उसका उद्देश्य सिर्फ हँसाना होता है, जबकि व्यंग्य के पीछे हमारी चारों तरफ की, हमारे जीवन की, व्यक्ति की आयरनी को, विडंबनाओं को, विद्रूप को उजागर करना होता है। व्यंग्य बहुत ही सकारात्मक और बहुत गंभीर विधा है, और बहुत कठिन। मैं गद्य का निकष मानती हूँ व्यंग्य को। तो मैं ऐसे ही बचपन से ही लिखती थी और ये नहीं मालूम था कि क्या लिख रही हूँ। ये भी तुमको बताऊँ कि व्यंग्य लिखना इसलिए मुश्किल है कि हर कोई नहीं लिख सकता। कहानी में सीधे-सीधे चलते हैं। व्यंग्य में हम गुगली मारते हैं। व्यंग्य में हम व्यंजना, जो कहते हैं लक्षणा, परिहास और कटाक्ष उसको इस तरह, उन्हीं चीजों को हमें अंदाज-ए-बयां इतना बदल जाता है कि पढ़ते हुए आदमी आह और वाह दोनों कह दे, तो ये विट और ह्यूमर हमारे घर में खूब था। जो मैंने तुमसे कहा हमारे पिता में था, बड़ी मजेदार पैरनियाँ बना दिया करते थे। हमारे आसपास था। हमारे घर की, बचपन में हमने अपने घर की स्त्रियों में देखा था तो वो शायद मेरी प्रकृति, मेरे स्वभाव में है और ये भी बताऊँ तुम्हें कि इसी प्रकृति, इसी की वजह से हमें अपने दुखों पर, अपने अभावों पर भी हँसना आया, तो अभावों पर हँसना जो होता है वह व्यंग्य होता है। तो इस तरह मैं लिखने लगी और लिखती थी कभी-कभी, लेकिन ये भी तुम्हें बताऊँ बड़ी मजेदार चीजें, तुमने पहली कहानी तो पूछी, पहला व्यंग्य नहीं पूछा।
हाँ, बताइए न।
लिखती रहती थी लेकिन ये नहीं मालूम था कि, वो ‘साप्ताहिक हिंदुस्तान’ और ‘धर्मयुग’ ये सब लेने लगी तो देख रही हूँ शरद जोशी छप रहे हैं, और कितने ज्यादा पढ़े जा रहे हैं। हरिशंकर परसाई, रवींद्रनाथ त्यागी, तब मुझे लगा कि ऐसे ही कुछ तो मैं भी लिखती हूँ। अब तुम्हें पहले व्यंग्य की कहानी सुनाती हूँ। जब मेरी पहली कहानी छप गई ‘सारिका’ में तो मेरे पास तो वो आत्मविश्वास आ गया कि मैं लिख सकती हूँ। हिंदी को कुछ अच्छी रचनाएँ दे सकती हूँ। उसी समय ‘धर्मयुग’ में एक विज्ञप्ति आई, दो-तीन महीने बाद ही। 72 में कहानी छपी थी और 73 के जनवरी में, कि ‘धर्मयुग’ का ये होली विशेषांक युवा व्यंग्यकारों को समर्पित है। जो भी युवा लेखक चाहें अपनी रचनाएँ भेजें ‘धर्मयुग’ को। जो भी रचनाएँ स्वीकृत होंगी वो ‘धर्मयुग’ में प्रकाशित होंगी। तो उस समय धर्मयुग में प्रकाशित होना बहुत बड़ी, वो बस अलादीन का चिराग हाथ में आ जाना। तो मैंने सोचा कि मेरी तो वो व्यंग्य प्रतिक्रिया ही थी जिस पर कमलेश्वर जी ने लिखा था, तो मैं भी इस पर डाल दूँ, ‘सारिका’ में कहानी छप गई है। तो मैंने एक व्यंग्य लिखा ‘खाना ईंट का, आना समाजवाद का’। उन दिनों समाजवाद की बहुत धूम थी। ‘धर्मयुग’ में भेज दिया। वो व्यंग्य रचना स्वीकृत हो गई। तो पहली कहानी ‘सारिका’ और पहली व्यंग्य रचना ठीक चार-पाँच महीने बाद, मार्च होली अंत में ‘धर्मयुग’ में, उस समय संपादक थे डॉ. धर्मवीर भारती। इसके बाद तो मुझे ऐसा ग्रीन सिग्नल मिल गया कि मुझे पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ा और हर एक-डेढ़ महीना, दो महीने बीतते न बीतते ‘धर्मयुग’ से एक पत्र आ जाता था, ‘सारिका’ से एक पत्र आ जाता था, कि बहुत दिनों से आपकी कोई कहानी नहीं मिली या फिर बहुत दिनों से आपका कोई व्यंग्य नहीं मिला। लोग बहुत हँसते थे, मेरे पति तो मुझे कहते, तुम कहानी लेखिका और व्यंग्य लेखिका बाद में हो, पहले तुम ‘धर्मयुग’ लेखिका हो। क्योंकि संस्मरण भी छपे। हाँ, ये भी मैं बताऊँ तुमसे कि ये जो तुमने कैनवस वाली बात कही न, तो उसमें एक ये भी बात थी कि मैं जो कुछ चल रहा होता है, ट्रेंड, फैशन, आंदोलन, विमर्श सब लोग लिख रहे होते हैं उसमें मेरा मन नहीं लगता। उससे कुछ, कुछ-कुछ अलग। उस समय मैंने एक कहानी लिखी थी लंबी कहानी, वो बहुत मील का पत्थर साबित हुई, लोग अभी भी याद करते है। ‘धर्मयुग’ में छपी थी लंबी कहानी–‘रेस’ मतलब ‘रेड रेस’। वो कॉरपोरेट के रेड रेस पर मैंने लिखा था और वो मेरी चौथी कहानी थी।
वाह, और वो अपने समय के लिए बहुत आगे थी वह कहानी।
समय से बहुत आगे, लोगों ने कहा कि कॉरपोरेट रेस पर। जबकि माना जाता था उस समय कि लेखिकाएँ बस घर-आँगन पर लिखती हैं। चार दीवारी के अंदर लेखन अपने घर-आँगन पर, ड्राइंग रूम सगल, पढ़ी-लिखी महिलाओं का ड्राइंग रूम सगल। तो बस ऐसे ही पहला व्यंग्य और चलता रहा।
तो आपके व्यंग्य लेखन का थोड़ा सा स्वाद हमें मिलेगा। आपका एक व्यंग्य ‘देश-सेवा के अखाड़े में’ बहुत सुंदर है। उसका थोड़ा सा अंश आप पढ़ के सुनाएँगी।
इसके ऊपर एक बड़ा मजेदार-सा एक, छोटा सा वाक्य है जो अभी वरिष्ठ व्यंग्यकार प्रेम जनमेजय ने मेरे लिए कहा है, कि जो तुमने कहा है न कि व्यंग्य, लेखिकाएँ नहीं लिखतीं, तो सचमुच मेरे से पिछली पीढ़ी में, मतलब मेरे से सीनियर पीढ़ी में, दस साल सीनियर, उसमें शांति मेहरोत्रा जी थीं वो थोड़ा बहुत हास्य-व्यंग्य लिखती थीं, और मेरे साथ एक थीं अलका पाठक। तो प्रेम जनमेजय ने एक वाक्य लिखा है कि यदि शांति मेहरोत्रा, सूर्यबाला और अलका पाठक जैसी लेखिकाएँ व्यंग्य नहीं लिखतीं तो व्यंग्य लेखन को पुरुषोचित लेखन मानने से आलोचकों को कोई रोक नहीं सकता था। और हिंदी व्यंग्य लेखन नारी विमर्शहीन होने का अभिशाप झेलता। तो ये उनका ऐसा वाक्य है जो सब जगह कोट किया जाता है–तीखा, बिलकुल सटीक। तो देश-सेवा के अखाड़े में। मुझे अच्छा लग रहा है, ये भी बता दूँ कि ये बहुत नया व्यंग्य नहीं है। मतलब एक लगभग नई लेखिका का ही व्यंग्य है–‘देश सेवा के अखाड़े में’।
ये खबर आग की तरह चारों तरफ फैल गई कि मैं देश सेवा के लिए उतरने वाला हूँ। जिसने सुना भागा आया और बधाई दी। सुना आप देश सेवा के लिए उतर रहे हैं। ईश्वर देश का भला करे। प्रस्ताव पर प्रस्ताव आने लगे। बाईदवे शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं, कौन सा एरिया चुन रहे हैं। हमारे अंचल से करिए न। बहुत स्कोप है। ईश्वर की दया से गरीबी, भूखमरी, अशिक्षा, किसी बात, किसी चीज की कमी नहीं है। लोग भी सीधे-सादे, नादान किस्म के हैं तो बहकने की कोई गुंजाइश नहीं और हेलिपैड बनाने के लिए इफरात जमीन पड़ी है। इन लोग को, यहाँ के लोग को हर हाल में मुँह सील कर रहने की जबरदस्त ट्रेनिंग मिली है। मन्नू बाबू ने इनको जबरदस्त ट्रेनिंग दी है। मैंने सोचा जगह तो सारी एक सी हैं। ऐसे स्कोप कहाँ नहीं, लेकिन जब कहा जा रहा है, ऑफर मिला है तो उन्हीं के एरिया से शुरुआत कर लेते हैं। मेरा निश्चय सुनते ही प्रेसवाले दौड़े आए और आग की तरह फैलती इस खबर में घी डाल गए। शाम को उस एरिया का सबसे बड़ा ठेकेदार आया और सलाम करके पूछने लगा–बँगला कहाँ छवेगा। मैं हैरान, कैसा बँगला, अभी देश सेवा तो हुई नहीं कुछ, उससे पहले बँगला छवाने लगा। उसने उसी अदब भरी मुस्तैदी से कहा–वही तो जबतक बँगला नहीं छवेगा, देश सेवा, जनहित जैसे महान काम कहाँ बैठ के करेंगे आप। लोकसेवक लोग कहाँ आकर ठहरेंगे। मुलाकाती लोग कहाँ लाइन लगाएँगे। फूस के छत या टिन के शेड के नीचे मुलाकाती नहीं इकट्ठे होते। सीधी सी बात है जो अपने सिर पर छत नहीं खड़ी कर पाया वो उनके सिरों पर साया कहाँ से करेगा। अपना नहीं तो कम-से-कम अपने दुःख-दर्द सुनाने आने वालों का तो खयाल कीजिए। मैंने कहा–तब फिर छवा दीजिए, जहाँ ठीक समझिए। वो खुश हो गया। वहीं का वहीं बैठकर नक्शा-वगैरह खींचकर बोला–गैराज एक रहेगा कि दो। मैंने कहा–अरे यार पहले कार तो हो, हं…हं। उसने कहा–आपकी न सही, मुलाकातियों की तो होगी। और फिर यों समझ लीजिए कि मन्नू बाबू को देश हित के पवेलियन में कुल छह महीने ही गुजरे हैं। और ऑल रेडी दोनों बेटों की ट्रकों और शिशिर बैगनों के लिए कई जगह की कमी पड़ रही है, समझे आप। मैंने आज्ञाकारी बच्चे की तरह कहा, तब जैसा आपलोग उचित समझें। कॉन्ट्रेक्टर खुश हो गया। ऐसा करते हैं एक गैराज बना देंगे और चार गैराज की जगह छोड़ देते हैं। पोर्ज पोर्टिको आलीशान बनाएँगे। नहीं तो संतरी टूटपुंजिये मुलाकातियों को फटकारेगा-दुतकारेगा कैसे? संतरी जितना कटखरा होता है आदमी उतना ही पहुँच वाला माना जाता है। अच्छा मैं चलता हूँ। हाँ बँगले का अहाता, लॉन, सींचने, साग-सब्जी, फूल-पत्तों की क्यारी सँवारने के लिए मेरा एक आदमी है। बड़ा नेक और विश्वासपात्र, इस काम के लिए उसी को रखिएगा। जनसेवा करने जा रहे हैं तो इस एरिया के नक्कालों से सावधान रहिएगा। शाम को उस एरिया के व्यापारी संगठन का प्रमुख आया और बड़ी विनम्रता से बोला–देश सेवकों का भोजन तो अत्यंत संतुलित व नियमित होता है। मन्नू बाबू तो अनाज को हाथ नहीं लगाते थे और देख लीजिए काठी ऐसी है कि सत्तर की उम्र में सताइस वालों को बगल में दबा कर घूमे। अखाड़ेवाजों-सा सधा हुआ, तना हुआ शरीर। सिर्फ भोजन के मेन्यू की ही बदौलत से तो, बाईदवे आपका मेन्यू। मैंने झेंप कर कहा–कभी बनाया नहीं। तो झटपट बना डालिए, खानपान की दुरुस्ती पहले, आप जानो रूखी-सूखी वाले नेता को कौन पूछता है। मेरा तो आजतक किसी नमक-रोटी खानेवाली महान आत्मा से साबका पड़ा नहीं। मेरे देखते-देखते देश सेवक, कित्ते ही देश सेवक, नमक, रोटी, प्याज से शुरू होकर आज फल, दूध और सूखे मेवों वाले मेन्यू पर स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। मैंने संकोच से कहा–सूखे मेवे थोड़े गरिष्ठ भी तो होते हैं। सोचता हूँ शुरू-शुरू में रोटी-दाल ही ठीक रहेगा। उसने फौरन टोककर कहा–देखिए आप दाल-रोटी खाइए या नमक-रोटी, एक बात समझ लीजिए। यहाँ भड़काने वाले बहुत हैं। घर घर ये बात पहुँच जाएगी कि जो खुद नमक खाता है वो हमें मालपूए कहाँ से खिलाएगा, और इस एरिया के लोग बड़े भोले-भाले नादान हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। मैंने कहा–आपकी बात तो ठीक है, लेकिन मेवे बहुत महँगे भी तो हैं। वो बेतक्कलुफी से बोला–क्यों शर्मिंदा कर रहें हैं आप। आप इस एरिया के जनसेवक हो कर आ रहे हैं और खरीद कर मेवे खाएँगे। लानत नहीं होगी इस जमीन के बाशिंदों के लिए, आखिर हम किस मर्ज की दवा हैं। आज ही सूखे मेवों का एक टोकरा आपके यहाँ भिजवाता हूँ। मैंने जल्दी से कहा–नहीं, नहीं आपके मेवे, उन्हें मेरे मेवे नहीं देश सेवा के मेवे समझकर खाइएगा। वैसे भी आप चखकर देखिएगा। तब समझ में आ जाएगा कि खरीद कर खाए मेवों में वो स्वाद और लज्जत कहाँ जो देश सेवा से प्राप्त मेवों में होती है। पैसों की चिंता मत कीजिएगा। मुझे आप पर भरोसा है। मेरे पैसे कहीं नहीं जाएँगे। सब वसूल हो जाएगा।
वाह, बहुत खूब-बहुत खूब। बिलकुल पैना और सटीक जैसा एक व्यंग्य को होना चाहिए। अच्छा समय का थोड़ा अभाव हो रहा है। मैं चाहती हूँ कि पहला जो उपन्यास आपका था–‘मेरे संधि पत्र’ उसके बारे में कुछ बात करें। पहले तो ये बताइएगा कि कहानियाँ आप लिखने लगी थीं फिर आपने अपना पहला उपन्यास लिखा–‘मेरे संधि पत्र’ जो आजतक बहुत प्रसिद्ध है, बहुत पढ़ा जाता है तो उसके बारे में कुछ संक्षेप में बताइए।
बहुत थोड़े में बताऊँगी, हालाँकि बहुत ही ज्यादा अभिभूत करने वाली वो स्मृति है, यादें। कि यों ही ढाई वर्ष हुआ था लिखते और यों ही उपन्यास शुरू कर दिए। नई सी लेखिका कुछ पता नहीं था। मेरे संधि पत्र डॉ. धर्मवीर भारती को इतना अच्छा लगा कि उस समय तक हम बॉम्बे आ गए थे। उन्होंने मुझे बुलवाया था ‘धर्मयुग’ कार्यालय और बड़ी वत्सल्य आँखों से, चक्षु से मुझे देखते हुए कहा था कि उपन्यास मुझे आपका बहुत अच्छा लगा। इसे मैं ‘धर्मयुग’ में धारावाही प्रकाशित करूँगा। तो वो क्षण मैं कभी भूली नहीं हूँ, और उस उपन्यास का, ‘मेरे संधि पत्र’ का ‘धर्मयुग’ में प्रकाशित होना था कि तीन वर्ष की ये लेखिका। ‘धर्मयुग’ जिन-जिन घरों में जाता था, उन सब घरों में ये लेखिका, सूर्यबाला पहुँच गई। अभी तक लोग मुझे ‘मेरे संधि पत्र’ की लेखिका के नाम से जानते हैं और तुम्हें ये जानकर बड़ा अच्छा लगेगा कि सिर्फ दो वर्ष पहले ‘पाखी’ पत्रिका ने एक नया स्तंभ निकाला–‘कालजयी कृतियों का पुनर्पाठ’। और उसमें पहली कृति ‘मेरे संधि पत्र’, तो ये कैसे एक नई लेखिका की कालजयी कृति हो गई, तो याद करते हैं। इसको मैं पढ़ती हूँ छोटा सा अंश, ये बता दूँ कि नायिका, जो मैंने कहा न कि उस समय चल रहा था स्त्री विमर्श का। मैंने स्त्री मुक्ति और ये सब पर नहीं, मैं अपने मन का लिखती थी जो मन में आया, तो इसमें जो इसकी नायिका है, युवती माँ वो सौतेली माँ है, उसकी दो छोटी-छोटी बेटियाँ हैं, सौतेली बेटियाँ। भारती जी ने मुझसे यही कहा था कि मुझे सबसे यही अच्छा लगा कि आपने इस उपन्यास में जो एक सौतेली माँ और उसकी बेटियों का जो रिश्ता-संबंध दिखाया है, बड़ा अलग सा है। और वो शिवा के लिए तो लोग मुझसे, जो पाठकों के इतने पत्र आए वो मुझसे कहते थे कि शिवा कभी मिले तो उन्हें मेरा प्रणाम दीजिएगा। किसी चरित्र के लिए ऐसा कहना।
तो पढ़ती हूँ इस उपन्यास की शुरुआत। इसको अभी तैतालीस वर्ष बाद अभी राजकमल प्रकाशन ने पिछले वर्ष छापा है। इसे मैं पाठक की, पाठकों की जीत मानती हूँ तो ये शुरुआत ही है उस उपन्यास की।
उसकी बड़ी सौतेली बच्ची अपने बचपन का लिख रही है।
वह दिन मेरे शिशु संसार का महान पर्व था जब पहली बार मम्मी को देखा। रंगीन लट्टुओं की रोशनी में कंदिल-सी झलमलाती हमारी हवेली के सामने, इंग्लिश बैंड की कतारें आ कर रुकी थीं। अनार छूटे थे। बंदूकें दगी थीं और फूलों से सजी कार फाटक से होती हुई सदर दरवाजे तक रेंगती हुई रुकी थी। अंदर-बाहर चहल-पहल मच गई। मैं और रिंकी अपने लाल-पीले साटन के कामदानी वाले गरारी सँभालती, सीढ़ियाँ उतरते जाते थे और अध तोतली बोली में उच्चारते जाते थे–‘मम्मी आ दई, मम्मी आ दई’, तब तक आया दौड़कर आई, रिंकी को गोदी में उठाया और मुझे उँगली पकड़ाकर हुलसते हुए सीढ़ियाँ उतर गई। मोतियों की झालर में उलझी एक सुकुमार-से चेहरे को देख मैंने, रिंकी ने बारी-बारी एक-दूसरे को देखा और आँखों-आँखों में पूछना चाहा–ये कैसी मम्मी, छोटी, दुबली, पतली-सी दीदियों जैसी। सेठानी माँ हमें भाँप गईं। सेठानी माँ यानी दादी। मुस्कुराती हुई समझाने लगी–‘अभी थकी हैं न मम्मी। हाँ हाँ तुम्हें प्यार करेंगी, कहानी सुनाएँगी, पढ़ाएँगी, अच्छे-अच्छे फ्रॉक सील के पहनाएँगी।’ फिर तो मम्मी ही है। मैंने और रिंकी ने एक दूसरे को देखकर चुपचाप स्वीकार लिया। सेठानी माँ हमारी बलैया लेती कह रही थीं–अब आफत है रिचा की मम्मी बुलाऊँ कि रिंकी की। क्यों किशोरी दोनों झगड़ा करेंगी न। अच्छा एक बार रिचा की मम्मी एक बार रिंकी। बर्तन धोने वाली बतशिया चिढ़ा रही थी हम दोनों को–ए…हे…अब क्यों मिजाज मिलेंगे, नई-नई मम्मी जो आ गईं। किशोरी कह रही थी मैं ले जाऊँगी रिंकी की मम्मी को अपने घर। आवाजों की भीड़ में कोई एक ही शब्द धक्के पर धक्का खा रहा था–मम्मी…मम्मी…मम्मी। अभी थकी हैं मम्मी आराम करने दो। रिंकी जाने कब चुपके-चुपके दरवाजे की दरार से झाँकी थी और ये देख के सकपका गई थी कि मम्मी तो आराम नहीं कर रही हैं, बल्कि मोतियों की झालर आँखों से सटाए सिसक-सिसक कर रो रहीं। एकाएक उसे कुछ सूझा, हर बार जब वह रोती है तो किशोरी पहले उसका मुँह ही तो धुलवाती है। सुबू दबे पाँव एक गिलास में पानी लाई और धीमे-धीमे डरती सी उनके पास पहुँची, बोली तुम थककर रो रही थीं न मम्मी। मैं दरार से झाँक रही थी। लो मुँह धो लो अपना। एक क्षण को उनके चेहरे की गरिमा उसे छू गई। रिंकी सिर नीचा किए अपने आप कह गई–‘हम कब से तुम्हारा इंतजार करते थे मम्मी।’ एकाएक उन्होंने जोर से रिंकी को बाँहों में भींच लिया। जैसे कोई बहुत पुरानी हमजोली मिल गई। उसके बालों में हाथ फेर कर उसे चूमा। रिंकी भागती सी मेरे पास आई, मेरे कान के पास मुँह ला के धीमे से बोली–‘रिचा, चल मम्मी प्यार करने को बुलाती है।’ इस बार मेरी उँगली पकड़े भागती सी विश्वस्त भाव से वो आई और मुझे पीछे से आगे करती बोली–‘मम्मी ये रिचा है मुझसे दो साल बड़ी।’ और अब मेरे बालों में भी उनकी दुबली हथेलियाँ फिर रही थीं। हम दोनों विभोर थे। उस दिन से वे हमारी मम्मी हैं, मेरा मतलब रिचा की, रिंकी की और बाद में रत्ना की भी।
बहुत सुंदर, बहुत ही मार्मिक कहानी ये है और एक बार पढ़ने वाला भुला नहीं सकता।
हाँ यही चीज, अब तुम समझ गई न।
लेकिन वक्त बहुत कम है, मैं आपको वेणु की डायरी के बारे में बताए बिना जाने नहीं दूँगी। जो आपका सबसे नया उपन्यास है ‘वेणु की डायरी’ मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इसके जो शुरू के प्रकरण हैं। मैं बता दूँ अपने श्रोताओं को कि कहानी है ‘वेणु की डायरी’ एक नवयुवक की जो अमेरिका में अपना जीवन शुरू करता है। पढ़ने जाता है। तो मैं शुरू के प्रकरण पढ़ रही थी। एक एक पन्ना पलटते हुए ऐसे लग रहा था जैसे, मेरी, जब मैं अमेरिकन यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी उसी की कहानी है। वही फटेहाल हरफनमौला जीवन जो जीते थे। तो फिर वही बात कहूँगी कि आपकी उस कहानी में, वेणु की कहानी में बिलकुल अलग लहजा और बहुत ही अच्छे से आपने उस समावेश को पकड़ा है। तो कुछ बताइए कि वो कहानी आपने कहाँ से शुरू की है, और उसकी रिसर्च कैसे की? जिस तरह स्टूडेंट बात कर रहे हैं, एक छोटे से बेसमेंट में एक-दूसरे के साथ, वहाँ से लेकर फिर बाद तक जब वह वापिस अपने घर आता है एक प्रवासी के रूप में। कुछ उसके बारे में बताइए और थोड़ा सा पढ़कर भी सुनाइए।
तुमने खुद देखा है, पढ़ा है आरती बहुत बड़ा उपन्यास है। मैं ये बता दूँ कि कोई रिसर्च नहीं की। कोई योजना नहीं बनाई थी, कुछ भी नहीं। मैं तो बस कुछ ऐसा रहा कि जब मैंने बताया न अभी अलविदा अन्ना में कि हर वर्ष छह-छह महीने के लिए विदेश जाती रही। विदेश मैं पहले भी गई थी लेकिन ये विदेश जाना अलग था। ये मैं अपने बेटे के घर में रह रही थी, और हर बार जाती थी और मेरी डायरियाँ भर जाती थीं। मैं अपने चारों तरफ के समाज को देखती थी, स्त्री को देखती थी, वहाँ के रिश्तों को देखती थी, वहाँ के, मतलब सारी संस्कृति को देखती थी। ये जो जिस तरह से हाफ ब्रदर, मैं बताऊँ कहते हैं न कि मानसिक विक्षिप्ताएँ, छुटे हुए बच्चे, तलाक, तो उसको देख-देख कर मन इतना दुखता था कि मेरी डायरियाँ भर गईं। और फिर जब छह-सात साल बहुत बढ़ते गईं, तब एक दिन लिखा, तो इस तरह से वेणु की डायरी बनी, हलाँकि बहुत मेहनत पड़ी उसे अध्याय में, करने के लिए। और जैसे तुमने बताया, मैं बता दूँ कि निम्न-मध्य वर्ग के जो युवक जाते हैं बाहर, और वो अपने साथ कैसे सपनों की पोटली लेकर जाते हैं, महत्त्वाकांक्षाओं की। पूरा परिवार चाहता है कि हाँ जाएगा, ये वहाँ जाकर कैसे संघर्षों से अपने को स्थापित करते हैं। तो इस उपन्यास के मूल में मेरे दो मुख्य भाव हैं। एक तो विस्थापन का दुःख, विस्थापित होने का। ये दुःख मेरे दूसरे उपन्यासों में भी आए हैं। पहला उपन्यास मेरा अग्निपंख ही है। इसमें गाँव से शहर आने का विस्थापन है। इस उपन्यास में देश से विदेश जाने का। तो वो दुःख कैसा होता है, और सबसे तड़प भरा होता है अपने लोगों से धीरे-धीरे छूटते जाने का दुःख, और आरती मैं जीवन में सबसे ज्यादा महत्त्वपूर्ण रिश्तों को समझती हूँ। रिश्ते हमारे लिए जीवनभर के साथी होते हैं वो रिश्ते हमारे छूटते चले जाते हैं, तो इसे लेकर ये उपन्यास लिखा पूरा, और अंत में, क्योंकि इतना ज्यादा समय लेने लगा तो मुझे ये भी लगने लगा कि हम वापस नहीं लौट सकते। लेकिन ये जरूर मुझे समझ में आया कि वहाँ जाकर, उस समाज को देखकर, अभी हमारे भारतीय परंपरा, और भारतीय अस्मिता और संस्कारों में बहुत कुछ इतना मूल्यवान है कि उसे सहेजकर रखना बहुत जरूरी है। अंततः हमारे जीवन को सुखद, और जो कहते हैं यही, ये मूल्य ही बना सकेंगे। क्योंकि ये भारतीय मूल्य नहीं ये मानवीय मूल्य, जीवन मूल्यों की बात मैंने की।
अब समय नहीं है तो मैं खाली एक छोटा सा, उसके फ्लैश बैक का पढ़ देती हूँ। क्योंकि बाकी अंश तो छोटे-छोटे कई अंश थे जहाँ एक बार वो जाने लगता, जब माता- पिता बहनों से बिछुड़ कर, वो पढ़ू मैं डेढ़ मिनट का है। मतलब वीजा मिल गया, जाने की तैयारी हो रही है। क्या परिवार है, कैसे करता है।
तो दिन व दिन गहमागहमी बढ़ी। तमाम भूली-विसरी चीजें ला-ला कर पैक की जाने लगीं। अपने जान-पहचान वालों में तो कोई विदेश गया नहीं था, इसलिए और, और लोग से सलाह लेते और हम तक पहुँचाते, आचार्य कॉलोनी वाले राय साहब मिले थे, उनका भतीजा फ्लोरिडा में है, बोले सर्दी-बुखार की गोलियाँ जरूर रख दें, वहाँ डॉक्टर नहीं बैठे होते हैं। सामने खुले, नए खरीदे, हल्के सस्ते सूटकेशों में मेरे साथ जाने वाले सामान जमा हो रहे थे। ये माँ कह रही है–सोचा था सब नया ही खरीदेंगे आखिर अमेरिका जा रहा है, कोई मामूली बात है। लेकिन हर बार खरीदते समय पैसे कम पड़ जाते, दो-चार चीजें छूट ही जाती, पैसे जोड़-जुटा कर फिर लाई जाती और अंत में लाए भी कितने गए, दो शर्टें, एक कोट, दो जोड़ी जूते और छोटी बहन बसु, छेद वाले मोजे जो निम्न-मध्य वर्ग की पहचान है। उसके छेद वाले मोजे को उठाकर बोली, बसु छेद वाले मोजे में उँगली डालकर हँसती, ‘दादा ये भी रख दूँ, इंडिया का सोविनियर’ और ये कहता अंत में किचेन में, मठरियाँ तलती वृंदा के पास जाकर खड़ा हो गया। बड़ी बहन कोशिश करके एक मठरी उठाई, अरे वाह। उसके आगे बोल नहीं पाया। न खा ही सका, जल्दी से स्टोर की तरफ बढ़ गया। कड़ाही में तली जाती मठरियों के बीच गर्म तेल में वृंदा की आँखों के आँसू की एक बूँद छनकी थी, वृंदा पसीना पोछने के बहाने आँसू पोछ रही थी। अब यह टूटी बटनों, उधड़ी सिवनों की दुरुस्ती कराने कभी नहीं आएगा। अरे बाबा ईश्वर भी न करे, ईश्वर न करे आए। अब ये मेहमान हो गया। आएगा भी तो पहले जैसी बात नहीं, नहीं होगी। पुरानी किताबें रखते-रखते वेणु ने चुपके से शर्ट के आस्तीन से आँखें पोंछ ली।
और एक थोड़ा सा है ‘किस्सा साढ़े चार यार’। इसको भी बहुत छोटा करके पढ़ती हूँ।
अपार्टमेंट मिला तो यूरेका-यूरेका कह कर दौड़ लगाने को मन हो आया। साथ में चार यार भी। एक तो वही हैदराबादी प्रसाद, दूसरा लुधियाने का प्रशांत उर्फ प्रशांत प्राजी, तीसरा अपने बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर से काफी ऊँची हैसियत वाला ऊटी के किसी टी-गार्डेन का मालिक, सर निरंजन मानसिंह का बेटा स्वामित्र मानसिंह और चौथा ये नाचीज वेणु माधव शुक्ला। जिसका नाम सुनते ही प्रशांत ने तपाक से कहा था–अरे वाह आप तो टू-इन-वन निकले। प्राजी सप्ताहांत खासे घमासान भरे होते। काम बँटे होने पर भी जमकर के हो-हल्ला होता। पहले तो यही बखेड़ा कि आज किसका टर्न है। जिस दिन खाना बनाने का मेरा टर्न होता उसे फास्ट डे कहा जाता, यानी ऐसे खाने से न खाना बेहतर। रात में थके होने के बावजूद सोने से पहले हम थोड़ी मटरगश्ती कर लेते। अमेरिका आने से पहले अपने-अपने घरों में हमें जो कस्मे दिलाई गई थीं, जो प्रतिज्ञाएँ कराई गई थीं। उसे हम बड़े मजे ले-ले कर दोहराते। जैसे हमने नारे बना लिया था–‘सिगरेट-शराब नहीं पीना है’, ‘गोरी मेमो को नहीं छूना है’ अबे उल्लू छूना नहीं, छूने का तो सवाल ही नहीं, उससे दूर रहना है, हाँ-हाँ दूर रहना है। और सिर्फ कुछ महीनों में हम में इतना बदलाव आ गया कि अब हम आराम से जुट-मिल कर चार-छह माह पहले वाली अपनी ही स्थिति पर हँसी-ठठा कर लेते थे जुलूस के नारों की तरह, कैसे–‘तुम्हारा कर्म, एम.एस. पढ़ाई’, ‘तुम्हारी कोशिश जमकर रगड़ाई’, ‘तुम्हारा उद्देश्य डॉलर कमाई’, ‘तुम्हारी दुनिया, माता-पिता, बहन-भाई’, ‘तुम्हारा त्योहार, राखी बँधवाई’, ‘नो शादी, नो सगाई, नो गोरी मेम’।
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सूर्यबाला जी मन तो नहीं भरा, तो मैं आशा करती हूँ आप फिर शीघ्र ही हमारे संवाद में, या किसी और कार्यक्रम में हमारी अतिथि रहेंगी। पर आज अपना समय देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
मेरी तरफ से भी धन्यवाद। इस संवाद शृंखला में आमंत्रित होने के लिए सबका हृदय से आभारी, पूरी टीम का।
संवाद का विडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक करें : https://youtu.be/N3VeEnWF1wU
Image: The Reader (Marie Fantin Latour, the Artist’s Sister)
Image Source: WikiArt
Artist: Henri Fantin Latour
Image in Public Domain