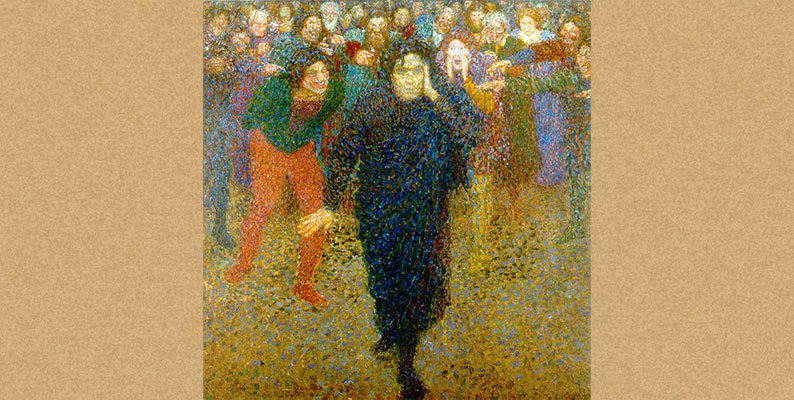काला कैक्टस और माँ
- 1 February, 2016
शेयर करे close
शेयर करे close

शेयर करे close
- 1 February, 2016
काला कैक्टस और माँ
सुबह के चार बजे हैं नींद टूट गई है, लेकिन बैठना मुश्किल है। ट्रेन में बीच वाली बर्थ पर कोई अधेड़ खर्राटे भर रहा है। तिरछा होकर बैठने की कोशिश करता हूँ लेकिन नीचे कागज की प्लेटें, डिसपोजबल ग्लास, तुड़े-मुड़े कागज और न जाने क्या-क्या चीजें ठीक मेरी बर्थ के नीचे फेंकी हुई हैं जो मेरे भीतर मरी हुई छिपकलियों की दुर्गंध भर रही हैं। सामने भी कोई महिला झल्लाते हुए अपने पति से कह रही है ‘देखिये-देखिये यह है देश के सफाई-अभियान की शल्य-क्रिया…इस देश के लोग कभी नहीं सुधर सकते।’
मेरी नजरें बिखरी हुई चीजों पर अटकी हैं। मुझे लगता है कि मेरे भीतर भी कुछ हैं जिनकी चिद्दियाँ तेज हवा में उड़ रही हैं। कड़वाहटें और मिठास हैं, हँसी और आँसू की कतरनें भी हैं जो रूई के फाहे की तरह उड़ती स्मृतियों को नये-नये रंगों में रंग रही हैं। मैं उन्हें समेटने की कोशिश करता हूँ कि बिखरती गुलाब की पंखुड़ियों के बीच काले कैक्टस-सा किसी का चेहरा दिखने लगता है ‘एक ही आदमी पर कितना बोझ? यह तो अच्छा नहीं है न? एक ही आदमी सारा भार क्यों उठाये?’ शब्द काँटों की तरह भीतर धँसने लगे हैं। मैं पीछे पलटता हूँ। भीतर से बिजली कड़कती है। ‘किसने कहा यह? मिट्टी उठी भी नहीं और इस तरह की बातें…छीः।’
बाहर और भीतर हलचल है…शोक है…आँसू हैं…। माँ के मुँह में घिसे सोना और चाँदी वाले पान डालता हूँ तो काँप उठता हूँ। ‘माँ जीवन भर मेरे साथ रही, लेकिन अब, जब मैं अकेला हूँ, तो तुमने मुझसे इन्हें छीन लिया ज्ञान?’
‘छीन लिया…। माँ क्या एक वस्तु है भैया? ऐसा कैसे कह दिया आपने?’
‘सबको आराम चाहिए, माँ को भी। लेकिन जब कोई नहीं था, तब…? वैसे अब तुम बड़े आदमी बन गए। तुम आराम दे सकते हो माँ को, मैं नहीं दे सकता। ठीक भी है। अब नहीं तो कब मिलेगा माँ को सुख। और मेरे पास है क्या जिससे उसे खुश रखूँ।’ कंपन था, आँसू थे, जिनके बीच मेरे शब्द गले में अटक रहे थे ‘कॉम्पलेक्स से बाहर निकलिये भैया। यह आपको किसी से जुड़ने नहीं देगा।’
‘रो क्यों रही हो माँ? मुझे जब छोड़ ही दिया तो फिर…।’
‘फिर यहाँ लौट सकूँगी या नहीं पता नहीं बेटा! तुम्हारे बाबूजी का यहीं दाह-संस्कार हुआ।’ गाड़ी के अंदर माँ थी। धँसी आँखों से गिरते आँसुओं को पोंछने की शक्ति भी माँ के शरीर में नहीं थी। गाड़ी से सटकर बाहर बड़े भैया थे फूटफूट कर रोते हुए। गाड़ी चल पड़ी थी और माँ ने थरथराते हाथ जोड़ लिये थे पता नहीं गाँव के लिए, घर के लिए या मेरे बाबूजी के लिए जिन्होंने गाँव कभी नहीं छोड़ा। गाँव का मोह भी ऐसा था कि पक्की नौकरी में भी बाहर छह महीने से अधिक नहीं टिक सके।
मेरी आँखों की नींद इस समय बिल्कुल शांत है। अब माँ की कराह से परेशान होकर उठना भी कहाँ है। माँ की झुंझलाहट, गुस्से में निकले अपशब्द…‘पापा देखिये दादी क्या-क्या बोल रही है?’ मैं शैलजा को देखता हूँ। उसका मुँह तमतमा रहा है। माँ को पिलाने जा रही जूस का ग्लास उसने दूर हटा लिया है। माँ का शरीर बिस्तर पर पड़ा है। शरीर कहाँ केवल हड्डियों में लगा झूलता चमड़ा। विगत दो वर्षों से बिस्तर पर पड़ी माँ बिस्तर में ही सट गई है। यह तो शैलजा की ही सूझबूझ थी कि बेड सोल नहीं हुआ। ‘दादी के पूरे शरीर में सरसों तेल लगाकर पाउडर छिड़किये।’ माँ चिल्लाती ‘देह चिपचिप करती है। सरसों तेल नहीं…।’ माँ की छटपटाहट देख मैं बोल उठता ‘जब माँ को पसंद नहीं तो जबरदस्ती क्यों करती हो?’ लेकिन शैलजा दृढ़ रहती ‘बेड सोल हो गया न पापा तो सबसे अधिक कष्ट दादी को ही होगा।’
मूँग दाल की खिचड़ी से भरी कटोरी नीचे गिरी है…टन-टन-टनाक..। ‘अरे…अरे…यह क्या किया दादी आपने? ओह, दादी भी न, तली-तली चीजें अब इन्हें नहीं पचती हैं लेकिन यह समझती ही नहीं हैं। अभी नीता ने घर साफ़ किया है और फिर यह…। ऐ नीता देख। फिर साफ़ कर यहाँ’। घर में देशी घी की चिकेन-बिरयानी की सुगंध फैली है। माँ की घ्राण शक्ति अभी पूरी तरह नष्ट नहीं हुई हैं। ‘शैलजा मुझे देखना ही नहीं चाहती हैं। यह चाहती है कि मैं मर जाऊँ। रोज-रोज देगी वही खिचड़ी। मुँह में धँसती ही नहीं है…।’ बड़बड़ाती हुई माँ करवट लेना चाहती है लेकिन ले नहीं पाती। कष्ट बढ़ता तो अपशब्दों की कतारें लग जातीं।…’ देखिये दादी इस तरह नहीं बोलिये।’ शैलजा के स्वर इस तरह कठोर हो जाते जैसे बिस्तर पर अस्सी साल की उसकी दादी न होकर पड़ोस का कोई बदतमीज बच्चा हो। माँ के मुँह से तो इस तरह के शब्द मैंने भी कभी नहीं सुने। माँ का वह अनुशासन… ‘मधुर वचन है औषधि कटु वचन है तीर, श्रवण द्वार हुए संचरै साले सकल शरीर…’ तो तब भी रहा, जब मैं दो बच्चे का पिता बन गया।
मैं पनियाई आँखों से शैलजा को देखता हूँ। ‘दादी को अब सेंस नहीं है बेटा। अब उनसे क्या गुस्सा करना’। ‘जानती हूँ पापा। लेकिन दादी मसालेवाली सब्जी खाना चाहती है। कहती है परवल तल दो, भरुआ करैला बना दो। चबा तो पाती ही नहीं। अभी देखा न आपने क्या हाल हुआ…। स्लाइन चढ़वानी पड़ी। पूरे घर वाले अब केवल दादी में ही तो नहीं लगे रह सकते हैं न। दूसरे काम भी तो करने ही हैं। अब देखिये गुस्से में इन्होंने कुछ खाया नहीं, कमज़ोरी बढ़ेगी या नहीं?’
‘दादी मुँह खोलिये।’ शैलजा की आवाज से माँ मुँह खोलती है। शैलजा ग्लास से थोड़ा-सा जूस माँ के मुँह में डालती है लेकिन सारा जूस नीचे बह जाता है…छाती पर, गर्दन पर…। ‘दादी पी ही नहीं रही है। फेंक दे रही है।’ मैं माँ के पास जाता हूँ। वह केवल देखती है। आँखों में पहचान नहीं, अजनबीपन है। मैं काँप उठता हूँ। ‘माँ…ऐ माय…।’ माँ आँखें बंद कर लेती है। ‘चम्मच से पिलाकर देखो। शायद पी ले।’ मेरी आवाज़ ही नहीं, पैर भी थरथराने लगे हैं।
डेढ़ बजे रात में गरीबरथ ट्रेन दिल्ली से भगवानपुर पहुँची है…17 घंटे देर से।
‘न कुहासा, न और कोई प्रॉब्लम, फिर भी ट्रेन इतनी लेट।’
‘हमारे देश में बुलेट ट्रेन चलाने की योजना बन रही है लेकिन किसी भी रूट पर चले जाओ, तब देखो भारतीय रेल का सिस्टम।’
‘कभी ट्रेन की प्रतीक्षा में बारह घंटे प्लेटफॉर्म पर ही बीत जाते हैं तब पता चलता है कि ट्रेन कैंसिल हो गई है…।’
उतरने वाले यात्री एक दूसरे के पीछे खड़े अपनी खीझ निकाल रहे हैं। गाड़ी प्लेटफॉर्म पर रुकी हैं। लेकिन रुकने पर भी शांति नहीं है। चारों तरफ शोर है, हलचल है, यह घबराहट है कि कोई लेने आया है या नहीं…।
‘माँ जीवनभर गाँव में रही। श्राद्धकर्म गाँव से ही हो तो अच्छा है’ बड़े भैया ने फोन पर विवश घबराहट के साथ कहा है। ‘हमलोग को तो दोहरा खर्च पड़ गया।पता नहीं कहाँ से होगा सबकुछ…।’ वह काला कैक्टस चेहरा बन रहा है मेरा या किसी और का, पता नहीं लेकिन काँटों की चुभन से मैं तिलमिला उठा हूँ। मेरी आवाज घुट रही है ‘माँ फिर लौटकर आएँगी क्या!!!’ पर उस चेहरे पर काँटे ही काँटे हैं। कोई काँटा है जो अंदर चुभ गया है। टीस अब भीतर ही जमी बैठी है।
प्लेटफॉर्म पर उमस है, गर्मी है और एक-दूसरे को धक्का देकर आगे बढ़ते लोग हैं। संदीप रूमाल से हवा करके अपने पसीने सुखा रहा है। ‘पापा अब हम यहाँ प्लेटफॉर्म पर क्यों हैं?’ शैलजा ने परेशान होकर कुछ रूखे स्वर में पूछा है। सुरभि आँखों में प्रश्न लिये मुझे देख रही है। मैंने उससे कहा है कि गाँव में बहू की तरह रहना। वह सिर पर पल्लू डालकर सूटकेश पर ही बैठ गई है।’
‘अभी गाँव जाने के लिए कोई सवारी नहीं मिलेगी। सुबह ही बस या ऑटो से निकल पायेंगे। फिर भी देखता हूँ शायद कुछ मिल जाए।’ मैं प्लेटफॉर्म पार करता हूँ। चारों तरफ़ गंदगी। पान की पीक से रंगे दीवारों के कोने, मटमैले फर्श…। पर छोटी-छोटी दुकानें सजी हुई हैं। दुकानदार निंदियाई आँखों से भी जाग रहे हैं, इस आशा के साथ कि कहीं से थोड़ी कमाई हो जाए।
‘ओफ्फ! ये सड़कें हैं यहाँ की! यहाँ के नेता इलेक्शन जीत कैसे जाते हैं?’ शैलजा बार-बार गिरते सामान को पकड़ रही है। ऑटो दायें-बायें गड्ढों से होते हुए हमें उछालते हुए आगे बढ़ रहा है। ‘क्या पूरा रास्ता ऐसा ही है?’ संदीप ऑटोवाले से पूछता है। ‘हाँ लगभग…।’ ‘माई गॉड’…संदीप सुरभि की ओर देखता है। ‘मुझे लगता था कि गाँव की लाइफ़ आसान है, लेकिन यहाँ तो…सड़कें भी नहीं हैं।’
‘अभी गर्मी और मच्छर झेलने के लिए तैयार रहना’ शैलजा सूटकेश के ऊपर से गिरे थैले को उठाकर फिर सूटकेश पर रखती है। सुरभि ने पल्लू से सिर और चेहरेा ढँक रखा है। उसे धूल से एलर्जी है। ‘देखों ट्रक! सँभालकर चलाओ’ मैं जल्दी से बोलता हूँ। ट्रक और ऑटो दोनों एक ओर झुके हुए हैं। ‘घबराइये नहीं, हमलोग को ऐसी सड़कों पर ऑटो चलाने की प्रैक्टिस है।’
‘आज हमारा योगा तो रास्ते में ही हो गया। अब घर जाकर तुम लोग पहले नाश्ते का प्रबंध करना’। संदीप की बात पर सब खिलखिला उठते हैं। मैं भी थोड़ा हल्का हो जाता हूँ।
‘ज्ञान आ गए तुमलोग। बहुत अच्छा किया। डीह से ही आदमी की पहचान होती है लेकिन तुमलोग ने इसी को छोड़ दिया। कोई बात नहीं फिर से अब इसको सँवारो।’ सामने गाँव के चक्रधर काका खड़े हैं। मैं पैर छूता हूँ तो कहते हैं ‘तुमलोग ने तो आना ही छोड़ दिया है। अब अपने घर को देखो तुमलोग। क्या था और क्या हो गया!’ मैं देखता हूँ कि घर के पास कहीं धनहर खेत नहीं है। अरहर, मकई, सरसों, चने का साग…। माँ चने के साग को खोंटकर (तोड़कर) मिट्टी की हाँड़ी में पकाती। उसकी सुगंध ऐसी कि खाने से मन ही नहीं भरता। शहर में वैसा साग कभी नहीं बना। न शैलजा बना पाई और न उसकी मम्मी। माँ ने तरीके बताये, फिर भी नहीं। मैं दूर तक नजरें दौड़ाता हूँ पर कहीं कुछ नहीं, किसी फसल के कटने की निशानी भी नहीं। हाँ हर जगह काफ़ी अच्छे-अच्छे दो मंज़िले, तीन मंज़िले मकान बन गए हैं। सड़कें चौड़ी और पक्की हैं। अब लोग कुआँ पर भी पानी भरने नहीं जाते। घर के सामने एक कुआँ था लेकिन लगता है कि उसे भी भरवा दिया गया है।
‘लोग पानी क्या यहाँ से लेते हैं?’ मैं घर के थोड़ा आगे लगे चापानल को देखता हूँ। ‘यहाँ सब लोगों ने अपनी बोरिंग करवा रखी है। सब घरों में टंकी और नल हैं। जब लाइट रहती है तो मोटर से पानी टंकी में चढ़ जाती है। अब इन्हें कुआँ और चापानल की कोई जरूरत ही नहीं है।’
बड़े भैया के सख़्त और खींचे चेहरे की झुर्रिया में काफ़ी दर्द है, बेतरतीब-सा। जैसे काफ़ी वर्षों से उन्होंने इसे हटाने की कोशिश भी नहीं की है। एक लंबी साँस लेकर मैं अपने घर को देखता हूँ। दरारों से भरी दीवारें जैसे हमें मुँह चिढ़ा रही हैं।
‘अब अगर एक भी भूकंप आया तो यह मकान तो गिरेगा ही गिरेगा।’ खिचड़ी बालों के बीच बड़े भैया का वही चेहरा…। जकड़े हुए जबड़े…। कोटरों में धँसी आँखों में टूटन…। पर नहीं टूटने का जबरन एहसास दिलाने की वही पुरानी जिद्द।
मेरी आँखें ढूँढ़ रही हैं पंचमुखी अढ़हुल, कचनार, हरसिंगार और द्वारपाल की तरह खड़े शीशम के दो पेड़ों को…। माँ कचनार के फूलों की पकौड़ी जब बनाती तो बनते-बनते ही सबकुछ चट हो जाता…। कुआँ के पास हरसिंगार था। छोटा-सा, पर छतनार…। नीचे बिड़े फूलों को हमलोग हथेलियों में लेकर जब सूँघते तो ऐसा लगता जैसे इसी में जिंदगी की सारी सुगंध निचोड़ दी गई हो। पंचमुखी अढ़हुल को तो सुबह तीन बजे से ही लोग तोड़ने की ताक में रहते, लेकिन बाबूजी…।’ ‘श्वान निद्रा, बको ध्यानम्…।’ यदा-कदा ही वे फूल लोगों के हाथ लग पाते। लेकिन अब कहीं कुछ नहीं है। शीशम का वह पेड़ भी नहीं…। गिरती हुई दीवारें…जिस पर अभी-अभी सफेदी हुई है से सटी टूटी आरामकुर्सी रखी है। ‘बहुत दिनों से अजित नहीं आया?’ ‘कौन अजित?’ ‘अरे संजय सिंह का बेटा जिसका ससुराल जगतपुर है। अरे मीरा की बेटी से उसका विवाह हुआ है न। मीरा मेरी बचपन की सखी थी। चली गई बेचारी। सुनते हैं बड़ा कष्ट था।’ क्यों क्या हुआ था?’ बहू बड़ी खड़मपड़ाही आई…।’ चश्मा के भीतर से जैसे आज भी माँ की आँखें झाँकती हैं।
‘तुम्हारी माँ के बिना यह द्वार सूना हो गया। यहीं बैठी-बैठी सड़क पर जाते लोगों में जैसे वह अपने परिचितों को तलाशती रहती थीं। जब से वे तुम्हारे साथ शहर गई, तब से हमलोग का भी मन इधर से उचट गया’। चक्रधर काका पास रखी चौकी पर बैठ गए हैं। मैं देखता हूँ काफी कुछ नहीं है। ‘आँवले का वह बड़ा-सा पेड़, वह कैसे गिर गया? वह तो काफ़ी घना था। खजूर का पेड़ भी नहीं है।’ ‘अरे सब खत्म हो गया तुमलोग शहर क्या गए वहीं के होकर रह गए। पलटकर देखा भी नहीं।’ चक्रधर काका गमछी से पसीना पोंछते हैं।
सामने संदीप है। खिले गुलमोहर के फूल उसके भीतर जैसे एक नया संसार रच रहे हैं। दूर सूरज की रोशनी में चमकते पर्वत को देखता हूँ तो लगता है कि यह जरा भी नहीं बदला। कहते हैं कि इसी पर्वत को मथानी बनाकर समुद्र मंथन हुआ था। पहले दुर्गा पूजा होती तो परिवार के सारे लोग यहाँ आते। ठहाके, मस्ती, जिंदादिली, नाटक…गीत, भजन…। तब परिवार में चचेरा, ममेरा और फुफेरा का अंतर कोई समझ ही नहीं पाता। पिकनीक के समय बड़ी माँ, माँ, काकी, भाभी सभी मिलकर कतरनी चावल की खिचड़ी पकातीं और हमलोग मंदार पर्वत पर घूमते हुए कभी शंख कुंड देखते और कभी शुकदेव मुनि की गुफा को देखने निकल पड़ते। शुकदेव मुनि की गुफा खतरनाक नुकीले चट्टानों से आगे काफी सँकरे रास्ते के बीच थी, जहाँ मैं कभी नहीं पहुँच पाया।
कहा जाता है कि मथानी बनाने के लिए इस पर्वत को शेषनाग से बाँधा गया था। पर्वत के चारों ओर साँप के चिह्नों को हम बड़े कौतूहल के साथ देखते। बाबूजी कहते थे कि पहले इस पर दूधिया नदी भी बहती थी। धारा बिल्कुल शीतल और दूध की तरह मीठी…। पर उस समय तक वह सूख चुकी थी। मधुकैटभ एवं अन्य असुरों की टूटी मूर्तियों को देखकर नरेन्द्र का जरूर बोलते ‘देखो इन असुरों को। भगवान मधुसूदन ने इसी पर्वत पर इन्हें मारा था।’
बचपन में बाबूजी के कारण कहानियाँ सुनने की ऐसी आदत पड़ी कि बिना कहानी सुने नींद ही नहीं आती। एक दिन बाबूजी ने एक साधु की कहानी सुनाई, जो पंद्रह दिनों तक इसी पर्वत पर अन्य साधुओं के साथ रहे थे। एक दिन कुछ साधुओं ने उनसे भाँग पीसने की जिद्द की तो वे वहीं पत्थर पर भाँग पीसने बैठ गए। लेकिन यह क्या जैसे ही उन्होंने भाँग पीसना शुरू किया कि पूरा पर्वत हिलने लगा। सभी साधुओं ने भयभीत होकर हाथ जोड़ लिये। पूछा कि आप कौन हैं? काफ़ी मिन्नत के बाद वे बोले ‘मैं अश्वत्थामा हूँ। यहाँ के शांत वातावरण को देखकर मैं यहाँ चला आया।’ बोलकर अश्वत्थामा तो गायब हो गए लेकिन अन्य साधु काफ़ी दिनों तक इस आत्मग्लानि से भरे रहे कि जिनसे आशीर्वाद लेना चाहिए उनसे उन्होंने भाँग पिसवाई।
मैं एक पल के लिए सोचता हूँ तो लगता है कि अभिशाप न जाने किसे, कहाँ और कितनी तरह का दंश सहने के लिए विवश कर देता है। न मृत्यु, न मोक्ष…और न जिंदगी। मैं कमरे की छत को देखता हूँ। प्लास्टर उखड़ा हुआ है। पता नहीं कब सिर पर गिर जाए। दीवार और छत की संधि रेखा में कोने पर दो छेद हैं…। पलंग पर बैठता हूँ तो लगता है कि उस छेद से कोई झाँक रहा है। बाबूजी कहते थे कि शांति न मिले तो आत्मा भटकती है।
‘सबने सब कुछ तो खतम कर दिया…।’ फिर वह काला कैक्टस किसी का चेहरा बन रहा है। उसकी भारी-सी आवाज में गजब का आकर्षण हैं…। मैं परेशान होकर टूटे दरवाज़े को देखता हूँ। शैलजा और सुरभि सामान अंदर ला रही हैं। कोने के छेदों में से फिर दो आँखें झाँकती हैं। मैं पहचान लेता हूँ माँ की ही आँखें हैं बड़ी-बड़ी भूरी-सी। ‘यही भंडार घर है। भोजभात में कुछ घंटे नहीं…जगहँसाई होती है।’ ‘करूँगा, सबकुछ करूँगा।’ मैं बेचैन होकर बाहर निकलता हूँ कि वह आवाज मेंरे दिमाग से चिपकने लगती है ‘क्या यह केवल तुम्हारा ही कर्त्तव्य है…?’ मैं गौर से देखता हूँ। चेहरे के ऊपर दो सींगें भी हैं नुकीले-नुकीले…जो मेरी ओर ही बढ़ रहे हैं।
‘यहाँ पर खाने की और उधर दक्षिण दिशा में पूजा की व्यवस्था करवा देता हूँ।’ बड़े भैया चलते हैं तो लगता है कि अब गिर पड़ेंगे। उनसे पूछना चाहता हूँ कि ‘आप खाना-पीना ठीक से क्यों नहीं करते? देह में तो जैसे कुछ बचा ही नहीं है’ लेकिन पूछता नहीं। कहता हूँ ‘हाँ, ठीक है।’
‘कौन-कौन कितना दे रहा है?’ सींगों की चोट से मैं घबराने लगा हूँ। बड़े भैया मेरी ओर ही आ रहे हैं। कोटरों में धँसी उनकी आँखों में चिंता है और व्याकुलता भी…।’ सबके पास सबकुछ हैं…पर कुछ लोग हमेशा रोते रहते हैं ताकि उन्हें किसी को कुछ देना नहीं पड़े।’ सींगों ने मुझपर वार करना शुरू कर दिया है।
‘यह तो यज्ञ है ज्ञान। निष्ठा और आस्था से सबकुछ हो तो अच्छा है।’ चक्रधर काका भी मेरी ओर ही देख रहे हैं। ‘हाँ, तो फिर इसे हवन सामग्री ही बना दो’ फिर वही नुकीला सींग…। मैं पसीने से तरबतर हो गया हूँ। काफ़ी बेचैनी है।
‘क्या हुआ ज्ञान? तुम्हारा ब्लडप्रेशर तो नार्मल है न?’
‘हाँ, हाँ बिल्कुल’। मैं बड़े भैया की पनियाई आँखों को देखता हूँ। इनका ब्लडप्रेशर तो काफ़ी हाई हो गया था। शैलजा ने बताया था कि बड़े पापा गिर गए हैं…लेकिन काम का प्रेशर इतना था कि मैं इनसे कुछ पूछ ही नहीं पाया।
‘पापा यहाँ की साइट तो काफ़ी अच्छी है।’ संदीप पर्वत की ओर देखता है। पुरवैया का झोंका उसके चेहरे से गुजर रहा है। ‘अरे दूर-दूर से लोग यहाँ इस पर्वत पर आते हैं’ चक्रधर काका के चेहरे पर गुलाब खिल रहा है, ‘लेकिन तुमलोग तो…लगता है कि इस बार दस-बारह वर्षों के बाद आए हो।’ काका मेरी ओर मुड़ते हैं। ‘ज्ञान अपना घर कोई इस तरह छोड़ता है क्या?’ ‘बाबूजी के बाद यह घर, घर रहा ही कहाँ काका!’ मैंने लंबी साँसें लीं। वह काला कैक्टस अब तर्जनी बन गया था। एक तर्जनी, दो तर्जनी, तीन, चार, पाँच…फिर लंबे हाथ…! एक हाथ में घड़ा, पानी से भरा हुआ। मेरा कंठ सूखने लगा। ‘शैलजा एक ग्लास पानी देना।’ ‘क्या हुआ पापा?’ शैलजा मेरी आवाज से चौंकी है, काफ़ी परेशान भी हो गई है।
हलचल…शोर…। जन्म ही नहीं, मृत्यु भी शायद एक उत्सव है। जीवन के संघर्षों से मुक्ति का उत्सव! ‘ज्ञान तुमने काफ़ी अच्छा निर्णय लिया माँ का क्रियाकर्म यहाँ से कराने का। तुम्हारे बड़े भैया तो बिल्कुल निरीह प्राणी हैं तुमलोग इसी तरह बीच-बीच में आया करो तो सबको अच्छा लगेगा…।’ ‘निरीह प्राणी’! मेरे भीतर कहीं कुछ चुभा है… ‘निरीह प्राणी’ ….‘निरीह प्राणी’ क्यों और कैसे…?’ मेरी आँखें बड़े भैया पर जम जाती हैं। दुर्बल शरीर…आँखों में न झुकने का भाव…, जर्जर अहंकार..! बड़े भैया रिश्ते को सहेज नहीं पाये। इसका ‘मैं’ प्रबल है या पैसों के प्रति मोह मैं समझ नहीं पाता लेकिन एक दिन यह अकेला रह जाएगा…’ मेरा शरीर झनझनाहट से भरने लगा है। मैं अँधेरे में देखता हूँ। बाबूजी भी यहीं कहीं हैं शायद माँ के ही साथ…।
वापस शहर लौट रहा हूँ। ट्रेन की रफ़्तार काफ़ी तेज़ है। ‘ज्ञान यहाँ घर बनवाओ। अब तो तुम्हारे बच्चे भी सेटल कर गए।’ चक्रधर काका की आँखें अब हर समय पानी से भरी रहती हैं। ‘हाँ पापा, बीच-बीच में आते रहेंगे हमलोग। यह पॉल्यूशन फ्री इलाका भी है।’
‘पॉल्यूशन केवल गाड़ियों और फैक्ट्रियों से नहीं फैलता बच्चे, शब्दों से भी फैलता है। इतना कि एलर्जी भी बीमारी बन जाती है।’ कैक्टस के काँटे चुभते ही नहीं बोलते भी हैं। लेकिन यह संदीप को नहीं मालूम है।
‘ज्ञान बाबू, देवरानी रुठी ही रहेगी क्या?’ ‘नहीं भाभी, उसका शूगर काफ़ी बढ़ा हुआ है, इसलिए डॉक्टर ने मना किया उसे यहाँ लाने से।’
मैं देख रहा हूँ कि पूरा मोहल्ला हमारा घर बन गया है। ‘अरे इसको यहाँ मत रखो…ध्यान रखना रसगुल्ले की चाशनी का पाक कड़ा हो ताकि गर्मी में यह खराब नहीं हो।’ ‘दूध को खूब औसाना। इससे दही अच्छा जमेगा।’ ‘रायता के लिए राई इधर दे दो मैं साफ़ कर देती हूँ नहीं तो किनकिन करेगा…।’
‘नहीं हमलोग हैं यहाँ। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमलोग सँभाल लेंगे।’ युवकों का समूह खड़ा है चार सौ लोगों को खिलाने के लिए…। पुष्पा भाभी दौड़-दौड़कर रसोईये को निर्देश देती हैं। अचानक बोल उठती हैं ‘अरे उनको बुलाया या नहीं? नहीं तो रुठे को मनाना मुश्किल होगी।’ वहाँ ठहाका गूँजता है। ‘उनको’ यानी सुलतानपुर वाली फूफी को जो हमारे गाँव में ही बस गई हैं, लेकिन बिना निमंत्रण-कार्ड के नहीं आ सकतीं। ‘परिवार के लोग नहीं आए क्या?’ ‘हाँ आ तो गए सब…बेटा, बेटी, पोता-पोती…भरा-पूरा परिवार है। सब चचेरा, ममेरा, फुफेरा कहाँ…? किसको और कौन देखता है?’ मैं गहरी साँसें लेकर व्हाट्स ऐप पर आए कई शोक सदेशों को देखता हूँ…। केवल औपचारिकता और व्यावहारिकता…। जगह की दूरियाँ कब संबंधों की दूरियाँ बन गई पता ही नहीं चला।
ऑफिस में वर्मा जी कहते हैं, ‘समय नहीं रुकता और काम भी नहीं…सो अब लोग तीन दिनों में ही पूजा-हवन करके सबकुछ निबटा देते हैं।’
‘माँ की इच्छा था कि सबकुछ वैदिक रीति से ही हो..इसीलिए…।’
‘पहले के लोग तो हमारी समस्याएँ नहीं समझते थे न ज्ञान बाबू। उनके लिए चौदह-पंद्रह दिन निकालना भी कठिन नहीं था, लेकिन अब तो नींद भी मेट्रो या बसों में खड़े-खड़े ही पूरी होती है। संडे को भी सप्ताह भर के पेंडिंग कामों का प्रेशर…।’ ‘अरे ज्ञान मेरे पास बैठो न थोड़ी देर। यह तो मेरे पास आता ही है फिर से चले जाने के लिए।’ माँ के कुंठित स्वर गर्म हो रहे हैं, पिघल रहे हैं और मेरे अंतर में फफोले उठ रहे हैं, एक…दो…तीन…चार…।
संदीप, सुरभि और शैलजा सामान बाहर निकाल रहे हैं। बड़े भैया सड़क के किनारे लाल कनेर के पास चुपचाप खड़े हैं। वे अब कम बोलते हैं लेकिन कभी-कभी जब बोलते हैं तो लगता है कि वे न बोलें तो ज्यादा अच्छा है। तने हुए धनुष की तरह उनकी मुखमुद्रा तब बदलती है, जब पुष्पा भाभी की तीन वर्ष की पोती हँसते हुए आती है और दादा जी कहकर उनसे लिपट जाती है। बड़े भैया उस समय बिल्कुल बच्चा बन जाते हैं। ‘अब तो तुमलोग यहाँ आओगी नहीं?’ बड़े भैया हँस रहे हैं या रो रहे हैं पता नहीं चलता।
‘हमलोग यहाँ अपना घर बनाएँगे बड़े पापा।’ मैं कुछ बोलूँ इससे पहले ही संदीप बोल उठता है।
‘इस घर को तो गिराना ही पड़ेगा। यह कब गिर जाए पता नहीं।’
‘हाँ सारी पुरानी चीजें तो खत्म ही हो गई।’ बड़े भैया की आवाज दूर से आती ट्रेन की घरघराहट की तरह लगती है। पटरियों का कंपन मैं अपने भीतर महसूस कर रहा हूँ। ट्रेन के शीशे पर बारिश की बूँदें गिरने और फिसलने लगी हैं। वहाँ से धूल, मिट्टी भी हटने लगी है। मेरी आँखें नींद से इस तरह बोझिल हैं जैसे वर्षों से मैं सोया ही नहीं हूँ। माँ ठीक कहती थीं। काँटे वाले पौधे को घर में रखने से गाहे-बगाहे काँटे चुभ ही जाते हैं।
Image :Profile Head of an Old Woman
Image Source : WikiArt
Artist :Jan Lievens
Image in Public Domain