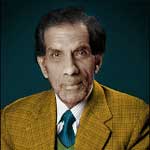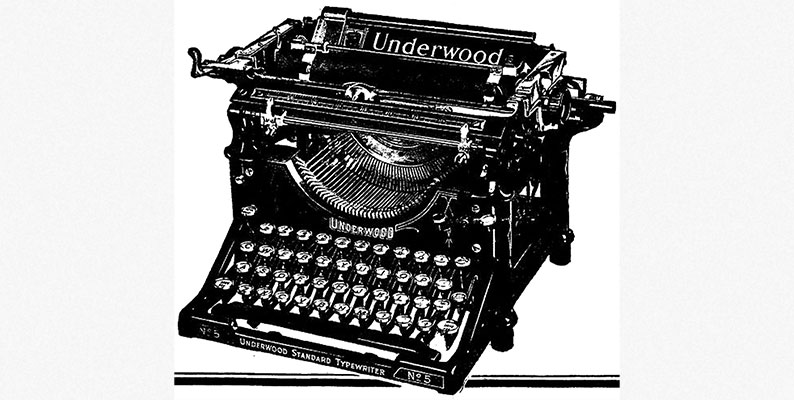पोस्टमार्टम
- 1 April, 2025
शेयर करे close
शेयर करे close

शेयर करे close
- 1 April, 2025
पोस्टमार्टम
कुछ घटनाएँ ऐसी होती हैं जो कि जीवन भर के लिए अपने स्मृतिदंश छोड़ जाती हैं। और मनुष्य वर्तमान में रहते हुए भी अतीत के आतंक से विवश हो जाता है। अनेक दुर्घटनाएँ प्रतिदिन घटित होती हैं। लोग समाचारपत्रों में शीर्षक मात्र पढ़कर रह जाते हैं। किसे फुर्सत है–व्यौरेवार पढ़ें। सरसरी तौर पर दृष्टि दौड़ा ली। कहीं दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति अपना परिचित तो नहीं। डॉ. चन्द्रप्रकाश द्विवेदी भी स्थानीय अख़बारों में एक ख़बर बन कर रह गए थे। नगर से जुड़े हुए कस्बे में स्थित राजा बल्देव प्रसाद महाविद्यालय के भूगोल विभाग के अध्यक्ष।
द्विवेदी जी अपनी ज़िंदादिली, परोपकारी प्रवृत्ति और सामाजिकता के कारण लोकप्रिय थे। चार भाइयों में तीसरे क्रम पर जन्मे चन्द्रप्रकाश को परिवार से विशेष सहायता नहीं प्राप्त हुई थी। घर में शिक्षा का न तो प्रचलन था न ही महत्त्व। अपनी जिद् से ट्यूशन व छोटे-छोटे काम करते, कठिनाइयों के साथ, पढ़ाई जारी रखी थी। अंततः प्रथम श्रेणी में एम.ए., रिसर्च तत्पश्चात् उन दिनों नए खुले महाविद्यालय में नियुक्ति। अपने अध्यवसाय के बल पर वे चर्चित हुए और सम्मानित भी। कम आयु में ही विभागाध्यक्ष भी बने। कुछ वर्षों के उपरांत एक छोटा-सा मकान भी बनवा लिया।
वह प्रतिदिन की भाँति मोटरसाइकिल से विद्यालय हेतु निकले थे। कस्बे वाले मार्ग में एक साइकिल सवार को बचाते-बचाते एक तेज़ रफ्तार से आ रहे ट्रक द्वारा पीछे से टक्कर लगी। ट्रक के पहिये उनके ऊपर से गुज़र गए। ट्रक की तोड़-फोड़, ड्राइवर को मारपीट कर पुलिस को सौंपना तथा सड़क पर जाम लगाने की परवर्ती घटनाएँ तो महत्त्वहीन थीं, परंतु डॉ. द्विवेदी का प्राणांत अस्पताल ले जाने से पूर्व घटनास्थल पर ही हो गया। जैसा कि आमतौर पर होता है पुलिस की जाँच के बाद लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने की तैयारी हो गई। इस समय तक कॉलेज के छात्र, प्राध्यापक और क्षेत्र के महत्त्वपूर्ण व्यक्ति एकत्रित हो गए थे। लोग अड़ गए–पोस्टमार्टम की क्या आवश्यकता है? मृत्यु के पीछे कोई रहस्य तो है नहीं। पुलिस विभाग की अपनी विवशताएँ थीं। आख़िर काफ़ी हील हुज्जत, जिसमें प्रभावपूर्ण स्थानीय नेताओं का दबाव भी शामिल था, पोस्टमार्टम नहीं हुआ। मजिस्ट्रेट के आदेश से पंचनामा आदि औपचारिकताएँ पूरी कर लाश परिजनों को सौंप दी गई। इस सब में शाम हो गई थी। इस बीच सहकर्मियों ने उनके गृहनगर में पारिवारिक सदस्यों को सूचित कर दिया था। ख़बर पाकर बिलखते वृद्ध पिता, भाई और रिश्तेदार आ गए थे। यहाँ गोरखपुर में तो पत्नी सुधा और बारह वर्षीय एक मात्र पुत्री सुमेधा को छोड़कर था ही कौन? यद्यपि डॉ. द्विवेदी के मित्रों की संख्या कम नहीं थी। कई परिवारों से घनिष्ट संबंध थे। रोती बिलखती पत्नी और पुत्री को इन्हीं लोगों ने सँभाला था।
अगले दिन प्रातः श्मशान घाट पर स्थानीय मित्रों, सहकर्मियों एवं परिचितों के अतिरिक्त बाहर से आए रिश्तेदार एकत्रित हो गए थे। बड़े भाई ने अनुज को मुखाग्नि दी। चिता प्रज्वलित होते ही लोग गुटों में बिखर गए थे। दुनिया-जहान की बातें। एक चाचा कह रहे थे, ‘भइए इसने तो पूरे समय मेरे यहाँ रह कर पढ़ाई की। अक्सर बेचारे के पास फीस तक न होती। मुझसे कहता…!’ श्मशान पर इस तरह की बातें शायद संवादहीनता की खाई को पाटने की कोशिश में होती हैं। क्योंकि मौन के शून्य से विचार उत्पन्न होता है और ऐसे वक्त पर लोग विचार के आर्तनाद से बचना चाहते हैं।
घाट के कार्यक्रम निपटते लौटते शाम धुँधला आई थी। घर के चार-पाँच कमरे जो लगभग बंद ही रहते, निकट और दूर के संबंधियों से भरे हुए थे। कुछ तो ऐसे थे जिन्हें बारह वर्षीय सुमेधा ने पहली बार देखा था। इसके लिए तो सभी अंकल या आंटी थे। ज्यादातर घर से बाहर रह कर पढ़ाई और दूर नगर में नौकरी और अंतरजातीय प्रेम विवाह के कारण जब चन्द्रप्रकाश के ही संबंध परिजनों से अधिक निकट नहीं रह पाए थे तो पत्नी और पुत्री के कैसे होते। दरअसल संपन्न परिवार में जन्म के बावजूद न के मोह और रूढ़िगत मान्यताओं के कारण पिता से सहायता तो नहीं ही मिली बल्कि उपेक्षा और अवरोधों ने उनके मन में एक विरक्ति सी पैदा कर दी थी। संस्कारी कर्तव्य भावना के कारण वह उनकी यथासंभव सहायता तो करते परंतु ज्यादा निकटता नहीं रही थी।
सुमेधा सहमी सी थी। एक ओर जड़ होकर रह गई। बीच-बीच में रोती माँ, फुसफुसाते इशारे, दूसरी ओर घर में अपरिचित चेहरों की भीड़। उसे इंगित कर फुसफुसाते इशारे–‘अभागी’…आदि। वह निष्प्रभ हो गई थी। इतनी समझदार तो थी कि पिता के न होने का मतलब समझ सके। उसे फूट कर रुलाई आती, परंतु उन सबकी बातें सुन और अव्यवस्थित घर देखकर उसे गुस्सा आता।
माँ-बाप के एकात्म प्यार और दुलार ने उसे कुछ जिद्दी और अंतर्मुखी बना दिया था। पिता से प्राप्त संस्कारों और अनुशासन की भावना ने इस उम्र में ही व्यवस्था प्रिय भी। अपने खिलौने, किताबें, कपड़े आदि यथास्थान रखती। वह देख रही थी घर आए मेहमानों, उनके साथ आए बच्चों ने उनके खिलौने, किताबें उलट-पुलट दिए थे। एक आंटी ने तो उसकी सबसे अच्छी फ्रॉक अपनी बच्ची को पहना दी थी। यद्यपि उसके बहुत ढीली थी। उसका मन विरोध करने का हुआ पर समझ गई कि यह समय उपयुक्त नहीं। वह रोना आ रहा था लेकिन यह सब देखकर क्षुब्ध थी कि लोग उसे रोने भी नहीं दे रहे थे।
रात में कमरे में परिवारजन के अतिरिक्त संवेदना प्रकट करने आए आत्मीयजन भी थे। बड़े भैया पोस्टमार्टम न होने की महिमा का बखान कर रहे थे, ‘यह तो कहो बहुत अच्छा हुआ जो पोस्टमार्टम नहीं हुआ। भाग्यवान थे। शरीर की दुर्गति बच गई।’
सुमेधा ने सोचा पोस्टमार्टम क्या होता है? उसने किसी से पूछना चाहा। माँ अंदर आँगन में औरतों से घिरी थी। ग़ौस चाचा सबके साथ कमरे में थे। उनसे भी नहीं पूछा जा सकता। ग़ौस मोहम्मद उसके पिता के निकटतम मित्र थे। एक दूसरे की सहायता को सदा तत्पर। रोज़ का मिलना-जुलना, द्विवेदी जी उन्हें अपना बड़ा भाई मानते। सुमेधा के ग़ौस चाचा कम, दोस्त अधिक थे। उसे जब कुछ पूछना होता–कोई शब्द या गणित का प्रश्न। वह पिता को सोते से जगा कर उसी समय पूछ लेती। ठीक है वह स्कूल में टीचर जी से पूछ लेगी।
तेरहवीं तक हलचल तो रही परंतु एक मर्यादित चुप्पी के साथ। लखनऊ वाले चाचा जी बोर हो गए थे। साथ लाई ‘सत्यकथा’ पढ़ डाली थी। समय काटने को कुछ चाहिए था। उन्होंने पुस्तकों की अलमारी देखी। डॉ. चन्द्रप्रकाश को पढ़ने का शौक़ी था। न केवल भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र बल्कि साहित्यिक पुस्तकों का अच्छा-ख़ासा संग्रह था। ‘ऊँह!’ उनके चेहरे पर ऊब के भाव आए, ‘भाई साहब ने भी क्या कूड़ा इकट्ठा कर रखा है।’ बुदबुदाते हुए उन्होंने इधर-उधर, दो-तीन पुस्तकें निकाल ली थीं।
तभी चाची उनके लिए चाय-नाश्ता ले आई। सुमेधा खड़ी रही। चाचा जी ने चाय का प्याला एक पुस्तक पर रख लिया। नाश्ता टूंगते दूसरी किताब के पृष्ठ पलटने लगे। चाची ने सुमेधा को वहाँ देख सहानुभूति प्रकट की, ‘ओ! क्या नाम सुमेधा, तू भी रसोई में जाकर निपट ले।’ फिर गहरी साँस ले चिंता प्रकट करते हुए एकालाप किया, ‘हाय! बिना बाप की जवान होती लड़की। भगवान की लीला।’ सुमेधा ने जैसे कुछ सुना ही नहीं था। वह तो किसी तरह प्रयास कर अपने को रोक पा रही थी। इतने ही दिनों में लगभग सभी ने उसे प्यार से बिगड़ी जिद्दी लड़की करार कर दिया था। उसके मन में आया चाय का कप किताब से उठा फेंके। और किताब अलमारी में वापस रख दें। पापा उससे कितना प्यार करते थे, परंतु किताबों के मामले में उसे भी डाँट पड़ जाती, ‘यह किताबें इस तरह क्यों फैली हैं’ अथवा ‘खाते हुए जूठे मुँह नहीं पढ़ते। सरस्वती का अपमान होता है।’ वे समझाते। वह रुआँसी कमरे से निकल आई; ‘ख़ुद ही विद्या नहीं आएगी। मुझे क्या?’
तेहरवीं के दो दिन पहले देवर ने सुधा से कहा, ‘भैया के बीमा, बैंक के काग़ज़ निकालो तो आगे की कार्रवाई शुरू की जाए।’ सुधा काग़ज़ों वाला बक्सा उठा लाई। देवर कलेक्ट्रेट में बाबू था। उसने काग़ज़ातों की पड़ताल आरंभ की। सुधा का भाई भी वहीं आ गया। सुधा औरतों के साथ एक कोने में बैठी थी। तीन बीमा पॉलिसियाँ। एक पॉलिसी, जो विवाह के पहले की थी–नामांकन पिता का था। चन्द्रप्रकाश नामांकन बदल कर पत्नी के नाम करने के लिए आज-कल में सोचते रह गए। उन्हें आगत का क्या पता था। शेष सभी बैंक और बीमा के काग़ज़ात पति-पत्नी के संयुक्त नामों से थे। देवर ने पिता के नामांकन वाली पॉलिसी रख ली। बाक़ी छोड़ दिए।
सुधा के लिए जैसे सब कुछ व्यर्थ था। अवाक्, निश्चल, कठपुतली की भाँति सब कुछ निपटा रही थी। बीमारी से होने वाली मृत्यु में आत्मीयजन, धीरे-धीरे आगत परिस्थितियों हेतु एक प्रकार से स्वयं को तैयार कर लेते हैं, परंतु आकस्मिक उपजे अभाव में तो मन विश्वास ही नहीं कर पाता। सब कुछ स्वप्नवत। सुधा के भाई को एतराज हुआ पर वह तेरहवीं होने तक मामला बढ़ाना नहीं चाहता था।
रिश्तेदारों ने जाने की तैयारी कर ली थी। छोटे चाचा ने अलमारी से किताबें छाँट कर रख ली थी। ‘भइय्या तो रहे नहीं पढ़ेगा कौन?’ बड़े चाचा ने पापा का सूट और पैंट का बंडल बना लिया था। ‘यहाँ क्या होंगे? ले दे के एक लड़की।’ कहते हुए उनके चेहरे पर दर्प उभर आया था। चार पुत्र थे उनके।
सुमेधा का दिल बैठा जा रहा था–‘क्या चाचा जी सचमुच सूट ले जाएँगे। इस नीले सूट में पापा कितने स्मार्ट दिखते थे।’ उनकी आँखें डबडबा आईं। उसने देखा कमरे में कोई नहीं था। उसने चुपके से कपड़ों का बंडल और किताबें बड़े बक्से के पीछे फेंक दिया। अगले दिन वे फिर एकत्रित हुए। ससुर, जेठ, देवर और भाई सभी चिंताग्रस्त थे। ससुर और जेठ ने एक प्रकार से आज्ञा देते हुए कहा, ‘बहू! कल तैयारी कर लो। गाँव चलना होगा। बिटिया भी बड़ी हो रही है। इसका भी वर-विवाह देखना है। यहाँ का मकान आदि बाद में बिकता रहेगा। तुम्हारे जेठ, देवर देख लेंगे।’ उन्होंने निर्णय सुनाया।
सुधा ने कुछ कहना चाहा पर चुप रह गई। उसने सहायता की याचना से इधर-उधर देखा। यद्यपि मकान के संबंध में विवाद था। जहाँ ससुर जी की राय उसे बेचने की थी। वहीं उनके पुत्रों के सामने अपना भविष्य था। उनके तीनों पुत्र मकान को किराये पर उठा देने के पक्ष में थे। रात की बहस के बाद भी सहमति नहीं बन पाई थी। भाई ने दबे स्वर में कहा, ‘मकान तो निकालना ही होगा। यहाँ तुम लोग कैसे रहोगी? चाहो तो साथ चलो।’
अब उससे रहा नहीं गया। वह सफ़ेद धोती सिर पर आगे खींच कर बोली, ‘ग़ौस भाई साहब बता रहे थे कि मुझे क्षतिपूर्ति आधार पर कॉलेज में नौकरी मिल जाएगी। फिर सुमेधा की पढ़ाई…!’
इस बार ससुर जी की आवाज़ तेज़ थी, ‘नौकरी-चाकरी तो हमारे ख़ानदान में किसी औरत ने की नहीं। रही क्षतिपूर्ति, तो अपना छुटका कर लेगा। हाईस्कूल पास बैठा है। बिटिया भी बहुत पढ़-लिख चुकी, दो-चार बरस देख-सुनकर कहीं नत्थी करना है।’
‘एक बात और कान खोलकर सुन ले, यह ग़ौस-बौस, म्लेच्छों का आना-जाना, मुझे पसंद नहीं।’ वह तैश में आ गए। पहले उन्होंने ग़ौस को कोई कायस्थ वग़ैरह समझा था। कल जब उनकी पत्नी को बुरका पहने देखा मन भिन्ना गया।
‘एक-दो दिनों में ट्रक की व्यवस्था हो जाएगी। फ़ालतू सामान किताबें, रद्दी आदि यहीं फरोख्त हो जाएगा। पोढ़ा-पोढ़ा सामान रख लो…’ जेठ ने निर्णय की घोषणा कर दी। जब सामान जाना ही है तो साथ रखने वाला सामान ट्रेन में भी जा सकता है। टूट-फूट भी नहीं होगी। जेठानी ने टू-इन-वन, देवरानी ने क्राकरी सँभाल ली थी। चाचा लोगों को कपड़ों का बंडल और किताबें नहीं मिल रहे थे। छोटी चाची ने उसे सामान छिपाते देख लिया था। उन्होंने बता दिया। प्रतिक्रिया स्वाभाविक ही थी, ‘यह जितनी ज़मीन से ऊपर नहीं, उतनी अंदर है।’
‘अरे ये शहर की अँग्रेज़ी पढ़ने वाली छोकरियाँ सब मामलों में चालू…’ सबने अपनी भड़ास निकाली। सुधा को क्रोध आ गया। उसने सुमेधा को दोनों हाथों से पीटते हुए, ‘अरे कुलच्छनी तू भी उनके साथ क्यों न मर गई।’ कह कर रो पड़ी। सुमेधा ने पहली बार माँ को इतने गुस्से में देखा था। वह सिसकने लगी।
रात में विवाद पुनः प्रारंभ हो गया। ‘आपने बीमा पॉलिसी रख ली। पत्नी का अधिकार पहला होता है। नॉमनी चाहे जो भी हो।’ सुधा का भाई कह रहा था। ‘देखिए हम भाइयों का कोई बँटवारा नहीं हुआ था। भाई ने कोई वसीयत भी नहीं की है। हम सभी संपत्ति में हिस्सेदार हैं।’ देवर ने तर्क दिए।
सिसकते-रोते सो गई सुमेधा तेज़ आवाज़ें सुनकर चौंककर जग गई। वह आश्रय हेतु माँ से चिपक गई। सुबह ससुर ने पूछा, ‘क्या सोचा बहू?’ उन्हें विरोध की ज़रा भी आशंका नहीं थी। संदेह था कि वह मायके जाने के पक्ष में निर्णय न ले ले।
‘बाबू जी मैं यह घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी। उनकी इच्छा इसे डॉक्टर बनाने की थी।’ उसने अपना निर्णय बता दिया। ‘क्या…?’ ससुर, जेठ, देवर, भाई सब अवाक् रह गए थे। इसके बाद समझाना, अकेले पड़ जाने की आशंका, प्रत्यक्ष धमकियाँ सब उपाय अजमाए गए, लेकिन उसका निर्णय दृढ़ था। उसी शाम और अगले दिन तक सभी लौट गए, भाई भी। सामने था गुबार-सा फैला अंतहीन समय।
सदा का सजा-सँवरा व्यवस्थित घर बारात की विदाई के बाद का-सा प्रतीत हो रहा था। सुधा थकी सी उठी। सुमेधा सो रही थी। सुधा ने उसके माथे पर हाथ रखा–जैसे संबल खोज रही हो। सुमेधा जाग गई। उसने चारों ओर देखा। तभी उसे अपना प्रश्न याद आ गया। उसने माँ से पूछा, ‘मम्मी पोस्टमार्टम क्या होता है?’