मैं बृहन्नला
- 1 August, 2024
शेयर करे close
शेयर करे close
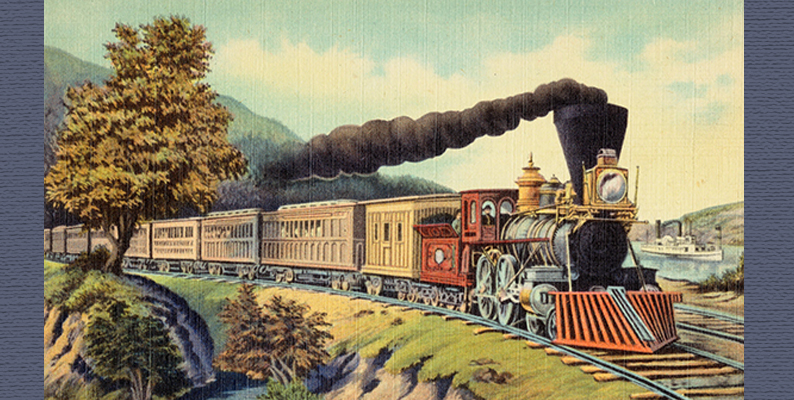
शेयर करे close
- 1 August, 2024
मैं बृहन्नला
उमाशंकर का परिवार चल पड़ा था उस ओर, जहाँ गंगा का उद्दाम वेग नहीं, चित्रोत्पला शांत और मंथर प्रवाह था। गंगा पर्वतराज हिमालय की पुत्री थीं। राजकुमारी का ओरा उनके साथ था। सो अलकनंदा और यमुना जैसी नदियों का सहज समर्पण मिला उन्हें। उन्हीं के सहारे ही तो गंगा, गंगासागर कहलायीं; मगर चित्रोत्पला? राजकुमारी नहीं एक कृषक बाला थी। उसका जन्म किसी पहाड़ की ऊँची चोटी से नहीं किसान के खेत हुआ था। सो वहाँ कोई ढलुआ राह थी ही नहीं जो उसे गति देकर उसकी राह आसान कर देती। उसकी राह में तो थे असंख्यक पथरीले टीले जिन्हें तोड़कर आगे बढ़ना उसे, तो उद्दाम वेग से बहने का न अवसर था और न ही आदत। सो जिन नदियों का साथ उसे मिला उसमें किसी ओरा का नहीं, उसके श्रम का हाथ था। सो विवश होकर नहीं वे सब ख़ुशी-ख़ुशी उसके साथ हो गईं और उसे नदी से महानदी बना दिया था। महानदी की प्रतिछाया पूरे अंचल में व्याप्त थी। सो यह दुनिया उमाशंकर की उस दुनिया से एकदम ही अलग दुनिया थी; मगर थी बहुत सुंदर।
उमाशंकर को भा गई थी यह दुनिया। गलाकाट प्रतिस्पर्धा से दूर अपनी चित्रोत्पला की तरह ही एकदम मंथर और शांत; मगर एकदम निर्मल। स्कूल का वातावरण तो एकदम गुरुकुल जैसा। यहाँ शिष्य जी मास्टर जी के सिवा और कोई शब्द उचारना जानते ही न थे। तनख्वाह तो बस ठीक-ठाक ही थी; मगर मान सम्मान बहुत था। छोटा सा गाँवनुमा कस्बा था। सो आराम से गुजारा होने लगा। विद्यार्थी ही नहीं गाँव-गिराव के सारे लोग उन्हें सम्मान से मास्टर जी कहते और सुलोचना को मास्टरिन। अम्मा जी तो फिर गुरु माँ थीं सो उनका तो और ज्यादा मान पान होने लगा। वे पूजा पाठ करती थीं। बच्चे सुबह-सबेरे फूल लेकर हाजिर हो जाते। मंदिर जातीं तो गाँव की स्त्रियाँ अपने संग ले जातीं। खेत का नया अनाज, बाड़ी की पहली सब्जी मास्टर जी के लिए ही होती। सो उमाशंकर और सुलोचना गंगा की उद्दामता हो भूल महानदी के मंथर प्रवाह संग बहने लगे। अम्मा जी भी खुश ही थीं; मगर अपने गाँव को याद कर एक उसाँस सी छूट जाती। फिर दीपालिका का जन्म हुआ और नातिन की अठखेलियों ने उन उसाँसों को अपनी किलकारियों में समेट लिया।
नातिन के संग उनका भी बचपन लौट आया था। सो वे उसके साथ कई खेल खेलतीं। अटकन-बटकन खेलते समय वह गीत गातीं, जो अपने बचपन में गाया करती थीं–
‘अटकन-बटकन दही चटकन
लहुरा देवरा बन के काँटा
बन झूले बनवरिया झूले
सावन मास करोंदा फूले
वही फूले के आरी-पारी
चिंऊँटी चिंऊँटा की रहवारी।’
फिर कहतीं–‘चिंऊँटी लेहव की चिंऊँटा।’
‘तींऊती।’ नन्हीं दीपिका कहती और वे धीरे से उसकी गदेली पर चुटकी काटतीं फिर दोनों एक दूसरे का कान पकड़कर–‘काना माना मकरी कय जाला’ गातीं। फिर जब वे उसे गुदगुदी करतीं तो दीपालिका हँसी से लोट-पोट हो जाती और वे उसे अपने सीने लिपटा लेतीं।
उमाशंकर का बचपन तो कब बीत गया उन्हें पता ही नहीं चला था। संयुक्त परिवार व्यस्तता और फिर जिंदगी की जद्दोजहद में उसका बचपना देखने और महसूसने का वक्त ही नहीं मिला। सो अब वे दीपालिका के बचपन को जी भरकर जी रही थीं। सो दादी-नातिन के धमा-चौकड़ी वाले खेल दिनभर चलते और रात को दीपालिका चूँकि पोरा की टोकरी उठा लाती और दादी के पलंग पर छोटा सा चूल्हा जल उठता। झूठ-मूठ का खाना बनाती। खुद खाती और दादी को खिलाती। खिलाती तो वह सुलोचना को भी थी; मगर सुलोचना कभी अपनी रसोई में इतनी व्यस्त होती तो कभी दूसरे कामों में। सो उसका मन रखने के लिए कुछ देर खाना खाने का अभिनय करती। फिर–‘जाओ दादी को खिलाओ।’ कहकर उनके पास भेज देती और अपने काम में जुट जाती। अक्सर यही होता है। लोग अपने बच्चों का बचपन महसूस ही नहीं पाते, तभी तो बुढ़ापे में नाती-नातिन पर अपना सारा संचित प्यार लुटाने को आतुर रहते हैं। सो वे भी अपनी संचित निधि लुटा रही थीं। दीपालिका बहुत प्यारी और सुंदर थी। जितना जगर-मगर उसका रूप-रंग था, उतनी ही जहीन भी थी, पर अम्मा जी की नजर में लड़की तो पराये घर की शोभा थी। सो उनकी दिली तमन्ना थी कि एक कुल का एक दीपक भी हो। उनकी यह तमन्ना पूरी भी हुई; मगर?
सरोजनी ने एक सुंदर से बालक को जन्म दिया। घर उछाह से भर उठा था। अम्मा जी की ख़ुशी छलक-छलक-छलक पड़ती। सो बहू के लिए हरीरा बनाते हुए उनके ओठों पर सोहर उमग आता–
‘जनम लिए रघुरइया, अवध म बाजे बधइया
महलन मंगल चौक पूर गए
जगर-मगर सब ठंइया अवध म…
राजा दशरथ कय बात न पूछो
मोहरे रहे लुटइया अवध म…।’
फिर ननद और भाभी के नोक-झोंक वाला यह सोहर गाने लगतीं जिसमें भाभी ननद को नेग देने में आना-कानी करती है–
‘लाल की बधाई जड़ाऊ बेंदा लेबय
लाल की बधाई…
संझा भई बेहाल अधरतिया जनमे ललनवा
सोर न मचाओ राजा ननदी सुन लेइहँय
बेंदा बेसर माँग लेगी लाल की बधाई…।’
फिर कुछ देर में और दूसरा गाने लगतीं–बहुत खुश थीं वे और उमाशंकर भी। उमाशंकर की हैसियत मोहरे लुटा देने की तो थी नहीं; मगर फिर भी अपनी हैसियत से बढ़कर किया था। अपनी कोई सगी बहन तो थी नहीं; मगर गाँव की सहोदरा को बहन का ही मान-पान दिया और हिजड़ों की टोली को तो उनका मुँह माँगा नेग दिया। तभी तो अपनी आशीषें बरसाते हुए विदा हुए थे वे। नामकरण हुआ और दादी ने पोते का नाम रखा दीपक; मगर उस दीपक से घर रौशन नहीं हुआ। वह दीपक तो था; मगर…? पहले पहल तो सब ठीक ही था। फिर जैसे-जैसे उसकी उम्र बढ़ने लगी उसमें कुछ और ही लक्षण उजागर होने लगे। फिर? फिर एक दिन…!
‘अरे अम्मा जल्दी करो न। चार बज गए। साढ़े आठ बजे की गाड़ी है और आप अभी तक।’
उमाशंकर की आव़ाज ने उन्हें वर्तमान में खींच तो लिया; मगर मन? मन का एक खूँट वहीं उलझा रह गया। मन में एक हूल सा उठा; मगर फिर मन को सहेजा और–‘बस अबहीं दुई मिंट में तैयार हुए जाते हैं।’ कहते हुए भरसक कोशिश की कि मन का दर्द उजागर न हो; मगर यह दर्द तो परिवार का साझा दर्द था। सरोजनी तो इतने बरस बाद उबर नहीं पाई थीं इससे और उमाशंकर? वे पुरुष थे। सो उनका दु:ख आँसू बनकर बह भी नहीं पाया और हृदय पथराता चला गया। इतना कि अब कोई ख़ुशी उनके ओठों पर मुस्कान नहीं ला पाती। यह ऐसा वज्रपात था जिसका कोई काट ही नहीं था। उन्होंने कहाँ सोचा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा कि…। उनकी फैमिली तो एक कंपलीट फैमिली बन चुकी थी। सो उन्होंने फैमिली प्लानिंग अपनाते हुए हम दो, हमारे दो की नीति अपनायी थी। अम्मा जी ने समझाया भी था–‘एक आँख को आँख और एक पूत को पूत नाहीं मानते। तव हमरी मानों त अबहीं अपरेसन सपरेसन रहिने दो।’
‘का अम्मा तुम भी न? तुमहीं तो कहती थीं न एक से सहास (सहस्त्र ) होते हैं। देखना हमारा ये बिटवा सहस्त्रों पर भारी पड़ेगा। इतना नाम करेगा कि अब तक किसी ने नहीं किया होगा।’ सरोजनी का ऑपरेशन करवा लिया।
7
खचाखच भरी सारनाथ में अपनी सीट तक पहुँचना एवरेस्ट फतह करने से कम न था। प्लेटफार्म पर ही मेला सी भीड़। सब लोग आगे बढ़ गए थे। अम्मा जी बहुत पीछे छूट गई थीं। तभी हिजड़ों की एक टोली ने अम्मा जी को आ घेरा।
‘आय हाय कुंभ अम्मा जी! कुछ हमारा हक हिस्सा भी दे दो। अब ये न कहना कि हमारे अँगने में तुम्हारा क्या काम है? हमारा अँगना तो आपलोगों ने छीन…’
उन लोगों से घिरी अम्मा जी अकबका सी गईं। जल्दी से अपना बटुआ टटोला। कुछ रेजगारी निकाली और एक सिक्का उसकी ओर बढ़ाया।
‘ये क्या माँ जी? हम भिखारी हैं क्या? हम भीख नहीं अपना हक माँगती हैं। हमारे घर आँगन छीनने की कीमत एक सिक्का? बहुते न-इनसाफी है।’
‘न-इनसाफी है। न-इनसाफी है।’ कहती उनकी टोली ने उनके इर्द-गिर्द घेरा बना लिया और ताली बजा बजाकर नाचने लगी। अम्मा जी की अकबकाहट और बढ़ गई। उन्हें डर लगा कि ये लोग कहीं…। सो उन्होंने हड़बड़ा कर अपने बटुआ में डाला और जो भी हाथ में आया उन्हें पकड़ाया और वहाँ से छूट भागीं। जैसे-तैसे उमाशंकर तक पहुँचीं, तो वे भीतर प्रवेश की जद्दोजहद में थे। फिर गाड़ी का सिग्नल भी हो गया; मगर वे द्वार तक भी नहीं पहुँचे थे। तभी–‘मास्टर जी प्रणाम।’
उन्होंने देखा काली कोट वाला एक युवक उनके कदमों में झुक आया था। वे उसे पहचान नहीं पाए थे। कोट पर लगी नामपट्टी आर.एन. जंघेल से भी कुछ याद नहीं आया। सो चेहरे पर अनचीन्हेंपन का भाव उभरा।
‘लगता है आपने पहचाना नहीं मुझे। मैं राजू, राजेन्द्र नाथ जंघेल।’
‘ओहो तो तुम हो! कितने बड़े हो गए हो।’ उन्हें याद हो आया शरारती राजू। शरारतें भी ऐसीं कि कभी मरा हुआ साँप धागे में बाँध लाता, तो कभी जिंदा मेंढक बाँधकर पूरी कक्षा को डराता। सो रोज ही कक्षा से बाहर करना पड़ता उसे। फिर उन्हें याद हो आई वह घटना जब उसने एक कुत्ते की पूँछ में फटाके लड़ी बाँध आग लगा दी थी। कूँ-कूँ करता कुत्ता इस कक्षा से उस कक्षा में दौड़ लगाता रहा। हंगामा सा मच गया था। सारे बच्चे कक्षा से भागने लगे थे। एक बच्चे की तो टाँग ही टूट गई थी। मारे डर के सीढ़ियों की रेलिंग से कूद गया था वह। अब तक तो उसे छोटी-मोटी सजाएँ मिल ही मिला करती थीं; मगर उस दिन उसके लिए निष्कासन जैसी एक बड़ी सजा मुकर्र की गई थी। सभी शिक्षक उस सजा के लिए एकमत थे। उसके पिता को बुलवाया था। उनका अनुनय-विनय भी काम नहीं आया था। प्रिंसिपल साहब उसके निष्कासन पर ही अड़े हुए थे; मगर उन्हें लग रहा था कि इस तरह तो उसका साल बरबाद हो जाएगा और किसी बच्चे का साल बरबाद कर देना शिक्षक को शोभा नहीं देता। सो उन्होंने उस सजा का विरोध किया और अपनी जिम्मेदारी पर उसकी सजा रुकवायी थी। उन्हें यकीन हो रहा था वही राजू आज टी.सी. उनके सामने खड़ा है।
‘सर लाइए अपनी अटैची मुझे दीजिए।’ उसने उनके हाथ से अटैची ले ली। टी.सी. को भीतर आता देख भीड़ तिरिया गई और उन्हें अपनी सीट तक पहुँचने की राह मिली। टी.सी. को आया देख उनकी सीट पर काबिज लोगों ने भी बिना हील हुज्जत के उनकी सीटें खाली कर दीं, वरना इस ट्रेन में अपनी ही सीटों के लिए भी मारा-मारी करनी पड़ती थी।
‘मास्टर जी! आपलोग अपनी सीट पर आराम से बैठिए। मैं कटनी तक साथ हूँ। बीच-बीच में आता रहूँगा। प्रणाम’ राजू ने फिर उनके पैर छुए और आगे बढ़ गया।
गाड़ी चली; मगर चलते ही घोंऽऽ घोंऽऽ के लंबे सायरन के साथ रुक गई। किसी ने चेन खींच ली थी। गाड़ी दस-पंद्रह मिनट खड़ी रही। फिर चली और चलते ही फिर रुक गई। फिर वही घोंऽऽ घोंऽऽ वाला लंबा सायरन बज उठा। ‘एक समय था जब गंभीर कारण के बिना चेन खींचना अपराध माना जाता था। सो चेन खिंचने पर पड़ताल की जाती थी और अपराधी को सजा मिलती थी; मगर अब…? अब कोई पड़ताल नहीं होती। सो कारण-अकारण चेन खींच ली जाती है।’ सोचते हुए उमाशंकर ने उन्हें देखा, जो चेन खिंचने के बाद गाड़ी रुकते ही शान से डिब्बे में चढ़ आए थे। उनके मन में कोई अपराध नहीं था।
अपने समय से एक घंटे के विलंब से गाड़ी चली तो; मगर रायपुर से बिलासपुर पहुँचने में ही चार घंटे लग गए। कारण वही हर स्टेशन पर चेन खिंचाई। बिलासपुर में तो सीटों के लिए कुछ लोगों में हाथापाई तक हो गई। दोनों पक्ष एक दूसरे को पुलिस कंप्लेन की थोथी धमकी देते रहे। दोनों को मालूम था पुलिस कुछ नहीं करेगी। उमाशंकर उनकी मदद करना तो चाहते थे; मगर वे तीन की सीट पाँच लोग पहले ही थे। अपनी सीट पर काबिज बूढ़े बाबा को उठाना उन्हें उचित नहीं लगा था। सो अब वे विवश थे।
‘देख भई लड़ने-झगड़ने से कुछ नइ होगा। आखिर जायबर तो सबको है न। परब का समय है, तो मिल बाँट के सफर कर लो। रातभर के तो बात है कोन सा मार इहाँ डेरा डालना हे। ये छोटे बच्चा ल मोर सीट म बैठा दे। आ बाबू तैं मोर पास बैइठ।’ और उसने जगह बनाकर बच्चे को बिठा लिया।
उस देहाती से दिखने वाले आदमी की बात का असर हुआ और जो आदमी सीट पर बेजा कब्ज़ा जमाए हुए था। उसने अपना कब्ज़ा छोड़ दिया और उसके साथ उसकी बूढ़ी माँ भी उठने लगीं तो–‘नहीं माँ जी! आप मत उठिए। मैं मैनेज कर लूँगा।’
सो उनके लड़ाई-झगड़े का अंत इस सुंदर समझौता से हुआ। अब बीच वाला गलियारा सामानों और लोगों से अट गया। बहुत से लोग जिनका रिजर्वेशन नहीं हो पाया था वे गलियारे में अपनी अटैचियों पर बैठ गए। गाड़ी चली तो उसकी हिलडुल ने सबको अपने भीतर समो लिया। जब गहराने लगी, तो नींद के नशे में लोगों के सिर एक दूसरे के काँधे पर जा टिके। अब स्त्री-पुरुष, अमीर-गरीब जैसे भेद वहाँ नहीं थे। नींद ने सबको एक धरातल पर ला दिया था। अम्मा जी को बाथरूम जाने की जरूरत हो आई; मगर जाएँ कैसे? भीड़ इतनी कि तिल भर भी जगह न थी। ऐसे में ‘किसी पर पैर न पड़ जाय।’ सोचकर वे देर तक अपनी सीट पर ही बैठी रहीं; मगर भीतरी दबाव ने उन्हें बेचैन कर रखा था। सो वे उसुक-पुसुक कर रही थीं। कुछ देर बाद जब उस दबाव को सहना मुश्किल हो गया, तो वे उठीं मगर अपनी बर्थ के नीचे लेटी औरत के पैर से टकरा कर उमाशंकर की बर्थ पर जा गिरीं। ‘अरे अम्मा! क्या हुआ?’
‘कुछ नाहीं तनी बाथरूम तक जात रहीं।’
‘हमको काहे नहीं जगाया? अभी चोट लग जाती तो? चलो हम चलते हैं।’
उमाशंकर ने उनका हाथ पकड़ा और जगह टटोलते हुए बाथरूम की ओर बढ़े; मगर वहाँ तक पहुँचना आसान कहाँ था। डिब्बे में ‘भूख न जाने जूठा भात, नींद न जाने टूटी खाट।’ वाली कहावत चरितार्थ हो रही थी। जिसे जहाँ जितनी जगह मिली, वह उसी में लुढ़का हुआ था। सो लोगों के चादर और कपड़ों से अरझते-अरझाते किसी तरह से बाथरूम तक पहुँचे।
8
कुंभ मेले के लिए लोग उमड़े पड़ रहे थे। गाड़ी हर जगह अपने समय से ज्यादा रुकती। सो दोपहर को पहुँचने वाली सारनाथ रात को नैनी पहुँची। कुंभ स्नान का पुण्य दिलाने वाले कुछ पंडे तो कई स्टेशन पहले से डिब्बों में दाखिल हो चुके थे। नैनी में तो एक रेला ही आ गया। लोगों को उनकी सात पीढ़ियों का लेखा-जोखा बताते जिधर देखो उधर वे ही वे नजर आने लगे। एक ने उमाशंकर को भी घेरा–‘जजमान! आपन कहँवा से आइल बा।’
‘कहीं नहीं हमारा कोई पुरखैती रिकार्ड नहीं है।’ उमाशंकर ने टालना चाहा।
‘अइसन भला हो सकत है का, के हम पंडन के पास केहू का पुस्तैनी रिकार्ड न होय? आप अपने पुरखन म कोई का नाम तो बताइए।’
‘रहने दीजिए महराज हमें अपने पुरखन की कुंडली देखने में कोई रुचि नहीं है। गंगा में डुबकी ही तो लगानी है न। हम खुद ही लगा लेंगे।’
उमाशंकर तो उसके आल-जाल से बचकर आगे बढ़ गए। सुलोचना भी उनके पीछे हो लीं; मगर अम्मा जी? धरम-करम को मानने वाली थीं। सो वे ठिठक गईं। उन्हें ठिठका देख उसने उन पर अपना घेरा डाला–‘अब आपहिं बताओ? भला अइसे भी कुंभ अस्नान होत है का, के गए और डुबकी मार के निकल गए? अरे कुछ धरम-करम भी तो है न। अब आपहिं बताओ पुरखन को पिंड दिए बिन आपका कुंभ असनान सुफल होई का?’
‘इ बात तो सही कह रहा है। फेर उमा? ऊ तो एकदमे अड़ियल है। फेर नाहीं वोह्का समझावे का तो परबे करी।’ सोचा और–‘महराज हिंया नाहीं। आप डेरे पे आएँ। हिंदी भुवन तव जानतय होंगे?’
‘अरे माता जी! हिंदी भवन यहाँ कौन नहीं जानता भला। होत बिहान हम हाजिर होय जाएँगे।’
आश्वस्त होकर पंडा दूसरे ग्राहक की तलाश में बढ़ गया और अम्मा जी। गुंताड़े में लग गईं कि किस तरह उमा को मनाएँ कि वह…? ‘ई सब मा उमा का कउनव बिसवास नाहीं है। फेर अइसे…? ठीकय तो कह रहा है ऊ पंडा। पुखरन का सुमिरे बिना, निखालिस बुड़की मार लेय से तो हमरे इ कुंभ असनान का कउनव फ़ाइदा नाहीं। तव…?’ सोचती वे पीछे रह गई थीं। सो लपकर आगे बढ़ चलीं। उनके मन में पंडा की कही बातें रातभर मन में डोलती रहीं।
सपने में अपनी सास को देखा। वे कह रही थीं–‘दुलहिन तुम पुरखन का छोड़ के, अइसे कइसे कुंभ कर लोगी। पुरखन कय नाव से पिंड (पिंडदान) तव देय क परी न।’
उन्होंने देखा सास के पीछे वे भी खड़े थे। उनकी याचित नजरों में सवाल लहरा रहे थे। उन्हें असमंजस में देख–‘रहय देव अम्मा। आपन पंचन कय किस्मत म मोछ (मोक्ष) नाहीं लिखा है।’ पति ने कहा और अपनी अम्मा का हाथ पकड़ जाने लगे।
‘नाहीं-नाहीं! अइसे न जाव। तनि रुक जाव। हम उमा से…।’ कहते हुए वे उनके पीछे दौड़ीं और आँख खुल गई। उठकर देखा बाहर उजास की एक महीन सी झाँई उभर आई थी। ‘ओह! भोर होय रही है। कहत हैं कि तड़के (भोर) का देखा सपना फुर (सच्चा) होत है। सही म पुरखन के बिना तो परागराज (प्रयागराज) असनान भी नाहीं फलत है। फिर यह कुंभ आय। तो पुरखन के बिना कइसे पुन्न। फेर जिनके संग साथ सात जनमिया (साथ जन्म) गाँठ जुरी है उनका छोड़ के…? दइव उनका उठाय न लेते, तो यह असनान तो उन्हीं के संग होता। न अइसे तो नाहीं चलेगा। उमा से बात तो करय का परी।’ सोचा और उठकर बाहर आईं। देखा उमाशंकर अभी उठे नहीं थे। सो अपनी बेचैनी में वे बाहर ही टहलने लगीं। तभी देखा सामने से पंडा महराज चले आ रहे हैं। ‘नाहीं! इसको सबेरे-सबेरे इहाँ देख के तो उमा का दिमागय चढ़ जाएगा।’ सोचा और–‘पंडा जी महाराज! अबहीं तव कोई उठा नाहीं है। अइसा करें आप कुछ देरी से आ जायँ। तब तक हम बचवा को मनाने की कोसिस करेंगे।’
‘अम्मा जी! जेतना अबेर होगा न, वोतना भीड़ बढ़ जाएगी। येही से हम जल्दी आए रहे। फेर कोई बात नहीं। हम कुछ देरी से आ जाएँगे।’
पंडा महराज चले गए; मगर वे वहीं टहलती रहीं कि उमाशंकर उठें तो उनसे बात करें। बहुत देर बाद उनके कमरे का दरवाजा खुला–‘अरे अम्मा आप। अतना जल्दी उठ गईं। रात नींद नहीं आई का?’
‘नींद? कुछ आई, कुछ नाहीं आई। बचवा सपना म तुम्हरी आजी (दादी) आई रहीं। हमका लागत है उनकी आत्मा…?’
‘अम्मा! आजी की आत्मा की बात भूल जाव। अपनी बात कहव। पिंडापारने (पिंडदान) का मन है न? पिंडा परवा लिया जाएगा।’
एक चकित सी ख़ुशी लिए वे बेटे को देख रही थीं। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कर्मकांडों के घोर विरोधी उनके बेटे ने पिंडदान की सहमति दे दी है। सो मारे ख़ुशी के उनकी आँखें अँसुआ आईं।
‘ये क्या अम्मा…? ये रोने का समय थोड़े है। चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ। घाट पर पंडा भी तो ढूँढ़ना होगा।’
‘हम हाजिर हैं जजमान।’
उमाशंकर ने देखा स्टेशन वाला पंडा सामने था। ‘लोग सच ही कहते हैं कि पंडा से प्राण छुड़ाना आसान नहीं।’ सोचा और–‘तो आपने हमें ढूँढ़ ही लिया।’
‘इलाहाबाद में किसी को ढूँढ़ना कौन मुश्किल है। फिर आपको प्रयाग हिंदी संस्थान कहते सुन लिए थे तो…।’
उसने रजिस्टर खोलकर उनके पुश्तैनी गाँव और उनके पुरखों का सारा लेखा बाँच दिया। काम के प्रति उसकी लगन और समर्पण उमाशंकर को प्रभावित किया और वे उसके साथ सपरिवार घाट की ओर चल पड़े।
9
पूस के मेले में भी घाट तक पहुँचना आसान नही होता। फिर यह तो कुंभ का मेला था। सो घाट पर पहुँचना आसान नहीं था। हदे निगाह तक मानव सैलाब ठाठे मार रहा था। ऐसे में पंडा अपने हाथों से चप्पू का काम लेता, उनके लिए राह बनाता आगे आगे चल रहा था। सो भारी मशक्कत के बाद वे घाट पर उस जगह पहुँचे, जहाँ पंडे का ठीहा था। अम्मा जी ने देखा, वहाँ और भी पंडे थे। वे लोगों से पिंडदान करवा रहे थे। अचानक उन्हें याद हो आया कि उनके पास पिंडा पारने का सामान तो है ही नहीं।
‘पंडा जी महराज! हमरे पास पिंड पारे का समान…?’
‘आप फिकिर न करें। हम हैं न। हम सब सरंजाम जुटा लेंगे।’
फिर उसने मिनटों में सब सामग्री जुटा दी और पूरे विधि-विधान से पुरखों का पिंडदान करवाया। उमाशंकर का इस तरह के कर्मकांड और दान पुण्य में कोई विश्वास नहीं था; मगर आज वे ख़ामोशी से सब कुछ किए जा रहे थे। कारण यह मामला उनकी अम्मा जी की भवनाओं से जुड़ा था। वे भूले नहीं थे कि अम्मा जी ने उनके लिए लोगों के घर कुटनी-पिसनी तक की थी। सो अम्मा जी की ख़ुशी के लिए वे कुछ भी कर सकते थे।
गंगा स्नान हो चुका था। अब मेला घूमने की बारी थी। यूँ तो मेले-ठेले में भी उनकी रुचि कोई न थी; मगर अम्मा जी के जीवन आस की ही था यह कुंभ। उनकी चिरसंचित अभिलाषा। सो वे इस मेले से जुड़ी उनकी हर साध पूरी कर कर देना चाहते थे। गंगा के रेतीले विस्तार पर तमाम तंबू लगे हुए थे। इतने तंबू कि तंबुओं का एक नगर सा बस गया था। कुछ तंबू गंगा तट के एकदम नजदीक थे। ये वी.आई.पी. तंबू थे। इनमें मंत्री, राजे-रजवाड़े और बड़े अधिकारियों के तंबू थे। उनके पीछे छोटे अधिकारी और व्यवसायों के तंबू और साधारण लोग? उनका ऐसा नसीब कहाँ कि…। यानी पुण्य की लूट में भी पैसा और प्रोटोकॉल ही बोल रहा था। सो वे सब गंगा के किनारे-किनारे चलते हुए मेले की ओर बढ़ ही रहे थे कि सामने से–‘हटो-हटो। सब किनारे खड़े रानी साहब की पालकी आ रही है।’
कारिंदे लोगों को तिरिया रहे थे। सरोजनी को सामने से एक पालकी आती दिखी। फिर हवा के झोंके से पालकी का ओहार (परदा) उड़ा और पालकी ठिठक गई–‘आपको रानी साहेब बुला रही हैं।’ कारिंदा सरोजनी से मुखातिब था।
‘रानी साहिबा? मगर हमारा तो उनसे…।’
‘तुम हमें भले ही भूल गई हो; मगर हम तुम्हें देखते ही चीन्ह लिए।’
वे पालकी से उतर कर सरोजनी के सामने आ खड़ी हुईं। सरोजनी ने पहचानने की कोशिश की; मगर बहुत याद करने पर भी याद नहीं आया कि किसी राजकुमारी से कभी कोई मुलाकात भी हुई हो। सो चेहरे पर अभी भी अनचीन्हेंपन का भाव ही था।
‘अरे हम राजदेई (राजदेवी)। तुम्हारे मामा के गाँव रहते थे हम। और हम दूनों सखी भी तो बदे थे न?’
‘सखी? तो ये देई है। राजदेई!’ सरोजनी ने उस भरी पूरी स्त्री को देखा। जो आज रानी साहेब कही जा रही थी; मगर रानी साहेब का राजदेई से कहीं कोई मेल ही न था। सरोजनी ने भरपूर नजरों से उसे देखा–लंबा कद, भरी हुई सुचिक्कन देह। सजे-सँवरे केश और राजघराने की स्त्रियों की तरह माथे से कुछ ऊपर उठा हुआ रेशमी आँचल। फिर सरोजनी की आँखों में वह दुबली-पतली और साँवली सी लड़की उभर आई। जो…
10
अपना ममियाउर (मामा का घर) तो सबको पसंद होता है; पर सरोजनी को तो बहुत ही पसंद था। कारण? कारण सरयू की मदिर धार; जिसमें उसके जैसे नौसिखिया पैंरना (तैरना) सीखा करते थे। सरयू में बहुत दूर तक पौंछल-पौंछल (पैरों तक) पानी ही था। सरोजनी तो एकदमें नौसिखिया थी। सो उस पौंछल पानी में ही तैरती। गहरे पानी में जाने से डरती थी वह। तैरने में प्रवीण बच्चे उसे उकसाते भी; चिढ़ाते कि उसे तो तैरना ही नहीं आता; मगर वह उनके उकसावे में नहीं आती, पर उस दिन? उस दिन–‘सबय मछरिया जल भीतर, पैंर (तैर) पार हो जाती है। सड़ी मछरिया तीरे-तीरे, रेती में लोट लगाती है।’
मौसेरे भाई देवीदीन ने तुकबंदी की और सब बच्चे एक सुर में चिढ़ाने–‘हेऽऽऽ ऊ देखव सड़ी मछरिया रेती में लोट रही है।’
‘नहीं हम सड़ी मछरी नहीं हैं।’
‘तो फिर हुआँ तक पैंर (तैर) कर दिखाओ?’
‘हाँ-हाँ इ लेव।’
वह गहरे पानी में चली गई और देर तक तैरती रही। बच्चों ने तो सोच रखा था कि वह डर कर गहरे पानी में नहीं ही जाएगी और वे उसे जी भर चिढ़ाएँगे। सो उन्हें, खासकर देवीदीन को उसका यूँ बेधड़क तैर लेना अच्छा नहीं लगा। सो उसने दूसरा चैलेंज दिया।
‘हुँह! ऐसे पौंछल पानी से मजे-मजे में गहरे जाके पैंरना भी कोई पैंरना है। अरे उस पार जाके ऊ कगार से कूद पैंरों तो जाने।’
गहरे पानी में तैर लेने से एक आत्मविश्वास से भरी उठी थी वह। सो उस चैलेंज को स्वीकारते हुए कहा–‘हाँ-हाँ हुआँ से भी कूद लेंगे।’
वह तैरते हुए उस पार गई। उस पार का किनारा बहुत ऊँचा था; मगर वह उस पर चढ़ गई। नीचे देखा। गहराई बहुत थी। पल भर को डर भी लगा; मगर तभी कानों में–‘सबय मछरिया…गूँज उठा और उसने छलाँग लगा दी। छलाँग तो लगा दी; मगर सम्हल नहीं पाई और…।
‘देखव-देखव ऊ तो बुड़ी जा रही है। अरे बचाव कोई।’ एक लड़का चिल्लाया।
सब बच्चे तैरना तो जानते थे; मगर डूबते को बचाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। सो किनारे खड़े चिल्ला रहे थे, तभी एक लड़की आगे आई और उन सबको तिरियाकर पानी गहरे में उतर गई। वह देर तक डुबकी लगाती रही; मगर कुछ हाथ नहीं आया। सब निराश हो चले थे; मगर उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। एक गहरी डुबकी मारी और उसके हाथ में सरोजनी का पैर आ गया। फिर तो वह पैर के सहारे उसकी कमर तक जा पहुँची और कुछ देर में किनारे की ओर लौट चली। सरोजनी बहुत पानी पी गई थी। सो एकदम निश्चेष्ट थी।
‘अरे! ई तो मर गई।’
एक लड़के ने कहा। सुनते ही देवीदीन को लगा कि अब तो उसकी खैर नहीं और वह भाग खड़ा हुआ।
‘अरे! नहीं। मरी नहीं है। तनिक निचेत हो गई है।’ उसने कहा और उसे उल्टा लिटाया। फिर पीठ पर दबाव बनाया, तो मुँह से भक-भक पानी निकलने लगा और कुछ देर में वह कुनमुना उठी। बच्चों के चेहरे खिल उठे।
‘अरे! तू तो बड़ी जोधा (योद्धा ) निकली।’
सरोजनी के ममेरे भाई ने कहा तो सब की आँखों में प्रशंसा उतर आई। अब वह उनकी नजरों में बकरी चराने वाली नहीं, एक साहसी लड़की थी और सरोजनी के लिए? उसके लिए तो उसकी प्रिय सखी थी। फिर तो वह प्रिय से प्रियतर होती चली गई थी।
अब वह जब भी अपने ममियउर आती दौड़कर उसके घर, अहिरन पुरवा जा पहुँचती। माँ और घर के लोग मना करते। अपने और उसके बीच का भेद बताते; मगर सरोजनी का बाल मन नेह की डोर से बँध चुका था। सो उसने उसके घर जाना छोड़ा नहीं। फिर तय किया कि वह गुड़िया (नाग पंचमी) पर उससे सखी बदेगी। उसने राजदेई को बताया तो उसकी ख़ुशी का तो ठिकाना ही न रहा।
सखी बदना या सखी बनाना गाँव-गिराँव की एक ऐसी प्रथा थी, जिसमें लड़कियाँ अपनी किसी प्रिय लड़की से सखी बदकर उसे और प्रिय बना लेती थी। आम तौर पर मेले-ठेले या तीज-त्यौहार पर ही सखी बदने का चलन था। सरोजनी को यह तो मालूम था कि सखी बदी जाती है; मगर कैसे बदी जाती है यह नहीं मालूम था। सो एक दिन जब माँ उसे लाड़ कर रही थीं। उसने पूछा–‘माँ! सखी कइसे बदी जाती है?’
‘मिठाई आउर पान से।’
फिर तो सरोजनी ने आने वाली गुड़िया (त्यौहार) पर उससे सखी बदने का तय कर लिया। माँ गुड़िया (नाग पंचमी) और ढूरेरी (होली) पर मायके आती ही थीं, तो गुड़िया पर सखी बदने में उसे कोई दिक्कत भी नहीं थी। बस डर था तो माँ का। सो अजोध्या मेले के लिए मिले पैसों से गट्टा (शक्कर की बनी मिठाई), बताशा और रूमाल खरीदा और उसे छुपाकर अपनी छोटी सी पेटी में रख लिया। ‘अब बचा पान। पान कइसे मिलेगा?’ सोचा फिर याद आया मामी का पनडब्बा और चेहरे पर छोटी सी मुस्कान खेल उठी। फिर तो वह निश्चिंत होकर गुड़ियन का इंतजार करने लगी। जैसे-जैसे गुड़िया नजदीक आने लगी, उसकी बेचैनी बढ़ने लगी। गुड़िया के कुछ पहले ही भाई लेवाने आने लगते हैं। सो उसकी नजरें उस कच्ची सड़क पर टिकी रहतीं, जहाँ से होकर मामा को आना था। भोर से साँझ तक राह देखती। फिर माँ से पूछती–‘माँ अबकी मामा नहीं आएँगे क्या?’
‘काहे? आएँगे काहे नहीं। अबहीं तो गुड़ियन मा पंद्रहियन (पंद्रह दिन) बाकी है।’
माँ की बात सुन आस तो बँधती; मगर बेचैनी कम न होती। सो राह निहारने का क्रम जारी रहा। जैसे-जैसे दिन नियराने लगे; बेचैनी और बढ़ने लगी। सो आम लाने के बहाने जाकर भदंइया आम के नीचे खड़ी हो जाती; मगर आम तोड़ने में मन ही न लगता। वह देखती सबके मामा, नाना आ रहे थे; मगर उसके नहीं। फिर उसे लगने लगा था कि अबकी मामा आएँगे ही नहीं। जब गुड़िया को दो दिन ही बचे, तब तो वह निराश ही हो गई थी। सखी बदने का उत्साह तेल की तलछट की तरह बैठ चला। फिर तो सरोजनी की माँ को भी लगने लगा था कि अबकी कोई नहीं आएगा। उड़ती-उड़ती खबर भी थी कि अबकी उधर बोउनी देर से हुई थी। सो खेत का काम ही पूरा नहीं हुआ है। सो निराश तो वे भी थीं; मगर सरोजनी? उसकी निराशा का तो कोई ओर-छोर ही न था। उसे लगने लगा था कि सखी बदने का उसका सपना ही रह जाएगा; सपना हकीकत में ढला। गुड़िया से एक रात पहले, मन में निराशा का अंधियारा और भी गहरा गया था। उसे ही नहीं, माँ को भी लगने लगा था कि अब तो…तभी–‘मुन्नी!’ आवाज के साथ बाहर वाले दरवाजे कुंडी खड़की।
‘कउन?’ माँ ने आवाज़ से जान तो लिया कि छोटकऊ (भाई) ही है; मगर गहराती रात का समय था। सो तस्दीक कर लेना जरूरी था।
‘अरे! हम हैं छोटकऊ।’
फिर तो माँ से पहले वही उठ दौड़ी। किल्ली खोली और–‘मामा कितना दिन लगा दिए। हमको और माँ को भी लगा कि…।’
‘सरोज!’ माँ बरजती रहीं; मगर उसने अपनी शिकायत दर्ज कर ही दी।
‘का करी बच्ची। खेत का काम खतमय नाहीं हो रहा था। बोवनी म अबेर हुई, तो सब काम म देर होता चला गया। काल बड़ी मुस्किल से सब समेट पाए। अब जल्दी से तैयारी कर लेव। बड़े भिनसारे चलय का है।’
‘का भैया अबहीं तो आए हो आउर चलय की बात। अइसे बिना मुह जुठारे। कइसे…?’
‘न मुन्नी। ई सब चक्कर म बिलकुल न पड़ना। बड़े भिनसारे निकरना है। नाहीं तो बहुत अबेर हो जाएगा।’
चलने की बात सुनते ही वह अपना सामान उठा लाई थी। फिर माँ की नजर बचाकर सखी बदने वाली थैली सबसे नीचे रख दी। चलने की तैयारी हो गई। अभी रात बाकी थी। सो–‘चलो अब कुछ देर सो जाओ। फिर तो चलना है न।’
माँ ने कहा तो लेट गई; मगर नींद कहाँ? सो उसुक-पुसुक करती करवट लेती रही और माँ के उठते ही झट से उठ बैठी।
‘अरे वाह! मुन्नी ई तो बड़ी हुसियार है। हमका तो लगा कि अतना सबेरे कैसे उठेगी, फेर ई तो हमसे पहिले उठ गई।’
‘कउनव हुसियार-उसियार नाहीं है। ननियउरे (नानी के घर) जाय क है न, एही से। नाहीं तव पहर भर चिल्लाये से भी नाहीं जागती।’
‘काहे महुआ बीने की खातिर नाहीं उठते हैं का? मामा आपके हिंया भी तो आम बीनने उठते थे न?’ मामा के सामने तौहीन न हो। सो उसने अपना पक्ष रखा।
‘हाँ ई तो एकदमें साँच बात है। कवनव बच्चा अतना जल्दी नाहीं उठता है। सबसे अच्छी है हमार भैना (भाँजी)?’ मामा की बात सुन ख़ुशी से उमग उठी और झटपट चलने को तैयार हो गई।