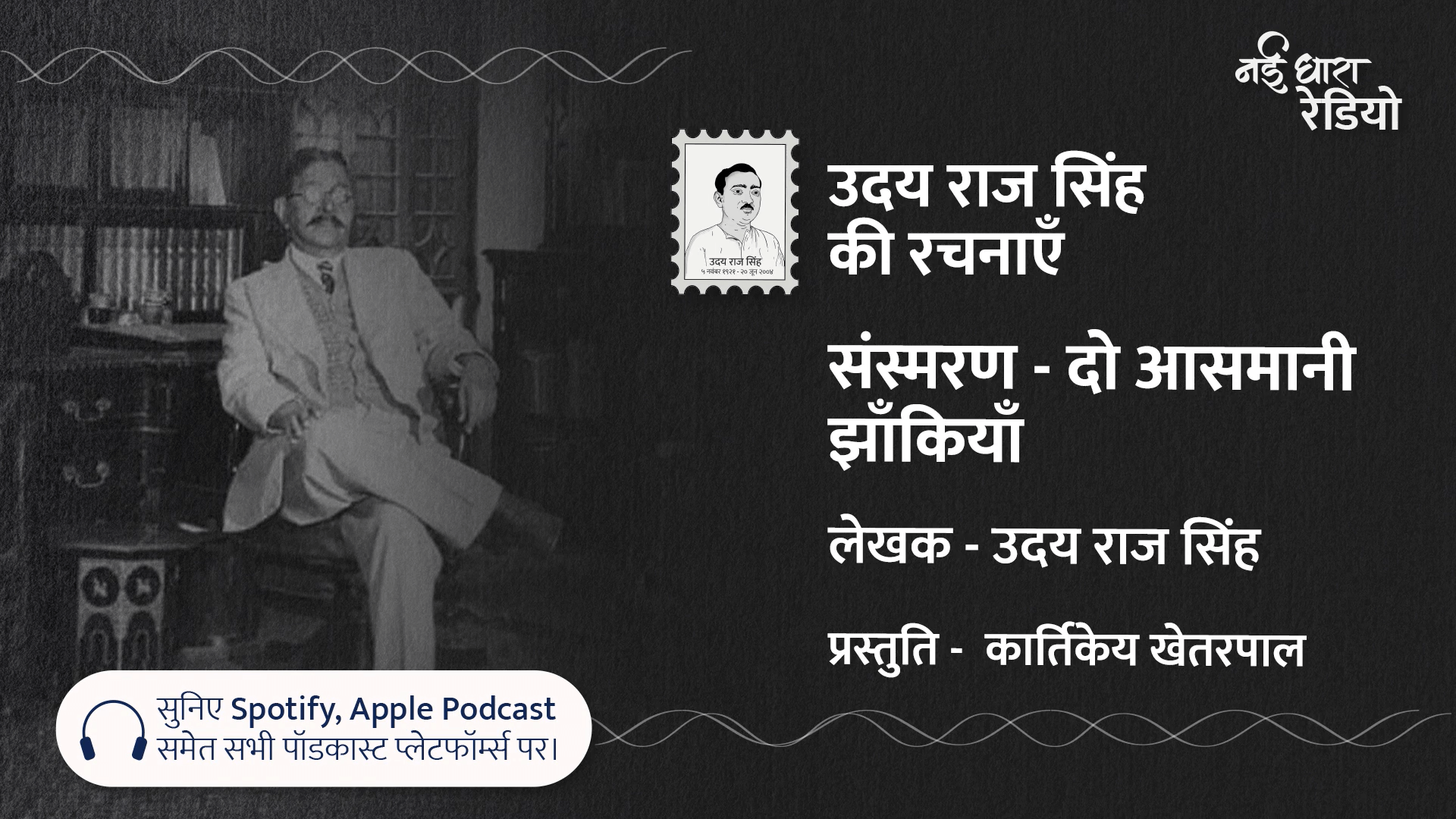तलाश
- 1 January, 1974
शेयर करे close
शेयर करे close
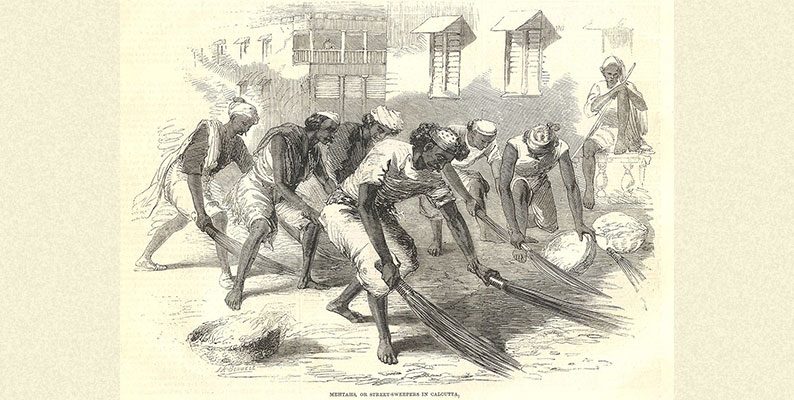
शेयर करे close
- 1 January, 1974
तलाश
हरिजन-सेवक-संघ की मंत्रीगिरी क्या आई, आँखों की नींद हराम हो गई। कोई पल चैन नहीं। हर समय कोई-न-कोई खड़ा है अपने नरद्दुदों का जंजाल लिए हुए। फूलबगान कलकत्ता के दलित-संघ के मंत्री अपनी फरियाद तथा कैमरा लिए कलकत्ता से दौड़े चले आए हैं, कहे जा रहे हैं–“गया जिले के सुदूर देहात में हरिजनों पर बड़ा जुल्म हो रहा है। खेत के मालिक उन्हें बँधे हुए बोझे उठाने नहीं देते। उनके हिस्से का भी धान छीन लिया गया। बोलने पर चोरी का इल्जाम ठोंक कर पुलिस को मिलाकर चालान करा दिया गया। मैं उसी गाँव का बाशिंदा हूँ, घर से तार पाकर आपके पास दौड़ा चला आ रहा हूँ। दिल्ली भी तार गया है, पटना भी। आप कोई ठोस कदम उठाएँ।”
मैं पूछ बैठता हूँ–“समाज-कल्याण विभाग में नहीं गए?”
“वहाँ भी ताला खटखटा आया हूँ। बस, आप ही बाकी बचे हैं…।”
मैं अपने राज्य-संगठक से पूछता हूँ–“बताइए साहब, ऐसी परिस्थिति में पुराने मंत्री जी क्या करते थे? यह तो आपकी तमाम योजनाओं के बाहर की बात है।”
“साहब, हमारा काम तो सिर्फ प्रयास ही करना है–बीच-बचाव करा देना। दफ्तर से किसी को भेजकर मुखिया और बी. डी. ओ. तक सिफारिश पहुँचा दें। आगे इनका भाग्य जाने!”
मुझे यह सुझाव जँच गया।
भंगी-मुक्ति योजना के एक सफाई-सेवक इस तरह के काम बरसों से करते आ रहे हैं। बस, उन्हें भी फूलबगान के मंत्री महोदय के साथ लगा दिया। जाते-जाते मंत्री महोदय ने मेरा और हमारे कर्मचारियों का फोटो भी ले लिया–कलकत्ते के किसी पत्र में छपवा देने के लिए। चलो, एक सरदर्द टला।
दिल्ली से आए हुए अनेकानेक सर्कुलर उठाकर पढ़ना चाहता हूँ कि चिथड़ों में लिपटा एक घिनौना काला-सा व्यक्ति फाटक खोलकर अंदर पहुँच जाता है।
“यह कौन है?”
“अकलू चमार।”
बुरी तरह खाँस रहा है–सारा शरीर डोल रहा है–अब गिरा, तब गिरा।
मैं अपने राज्य-संगठक की ओर मुखातिब होता हूँ। वह चट बोल उठते हैं–“जनाब, यह हमारा पुराना मरीज है–तपेदिक का। किसी तरह हमलोग ने जिलाकर रखा है, दवा के लिए आया है।”
मैं चौंक पड़ता हूँ–“संगठक महोदय, सफाई-सेवक को तो फूलबगान केंद्र के मंत्री अपने पैसे से बी. डी. ओ. के यहाँ ले गए। अब इसे पैसे कहाँ से दिए जाएँ? सरकारी अनुदान पर चलनेवाली संस्था भला सरकारी योजनाओं से बाहर कैसे कुछ कर सकती है? सर पर ऑडिट की तलवार जो नाच रही है!”
“साहब, कीजिएगा क्या? हमारा यह धंधा ही ऐसा है–मुझे दो बजे रात में मुसहरटोली में भूत झाड़ने जाना पड़ता है। क्या करूँ, कभी चैन नहीं! तेतरी मुसहरिन जब पगला जाती है तो उसका पति सुगना मुझे ही पकड़कर ले जाता है। कितना कहता हूँ कि उसे काँके के पागलखाना में भेजो तो वह सोये हुए में पैर टीपने लगता है–‘मालिक! तनी एह बार चलीं, फिर किचिन चढ़ल बीया। खूनखराबी होके रही!’ क्या करूँ, जाना ही पड़ता है। संघ ने मुझे भंगियों को ऋण-मुक्त करने को बहाल किया है, मगर यहाँ तो ‘आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास’ और कभी आधी रात में कोई किसी की बीवी को ले भागा तो मेरी खैर नहीं। रातभर बीच-बचाव करते रहिए। पुलिस-थाना को खबर करते-करते जान आफत में पड़ जाती है।”
अकलू फिर खाँसता है। इस बार की खाँसी बड़ी दर्दनाक रही।
मैं घबराता हूँ कि कहीं मेरी मखमली लॉन पर थूक न दे और मेरा घर भी तपेदिक के कीटाणुओं से भर जाए। मैं उसे जल्द भगाना चाहता हूँ।
“खैर, बंद कीजिए अपना किस्सा, आज अकलू का क्या होगा? पुराने मंत्री जी क्या करते थे ऐसी हालत में?”
“इधर-उधर का बजट कतर-ब्योंत कर कुछ दे दिया करते थे।”
“तो जाइए, आप भी कुछ उसे दे दीजिए–जान तो बचे!”
“पूरे अठारह रुपये की दवा चाहिए। तब शायद 15 दिन फिर चैन से रह ले। मुझे तो पिछले छह महीने से एक पैसा भी नहीं मिला। सरकारी अनुदान आया नहीं–बस, मेरा वेतन बंद हो गया। यह तो हाथ भी पसार सकता है। मैं तो वह भी नहीं कर सकता।”
मैं पसोपेश में हूँ–संगठक महोदय सब समझ रहे हैं। बोले–“अरे ओ अकलू! जाओ-जाओ, मेरे घर चलो–देखो, कोई उपाय लगेगा। उठो-उठो, भाग जाओ।”
वह बेचारा पूरी आस्था लिए वहाँ से चल देता है।
संगठक महोदय मुझे समझाने लगे–“कुछ अतिरिक्त पैसे की व्यवस्था तो करनी ही होगी। ऐसे दो-चार केस प्रतिदिन आएँगे। अकलू मुझ पर भरोसा रखता है, इसलिए उठकर चला गया, वरना हटता नहीं…।”
मैं हँसकर फिर दिल्ली के सर्कुलर पढ़ने लगता हूँ। दो-चार पन्ने मुश्किल से पढ़ पाता हूँ कि दो काली कुच-कुच सूरतें लॉन के एक कोने में दिख जाती हैं। मैं थर्रा उठता हूँ। यह तीसरी बला कौन? फटे-मैले कपड़ों में लिपटी हुई उनकी काया मेरे सामने धीरे-धीरे आकर खड़ी हो जाती है। एक मर्द और दूसरी औरत–बुढ़ापे और गरीबी के बोझ से झुकी हुई–टूटती हुई।
हमारे राज्य-संगठक महोदय हँस पड़ते हैं–“जनाब, रतनपुरा के ये मुसहर हैं। बहुत गरीब। इस साल बरसात में रही-सही झोपड़ी भी बह-बिला गई। इस घोर गरीबी में इन्हें आफत की मारी अपनी बेटी ब्याहनी है। पास में एक छदाम भी नहीं। दिनभर बाबुओं के खेतों में कमाकर पेट तो पल जाता है मगर उससे बेटी का विवाह तो पार न लगेगा। सुना, नए मंत्री जी बहाल हुए हैं–बस, ये दौड़े चले आए। फागुन के अँजोरा में शादी है।”
संगठक महोदय मेरी ओर देखकर इस बार जरा व्यंग्य की हँसी हँसने लगे।
“ये कितना चाहते हैं? कितने में इनका काम चल जाएगा?”
“सिर्फ पचास रुपये में।”
“हाँ मालिक, पचास रुपया में कपड़ा-लत्ता, बर-विदाई, खाना-पीना सब हो जाई। अतने में झुनिया के बिआह मजे में पार लग जाई। अब सरकार माई-बाप बानीं।”
दोनों आर्त हो कलपने लगे।
इधर पोर्टिको में खड़ी मोटर पर सुषमा झट सवार हो इम्तहान देने महिला कॉलेज की ओर चल पड़ी। उसके मुरझाए चेहरे पर अभी भी पुरानी कांति, चिरपरिचित दीप्ति नहीं लौट पाई है।
अभी कुछ ही महीने पहले उसकी शादी दिल्ली में एक संभ्रांत घराने में हुई। रुपयों के नोट में आग लगाकर आतिशबाजी उड़ाई गई। हजारों हजार बिजली बल्ब की रंग-बिरंगी रोशनी में मेरा सारा महल जगमगा उठा। बारातियों की खातिरदारी में मेरे तमाम दोस्त-अहवाब और रिश्तेदार एक पैर पर खड़े रहे। कहीं विलायती बोतलों के काग उड़ रहे हैं तो कहीं छुम-छनन-छुम की मदमाती आवाज से सारे वातावरण में एक अजीब मस्ती बिखर रही है। मैंने अपनी बेटी की लेन-देन, तिलक-दहेज में भी कोई कमी नहीं की। पचासों हजार के सामान बेटेवाले अपने स्पेशल में लादकर दिल्ली ले गए। पहले तो नई ले आई बहू की खूब तारीफ हुई–उसे सर-आँखों पर बिठाया गया मगर ज्यों-ज्यों समय बीतता गया, बेटे के माँ-बाप के पेट में बैठा शैतान जवान हो उठा। एक दिन दोनों ताव पर चढ़ गए। बस, बहू को ड्राइंगरूप में बैठाकर दोनों ने उसकी और उसके माँ-बाप की धज्जी-धज्जी उड़ा दी। उफ, तुम्हारी शादी क्या हुई, सिर्फ रस्म की एक तामीली हुई। हमें कुछ न मिला। हमारे रिश्तेदारों की बड़ी बेइज्जती हुई। उनके मुँह लायक उनकी विदाई न हुई। हमारे बेटे को दहेज में भी कुछ न मिला। श्वसुर को एक सूट तक नहीं मिला। सास की साड़ी महज मामूली रही। घर की अन्य औरतों की साड़ियाँ तो बस गिनाने भर को रद्दी खरीदी गई थीं। हमारी इज्जत लायक शादी न हुई। हम तो बुरी तरह ठगे गए।
सुषमा को तो काठ मार दिया। आसमान से पाताल में जा गिरी। कहाँ नई जिंदगी का सुनहला सपना और कहाँ परदे की आड़ से यह धाँधली! आधी रात के उपरांत तक सास-ससुर के ताने वह सुनती रही, सुबकती रही; और संभ्रांत घराने की संस्कृति और शिष्ट रीति-रिवाज के जो सब्जबाग उसे शादी के पहले दिखाए गए थे–वे सब बिखर गए। शायद हाथी के दाँत दिखाने के और, और खाने के और थे।
फिर तो प्रतिदिन उसे फब्तियाँ सुननी पड़तीं और खाने की मेज पर श्वसुर उसे बिठाकर खुलेआम अपनी पत्नी से पूछते–“बताओ तो कैकेयी! वह एक लाख देनेवाला कौन पार्टी था?” फिर सुषमा की ओर व्यंग्य की एक दृष्टि फेंककर हँस पड़ते। उस बेचारी को खाना निगलना मुश्किल हो जाता।
दो महीने बाद, जब कॉलेज खुलने पर सुषमा इम्तहान देने मेरे घर आई तो सारा किस्सा सुनकर सभी अवाक हो रहे। मैं तो बुरी तरह आहत हुआ। उच्च शिखर से खाई में जा गिरा। क्या सोचता था और क्या हो रहा है! प्रताड़ना सहते-सहते सुषमा सूखकर काँटा हो गई है। मैं उसे जब देखता हूँ तो अपने को दोषी समझने लगता हूँ।
“का मालिक, कुछ हुकुम ना भइल! बहुत बेर बीत गइल।”–उस मुसहर ने फिर टोका।
मैं चौंककर जाग पड़ता हूँ। पचास हजार नहीं–सिर्फ पचास रुपयों में वह झंझटों को पार कर अपनी बेटी को सुखी कर लेगा। इसके लिए इतना ही सब कुछ है। मगर वह भी मयस्सर नहीं। उधर उतना सब कुछ पाने पर भी तसल्ली नहीं।
हसरत होती है ऊँची हवेली में पलनेवालों को देखकर कि वे आज भी नहीं चेत जाते–यही विषमता एक दिन उनकी आलमगीर इमारत को जमींदोज कर देगी!
(आकाशवाणी के सौजन्य से)