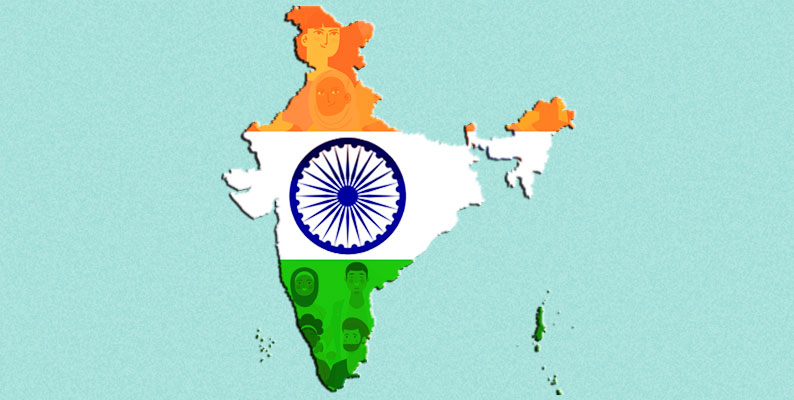चार चाँद
- 1 December, 1951
शेयर करे close
शेयर करे close

शेयर करे close
- 1 December, 1951
चार चाँद
(तिलक-कामोद : त्रिताल)
•
चाँद, तुम सब के, किसी का मैं नहीं हूँ!
भाग्य ऐसा, तुम कहीं हो, मैं कहीं हूँ!!
तुम अगम आकाश में, वातास में हो,
भूमि पर मैं, दूर-दूर, प्रवास में हूँ!
तुम मुकुट-तट में जटित, मुझ पर चरण हैं–
राज्य में तुम और मैं वनवास में हूँ!!
हास बरसाते गगन से मगन-मन हो,
कह सकोगे, यह उसाँस उदास क्यों है?
तुम उठाते हो लहर पर लहर प्रतिपल,
हंत! अंतर यह हताश, निराश क्यों है?
अमृतमय कर हैं तुम्हारे स्वेद-शीतल,
विष-बुझे शर हो रहे मेरे लिए क्यों?
चाँद, सबका जी जुड़ाते ही रहे तुम,
निज सुजस वह खो रहे मेरे लिए क्यों?
तुम उतर सकते न धरती पर कभी हो,
मैं न आ सकता कभी आकाश में हूँ!
हम न हो सकते निकटतर हैं परस्पर,
तुम अमर आवास में, मैं नाश में हूँ!!
एक ऐसी हूक उठती हत हृदय में,
कूक कर कोयल बता पाती नहीं जो!
आग खाता है विभोर चकोर भी चुप,
दग्ध उर की आग दिख पाती नहीं जो!!
क्या कहूँ, है कंठ से कढ़ती न वाणी,
हम न प्राणी एक जग के, एक मग के!
अलग झर कर भी कभी मिलते कहीं तो,
पर रजत-निर्झर नहीं हम एक नग के!!
देखने भर को मिली आँखें मुझे हैं,
पर कहाँ पाँखें कि उड़ कर आ मिलूँ मैं!
है न वसुधा पर सुधा की धार, जिसमें
खोल कर अनबोल शत-शत दल, खिलूँ मैं!!
इस तरह घुलने-तड़पने में निरंतर,
आह! किस मुख से कहूँ–सुख ही नहीं है!
छीजते-घटते तुम्हें भी देख कर, या–
शांत अंतर हूँ; मुझे दुख ही नहीं है!!
पर बताऊँ पीर मैं किस भाँति अपनी,
ये फफोले फूटने वाले नहीं हैं!
लाख बिलखाऊँ, खिझाऊँ या दुराऊँ,
प्राण मेरे छूटने वाले नहीं हैं!!
… … ….
तुम रहो आकाश में, वातास में ही,
मैं कभी-न-कभी वहाँ आकर रहूँगा!
प्राण मेरे, प्राण से मिल जाएंगे जब,
तुम सुनोगे क्या?–न मैं कुछ भी कहूँगा!!
••
(मांड रागिनी : कहरवा)
पीला चाँद हुआ जाता है, गीला मेरा मुखड़ा,
सुख सुनने को आकुल अग – जग;
किसे सुनाऊँ दुखड़ा?
चाँद स्वयं ही नहीं जानता,–उस पर कितनी ममता!
धरती करती भी तो कैसे आसमान से समता!!
मेरे हँसने-रोने से उसका क्या आता-जाता!
रात-रात भर उसे देखता,–इतना ही तो नाता!!
–फिर भी मेरा हिया फट रहा; होता टुकड़ा-टुकड़ा,
–सूखा जाता आह! चाँद का प्यारा-प्यारा मुखड़ा!
… … ….
संध्या ही पर आँख रुकी थी, ध्यान न रहा उषा का,
चाँद खिलखिलाता जाता, थी खुलती जाती राका;
किंतु बात की बात में गई रात बीत अनजाने,
रहे जहाँ के तहाँ अधबुने दिन के ताने-बाने!
कैसे कहूँ कि वैसे था क्या बना और क्या बिगड़ा!
बादल के टुकड़े-टुकड़े में जड़ा चाँद का मुखड़ा!!
… … ….
वह क्या जाने, टिका गगन-मन किसके अहा, सहारे!
मेरे स्वप्न-सिंधु के बुद्बुद्-से लगते ये तारे!!
उसे ज्ञात मत हो कि उसी से रातें बढ़तीं-घटतीं!
उसकी उजली परिछाईं में काली घड़ियाँ कटतीं!!
कड़ा न कर सकता अब जी को, जीवन से मन उखड़ा!
मैं न चाँद का देख सकूँगा पीला-पीला मुखड़ा!!
•••
(वागीश्वरी : त्रिताल : मध्यलय)
बादलों से उलझ, बादलों से सुलझ,
ताड़ की आड़ से चाँद क्या झाँकता?
–‘मैं न हूँगा यहाँ,’–कह रहा नभ यही;
‘मैं न हूँगा कहीं?’–भूमि कहती–‘नहीं’!
तुम हवा, मैं दवानल वृथा ढाँकता!
ताड़ की आड़ से चाँद क्या झाँकता?
जीतने का कलक,–वेदना हार की,
क्या कथा स्वप्न से भिन्न संसार की?
दर्द तुम, घाव मैं क्यों वृथा टाँकता!
ताड़ की आड़ से चाँद क्या झाँकता?
रंग आया नहीं, रश्मि-छाया घुली,
रेख खुलती नहीं, तूलिका यों तुली!
शून्य तुम, चित्र मैं क्यों वृथा आँकता!
ताड़ की आड़ा से चाँद क्या झाँकता?
••••
(विहाग)
कौन तुम सबसे परे?
चाँदनी बरसा रहे हो बाँसुरी में सुर भरे!
सतह की हिलकोर से चंचल नहीं,
यह लहर-उन्माद, रस-संबल नहीं,–
मर्म-मर्मर क्षोभ का प्रतिफल नहीं,–
मानते हो, गान वह जो प्राण को पागल करे!
सुन रहे, क्या बात तारे कर रहे,
सह रहे, शत घात हारे कर रहे,
सब तुम्हें, ललकार, न्यारे कर रहे!
मुसकिराते तुम कि चंदन से द्रवित सौरभ सरे!
होड़ में बौने उठाए हाथ हैं–
–‘पास ही क्या, लो, तुम्हारे साथ हैं!
–उर तुम्हारे औ ‘हमारे साथ हैं!’
राहु कहता है, अमर सुंदर, अरे, हम तो मरे!
किंतु तुम हो, चाँदनी है, मौन है,
शूल में कलियाँ खिलाता कौन है!
पूछता हूँ शिशिर-कण से, कुछ कहे,–
नीलिमा तज कर भला क्यों वह हरितिमा पर झरे!
Image: The Starry Night
Image Source: WikiArt
Artist: Vincent van Gogh
Image in Public Domain