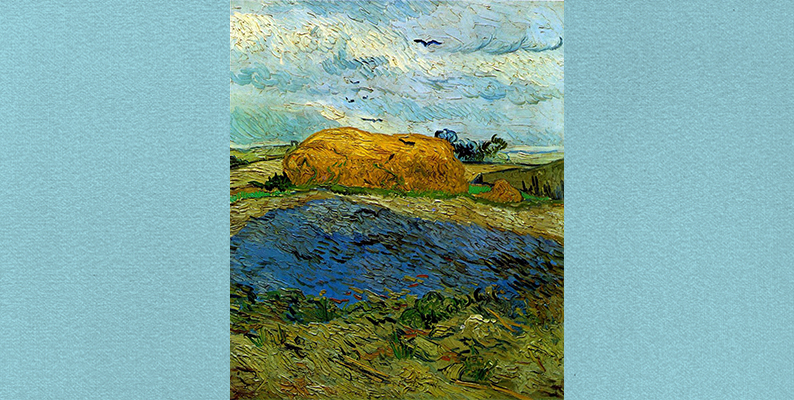एक कोमल-सी याद : रमेश रंजक
- 1 August, 2022
शेयर करे close
शेयर करे close

शेयर करे close
- 1 August, 2022
एक कोमल-सी याद : रमेश रंजक
रमेश रंजक की काव्य यात्रा को अगर ध्यान से देखें तो उनकी इस यात्रा में चार पड़ाव देखने को मिलेंगे। जीवन में इस तरह के पड़ाव आम आदमी की जिंदगी में भी आते हैं। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। आम से खास होने के लिए जिस कठोर साधना की दरकार होती है, वह सबके बूते की बात नहीं। महज खास होने की महत्त्वाकांक्षा काफी नहीं होती, रचनाकार के कृतित्व में निहित जीवन का ताप उसे खास बनाता है।
रमेश रंजक ने भी आम से खास बनने के लिए जो संघर्ष किया है वह साफ नजर आता है। रंजक की साहित्य साधना का प्रारंभ सन् 1951 नवंबर का वह दिन है जब रंजक का दर्द काव्य का रूप लेकर कागज पर उतरा। यह एक अविस्मरणीय घटना है जिसने रमेशचंद्र उपाध्याय को रमेश रंजक बना दिया। हुआ यों–रमेश ने अपने छोटे भाई के साथ गंगा नहाने का प्रोग्राम बनाया। समूचे उत्तर भारत में कार्तिक पूर्णिमा का सरकारी अवकाश रहता है। कहीं यह अवकाश गुरु नानक जयंती के रूप में तो कहीं गंगा स्नान के रूप में मनाया जाता है।
उन दिनों रमेश के पिता जी उत्तर प्रदेश के एटा जनपद के शिक्षा विभाग के कार्यालय के सुपरिनटेंडेंट के पद पर थे। एटा शहर से गंगा जाने के लिए सोरों उपयुक्त स्थान था और आज भी है क्योंकि तुलसी ने सर्वप्रथम राम कथा यहीं सुनी थी। यह रास्ता तीस मील के करीब तो होगा ही। बहुत लोग जाया करते थे। आम आदमी के लिए आने-जाने के तब ऐसे साधन कहाँ थे जो वर्तमान में उपलब्ध हैं। बसों की छतों पर भी लोग खुशी-खुशी बैठते थे। बड़ी निर्भीकता और श्रद्धा के साथ ‘गंगा मइया की जय’ का नारा लगाते हुए अपने आपको उसके प्रति समर्पित करते हुए चल दिया करते थे। एटा में उन दिनों रेल की व्यवस्था न थी। ऊँट गाड़ी, बैलगाड़ी, साइकिल और बहुत से तो पैदल ही अपने-अपने घरों से यह सफर तय किया करते थे। उन दिनों पैसा भी हर एक के पास कहाँ था। हाँ समय था। इसलिए आम आदमी पैसा बचाता और समय खर्च करता था।
रमेश ने भी अपने पिता से गंगा स्नान की बात कही। उसके पिता जी कुछ अच्छे ही मूड में थे। उन्होंने कहा–किसके साथ जाओगे? रमेश ने पड़ोसी परिवार का नाम लेते हुए कहा–महेश को भी तो साथ ले जा रहा हूँ। वैसे हम दोनों साथ हैं तो आपको कभी भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप ही तो कहते हैं ‘दो तो चून से भी ख़तरनाक होते हैं।’ रमेश के उत्साहवर्धक शब्दों को सुनकर पिताश्री बहुत खुश हुए और कहा–‘कल चले जाना’।
रमेश ने अपने ही नहीं, महेश के भी एक-एक जोड़ी कपड़े तैयार किए। दोपहर को चूल्हे से दहकते हुए कोयले निकाले और बिना पैंदी के लोटे में उनको डाला और फिर अपने और महेश के कपड़ों पर घुमाया यानी प्रेस किए। शाम होने लगी थी। सूर्य देवता भी अब जाने ही वाले थे कि तभी गाँव से ताऊ जी आ गए। जिस तरह का दुआ-सलाम का जो शिष्टाचार निभाया जाता है निभाया गया। समय पर सबने खाना खाया और समय पर ही सोने चले गए। पिताश्री और उनके बड़े भाई की चारपाइयाँ नीम के नीचे लगा दी गईं। वे दोनों क्या बातें करते रहे और कब सोये वे जाने लेकिन इधर सुबह की प्रतीक्षा में रमेश-महेश को उस रात वो नींद नहीं आई जैसी आया करती थी।
सुबह नित्य कर्म करने के लिए सभी को जंगल ही जाना पड़ता था। रमेश-महेश भी विचारों में खोये हुए जब दिशा-मैदान से फारिग होकर घर आए तो पिताश्री ने उन्हें कहा–तुम दोनों भाई अब गंगा स्नान को नहीं जा सकोगे। तुम्हारे ताऊ जी को पैसों की जरूरत है। तुम फिर कभी चले जाना। पिताश्री अपने बच्चों को गंगा स्नान न करा सके, इसका उन्हें बहुत अफसोस था। लेकिन अपने बड़े भाई को सम्मान पूर्वक भेजने की खुशी उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। वे एक ईमानदार सरकारी कर्मचारी थे। नौकरी पेशा ईमानदार व्यक्ति अपना और परिवार का जीवन निर्वाह तो कर सकता है लेकिन मौज-मजे नहीं। बड़ा परिवार और कुटुंब की आर्थिक समस्याओं के समाधान के कारण कितनी ही बार पैच लगी धोती पहन कर दफ्तर चले जाने में उन्हें कभी संकोच न हुआ। वे ‘सिम्पिल लिविंग, हाई थिंकिंग’ विचार के थे। उनकी सादगी ही उनका आभूषण था, इसी कारण उनके अफसर उन्हें आदर के साथ प्रणाम करते थे।
पिताश्री की बात सुनकर रंजक का बोलना-हँसना एकदम बंद-सा हो गया। वे कहीं गहरे में ऐसे खो गए कि जब महेश ने उनसे स्नान करने के लिए कुएँ पर चलने को कहा तो वे यकायक चौंक कर कहने लगे–हाँ! हाँ! चलो। घर से कुआँ लगभग तीस-चालीस कदम की दूरी पर था। महेश ने एक डोल, उसमें एक छोटी बाल्टी लोटा डालकर उसे दाहिने हाथ लिया और दूसरे हाथ में रस्सी लेकर चल दिया और रमेश साबुन और कपड़े। वैसे रोज रमेश ही महेश को नहलाते थे लेकिन उस रोज उन्होंने महेश से कहा–‘आज तुम हमको नहलाओ।’
महेश ने अपने बड़े भाई की यह बात खुशी से स्वीकार कर ली। उसने छोटी बाल्टी भर कर अपने भाई के सिर पर धार बाँध कर डाली। जब वह दूसरी बाल्टी सिर पर धार बाँध कर डालने लगा तो अनायास ही रमेश के मुख से ये शब्द उच्चारित हुए–
‘गंगा तेरी निर्मल धारा।’
इस पंक्ति को उन्होंने दो-तीन बार दोहराया। जब तक महेश उनके सिर पर तीसरी बाल्टी डालने के लिए तैयार हुए वे इसी अवस्था में दौड़कर घर आ गए। महेश को तब ऐसा लगा मानो एक दूसरा आर्कमिडीज़ पैदा हो गया है जिसने नये सिद्धांत की खोज कर ली है।
जब महेश घर पहुँचा तब तक रमेश ने अपना प्रथम गीत पूरा कर लिया था। उनके चेहरे को बहुत ही साफ तरीके से पढ़ा जा सकता था। चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था मानो रमेश ने गीत गंगा में गोते लगा कर उस तीव्रतर आवेग को शांत किया है, जो उन्हें कुछ समय पहले बेचैन कर रहा था। गीत इस प्रकार से है–
गंगा तेरी निर्मल धारा।
जो मानव तट तेरे आया
उसने तेरा आशीष पाया
सूने मन का एक सहारा
गंगा तेरी निर्मल धारा।
छोड़ अंत जो तुझको जाते
मगहर को जा चमन बनाते
क्या वो था सचमुच ही न्यारा
गंगा तेरी निर्मल धारा।
बिन पैसे के मन हो चंगा
पाता वही कठोती गंगा
मन नहीं चंगा वो ही हारा
गंगा तेरी निर्मल धारा।
महेश ने रमेश से कहा–गीत तो लिख लिया। अब यह तो बताओ अपना उपनाम क्या रखोगे?
रमेश ने बहुत से उपनाम कागज पर लिखे लेकिन महेश को पसंद नहीं आए।
रमेश ने कहा–तुम कैसा उपनाम चाहते हो?
महेश ने कहा–जैसे भागीरथ भास्कर, भगवान सहाय पचौरी ‘भवेश’।
यह सुनकर रमेश ने उसी समय गीत के नीचे लिखा–रमेशचंद्र उपाध्याय ‘रंजक’ जो बाद में रमेशचंद्र रंजक होता हुआ रमेश रंजक हो गया और आज मात्र रंजक संबोधन भी अपने आप में एक गीत कवि की पहचान छोड़ देता है। रमेश का प्रथम गीत उनके पिताश्री ने भी सुना वे खुश हुए और इतने खुश हुए कि दूसरे दिन जब वे नहाने के लिए कुएँ पर गए उनकी दृष्टि नव अंकुरित पत्ते वाले बरगद के पौधे पर पड़ी, जो कुआँ की पथरीली दीवार को तोड़ता हुआ अपना कद निकालने का प्रयत्न कर रहा था। उन्होंने उसे बड़ी सावधानी से जड़ सहित उखाड़ लिया और घर लाकर पुराने कनस्तर में मिट्टी-गोबर मिलाकर उस पौधे को जमा दिया। जब तक उसमें दो-तीन पत्ते और नहीं आ गए तब तक वे चिंतित ही रहे। धीरे-धीरे वह पौधा बढ़ने लगा। उधर रंजक के गीतों की संख्या भी बढ़ने लगी।
रिटायर होने के बाद रंजक के पिता ने लगभग पाँच वर्ष के उस पौधे को गाँव ले जाकर अपने खेतों के चौपुरा कुएँ पर लगा दिया। गूल के किनारे होने के कारण पानी की कमी न रही। धीरे-धीरे बरगद बढ़ने लगा। झालरा होने लगा। आस-पास के खेतिहर मजदूर भरी दुपहरी उसके नीचे आकर बिरमाने लगे। रंजक के कृतित्व में जहाँ क्रमिक रूप में उत्कर्ष नजर आने लगा वहाँ वटवृक्ष थके-हारे किसान एवं राहगीरों को घनी छाया देकर सुख प्रदान करने लगा।
रंजक जब कभी गाँव जाते उस वटवृक्ष के नीचे अवश्य बैठते। उसके तने को दोनों हाथों से ऐसे समेटते जैसे सहोदर से मिल रहे हों। तना जब हाथों की पकड़ से बाहर होने लगा, तब वह ज्यादा खुश नजर आने लगे। वह उसकी शाखाएँ उपशाखाएँ बड़े चाव से गिनते। उसके पत्तों से कान लगाकर अपने गीतों की लय को सुनते। जड़ की गहराई और फैलाव की जिज्ञासा उनके चेहरे पर सहज ही आ जाती। वट वृक्ष के बाह्य और भीतर फैलाव का सामंजस्य वह अपनी काव्य साधना से करने लगते। बरगद की कला को रंजक धीरे-धीरे पचाते रहे। भीषण गर्मी में जब आस-पास के पेड़ सूखने लग जाते तब अपने हरेपन को बरकरार रखने के लिए वटवृक्ष की जड़ें कहीं गहरे में संघर्षरत होतीं। रंजक ने भी अपने हरेपन को बरकार रखने के लिए जीवनभर संघर्ष किया।
‘स्रोत उत्साह का तू बहा
हर विपत पर लगा कहकहा
मुस्करा बिजलियों के तले
थाम ले रश्मि-रथ बाँध ले
मुटि्ठयों में समय
हो अभय
पाँव धर प्राप्त कर दिग्विजय।’
सन् पैंसठ में गाँव की चकबंदी हुई। रंजक के पिता के हिस्से में बरगद वाला खेत नहीं आया। उन्हें दु:ख हुआ। अपने पिता को मन ही मन खामोश और चिंतित देखकर महेश ने कहा–इसमें परेशान होने की क्या बात है? हमारे पास न सही चाचा के पास ही सही, बरगद है तो घर में ही और किसी के पास तो नहीं है। तब पिताश्री ने उसे समझाया–बेटा! बरगद जब अपनी उम्र पर आता है तब आस-पास की डेढ़-दो बीघा जमीन को अपने तने, टहनियों एवं पत्तों से इस तरह ढक लेता है कि उस जमीन पर डाला हुआ बीज भी लगभग व्यर्थ ही चला जाता है। बरगद के आस-पास की जमीन मेरी होती तो मैं बरगद के लिए छोड़ देता क्योंकि मेरे लिए बरगद रंजक का पर्याय है। लेकिन अब यह जमीन तुम्हारे चाचा के पास है। वह इतनी जमीन बरगद के लिए क्यों छोड़ेंगे?
रंजक के पिताश्री का निधन 22 नवंबर 1966 को हो गया। उन्हें जिस बात की शंका हुई थी, वो सच साबित होने लगी। उनके निधन के बाद समय-समय पर बरगद की छटाई और आवश्यकतानुसार कटाई भी होती रहती है। बरगद आज भी झालर है लेकिन उसका फैलाव उस अनुपात में नहीं हुआ जिस अनुपात में होना चाहिए।
रंजक की सृजनात्मकता के विषय में भी कुछ ऐसा ही प्रतीत होता नजर आता है। उन्होंने जो कुछ भी लिखा और जितना भी लिखा है उसे सब मन ही मन स्वीकर करते हैं लेकिन उनके फैलाव पर मौन हैं। शायद इसी बात को ध्यान में रखकर डॉ. विजय बहादुर सिंह ने कहा है–
रंजक जनकवि थे। उन्हें जनता के बीच दुबारा कैसे लाया जाय, इसकी फ़िक्र फ़िक्रमंदों को करनी चाहिए। उनकी प्रशंसा के पुल बाँधकर हम वह नहीं कर पाएँगे जो यह कविताएँ चाहती हैं। रंजक अपनी कविताओं में ही बचे हैं। हमें कविताओं से पूछना चाहिए कि वे क्या चाहती हैं और हमें करना क्या है?