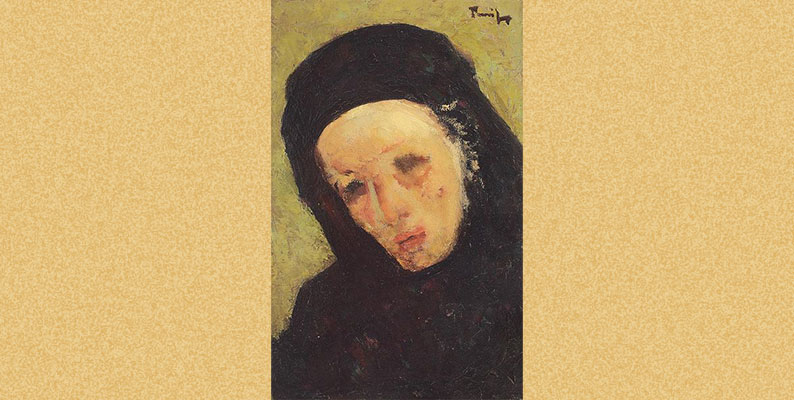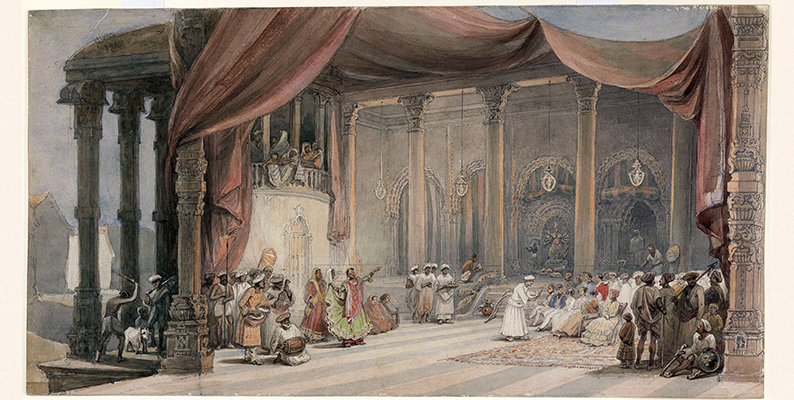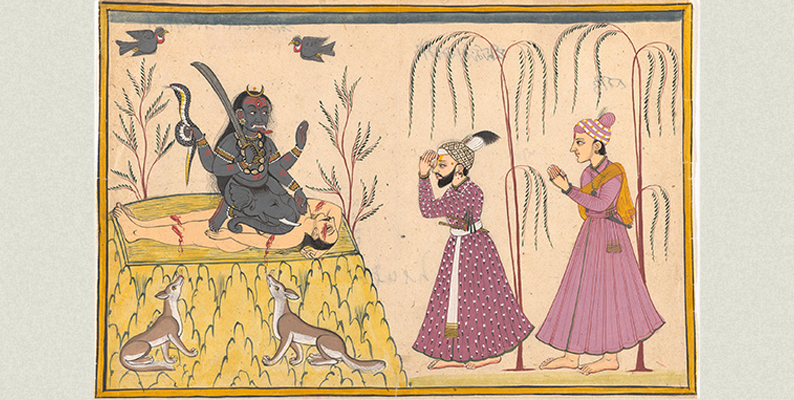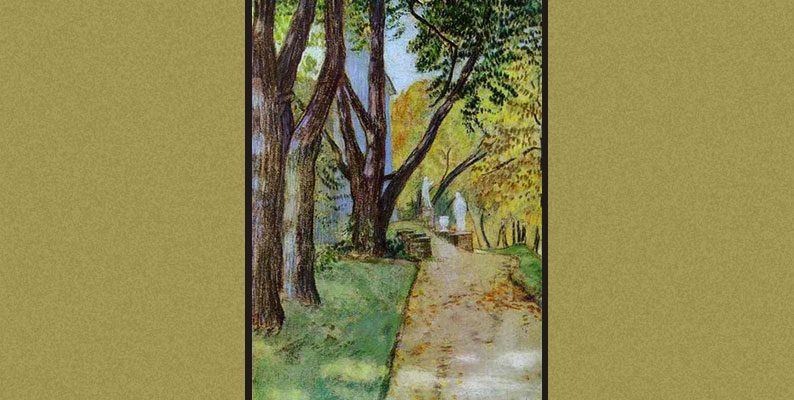जाति और रंग
- 1 July, 1953
शेयर करे close
शेयर करे close

शेयर करे close
- 1 July, 1953
जाति और रंग
एक दिन वह था कि हर गोरा, सम्राट् का जोड़ा बन कर मूँछों पर ताव दिए इठलाता रहा हमारे यहाँ–‘सम्राट भाविया पूजि सबारे’। किसी ट्रेन में वह नज़र आ गया तो बग़ैर उसकी मर्ज़ी उस डब्बे में क़दम रखना भी हमारे लिए खतरे से ख़ाली नहीं था। और, लीजिए, 1947 का एक वह दिन भी आया कि हमारे प्रांत के एक कड़ियल साहब-बहादुर अपना बिस्तर समेट चलते हुए, तो किसी डब्बे में खड़े होने की जगह भी नसीब न होती, अगर उनकी बेबसी पर हम वहाँ खिंच न आए होते उस पल। तो यही दुनिया का दौर है–यही दिन का फेरा। कभी कुछ, कभी कुछ। और, अपना किया-कराया भी तो लौट आता है अपने सर पर एक दिन !
तो जाने कितने साल, याद नहीं, यह ज़मीन उनकी थी–आसमान उनका। सूरज को भी यह हुक्म था कि खबरदार, ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर कभी डूबना नहीं ! हमारी तो कोई हस्ती ही न थी–घर के न घाट के। अपने बड़े-बड़ों का भी कहीं गुज़र नहीं। कोई तैश में आकर अपना हक़ माँग बैठा तो खड़े-खड़े कोरा जवाब पा गया कि जा-जा, यह मुँह और मसूर की दाल ? तेरी दाल तो यहाँ गलने से रही ! हाँ, लाख-दल-लाख में कोई तक़दीर का सिकंदर उनकी नाक का बाल चाहे जो रह आया हो, यह ऊँचे पद का प्रसाद तो कोई नियम नहीं, नियम का व्यतिक्रम था उन दिनों।
मगर हाँ, जब ज़माने की ठोकर पर हमारी आँखें भी खुलते-खुलते खुल गईं और दुनिया के आईने में हमने अपनी गई-बीती सूरत, देखी, तो लीजिए, हमारे अंदर भी स्वाभिमान ने अँगड़ाई ली और अपने पैरों पर खड़े होने की सुध आई।
बस, आँख खुली, अंदर के पट खुले पड़े होठों पर लगे ताले भी। फिर क्या ? ताल ठोंक उतर आए मैदान में। कितनों ने तो हथेली पर जान तक रख दी। बंग-भंग की क्रांति आई। सरगर्मी आई। और, उस खींचतान की दीवार पर लगे रद्दे पर रद्दे चढ़ने।
अँग्रेज बौखला उठे। साम, दाम, दंड और विभेद–ये चारो हथियार आज़माते चले। मगर जब साबरमती फैक्ट्री से अहिंसा का अनूठा अस्त्र ढल कर आया तो फिर इस ब्रह्मास्त्र का जवाब तो सरकारी तरकस में मिलने से रहा।
तो उसी ‘साम’ की देन हमारे आँसू पोछने ‘मान्टेगु रिफॉर्म’ आया और वह अँग्रेजी सत्ता का फौलादी पंजा ज़रा ढीला पड़ा। लीजिए, इक्के-दुक्के हिंदुस्तानी कहाँ से कहाँ उठ आए ! शासन के प्रांगण में जो हाथ बाँधे खड़ रहते बराबर, वे अब अफसरी की ऊँची कुर्सी पाने के हकदार हो गए !
मगर, सौ बात की एक बात, यह बराबरी की ऊँची कुर्सी सरकारी नीति थी–नीयत नहीं ! हमारी कमर में तलवार झूम गई तो क्या, वह कमर की मेखला ही रही–कोई हाथ की सत्ता नहीं। गंगा-यमुनी म्यान से बाहर निकाल अपनी मुट्ठी में थाम ले कोई–यह ज़ोर तो हमारी उँगलियों को नसीब न था। हाथी के दाँत दिखाने को और, खाने को और !
फिर भी ग़नीमत थी यह ऊँची कुर्सी की अफसरी उन दिनों। कितने छोटे-मोटे साहबों ने तो लहू का घूट पिया। विलायती सरकार की ऐसी शुखामदी नीति के धुर्रे उड़ाते रहे अपनी खास मजलिस में गुपचुप। मगर चारा ? घड़ी की सूई तो पीछे लौटने से रही !
हमारे जिलाधीश की तो पाँव-तले की धरती सरकने पर आई। जिलाबोर्ड की चेयरमैनी की कुर्सी छोड़ते उनकी जान पर आ गई जैसे। वे चाहने लगे कि सारे मेंबर लिख कर यह फतवा दे दें कि इस जिले के अंदर कोई ऐसा हिंदुस्तानी नहीं जो इस कुर्सी की ज़िम्मेवारी उठा पाए। और लीजिए, हमारे कितने भाई-बिरादर साहबी हवा का रुख देख अपनी नाव पर पाल बदलने के लिए तैयार भी हो गए ! देश की मर्यादा की नाव मँझधार में जाती है तो जाए, उनकी निगाह पर तो देश नहीं–साहब का आदेश था बस ! हाँ, दो-चार ऐसे ज़रूर निकले जिनके स्वाभिमान की आँख का पानी मरा नहीं था। उन्होंने साहब के विरोध में हमारा नाम रख दिया।
एम.ए. की डिग्री लेकर हम नए आए थे इस मेंबरी की गली में–नई चाह थी, नया उत्साह। सरकारी नीयत चाहे जो हो, सरकारी नीति तो एलान हो चुकी थी और उस नीति के पाबंद जिलाधीश की यह अनधिकार चेष्टा नहीं तो क्या थी ? उनमें कौन ऐसे लाल जड़े हैं कि ऊँची कुर्सी पर गोरा ही बैठे, दूसरा नहीं ? जो दिन गए–गए। अब यह कैसे संभव है कि हम इस आए हुए अवसर का अपने हाथों गला घोंट दें !
बस, लीजिए, बाज़ी छिड़कर रही। क्या-क्या नहीं पैंतरे चले ! मगर साहब और उनके खुशामदी मुसाहबों के हज़ार बंदिशों के बावजूद भी हमारा मोहरा लाल होकर रहा। रह गए जिलाधीश टका-सा मुँह लिए ! यही नहीं, प्रांत के ऊँचे अफसरों के हाथ उनकी मरम्मत भी अच्छी हुई चूँकि दी हुई चीज़ के लिए यह अपनी रीझ कैसी ! और, जाने-अनजाने रीझ आई भी तो फिर बाज़ी न आई, बदनामी ही हाथ आकर रह गई !
उन दिनों जिलाधीश की मर्ज़ी तो विधि की मनमानी रही जैसे। हम पर अपना गुस्सा उतारने से बाज़ न आए। क्या-क्या सितम नहीं ढाए ! मगर कब किसकी बनी रही है और कब किसकी बनी रहेगी निरंतर ?
आखिर–
“सितम बेगुनाहों पर आसाँ न समझें,
तड़प जाइएगा जो तड़पाइएगा !”
तो बस, हुआ वही। हमने ऊबकर प्रांत के गवर्नर के आगे सारे कच्चे चिट्ठे खोलकर धर दिए, साँच को आँच क्या ? बात लग गई और जिलाधीश को मुँह की खानी पड़ी आख़िर !
तभी हमें पता चला कि साहब के साथ कुछ ऊँची कुर्सी की ही लगी न थी, अपने भाई इंजीनियर का साथ जो छूट रहा है ! वह जा रहा है एक नेटिव की उँगलियों के इशारे पर थिरकने–यह तो साहबी शान और मान पर एक धब्बा था जैसे। गवर्नर की उँगली उस दुखती रग पर जा पड़ी और उन्होंने इंजीनियर रॉस्टन साहब को और हमको अपने यहाँ डिनर पर बुलाकर आपस के मेलजोल का रास्ता साफ़ कर दिया–किसी छत्तीस के रिश्ते की गुंजाइश ही न रही !
वह सर पर छाए हुए बादल छँट गए। आसमान साफ़ हो गया और हमने इस नई दुनिया की जिम्मेवारियों को जी उड़ेल उठा लिया अपने कंधे पर। रॉस्टन साहब कुछ ऐसे-वैसे नहीं, अपने ढंग के निराले निकले। कभी तो लगा कि कोई सगा भी वैसा क्या होगा ! वह बेतकल्लुफ़ी, हँसी-खुशी कि उमड़ा आता हो दिल जैसे ! और, कभी वह दूरी–वह अपने काम से काम की मनोवृत्ति कि उनके अंदर का ताल-सुर उनका मौला ही जाने !
हाँ, जानते-जानते हम एक-दूसरे को जान गए, पहचान गए। उन्होंने हमारे अंदर क्या-क्या पाया, जानें वह। हमने तो पाया कि उनके अंदर एक ओर मानव है तो दूसरी ओर दानव। और, हो-न-हो, वह फिरंगी पहले हैं आदमी पीछे। वैसे तो वह अच्छे ही रहे–हमसे कहीं अच्छे। अपनी ज़बान, अपने ईमान के सच्चे ही दीखते, इंसाफ़ पसंद और दर्दमंद भी ! गरीब की आह का भी एक असर था उनके दिल पर। मगर ये सारी बातें रहीं तो क्या, कहीं किसी के चलते फिरंगी अमलदारी की किलेबंदी पर की आँच आने का अंदेशा दीख गया तो फिर ईमान क्या और जान क्या ? अपने देश के स्वार्थ की रक्षा के लिए सर्वस्व निछावर ! बस, जहाँ अपनी शाहंशाही का प्रश्न आया–ब्रिटिश साम्राज्य की आन-बान का सवाल, वहाँ तो किसी समझौते की गुंजाइश ही नहीं। बस, वही–‘सूच्यग्र नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव’ !
मगर यह सब होते हुए भी वह कुछ ऐसे अंधे न थे कि जब गाँधी की आँधी आई और गोरों के लहू-पसीने से सींचे हुए पेड़-पौधे उखड़ने पर आए तो शुतुरमुर्ग की तरह रेत में अपनी चोंच को गाड़ अपने सपनों की मौज में मग्न रहें। उनके चेहरे पर भी एक रंग आने लगा, एक रंग जाने लगा। वैसे तो आमने-सामने उस आँधी की खिल्ली ही उड़ाते रहे, हँस-हँस कर क्या नहीं चुटकुले छेड़ते ! मगर हमारे लिए तो पते की बात यह थी कि वह रहा-सहा तान-तेवर भी दूर होता गया और रह-रह कर लगे उनके पैर ज़मीन पर आने।
अक्सर हम साथ ही दौरे पर जाते। डाक-बंगले में साथ ही ठहरते, साथ खाते-पीते भी। दिनभर तो अपने काम से काम रहता–वह कहीं, हम कहीं; मगर जब बेर डूबती और थके-मांदे लौट आते हम बंगले की पौर पर, तो लीजिए, बैठे-बिठाये मीने की परी आती; उनकी आँखों में तरी लाती, उनकी ज़बान में फुर्ती भी।
जेठ की दुपहरी। लौट रहे हैं ‘मोहनिया’ से रॉस्टन साहब के साथ। मोटर की सवारी है तो क्या, ऐसी धूप और लू में देहाती सड़कों की धूल छानना कोई बाएँ हाथ का खेल नहीं। कहाँ ख़सख़स की टट्टी की आड़, पंखे की हवा खाते, कहाँ खा रहे हैं बालू की रेत में अंधड़ के लौ उगलते झोंके ! और, हम तो हम, साहब-बहादुर के तो होंठों पर दम है जैसे ! मगर चारा ? बरसात के पहले पड़ोस का पुल जो तैयार कर देना ठहरा और उनके साथ अपना काम पहले है, आराम पीछे। यह ज़िम्मेवारी की मनोवृत्ति न होती तो कभी की सरक गई होती उनके पाँव-तले की धरती।
छोटे-से एक गाँव से मोटर पास कर रही है। हैं ! यह क्या ? एक हंगामा खड़ा है सामने। यह भीड़ कैसी ? यह चीख-पुकार कैसी ? आयहाय ! यह कहाँ आ गए हम ! मोटर तो आगे बढ़ने से रही !
देखा, गाँव के चंद बड़े-बूढ़े बड़े तैश में हैं। उनके कूएँ के अंदर किसी चमार के छोकरे ने अपनी डोलची लटका दी थी पानी भरने। सामने के बंद किवाड़ की फाँक से बड़ी बहू की नज़र जा पड़ी। फिर क्या ? उन्होंने आसमान सर पर उठा लिया ! छोकरा सर पर पाँव रख कर भागा, मगर भागकर जाता कहाँ ! घिर गया। और, लीजिए, बरसने लगे उस पर लात-जूते ! चमार टोली से उसका बाप दौड़ कर आया तो वह भी लगा बेटे ही पर हाथ साफ़ करने कि ऐसा क्या क्यों ? बड़ी प्यास थी तो टोले-मुहल्ले से दो चुल्लू माँग ही लेता। ऐसा क्यों किया ?
हम तो दंग। पता चला, गाँव में दो ही कूएँ ठहरे। दोनों ही उनकी पहुँच के परे। उनका अपना कूआँ तो कच्चा ही ठहरा जो जेठ आते-आते दम तोड़ बैठा। आस-पास कोई नदी-नाला नहीं। अब किसी कुलीन की आँख में पानी रहा तो अपने घड़े से उनके घड़े में उड़ेल दिए पानी, नहीं तो चलिए, एकाध मील एड़ियाँ रगड़िए किसी तलैया की तलाश में !
चमारों का चेहरा उड़ चुका था। पानी तो पानी, अब तो दो दाने चने के भी लाले पड़ जाएँगे–लाले ! उनमें से एक रॉस्टन साहब के पैरों पर लोट गया। साहब बहादुर आ गए बड़े ताव में।
“अब पागले ! तुम्हें चाहिए क्या, तुम नहीं जानते। हाँ, तुम चाहते क्या हो, मुझे सब पता है। मैं तो कहता हूँ, इस हवा-पानी में तुम्हारा गुज़र नहीं। बस, अभी बिस्तर समेट चल पड़ो यहाँ से। हमारा क्रिश्चियन मिशन कुछ दूर नहीं। वे तुम्हें खुशी-खुशी अपना लेंगे। वहाँ तुम्हें खाने-पीने ही की नहीं, तुम्हारे बच्चों के पढ़-लिख कर ऊँचे उठ इन जल्लादों के कान उमेठने की बी बन आएगी एक दिन–समझे ?”
वे लगे आँखें फाड़ उनका मुँह जोहने। कोई जवाब नहीं। कुलीनों की टोली लगी तालियाँ देने–“ले सुन, कहाँ लिए जा रहे हैं यह साहब बहादुर…कूएँ में भठने–कूएँ में।”
उनको तो साँप सूँघ गया जैसे–बुत ! मुड़ आए हमारी ओर। हमने कहा कि तुम्हें तो एक अपना कूआँ चाहिए न–यह कोई बड़ी बात नहीं।
“क्या सच, ऐसा ?”–उनकी बाछें खिल उठीं।
“इसमें पूछना ही क्या, अभी आर्डर दिए देते हैं।” और हमने चट एक आर्डर लिखकर रॉस्टन साहब के हवाले किया कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के रुपए से इनके लिए एक पक्का कूआँ अलग तैयार करा दिया जाए ! साहब छेड़ बैठे कि पहले मीटिंग से बाक़ायदे मंजूरी जो लेनी ठहरी !
“कोई बात नहीं, यह ज़िम्मेवारी मेरी रही; आप अपना काम अंजाम दें।”
लीजिए, कुलीनों की टोली बौखला उठी। उन्हें जानने को बाकी न रहा कि आर्डर देने वाला यह है कौन–कहाँ का ! बस, घेर लिए हमको। दो-चार लगे स्तोत्र पढ़ आशीर्वाद देने, अपनी गाथा भी सुनाने। उनकी दलील कि कसूरवार जब ये ठहरे, आए कुलीनों के कूएँ में दिन-दहाड़े ही सेंध देने, तो फिर यह कैसा इंसाफ़ कि कोतवाल की जगह उल्टे चोर ही इनाम पाए–वह भी अपने जिले के एक माने-जाने रईस के हाथ !
हमने कहा कि हवा और पानी का कहीं बँटवारा नहीं। उनका हक़ भी इस कूएँ पर बराबर ठहरा। आखिर, कूएँ के अंदर रेंगते कीड़े-मकोड़े से भी ये गए-गुज़रे हैं क्या ?
उनमें एक ज़रा होशियार रहा–दुनियादार भी। भाँप लिया हमारा रुख। चट अपना पहलू बदल दिया। लगा कहने कि यह कूआँ भी तो सूख ही चला है। वैसा पानी होता तो फिर आज यह छीना-झपटी की नौबत आती ?
हमने कहा कि बनो मत ! तुम्हारे कूएँ में पानी न हो, न सही, तुम्हारी आँख में पानी जो नहीं ! और, बनते हो तुम बड़े पानीदार ! यही अति आचार तो अत्याचार ठहरा ! आज तुम उन्हें कूएँ में पानी भरने नहीं देते–न दो, मगर एक दिन इसका अंजाम तुम्हारे सर बीत न गया तो कहना ! तुम उनके सामने पानी भरोगे–पानी !
मोटर से चल दिए हम। रॉस्टन साहब के पेट में तो पानी पचने से रहा। उगल बैठे–
“आज जो तुम उठे हो पश्चिम से जिस बराबरी का तोहफ़ा माँगने, उस बराबरी के दो दाने भी अपने यहाँ इन गरीबों को दिए रहते तो तुम्हारी बात अपनी एक जगह रखती। यों तो यह ज़बानी लनतरानी ठहरी जो हम जैसे जानकारों पर कोई रंग लाने से रही !”
“जी, अब देर नहीं–गाँधी की चौतरफ़ी आँधी में वह ज़ोर है कि कट्टरता के तमाम कुलाबे उखड़ कर रहेंगे–देशी हों या विदेशी…हाँ, मैं भी पूछता हूँ, आपने कब-कहाँ दिया वह बराबरी का दर्जा एशिया के अंदर…?”
“क्या कह रहे हो तुम ? हमारे यहाँ तो जो भी आदमी के लिबास में आए, वह बराबरी का दर्जा पाकर रहेगा–देर-सबेर। उसका हक़ है यह। वह कौन है, क्या है, कहाँ का है–कोई बात नहीं। तुम्हें भी आदमी की पौर पर लाने के लिए हमने कुछ उठा रखा ? भूल गए, कल की बात है, तुम अपनी बहू-बेटियों को जलती चिता में झोंक देते रहे बेकसूर ! हमारे लार्ड बेंटिक न आए होते तो कौन तुम्हारे सर से वह भूत उतार फेंकता ? आज भी उस बेचारी को खुली हवा, खुली रोशनी तक नसीब नहीं, बराबरी की जगह तो दूर। वही हमारा चपरासी है रोशन, जो जब कभी बाहर जाता है तो घर में ताला ठोंककर जाता है…इतमीनान जो नहीं !”
हम चुप सुना किए। क्या कहें, क्या न कहें–यही उधेड़-बुन बनी रही।
रॉस्टन साहब कहते चले–
“वही कहता हूँ कि तुम पहले अपने को ही देखो। अपनी कमजोरियों से आँखें मूँद न लो। हम न आए होते तो तुम कहाँ के होते आज ? तुम्हारे नाम से भी दुनिया को शर्म आती रही–शर्म !…तो भाई मेरे ! इन गरीबों की आह बेकार न होगी। तुम नहीं मानते, न मानो, पर मेरी बात गिरह बाँध रखो, वह दिन दूर नहीं, जब यह जाति-भेद का जुल्म पलट कर आएगा तुम्हारे सर, और आभिजात्य साम्राज्य की यह बोझी हुई नाव मँझधार में डूबकर रहेगी।”
हम लहू का घूँट पीते रहे। कहते क्या ? यही जाति-भेद का भूत तो भारत के सर पर शनिश्चर का तेवर है आज भी !
[2]
दिन पर दिन जाते रहे। क्या-क्या दिन आए और क्या-क्या दिन गए ! लीजिए, वह दिन भी आया कि हमारे जिले के गोरे-अफसरों की किलेबंदी की नींव की ईंटें भी खिसकने पर आईं !
अब तक अँग्रेज अफसरों का अपना अड्डा रहा–आरा क्लब। शाम आई और क्लब में जान आई। वह खान-पान, वह हँसी-खेल की हिलोरें उठतीं कि रात को रात क्या कहे कोई ! एक-से-एक राग, एक-से-एक रंग ! और, सनीचर की रात तो उनकी अपनी रात थी–बहार की सौगात लिए आती वह। जिले के जाने कितने जाने-माने अँग्रेज प्लैंटर भी आकर शामिल जो जाते।
तो लीजिए, इसी क्लब की मेंबरी के लिए हमारे नए सिविल सर्जन भी उमीदवार हुए। आप ठहरे देशी, कोई विदेशी नहीं। हाँ, आई.सी.एस. होते तो दो पल में उनका मोहरा लाल हो जाता। वैसी उमीदवारी होती न पैरवी।
आई. सी. एस. होना उन दिनों इसी शरीर से गौरांग देवों के दिव्य धाम तक उठ जाना था। ज़मीन उनकी–आसमान उनका। क्लब में उनकी पैठ धरी होती–पूछ वैसी न हो, न सही। जभी तो मिस्टर दत्त और उनकी पत्नी सरोज नलिनी देवी हमारे जिले में कदम रखते ही क्लब में तो दाखिल हो गए पर जब टेनिस के डंडे लेकर लॉन में खेलने उतरे तो मियाँ-बीबी ही रह गए गेंद उछालते–दो-के-दो, बस ! न दो और आए और न खेल में जान आई। और तो और, मिस्टर मेटलैंड आई.सी.एस. अँग्रेज होकर भी जब एक बंगाली युवती को ब्याह कर क्लब में ब्रिज खेलने आए तो अपने भाई-बिरादर भी वह रुख़ पलट बैठे कि दो से चार होने की नौबत ही नहीं आई कि ताश बँटे !
मगर तब से अब तक जाने कितना गंगा का पानी पुल के तले से जा चुका था ! अब तो हिंदुस्तानी की पैठ ही नहीं, पूछ भी रही–बला से, दिखावे की ही सही ! क्या टेनिस, क्या ब्रिज–साथ-साथ हँसते-खेलते और कहीं श्रीमतीजी नई रोशनी की प्रगतिशील निकलीं तो फिर क्या ? हाथ से हाथ ही नहीं–सीने से सीने भी मिलते डांसिंग फ्लोर पर ! हाँ, दिल से दिल मिलने का तो सवाल ही नहीं आज की दुनिया के हवा पानी में !
तो यह हमारे नए डॉक्टर चिकित्सा-विभाग के दफ्तर में जिस फिरंगी सिविल सर्जन की कुर्सी पर आए, क्लब में भी उसी साहब की कुर्सी पर उनकी जगह बनी की बनी चाहिए–इस दलील की उपेक्षा नहीं की जा सकती, नहीं की जानी चाहिए। मगर आप आई.सी.एस. तो थे नहीं–थे एक डॉक्टर। माना कि ऊँची विलायती डिग्री थी, विलायती सज-धज भी। जो हो, किसी के दर पर जाकर माथा टेकना आपसे बना नहीं। नए आए थे–हसब दस्तूर सबके घर गए, सबसे मिले भी, मगर घुटने टेक उनके वोट के लिए अपनी अर्ज़ी भी पेश करें, ऐसी हथजोरी तो उनसे होने से रही। यही अपनी तमीज़ की चुस्ती तो ताजदारों की चर्बी छाई हुई आँखों में काँटे की तरह चुभ गई जैसे। और फिरंगी अफसरों के साथ अपने लिए एक न्याय था, हमारे लिए दूसरा।
लीजिए, उन्होंने न दाएँ देखा न बाएँ, चट हमारे नए डॉक्टर को ब्लैक बॉल (black ball) कर दिया, चुनाव से खारिज ! और तो और, रॉस्टन साहब भी ज़बान देकर मुकर गए–वोट ख़िलाफ़ दे बैठे। अब सामने आने से रहे वह। जानें कहाँ दौरे पर चल दिए। बात फूट कर रही–जानने वाले जान गए कि वह भी कहते हैं कुछ और रहते हैं कुछ।
शहर में बड़ी सनसनी रही–कानो कान बात फैल चली। वह मेल-जोल का मुलम्मा दो दिन भी नहीं टिका–पोल खुल गई। डॉक्टर साहब का तो कुछ गया नहीं–गया उनका, जो आए थे अपनी समता और समानता के क्या-क्या नक्शे लिए हमारी आँखें खोलने !
कोई दस दिन बाद चंद फाइल लिए रॉस्टन साहब हमसे मिलने आए। टमाटर-सा सुर्ख़ चेहरा गुलफुल तो जरूर था, होंठों पर बारीक हँसी भी थी, पर हाथ से हाथ जो मिला पाए, नज़र से नज़र नहीं।
काम की बात रही। कहाँ क्या करना है, क्या नहीं–सब कह गए, समझा गए। बातों के सिलसिले में उस कूएँ की चर्चा भी छिड़ आई। वह कूआँ तो कभी का तैयार हो चुका था पर उसे ‘बोर’ कर देना ज़रूरी था। हरिजनों ने अर्ज़ी भी दे रखी थी।
हमने कहा–“भले याद दिलाई, याद है न उस दिन की बात ?”
“सो क्या ?”
“वही जो आपने बड़े तपाक से कहा था कि यह जाति-भेद का जुल्म तो पलट कर आएगा एक दिन हमारे सिर !”
वह लगे आँखें फाड़ हमारा रुख़ जोहने । बोले–
“तो कुछ ग़लत क्या कहा, कहिए !”
“जी, पते की बात थी वह ! मगर हम भी कहे देते हैं, आप गिरह बाँध रखें, वह दिन दूर नहीं कि यह रंग-भेद का जुल्म पलट कर आएगा आपके सिर बेतहाशा और गौरांग साम्राज्य की बोझी हुई नाव मँझधार में डूबकर रहेगी !”
रॉस्टन साहब बुत ! झुक गए शर्म से। लगे यों ही सामने की फाइल के पन्ने उलटने।
दो पल बाद नज़दीक सरक कर, आँखें मटका, एक अजब अंदाज़ से हाँसी में बोले–
“जानते हो, वह अक्सर खद्दर जो पहिनते हैं ! जिलाधीश से भी पर्दा नहीं।”
“ओ ! यह बात है ?…तो फिर बंदा भी कसूरवार ठहरा–खादी से इनकार नहीं !”
“मगर तुम तो कोई सरकारी अफसर नहीं; कहाँ वह ठहरे मेडिकल डिपार्टमेंट के अध्यक्ष !”
“तो यह खादी आई है सरकारी हुकूमत की जड़ खोदने–ऐसा ?”
“बेशक ! क्रांति का ही प्रतीक है खद्दर।”
“ऐसे आप जो कहिए, पर हम तो समझते हैं कि आप भी खादी अपना पाते तो फिर देखते…”
कि हठात् वह बीच ही में टोक बैठे–“भला विदेशी चीज…जान रहते…”
“जी ! मगर हमारे लिए विदेशी विदेशी नहीं–मुँह की लाली ठहरी ! है न ? अपने लिए एक नीति, हमारे लिए दूसरी !”
रॉस्टन साहब सन्न। अब कैसे-क्या कहें ? अपने ही में खोए-से बैठे रहे। लीजिए, एकाएक उठ खड़े हुए, बोले–
“क्या बताऊँ, कुछ ऐसी हवा उठ आई उस दिन कि कोई भी अपने-आप में न रहा। क्या से क्या…”
“जी नहीं, यह हवा-पानी तो चिरंतन ठहरा । कोई बरी नहीं। यह मैं और तू की धुँध कहाँ नहीं, कब नहीं ? कहीं जाति है, कहीं मत, कहीं रंग, कहीं और कुछ–कोई हद है इस अँधेरे की ? हाँ, अपनी आँख का माड़ा तो दिखता नहीं, पर पड़ोसी की आँख की फूली बराबर दिख जाती है !”
–[ऑल इंडिया रेडियो के सौजन्य से]
Original Image: George Clive and his Family with an Indian Maid
Image Source: WikiArt
Artist: Joshua Reynolds WikiArt
Image in Public Domain
This is a Modified version of the Original Artwork