शरतचंद्र संबंधी मेरे संस्मरण (दूसरी कड़ी)
- 1 October, 1951
शेयर करे close
शेयर करे close
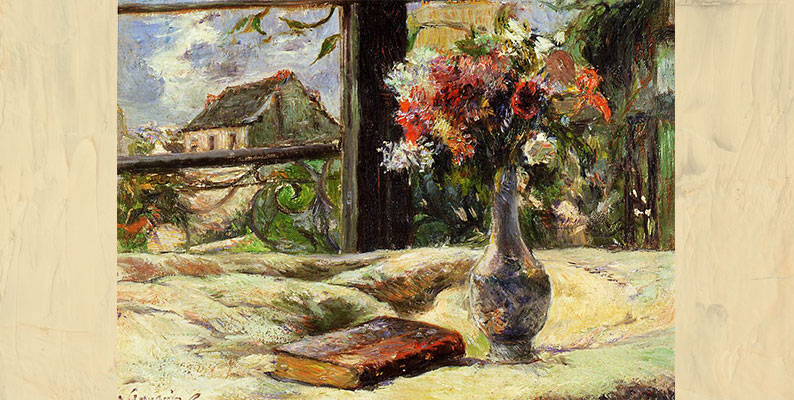
शेयर करे close
- 1 October, 1951
शरतचंद्र संबंधी मेरे संस्मरण (दूसरी कड़ी)
“किसी व्यक्ति के चरित्र-चित्रण या किसी विशेष परिस्थिति के वर्णन के सिलसिले में जितने भी भाव किसी कवि, नाटककार या उपन्यासकार के भीतर उमड़ते हैं उन सबको उगल देना उतना कठिन नहीं है, जितना उन सबको संयत करके, उन्हें दबाकर केवल इंगितों और आभासों द्वारा गहरा असर पैदा करना।”
दूसरे दिन जब मैं शरत् चंद्र के यहाँ पहुँचा, तब वह तन्मय भाव से एक पुस्तक पढ़ रहे थे। मैं सीधे उनके बैठक के कमरे में चला गया था। बाहर से दरवाजा खटखटाने, नौकर से पूछने या नौकर के न दिखाई देने पर बाहर खड़े रहने की कोई आवश्यकता ही मुझे नहीं महसूस हुई। मुझे मेरे मित्रगण आज भी अव्यावहारिक बताते हैं, पर तब की बात जब मैं सोचता हूँ। तब अपनी अव्यावहारिकता के चरम निदर्शनों की याद से आज भी संकुचित हो उठता हूँ। तब मेरे दिमाग में यह बात ही नहीं आई कि इतने बड़े और प्रसिद्ध लेखक, जिनसे मेरा केवल एक दिन का परिचय है, अपने घर के भीतर बीस तरह के कामों में व्यस्त हो सकते हैं और इस विशेष क्षण में किसी अत्यंत महत्त्वपूर्ण रचना में तल्लीन हो सकते हैं, इसलिए बिना पता लगाए या नौकर से अपने आने की सूचना दिलाए ही सीधे उनके अध्ययन के कमरे में घुस जाने के बराबर अशिष्टिता और अव्यावहारिकता दूसरी नहीं हो सकती। उस समय तो मेरे अंतर में यह विश्वास जमा हुआ था कि एक ही दिन के परिचय में उस महान् लेखक ने जिस स्नेह और सौहार्द का परिचय मुझे दिया है, उससे मैं निश्चित रूप से इस बात का अधिकारी सिद्ध हो जाता हूँ कि जब चाहूँ तब बिना पूछे ही उनके कमरे में घुस सकता हूँ।
जो भी हो, जब उस निश्चित विश्वास के साथ मैंने उनके बैठक के कमरे में (जो उनका ‘स्टडी रूम’ भी था) प्रवेश किया तब उन्हें एक पुस्तक में तन्मय देखकर मैंने उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के उद्देश्य से कहा “नमस्कार! यह कौन सी पुस्तक है जिसे आप इस प्रकार तन्मय भाव से पढ़ रहे हैं?” बिना तनिक भी संकोच के मैंने यह प्रश्न किया। मुझ जैसा संकोची आदमी एक ही दिन के परिचय के बाद उनसे इस प्रकार की ढिठाई से भरा प्रश्न कैसे कर सका इस बात पर मुझे स्वयं भी आश्चर्य हो रहा था। आज मैं जानता हूँ कि यह उनके स्वभाव की महान् उदारता का ही परिणाम था कि मैं इस कदर दुस्साहस कर सका।
उन्होंने आँखों की पुतलियों को पढ़ने के चश्मे के ऊपर घुमाकर मेरी ओर देखा और बोले–“आइए, बैठिए!” उसके बाद चश्मा उतार कर मेज पर रख दिया और खुली हुई पुस्तक को औंधा कर के रख दिया। मैं सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। कवर पर छपे नाम पर मेरी नजर गई। वह था गोर्की का विश्वविख्यात उपन्यास ‘मदर’। मेरे हाथ में काले कपड़े में बँधी हुई रवींद्र की ‘चयनिका’ थी। उसे मेज के एक किनारे पर रखकर मैं भी इतमीनान से बैठ गया।
“बहुत बड़ा लेखक है यह गोर्की”–उन्होंने हुक्का गुड़गुड़ाते हुए आवेश के साथ कहा।
तब तक मैं दूसरे सभी लेखकों की रचनाएँ पढ़ चुका था, पर गोर्की की कोई रचना मैंने नहीं पढ़ी थी–हालाँकि पढ़ने का इरादा कई दिनों से कर रहा था।
मैंने कहा; “मुझे तो रूसी लेखकों में डास्टाएव्सकी सबसे बड़ा उपन्यासकार लगता है। उसमें बाहरी जीवन के पर्यवेक्षण की बारीकी के साथ मनुष्य के अंतस्थल में डूबकर उसके स्तर-प्रति-स्तर के सूक्ष्म विश्लेषण करने और उस पंक के मथन से मानवत्व के कमल को परिस्फुट करने की जो क्षमता वर्तमान है, वह मुझे आश्चर्यजनक लगती है।”
“यह ठीक है, पर गोर्की की रचनाएँ पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि जीवन की जैसी पकड़ उसमें है वैसी न डास्टाएव्सकी की रचनाओं में पाई जाती है न कहीं और। आपने पढ़ी है गोर्की की कोई रचना?”
“जी नहीं, अभी तक नहीं पढ़ पाया। पर आपकी बात सुनने के बाद पढ़ने की तीव्र इच्छा हो रही है, आप ही सुझा दें कि पहले कहाँ से शुरू करूँ?”
“उसका ‘क्रीचर्स दैट वन्स वेयर मैन’ नामक एक कहानी संग्रह अभी हाल में अँग्रेजी में अनुवादित होकर मार्केट में आया है। पहले उसे पढ़ डालिए। उसमें आप जीवन के प्रति एक बिलकुल नया दृष्टिकोण, नई भावधारा, नई शैली और नई ही टेकनीक पाएँगे। गोर्की मानवता के प्रति एक बिलकुल ही नया संदेश लेकर आगे बढ़ा चला जाता है। उसे न पढ़ने से आप जीवन के एक बहुत बड़े पहलू की जानकारी से वंचित रह जाएँगे।”
“ठीक है” मैंने कहा, “मैं आज ही शाम को वह पुस्तक खरीद लूँगा और पढ़ूँगा। पर डास्टाएव्सकी के संबंध में आपकी क्या धारणा है, यह मैं जानना चाहता हूँ।”
“डास्टाएव्सीकी भी निस्संदेह बहुत बड़ा लेखक है–इतना बड़ा कि उसकी उँचाई, गहराई और विस्तार तक पहुँच सकने वाला कोई दूसरा आधुनिक लेखक मेरे ध्यान में नहीं आता। यह सब होने पर भी उसने जीवन को सीधे और सहज भाव से नहीं पकड़ा है, जबकि गोर्की बिना किसी हेर-फेर के सीधे जीवन के मर्म को छूता है। इसलिए मैं गोर्की को बड़ा मानता हूँ।”
मुझे तब भी यह विश्वास था और आज भी है कि शरतचंद्र पर डास्टाएव्सकी का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था, विशेष कर पतित नर-नारियों के संबंध में उनका जो दृष्टिकोण था उसकी प्रेरणा में डास्टाएव्सकी का भी बहुत बड़ा हाथ रहा। पर तब–1922 में–वह पतित नर-नारियों से संबंधित रचनाओं का युग पार कर चुके थे और अपने रचना-काल के तीसरे चरण में प्रवेश कर रहे थे। ‘पथेर दावी’ के कुछ परिच्छेद वह लिख चुके थे और अब वह उसे एक नया मोड़ देना चाहते थे। इसलिए अब गोर्की उन पर बड़े जोरों से हावी हो रहा था।
मैंने तब उस बहस को आगे नहीं बढ़ाया। इसका एक कारण तो स्पष्ट ही यह था कि तब तक मैंने गोर्की की कोई चीज पढ़ी ही नहीं थी, और दूसरा कारण यह था कि मैं उन पर डास्टाएव्सकी के प्रभाव की चर्चा चलाकर उनका गोर्की संबंधी ‘मूड’ खराब नहीं करना चाहता था। इसलिए मैंने एक बीच का प्रश्न खड़ा किया। मैंने कहा, “प्राय: सभी श्रेष्ठ रूसी उपन्सासों, में जीवन के जिस प्रचंड हाहाकार, जिस प्रबल भूकंपीय कंपन और तूफानी आंदोलन का वर्णन पाया जाता है और कठोर संघर्षमय यथार्थ जीवन के भीतर उत्पन्न होने वाले जिन भीषण अंतस्फोटों का सजीव और मार्मिक चित्रण पाया जाता है, भारतीय उपन्यासों में वैसा क्यों नहीं मिलता? क्या जीवन के गहरे, तीखे और व्यापक अनुभवों के संबंध में यहाँ लेखकों की कमी इसका एक कारण नहीं है?”
“कम से कम यह कारण तो नहीं ही है” उन्होंने शांत भाव से उत्तर दिया। “क्योंकि जीवन के जो अनुभव मैंने प्राप्त किए हैं वे अपनी विविधता और तीखेपन में किसी भी रूसी लेखक के अनुभवों से कुछ कम नहीं है। मैंने समाज की हीनतम परिस्थितियों में रहनेवाले लोगों के बीच में उन्हीं में से एक बनकर जीवन बिताया है; जरायमपेशा लोगों के साथ मैं रह चुका हूँ और उनके जीवन का अध्ययन मैंने बहुत निकट से किया है; निम्न-मध्यवर्गीय ग्रामीण समाज के प्रति दिन के जीवन के सुख-दु:ख में मैं शरीक रहा हूँ; जिन पतिता नायिकाओं और चरित्रहीन नायकों का चित्रण मैंने अपनी रचनाओं में किया है वे मेरी कोरी कल्पना की उपज नहीं हैं। इस तरह के स्त्री-पुरुषों के संपर्क में मैं रहा हूँ। यह सही है कि उनके जीवन की यथार्थता का नंगा चित्र न खींचकर मैंने उन्हें ‘आइडिएलाइज’ किया है–पर वह अनुभव की कमी के कारण नहीं, अपने भीतरी विश्वास और कला के उद्देश्य के संबंध में अपनी निजी धारणा के कारण। तरह-तरह के आवारा लोगों साथ मेरी घनिष्टता रही है। छोटी-छोटी ‘भूलों’ के कारण समाज से बहिष्कृत स्त्री-पुरुषों के लांछित और उपेक्षित जीवन से मेरा निकटम परिचय रहा है, किसानों और मजूरों के जीवन के संबंध में प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त करने के अलावा मदारियों, सँपेरों, नटों, बहुरूपियों, नागा या अधनंगे साधु-संन्यासियों के साथ मैं जीवन बिता चुका हूँ। गरज यह कि जीवन के किसी भी क्षेत्र के अनुभवों से मैं वंचित नहीं हूँ। फिर भी यदि मेरी रचनाओं में जीवन के प्रचंड हाहाकार और भूकंपी विस्फोटों का चित्रण आपको नहीं मिलता तो उसका कारण कहीं और सोचना होगा। इस देश की सांस्कृतिक और सामाजिक परंपराएँ कुछ ऐसी रही हैं जो जीवन के कठोर यथार्थता को झकझोर कर, उसमें से कटु सत्यों को बटोर कर उन कटु सत्यों के सूक्ष्म विश्लेषण द्वारा आदर्शात्मक सत्यों की स्थापना पर जोर नहीं देतीं। यहाँ कटु यथार्थ को भरसक दबाकर, उसे पृष्ठभूमि में–नेपथ्य में–रखकर, उस वास्तविकता के भीतर दूध में मक्खन की तरह निहित उन्नत आदर्शों को रंगमंच के खुल प्रकाश में रखने की परंपरा प्रचलित रही है। पाश्चात्य देशों के और यहाँ के दृष्टिकोणों का यह अंतर कालिदास और शेक्सपीअर के नाटकों और काव्यों की तुलना से स्पष्ट हो जाएगा। शेक्सपीअर के नाटकों में पात्रों के जीवन के भीतर और बाहर जो भीषण तूफानी बादल उमड़ते रहते हैं, हिंसा-प्रतिहिंसा के जो भयावने चक्कर चलते रहते हैं, ज्वालामुखियों के-से जो विस्फोट और भूकंपों-से जो आंदोलन मचते रहते हैं वे कालिदास की दुनिया के लिए एकदम विजातीय हैं। कालिदास ने केवल करुण और कोमल, शांत और स्निग्ध जीवन के चित्रों को रंगमंच की अग्रभूमि पर रखा है। ‘अभिज्ञान शाकुंतला’ की तुलना ‘हेमलेट’, ‘ओथेलो’ या ‘मेकबेथ’ से करने पर यह बात स्पष्ट हो जाएगी। कालिदास ने दुष्यंत की नीचता और हीनता को पृष्ठभूमि में रखा है, उसकी त्रुटियों और कमजोरियों पर ऐसे काव्यात्मक रंग चढ़ाए हैं जो उनकी उन्नत प्रवृत्तियों को और अधिक उभार में रखते हैं। शकुंतला के विद्रोह को कवि ने केवल छिट-फुट उद्गारों और इंगितों द्वारा व्यक्त किया है। सारे नाटक में आदि से अंत तक एक शांत कोमल, करुण और स्निग्ध वातावरण छाया रहता है। स्थान-स्थान में तूफानी बादल उमड़ते-उमड़ते रह जाते हैं, विस्फोट होते-होते दब जाता है। इसके विपरीत शेक्सपीअर के नाटकों में सर्वत्र भीतर और बाहर–तर्जन-गर्जन, संघर्ष-विघर्ष, विद्रोह और विस्फोट, आँधी और तूफान का जोर रहता है। जीवन के ये दोनों रूप सत्य हैं, दोनों पहलू महत्त्वपूर्ण हैं। फिर भी कालिदास की कला अधिक कठोर है। किसी व्यक्ति के चरित्र-चित्रण या किसी विशेष परिस्थिति के वर्णन के सिलसिले में जितने भी भाव किसी कवि, नाटककार या उपन्यासकार के भीतर उपड़ते हैं उन सबको उगल देना उतना कठिन नहीं है, जितना उन सबको संयत करके, उन्हें दबा कर केवल इंगितों और आभासों द्वारा गहरा असर पैदा करना। कालिदास ने इसी संयमवाली कला को अपनाया था। रूसी लेखक उस शैली से प्रभावित हुए हैं जिसे शेक्सपीअर से लेकर अठारहवीं और उन्नीसवीं शताब्दियों के सुप्रसिद्ध पाश्चात्य-कलाकारों ने अपनाया था। उसका भी अपना महत्त्व है, पर मैं कालिदास की कला का ही कायल हूँ। जीवन के कटु और कठोर सत्य के पूर्ण और सर्वांगीण चित्रण के बिना भी सुंदर कलात्मक अभिव्यक्ति हो सकती है और साथ ही उस महत्त्वपूर्ण सत्य की उपलब्धि भी हो सकती है जो सभी बड़े कलाकारों को अभीष्ट रहा है…”
इस संबंध में मेरा सुस्पष्ट मदभेद था। मैं तब भी कालिदास का बहुत बड़ा प्रशंसक था और आज भी हूँ। प्रशंसक ही नहीं, मैं बराबर कालिदास का बहुत प्रेमी पाठक रहा हूँ। पर बीसवीं शताब्दी में भी, जबकि यथार्थ जीवन के कठोर सत्य की चेतना मानव-मन में अत्यंत निविड़ रूप से घनीभूत हो उठी है, उसी तथाकथित संयमवाली कला पर जोर देना, मेरे मत से, जीवन की सच्चाई से कतराना है। मैं प्रारंभ ही से उस कला का उपासक रहा हूँ जो जीवन की गहराई में पैठकर, परंपरागत बूजुर्वा संस्कारों से निर्मित झूठे आवरणों को पर्दा-दर-पर्दा चीरकर उनके भीतर ढके हुए नग्न सत्य को बाहर निकालती है और उस नग्न सत्य को जीवन की यथार्थता के बीच में लाकर यथार्थवादी उपायों द्वारा एक ऐसे आदर्श की ओर उन्मुख करती है जो यथार्थ पर ही आधारित है। इसके लिए जीवन की उन जटिल गहन परिस्थितियों की अवतारणा आवश्यक है जिन्हें शेक्सपीअर से लेकर डास्टाएव्सीकी तक ने अपनाया है, और साथ ही उन भीतरी और बाहरी परिस्थितियों के सूक्ष्मतम विश्लेषण का भी बहुत बड़ा महत्त्व है।
मैंने शरतचंद्र के आगे अपना यही मत प्रकट किया। साथ ही उनका ध्यान इस बात की ओर भी आकर्षित किया कि भारत में भी इस प्रकार की विराटवादी कला किसी जमाने में अपनाई जा चुकी है और इस संबंध में महाभारत का उल्लेख किया। मैंने कहा कि मैं महाभारत को कोई ऐतिहासिक महाकाव्य नहीं मानता हूँ। जिस महापुरुष ने इस विराट काव्य की रचना की उसने स्वयं एक परंपरा-प्रचलित पौराणिक कहानी का केवल सूत्र पकड़ा था। उस सूत्र से उसने एक ऐसा ढाँचा तैयार किया जो उस महाकवि के स्वयं अपने युग के अस्त-व्यस्त और संघर्षमय जीवन के चित्रण के लिएये ‘फिट’ बैठता था। उसने ऐसे पात्रों और पात्रियों की अवतारणा की जो अपने जटिल और गहन प्रतिभाशाली व्यक्तित्व की परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों के द्वंद्व में बुरी तरह उलझे हुए थे और उस उलझन से मुक्त होने के लिए जो आजीवन संघर्ष करते रहे। केवल उन पात्रों और पात्रियों के जीवन ही नहीं बल्कि, उस सारे युग की धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियाँ बहुत ही उलझी हुई और अस्त-व्यस्त थीं। पर महाभारतकार युग की उन उलझी हुई परिस्तिथियों से कतराना नहीं चाहता था। उसने जानबूझकर, सचेष्ट और सक्रिय रूप से उन घोर यथार्थ और तूफानी परिस्थितियों की अवतारणा की। और उस विराट पृष्ठभूमि में वैयक्तिक और सामूहिक जीवन के ऐसे लोमहर्षक चित्रों, ऐसी जटिल किंतु गंभीर समस्याओं का उद्घाटन किया जो आज के जीवन में भी सत्य उतरता है। और अंत में उन जटिल समस्याओं का समाधान यथार्थ पर आधारित आदर्शात्मक उपायों से किया। महाभारतकार ने जीवन के कठोर और कटु पदार्थ को किस तरह निरावरण रूप में उभारकर रखा है, इसका एक उदाहरण यह है कि उसने एकवस्त्रा रजस्वला दौपदी को नीच दु:शासन द्वारा बीच सभा में खड़ा करवाया। यदि वह कालिदासीय संयत कला का कायल होता तो उस चीर-हरण संबंधी घटना का इंगित मात्र देकर चुप लगा जाता। पर नहीं; उसने नारी जाति के ऊपर पुरुष जाति द्वारा किए जाने वाले अत्याचार के उस चरम प्रतीक पर पूरा ‘फोकस’ डाला है और उस घटना पर अत्यधिक महत्त्व आरोपित करके पूरे विस्तार से उसका वर्णन किया है। इसके पूर्व महाभारत के प्रधान नायक धर्मराज युधिष्ठिर का जुए के नशे में अंधा हो कर अपनी पत्नी तक को दाँव में लगाने की घटना पर भी महाभारतकार ने पूरा प्रकाश डाला है, यह उसकी यथार्थवादिता का एक दूसरा लघु उदाहरण है। व्यक्तिगत और वंशगत हिंसा-प्रतिहिंसा और राग-द्वेष की परिणति सामूहिक हिंसा, विध्वंस और विनाश में दिखाने के उद्देश्य से उसने बीच में जिस व्यापक जीवन-संघर्ष, द्वंद्व-प्रतिद्वंद्व, उत्थान-पतन, भीतरी और बाहरी चक्रों के घात-प्रतिघात का चित्रण किया है वह उस विराट कलात्मक प्रतिभा का चरम निदर्शन है जिसका एक अस्फुट स्वरूप हम शेक्सपीअर की समन्वित रचनाओं में पाते हैं। महाभारतकार की घोर यथार्थवादी और घनघोर जीवनवादी प्रवृत्ति का सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि कृष्ण जैसे मानव-जाति के महान नेता को, जो सांस्कृतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक प्रगति और सामूहिक शांति के प्रमुख आचार्य थे, उस युग की उलझी हुई राजनीतिक (राष्ट्रीय और अंतर-राष्ट्रीय) समस्याओं का हल एकमात्र महायुद्ध–सामूहिक हिंसा–में ही दिखाई दिया। युद्ध के निवारण के लिए उन्होंने पूरी शक्ति से उद्योग किया; पर सफल न होने पर उन्होंने युद्ध की पूरी तैयारी के लिए जोर दिया। यह नहीं कहा कि “चाहे सारे महादेश में अत्याचारी कौरवों का एकच्छत्र राज हो जाए, पांडवों को चाहिए कि विश्व-शांति के रक्षार्थ युद्ध से विरत रहें और निपट दीनता का जीवन बिताते हुए संतोष कर लें।”
महाभारत की उक्त विशेषताएँ बताते हुए मैंने शरतचंद्र से कहा कि मैं उक्त महाकाव्य को संसार का सबसे पहला यथार्थवादी उपन्यास मानता हूँ। शरतचंद्र ने मेरी बातें बड़े ध्यान से सुनीं और इस बात पर आश्चर्य प्रकट किया कि इतनी कच्ची उम्र में ही–तब मेरी उम्र प्राय: बीस वर्ष की रही होगी–मैं जीवन के ऐसे गंभीर और जटिल पहलुओं में रस लेने लगा हूँ। उन्होंने कहा, “मेरे पास जो भी नवयुवक आते हैं वे प्राय: सभी देवदास की दुनिया की सीमा के भीतर ही भूले-से लगते हैं। वे मेरे प्रशंसक होते ही केवल इस कारण हैं कि मैंने देवदास, पार्वती और उन्हीं की तरह के दूसरे पात्र-पात्रियों के विफल रोमांटिक प्रेम का चित्रण बड़ी ही मार्मिकता से किया है (जैसा कि वे बताते हैं)। आप मुझे पहले ऐसे नवयुवक मिले जो उपन्यासों में यथार्थ जीवन के गहन प्रश्नों की खोज करते हुए उनके आदर्शात्मक हल में दिलचस्पी लेते दिखाई देते हैं। यह बात मैं किसी प्रशंसा की दृष्टि से नहीं कह रहा हूँ। क्योंकि मेरी राय में यह आप में एक ‘एबनार्मल’ प्रवृत्ति है जो आपको इस भरी जवानी में एक बहुत बड़े रस से वंचित कर सकती है। वह रस है रोमांटिक रस। इस रस को उन लोगों ने बहुत बदनाम कर रखा है जो प्रेमतत्व की गहराई के संबंध में बहुत ही छिछला दृष्टिकोण रखते हैं। मैं मानता हूँ कि रोमांटिक रस ही जीवन का मूल रस नहीं है। जीवन का क्षेत्र बहुत विस्तृत है; फिर भी यह रस किसी भी दृष्टि से उपेक्षणीय नहीं है, क्योंकि उसके भीतर ऐसे बीज निहित हैं जो ठीक ढंग से पनपने पर अपनी शाखाओं और प्रशाखाओं को जीवन के विविध क्षेत्रों में विचित्र रूपों में फैला सकते हैं। सच तो यह है कि व्यापक दृष्टि से देखने पर जीवन का कोई भी क्षेत्र उससे छूटा नहीं लगेगा। इसलिए आपको इस संबंध में सावधान रहने की आवश्यकता है कि यह जो सहज स्वाभाविक रस है, जिसका अनुभव आप ही की उम्र में अधिक तीव्रता के साथ किया जा सकता है; कहीं आप जीवन की गहन गंभीर समस्याओं की जटिलता में उलझकर उसके प्रति एकदम उदासीन न हो जाएँ…”
मैंने मंद-मंद मुस्कराते हुए कहा–“यदि ऐसी बात होती तो मैं आपकी रचनाओं के प्रति आकर्षित ही न होता। मेरा अपना ऐसा अनुमान है कि रोमांटिक रस मुझ में सूख नहीं रहा है, बल्कि संभवत: और गहरा होता जा रहा है। जीवन के गहन-गंभीर प्रश्नों में मैं जो अभी से दिलचस्पी लेने लगा हूँ उसका एक कारण यह भी हो सकता है कि ‘रोमांटिक रस’ को मैं गहरे ही रूप में ग्रहण करना पसंद करता हूँ, छिछले रूप में नहीं। देवदास की दुनिया को मैं जो गंभीर रूप से ग्रहण नहीं कर पाता उसका भी कारण मुझे यही लगता है। देवदास और पार्वती के पारस्परिक प्रेम और उसकी प्रतिक्रिया को मैं एक हलके ढंग की भावुकता मानता हूँ, जिस पर केवल आपकी कलात्मक प्रतिभा ने एक गहरा रंग चढ़ा दिया है।”
“देवदास के संबंध में मैं आपकी बात से कुछ अंशों तक सहमत हूँ। सच बात यह है कि यह उपन्यास मैंने तब लिखा था जब मेरी अवस्था केवल उन्नीस वर्ष की थी–हालाँकि वह छपा है कई वर्षों बाद…” हुक्का जोर से गुड़गुड़ाकर उससे अधिकाधिक धुआँ निकालने का प्रयत्न करते हुए शरतचंद्र ने कहा, पर धुआँ कुछ विशेष निकला नहीं। बहस के दौरान में हुक्का पीना वे भूल गए थे, और इस बीच चिलम ठंढी हो गई थी।
उन्होंने नौकर को पुकारा और चिलम को ताजा करने का आदेश दिया।
“यह कौन-सी पुस्तक आप लाए हैं?” मेज पर बहुत देर से उपेक्षित पड़ी हुई मेरी ‘चयनिका’ पर दृष्टि डालते हुए उन्होंने कहा। “जरा देखूँ…”
मेरे आगे यह स्पष्ट हो गया कि जो बहस चल रही थी उसे वह खतम करना चाहते हैं।
‘चयनिका’ खोलकर, दो-चार पृष्ठ उलटकर उन्होंने उसे रख दिया। फिर बोले, “आप रवींद्र की कविता के बहुत बड़े प्रेमी मालूम होते हैं, और यह स्वाभाविक भी है।”
“आपने यह अनुमान कैसे लगाया?” मैंने पूछा।
“इसमें कौन कठिनाई है! बहुत बढ़िया चमड़े में बँधी हुई पुस्तक को आप हाथ में लिए फिर रहे हैं, वही काफी प्रमाण है; फिर आपकी बातों के ढंग से भी यह अनुमान लगाना कठिन नहीं है कि जीवन के बहुविध रूपों को पूर्णतया अपनाने वाले विराट कवि की कविता में आपको वह रस भरपूर मिलेगा जिसकी गहरी पिपासा आपके भीतर छिपी है।”
मैंने पुलकित होकर कहा, “मैं आजकल प्रतिदिन उनकी कविता का पाठ करता हूँ।”
“यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, मैं स्वयं प्रतिदिन नहीं तो हर तीसरे-चौथे रोज उनकी कई कविता-पुस्तक लेकर बैठ जाता हूँ। इतना बड़ा कवि आज संसार में खोजे न मिलेगा।”
“आप क्या उनकी प्रत्येक कविता का अर्थ आसानी से समझ लेते हैं?” अपनी ढिठाई पर तनिक भी लज्जित न होकर मैंने पूछा। यदि सच पूछा जायए, तो मैं केवल इसी एक प्रश्न के उद्देश्य से ‘चयनिका’ को अपने साथ लेता गया था। रवींद्र की संपूर्ण कविताओं का अध्ययन मैंने अकेले ही किया था। एक भी गुरु मुझे नहीं मिला था और यदि गुरु मिला भी होता तो मैं संभवत: उसके पास न जाता। क्योंकि प्रारंभिक जीवन में मैं बहुत संकोचशील था। इसलिए पूर्णत: स्वचेष्टित उपायों से बड़ी कठिनाई के साथ उनकी अधिकांश कविताओं का अर्थ संतोषजनक रूप से समझ पाने में समर्थ हो पाया था। फिर भी कुछ कविताएँ ऐसी रह गई थीं जिनका कुछ भी निश्चित अर्थ मेरी समझ में नहीं आता था। अतएव कोई दूसरा रवींद्र-काव्य-प्रेमी उन्हें किस रूप में समझ पाता है यह जानने के लिए मैं बहुत दिनों से उत्सुक था। इसके भीतर किसी हद तक निश्चय ही मेरा यह बाल-अहंकार काम कर रहा था कि रवींद्र की जो कविता किसी भी उपाय से मेरी समझ में नहीं आती उसे कोई दूसरा कैसे समझ सकता है, फिर चाहे वह कैसा ही विद्वान और प्रतिभाशाली क्यों न हो।
जो भी हो, मेरे ढीठ प्रश्न के उत्तर में शरतचंद्र ने शांत भाव से धीरे-धीरे हुक्का गुड़गुड़ाते हुए कहा, “हाँ। मुझे तो पूरा विश्वास है कि उनकी किसी भी कविता का अर्थ मेरे आगे अस्पष्ट नहीं रह गया है।”
मैंने ‘चयनिका’ हाथ में लेकर पन्ने उलटे और एक चिह्नित कविता खोलकर पुस्तक उनके आगे बढ़ाते हुए कहा–“मैं इस कविता का अर्थ जानना चाहता हूँ। इसके पीछे मैं बहुत माथापच्ची कर चुका हूँ।”
उन्होंने हुक्का छोड़कर आँखों में चश्मा जमाया और कविता को देखने लगे। वह थी रवींद्रनाथ की सुप्रसिद्ध ‘सोनार तरी’ शीर्षक कविता। देखते ही मुस्कराते हुए बोल उठे–“यही एक कविता आपने ऐसी दिखाई जिसका अर्थ स्वयं रवींद्रनाथ नहीं बता पाते–लोगों ने उनसे पूछकर देखा है। तरह-तरह के पंडित लोग इसका तरह-तरह का अर्थ लगाते हैं, और प्रत्येक का अर्थ एक-दूसरे का विरोधी पड़ता है। अकेली यही नहीं, इसी ‘सिरीज’ की कुछ और भी कविताएँ हैं जिनका निगूढ़ रहस्यात्मक अर्थ समझ पाना कठिन है…” कहते हुए उन्होंने चश्मा उतार कर रख दिया और फिर हुक्का गुड़गुड़ाने लगे।
बंगला-प्रेमी पाठकों की जानकारी के लिए मैं पूरी कविता को नीचे उद्धृत करता हूँ–
गगने गरजे मेघ घन वरषा।
कूले एका बसे आछि नाहि भरसा।
राशि राशि भाराभारा धान काटा होलो सारा
भरा नदी क्षुर धारा खर-परशा।
काटिते-काटिते धान एलो वरषा।
एकखानि छोटो खेत आमि एकेला,
चारिदिके बाँका जल करिछे खेला।
परपारे देखि आँका तरुछाया मसीमाखा,
ग्रामखानि मेघे ढाका प्रभात वेला।
गान गेये तरी बेये के आसे पारे।
देखे जेन मने हय चिनि उहारे।
भरा पाले चले जाय होनो दिके नाहि चाय,
ढउगुलि निरुपाय भाड़े दुधारे।
ओगो तुमि कोथा जाओ कोन विदेशे।
बारेक भिड़ाओ तरी कूलेते एसे।
जेयो जेथा जेते चाओ जारे खुशी तारे दाओ,
तुमि शुधु निये जाओ क्षणिक हेसे
आमार सोनार धान कूलेते एसे।
जग चाओ तत लओ तरणि परे।
आरो आछे–आर नाई दियेछि भरे।
एतकाल नदी कूले जाहा लये छिनु भूले
सकलि दिलाम तुले थरे बिथरे
एखन आमारे लहो करुणा करे।
ठाँइ नाई ठाँइ नाई छोटो से तरी
आमारि सोनार धाने गियेछे भरि
श्रावण-गगन घिरे घन मेघ घूरे फिरे,
शून्य नदीर तीरे रहिनु पड़ि,
जाहा छिलो निये गेलो सोनार तरी॥
इस कविता के शब्दार्थ से यह सार निकलता है कि वर्षाकाल है, प्रभात का समय है, बादल गरज रहे हैं और झमाझम पानी बरस रहा है। कवि उमड़ती हुई नदी के किनारे एक छोटे से खेत पर हताश भाव से अकेला खड़ा है, जहाँ बहुत-सा धान कट चुका है। इतने में उस पार से एक नाव में बैठकर कोई गान गाता हुआ इस पार की ओर आता है। कवि की अंतरात्मा को सूरत पहचानी भी लगती है, हालाँकि वह प्रकट में कोई अनजान विदेशी-सा मालूम होता है। उस अजनबी को देखकर कवि के मन में यह इच्छा जगती है कि उस पर अपना सर्वस्व निछावर कर दे। वह उस विदेशी से प्रार्थना करता है कि “तुम अपनी नाव को किनारे पर लगाकर मेरे इन सब सोने की तरह पके हुए धानों को प्रसन्न मन से ले जाओ, उसके बाद फिर जिसे चाहो दे देना।” जब नाव धान की बालियों से भर जाती है तब वह कहता है कि “इतने दिनों तक मैं जिस संपत्ति को लेकर नदी के किनारे भूला हुआ पड़ा था वह सब मैं अब तुम्हें अर्पित कर चुका हूँ। अब करुणा करके तुम मुझे भी अपने साथ लिए चलो।”
पर वह छोटी-सी नाव धान से इस कदर भर चुकी है कि उसमें कवि के लिए स्थान नहीं रह जाता, और वह शून्य नदी के किनारे ही पड़ा रह जाता है।
कुछ भाष्यकारों को यह मर्ज होता है कि कोई कविता चाहे कैसी ही ‘फेंटेस्टिक’ क्यों न हो, उसका कुछ न कुछ अर्थ वे अवश्य ही कविता को तोड़-मरोड़कर निकालेंगे ही। रवींद्र की इस कविता का भी मनमाना अर्थ लगाने का प्रयत्न बहुत से तथाकथित पंडितों ने किया है। पर सब बुरी तरह असफल और परस्पर विरोधी सिद्ध हुए हैं। यदि हम इस कविता को रहस्यवादी कवि के किसी विशेष ‘मूड’ में निकली हुई ‘फेंटेसी’ माने, तो इस रूपक का यह अर्थ लगाया जा सकता है कि सहसा किसी दिव्य प्रेरणा के फलस्वरूप कवि के अंतर्जगत में एक ऐसी आश्चर्य प्रकाश-मूर्ति का अविर्भाव हुआ कि कवि समस्त भौतिक बंधनों या अपने भीतर उतने दिनों तक पाली हुई समस्त लौकिक धारणाओं के जाल से मुक्त होकर उसी दिव्य चेतना के प्रति अपना सब कुछ अर्पित कर देना चाहता है और स्वयं भी उसी में लीन हो जाने की इच्छा रखता है। कवि की ‘फेंटेसी’ को अपनी कल्पनानुसार तोड़-मरोड़कर किसी तरह इतनी दूर तक तो घसीटा जा सकता है, पर अंतिम पद फिर से एक नई ही उलझन में डाल देता है। अंतिम पद का शब्दार्थ इस प्रकार है।
“उस छोटी-सी नाव में मेरे लिए जगह नहीं रह गई है। वह तो मेरे धान की सोने की बालियों से ही भर गई है। श्रावण के गगन को घेर कर घने बादल उमड़ रहे हैं, और मैं सुनसान नदी के किनारे अकेला रह गया हूँ। मेरा जो कुछ था वह सोने की नाव उठा ले गई।”
इसे पढ़कर स्पष्ट ही यह प्रश्न उठता है कि वह दिव्य प्रकाश-मूर्ति इतनी सीमित और संकीर्ण कैसे हुई कि उसकी छोटी-सी नाव में केवल कवि के अंतर में अंकुरित हुए सोने के धान की बालियों के समान भाव ही भरे जा सके और स्वयं कवि की आत्म-चेतना उसमें विलीन होने के लिए स्थान न पा सकी? इसी प्रकार किसी भी छायात्मिका कल्पना का रूपक उस कविता के ढाँचे के भीतर ‘फिट’ करने का प्रयत्न कीजिए वह कहीं न कहीं अवश्य गड़बड़ा जाएगा।
शरतचंद्र ने कहा–“इस कविता को या इसी ‘सिरीज’ की कुछ और कविताओं को छोड़ दीजिए, रवींद्रनाथ की शेष सब कविता साफ और सुलझी हुई है। रवींद्रनाथ ने भाव-जगत् का एक भी ऐसा क्षेत्र नहीं छोड़ा है जिसे कवित्व के भीतर न बाँधा हो। और उन सर्वग्राही भावों के परिस्फुटन के लिए उन्होंने विविध शैलियों और विभिन्न रूपकों को अपनाया है। ऐसी हालत में यह स्वाभाविक है कि कुछ थोड़ी-सी कविताएँ अत्यधिक रहस्यात्मक और अस्पष्ट रह गई हैं। उन थोड़ी सी कविताओं के कारण कुछ आलोचकों ने उन्हें बदनाम कर रखा है, और कुछ तो उनकी सभी कविताओं को निरर्थक शब्दजाल तक सिद्ध करने पर तुले हैं। सच बात यह है कि इस तरह के आलोचक किसी बड़े कवि की किसी भी कविता का अंतर्भाव समझने योग्य न तो बुद्धि ही रखते हैं न हृदय। श्रेष्ठ कवियों की कविताओं को समझने के लिए सबसे पहले यह आवश्यक है कि पाठक ने कवि-हृदय पाया हो, और दूसरी आवश्यकता इस बात की है कि वह कविता की विभिन्न शैलियों, रूपकों और सांकेतिक भाव-चित्रों की अभिव्यंजना के तौर-तरीकों के संबंध में शिक्षा पाया हुआ हो, इन दोनों शर्तों की पूर्ति न होने पर कवि की सुस्पष्ट कविता भी समझ में न आ सकेगी। जिस ‘गीतांजलि’ पर रवींद्रनाथ को नोबेल पुरस्कार मिला था उसकी कविताएँ कैसी सरल और सुस्पष्ट हैं, यह आप जानते ही होंगे पर वे सरल और सुस्पष्ट कविताएँ भी उन लोगों को अस्पष्ट और छायात्मक लगने लगती हैं जिन्हें अंतर्भावनाओं को चित्रित करने वाले सांकेतिक रूपकों के संबंध में कोई जानकारी नहीं है।…”
वाद-विवाद में काफी देर हो चुकी थी, मैं उनका मूल्यवान समय अधिक नष्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं सहसा उठ खड़ा हुआ और हाथ जोड़ता हुआ चलने की आज्ञा माँगने लगा।
“अभी कुछ देर और बैठिए, चाय आ रही है।”
इस प्रेम-भरे आदेश को मैं भला कैसे टाल सकता था? अत्यंत प्रसन्न होकर बैठ गया। प्राय: दूसरे ही क्षण नौकर दो प्यालों में चाय लाकर रख गया। चाय पीते हुए शरतचंद्र ने पूछा–“आपने अभी तक क्या-क्या लिखा है, अभी क्या लिख रहे हैं और आगे क्या लिखने का विचार है?”
मैंने कहा, “अभी तक मैंने कुछ कहानियाँ, कविताएँ और साहित्यिक निबंध ही लिखे हैं, जो अभी तक पुस्तक-रूप में नहीं छपे हैं। आगे क्या लिखूँगा, अभी से इस संबंध में कुछ नहीं कह सकता। वैसे उपन्यास लिखने की ओर मेरा रुझान है। इस समय कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ।”
“तब आप मेरे उपन्यासों का अनुवाद हिंदी में क्यों नहीं कर डालते!” उन्होंने सहज भाव से कहा।
यह प्रस्ताव उनकी तरफ से आएगा, इसका स्वप्न भी मैं नहीं देख सकता था। और साथ ही यह भी उतना ही सत्य है कि मैंने स्वयं कभी उनके उपन्यासों के अनुवाद की बात नहीं सोची थी। उनके उस आकस्मिक और अप्रत्याशित प्रस्ताव ने मेरे भीतर एक द्वंद्व उत्पन्न कर दिया। सच बात यह है कि प्रारंभ ही से मेरे मन में यह (गलत या सही) धारणा जम चुकी थी कि अनुवाद का काम किसी भी ऐसे लेखक के लिए अपमानकर है जो अपने भीतर मौलिक विचारों की प्रेरणा पाता है। कम से कम अपने लिए तो मैं यह निश्चय कर चुका था कि मैं कभी किसी लेखक की किसी भी रचना का अनुवाद नहीं करूँगा। उन दिनों हिंदी में कथा साहित्य संबंधी मौलिक रचनाओं का बहुत अभाव था और बंगला के तीसरी और चौथी श्रेणी के लेखकों की भी रचनाएँ पेशेवर अनुवादकों द्वारा धड़ल्ले से अनुवादित होकर छपती चली जाती थीं। संभवत: इस बात की भी कुछ प्रतिक्रिया मेरे मन में हुई हो। या यह भी संभव है कि यह मेरे घमंडी मन की ही जिद रही हो, जो हिंदी साहित्य के भीतर गहन गुफा में छिपे हुए बीजों को निकाल कर उन्हें उपयुक्त मिट्टी में बो कर उनके दूसरे साहित्य की छाया से अलग रहकर अच्छी तरह पनपने उन्नततम रूपों में विकसित होने का स्वप्न देख रहा था।
कारण जो भी रहा हो, मैं अनुवाद के लिए राजी न हुआ और विनम्र भाव से हाथ जोड़कर क्षमा याचना का भाव जनाते हुए बोला : “अभी आप मुझे क्षमा करें। इसके अलावा, मेरी कुछ ऐसी धारणा है कि अभी आपके साहित्य के स्वागत के लिए पूरी तरह से उपयुक्त वातावरण भी हिंदी जगत में तैयार नहीं हुआ है।” मैं जानता हूँ कि जो दूसरा कारण मैंने बताया था वह गलत था। पर मैं किसी तरह शिष्टापूर्वक उस प्रस्ताव को टाल जाना चाहता था।
चाय पीकर मैं नमस्कारपूर्वक विदा हुआ।
Image: Still life. Vase with flowers on the window
Image Source: WikiArt
Artist: Paul Gauguin
Image in Public Domain
