शरतचंद्र संबंधी मेरे संस्मरण
- 1 September, 1951
शेयर करे close
शेयर करे close
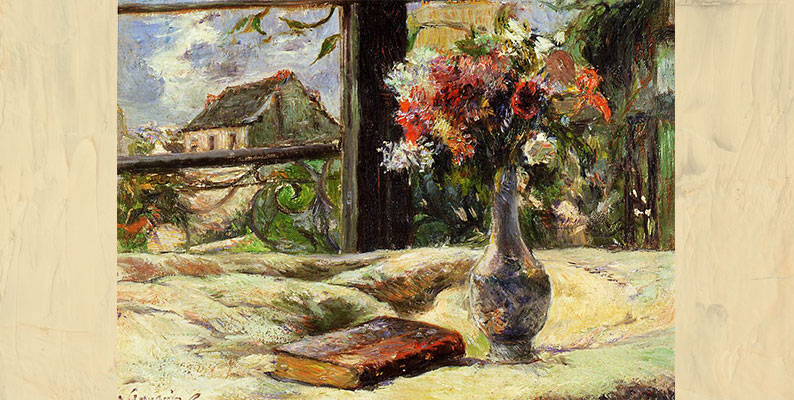
शेयर करे close
- 1 September, 1951
शरतचंद्र संबंधी मेरे संस्मरण
शरतचंद्र का पहला परिचय मुझे उनकी जिस रचना द्वारा मिला था वह था उनका सबसे नीरस उपन्यास–‘पल्ली-समाज’। तब हिंदी में ऐसे लोगों की संख्या नहीं के बराबर थी जो शरत् के नाम से भी परिचित रहे हों। उन दिनों मैं एक स्कूली लड़का था, पर बंगला साहित्य की तत्कालीन गतिविधि से बहुत-कुछ परिचित हो चुका था। तब बंगला मासिक पत्रों में शरतचंद्र की क्रांतिकारी प्रतिभा की काफी चर्चा होने लगी थी, इसलिए उनकी रचनाएँ पढ़ने के लिए मैं उत्सुक हो उठा। ‘पल्ली-समाज’ उन दिनों गुरदास चटर्जी की आठ आना ग्रंथमाला के अंतर्गत ताजा-ताजा निकला था। इसलिए सबसे पहले उसी को मैं पढ़ने लगा। मुझे वह एक विचित्र ही चीज लगी। उसमें न तो प्रचलित अर्थ में कोई नायक ही था न नायिका। न तो सारे उपन्यास में रोमांस की रंगीनी का ही कोई लेश था, न पाठकों का कुतूहल उभारती रहने वाली घटनाओं की बहुलता। उसमें था केवल दु:ख-दैन्य से पीड़ित, संकीर्ण सांस्कृतिक घेरे के भीतर बंधे हुए, परंपरा-प्रचलित कुसंस्कारों से घिरे हुए बंगाल के निम्न-मध्यवर्गीय देहाती समाज का सीधा-सादा यथार्थ चित्रण। उपन्यास का सारा वातावरण मुझे एकदम विजातीय, अपरिचित-सा लगा। पर यह सब होने पर भी लेखक की वर्णन और चित्रण शैली ऐसी सजीव और आकर्षक लगी कि मैं बड़े धैर्य से उसे अंत तक पढ़ गया। उस ‘नीरस’ उपन्यास के वास्तविक महत्त्व का अनुभव मुझे बाद में हुआ।
पर उस रचना को पढ़ने के बाद लेखक की अन्य रचना को पढ़ने की उत्सुकता मुझे नहीं हुई। उसके प्राय: एक वर्ष बाद मेरे हाथ शरत् की एक ग्रंथावली लग गई, जो वसुमती कार्यालय से प्रकाशित हुई थी। उसमें उनके कई उपन्यास और कहानियाँ एक साथ संगृहीत थीं–‘बैकुंठेर उइल’, ‘चंद्रनाथ’, ‘बड़ दीदी’, ‘स्वामी’, आदि। उनके बाद तब तक प्रकाशित शरतचंद्र के सभी उपन्यास और कहानियाँ मैंने पढ़ी–‘चरित्रहीन’, ‘देवदास’, ‘श्रीकांत’, ‘दत्ता’, ‘पंडित मोशाई’, ‘विराज बऊ’, ‘बिंदुर’, ‘छेले’, आदि-आदि। उन्हें पढ़कर भारतीय निम्न-मध्यवर्गीय समाज की ऐसी सजीव झाँकियाँ मेरी किशोर-वयस्क आँखों के आगे से होकर गुजरती चली गईं जिन्हें किसी तरह भी भुलाया नहीं जा सकता था। वह सारी चित्रावली एक ऐसे सूक्ष्म निरीक्षक द्वारा अंकित लगीं जिसकी केवल बाहरी दृष्टि ही पैनी नहीं थी, बल्कि अंतर्दृष्टि भी सीधे मर्म में प्रवेश करने वाली थी। एक पूर्णत: नई दुनिया मेरे आगे उद्घाटित हो गई, जिससे मुझे इस कच्ची उम्र में ही जीवन और जगत के सूक्ष्म, गहन और व्यापक अध्ययन के लिए प्रेरणा मिलने लगी। निम्न-मध्यवर्गीय सामाजिक और गार्हस्थिक परंपरा में पले हुए आलसी और निकम्मे किंतु भावुक और कवि-हृदय नवयुवकों के ऊपर बाहरी दुनिया से पड़ने वाले प्रभाव के फलस्वरूप उनमें धीरे-धीरे जो सामाजिक भावना जग रही थी वह उनकी चारित्रिक दुर्बलता के कारण किस प्रकार आत्म-विद्रोह में परिणत हो रही थी इसका निदर्शन शरत् ने आश्चर्यजनक कला-कौशल के साथ किया था। उनकी जादू भरी तूलिका अपने चित्रों में ऐसे आकर्षक रंग भरती जाती थी जो उनके पात्रों की दुर्बलता जनित विकृतियों को भी अपूर्व सुंदर और सम्मोहक रूप में पाठकों के आगे रखती थी। किशोर हृदय सबसे अधिक भावुक होता है, इसलिए शरत् का जादू मेरे सिर पर चढ़ कर बोलने लगा था। उनकी पात्रियों का व्यक्तित्व उनके पात्रों से कुछ कम आकर्षक नहीं था। उनके पात्र जितने ही उच्छृंखल, चरित्रहीन, इच्छाशक्ति-रहित और सस्ते ढंग की भावुकता से ग्रस्त थे, उनकी पात्रियाँ उतनी ही संयत, दृढ़ चरित्र-शक्ति-संपन्न और गंभीर भाव प्रवणता से प्रेरित थीं। दोनों अंध सामाजिक परिस्थितियों से विद्रोह करने के लिए छटपटा रहे थे, पर पुरुष-पात्रों का विद्रोह जहाँ आत्मघात का पथ पकड़ने को आतुर था वहाँ स्त्री पात्रों की विद्रोह-भावना आत्म त्याग द्वारा अपनी अंत: प्रवृत्तियों के अधिकाधिक उदात्तीकरण की ओर उन्मुख हो रही थी। उन स्त्री-पात्रों के चरित्र की समुद्रवत अतल गहराई के ऊपर शरत् के चंचल-प्राण पुरुष पात्र फेनिल लहरों की तरह उमड़ते और टूटते चले जा रहे थे। कुल मिलाकर शरत् के पात्र-पात्रियों का सम्मिलित संसार मेरे किशोर मन पर एक अजीब रहस्यमय प्रभाव छोड़ता चला जा रहा था।
प्राय: दो वर्ष बाद मैं अपने चारों ओर की बंधनग्रस्त परिस्थितियों से उकताकर भागकर कलकत्ते चला गया–वहाँ के विशाल जन-समूह के बीच में अपने लिए मुक्ति का पथ खोजने की दुराशा से। पर एक दूसरा कारण भी मेरे कलकत्ता भागने की प्रेरणा के पीछे था। कलकत्ता जाकर शरत् की दुनिया को प्रत्यक्ष देखने की आकांक्षा मेरे मन में बहुत दिनों से थी। और साथ ही उस महापुरुष के दर्शन करने की भी तीव्र इच्छा थी जिसने एक नए ही संसार को मेरे आगे पर्दा-दर-पर्दा खोल दिया था। शरत् ने अपने उपन्यासों और कहानियों में कलकत्ते के जिन-जिन स्थानों का उल्लेख किया था उन्हें देखने के लिए मैं कुछ दिनों तक दिनभर और रात में बहुत देर तक पैदल चक्कर लगाता रहा। इस प्रकार चीतपुर (जहाँ भग्नहृदय देवदास अपने को गले तक गंदगी में डुबोकर आत्महत्या कर रहा था), चोर-बगान (जहाँ बिजली अपने भीतर में प्रस्फुटित सहस्रदल कमल को स्वयं अत्यंत निममता से कुचलकर कीचड़ में लोटती हुई मोहवश अपने नारी हृदय के मूल्य को एकदम भूली हुई थी, और जहाँ सहसा उसने एक दिन तूफानी झोंके से, बिजली की झलक में, सत्य को पाया था) और पाथुरेघाटा (जहाँ ‘चरित्रहीन’ की अत्यंत रहस्यमई पात्री किरणमयी तीव्र अंतर्द्वंद्वों के कठोर आघात-प्रतिघातों का अनुभव करती हुई पति सेवा और पर पुरुष सेवा के बीच की उलझन में पड़ी हुई थी), आदि स्थानों के गंदे और अभावग्रस्त जीवन के बाहरी निरीक्षण और ऊपरी अध्ययन का थोड़ा बहुत अवसर मुझे मिला। भीतरी निरीक्षण और गहरे अध्ययन के योग्य न तब मेरी उम्र ही थी, न प्रवृत्ति ही।
पहली बार कलकत्ता पहुँचने के प्राय: एक वर्ष बाद तक मेरा मानसिक वातावरण एकदम शरतमय बना रहा। तब मेरी उम्र प्राय: बीस वर्ष की होगी। मैं सारी दुनिया को शरत् की ही आँखों से देखता था और उन्हीं के पात्रों और पात्रियों को सर्वत्र खोजता फिरता रहता था। शरतचंद्र से मिलने की तीव्र लालसा हर समय मन में बनी रहती थी, पर उन दिनों मैं अत्यंत संकोचशील था, और जिस व्यक्ति की प्रतिभा ऐसे प्रबल रूप से मेरे ऊपर छाई थी उसके पास फटकने का साहस मुझे नहीं हो पाता था। अंत में जब उस लालसा ने दुर्दमनीय रूप धारण कर लिया तब एक दिन मैंने हिम्मत बाँधकर एक जवाबी कार्ड उनके प्रकाशक को लिख भेजा जिससे उनका पता मैंने जानना चाहा था। उत्तर बिना विलंब के मिल गया। मालूम हुआ कि शरतचंद्र हावड़ा के पास शिवपुर नामक स्थान में रहते थे। पत्र में न कोई दिशा-निर्देशन था, न मकान का नंबर ही बताया गया था। बहुत संकल्प-विकल्प के बाद अंत में एक दिन मैं अपने बहु आकांक्षित मंदिर की खोज में निकल ही पड़ा। हावड़ा स्टेशन पार करके ट्राम पकड़ी और जहाँ तक ट्राम जाती थी वहाँ तक चला गया। ट्राम के अंतिम स्टेशन पर उतर कर लोगों से पूछता हुआ एक ऐसी जगह चला गया जहाँ का वातावरण बिलकुल देहाती लग रहा था। जगह-जगह ताड़, नारियल और सुपारी के पेड़ लगे हुए थे और उनके बीच से होकर छोटी-छोटी कच्ची सड़कें अज्ञात दिशाओं की ओर चली गई थी। बीच-बीच में खाई, खंदक और नाले भी पार करने पड़ते थे। इधर-उधर एक दूसरे से काफी दूरी पर छोटे-छोटे बंगलों की तरह के मकान बने हुए थे।
रास्ते में जो भी मिलता उसी से मैं पूछता कि विख्यात उपन्यास-लेखक शरतचंद्र चट्टोपाध्याय कहाँ रहते हैं? दो-एक मिनट तक काफी सोच-विचार करने के बाद भी कोई बता नहीं पाता था। प्राय: एक घंटे तक मैं इधर-उधर चक्कर काटता रहा और लोगों से पूछता रहा पर कोई फल नहीं मिला। मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं था कि इतने बड़े लेखक का पता शिवपुर जैसे छोटे स्थान में नहीं लग पा रहा है। अंत में एक सज्जन ने कहा–“हाँ, हाँ शरतचंद्र चट्टोपाध्याय यहाँ रहते हैं।” और उन्होंने पूरब की ओर उँगली करके एक सफेद मकान दिखाया। कहा कि वही शरत् बाबू का मकान है।
तब तक मैं इस कदर थक चुका था कि उनसे पूछने और कहने के लिए जो-जो बातें मैंने सोच रखी थीं उन सबको भूल गया था। मैंने सोचा कि मकान का पता तो अब लग ही गया है, इसलिए यह अच्छा होगा कि मैं कल ताजा हो कर आऊँ और तब मिलूँ।
दूसरे दिन सबेरे ही मैं अपने कलकत्ता-स्थित वासस्थान से रवाना हो गया। हावड़ा पार करके जब शिवपुर पहुँचा तो उत्सुक और साथ ही आशंकित हृदय से धीरे-धीरे कदम रखता हुआ उसी सफेद मकान के दरवाजे पर पहुँचा। वहाँ एक अधेड़ सज्जन दतौन कर रहे थे। मैंने उनसे कहा कि मैं शरत् बाबू से मिलना चाहता हूँ। उन्होंने कहा–“कहिए, क्या काम है? मैं ही हूँ।” तब तो मैंने अत्यंत श्रद्धापूर्वक हाथ जोड़े और संकोच-जड़ित स्वर में उन्हें बताया कि उनकी रचनाएँ पढ़कर मैं किस कदर प्रभावित हुआ हूँ, और उनसे मिलने की तीव्र इच्छा बहुत दिनों से थी, जो आज पूरी हुई है; आदि-आदि। पहले वह कुछ समझे नहीं, फिर बोले–“ओह! आप उपन्यासकार शरत् चाटुज्जे से मिलना चाहते हैं?” मेरा उत्साह एकदम ठंडा पड़ गया। मालूम हुआ कि स्वयं उन सज्जन का नाम भी शरतचंद्र चट्टोपाध्याय है, पर वह उपन्यासकार नहीं है। मैंने हताश भाव से कहा–“जी हाँ।”
“वह उस तरफ रहते हैं।” कहकर उन्होंने उत्तर की ओर उँगली दिखाई–“वह जो उस गली के बाईं ओर लाल मकान दिखाई दे रहा है, वहीं वह मिलेंगे।”
निराश मन से मैं उसी मकान की ओर बढ़ा। निर्दिष्ट मकान पर पहुँचकर दो-तीन सीढ़ियाँ चढ़कर मैं बरामदे पर खड़ा हो गया। सामने एक छोटा-सा कमरा खुला था, जहाँ तीन-चार आदमी एक मेज पर बिछे हुए शतरंज के फड़ को घेरकर ध्यानमग्न भाव से बैठे हुए थे। मैंने बरामदे से ही हाँक लगाई–“क्या विख्यात उपन्यासकार शरत् बाबू इसी मकान में रहते हैं?”
एक अधेड़ सज्जन जिनके सिर के प्राय: आधे बाल पक चुके थे, दाढ़ी-मूँछ साफ थी, केवल चेहरे पर सफेद बालों की खूँटियाँ यत्र-तत्र दिखाई देती थीं, और जो बंडी और धोती पहने शतरंज के खेल में बड़ी दिलचस्पी ले रहे थे, सिर उठाकर बोले–“जी हाँ। कहिए आप कैसे आए हैं? आइए, बैठिए।”
मैंने ससंकोच भीतर प्रवेश करते हुए कहा–“मेरा उन्हीं से कुछ काम है।”
“बैठिए। मैं ही शरतचंद्र हूँ। कहिए।”
“विख्यात उपन्यासकार शरतचंद्र?” यह प्रश्न स्वयं मुझे अशोभन लगा, पर चूँकि एक बार धोखा खा चुका था, इसलिए यह पूछना आवश्यक था।
वह बड़ी शालीनता से मुस्कुराए। फिर बोले–“हाँ, एक प्रकार विख्यात ही हूँ।”
मैं सहम गया। कुछ घबराए हुए तरीके से मैंने सीधा-सादा नमस्कार किया और बैठने के लिए कोई कुर्सी खोजने लगा। पर इस छोटे-से कमरे में कहीं कोई खाली कुर्सी नहीं थी, एक सज्जन उठ खड़े हुए और बोले–“बैठिए?”
थोड़ी-सी तकलुफ़्फ़ के बाद मैं बैठ गया। बैठते ही मैंने कहा–“आपसे मैं बहुत-सी बातें पूछना चाहता था।” इस छोटे से कमरे में उपस्थित सज्जनों के बीच में मुझे उत्साह नहीं हो रहा था।
“तो चलिए मेरे मकान में। पास ही है।” तो वह भी उनका मकान नहीं था!
वह उठे और मैं उनका अनुसरण करता चला, पास ही एक मकान के भीतर हम लोगों ने प्रवेश किया। एक कुत्ता, जिसकी सूरत बहुत भयावनी थी, और जो किसी अच्छी जात का नहीं, बल्कि आवारा-सा दिखाई देता था, मुझे देखते ही विकट स्वर में भूँकने लगा। “भेलू! भेलू!” कहकर शरतचंद्र ने प्रेमपूर्वक उसे डाँटा। मैंने भी पुचकार के साथ सीटी बजाई, तब वह मुझे चाटने लगा।
जिस कमरे में हम लोगों ने प्रवेश किया वह काफी बड़ा था, पर कुछ सजा हुआ नहीं था और फर्निचर भी वहाँ बहुत साधारण था। कुछ कुर्सियाँ, बेंच, एक कुछ बड़ी-सी और एक छोटी-सी मेज। दीवार से सटाए हुए कुछ ‘रैक’ थे, जिनमें पुस्तकें सजाकर रखी गई थीं। पर कमरा एकांत था और मुझे इस समय इसी बात की आवश्यकता थी। अपने इतने दिनों के स्वप्नाकांक्षित जन से बड़े झंझटों के बाद भेंट हो पाई थी, इसलिए कुछ क्षण उनके साथ मैं एकांत में बिताना चाहता था!
एक नौकर ताजा हुक्का भरकर रख गया। हम दोनों इत्मीनान से एक दूसरे के आमने-सामने बैठ गए। शरतचंद्र ने बड़े आराम से हुक्का गुड़गुड़ाते हुए बड़े प्रेम से कहा–“अब कहिए।”
मैंने उन्हें विस्तार से बताया कि मैं अबंगाली होते हुए भी बचपन से ही बंगला साहित्य में दिलचस्पी लेता आया हूँ और उनकी तब तक प्रकाशित प्राय: सभी रचनाएँ बड़े चाव से मैंने पढ़ी हैं। उन्हें पढ़ने पर कुछ प्रश्न मेरे मन में उठे हैं, उन्हीं के संबंध में मैं बातें करना चाहता हूँ।
तब तक हम लोगों के बीच बंगला में ही बातें हो रही थीं। बंगला भाषा का ज्ञान तो मुझे पहले से ही था, कलकत्ते में रहने पर मैंने अपने बंगला उच्चारण को भी काफी दुरुस्त कर लिया था, जो अब अभ्यास न रहने से फिर गड़बड़ा गया है। उन दिनों पोशाक पहनावा भी मेरा बंगालियों का-सा ही था। इसलिए संभवत: शरतचंद्र के मन में तब तक मेरे अबंगाली होने का संदेह नहीं उत्पन्न हुआ था। मेरे बताने पर, कि मेरी मातृभाषा हिंदी है, उन्होंने स्वयं भी शुद्ध हिंदी में बोलना आरंभ कर दिया। कहने लगे–“मैंने हाई स्कूल में हिंदी ही पढ़ी थी और हिंदी मैं बहुत अच्छी बोल लेता हूँ।” सचमुच उनके हिंदी उच्चारण से यह नहीं लगता कि कोई बंगाली बोल रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि वह कलकत्ते में किसी एक ऑफिस में अँग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करने का काम भी कर चुके हैं!
मुझे यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई। उसके बाद हम दोनों कभी हिंदी में और कभी बंगला में बातें करने लगे। मैं तब तक स्थिर चित्त हो चुका था और उनके साथ घर के-से वातावरण का अनुभव करने लगा था।
मैंने पूछा–“आपने अपनी बहुत सी रचनाओं में वेश्याओं और तथाकथित असती नारियों को जो नायिकाओं के रूप में चुना है, इसका कारण क्या आपकी व्यक्तिगत रुचि है या किसी विशेष आदर्शात्मक उद्देश्य से प्रेरित होकर, केवल अपने सैद्धांतिक पक्ष के समर्थन के लिए आपने ऐसे चरित्रों की अवधारणा की है?”
‘व्यक्तिगत रुचि’ वाला प्रश्न बड़ा रूढ़ था, यह मैं मानता हूँ। पर मैं एक तो तब तक उनके स्वभाव की बेतकलुफ़्फ़ी से परिचित हो चुका था, दूसरे जिस विशेष प्रश्न पर मैंने अपने ढंग से बहुत दिनों तक सोचा था उस पर लेखक का मत स्वयं उसी के मुख से जानने के लिए मैं अत्यंत उत्सुक था। इसलिए रूढ़ समझे जाने का खतरा उठाकर भी मैं पूछ ही बैठा!
“दोनों बातें हैं”, सहज भाव से उन्होंने कहा–“मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसे चरित्रों के घनिष्ट संपर्क में आया हूँ। और इसी कारण मुझे अत्यंत तीव्र रूप से यह अनुभव हुआ है कि वेश्याएँ समाज की सबसे अधिक शोषित, सबसे अधिक अत्याचार पीड़ित नारियाँ हैं। आर्थिक विवशता से वे जिस प्रकार का गंदा और घृणित जीवन बिताती हैं उससे उबरने के लिए वे जानकर या अनजान में सब समय छटपटाती रहती हैं। उनका वह छटपटाना देखने का सुयोग सबको सब समय नहीं मिलता पर जब कभी किसी को किसी कारण से वह सुयोग मिल जाता है, तब वह उसे जीवन पर नहीं भूल सकता। उनके अंतर के उस मूक विद्रोह को वाणी देने का निश्चय मैं बहुत पहले कर चुका था और अपने उस ‘मिशन’ को कार्यान्वित करने में मैंने कोई बात उठा नहीं रखी है।”
रवींद्रनाथ ने एक बार अपने एक लेख में शरतचंद्र पर परोक्ष रूप से छींटे कसते हुए लिखा था कि कला विशुद्ध आनंदमूलक सौंदर्य से संबंध रखती है; उसका निवास चीतपुर की गंदी गलियों में नहीं, बल्कि वाणी के अकलुष मंदिर में है। मैंने शरतचंद्र के आगे उसका उल्लेख करते हुए पूछा कि उस संबंध में उनकी क्या राय है।
उन्होंने कहा–“उस लेख में किसी अज्ञात कारण से रवींद्रनाथ उलझ गए हैं; नहीं तो उनके समान महान द्रष्टा कला के क्षेत्र और उद्देश्य की व्यापकता के संबंध में अपरिचित हो, ऐसा मैं नहीं मानता। इस लेख में उन्होंने स्वयं अपनी पिछली बातों का खंडन किया है। वह आनंद-मूलक सौंदर्य के कवि रहे हैं और हैं, इसमें संदेह नहीं, पर साथ ही दु:ख-दैन्य अभाव-शोषण और अत्याचार से पीड़ित जीवन के कठोर वास्तविक पहलू की उपेक्षा उन्होंने कभी नहीं की है। जिस कवि ने अपनी एक कविता में वेश्याओं और दूसरी पतिता रमणियों को सती-शिरोमणि माना हो और अपनी ‘पतित’* शीर्षक कविता में एक वेश्या के अंतर में निहित देवत्व को अत्यंत मार्मिक सुंदरता से प्रस्फुटित किया हो, वह आज यह कहे कि चीतपुर की गंदी गलियों से कला का कोई संबंध नहीं है, इसमे स्वभावत: यह संदेह होता है कि उनके इस लेख के पीछे कोई रहस्यमय कारण छिपा है! वह कारण व्यक्तिगत भी हो सकता है।”
मैं पूछना चाहता था कि “व्यक्तिगत किस रूप में?” पर कहीं पहले ही दिन की मुलाकात में कोई अप्रिय प्रसंग न चल जाए इस आशंका से मैं चुप लगा गया।
मैंने पूछा–“भारतीय नारी के सतीत्व के आदर्श के संबंध में आपके क्या विचार हैं?”
उन्होंने जो उत्तर दिया था उसका भाव इस प्रकार है–“मैं मानव-धर्म को सतीधर्म के बहुत ऊपर स्थान देता हूँ, सतीत्व और नारीत्व ये दोनों आदर्श समान नहीं हैं। नारी-हृदय की मंगलमई करुणा उसकी जन्मजात मातृवेदना उसके सतीत्व से कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण है। बहुत सी स्त्रियाँ मैंने ऐसी देखी हैं जिनका किसी दूसरे पुरुष से कभी किसी प्रकार का शारीरिक या मानसिक संबंध नहीं रहा है, तथापि उनके स्वभाव में अत्यंत नीचता, घोर संकीर्णता, विद्वेष भावना और चौरवृत्ति पाई गई है। इसके विपरीत ऐसी पतिताओं से मेरा परिचय रहा है जिनके भीतर मैंने मातृ-हृदय की नि:स्वार्थ ममता और करुणा का अथाह सागर उमड़ा हुआ पाया है।”
मैंने फिर प्रश्न किया–“यदि यही बात है, तो आपने श्रीकांत में अन्नदा दीदी के सतीत्व की महिमा ऐसे जोरदार शब्दों में क्यों वर्णित की है कि उसके दीप्त प्रकाश के आगे आपके दूसरे नारी-चरित्र म्लान पड़ जाते हैं?”
इस बात पर शरतचंद्र मंद-मंद मुस्कुराए और बोले–“आपकी यह बात मैं मानता हूँ! अन्नदा दीदी के प्रति वास्तव में मेरी भी आंतरिक श्रद्धा रही है। मेरे जन्मगत संस्कार आखिर भारतीय ही हैं। फिर भी मैं इतना बता देना चाहता हूँ कि उसके एकनिष्ठ पतिव्रता धर्म ने मेरी श्रद्धा उतनी नहीं उभारी है, जितनी उसकी प्रेम प्लावित आत्मा के मुक्त प्रवाह ने।”
सहसा मैं चंचल बाल-प्रवृत्ति से प्रेरित होकर एक दुस्साहसिकतापूर्ण प्रश्न कर बैठा। मैंने पूछा–“क्या श्रीकांत के माध्यम से आपने स्वयं अपना ही चरित वर्णित नहीं किया है?”
हुक्के की सटक मुँह से निकालकर शरतचंद्र ने कहा–“यही प्रश्न मुझसे और भी बहुत से लोग कर चुके हैं। पर वास्तव में लोगों की यह धारणा गलत है। यह ठीक है कि ‘श्रीकांत’ में जीवन के उन्हीं रूपों का वर्णन मैंने किया है। जिनसे मेरा व्यक्तिगत परिचय है और उन्हीं चरित्रों को मैंने लिया है जिनका अध्ययन निकट से करने का अवसर मुझे मिला है। पर इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि वह मेरा आत्मचरित है। फिर भी मुझे लोगों की यह धारणा जानकर प्रसन्नता ही होती है क्योंकि उससे यह प्रमाणित होता है कि मेरे पात्र पाठकों को सजीव लगते हैं और मेरा जीवन वर्णन और चरित्रांकन यथार्थ जीवन के बहुत निकट है।”
इतने में नौकर दो प्याले चाय दे गया, जिसके लिए शरतचंद्र पहले ही आर्डर दे चुके थे। एक घूँट पीकर मैंने पूछा–“क्या आपका यह मत है कि औपन्यासिक यथार्थ जीवन के यथार्थ का अविकल प्रतिबिंब होना चाहिए?”
“नहीं। मैं ऐसा नहीं मानता। जो अति-यथार्थवादी लेखक उपन्यास या कहानी को वास्तविक जीवन के अविकल फोटो के रूप में प्रस्तुत करने को बहुत बड़ी कला मानते हैं, मेरा उनसे मतभेद है। वह तो वैसे ही कला हो गई जिस तरह फोटोग्राफी भी एक कला है। तब फोटोग्राफर में और जीवन के द्रष्टा में अंतर ही क्या रह गया! यह ठीक है कि जीवन के सच्चे रूप को चित्रित करना प्रत्येक श्रेष्ठ कलाकार का कर्तव्य है पर नग्नता को केवल नग्नता के लिए प्रदर्शित करने तक ही कलाकार का कर्तव्य समाप्त नहीं हो जाता। नग्नता से रूढ़िपंथी सुधारवादियों की तरह कतराना कायरता है, यह मैं मानता हूँ, इसलिए सच्चा कलाकार जीवन की नग्नता का सही-सही आभास देने के उद्देश्य से रूढ़ यथार्थ को एक कारीगर की तरह तराश-तराश कर कलात्मक रूप में पाठकों के आगे रखता है और इस पर आदर्श की रंगीनी चढ़ाकर एक अभिनव समन्वयात्मक कला-कृति प्रस्तुत करता है।”
इस पर मैंने रूसी कलाकारों की प्रशंसा की। उन दिनों मैं चेखोव से विशेष प्रभावित था। मैंने कहा कि ऐसा सच्चा कलाकार मैंने अभी तक कोई दूसरा नहीं पाया। चेखोव के कथा-चित्र के सीधे जीवन से लिए गए हैं। मध्यवर्गीय और निम्न-मध्यवर्गीय जीवन की विपन्नता और विकृतियों का ऐसा सच्चा और मार्मिक चित्रण अन्यत्र नहीं पाया जाता। चेखोव ने अपनी कहानियों में कहीं भी अपने आदर्शमूलक विचारों को ठूँसने का प्रयत्न नहीं किया है और न किसी नीति पर पहुँचने का ही। किंतु उसने अपने चित्रों को जिस प्रकार के रंगों में रंगा है, वे ऐसे सच्चे हैं कि अपने आदर्शों को अपने साथ ठीक उसी प्रकार वहन करते हुए चले जाते हैं–जिस प्रकार तिल तेल को, मधु मिठास को और कुसुम गंध को।
शरतचंद्र ने मेरी बात का समर्थन किया, पर साथ ही कहा–“भारतीय सत्य का आदर्श कुछ दूसरा ही है। निरर्थक सत्य को हमारे यहाँ कभी महत्त्व नहीं दिया गया। हमारे यहाँ कला में कल्याण और मंगल की भावना को सदा प्रमुख स्थान दिया गया है, इसलिए जिस कलात्मक सत्य की पृष्ठभूमि में वह भावना न हो उसके प्रति कभी मेरे मन में आदर का भाव नहीं रहा है। मैंने कला को कभी क्रीड़ा-कौतुक के रूप में नहीं देखा है, मैं उसे मनुष्य के जीवन की चरम साधना के रूप में मानता हूँ।”
इसके बाद कुछ क्षणों तक हम लोग चुप रहे। शरतचंद्र लंबी कशें खींचते हुए हुक्का गुड़गुड़ाते चले गए। वातावरण काफी गंभीर बन गया था। वास्तव में मैं इतने गंभीर विषयों–कला संबंधी निगूढ़ तत्त्वों–की आलोचना के उद्देश्य से उनके पास नहीं गया था।
कुछ खाँसकर विषय को बदलने और वातावरण को हल्का करने के उद्देश्य से मैंने पूछा–“आपने सबसे पहले अपनी किस रचना से ख्याति पाई?”
“सबसे पहले मेरी ‘रामेर सुमति’ शीर्षक कहानी ‘यमुना’ नाम की एक अत्यंत साधारण पत्रिका में छपी। वह नई निकली थी और तब उसके केवल पचास ग्राहक थे। मेरी कहानी लोगों को इतनी पसंद आई कि दूसरे ही महीने उसके पाँच सौ ग्राहक हो गए।”
शरतचंद्र ने परिहास के स्वर में कहा–“इस प्रकार बायरन की तरह एक विशेष रात में सोकर जब उठा तब अपने को मैंने प्रसिद्ध हुआ पाया!”
और उसके बाद उनका कुछ ऐसा ‘मूड’ जगा कि मेरे बिना कुछ पूछे ही अपने उपन्यासकार के जीवन से संबंधित घटनाओं को एक-एक करके बताते चले गए। उन्होंने बताया कि छोटी उम्र से ही जब वह भागलपुर में पढ़ते थे, तभी से वह कहानियाँ और उपन्यास लिखने लगे थे। पर कभी अपनी कोई रचना उन्होंने छपाई नहीं–उन्हें छपाने से कोई लाभ होगा ऐसा विश्वास उन्हें नहीं था। जनता उन्हें ठीक रूप में ग्रहण करेगी या नहीं, इस संबंध में वह काफी संदिग्ध थे, इसलिए वर्षों तक उनकी वे रचनाए अप्रकाशित पड़ी रहीं। बाद में जब वह एक ‘आवारा’ की हैसियत से बर्मा गए तो वहाँ भी वह कुछ-न-कुछ लिखते चले गए, पर कभी किसी प्रकाशक से कोई बातचीत उन्होंने नहीं चलाई। अंत में एक दिन मकान में आग लग जाने से उनकी अधिकांश अप्रकाशित रचनाएँ जलकर नष्ट हो गई, जो दो-एक रचनाएँ नष्ट होने से बच गई, उनमें ‘देवदास’ भी एक था। बर्मा में ही उन्होंने अपना विख्यात उपन्यास ‘चरित्रहीन’ लिखना आरंभ कर दिया था! अपने एक विशेष मित्र के अत्यधिक आग्रह से उन्होंने उसे ‘भारतवर्ष’ नाम की प्रसिद्ध मासिक पत्रिका में धारावाहिक रूप से प्रकाशनार्थ भेज दिया। पर उसे ‘अनीति-मूलक’ समझकर ‘भारतवर्ष’ के तत्कालीन संपादक ने उसे न छापा। बाद में ‘चरित्रहीन’ भी ‘यमुना’ में ही धारावाहिक रूप से छपने लगा।
बर्मा में दीर्घ प्रवास के बाद जब अपने ऑफिस के साहब से झगड़कर नौकरी छोड़ वह कलकत्ते चले आए तब ‘भारतवर्ष’ से उन्हें 100 रु. मासिक का ‘ऑफर’ मिला–सहकारी के रूप में काम करने के लिए। उन्होंने मुझे बताया कि वह बहुत प्रसन्न हो गए, क्योंकि 100 में वह अपनी गुजर मजे में कर लेते थे और उससे अधिक कोई आकांक्षा तब उन्हें नहीं थी। उसके बाद ‘भारतवर्ष’ के प्रकाशक ने ही उनकी दो पुस्तकें–‘बिंदुर छेले’ और ‘विराज बऊ’ छापीं। दोनों का स्वत्वाधिकार एक प्रकार से प्रकाशक के ही अधीन था। शरतचंद्र ने बताया कि जब उन पुस्तकों की बिक्री बहुत अच्छी हुई तब उन्होंने कुछ मित्रों के सुझाव से अपनी नई पुस्तकों को स्वयं अपने ही खर्चे से छपाना शुरू कर दिया। बेचने का अधिकार अपने पूर्व प्रकाशक को ही कमीशन के आधार पर दे दिया। इस प्रकार उन्हें बहुत लाभ होने लगा। जब मैं उनसे पहली बार (1922 में) मिला था तब उन्हें प्राय: 6,000 रु. साल अपनी तब तक की स्वयं प्रकाशित पुस्तकों से मिलने लगा था। उस समय के भारतीय लेखकों की दशा को ध्यान में रखते हुए यह बहुत अच्छी रकम थी। शरतचंद्र ने मुझसे कहा कि तब उनकी समझ ही में नहीं आता था कि उतने ‘अधिक रुपयों’ से वह क्या करें? वह बराबर ‘आवारा’ जीवन बिताने के आदी थे–नौकरी करके सौ पचास रुपया माहवार कमाकर, उतने से ही गुजर करके वह प्रसन्न रहते थे। अब ‘इतना अधिक’ रुपया कमाने पर उन्हें पूरा संसारी बनना पड़ा। वैसे कुछ वर्ष पूर्व वह कलकत्ता आकर जमने के पहले बर्मा में ही विवाह कर चुके थे, इसलिए उन्हें अब बाकायदा ‘संसारी’ (बंगला में जिसका अर्थ गृहस्थ होता है ) बनना आवश्यक भी था। मेरा ख्याल था कि वह अविवाहित हैं। यह धारणा मेरे मन में क्यों बन गई, मैं कह नहीं सकता। उनके उपन्यासों के ढर्रे में कोई बात ऐसी अवश्य थी जिससे लगता था कि उनका लेखक कभी विवाहित जीवन के बंधन में नहीं बंधना चाहेगा। मैंने दूसरी बार मिलने पर शरतचंद्र के आगे अपनी इस लड़कपन की धारणा को प्रश्न के रूप में प्रकट कर ही दिया। वह स्नेहपूर्वक मुस्कुराते हुए बोले–“तुम्हारी यह धारणा ठीक ही उतरती, पर एक चक्कर ऐसा आया कि मैं वैवाहिक बंधन में बंध ही गया।” दूसरी बार से ही वह मुझे स्नेहवश ‘तुम’ कह कर संबोधित करने लगे थे। वह क्या चक्कर था, उस समय मैंने नहीं पूछा।
जो भी हो, 6,000 रु. साल पाकर वह आर्थिक दृष्टि से अपने को बहुत स्वच्छंद मानने लगे। उसके बाद–शरतचंद्र ने बताया–एक दिन ‘वसुमति’ वाले उनके पास आए और उन्होंने उनके आगे यह प्रस्ताव रखा कि वे उनकी सभी पुस्तकों का सस्ता संस्करण चार-पाँच ग्रंथावलियों के रूप में निकालना चाहते हैं और उन सबके लिए वे उन्हें सालाना 8,000 रु. देंगे। इस प्रस्ताव से मैं बड़े असमंजस में पड़ गया, शरतचंद्र ने मुझसे कहा, “क्योंकि यह तो मुझे बिल्कुल स्पष्ट लगा कि मेरी पुस्तकों का सस्ता संस्करण छप जाने पर फिर उन पुस्तकों की बिक्री न हो सकेगी जिन्हें मैं स्वयं छापता था, और जिनसे मुझे 6,000 रु. सालाना आमदनी होती थी, पर चूँकि वसुमतिवाले 2,000 रु. अधिक दे रहे थे, इसलिए कुछ सोच-विचार के बाद राजी हो गया। पर मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब साल के अंत में मैंने देखा, मेरे अपने प्रकाशन से 6,000 रु. में एक कौड़ी की भी कमी नहीं हुई और उधर से 8,000 रु. और मिलने लगा! इस प्रकार अब मुझे साल में 14,000 रु. की आमदनी होती है! अब मेरे पास बहुत रुपया हो गया है! और यह ‘बहुत’ भी इस हालत में जब वह बैंक जिसमें मेरे रुपये जमा थे (एलाइंस बैंक ऑफ शिमला लिमिटेड) फेल हो गया है और करीब 50 प्रतिशत रुपया ही अब जमा करने वालों को मिला है!” (वह 50 प्रतिशत भी इसलिए दिया गया था कि उसमें जमा करनेवालों में अँग्रेजों की संख्या बहुत अधिक थी और सरकार ने बैंक की सहायता की थी।) मैं तब यद्यपि लड़का ही था, और जीवन में आर्थिक पहलू के महत्त्व से परिचित नहीं था, तथापि शरतचंद्र के भोलेपन पर मुग्ध होने के साथ ही मुझे हँसी भी आई और रुलाई भी। क्योंकि इतना तो मुझ जैसा अनुभवहीन व्यक्ति भी जानता था कि कलकत्ता शहर में ही बहुत से ऐसे ‘निरक्षर भट्टाचार्य’ पड़े हुए हैं जो एक ही दिन में 14,000 रु. से अधिक कमा लेते हैं और तब भी संतुष्ट नहीं रहते, जबकि इतना बड़ा ‘मनीषी’ 14,000 रु. साल पाकर उसे ‘बहुत अधिक’ मानता है। पाश्चात्य देशों के लेखकों की आय से भी मैं पुस्तकों और सामयिक पत्रों के जरिए थोड़ा-बहुत परिचय था। अपने उपास्य लेखक के प्रति श्रद्धा और देश की दयनीय आर्थिक और सांस्कृतिक दशा के ख्याल से मेरे भीतर ही भीतर आँसू उमड़ उठे, और संभवत: बाहर आँखों में भी चमकने लगे। तब मैं बहुत अधिक भावुक था।
पहले ही परिचय से मेरे समान एक अदने लड़के को शरतचंद्र ने अपने व्यक्तिगत जीवन की इतनी अधिक बातें ऐसे प्रेम से बताई जैसे मेरा बरसों से उनसे परिचय हो और मैं उनका समवयस्क भी होऊँ। मेरे साहित्य-संबंधी प्रत्येक प्रश्न का उत्तर भी उन्होंने ऐसी गंभीरता से दिया कि मुझे यह अनुभव भी नहीं होने दिया कि मैं एक नासमझ छोकरा हूँ। दो घंटे से भी अधिक तक मैं उनका मूल्यवान समय नष्ट करता हुआ बैठा रहा, और जब उठने लगा तब भी उन्होंने कहा–“कुछ देर और बैठिए, एक प्याला चाय और पीजिए!” उनकी उदारता के बोझ से मैं इतना अधिक दब चुका था कि बैठने की इच्छा होने पर भी मैं उठ खड़ा हुआ और हाथ जोड़कर क्षमा माँगता हुआ जाने लगा।
“फिर कभी मिलिएगा!” बड़ी ही मीठी वाणी में उन्होंने कहा।
“अवश्य, मैं अपनी ही गरज से आऊँगा” कहकर मैंने हाथ जोड़े और लौटते हुए मन के भीतर ही उस मनीषी को परिपूर्ण श्रद्धा से प्रणाम किया जिसके सहृदय स्वभाव की सरलता पर मैं अपना सब कुछ (हालाँकि तब मैं भीतर और बाहर दोनों तरफ से अकिंचन था ) वारने को तैयार था।
* उस कविता की कुछ पंक्तियों का अनुवाद यहाँ दिया जाता है–“सती लोक में न जाने कितनी ऐसी पतिव्रताएँ वास करती हैं, जिनकी कथाएँ पुराणों में उज्ज्वल रूप में वर्तमान हैं । उनके अतिरिक्त और भी लाखों अज्ञात-नारी, ख्यातिहीना, कीर्तिहीना सतियाँ रही हैं । उन्हीं सतियों के बीच में पतिता रमणियाँ भी विराज रही हैं, जो मर्त्य में कलंकिनी हैं, पर स्वर्ग में सती शिरोमणि मानी जाती हैं । उन्हें देखकर सतीत्व के गर्व से गर्विणी स्त्रियाँ लज्जा से सिर झुका लेती हैं । उनकी वार्ता तुम क्या समझोगे ? केवल अंतर्यामी ही उनके सतीत्व की गाथा से परिचित हैं ।”
Image: Still life. Vase with flowers on the window
Image Source: WikiArt
Artist: Paul Gauguin
Image in Public Domain
