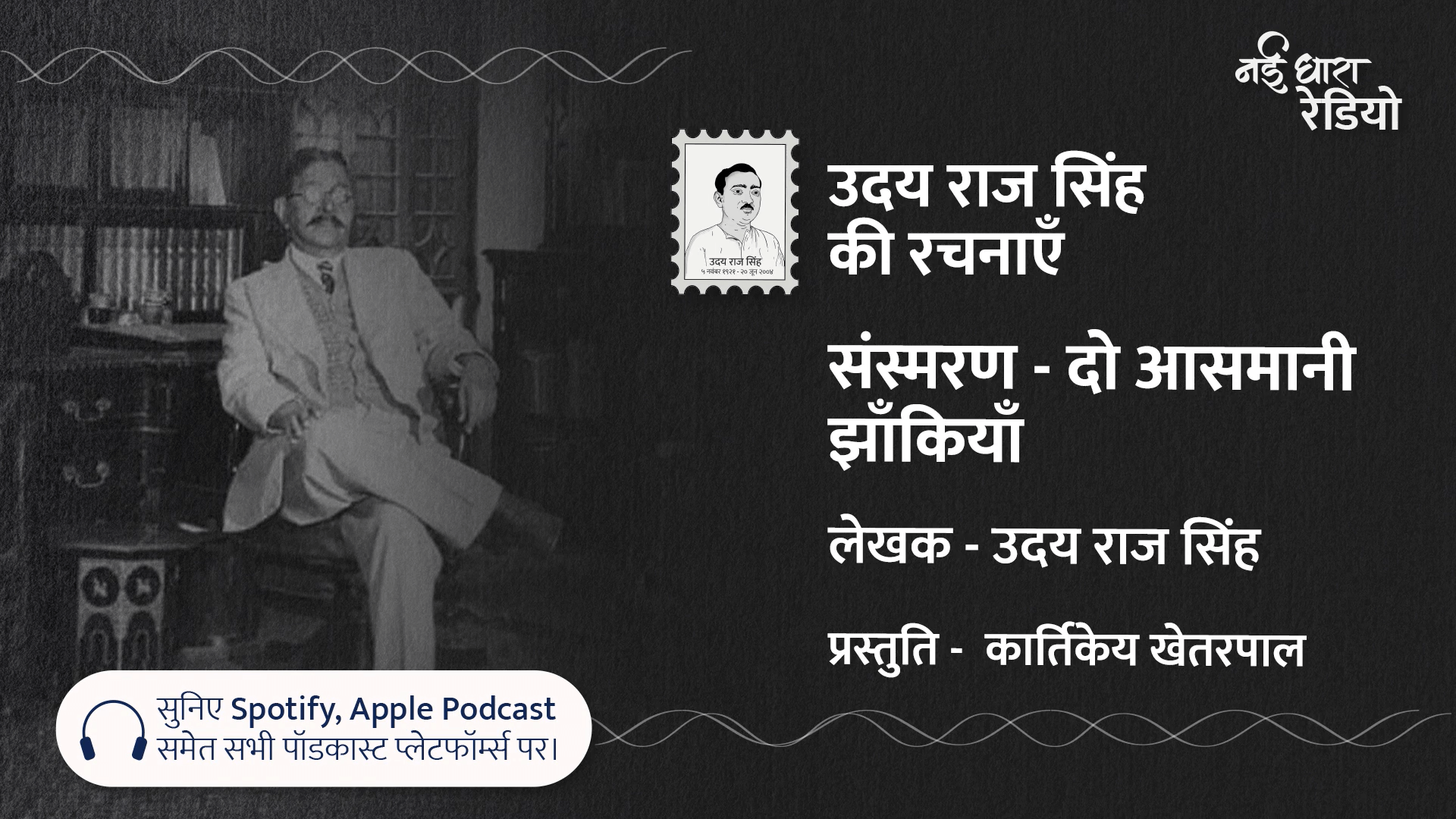वह विस्मयकारी व्यक्तित्व!
- 1 January, 1979
शेयर करे close
शेयर करे close

शेयर करे close
- 1 January, 1979
वह विस्मयकारी व्यक्तित्व!
‘एडवानटेज इन’–चिल्लाते हुए मास्टर साहब ने जोर से कहा–“देखिए, ध्यान से खेलिए, गेम हमारा होकर रहेगा।” मैंने बल्ला सँभालते हुए कसकर बॉल को बेस लाइन पर गिराया, कोई उसे लौटा न सका और गेम हमारा होकर रहा।
“देखिए, वन ऑल से सँभालते-सँभालते एक सेट तो आपको जिता दिया। अब मैं थक गया हूँ। दूसरा सेट आपको खेलना है–ठीक से खेलिए।”
मास्टर साहब का आदेश सर-आँखों पर, मगर ये निगोड़ी आँखें मानें तब तो! जब-न-तब टेनिस कोर्ट से उचककर दक्खिन के बरामदे में बैठे उस आगंतुक पर जा बैठतीं जो मेरे पिता की बगल में बैठे-बैठे उनकी वाणी का रसास्वादन कर रहा है। फिर कान भी उधर ही भाग जाते–“…यह भी बिहार का एक कोना है जहाँ बहार की आबोहवा नहीं,…छोटे-बड़े सभी अपने घरौंदे में धँसे पड़े हैं। भाव और भावनाओं की दुनिया अभाव की भूमि में हरी-भरी नहीं हो पाती…”
“देखिए, फिर आपका ध्यान बँटा। इस बार तो हमलोग जीतने से रहे…”
मैं तन्मय हो खेलने लगा मगर आँखों ने फिर मुझे नचाना शुरू किया और कानों का क्या कहना…फिर सुनिए–“मेरे ये अँजुरीभर श्रद्धा के दाने आपके दिल के पहलू तक पहुँच जाएँ, तो सच मानिए…” किसी-किसी तरह खेल समाप्त हुआ। गाँव की जाड़े की संध्या–झट अँधेरा छा गया। स्वेटर पहनकर जब मैं अपना बल्ला लिए टेनिस कोर्ट से बाहर आया तो देखा कि वह आगंतुक वहाँ से उठ चुका था और राधाबाबू के साथ उद्यानभवन के मुख्य द्वार की ओर बढ़ता चला जा रहा था। संध्या घनी हो चली थी। उसे मैं दूर तक नहीं देख सका। उसकी झीनी आकृति जाड़े की संध्या की धुंध में विलीन हो गई। मैं अवाक था कि पंडित जी ने हँसते हुए टोका–“किन्हें देख रहे हैं आप?”
“उन्हें ही जो अभी-अभी राधाबाबू के साथ बोर्डिंग हाउस की ओर बढ़े चले गए।”
“पहचाना आपने उन्हें?”
“नहीं तो।”
“वाह! वही न शिवपूजन बाबू हैं–‘देहाती दुनिया’ के लेखक–‘बालक’ के संपादक जिनका जिक्र मैं अकसर आपको पढ़ाने के समय करता रहा हूँ।”
“ओ…मैं तो उन्हें पहचान ही न सका। खद्दर के कपड़े में लैस मैं तो उन्हें कोई गाँधी टोपीवाला काँग्रेसी समझ बैठा था। आजकल काँग्रेसी मिनिस्टरी की धूम है–सोचा कोई काँग्रेसी…।”
पंडित जी हँस पड़े–“आपने भूल की।”
“हाँ, सचमुच मैंने भूल की। देखने में तो वह विशुद्ध कलाकर सरीखे ही दीखते रहे। ओठों पर लाल धारी, आँखों में एक अभिनव ज्योति, एक पंक्ति सुनते और फड़क उठते–हँस देते–खिलखिला पड़ते…।”
“आप शायद जानते नहीं–अगले हफ्ते आरा में बिहार-प्रांतीय हिंदी-साहित्य-सम्मेलन का अधिवेशन होने जा रहा है। राजासाहब स्वागताध्यक्ष हैं। शिवपूजन बाबू राजासाहब के अभिन्न मित्रों में हैं। इसलिए राजासाहब ने उन्हें पहले ही बुला लिया है अपना भाषण उन्हें सुनाने तथा उनकी राय लेकर कुछ रद्दोबदल करने के लिए। अभी-अभी राजासाहब अपना भाषण ही उन्हें सुना रहे थे।”
“ओ…अब समझा।”
यह स्मृति मुझे और भी पीछे खींचकर लिए चली गई जब शिवपूजन बाबू ने मेरी एक बालसुलभ रचना ‘बालक’ में पहली बार छापी थी और मुझे प्रोत्साहन का एक छोटा पत्र भी भेजा था।
“अभी आपसे-उनसे प्रणाम-पाती भी नहीं…”
“नहीं।”
“तो कल मैं आपको उनसे मिलाऊँगा।”
हाँ, यह घटना सन 1937 के दिसंबर की है–जब मैं सूर्यपुरा स्कूल का एक छात्र था। दूसरे दिन हमारे पूज्य शिक्षक राधाबाबू शिवपूजन बाबू को लेकर फिर हमारे बँगले पर आए। उन दिनों जब भी शिवपूजन बाबू सूर्यपुरा आते तो टाउन स्कूल आरा के अपने पुराने मित्र श्री राधा प्रसाद, जो अब हमारे स्कूल के उपप्रधानाध्यापक हो गए थे, के साथ छात्रावास में ही ठहरते। उस दिन राधाबाबू तथा हमारे पंडित जी जगदीश शुक्ल ने मेरा परिचय उनसे कराया। जिस आत्मीयता और स्नेह से शिवपूजन बाबू उस दिन मुझसे मिले वह स्नेह उनके जीवन के अंतिम दिनों तक उसी तरह बरकरार रहा। उसमें कभी भी कोई कमी नहीं आई। फिर यह कौन जानता था कि उस दिन का परिचय मेरे पिता के साहित्यिक मित्र शिवपूजन बाबू से ही केवल नहीं था, वरन मेरे सर्वस्व–मेरे आनेवाले कल के सबसे बड़े हितैषी, उद्धारक से भी था! भविष्य के गर्भ में फिर यह अनूठा रत्न मुझे कब और कैसे मिलेगा–कौन जाने! समय का प्रवाह अटूट है। उसकी गति को भला कौन रोक सकता है? सन सैंतीस से सन बयालीस–यह पाँच वर्ष का अर्सा यों आया और यों चला गया। स्कूल और कॉलेज के दिन–न आते देर, न जाते देर। इस अवधि में शिवपूजन बाबू से मेरा संपर्क बिलकुल छूट-सा गया था। उन दिनों मैं विज्ञान का विद्यार्थी था और साहित्य से भी नाता टूट चुका था। मगर मेरे पिता जी की लेखनी इन वर्षों में, काफी दिनों तक विश्राम कर सजग हो गई थी। ‘राम-रहीम’, ‘गाँधी टोपी’, ‘सावनी समाँ’, ‘पुरुष और नारी’ और ‘टूटा तारा’ का अवतरण इन्हीं वर्षों में होता रहा। मेरे पिताजी की पुस्तक जब कभी तैयार होती तो शिवपूजन बाबू सूर्यपुरा अवश्य आते और उसकी पांडुलिपि बनारस या पटना ले जाते और अपनी देख- रेख में उसकी छपाई कराते। छुट्टियों में जब कभी सूर्यपुरा आता तो वहाँ के लोगों से उनकी कहानी सुनता या उनसे कभी-कभी मिलने का सुअवसर भी मिल जाता। आज भी सूर्यपुरा में अनेक व्यक्ति हैं जो उन दिनों के उनके प्रवास की कहानी कहते नहीं अघाते। उनका स्वभाव ऐसा विनम्र, विनोदप्रिय था कि वे वहाँ जिनके-जिनके संपर्क में आए उन्हें अपना बना लिया। उनकी मृत्यु के उपरांत वहाँ के कई एक व्यक्ति ने मुझे उनके सूर्यपुरा-प्रवास की बड़ी मनोरंजक घटनाओं का जिक्र किया जिससे पता चलता है कि उनकी खुशमिजाजी तथा हरदिल अजीजी उनकी अपनी खसूसियत थी। मेरी अपनी अनुभूति है कि किसी के अंदर का साहित्यकार कभी मरता नहीं। प्रतिकूल परिस्थितियों में वह सोया जो रहे मगर अनुकूल परिस्थितियों में वह जाग ही पड़ता है और आप चाहे कलम से कितनी ही दूर भागना चाहें वह आपको भागने नहीं देगा–एक-न-एक दिन आपको कलम थमाकर ही दम लेगा। यही बात मेरे साथ भी घटी और विश्वविद्यालय की शिक्षा खत्म होते ही ‘अधूरी नारी’ का लिखना अनायास ही प्रारंभ हो गया। जाने कैसे यह बात शिवपूजन बाबू को मालूम हो गई। एक दिन आरा में उनसे भेंट हुई तो उन्होंने हँसते हुए कहा–“एक बड़ी खुशखबरी सुन रहा हूँ। आप भी कुछ लिखने…।”
“नहीं, यों ही…।”
“तो ऐसे ही न मन रमेगा!”
“मगर उसे प्रेस भेजने की हिम्मत नहीं होती। आप उसे एक बार देखकर आशीर्वाद दे देते…।”
“अवश्य–जब बुलाएँ मैं चला आऊँगा। अब ज्यादा बाहर निकलना नहीं होता–राजेंद्र कॉलेज की प्रोफेसरी जो लग गई है। हाँ, छुट्टियों में जब बुलाएँ…।”
उनका इतना प्रोत्साहन तो मेरे लिए एक अपूर्व वरदान था। अनायास ही जैसे भक्त को भगवान मिल गए। फिर शिवपूजन बाबू छुट्टियों में सूर्यपुरा आए और मेरे साथ तीन दिनों तक रहकर ‘अधूरी नारी’ की सारी पांडुलिपि पढ़ गए और मोतियों की तरह अपने लाल-लाल अक्षरों से उसे सजाकर उसमें चार चाँद लगा दिए। मेरे जैसे कितनों को वे अंधकार से प्रकाश में लाए–इसकी चर्चा अनेक की ज़ुबान पर है आज। उनके सान्निध्य के वे तीन दिन मेरे जीवन के अमिट दिन रहे। उन्हें बड़े समीप से देखा मैंने और वही पाया जो सबों ने उनके समीप जाकर पाया कि वे कितने महान रहे और हम कितने लघु; मगर उनकी महानता भी कैसी निराली कि उसका बोझ किसी पर पड़ने से रहा “He was of the crowd but above the crowd.” मेरे नौकर, निपट देहाती धेनुकी ने भी कहा–“महात्मा हवन। कभी कोई कामे न लेत रहन। हम करीं भी त हाथ पकड़ लेस–ना धेनुकी जी, रउआ रहे दिहीं।” और यही बात मैंने भी पाई। बड़ा ही सादा बिछावन, सादा कपड़ा, बिलकुल सादा खाना, कभी किसी वस्तु की फरमाइश न की, दिनभर और रातभर लालटेन की रोशनी में आँखें गड़ाकर पान खाते पांडुलिपि सँवारते चले जा रहे हैं–उस कुशल कुलांगना की तरह जो घर में आई नववधू को अपने हाथों सजा रही हो। यदि ललाट सूना लगता तो उसमें एक हल्की बिंदी उगाकर–पाटी में गुँथी हुई चंद लटों को खींचकर इस तरह लटका देती कि सभी उसे उसके सहज शृंगार का अंग ही मानने लगते। और यदि चेहरा सूना-सूना लगता तो चिबुक पर ऐसी काली बिंदी उगा देती कि ननदों की टोली में आग लग जाती। और हाँ, इतने पर ही उसे संतोष नहीं होता–नख से शिख तक जहाँ कहीं भी कोई कमी मालूम पड़ती उसे इस तरह दूर कर देती कि उसके पति को छोड़कर कोई उसे परख भी नहीं पाता। तो उनकी आँखों में, उनकी उँगलियों में वह करिश्मा था कि कोई क्या कहे, कैसे और कितना सुनाये!
सन बयालीस में विश्वविद्यालय की पढ़ाई समाप्त कर इस्टेट के कार्यों में बुरी तरह फँस गया। छोटे बाबू जी बहुत बीमार रहा करते थे इसलिए मेरे पिता जी सारे परिवार के साथ सूर्यपुरा से प्रायः बाहर ही रहा करते थे। पुराने मैनेजर भी अवकाश ग्रहण कर चुके थे। इसलिए इस्टेट की सारी जिम्मेवारी उन दिनों मेरे ही सर थी। इसी झमेले के चलते ‘अधूरी नारी’ लिखने के बाद कुछ आगे लिखा न जा सका। जिंदगी की दिशा बदल चुकी थी। सुना है सहस्त्राब्दियों बाद अहिल्या का उद्धार भगवान रामचंद्र के चरण-स्पर्श से त्रेतायुग में हुआ था मगर कलयुग में मेरा उद्धार शिवपूजन बाबू की कृपा से चार वर्षों में ही हो गया।
सन 1946 में पटना में मेरे निवास-स्थान पर शिवपूजन बाबू से एक दिन अचानक भेंट हो गई। बातें होने लगीं और उसी सिलसिले में वह बड़े खिन्न हो कहने लगे–“आपके पिता जी की सारी साहित्यिक निधि नष्ट हो रही है। ‘श्रीराजराजेश्वरी ग्रंथावली’ तथा ‘राम-रहीम’ का राजसंस्करण मैंने अपनी देख-रेख में लहेरियासराय में तैयार कराया, फिर लक्ष्मीनारायण प्रेस, बनारस तथा पूज्य प्रेमचंद जी के पुत्र श्री अमृतराय के सरस्वती प्रेस में ‘गाँधी टोपी’ तथा ‘सावनी समाँ’ की सुंदर नयनाभिराम छपाई करवाई। पटना से ‘टूटा तारा’ निकलवाया। मगर इन सारी पुस्तकों की प्रतियाँ तितर-बितर हो गईं–कहीं कुछ पता न चला। जो इन पुस्तकों के वितरक बने वही उन्हें पचा गए। इनकी छपाई-सजाई में इतने पैसे लगे मगर वे सब डूब गए। राजासाहब मुझ पर भरोसा किए किताबें छपवाते जाते हैं मगर उनसे न समाज का कल्याण होता है और न साहित्यकार का ही।” इतना कह वे मौन हो गए। चेहरे पर विषाद और ग्लानि की गहरी रेखाएँ दौड़ गईं। मैं उन्हें अवाक हो देखता रहा। कुछ देर बाद उन्होंने मौन भंग किया और बड़ी आत्मीयता से कहा–“आप किस चक्कर में पड़ गए? अँग्रेजी राज्य तो चला गया। काँग्रेसी राज्य में जमींदारी का उन्मूलन होकर रहेगा। आप अपनी जिंदगी इसमें क्यों खपा रहे हैं? राजासाहब की लेखनी इसी झंझट के चलते 15 वर्षों तक नजर-बंद न रहती तो आज वह कहाँ पहुँचे रहते राम जाने। आप ही पटना में एक प्रेस क्यों नहीं खोलते–राजासाहब की सभी पुस्तकें वहीं से प्रकाशित होतीं और उनका वितरण भी सुचारु रूप से होता। आपको भी पढ़ने-लिखने से शौक है–इस दुनिया से आपका संपर्क बढ़ेगा। राजासाहब की अमूल्य निधि भी सुरक्षित रहेगी और आपको जमींदारी-उन्मूलन भी पीछे नहीं खलेगा। इस्टेट का भार तो बहुत लोग सँभाल लेंगे मगर इस नए इस्टेट का भार सभी नहीं उठा सकते। यदि आप मन मजबूत करें तो मैं राजासाहब से एक ट्रेडिल, एक फ्लैट तथा आवश्यक टाइप खरीद देने के लिए सिफारिश करूँ।”
वह हँस पड़े और इस तरह मुझे देखने लगे जैसे मुझसे ‘हाँ’ कहलाने को तुले हों। मैं बड़े पशोपेश में पड़ा। इस प्रस्ताव की ओर मेरा कभी ध्यान ही नहीं गया था–बिलकुल अनोखा प्रस्ताव। “क्यों? क्या मेरी बात आपको जँची नहीं? या मैं यह मान लूँ कि ‘मौन स्वीकृति-लक्षणम्?’ उन्होंने फिर कहा।
“नहीं-नहीं, आपकी बात मुझे खूब जँची। मैं इस प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार करता हूँ। मगर इस दुनिया का मुझे कुछ अनुभव नहीं–भला कैसे-क्या…?”–मैंने बड़ी चिंता जताई। “आप बेफिक्र रहें। और मैं जो हूँ। सब रास्ता निकल आएगा।” शिवपूजन बाबू का यह आश्वासन–यह प्रोत्साहन एक ऐसा प्रेरक बन गया जिसने उस दिन मेरे जीवन की दिशा ही बदल दी। सन 46 के अंत तक अशोक प्रेस की मशीनें, टाइप इत्यादि इलाहाबाद से खरीद कर लाए गए। पटना में मकान भी ठीक हो गया। प्रेस में शिवपूजन बाबू प्रायः प्रतिदिन आते और उसे खड़ा करने में पूरी सहायता करते। लहेरियासराय के अपने पुराने सहयोगी हवलदार त्रिपाठी को उन्होंने प्रेस का व्यवस्थापक बना दिया।
15 जनवरी 1947 को प्रेस का उद्घाटन हुआ और तब से लेकर अपने जीवन के अंतिम दिनों तक अशोक प्रेस से उनका बड़ा ही घनिष्ठ संबंध रहा। उनके ऋण से न अशोक प्रेस कभी उऋण हो सकता है और न मैं। मासिक ‘हिमालय’ का प्रकाशन बंद होने के बाद बिहार में एक विशुद्ध साहित्यिक पत्रिका की कमी उन्हें बड़ी ही खल रही थी। अशोक प्रेस की स्थापना के उपरांत अकसर उनसे एक ऐसी मासिक पत्रिका निकालने की बात होती और वे उस योजना को कार्यान्वित करने पर पूरा जोर भी देते। मेरा यह बराबर अनुरोध रहता कि वे इस पत्रिका का संपादन करें। उन्होंने मेरी विनती मान ली और यह तय हुआ कि राजेंद्र कॉलेज, छपरा से ही वे संपादन का काम करेंगे हालाँकि वे पटना आकर रहने को भी तैयार थे।
पत्रिका निकालने की जब सारी व्यवस्था ठीक हो गई तो शिवपूजन बाबू को बिहार सरकार ने बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद का संचालक बना दिया और हमारी सारी योजना खटाई में पड़ गई। परंतु शिवपूजन बाबू हतोत्साह न हुए। उन्होंने पटना में हमारे निवास- स्थान पर दिनकर जी तथा बेनीपुरी जी को आमंत्रित किया और पिता जी के समक्ष यह तय हुआ कि बेनीपुरी जी अशोक प्रेस की पत्रिका का संपादन करेंगे और तब बेनीपुरी जी के कुशल संपादकत्व में ‘नई धारा’ निकल पड़ी। यह तो रही मेरी कहानी परंतु शिवपूजन बाबू के उपकार की कहानियाँ तो गिनाई नहीं जा सकतीं। वे तो अनगिनत हैं और आज हजारों-हजार की जबान से बोल रही हैं। महात्मा गाँधी के निधन पर प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइंस्टाइन ने कहा था कि आनेवाली पीढ़ी विश्वास न कर सकेगी कि गाँधी ऐसा भी कोई मानव इस धरती पर अवतरित हुआ था। मेरी ऐसी धारणा है कि कुछ दिनों बाद शिवपूजन बाबू के विषय में भी लोग ऐसा ही सोचेंगे–क्या सचमुच ऐसा संत साहित्यकार हिंदी- संसार में जन्मा था?
Image: Udaya Raj Sinha Archieve