अफ़सर का दु:ख
- 1 June, 2024
शेयर करे close
शेयर करे close
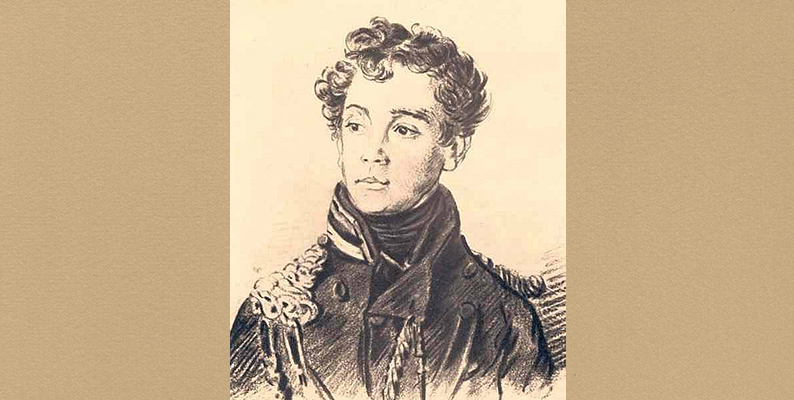
शेयर करे close
- 1 June, 2024
अफ़सर का दु:ख
माना कि अफ़सर बनते आदमी सुहागन हो जाता है लेकिन सुहागन बनना एक बात है, सौभाग्यवती होना बिलकुल अलग बात है। सुहाग सौभाग्य की गारंटी नहीं है। मैं यहाँ थोड़ी देर के लिए लिंग-भेद भूल गया हूँ। अफ़सर को लिंग, जाति, धर्म आदि के दायरे से बाहर रख कर देखा जाना चाहिए। अफ़सर की कोई जाति नहीं होती, वह केवल अफ़सर होता है–खालिस अफ़सर। यहाँ थोड़ी उदारता बरतने की अपील करता हूँ। यह भी कहने की कोई बात है कि सौभाग्यवती के सौ भाग्य होते हैं और सुहागन का दुर्भाग्य भी हो सकता है। कुछ अफ़सरों के साथ भी यही होता है। अव्वल तो अफ़सर को अफ़सर की तरह दिखना चाहिए। उसे और उसके शागिर्दों को भी हर समय उसकी अफ़सरी का एहसास होना चाहिए। वह अफ़सर ही कैसा जिसे देखकर मातहत उठ कर खड़े न हो जाएँ। यदि दस-पाँच आदमी प्रणाम सर नहीं कहे तो अफ़सर को खुद अपनी अफ़सरी की प्रामाणिकता पर संदेह होने लगता है। उसके कान खड़े हो जाते हैं। आँखें चौकन्ना हो जाती हैं। वह ऊपर से नीचे तक खुद को ही निहारना शुरू कर देता है। वह बहुत बारीकी से जाँच-पड़ताल में जुट जाता है कि कहाँ चूक हो रही है कि लोग उसे अफ़सर नहीं समझ रहे हैं। वह अपनी अफ़सरी साबित करने के लिए तमाम तरह के नुस्खे, दाँव-पेंच आजमाना शुरू कर देता है। बार–बार घंटी बजाकर मातहतों को बुलाना, डाँटना जैसे कुछ अचूक प्रयोग करता है। कुछ तो अपनी अफ़सरी सिद्ध करने के लिए अटेंडर के सामने खड़े होने के बावजूद घंटी बजाते रहते हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार एक अफ़सर ने तो इतनी घंटियाँ तोड़ीं कि भंडार वाले आपूर्ति करते-करते परेशान हो गए। इतना पर भी धौंस नहीं जमने पर ऐसा अफ़सर बड़े साहब का बात-बात पर हवाला देने जैसे ब्रह्मास्त्र का भी सहारा लेता है। काम में नुख्स निकालना तो उसके दिनचर्या का अनिवार्य हिस्सा होता है।
अफ़सरों की जाति भले ही एक हों, लेकिन उनकी प्रजातियाँ भिन्न-भिन्न होती हैं। एक दिन एक साहब अपने बेटे को नसीहत दे रहे थे कि अफ़सर के बेटे को अफ़सर के बेटे से ही दोस्ती करनी चाहिए। कुलीनता की सुरक्षा बहुत जरूरी है। अब बेटे की यह स्थिति है तो साहब की बीवी के स्टेटस का अंदाजा आप स्वयं लगा सकते हैं। यह तो बात हुई वैसे अफ़सरों की जिनके मातहत दो-चार लोग काम कर रहे हों। समय ऐसा है कि सारे अफ़सरों को ऐसा सौभाग्य कहाँ मिल पाता है। उन अफ़सरों की बदकिस्मती का क्या कहिए जो एकल हैं। अब वह किसके लिए शृंगार करें। लेकिन जो भी हो, हैं तो अफ़सर ही। शेर भूखा रहने पर घास चरेगा? एकल अफ़सर होने का एक लाभ यह है कि ऐसे अफ़सर को अपने बड़े अधिकारियों के सामने अकेला होने का विलाप करने की पूरी स्वतंत्रता मिल जाती है। वह अति उत्साह में अपनी कर्मठता का राग अलापते हुए स्वयं को वन मैन आर्मी घोषित कर सकता है। अतीत की अपनी उपलब्धियों को रिटायरमेंट के समय तक भुना सकता है। बड़े साहब के पास अपना दुखड़ा सुना सकता है। क्या हुआ जो उनके पास मातहत नहीं है, पास-पड़ोस में अपनी अफ़सरी की आभिजात्य खूशबू तो फैला सकता है। ऐसे कितने अफ़सरों को मैंने बहुत नजदीक से दूरी बनाते हुए देखी है। कारण यह कि अफ़सर के आगे और घोड़ा के पीछे कभी नहीं रहना चाहिए। अँग्रेज़ के जमाने की इस सीख का मर्म मैं बेहतर तरीके से समझता हूँ। यही कारण है कि अफ़सर क्या हर बड़े आदमी से उचित दूरी बनाए रखता हूँ। बड़ी गाड़ियों की धमक दूर से सुनाई देती है और उनके लिए रास्ता पहले ही खाली कर देता हूँ।
अफ़सरी का जादू-लोक इतना मायावी है कि इसको जानने के लिए सैद्धांतिक और प्रायोगिक कक्षाओं में प्रवेश लेना होगा। अब उतना तो किसी के पास धैर्य या समय नहीं है कि इन चीजों को समझे। अतः कलि-कल्याणकारी इस कथा को रससिक्त बनाने के लिए मैं प्यारेलाल जी जैसे अनुभवी अफ़सर को आमंत्रित करना आवश्यक समझता हूँ। उनकी किस्मत कुछ यूँ पलटी कि जैसे बिल्ली के भाग्य से सिकहड़ टूट गया हो। वर्षों तक कनीय बने रहे और लोग उनको देख कन्नी काटते रहे। अचानक चौथेपन में वरीय बन गए, मानो कनिया को वर मिल गया। साफ शब्दों में अफ़सर बन गए। परंतु उन्हें अफ़सरी वाली फीलिंग आती ही नहीं थी। अपने नोटिंग लिखते और अपने को ही फाइल बढ़ा देते। बाद में उन्हें याद आता कि अब तो वह अफ़सर हैं। यह दूसरी बात है कि उनका कोई चपरासी नहीं था। वह घंटी नहीं बजा सकते थे। कोई मातहत नहीं था कि उसे आदेश दे सकते थे। कभी फोटोकॉपी कराने के लिए दौड़ते दिखते तो कभी फाइल लेकर सरपट भागते। लोग उनकी दयनीयता देखते तो कहते कि स्टाफ क्यों नहीं माँग लेते? वे लगभग रुआँसा होकर बोलते–‘अब किसी से क्या कहना। छह महीने बचे हैं। जीवन भर कर्मचारी रहा। अब आखिरी समय में मुझसे अफ़सरी नहीं हो पाएगी। अफ़सरी और घुड़सवारी सबसे सधती भी नहीं। जिस तरह घोड़े की लगाम को ठीक से थामना पड़ता है, उसी तरह अफ़सरी को सँभालना पड़ता है। इस बुढ़ापे में घुड़सवारी कर हड्डी नहीं तोड़वानी है। ज़िंदगी भर कर्मचारी रहा, कर्म के बोझ तले दबा रहा। अब चलने के समय अफ़सर बनना रास नहीं आ रहा। चाचा गालिब ठीक ही कह गए हैं–आखिरी वक्त क्या खाक मुसल्म्माँ होंगे। जिस से कहो, सिस्टम की मजबूरी बतलाकर पल्ला झाड़ लेता है।’
ऐसे ही निराश मन से एक दिन चैंबर में लौट कर प्यारेलाल जी ने फुल पावर में फैन चला दिया। जाड़े के दिन में भी माथे पर चुहचुहाते पसीना को पोंछा कि अचानक उनकी अँगुली घंटी की तरफ चली गई। जल्दी ही वह सतर्क हो गए। मन को समझाया कि घंटी सुनने के लिए चपरासी तो है नहीं। धम्म से चक्करदार आराम कुर्सी में धँस कर पैरों का सहारा लेकर एक राउंड घूम गए। कुर्सी जब विरामावस्था में आ गई तो यह याद आया कि स्टाफ हो या नहीं हो, मीटिंग तो करानी पड़ेगी। चाबी लेकर आलमीरा खोला। फाइलों पर पड़ी धूल को झाड़ा। नोटिंग लिखा। पैंट की बेल्ट को टाइट कर सलीके से फाइल लेकर बड़े साहब के चैंबर की ओर इस तरह प्रस्थान किया मानो कोई सैनिक युद्ध के मोर्चे पर जा रहा हो। उस सायंकाल में मुझे अफ़सर का दु:ख किरानी के दु:ख से कहीं बड़ा लगा। अफ़सर अपना दु:ख अपनी पत्नी को नहीं बतला सकता। अचानक मैं सोचने लगा कि क्या कुछ अफ़सर समय के साथ इसीलिए गंभीर होते जाते हैं? मेरा ऐसा मानना है कि अफ़सर एक ऐसा नितांत अकेला प्राणी होता है जो अपना दु:ख पीते हुए नीला टाई लगाकर अपनी अफ़सरी को सार्वजनिक करता है। दुनिया की नजरों में जो अफ़सर है, उससे बेहतर अफ़सरी की हकीकत कोई नहीं जान सकता है। वैसे तो एक दिन सबकी अफ़सरी जानी है लेकिन अफ़सर होने के बावजूद यदि अफ़सरी वाली सुख-सुविधा न मिले तो किसे दु:ख नहीं होगा?
कथा लंबी है पर इस अध्याय का प्रसाद मैं सबसे पहले प्यारेलाल जी नामक दु:खी अफ़सर को समर्पित करना चाहूँगा। आशा है इस प्रसाद को ग्रहण करने के उपरांत शायद थोड़ा सा कम हो जाए। आप भी थोड़ा सा ग्रहण कर लें–साँप यदि विषरहित भी हो तो भी उसे फुफकारते रहना चाहिए वरना दुनिया के हाथों में अर्चना के पुष्प नहीं दंड है।